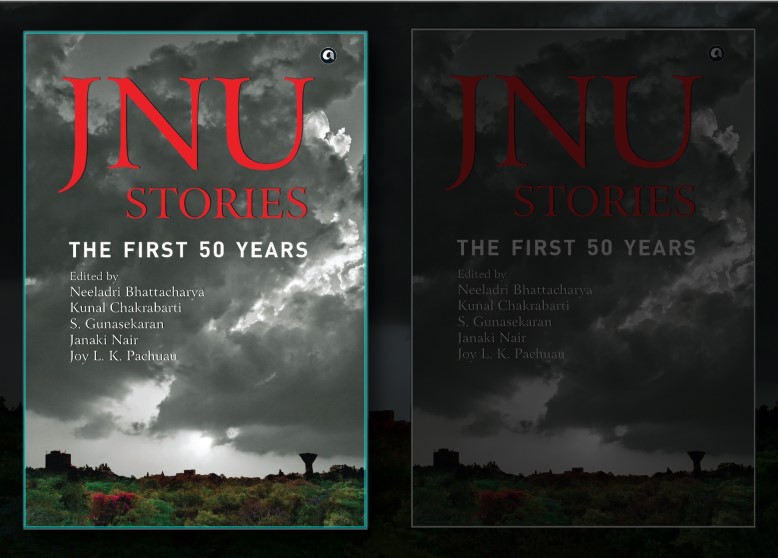पुस्तक समीक्षा: जेएनयू स्टोरीज़- द फर्स्ट फिफ्टी ईयर्स इस संस्थान से ताल्लुक़ रखने वाले कई लेखकों के लघु निबंधों का संग्रह है, जिसे पढ़ने पर साफ पता चलेगा कि विश्वविद्यालय भी सांस लेते जीवंत संस्थान हैं और उनका भी गला घोंटा जा सकता है.

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) की अर्ध-शताब्दी के अवसर पर प्रकाशित लघु-निबंध संग्रह, जेएनयू स्टोरीज़- द फर्स्ट फिफ्टी ईयर्स को पढ़ते हुए मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी कपिल देव का एक पुराना विज्ञापन याद आता है. आज के क्रिकेट-प्रेमियों ने न देखा हो, लेकिन तीन दशक पहले हिंदी और अनेक भारतीय भाषाओं में प्रसारित इस विज्ञापन में कपिल पूछते हैं, ‘क्या जूते भी सांस लेते हैं?’ और सवाल का जवाब हां में देते हुए किसी कंपनी के श्ववास-युक्त जूतों की प्रशंसा करते हैं.
इसी तर्ज पर, अगर विश्वविद्यालय जैसे संस्थान भी सांस लेते जीव हैं, तो मौजूदा किताब हमें उल्टे सवाल पूछने को मजबूर करती है- क्या संस्थानों का भी दम घुटता है? क्या विश्वविद्यालय जैसे युवा उत्साह से भरे महकमे को भी जिंदा लाश बनाया जा सकता है?
2015 से 2020 तक जेएनयू पर जितने अलग-अलग तरह के प्रहार हुए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए कोई ताज्जुब नहीं कि यह निबंध-संग्रह सुनहरे अतीत को याद करते हुए संकटग्रस्त वर्तमान का मातम मनाता नज़र आता है.
पुस्तक की भूमिका के पहले वाक्य में ही इतिहासकार नीलाद्री भट्टाचार्य और जानकी नायर पाठकों को याद दिलाते हैं कि हमारे यहां ‘सांस्थानिक स्मृति’ यानी किसी संस्थान द्वारा अपने अतीत को अभिलेखित कर उसे सहेजने के व्यवस्थित प्रयास का अभाव रहा है.
वैसे भी भारतीय संस्थानों की जीवनी प्रायः दो ही शैलियों में लिखी जाती है- गौरव-गाथा या पतन-पुराण. दोनों शैलियां विरोधी होते हुए भी परस्पर पूरक हैं क्योंकि गौरव की ऊंचाई या पतन की गहराई को रेखांकित करने के लिए एकदूसरे की ज़रूरत पड़ती है. भारतीय मध्यवर्ग के कमोबेश दोषदर्शी मानस के कारण पतन-पुराणों का खास दबदबा रहा है.
ऐसा ही कोई दोषदर्शी पाठक चाहे तो इस संग्रह पर इन एक-आयामी शैलियों का शिकार होने का आरोप लगा सकता है. लेकिन ऐसा करना नासमझी ही नहीं नाइंसाफी भी होगी. नासमझी इसलिए कि जिस संस्थान पर जानलेवा हमला हो रहा हो उससे उसी वक्त सख्त आत्मनिरीक्षण की अपेक्षा नहीं की जा सकती.
नाइंसाफी इसलिए कि यह पुस्तक जेएनयू की आत्मा को, उसके बुनियादी उसूलों को, जिंदा रखने के संघर्ष का हिस्सा है- यह विश्लेषण का ग्रंथ नहीं बल्कि प्रतिरोध का दस्तावेज है.
लगभग 470 पन्नों के इस संग्रह में भूमिका के अलावा कुल 75 छोटे निबंध हैं, जिनके सभी लेखकों का जेएनयू से करीबी रिश्ता रहा है. ज़्यादातर लेखों का स्वर निजी और संस्मरणात्मक है.
संग्रह के बारह खंडों में जेएनयू की दुनिया के विभिन्न पहलू प्रस्तुत किए गए हैं. परिसर के पर्यावरण और जीव-जंतुओं से लेकर छात्रावासों में आम छात्रों की जिंदगी तक, विश्वविद्यालय की शुरुआती धारणा से लेकर उसे स्थापित करने की प्रक्रिया तक, और शिक्षण पद्धति के नवाचारों से लेकर परिसर की राजनीतिक संस्कृति तक का आंखोंदेखा हाल इन पन्नों में मिलता है.
लेखकों में शिक्षकों और छात्रों के अलावा दो पूर्व कुलपति, कुछ प्रशासनिक कर्मचारी, ढाबा-कैंटीन और फोटोकॉपी की दुकान चलाने वाले, और कुछ विदेशी छात्र व शिक्षक भी हैं. पुस्तक की पहल इतिहास विभाग की ओर से की गई है और पांचों संपादक इसी विभाग के हैं.
अभिजात विश्वविद्यालय होने के नाते जाहिर है कि संग्रह की भाषा अंग्रेज़ी है. हिंदी के पाठकों को यह जानकर खुशी होगी कि अन्य भाषाओं के प्रतिनिधित्व का श्रेय सिर्फ हिंदी को मिला है. लेकिन कई लेखकों ने भाषा के सवाल को उभारा है और अंग्रेज़ी-प्रधान पाठ्यक्रम में पैर जमाने के संघर्ष के दिनों को याद किया है.
ग़ैर-अंग्रेज़ी पृष्ठभूमि से आने वाले पूर्व छात्रों के व्यक्तिगत अनुभवों से जेएनयू परिसर की भाषाई विविधता का पता चलता है, जो इस परिसर की विलक्षणता का महत्वपूर्ण पहलू है. यहां ग़ैर-हिंदी प्रदेश- ख़ासकर दक्षिण और उत्तर-पूर्व से आए छात्रों का जिक्र भी ज़रूरी है, जिन्हें अंग्रेज़ी की अकड़ के अलावा हिंदी की हेकड़ी का भी सामना करना पड़ा है.
बहरहाल, हिंदी के कुल तीन लेख प्रतिनिधि कम और अपवाद ज़्यादा दिखते हैं. इन अपवादों में भी एक अपवाद है- केदारनाथ सिंह की यादगार कविता ‘जेएनयू में हिंदी’, जो बाकी सभी लेखों से अलग अपना अनन्य स्थान बनाती है.
संस्मरणात्मक संग्रह होने के नाते इसमें अतीत-मोह या नॉस्टेलजिया की उपस्थिति लगभग लाज़िमी है, किंतु यह संपादक मंडली की महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि इसे हावी नहीं होने दिया गया है. पुस्तक का बुनियादी सवाल सत्ता और ज्ञान के आपसी रिश्ते का है. इस रिश्ते का ताना-बाना तीन तथ्यों से तय होता है.
पहला यह कि सार्वजनिक विश्वविद्यालयों का खर्चा सरकार को उठाना पड़ता है ताकि बेहतर उच्च-शिक्षा को अमीरों की जागीर बनने से रोका जा सके. दूसरा कि अगर शिक्षा मात्र प्रशिक्षण से ऊपर उठना चाहती है- यानी ‘उच्च’ कहलाने लायक बनना चाहती है, तो शिक्षा-तंत्र का सत्ता-तंत्र से आज़ाद होना अनिवार्य है. तीसरा तथ्य यह है कि सरकारी पैसों से चल रही स्वायत्त संस्थानों को जनता और देश के प्रति जवाबदेह बनाए रखने के लिए एक ऐसी प्रणाली की ज़रूरत होती है जो लचीली होते हुए भी मजबूत और भरोसेमंद हो.
इन तीनों तथ्यों, या अनिवार्यताओं, में आपसी तनाव और खींचतान स्वाभाविक है. जाहिर है कि सत्ता के तराजू में विश्वविद्यालय के मुकाबले सरकार का पलड़ा हमेशा भारी पड़ेगा, इसलिए सत्ता के तौर-तेवर तीनों आयामों के संतुलन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं.
यदि सत्ता के संचालक में आत्मविश्वास और सांस्थानिक मूल्यों के लिए श्रद्धा है तो ऐसे राज में तमाम समस्याओं और विरोधाभासों के बावजूद विश्वविद्यालय जैसे संस्थान न केवल सांस ले पाते हैं बल्कि फलते-फूलते हैं. वहीं, अगर सत्तापक्ष वैचारिक रूप से अपने को असुरक्षित महसूस करता है और उसे संस्थानों की नाज़ुक सेहत की परवाह नहीं, तो ऐसे राज में विश्वविद्यालयों का दम घुटने लगता है और वे बीमार हो जाते हैं.
मोदी-राज में विश्वविद्यालयों पर जितने और जिस तरह के हमले हुए हैं उतने पिछले किसी भी सरकार के तहत नहीं हुए. जेएनयू को मीडिया ने कुछ ज़्यादा तूल दिया हो, लेकिन सत्तापक्ष के कोप के पात्रों की सूची में देश के कई जाने-माने संस्थानों के नाम दर्ज हैं. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय, भारतीय फिल्म और टेलेविज़न संस्थान, पुणे, टाटा समाज विज्ञान संस्थान मुंबई, इलाहाबाद विश्वविद्यालय- इन सबमें सत्ता के रौद्र अवतार के दर्शन हुए.
इस अभूतपूर्व खतरनाक परिघटना से देश ने मुंह मोड़ लिया तो हमारे श्रेष्ठ कहलाने वाले विश्वविद्यालयों का भविष्य अंधकारमय ही नहीं सीमित भी होगा.
ऐसा नहीं है कि पिछली सरकारें इस मामले में दूध की धुली थीं, लेकिन अपनी सारी काली करतूतों के बावजूद उनमें छात्र प्रतिरोध के युवा उत्साह, अतिरेकी भाषा और कड़वी शिकायतों और आरोपों के सामने संयम बरतने का धीरज था, और साथ में विचारों की दुनिया को तवज्जो देने की तमीज़ भी थी.
मौजूदा किताब के पृष्ठ 342 पर एक तस्वीर छपी है जो बिना शब्दों के बात को स्पष्ट कर देती है. 1977 का साल है, इमरजेंसी के उठने के तुरंत बाद जेएनयू छात्रसंघ का एक जलसा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी (जो उन दिनों विश्वविद्यालय की कुलाधिपति थीं) के घर पहुंचकर उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है. इंदिरा शांत भाव से हाथ पर हाथ बांधे छात्रसंघ अध्यक्ष के बगल में खड़ी हैं, जो उन्हें छात्रों की मांगें पढ़कर सुना रहे हैं. चित्र के शीर्षक से पता चलता है कि अगले ही दिन इंदिरा गांधी ने कुलाधिपति के पद से इस्तीफा दे दिया.
वैचारिक जगत में, विश्वविद्यालयों या फिर देश के भविष्य में आपकी थोड़ी भी रुचि है, तो इस पुस्तक को ज़रूर पढ़िएगा. पढ़ने पर आपको साफ पता चलेगा कि हां, विश्वविद्यालय भी सांस लेते जीवंत संस्थान हैं और उनका भी गला घोंटा जा सकता है.
(लेखक पूर्व जेएनयू छात्र हैं और वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र पढ़ाते हैं.)