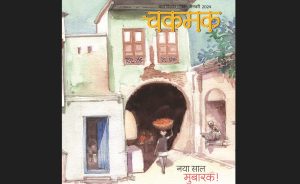कभी-कभार | अशोक वाजपेयी: हम स्वतंत्रता के पहले सर्जनात्मक और बौद्धिक रूप से अधिक स्वतंत्र थे और स्वतंत्रता के बाद पश्चिम के अधिक ग़ुलाम होते गए हैं.

स्वतंत्रता मिलने के पचहत्तर वर्ष बाद भी भारतीय साहित्य, ज्ञान और ज्ञानमीमांसा का उपनिवेशन न सिर्फ़ जारी है बल्कि कई बाद तो यह सामान्यीकरण करना उचित लगता है कि इस दौरान यह प्रक्रिया अधिक तेज़, अधिक व्यापक और अधिक गहरी हो गई है. इस पर विचार कम हुआ है और उसके वे अनेक रूप पहचाने तक नहीं गए हैं जो भारतीयता या देशजता के नाम पर इधर प्रचारित-प्रसारित हैं और जिन्हें उपनिवेश से मुक्ति के चिह्न मानने की मूल्यमूढ़ता दरपेश है.
आंबेडकर विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के ‘देशिक’: अभिलेख-अनुसंधान केंद्र ने अभय कुमार दुबे के नेतृत्व और वैभव सिंह के बीजपत्र के आधार पर दो दिनों का एक विशद परिसंवाद ‘हिंदी साहित्य पर पश्चिमी प्रभाव और देशज प्रतिमान’ विषय पर आयोजित किया. मुझे उसके शुभारंभ पर बोलने का अवसर मिला.
भारत में साहित्य और कलाओं को इतिहास के दौरान कई विदेशी वैचारिक और साहित्य-कला दृष्टियों से प्रतिकृत होने का अवसर मिला है. उनसे प्रभावित होने के कारण ही, उदाहरण के लिए, गांधार स्थापत्य, मिनिएचर कला, उर्दू काव्य, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में ख़याल आदि संभव हुए हैं.
इस आदान-प्रदान, संवाद ने भारतीय मनीषा और सृजन को प्रभावित किया पर वे उनसे आक्रांत या लगभग अपदस्थ नहीं हुए. यह स्थिति हमारे पश्चिम से हमारी वैचारिक और सर्जनात्मक मुठभेड़ से बदली है पर सारा पश्चिमी प्रभाव अनिवार्यतः औपनिवेशिक नहीं रहा है.
पश्चिम से हमारे यहां नई विधाएं, नई अवधारणाएं और नई टेक्नोलॉजी आई हैं- उपन्यास, कहानी, आलोचना, डायरी, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, पत्रकारिता, पत्रिकाएं. यथार्थ, समकालीनता, आधुनिकता, सामाजिक ज़िम्मेदारी, समाज-साहित्य-संबंध, साहित्य और कलाओं के सामाजिक-राजनीतिक-सांस्कृतिक आशय, संसार की मनुष्यकेंद्रीयता, मनोविज्ञान, समाजशास्त्रीयता, प्रतिबद्धता, पक्षधरता, साहित्य की सोद्देश्यता, प्रश्नवाचकता आदि. पुस्तकें, पत्रिकाएं, छापाखाना, डाकखाना, रेलगाड़ी, साइकिल, मोटर, बसें, फोन, मोबाइल, पेन, पेंसिल, कागज़, टाइपराइटर, रेडियो, टेलीविज़न, अख़बार, सिनेमा. शहर नियोजन, स्थापत्य, कपड़े, जीवनशैली, अनेक भोजन.
पहले के प्रभावों के पीछे किसी उपनिवेश की मंशा नहीं थी जबकि ब्रिटिश उपनिवेश का एक स्पष्ट और घोषित उद्देश्य भारत में अंग्रेज़ी भाषा और दृष्टि का स्थायी दूरगामी उपनिवेशन था. पश्चिम से आए सभी प्रभाव ज़रूरी तौर पर औपनिवेशिक मंशा वाले नहीं थे पर पश्चिम के भारतीय मानस में समावेशन के उपनिवेशन में बदलने की गाथा स्वतंत्रता से पहले शुरू हुई और स्वतंत्रता के पचहत्तर वर्ष बाद न तो समाप्त हुई है, न ही उसे समाप्ति की ओर बढ़ते देखा जा सकता है.
विडंबना यह है कि हिंदू राष्ट्र, हिंदू-मुसलिम भेदभाव, सांप्रदायिकता आदि अपने मूल में औपनिवेशिक हैं. वे औपनिवेशिक ज़हनियत का ही उत्पाद हैं. लोकतंत्र, संविधान, चुनाव प्रणाली, विधायिका, संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका, नगरपालिका, प्रशासन, क़ानून आदि बहुत-सी व्यवस्थाएं पश्चिम के प्रभाव में ही जन्मी और विकसित हुईं हैं. सभी प्रभाव अवांछनीय नहीं रहे हैं और उनमें से अधिकांश को हमने अपनी पारंपरिक ग्रहणशीलता और खुलेपने के कारण भी स्वीकार किया है.
उपनिवेशन की अवधारणा और प्रक्रिया का एक ज़रूरी हिस्सा था पश्चिमी ज्ञान का सार्वभौमिकीकरण. उसकी एक स्थायी उपलब्धि यह है कि उसने पश्चिमी ज्ञान का न सिर्फ़ वर्चस्व स्थापित किया, उसे सार्वभौमिक ज्ञान की तरह प्रतिष्ठित भी कर दिया.
पश्चिम से अलग विकसित ज्ञान और ज्ञान-पद्धतियों को ‘क्षेत्रीय’ क़रार दिया और औद्योगिकीकरण और टेक्नोलॉजिकल सफलताओं के आधार पर पश्चिमी ज्ञान को ऊंचा दर्ज़ा दे दिया गया. उत्तर-आधुनिकता के अंतर्गत इस सार्वभौतिकीकरण को स्वयं पश्चिम में प्रश्नांकित किया गया पर उससे स्थिति में कोई मौलिक बदलाव आया नहीं लगता.
उपनिवेशन, अनुकूलन और पश्चिमी ज्ञान के सार्वभौमिक आतंक से हिंदी आलोचना ने मुक्त होने की बहुत कम चेष्टा की है. स्वतंत्रता के पहले और उसके बाद ऐसे मक़ाम आए ज़रूर, जब कुछ प्रश्नांकन हुआ पर, कुल मिलाकर, वह अनुकूलन की जकड़ से बाहर नहीं आ सकी.
अकेले आलोचना के क्षेत्र में ही नहीं पश्चिम ने हमारी भारतीय समाज की समझ को बदल डाला है. समाज की यथार्थवादी समझ साहित्य में तो लगभग केंद्रीय हो गई जबकि रंगमंच, संगीत, चित्रकला, नृत्य और लोककलाओं में गै़र यथार्थवादी समझ बनी रही.
साहित्य में प्रतिनिधित्व का आग्रह बढ़ा. बहुसमयता के बोध के बजाय एकरैखिक ऐतिहासिक समय की जगह बहुत बढ़ गई. रसिक या सहृदय के स्थान पर पाठक-श्रोता-दर्शक आ गए. लोक-संबोधित साहित्य समाज-संबोधित होकर रह गया. ‘आत्मप्रतिष्ठ’ जैसी अवधारणा के स्थान पर ‘अमूर्तन’ जैसी नकारात्मक अवधारणा प्रचलित हो गई.
हमारे यहां साहित्य की स्वायत्तता की जो अवधारणा कवि को प्रजापति मानने और उस अपनी रुचि के अनुसार अपना संसार रचने की स्वतंत्रता के रूप में थी उसे कलावाद और समाज-विरोधी बताया जाने लगा. श्रृंगार और ऐन्द्रियता की लंबी भारतीय परंपरा विक्टोरियन मानसिकता के प्रभाव में साहित्य में अवमूल्यित हो गईं, भले संगीत और नृत्य में बची रहीं.
सारा अध्यात्म साहित्य से अपदस्थ हो गया भले वह मनुष्य की स्थिति-स्मृति-संस्कृति का अनिवार्य आयाम रहा है और अब भी है. धर्मों की सक्रियता और सामाजिक उपस्थिति के बावजूद उनसे हमारा असंवाद और उनकी सर्वथा उपेक्षा इस बीच हुए हैं, जबकि वे सामाजिक यथार्थ का ज़रूरी हिस्सा हैं. उदात्त और पवित्र हाशिये पर फिंक गए और उन्हें साहित्य से बाहर सामाजिक और पारिवारिक अनुष्ठानों तक महदूद कर दिया गया.
साहित्यक चेतना में संघर्ष ने सौंदर्य को अपदस्थ कर दिया और वह किसी हद तक संगीत और नृत्य के अहाते में रहा आया. भारतीय सौंदर्यशास्त्र और उसकी अवधारणाओं से अपरिचय और अज्ञान बहुत व्यापक हो गए जबकि उनमें से कई अपने आप में सार्वभौमिक होने का दर्ज़ा पाने योग्य हैं.
सोच-विचार, पूर्वपक्ष-उत्तरपक्ष की भारतीय ज्ञान-भाषा नष्ट-ध्वस्त हो गई, इधर कुछेक अपवाद जैसे समाज-विज्ञान को छोड़कर सारा वैचारिक उद्यम अंग्रेज़ी में होने लगा है. भाषाओं का धीरे-धीरे वैचारिक स्मृतिहीन होना उस सत्तारूढ़ राजनीति के बहुत अनुकूल है, जो इन दिनों उग्र और आक्रामक ढंग से जातीय समृति को ध्वस्त कर विस्मृति फैलाकर, नई छद्म स्मृति आरोपित कर रही है.
एक विडंबना यह भी है कि ठीक उस समय जब भारतीय मानस उपनिवेशित हो रहा था, पश्चिम में भाषा-चिंतन, संगीत, कविता में भारत की उपस्थिति बढ़ रही थी जैसे कि बीथोवन, फर्नांदो पेसोआ, जोसेफ़ ब्रॉडस्की, रोमन जैकबसन आदि के उदाहरणों में देखा जा सकता है. दूसरी ओर, भारतीय आधुनिकता के अपने जातीय तत्वों की अवहेलना और उन्हें पश्चिमी आधुनिकता के संस्करण के रूप में देखने की सफल पर दयनीय चेष्टा होती रही है.
वर्तमान भारतीय आधुनिकता की शुरुआत में बीसवीं शताब्दी के आरंभ में भारत से पश्चिमी सभ्यता और आधुनिकता का रैडिकल क्रिटीक गांधी जी ने ‘हिंद स्वराज’ में, रवींद्रनाथ ने विश्व मानव की अवधारणा में, श्री अरविंद ने अध्यात्म के पुनराविष्कार के रूप में किया था. कृष्णचंद्र भट्टाचार्य ने ‘विचारों के स्वराज’ की कल्पना की थी और स्वतंत्रता के बाद में लोहिया ने ‘आगेदेखू-पीछेदेखू आधुनिकता’ की बात की थी.
लेकिन लगता यह है कि हम स्वतंत्रता के पहले सर्जनात्मक और बौद्धिक रूप से अधिक स्वतंत्र थे और स्वतंत्रता के बाद पश्चिम के अधिक गुलाम होते गए हैं. इसका कोई व्यापक एहसास, आत्मालोचन हमारी आलोचना में नहीं है. हुआ तो यह भी है कि हमने साहित्य को साहित्य की तरह लिखना-पढ़ना-समझना-सराहना बहुत कम कर दिया है- साहित्य और सामाजिक यथार्थ के अन्वेषण, ऐतिहासिक राजनीतिक-सामाजिक दस्तावेज़ के रूप में लिखना-देखना बढ़ता गया है.
इस समय हिंदी अंचल में विघटन चरम पर है. आलोचना मात्र, असहमति की अभिव्यक्ति का अपराधीकरण हो चुका है. ग़नीमत यह है कि साहित्य में, सर्जनात्मक साहित्य में, फिर भी आलोचना, असहमति और विवाद की स्थिति और संभावना दोनों ही बची हुई हैं.
(लेखक वरिष्ठ साहित्यकार हैं.)