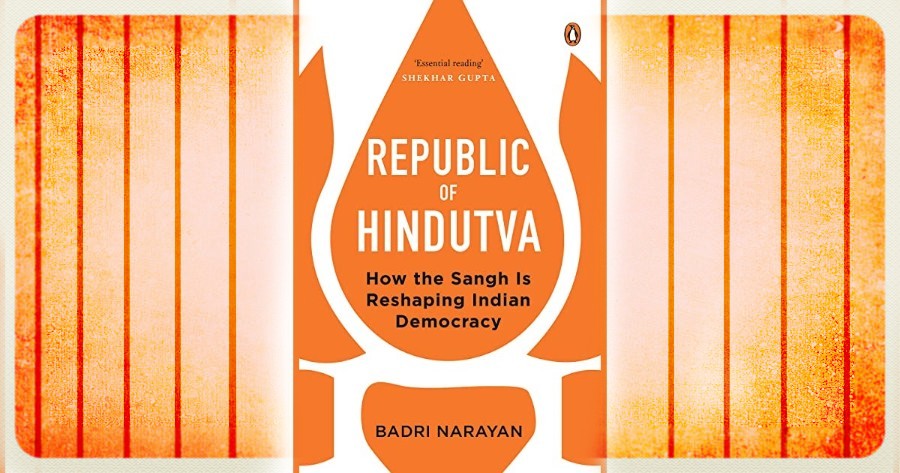पुस्तक समीक्षा: पढ़े-लिखे शहरियों और लेफ्ट-लिबरल तबकों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर जो धारणा रही है वह यह है कि संघ बहुत ही पिछड़ा संगठन है. बद्री नारायण की किताब ‘रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्व: हाउ द संघ इज़ रिशेपिंग इंडियन डेमोक्रेसी’ दिखाती है कि संघ ने इसके उलट बड़ी मेहनत से अपनी छवि तैयार की है.

इधर के कुछ वर्षों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (संघ) के बारे में लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है. 1925 में स्थापित संघ के बारे में 2014 से पहले कुछ इक्का-दुक्का किताबें ही मौजूद थीं जो अकादमिक और कभी-कभी लोकप्रिय तरीके से संघ के इतिहास, उसके सिद्धांतों और उससे जुड़े प्रमुख व्यक्तियों के बारे में जानकारी देती थीं.
वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सफलता ने समाज विज्ञानियों और चुनाव विश्लेषकों को हैरान कर दिया. एक-दो वर्षों की आरंभिक हिचकिचाहट के बाद लोगों ने यह मानना शुरू किया कि भाजपा की इस सफलता के पीछे संघ के कार्यकर्ता और उनका संगठन था.
यह सब जानते हैं कि 1990 के बाद के भारत के राजनीतिक दलों को बहुत आराम से समझ में आ गया था कि भारत में चुनावी सफलता तब तक संभव नहीं है जब तक दलित-बहुजन समुदायों के सबसे बड़े चुनावी खित्ते को अपनी ओर न मिलाया जाए.
कांशीराम, मायावती, मुलायम सिंह, यादव, रामविलास पासवान, लालू यादव और एचडी देवगौड़ा जैसे नेताओं ने 1989 से लेकर 2004 तक इसे सिद्ध भी किया. भाजपा, कांग्रेस और यहां तक कि कम्युनिस्ट पार्टियां भी इसे उपेक्षित नहीं कर सकती थीं. दलित-बहुजन राजनीतिक उभार के पहले उनके वोटर और कैडर का बड़ा हिस्सा इन समूहों से ताल्लुक रखता था.
वर्ष 2009 में ही इतिहासकार और मानवविज्ञानी बद्री नारायण ने अपनी किताब ‘फैसीनेटिंग हिंदुत्व: सैफरन पॉलिटिक्स एंड दलित मोबीलाइजेशन’ में इसे रेखांकित किया था कि संघ किस प्रकार दलित समुदायों के बीच पैठ बनाता है और उसका पैटर्न क्या है और यह सब भाजपा की मदद कैसे करता है.
लगभग एक दशक से ज्यादा समय के बाद उन्होंने अपने कहे हुए को न केवल फिर से देखा है बल्कि नए फील्ड डाटा के साथ एक नई किताब लिखी है.
उनकी किताब ‘रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्व: हाउ द संघ इज़ रिशेपिंग इंडियन डेमोक्रेसी’ इस बात की पड़ताल करती है कि संघ की वृहत्तर संरचना में ‘संगठन, विचार और व्यक्ति’ एक ही धरातल पर किस तरह काम करते हैं और वे किस तरह वे एक ‘हिंदू गणतंत्र की स्थापना’ की ओर अग्रसर हैं.
अपनी बात की पुष्टि के लिए बद्री नारायण किसी पूर्व निश्चित सिद्धांत से उसे नत्थी नहीं कर देते हैं बल्कि उसे समाज के बीच जाकर ही परीक्षित (टेस्टीफ़ाई) कर रहे हैं.
उन्होंने विभिन्न आयु वर्गों के स्त्रियों, पुरुषों, संघ से जुड़े कार्यकर्ताओं और नेताओं से लंबी बातचीत की है, उन्हें बोलने दिया है और इससे निकली बात को एक रोचक वृतांत में प्रस्तुत कर दिया है. ले
किन यह सब कोई एकरैखिक अकादमिक अभ्यास नहीं है बल्कि उसमें भारत का इतिहास, आजादी के बाद के भारत की विभिन्न जातियों के अनुभव, दलित सबलीकरण की परियोजनाएं और चुनावी राजनीति शामिल हैं.
पढ़े-लिखे शहरियों और लेफ्ट-लिबरल तबकों में संघ को लेकर जो धारणा रही है वह यह है कि संघ बहुत ही पिछड़ा और विभाजनकारी संगठन है. जैसा बद्री नारायण की यह किताब दिखाती है कि संघ ने इसके उलट बड़ी मेहनत से अपनी छवि तैयार की है.
उसने लोगों के जीवन में शामिल होने के लिए सेवा का सहारा लिया है. जनता के बीच अपनी पैठ सुनिश्चित करने के लिए उसने लगातार प्रतीकों, नायकों, विचारों और दायरों (स्पेस) का समाहारीकरण (एप्रोप्रियेशन) किया है.
इस प्रक्रिया से निकलने वाली राजनीति लोकसभा और विधानसभा चुनावों में रंग दिखाती है. इस समय विश्लेषकों एवं विपक्षी पार्टियों के हाथ में संघ नहीं बल्कि उसकी छाया हाथ में आती है. वे उससे पूरी कोशिश से लड़ना तो चाहते हैं लेकिन यह एक छाया-युद्ध साबित होता है क्योंकि तब तक संघ अपने आपको बदल लेता है.
हालांकि लेखक ने इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया है संघ के कई पुराने कार्यकर्ता उनकी इस बात से ताल्लुक न रखते हों.
यह किताब बिल्कुल शुरुआत में ही बताती है कि भारतीय समाज के वे सभी तबके (मुस्लिमों को छोड़कर) जो संघ की सामाजिक-सांस्कृतिक राजनीति के विरोध में खड़े थे, उन्हें संघ अपने आप में समाहित करता जा रहा है और वह एक नए प्रकार का समाज निर्मित कर रहा है. ‘रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्व’ इसी समाज का प्रकटीकरण है.
इस किताब का सबसे प्रमुख और अंतर्निहित तर्क यही है कि संघ और भाजपा एक दूसरे से नाभि-नालबद्ध हैं, हालांकि समय-समय पर भाजपा और संघ के पदाधिकारी इस बात पर जोर डालते रहे हैं कि दोनों स्वतंत्र सत्ताएं हैं और संघ का काम ‘सांस्कृतिक राष्ट्रवाद’ को बढ़ावा देना है. भाजपा का काम राजनीति से जुड़ा है.
यह किताब इस तर्क से आगे जाते हुए बताती है कि यह संघ का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद संपेरों, मुसहरों जैसी उपेक्षित जातियों और घुमंतू एवं अर्ध-घुमंतू समुदायों के बीच किस प्रकार रूप ग्रहण करता है और यह समुदाय भाजपा की वृहत्तर चुनावी कल्पनाओं में समाहित होते चले जाते हैं.
संघ इसके लिए लक्षित समुदायों और दायरों में ‘सेवा’ कार्यों का विस्तार करता है और जनता के एक बड़े हिस्से को अपने से जोड़ने का प्रयास करता है.
राष्ट्रीय सेवा भारती, विद्या भारती, वनवासी कल्याण आश्रम, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, शिशु शिक्षा प्रबंध समिति, सहकार भारती जैसे संघटक-संगठन शिक्षा, श्रम, सहकारी समितियों और मजदूरों के बीच काम करते हैं और बजरंग दल एवं विश्व हिंदू परिषद हिंदू हितों को आगे ले जाने का दावा करते हैं.
एक व्यापक संगठन के ढीले-ढाले ढांचे के अंदर यह सभी संरचनाएं काम कर रही होती हैं. भारतीय मजदूर संघ और स्वदेशी जागरण मंच जैसे संगठन सरकार से विभिन्न मुद्दों जैसे भूमि-अधिग्रहण और विदेशी पूंजी के प्रवेश के मुद्दे पर अलग रवैया रखता है लेकिन अंतत: उन सबका समाहार संघ के अंदर हो जाता है.
संघ जहां अपनी अंदरूनी दिक्कतों को समायोजित कर लेता है वहीं भारतीय समाज की उन सच्चाइयों का समाहारीकरण कर लेने की कोशिश करता है जो उसके रास्ते में रुकावट पैदा करती हैं.
एक तरफ संघ दलितों के बीच पैठ बनाता है, उन झुग्गी-बस्तियों का भगवाकरण करता है जहां आंबेडकर और कांशीराम की राजनीति परवान चढ़ी थी.
बद्री नारायण इसके लिए ‘सैफरन स्लम’ पद का इस्तेमाल करते हैं. एक समय माना जा रहा था कि इन झुग्गी-बस्तियों से नयी दलित राजनीति निकलेगी. अब उस राजनीति ने भाजपा की तरफ मुंह कर लिया है.
भाजपा की चुनावी सफलता को तब तक डिकोड नहीं किया जा सकता है जब तक ऐसे उपेक्षित दायरों का गहन समाजशास्त्रीय अध्ययन न किया जाए. बद्री नारायण यह करते रहे हैं.
वे संघ की उस दुविधा पर भी उंगली रखते हैं कि समाज के निचले तबकों के बीच अपना राजनीतिक आधार बढ़ा रहे संघ की एक परेशानी यह भी है कि वह अपने ‘कोर सपोर्टर्स’ यानी उच्च जातियों को भी नाराज नहीं करना चाहता है.
इस किताब का सबसे महत्त्वपूर्ण हिस्सा वह है जहां बद्री नारायण संघ, भाजपा और उसके मतदाताओं के रिश्ते की विवेचना करते हैं. वास्तव में वर्तमान भारत में चुनावों में किसी पार्टी की जीत दरसअल उसके नैरेटिव की जीत है.
सभी पार्टियां अपने इतिहास, विचारधारा और संभावित मतदाताओं को ध्यान में रखकर नैरेटिव की रचना करती है. भाजपा ने 2014 में विकास और हिंदुत्व का नैरेटिव सामने रखा और फरवरी 2019 में इसे थोड़ा पीछे रखते हुए इसमें बालाकोट की घटना का नैरेटिव राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल के साथ जोड़कर प्रस्तुत कर दिया.
उधर मायावती और अखिलेश यादव ने दलित-पिछड़ा गठजोड़ का नैरेटिव रचने का प्रयास तो किया लेकिन वह चल नहीं पाया. यहां तक की मायावती जी को अली-बजरंग बली का नैरेटिव गढ़ना पड़ा.
उत्तर प्रदेश के भाजपाई मुख्यमंत्री ने विकास और हिंदुत्व के आख्यान को कुंभ 2019 के मेले में एक बार फिर मिला दिया. अपनी सुविधा और अवसर के अनुसार भाजपा और संघ हिंदुत्व का नैरेटिव प्रस्तुत करते रहते हैं और इसके लिए जमीन तैयार करने का काम संघ करता है.
ऐसे बहुत सारे विवरणों के द्वारा बद्री नारायण यह दिखाते हैं कि चुनाव किस प्रकार आख्यानों की लड़ाई में बदल जाते हैं और वर्तमान संदर्भ में भाजपा और संघ अपने नैरेटिव से इन चुनावों में कैसे आगे निकल जाते हैं.
जब मैं यह लेख लिख रहा हूं तो कोरोना के मामलों में भयावह उछाल देखा जा रहा है. लोगों का जीवन संकट में है और हरिद्वार में कुंभ चल रहा है. वहां भी कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या की खबरें आ रही हैं.
बद्री नारायण अपनी किताब के पश्चातकथन में कहते हैं कि जब जब कभी यह महामारी नियंत्रित हो जाएगी, सामाजिक जीवन सामान्य हो जाएगा तो संघ हिंदुत्व पब्लिक और बायो पब्लिक को आपस में मिला देगा.
2020 में कोविड के शुरुआती समय में ही दार्शनिक ज्यार्जीओ अगमबेन ने इस बात की ओर इशारा किया था कि ऐसी विपदाओं में किस प्रकार सामान्य जनता को केवल जीने की पड़ी रहती है और शरीर ही उसकी चिंता का प्रमुख केंद्र बन जाता है. भारतीय परिदृश्य में जाति और अस्पृश्यता पहले से ही थे. कोरोना ने इसे तीखा कर दिया है.
बद्री नारायण इसे मानते हुए भी यह कहते हैं कि कुछ स्थानों पर जाति-भेद कुछ समय के लिए कमजोर भी हुए लेकिन इसे हमेशा के लिए तो नहीं कहा जा सकता है. संघ इन्हीं भेदों को कम करके अपनी संरचना में मिला लेना चाहता है.
यह किताब भारतीय राजनेताओं, विद्वानों, पत्रकारों के लिए जरूरी किताब तो है ही, यह समाज विज्ञान के शोध छात्रों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित हो सकती है जो किसी परिघटना की निर्मिति और उसके सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रभाव का अध्ययन करना चाहते हैं.
(लेखक स्वतंत्र शोधकर्ता हैं.)