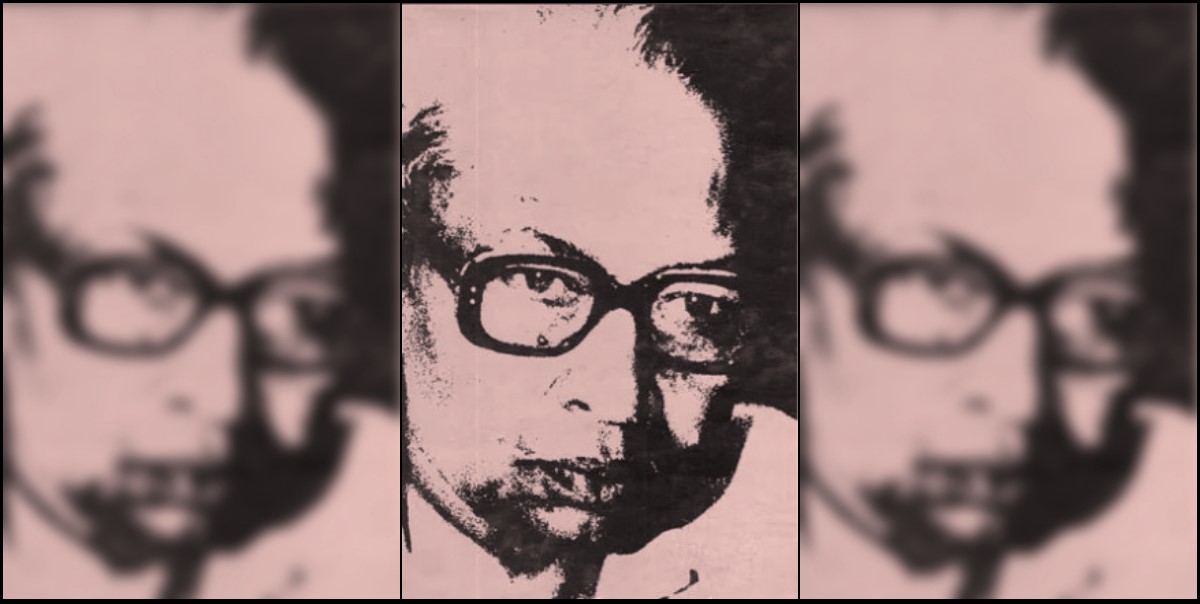जन्मदिन विशेष: रघुवीर सहाय की कविता राजनीतिक स्वर लिए हुए वहां जाती है, जहां वे स्वतंत्रता के स्वप्नों के रोज़ टूटते जाने का दंश दिखलाते हैं. पर लोकतंत्र में आस्था रखने वाला कवि यह मानता है कि सरकार जैसी भी हो, अकेला कारगर साधन भीड़ के हाथ में है.

हिंदी कविता के मुक्त आकाश में हर विचारधारा और हर विषयवस्तु ने खुलकर अपना रूप प्राप्त किया है. इसलिए यह आश्चर्य नहीं है कि कभी छायावाद की-सी अतिशय भावुकता से भरी पीढ़ी कविताओं के माध्यम से अपना मन खोल सकी तो वहीं मार्क्सवादी सामाजिकता से डूबी हुई कविताएं प्रगतिशील साहित्य के नाम पर अपना मुक़ाम पा सकीं.
इन सबके बाद एक वर्ग वह भी आया जिसने कविता को एक प्रयोग मानकर पुराने सभी बासी पड़ गए उपमानों को खारिज करने का घोष किया तो वहीं नेहरू युग के साथ-साथ विकसित हुई नई कविता ने लघुमानव को साहित्य का सूत्रधार बनाया.
हिंदी कविता के इस आधुनिक विकास यात्रा में कवि रघुवीर सहाय को अगर ढूंढना हुआ तो हम पाएंगे कि वह, जैसा कि आलोचक परमानंद श्रीवास्तव कहते हैं ‘प्रयोगवाद और नई कविता की संधि’ पर कहीं खड़े हैं और बड़ी मजबूती से खड़े हैं. यह संधि राजनीतिक फलक पर साठ के दशक के उत्तरार्ध में- यानी नेहरू युग की समाप्ति और लोहिया की मृत्यु पर- देखी जा सकती है .
सहाय उस पीढ़ी के प्रतिनिधि कवि हैं जिन्होंने राष्ट्र निर्माण के स्वप्नों को चुकते देखा था. ‘दिल्ली मेरा परदेस’ की भूमिका में 1957-67 के पूरे दौर को वे ‘एक विश्वास के बार-बार झकझोरे जाने का दौर’ बताते हैं- जो कि वह दौर है जो 1947 से 1957, माने स्वतंत्रता के शुरुआती दस वर्षों, जो सहाय के शब्दों में राष्ट्रनिर्माण के उत्साह का वर्ष थे, का उत्तराधिकारी था.
यहां अब युवा भारत के प्रति वह मोह नहीं दिखता जो पहले कि कविताओं में दिखाई पड़ता है. नेहरू के देहांत के तीन वर्षों के अंदर राममनोहर लोहिया का भी अंत हो जाना और इस तरह समाजवादी राजनीति के अवसर के अवसान से लोकतंत्र पर आने वाले संकट की आशंका सहाय के कवि-मन को घेरती है, जिसकी सबसे सुंदर अभिव्यक्ति वह अपने काव्य संग्रह ‘आत्महत्या के विरुद्ध’ में करते हैं.
‘अधिनायक‘ कविता में वह लिखते हैं:
राष्ट्रगीत में भला कौन वह
भारत-भाग्य-विधाता है
फटा सुथन्ना पहने जिसका
गुन हरचरना गाता है.
संयुक्त प्रांत के लखनऊ में 9 दिसंबर 1926 को जन्मे रघुवीर सहाय सामान्य मध्यवर्गीय परिवार से थे, जहां एक साथ सरकारी, आर्यसमाजी और कांग्रेसी प्रभाव में वो पलते-बढ़ते रहे. स्वयं को औसत दर्जे का विद्यार्थी मानने वाले सहाय, साहित्य लेखन में अपनी रुचि के संदर्भ में कहते हैं: ‘यह मैं नहीं कह सकता कि कला के लिए अपनी रुचि मैंने किसी एक व्यक्ति से पाई, मगर यह शायद सच हो कि पिताजी की सादगी से मैंने कला की प्रेरणा ली हो.’
सहाय के लेखक जीवन की शुरुआत साल 1947 में हुई, जब एक बार उन्होंने हरिवंश राय बच्चन की कविताएं पढ़ीं और बकौल सहाय ‘उनकी वेदना से मेरा कंठ फूटा… तभी से लिखना आरंभ किया. पंत और निराला का अगर असर हुआ तो बहुत टेढ़े तरीके से. अन्य आधुनिक कवियों में अज्ञेय और शमशेर बहादुर ने -जिनकी बौद्धिक आत्मानुभूति और बोधगम्य दुरूहता किसी हद तक एक ही-सा प्रभाव डालती हैं- मुझे अपनी आगामी रचनाओं के लिए काफी तैयार किया.’
रघुवीर सहाय ने सक्रिय जीवन जिया- हलचलों से भरा. अपने लेखन के आरंभिक वर्षों से अंतिम समय तक वे निरंतर रचना के मोर्चों पर सक्रिय रहे. साहित्य और पत्रकारिता की शुरुआत उन्होंने लखनऊ में की. लखनऊ से निकलने वाले ‘नवजीवन’ दैनिक पत्र से पत्रकारिता की शुरुआत हुई. 1946-51 तक वे रेडियो से जुड़े, जहां पर कविताओं के अलावा बच्चों के लिए अनेक कहानियों का भी प्रसारण किया.
तार सप्तक के दूसरे संस्करण के लिए अज्ञेय ने साल 1949 में पहले-पहल उनसे कविताएं मांगीं. ‘बसंत’, ‘पहला पानी’ जैसी कविताएं इस संकलन का हिस्सा बनीं. ‘प्रतीक’ का सहायक संपादक बनाकर अज्ञेय ने ही उन्हें दिल्ली बुलवाया और अज्ञेय के साथ शुरू हुई यह साहित्यिक-बौद्धिक साझेदारी आगे भी बनी रही जब, वर्ष 1959 में अज्ञेय ने अंग्रेज़ी का त्रैमासिक वाक् निकाला.
आकाशवाणी से लंबे समय तक जुड़े रहने वाले रघुवीर सहाय ने संवाददाता की लंबी पारी खत्म करने के बाद, नवभारत टाइम्स और फिर हिंदी के प्रसिद्ध पत्र दिनमान का संपादन भी 1970 से 1983 तक किया. इसके बाद स्वतंत्र रूप से अपने जीवन के अंतिम दिनों तक वह साहित्य लेखन या फ्रीलांसिंग करते रहे.
मीडिया और संचार माध्यमों की निहायत ही व्यस्त और भाग-दौड़ से भरी ज़िंदगी के बीच ही उन्होंने प्रचुर साहित्य भी लिखा. लगातार ही उनकी कविताएं प्रकाशित होती रहीं और उस दौर के साहित्यिक विमर्श और आलोचना के केंद्र में बनी रहीं. अपनी रचनाशीलता के 45 वर्षों में सहाय ने विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट साहित्य रचा जो प्रकाशित और अप्रकाशित सभी रूप में ‘रघुवीर सहाय रचनावली‘ के छह खंडों में संकलित है.
कुछ प्रमुख कविता संग्रह सीढ़ियों पर धूप में (1960), आत्महत्या के विरुद्ध (1967), हंसो-हंसो जल्दी हंसो (1975), लोग भूल गए हैं (1982), कुछ पते कुछ चिट्ठियां (1989), प्रतिनिधि कविताएं (1994), एक समय था (1995) हैं. इसके अलावा, रास्ता इधर से है (1972) , जो आदमी हम बना रहे हैं (1982) सहाय के प्रमुख कहानी संग्रह हैं.
कविता या कवि-कर्म समाज को बदलने का एक उपकरण हो सकता है, सहाय इस विश्वास के साथ यथार्थ की अवधारणा को समझते थे. अपने एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा भी कि ‘कविता लिखने के कर्म में ही निहित है कि दोतरफ़ा (स्वयं और लोगों का) बदलाव होगा. इस आधार पर यथार्थ की यह परिभाषा कर सकते हैं कि वह जो बदलने के लिए हमें प्रेरित करे, यथार्थ है. इसके अतिरिक्त यथार्थ का अगर कोई अर्थ निकलता है तो वह हमारे काम का नहीं है.’
नई कविता के बाद की युवा विद्रोही कविता का मुहावरा बनाने वालों में रघुवीर सहाय अग्रणी हैं. उनका काव्य संग्रह ‘आत्महत्या के विरुद्ध’ काव्यात्मक सृजनशीलता के स्तर पर एक नई कवि-दृष्टि और साहस का परिचायक है. यह साहस किसी भी किस्म की रोमांटिक गंभीरता को ध्वस्त कर नई अर्थ-छवियों को जन्म देता है. शब्दों के इस खेल से, इस कौतुक से सहाय लगभग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की सरोज स्मृति की तरह ही करुणा और हास्य को मिलाकर जीवन की त्रासद विडंबनाओं को काव्य में ढालते हैं.
रघुवीर सहाय सामाजिक यथार्थ को प्रस्तुत करने के पक्षधर थे पर समाज को समझने की उनकी दृष्टि वैज्ञानिक थी. मार्क्सवाद को कविता पर जबरदस्ती गिलाफ की तरह चढ़ाए जाने के वो सख्त खिलाफ थे. इसके बजाय वह मानते थे कि कविता में अगर जान और माने लाने हैं तो अपनी मध्यवर्गीय बौद्धिक चेतना को जागरूक रखना पड़ेगा और बराबर जागरूक रहकर एक दृष्टिकोण बनाना होगा.
अपनी कविताओं को इसलिए वह साधारण बोल-चाल की भाषा में ही लिखते हैं ताकि वह जन-जीवन से अपना सरोकार जोड़ सके. पर वह मानते हैं कि इस कारण ‘कहीं-कहीं भाषा की फ़िजूलखर्ची उन्हें करनी पड़ी है.’ कविता के लिए सबसे जरूरी जो तत्व सहाय मानते हैं, वह शिल्प से अधिक विचार वस्तु ही थी. और विचार वस्तु से उनका तात्पर्य वे वास्तविकताएं थीं, जिनसे एक कवि प्रेरणा लेता है.
दूसरा सप्तक में कविताओं से पूर्व अपने वक्तव्य में इसी संदर्भ में वह लिखते हैं:
‘विचारवस्तु का कविता में खून की तरह दौड़ते रहना कविता को जीवन और शक्ति देता है, और यह तभी संभव है जब हमारी कविता की जड़ें यथार्थ में हों.’
आत्महत्या के विरुद्ध, जिसमें रघुवीर सहाय की 1957-67 के बीच की लिखी कविताएं संकलित हैं, न केवल स्वयं सहाय की प्रतिनिधि रचना है, बल्कि इस पूरे दशक की भी सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक-साहित्यिक व्याख्या है.
स्वतंत्रता के बाद जिस लोकतंत्र का वादा सत्ता पर आसीन राजनेताओं ने अपनी जनता से किया था, उसी लोकतंत्र की सच्चाई उधेड़ते हुए सहाय इस संकलन के वक्तव्य में लिखते हैं, ‘लोकतंत्र- मोटे, बहुत मोटे तौर पर लोकतंत्र ने हमें इंसान की शानदार ज़िंदगी और कुत्ते की मौत के बीच चांप लिया है.’
पर इस स्थिति में एक संवेदनशील साहित्यिक होने की क्या भूमिका होनी चाहिए, इस पर भी वह ग़ौर करते हैं:
‘इस स्थिति में सबसे आसान यह पड़ता है कि व्यक्ति-स्वातंत्र्य की अभी तक बची सुविधा का फ़ायदा उठाकर मैं, अपने लिए बचे रहने की निजी, बिल्कुल अहस्तांतरीय रियायत ले लूं. उससे कुछ मुश्किल यह है कि मैं यह रियायत अस्वीकार करूं और उनके आसरे जिंदा रहूं जो इंसान के लिए दूसरे हथियारों से लड़ते हैं- साहित्येतर हथियारों से.
सबसे मुश्किल और एक ही सही रास्ता है कि मैं सब सेनाओं में लड़ूं -किसी में ढाल सहित, किसी में निष्कवच होकर-मगर अपने को अंत में मरने सिर्फ अपने मोर्चे पर दूं-अपनी भाषा के, शिल्प के और उस दोतरफ़ा ज़िम्मेदारी के मोर्चे पर जिसे साहित्य कहते हैं.’
सहाय की कविता राजनीतिक स्वर लिए हुए वहां जाती है, जहां वह स्वतंत्रता के स्वप्नों के दिन-ब-दिन टूटते जाने का दंश दिखलाते हैं. पर लोकतंत्र में आस्था रखने वाला कवि यह मानता है कि विराट भीड़ों के समाज को बदलने का आज सिर्फ एक साधन है: वह है उस सत्ता का उपयोग जो समुदाय का एक-एक व्यक्ति अलग-अलग निर्णयों से कुछ हाथों में देता है. सरकार जो राज्य की प्रतिनिधि है, जो समाज की प्रतिनिधि है, वह जैसी भी हो सकती है- अधूरी, टूटी, नकली मिलावटी, मूर्ख- अकेला कारगर साधन भीड़ के हाथ में है.
और इस साधन के अधिकाधिक सही इस्तेमाल के लिए लड़ाई ही उनकी कविता का प्रमुख स्वर थी. और इसलिए जनता के प्रति ही अपनी संवेदना वह कुछ इन शब्दों में व्यक्त करते हैं:
‘एक मेरी मुश्किल है जनता
जिससे मुझे नफरत है सच्ची और निस्संग
जिस पर कि मेरा क्रोध बार-बार न्योछावर होता है.’
इसी कड़ी में, मनुष्य को बचाने में निरंतर अधिकाधिक असमर्थ होते समाज की सबसे परिपक्व अनुकृति उनकी ‘रामदास’ शीर्षक कविता है, जो 1974 में- यानी आपातकाल के एक साल पहले लिखी गई थी. यह कविता निरंकुश समाज व्यवस्था की निरंकुशता, असहृदयता को दिखलाने वाली उत्कृष्ट रचना है. यहां सब तमाशबीन हैं उस घोषित हत्या के, जो निर्धारित थी, जिसका सभी को पता था. पर कोई भी इसके विरुद्ध आवाज़ उठाने वाला नहीं है.
रामदास, प्रतीक सिर्फ व्यक्ति का ही नहीं, बल्कि संभवतः उस अवधारणा का भी है, जिसे हम लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, सहिष्णुता, सद्भावना जैसी शब्दावली में ढाल सकते हैं.
‘हंसो हंसो जल्दी हंसो’ संग्रह में संकलित यह कविता आज के सामाजिक संदर्भों के लिए भी उतनी ही या उससे ज्यादा प्रासंगिक है, जहां हमें कवि यह बारम्बार आगाह करते हुए नजर आते हैं कि तमाशबीनों में तब्दील होते हुए लोगों की स्वयं की भी नियति किसी भी दिन रामदास की तरह हो सकती है, जिसे दिनदहाड़े सड़क के बीचों-बीच निहत्था मारा जा सकता है.
‘निकल गली से तब हत्यारा
आया उसने नाम पुकारा
हाथ तौलकर चाकू मारा
छूटा लोहू का फव्वारा
कहा नहीं था उसने आखिर उसकी हत्या होगी.’
और इसलिए वह चाहते हैं कि हम बोलना सीख जाएं- अन्याय , अव्यवस्था, गरीबी, भुखमरी, विषमता के विरुद्ध. आत्महत्या के विरुद्ध कविता में वह लिखते हैं:
‘कुछ-न-कुछ होगा अगर मैं बोलूंगा
न टूटे, न टूटे तिलिस्म सत्ता का
मेरे अंदर एक कायर टूटेगा
मेरे मन टूट एक बार सही तरह.’
यह बोलना ही शायद अपने जीवित रहने की निशानी है, क्योंकि ‘हर दिन मनुष्य से एक दर्ज़ा नीचे रहने का दर्द’ अपने आस-पास फैली विषमता को अस्वीकारने का प्रोत्साहन है, जो रघुवीर सहाय अपनी रचनाओं के माध्यम से हमें देते हैं. व्यक्ति की वैचारिक स्वतंत्रता के संकट को बहुत पहले से सहाय अपनी रचनाओं में उठाते हैं, और गुजरते दौर के साथ उनका यह आग्रह बढ़ता जाता है.
अपनी एक कविता ‘स्वाधीन व्यक्ति’ में वह लिखते हैं:
‘बहुत दिन हुए तब मैंने कहा था लिखूंगा नहीं
किसी के आदेश से
आज भी कहता हूं
किंतु आज पहले से कुछ और अधिक बार
बिना कहे रहता हूं
क्योंकि आज भाषा ही मेरी एक मुश्किल नहीं रही.’
और वैचारिक स्वतंत्रता को मूलभूत मानने का उनका आग्रह अपने समय और समाज में पल रही जनता से इसलिए ज्यादा है क्योंकि यह जनता ही है जो भेड़ों में तब्दील हो जाने का खतरा रखती है. जिनसे राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्वार्थसिद्धि के लिए कुछ भी करवाया जा सकता है. और जो इस प्रकार भेड़ बन जाने के बरअक्स स्वतंत्र रहने का खतरा उठाते हैं वह व्यवस्था की, समाज की आंखों की किरकिरी बन जाते हैं.
इस विडंबना को ही ध्यान में रखते हुए 1966 में रघुवीर सहाय यह पंक्तियां लिखते हैं: ‘स्वाधीन इस देश में चौंकते हैं लोग/एक स्वाधीन व्यक्ति से.’
रघुवीर सहाय का साहित्य पढ़कर यह अवश्य लगता है कि- सत्ता का हृदय परिवर्तन हो जाएगा और एक समतामूलक समाज, शोषण विहीन समाज बन सकेगा- ऐसी गलतफहमी के वह शिकार नहीं थे. पर वह यह ज़रूर मानते थे कि लोग न्याय और बराबरी के जन्मजात आदर्श को नहीं भूलते: इतिहास के किसी दौर में कुछ लोग अवश्य इन्हें भूल जाते हैं पर इन्हें याद कराने के लिए उनसे कहीं बड़ी संख्या में मनुष्य जीवित रहते हैं. उनकी कविताएं इन्हीं मनुष्यों को ढूंढने का, ढूंढकर जगाए रखने का आवश्यक काम करती है.
(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में शोधार्थी हैं.)