‘सनातन धर्म’ को लेकर हालिया विवाद में भाजपा के रवैये के विपरीत हिंदुत्व के सबसे प्रभावशाली विचारक विनायक दामोदर सावरकर ने शायद ही कभी ‘सनातन धर्म’ को पूरे हिंदू समुदाय से जोड़ा.

1 जुलाई, 1941 को हिंदू महासभा के तत्कालीन अध्यक्ष विनायक दामोदर सावरकर ने सनातन धर्म को समर्पित एक संगठन के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की. श्री भारत धर्म महामंडल के प्रतिनिधिमंडल के साथ उनकी बातचीत राजनीतिक संदर्भ में थी- हिंदू महासभा बंगाल समेत मुस्लिम बहुल प्रांतों में मुस्लिम लीग या उसके पूर्व सहयोगियों के साथ गठबंधन सरकारों में शामिल होकर प्रांतीय स्तर पर सत्ता का स्वाद चखने की कोशिश में थी.
जाति सुधारों के साथ उनके बहुप्रचारित जुड़ाव के कारण वे सनातनी चिंतित थे कि क्या सावरकर, बॉम्बे और मद्रास प्रेसीडेंसी में कांग्रेस द्वारा स्थापित की गई मिसाल का पालन करते हुए, अछूतों के लिए मंदिरों को खोलने वाले कानून का समर्थन करेंगे.
उनकी चिंताओं पर बात करने के बाद सावरकर की उस बैठक का विवरण इस स्पष्ट स्वीकारोक्ति के साथ शुरू हुआ कि ‘हिंदू महासभा और सभी सनातन संगठनों में 95% समानताएं हैं.’ यहां तक कि सावरकर ने वादा किया था कि हिंदू महासभा मंदिरों के क्षेत्र में किसी भी तरह के विधायी हस्तक्षेप की अनुमति नहीं देगी.
उन्होंने कहा था, ‘जहां तक विचारों में 5% मतभेद का सवाल है, मैं गारंटी देता हूं कि हिंदू महासभा कभी प्राचीन मंदिरों में अछूतों के प्रवेश के संबंध में किसी भी कानून को लागू नहीं करेगी या उन मंदिरों में प्रचलित किसी भी पवित्र प्राचीन और नैतिक कामकाज या रीति-रिवाज को कभी भी कानून द्वारा बाध्य नहीं करेगी.’
इस प्रकार, भले ही उन्होंने रूढ़िवाद से समझौता किया, हिंदुत्व के सबसे प्रभावशाली विचारक ने यह स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने सनातन धर्म की पहचान को जाति अलगाव से जोड़ा था. ‘सनातन धर्म’ को लेकर मौजूदा विवाद में भाजपा के कथन के विपरीत, सावरकर ने शायद ही सनातन धर्म को पूरे हिंदू समुदाय के साथ जोड़ा था.
यह उस अपील से और भी स्पष्ट है, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि उन्होंने उसी बैठक में उस रूढ़िवादी वर्ग से सुधारवादियों को कानून के अलावा अन्य तरीकों से हिंदुओं के बीच समानता लाने के प्रयास करने की अपील की थी:
‘सामान्य तौर पर महासभा हमारे सनातनी भाइयों पर सुधारवादी विचार थोपने के लिए किसी भी कानून का समर्थन नहीं करेगी, जहां तक पर्सनल लॉ का सवाल है, लेकिन इसके विपरीत सनातनियों को यह मानना चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में सभी हिंदुओं को समानता के आधार पर देखा जाना चाहिए और सुधारवादियों को अनुनय (समझाने-बुझाने) और सोच में बदलाव के जरिये उनके धार्मिक सुधार आदि करने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए.’
हालांकि, यह बहस का विषय हो सकता है कि क्या सावरकर, जो खुद एक बैरिस्टर थे, यह मान सकते थे कि सुधारवादी वर्ग के पास कानून का सहारा लिए बिना हिंदू समुदाय के भीतर समानता लाने का विकल्प था. चाहे वह दलितों के लिए मंदिर में प्रवेश के बारे में हो या हिंदुओं के लिए अंतरजातीय विवाह को वैध बनाने के बारे में, इतिहास इस बात की गवाही देता है कि ये समाज सुधार तभी हो सके जब रीति-रिवाजों और धर्मग्रंथों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को कानून के माध्यम से ख़त्म किया गया.
फिर भी, 1941 में ‘व्हर्लविंड प्रोपेगैंडा’ शीर्षक से अपनी घोषणाओं के अधिकृत संग्रह में सावरकर ने जाति सुधार के लिए अपने ‘गैर-जबरिया दृष्टिकोण’ के सनातनियों पर प्रभाव के बारे में दावा किया है: ‘इस रवैये की सनातनी नेताओं ने बहुत सराहना की है और कई प्रमुख हलकों में इस पर सौहार्दपूर्ण और ईमानदार चर्चा हो रही है.’
जाति सुधार के सवाल पर गैर-सनातनवादी हिंदुओं के प्रति उनकी कथित सहानुभूति को देखते हुए एक और कारण था कि सावरकर को कानून की अपरिहार्यता के बारे में पता होना चाहिए था: सनातन धर्म की वो बहस, जो एक दशक पहले हिंदू दक्षिणपंथ के एक अन्य प्रतीक- मदन मोहन मालवीय और अस्पृश्यता के खिलाफ रहे सबसे प्रसिद्ध नेता महात्मा गांधी के बीच हुई थी.
ऐतिहासिक पूना समझौते के बाद हुई 1933 की उक्त बहस दलितों के लिए मंदिरों को खोलने के लिए विधायी मार्ग को गांधीजी के देर से मिले समर्थन के बाद सामने हुई थी.
हालांकि, गांधी-समर्थित विधायी प्रस्ताव ने बहुत कुछ हिंदुओं की समझदारी, उनके विवेक पर छोड़ दिया था, लेकिन यह मालवीय को विरोध के लिए उकसाने को पर्याप्त था, जिन्होंने 23 जनवरी, 1933 को वाराणसी में ‘सनातन धर्म महासभा’ के रूप में एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया था.
उस सभा में अन्य सनातनियों से मिले समर्थन से उत्साहित होकर मालवीय ने 8 फरवरी, 1933 को गांधी को पत्र लिखा, जिसमें महात्मा की धर्मग्रंथों की व्याख्या से उनकी कोई असहमति नहीं थी: ‘इस विचार के लिए बहुत समर्थन है कि कुछ व्यक्ति कुछ शर्तों के तहत अछूत हैं और कुछ अन्य व्यक्ति अपने जन्म और व्यवसाय के कारण अछूत हैं.’
चूंकि दलितों के सबसे बड़े नेता बीआर आंबेडकर ने तब तक जाति के आधार पर हिंदू समुदाय में सुधार करना छोड़ दिया था, तो उन्होंने मंदिर प्रवेश कानून का समर्थन करने के गांधी के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया. 14 फरवरी, 1933 को गांधीजी को लिखे उनके पत्र की शुरुआत इस खंडन के साथ हुई कि ‘मंदिर में प्रवेश के सवाल पर विवाद सनातनवादियों और महात्मा गांधी तक ही सीमित है.’
औपनिवेशिक काल के दौरान सनातनवादियों द्वारा किए गए ऐसे प्रतिरोध के कारण सुधारवादी खेमा स्वतंत्रता के समय के आसपास ही अधिकार-आधारित दृष्टिकोण के साथ मंदिर प्रवेश कानूनों को लागू करने में सफल रहा, जो पिछली बिना किसी अधिकार के परोपकार की नीति के विपरीत था. उस समय देश में समानता का बोलबाला था, विशेषकर संविधान सभा की समसामयिक कार्यवाही के कारण, जिसने सनातनियों को हाशिए पर धकेल दिया था.
उस छोटी अवधि के दौरान उनका प्रभाव किस हद तक गिर गया था, यह उस असामान्य रणनीति से स्पष्ट था, जो बॉम्बे मंदिर प्रवेश विधेयक पर अपनी आवाज सुनाने के लिए पूना में सनातनियों ने मजबूरअपनाई.
उस विधेयक के अधिनियमित होने की पूर्व संध्या- 10 सितंबर, 1947 को सनातनी हिंदुओं का एक प्रतिनिधिमंडल बॉम्बे सरकार के प्रमुख बीजी खेर से मिला. वे विधानसभा में एक याचिका प्रस्तुत करना चाहते थे ‘लेकिन उन्हें ऐसा एक भी सदस्य नहीं मिला जो यह करने को तैयार होता.’
उस समय की टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि इस बात का खुलासा अगले दिन सदन में खेर ने सनातनी याचिका को फॉरवर्ड करते समय किया, जब उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से यह डिस्क्लेमर भी दिया कि ‘वह याचिका के विचारों से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते.’
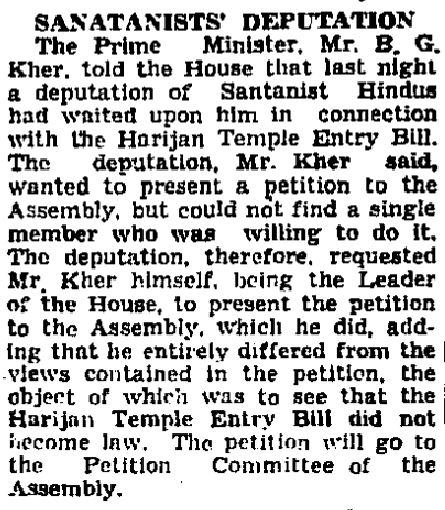
अख़बार की यही रिपोर्ट खेर के वक्तव्य पर कहती है: ‘उन सनातनियों, जो नहीं चाहते थे कि सरकार धर्म में हस्तक्षेप करे, को जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि उनके मन में कोई संदेह नहीं था कि इतने बड़े वर्ग को हरिजन के तौर पर समाज से बाहर रखना और उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना जैसा सदियों से उनके साथ किया जाता रहा है, अधर्म है.’
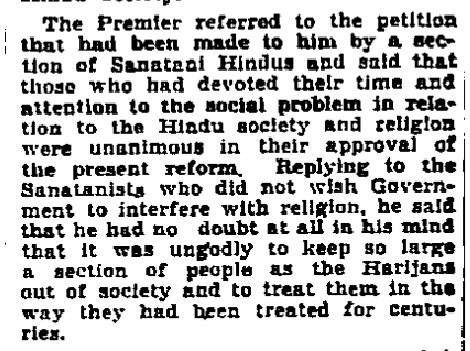
विधानसभा में विधेयक को रोकने में अपनी विफलता से अप्रभावित सनातनवादियों ने अपना ध्यान बॉम्बे विधान परिषद की ओर केंद्रित किया. 18 अक्टूबर, 1947 को वर्णाश्रम स्वराज्य संघ के सदस्यों ने काउंसिल हॉल में घुसकर विधेयक को खारिज करने की मांग की. उनकी हताशा इतनी थी कि उन्होंने जाति प्रतिबंध पर कानून की तुलना पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ विभाजन के समय हुई हिंसा से की.
टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर कहती है, ‘सनातनियों के नेता पंडित अन्ना शास्त्री उपाध्याय ने हाथ जोड़कर कहा कि भारत में सरकार रूढ़िवादी हिंदुओं के साथ उसी तरह का बर्ताव कर रही है जैसे पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ किया जा रहा है.’
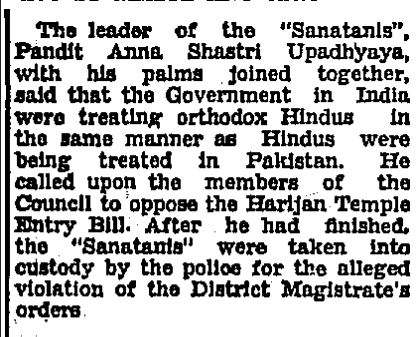
हिंदू सामाजिक संरचना में किसी भी बदलाव का विरोध करने वाली विचारधारा के रूप में सनातन धर्म की अवधारणा न केवल राजनीतिक चर्चा में थी, बल्कि देश के भी दर्ज हुई है.
वाराणसी के सबसे पवित्र माने जाने वाले काशी विश्वनाथ मंदिर में दलितों के प्रवेश के सनातनी विरोध पर 1954 के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को ही लें. विवाद इस बात पर था कि संयुक्त प्रांत के 1947 के मंदिर प्रवेश कानून के तहत जब दलित अंततः 17 फरवरी, 1954 को काशी विश्वनाथ मंदिर जाने पर अपने इस अधिकार को अमल में लाने की हिम्मत कर सके, तब क्या उन्हें काशी विश्वनाथ के मुख्य प्रवेश द्वार- सिंहद्वार से प्रवेश करने की अनुमति थी.
जहां सनातनवादियों ने दावा किया कि दलितों को ‘मुख्य द्वार से प्रवेश करने से नहीं रोका गया’ था; वहीं राज्य सरकार ने दावा किया कि उन्हें ‘सिंहद्वार के माध्यम से प्रवेश करने से मना कर दिया गया था.’ शपथ लेकर दिए गए परस्पर विरोधी बयानों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने पाया था कि ‘हरिजन, निर्बाध रूप से मुख्य द्वार से प्रवेश नहीं कर सकते थे… क्योंकि सनातनवादी… उनके प्रवेश में बाधा डालने के लिए घटनास्थल पर मौजूद थे.’
(मनोज मित्ता वरिष्ठ पत्रकार हैं. उन्होंने हाल ही में भारत में जाति और समानता को लेकर ‘कास्ट प्राइड’ नाम की किताब लिखी है.
(इस लेख अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.)




