एक सरकारी नौकरी को पाने के लिए लाखों लाख युवा अपनी युवावस्था, अपनी उत्पादकता के सबसे चरम वर्षों को जिस पूरी यंत्रणा से गुज़ारते हैं, क्या वह वाकई ज़रूरी है?

फिल्म 12th फेल को लेकर अभी कई प्रतिक्रियाएं हुईं. होनी भी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी को लेकर सिनेमा बनाना एक ऐसे देश में जहां इस परीक्षा को लगभग राष्ट्रीय स्वप्न समझ जाता है, है तो वाकई हिम्मत का काम. हिम्मत इसीलिए कि यूपीएससी की छवि को भी इतनी ही प्रामाणिकता से दिखलाना है तो इस परीक्षा की तैयारी करने वाले लाखों युवाओं के संघर्ष के प्रति भी ईमानदारी रखनी थी. ऐसे में सिनेमेटिक लिबर्टी का प्रयोग बिल्कुल किया जा सकता है, पर 12th फेल इस आज़ादी का बहुत हद तक दुरुपयोग करती नहीं दिखती.
युवाओं की जनसंख्या में भागीदारी को देखते हुए भारत को एक युवा राष्ट्र माना जाता है और इसीलिए जब बात इतनी बड़ी जनसंख्या के सपनों और संघर्षों की होती है, तब प्रायः हम उससे जुड़ाव महसूस कर लेते हैं. 12th फेल यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के तैयारी के संघर्ष को, इस तैयारी के पूरे दुश्चक्र को अपनी विषयवस्तु बनाती है और यह चित्रण बहुत हद तक विश्वसनीय है. पर इस लेख को लिखने का उद्देश्य फिल्म की समीक्षा करना नहीं हैं, बल्कि हमारे इस राष्ट्रीय जुनून की समीक्षा करना है.
इतनी बड़ी आबादी वाले देश में अगर औसतन बात की जाए तो हर साल लाखों लोग इस परीक्षा का आवेदन भरते हैं. अभी साल 2023 में ही, महज़ 1105 रिक्तियों के लिए दस लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था. जितनी बेसब्री और तृषित आंखों से यूपीएससी के नोटिफिकेशन की प्रतीक्षा की जाती है, वह यह दिखलाता है कि कैसे असल परीक्षा तो इस सूचना के साथ ही शुरू हो जाती है. दिल्ली के कोचिंग संस्थान ही नहीं, बल्कि मुखर्जी नगर, करोल बाग जैसे तैयारी के मठों में किराये पर कमरा देने वाले मकान मालिकों में भी उत्साह की लहर दौड़ जाती है कि अब बस विद्यार्थियों का रेला उमड़ता हुआ उनके वीरानों को आबाद करेगा.
फॉर्म भरने के भी अपने गणितीय समीकरण हैं. कौन कितनी जल्दी प्रारंभिक परीक्षा के फ़ॉर्म भर ले, ताकि मनचाहा परीक्षा केंद्र मिल सके, घर के नज़दीक केंद्र हुआ तो दो पर्चों के बीच वाले समय में कमरे आकर पढ़ाई कर सकें, यह सब भी प्रतियोगिता का ही एक हिस्सा है. हमारे अंधविश्वासों और मान्यताओं से भरे सामाजिक संदर्भों में तो फ़ॉर्म भरने के दिन भी अच्छे से ग्रह-नक्षत्र देखकर के भरे जाते हैं ताकि क़िस्मत अपना वरदहस्त बनाए रखे.
इसीलिए यह फिल्म उन तमाम विद्यार्थियों को संबोधित करती है, जिन्हें अभ्यर्थी या aspirants कहा जाता है क्योंकि वे इस दुर्गम परीक्षा में विजयी हो जाने की महज़ इच्छा नहीं, महत्वाकांक्षा रखते हैं. पर इस सिनेमा के बहाने हम इस महत्वाकांक्षा के औचित्य पर ही नहीं बल्कि एक व्यापक स्तर पर उस सामाजिक परिवेश पर विचार करेंगे जहां ऐसी महत्वाकांक्षाओं का जन्म होता है. जहां सरकारी नौकरी का आकर्षण इतना प्रबल होता है कि तैयारी भले एक अभ्यर्थी की हो पर उसके साथ पूरे परिवार, समाज और जाति की आकांक्षाएं जुड़ जाती हैं.
मनोज शर्मा के बनने में भी सिर्फ उनका अपना संघर्ष नहीं बल्कि पिता की ग़ैरमौजूदगी में पूरा घर अकेले संभालती मां की व्यथा भी थी, दूर दिहाड़ी पर काम करने चले गए भाई का भी संघर्ष था और समय से पहले ज़िम्मेदार हो गई बहन भी थी, जिसकी आकांक्षा भी अपने भाई को बड़ा अफसर बनता देखने की थी.
सरकारी नौकरी और उसमें भी देश की सबसे सर्वोच्च नौकरी के लिए हमारी राष्ट्रीय लालसा का जन्म, उच्च पद, सामाजिक प्रतिष्ठा, पारिवारिक गौरव इन सब के वृत्त में होता है. एक ऐसा सामाजिक-आर्थिक पारिस्थितिकी तंत्र, जहां परिवार, जाति, समाज, गांव-शहर, सब इस परीक्षा को शक्ति और प्रतिष्ठा से जोड़कर अपनी सांस्कृतिक समृद्धि और आर्थिक गतिशीलता का सबसे बड़ा ज़रिया मानते हैं. विशेषकर निम्न और मध्य वर्ग, जिनके पास पैतृक संपत्ति और सांस्कृतिक पूंजी जैसे शब्दों से मिलने वाली ताकत नहीं होती, उन्हें यूपीएससी के द्वारा राज्य के सर्वोच्च सरकारी तंत्र का एक उपकरण बनकर शक्ति के गलियारे से संबंध जोड़ लेना किसी दिवास्वप्न के पूरे हो जाने से कम नहीं लगता.
इसीलिए यह फिल्म जो एक व्यक्ति के वास्तविक अनुभवों पर आधारित है, उस व्यक्ति के संघर्ष द्वारा सब का नहीं भी तो एक बड़ी आबादी के हिस्से का सच अवश्य दिखलाती है. पर हां, जैसा कि कवि अज्ञेय कहते थे ‘जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो’, यह सच हर अभ्यर्थी का सच नहीं है न ही सब की कहानी ही एक-सी होती है, पर इस तरह की सिनेमा से इस सामाजिक मानसिकता की जड़ों और यूपीएससी के व्यवसायीकरण पर विचार करने का अवसर ज़रूर मिलता है.
एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि यह बड़ी आबादी जिन्हें यूपीएससी में अपने जीवन, अपने परिवार, अपनी जाति की सार्थकता नज़र आती है, उन्हें इस नौकरी के बाद की वास्तविकताओं का कितना पता होता है या बस लाल बत्ती जैसे रूपकों से प्रभावित होकर वह एक भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं? सवाल यह भी है कि वास्तविक रूप में इस नौकरी से उनकी अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं का कितना मेल हो पाता है?
इस फिल्म में भी ऐसे पात्र हैं, जैसे प्रीतम पांडे, जो अपने पिता के दबाव से यह परीक्षा देने के लिए बाध्य होते हैं. उनका बस चले तो वह कुछ और करना पसंद करते जो वाकई उनके व्यक्तित्व और क्षमता के अनुरूप है. हालांकि इस लेख में हमारी चिंता उन तमाम अभ्यर्थियों या इस सिनेमा के मुख्य पात्र मनोज शर्मा जैसे युवाओं से है, जो इस दिन-ब-दिन कठिनतम और अप्रत्याशित होती जा रही प्रतियोगिता को अन्य सभी नौकरियों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ मान कर साल-दर-साल इसकी तैयारी में झुलसते रहते हैं. अपनी युवावस्था के कई ऊर्जावान वर्ष एक सरकारी नौकरी के स्वप्न में आहुति दे देते हैं.

आईएएस, आईपीएस बनने का सपना उनमें किसी भी कठिन परिस्थिति में रहकर उस वक़्त को काट लेने की जिजीविषा भर देता है, क्योंकि अगर इस परीक्षा में वह सफल हो गए तो फिर हर कष्ट, हर भोगी गई यातना क्षम्य और मूल्यवान है. परिवार, पास-पड़ोस, निकट या दूर के संबधियों द्वारा की गई छींटाकशी, बेरोजगारी पर दिया गया ताना, सब कुछ उस एक उम्मीद पर हंसते-हंसते ग्रहण कर लिया जाता है जब वह अपना नाम सफ़ल हुए अभ्यर्थियों की सूची में देखेंगे.
पर यह परीक्षा सिर्फ मेहनत, लगन, रणनीतिक तैयारी से ही निकलती हो यह नहीं कहा जा सकता. संभवतः कई और चीजें जिन्हें समझाया नहीं जा सकता या जिसे हम भाग्य या प्रारब्ध कहते हैं, वह भी पृष्ठभूमि में अपना काम करती हैं. कुछ नियति की भी बात है. कुछ सितारों के एक सीध में होने का मामला भी है. इस फिल्म में भी मनोज शर्मा के साथ नियति अपना खेल खेलती है, मसलन कि जब वह पुलिस अफसर बनने का ठानते हैं, उसी साल राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं स्थगित हो जाती हैं और इस प्रकार उन्हें ऑल इंडिया सर्विसेज़ का पता चलता है. या स्टेशन पर मनोज शर्मा का एक ऐसे दोस्त, प्रीतम पांडे, से मिल जाना जो उन्हें दिल्ली लेकर आता है या फिर दिल्ली में गौरी भैया जैसे फ्रेंड, फिलासफर, गाइड का मिल जाना, जो उन्हें हमेशा प्रेरणा देते हैं.
पर यहीं पर एक सामान्य-सी उत्सुकता मन में उठती है कि एक सरकारी नौकरी को पाने के लिए ये लाखों लाख युवा अपनी युवावस्था के, अपनी उत्पादकता के सबसे चरम वर्षों को जिस पूरी यंत्रणा से गुज़ारते हैं, क्या वह वाकई ज़रूरी है?
अमूमन इस प्रश्न पर सब की अलग-अलग राय होती है और होनी भी चाहिए. पर जैसा कि मनोज कुमार शर्मा अपने साक्षात्कार में फिल्म में जब यह कहते हैं कि परीक्षा न हो पाने पर वह वापस अपने गांव जाकर स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे और तब भी वह देश की सेवा कर सकेंगे, तो यह वाकई हमें सोचने को बाध्य करता है कि अपनी ऊर्जा को साल-दर-साल इस परीक्षा के चक्र में झोंकते रहने और प्रायः असफल होकर अवसादग्रस्त और निराश होते रहने से क्या यह कहीं बेहतर नहीं है कि हम अलग-अलग तरीकों से अपने समय और समाज के लिए कुछ करने के स्वप्न को पूरा करें?
बहरहाल, फिल्म में जिस प्रकार मनोज शर्मा को दिल्ली में मुखर्जी नगर पहुंचकरपरीक्षा की तैयारी करते हुए दिखलाया है वह लाखों युवाओं का सच है. हां, लाख ऐसे भी हैं जिनके पास दिल्ली आकर, मुखर्जी नगर या राजेंद्र नगर में तैयारी करने के लिए न तो सहूलियत है और न ही संसाधन, और वो अपने घरों पर रहकर ही इस परीक्षा की तैयारी करते हैं. पर जो दिल्ली आकर कोचिंग संस्थाओं, कबूतर के दड़बों जैसे पीजी और विद्यार्थियों के रेले के त्रिकोण पर खड़े हो कर इस परीक्षा को देने का हौसला रखते हैं उनकी स्थिति वाकई अलग होती है. अपने रहने-खाने की जिम्मेदारी खुद उठा कर कोचिंग संस्थाओं के चकाचौंध को झेल पाना आम बात नहीं है.
इन सरकारी नौकरियों की प्रतियोगी परीक्षाओं की वजह से जो एक समानांतर-चक्रीय अर्थव्यवस्था बन जाती है उसमें एक प्रमुख भूमिका है, मुखर्जी नगर, करोल बाग़, राजेंद्र नगर जैसे इलाकों में अपने पुरखों के बनाए घरों से अपने आने वाली नस्लों का भाग्य संवारते मकान मालिकों की. कैसे भी घर क्यों न हो, उसे पेइंग गेस्ट कमरों की शक्ल देकर एक-एक बिस्तर के हिसाब से दिल्ली जैसे महानगरों में मकान मालिक जिस प्रकार युगों से अपनी संपत्ति को दो दूना चार करते जा रहे हैं वह अद्भुत है. यह एक ऐसी दबी-छुपी व्यवस्था है जिस पर कोई सवाल नहीं उठाता है.
मनमाफ़िक किराया वसूलने वाले मकान मालिक, इन परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने की ज़रूरत, मजबूरी और जुनून से लाभान्वित होने वाले सबसे बड़े खिलाड़ी हैं. छोटे-छोटे शहरों से, दूर-दराज़ के गांवों से आए विद्यार्थी की पहली समस्या घर की ही होती है, इस बात को कोचिंग संस्थान वाले भी बखूबी इस्तेमाल करते हैं. प्रॉपर्टी डीलरों के साथ मिलीभगत कर अपने संस्थान आए विद्यार्थियों की उनकी हैसियत का घर मुहैया करा देने का साइड बिज़नेस भी खूब चलाते हैं.
इस पूरी प्रक्रिया में भी मनोविज्ञान का ख़ासा प्रयोग होता है. लड़के तो कहीं भी रह लेंगे, उनके लिए अच्छे, सुरक्षित, समृद्ध इलाकों की उतनी दरकार नहीं होगी पर लड़कियां, जिनमें से कई तो पहली बार घर के बाहर कदम रख रही होती हैं, उनके माता पिता को सुरक्षा, सेफ़्टी, सहूलियत इत्यादि का झांसा देकर महंगे पीजी भी, जिन्हें मकान मालिकों को निकालना आम तौर पर मुश्किल होता है, मुंहमांगी कीमतों पर दिलवा देते हैं. बेचारे मां-बाप भी सरकारी नौकरी के इंद्रधनुषी मोहजाल में फंसे कुछ भी करने को तैयार रहते हैं.
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के इन गढ़ों में घरों की हालत देखने लायक है. एक-एक कमरे में जहां दो लोग बमुश्किल रह सकते हैं, वहां आठ-आठ के रहने की व्यवस्था कर दी जाती है. फ़ाइबर के पार्टिशन डालकर सिंगल सीटर कमरे कबूतर के दड़बों की मानिंद लगते हैं.
बहरहाल, मुखर्जी नगर में जहां चप्पे-चप्पे पर यूपीएससी ‘क्रैक’ करवा देने के दावों के साथ संस्थानों के छोटे-बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं, ऐसे में अपनी परिवार की जमापूंजी को फीस के नाम पर लुटा देना बड़े हिम्मत की मांग करता है. कोचिंग संस्थानों की फीस वाकई एक बड़ा मसला है. जो अब दशकों से इस महायुद्ध के खिलाड़ी हैं, वह मुंहमांगी फीस रखते हैं तो केवल इसलिए क्योंकि अब उनका नाम ही ब्रांड है. अपने विज्ञापनों पर वह इतना खर्च करते हैं कि दूर-दराज़ के गांव में भी इनकी लोकप्रियता रहती है और छात्र सीधा इनके ही दरवाज़े पर रुकते हैं.

और एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि जैसा कि हम प्रायः ब्रांड के साथ देखते हैं, जहां रिबोक के जूते रीबूक हो जाते हैं, इन संस्थानों के भी नकली संस्करण निकल पड़ते हैं. मसलन वाजीराम जैसे संस्थान के सालों के अनुभव और सफलता के तथाकथित ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए वाजीराव नाम से नए संस्थान का खुल जाना आम बात है और दिग्भ्रमित होकर छात्र इनमें दाखिला भी ले लेते हैं. और सबसे मजेदार वाकया यह कि हर संस्थान अपने आप को दूसरे से श्रेष्ठ घोषित करने के लिए पिछले सालों के टॉपरों को अपने संस्थान का दिखला कर बेवकूफ बनाते हैं.
फिल्म में इस तथ्य को जिस व्यंग्यात्मकता से दिखलाया गया है वह मार्के का है. कैसे इन तथाकथित टॉपरों को कुछ बड़ी रकम देकर अपने संस्थान का चेहरा बना दिया जाता है, वह भारत जैसे विकासशील देश के रगों में घर कर गए भ्रष्टाचार की बानगी है. अगर एक सफ़ल अभ्यर्थी के चेहरे खरीदने के लिए उन्हें कुछ पैसे देने भी पड़ रहे हैं तो उससे कहीं ज़्यादा कमाई वो उन सफ़ल चेहरों के नाम पर संस्थान में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों से कर लेंगे. कहीं-न-कहीं यह एक छोटी सी झांकी भी है कि कैसे इन सफ़ल हुए अभ्यर्थियों के आत्म मूल्य को, उनकी सफलता को महान बतलाकर उनकी चापलूसी की शैशव शुरुआत हो जाती है. फिल्म ने इस पूरे वाकये को बड़े ही प्रभावी ढंग से दिखलाया है.
जिस तरह से फिल्म में मनोज की दादी, जीवन की जमापूंजी अपने पोते के सरकारी अफसर बनने के स्वप्न पर थमाती हैं, वह वाकई में बहुतों का सच है. लोग अपनी ज़मीन-खेत बेचकर इस जुए में दांव लगाने आते हैं. हर किसी के पास इन कोचिंग संस्थानों की भारी भरकम फीस देने की कूवत नहीं होती और फिर कई ऐसे हथकंडे अपनाए जाते हैं जहां इनका विकल्प निकाला जाता है. चाहे वह मुखर्जी नगर में क़तार से लगी दुकानों में बिकते हुए फोटो कॉपी नोट्स हों जो किसी संस्थान के विद्यार्थी ने सबके लिए रखवा दिए हों, या अपने सीनियरों के पुराने नोट्स.
कहने का अर्थ यह कि परीक्षा पास कर पाने का लोभ कब जुनून बन जाता है यह ठीक से कहा नहीं जाता. इसके लिए जो कुछ भी बन पाए कर गुज़रना आम बात है. फिल्म में मनोज शर्मा जिस तरह से कहीं भी रहकर, कठिन-से-कठिन परिस्थितियों में रहकर बस इस परीक्षा को निकालने की धुन में रहते हैं, वह एकदम विश्वसनीय है, हां हर किसी को उनकी तरह आटा चक्की नहीं चलाना पड़ता हो पर देखा जाए तो वह एक रूपक ही है अभ्यर्थियों का मानसिक रूप से इस परीक्षा के चक्र में पिसते रहने का.
हालांकि कई संस्थान ऐसे भी हैं जो आज भी इन अतिशय व्यावसायिकता के दौर में स्वयं को छोटे स्केल पर रखकर अपने अभ्यर्थियों की पूरी यात्रा में व्यक्तिगत रूप से शामिल रहते हैं. पर व्यावसायिकता का दबाव कह लें या सफलता प्रेमी हमारी उपभोक्ता संस्कृति, कोचिंग इंडस्ट्री जिस तेजी से अपने अभ्यर्थियों को रातों-रात सुपरस्टार के ख़िताब से नवाजती है, उनकी सफलताओं को भुनाती है तो, वहीं अगले साल नए चेहरों पर अपना दावा क़ाबिज़ करती नज़र आती है.
इसलिए यूपीएससी की तैयारी जो एक व्यवसाय में बदल गई है, यह इस फिल्म की समस्या नहीं बल्कि देश में बढ़ती बेरोज़गारी की जड़ों को समझने की एक कुंजी होनी चाहिए. अभी जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने कोचिंग संस्थानों को विद्यार्थियों को भ्रमित करने के गलत दावे किए जाने संबंधी आदेश जारी किए हैं वह इस दिशा में एक सराहनीय प्रयास है.
हालांकि इस जुए जैसी परीक्षा में सफलता और असफलता के बीच की रेखा इतनी महीन होती है कि कोई भी परिणाम किसी की योग्यता-अयोग्यता को सिद्ध करने में नाकाफ़ी है.
बहरहाल, इतने सर्वोच्च सरकारी नौकरी में चयनित हो जाने की लालसा रखना गलत नहीं है. पर इस लालसा के नाम पर अपनी क्षमताओं का भी आकलन जरूरी है. वैसे भी यूपीएससी की परीक्षा जो किसी भी दृष्टि से विशेषज्ञता की अपेक्षा नहीं रखती अंततः एक सामान्य स्तर पर चयन करने की प्रक्रिया रखती है. ऐसे में जितनी वस्तुनिष्ठता लाई जा सकती है वह प्रारंभिक चरण जिसे प्रिलिम्स (prelims) कहते हैं उसमें रखी जाती है. एक ऐप्टिट्यूड का प्रश्न पत्र और एक सामान्य अध्ययन का, जिसमें निगेटिव मार्किंग की योजना रहती है, वह केवल लालसा रखने वालों की बाढ़ को काफी हद तक थाम लेती है.
कट ऑफ मार्क्स को अधिकांश अभ्यर्थी नहीं क्रॉस कर पाते हैं जो उनके सपनों पर पहले ही लगाम लगा देता है. पर इस सिक्के के भी दो पहलू हैं, जो इस चरण को पार कर लेते हैं वह अच्छे हैं इसकी कोई गारंटी नहीं होती. वैकल्पिक प्रश्नों में अगर स्मरणशक्ति और विकल्प चुन लेने की योग्यता उस नियत दिन काम कर जाती है तो बहुत संभव है कि औसत-से-औसत विद्यार्थी भी यह चरण निकाल लें. और जो कुछ दुर्भाग्य के मारे विकल्पों में सही उत्तर नहीं छांट पाते, लाख योग्य विद्यार्थी होते हुए भी अगले चरण के लिए नहीं जा पाते. इसीलिए वस्तुनिष्ठता की भलमनसाहत रहते हुए भी परीक्षा इतने सारे अन्य कारकों पर निर्भर करने लगती है कि यह परीक्षा, परीक्षा कम बल्कि एक जुआ ज्यादा लगती है.
परीक्षा का अगला चरण, जिसे मुख्य परीक्षा या मेंस (Mains) कहा जाता है, जहां पांच दिनों तक दो-दो पालियों में नौ प्रश्नपत्रों के उत्तर हल किए जाते हैं, वह सही मायनों में धैर्य और जुझारूपन की परीक्षा है. यह वस्तुनिष्ठ न भी सही पर जिस तरह से अब अधिकांश अभ्यर्थी इंजीनीयरिंग पृष्ठभूमि से आते हैं, मुख्य परीक्षा को भी एक कोड की तरह क्रैक कर लेना चाहते हैं. कुछ बंधे-बंधाए फॉर्मूला- 8 से 9 मिनटों में एक प्रश्न को लिख पाने का गणितीय आकलन, वस्तुनिष्ठ तरीकों से उत्तर को कम से कम में गागर में सागर भरने की तकनीक से लिखना, ज्यादा से ज़्यादा फ़्लो चार्ट, ग्राफ, मानचित्र, स्केच इत्यादि के माध्यम से आकर्षक प्रस्तुति- यह सब कमोबेश हर गंभीर अभ्यर्थी जान चुका होता है.
और इस पर से भी कमाल यह कि अभी तक अपने क्षेत्र या अपनी पसंद के ऑप्शनल विषय रखने के समय भी अक्सर विशेषज्ञता जैसी वजूहातों को ताक पर रखकर, उस विषय को चुनने पर बल दिया जाता जिसमें अधिकतम नंबर लाए जा सके. इसीलिए ऐस्ट्रोफिज़िक्स की विशषज्ञता रखने वाले या मेडिकल के छात्र मैथिली या पाली विषय ऑप्शनल के तौर पर जब लेते हैं तो यूपीएससी के चयनकर्ताओं की सारी तैयारी धरी-की-धरी रह जाती हैं.
इसीलिए परीक्षा जिसे दिन-ब-दिन अधिक सामान्य बनाया जा रहा है, उसमें भले ही पूरे देश के छात्रों को एक समरूपी प्लेटफॉर्म देने की समावेशी दृष्टि आयोग के तरफ से दिखलाई पड़ती हो, पर उसे अब प्रायः वही उत्तीर्ण कर पा रहे हैं जो इस ऊपर कही गई चालाकियों और फॉर्मूले को सबसे अधिक बहुगुणित कर के इस्तेमाल में ला पाते हैं. कम-से-कम टॉपरों के व्याख्यानों और उनकी सफलता की रणनीतियों का सार तो यही है. उसमें भी भारत जैसे देश में जहां हर किसी को अंग्रेज़ी माध्यम में शिक्षा नहीं मिल सकी है तो अपनी मातृभाषा में या हिंदी में परीक्षा देने के संघर्ष पर तो एक पूरी किताब ही लिखी जा सकती है.
इसीलिए, बहुत सारे सूरमा तो हिंदी अंग्रेजी के चक्रवात में फंसकर ही ढेर हो जाते हैं. प्रारंभिक परीक्षा में सीसैट ( CSAT- सिविल सर्विसेज़ ऐप्टिट्यूड टेस्ट) के इर्द-गिर्द हुआ विरोध इस परीक्षा में अंग्रेज़ी माध्यम के अभ्यर्थियों को मिलने वाली बढ़त या वरीयता के संदर्भ में ही था. इस फिल्म में भी नायक मनोज शर्मा अपने एक प्रयास में इसीलिए असफल रह जाता है क्योंकि वह टेररिज़्म और टूरिज़्म का फ़र्क नहीं समझ पाता और टूरिज़्म के स्थान पर टेररिज़्म पर निबंध लिख देता है.
पर, जैसा कि ऊपर कहा सारा शोर सिर्फ सफ़ल हुए अभ्यर्थी के आस-पास हो कर रह जाता पर एक बड़ा हिस्सा जो इस परीक्षा को अंततः नहीं निकाल पाता उनकी ज़िंदगी भी चलती ही है. कुछ राज्य के पीसीएस इत्यादि परीक्षाओं में विजयी हो जाते हैं जैसा कि फिल्म में श्रद्धा जोशी के साथ होते दिखलाया गया है या कई अन्य वह करने के लिए तकनीकी रूप से मुक्त हो जाते हैं जो वह वाकई करना चाहते थे जैसा कि प्रीतम पांडे के साथ होता है.
पर एक वर्ग और भी है जो परीक्षा को न निकाल पाने पर भी इस परीक्षा के इंद्रजाल से नहीं निकल पाता. उनमें से कइयों के लिए अपने जीवन की उत्तरोत्तर सार्थकता इसी परीक्षा के मेंटर-शिक्षक बन जाने में दिखती है. अभ्यर्थियों की नई खेप को अपने अनुभवों और सीखे हुए पाठों से इस परीक्षा की अप्रत्याशित नवीनता के लिए तैयार करना उनके जीवन का ध्येय बन जाता है. कुछ वाकई बहुत सधे हुए शिक्षक भी सिद्ध होते हैं और लगता है कि उनका मार्गदर्शन इस परीक्षा को थोड़ा आसान कर सकता है.
इस फिल्म में भी जब यूपीएससी कोचिंग जगत और समकालीन सोशल मीडिया के चहेते मेंटर विकास दिव्ययकीर्ति छात्रों से भरी कक्षा को संबोधित करते हैं, तो मनोज जैसे हजारों युवाओं को अपनी दृष्टि और इस परीक्षा के प्रति एक सार्थक नज़रिये से प्रभावित करते हैं. पर हर कोई ऐसा नहीं बन पाता. बढ़ती बेरोज़गारी के आलम में ऐसा भी प्रायः ही होता है कि कई कोचिंग अर्थव्यवस्था में बस कॉग इन द ह्वील बनकर अलग-अलग क्षमताओं में काम करने लगते हैं. बड़े-बड़े कोचिंग संस्थान छात्रों से मोटी फीस वसूलते हैं और जिन मेंटरों के बदौलत यह पूरा कारोबार खड़ा किया जाता है उन्हें भी प्रायः अच्छी तनख्वाह देते हैं. इस मोटी तनख्वाह का आकर्षण इतना प्रबल होता है कि कई बार यूपीएससी में निचली रैंकों से पाई गई नौकरियों को छोड़कर वह कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने आ जाते हैं.
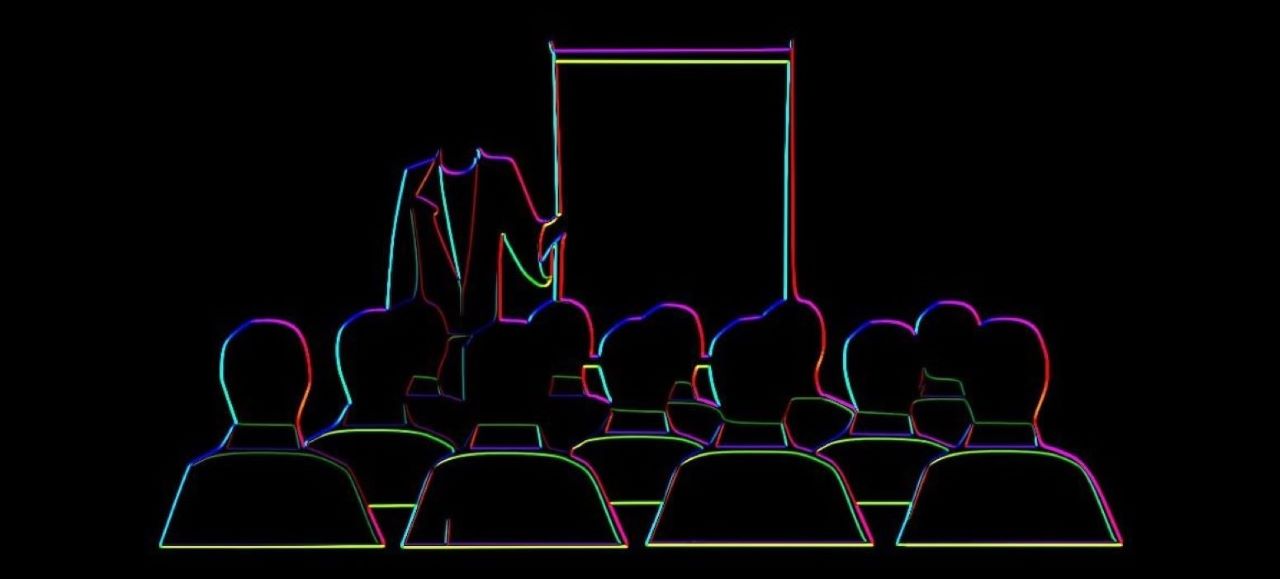
इस प्रकार यह पूरी अर्थव्यवस्था चक्रीय हो कर रह जाती है और मांग व आपूर्ति के नियम पर बदस्तूर बनी रहती है. हर साल जितनी तेजी से नए-नए स्नातक हुए छात्रों (इस परीक्षा के लिए न्यूनतम वरीयता) की लहर पिछली लहर में जुड़ती जाती है तो वहीं हर रोज़ कोई नया शिक्षक, किसी नए संस्थान के होर्डिंग्स के साथ पर सफलता की पैसा वसूल गारंटी के वादों के साथ उगा हुआ दिखता है.
कोई वजह है कि सालों से मुखर्जी नगर, करोल बाग, ओल्ड राजेंद्र नगर अपने आड़े-तिरछे होर्डिंग बोर्डस, तंग सड़कों के इर्द-गिर्द खड़ी की गई किताबों की दुकानों और छात्रों की टूट पड़ती हुई भीड़ के अतिरिक्त और कुछ नज़र नहीं आते. छात्रों की पीढ़ियां बदलती हैं, पर इन जगहों के हुलिये ज्यों के त्यों हैं.
प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा तक यूपीएससी की तैयारी करने वाले सिर्फ एक भीड़ हैं- अनाम, अदृश, निराकार भीड़. यह इस परीक्षा का अंतिम चरण यानी साक्षात्कार है जब यह बिना रूप-आकार वाली भीड़ रातों रात चंद अभ्यर्थियों के नामों और चेहरों में बदल जाती है. सब भावी प्रशासक बनने का सपना आंखों में लिए बस आखिरी चरण की तैयारी में लग पड़ते हैं. मंजिल अब दूर नहीं – यह भाव लिए कई जो अपने-अपने घरों से इस खेल को खेल रहे थे, अब साक्षात रणक्षेत्र में पहुंच जाना चाहते हैं. दिल्ली के कोचिंग संस्थानों के लिए यह अलग ही सावन का महीना होता है. चप्पे-चप्पे पर अंतिम संग्राम से पहले की तैयारी के लिए मॉक ड्रिल करने के इश्तिहार लगे रहते हैं.
इस फिल्म में जिस तरह से साक्षात्कार के लिए यूपीएससी भवन में अभ्यर्थियों का जाना दिखलाया गया है, वह ठीक उस वक़्त उनके मन में चलने वाले द्वंद्वों को थोड़ा बहुत दिखला पाता है. अब तक जिस ग़ुमनामी में इस परीक्षा के सभी चरणों को दिया जा रहा था, जहां परीक्षा के पर्चे में होने वाली ग़लतियों के माफ हो जाने की थोड़ी बहुत गुंजाइश थी, जहां अभी तक बस आपके लिखने-पढ़ने की क्षमता के आधार पर आंका जा रहा था, वहीं अब एक ऐसा चरण है जहां अब कुछ साफ हो जाना है. अब आयोग को वाकई में इस देश के चप्पे-चप्पे को चलाने के लिए प्रशासक चाहिए होते हैं. साक्षात्कार उसकी अंतिम प्रक्रिया है.
इंटरव्यू के लिए चयनित होते ही अभ्यर्थियों को अपने हुलिये का भी खयाल आ जाता है. हर तैयारी का एक प्रोटोकॉल. जिन्होंने कभी थ्री पीस सूट जीवन में पहना नहीं होगा, उन्हें अब वही नायाब कपड़े डाटे आयोग के समक्ष उपस्थित होना होगा. फिल्म में बाल कटवाने के लिए जब आईएएस-आईपीएस हेयर कट की बात की गई है, तो हंसने की बजाय इस पर अफ़सोस व्यक्त करना चाहिए. ऊंची हील की चप्पलों-सैंडल और सलीके से पहनी गई सूती साड़ियों में लड़कियां लाख असहज महसूस करते हुए भी साक्षात्कारकर्ताओं को यह यकीन दिला देना चाहती हैं कि बस उन्हें उनका सबसे क़ाबिल और गंभीर प्रशासक मिल गया. भले ही इन बनावटी लिबासों और गंभीरता का लबादा ओढ़े हुए अभ्यर्थियों को यह भनक तक नहीं लग पाती कि दरअसल उनके कपड़ों को नहीं बल्कि उनके इस अश्वमेध नौकरी के दबाव को झेल पाने की जांच हो रही है.
इस फिल्म में भी साक्षात्कार वाले दिन जिस प्रकार नायक मनोज शर्मा अपने गले पर कसी हुई टाई और पैर काटते हुए चमड़े के जूतों में असहज महसूस कर रह थे, वह तो शारीरिक असहजता थी. इस पूरी प्रक्रिया के तनावपूर्ण माहौल के प्रति मानसिक असजहता कमोबेश सभी अभ्यर्थियों की वास्तविकता है. ऐसा लगता है सब पर साक्षात्कार में अपने अच्छे प्रदर्शन का तनाव कम नहीं होता कि यह एक और चिंता उनके सर पर सवार कर दी जाती है साक्षात्कार बोर्ड के सदस्यों को वह भा सकें. अपने हुलिये से, अपने लहजे से, अपनी शारीरिक भाषा (बॉडी लैंग्वेज) से, अपनी आत्मविश्वास भरी आंखों से- उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त कर सकें कि वह बाकी उम्मीदवारों से बेहतर हैं, कि वह बेहतर प्रशासक सिद्ध हो सकते हैं. हालांकि सिवाय उनके, जिनके पिता या कोई संबंधी प्रशासनिक अधिकारी रहे हों, किसी को इस परीक्षा के निकाल लेने के बाद क्या सब पापड़ बेलने होते हैं दूर-दूर तक अंदेशा भी नहीं होता है.
बहरहाल, फिल्म में जिस प्रकार से इंटरव्यू वाला पूरा प्रकरण फिल्माया गया है वहां अवश्य कुछ सिनेमेटिक लिबर्टी का लाभ लिया गया है. अभ्यर्थी को इस प्रकार बाहर भेजकर वापस बुलाना प्रायः नहीं होता है और जिस तरह से सभी साक्षात्कारकर्ता पूर्वाग्रहों से भरे और थोड़े आक्रामक से लगते हैं वह अमूमन नहीं होता. हालांकि यूपीएससी इंटरव्यू बोर्डस के कई चेयरमैन अपने उग्र और आक्रामक लहजों के लिए, अभ्यर्थी को सन्न कर देने के लिए कुख्यात रहे हैं. पर जो मुख्य बात यहां कहनी है वह यह कि साक्षात्कार इस परीक्षा का अंतिम चरण है, पर सही मायनों में बड़ी ज़िम्मेदारी वाला चरण है.
अब तक थोड़ी बहुत वस्तुनिष्ठता से सिर्फ मेरिट के आधार पर चुनाव हो रहा था पर यहां तक आते-आते, बात अब अभ्यर्थी के सर्वांगीण व्यक्तित्व पर आ जाती है. यहां अब तक झेली गई सभी तकलीफों को, पिछले प्रयासों में मिली असफलताओं के दंश को भुलाकर एक नए सिरे से, आत्मविश्वास से लबरेज़ हो कर अंदर जाना होता है और इस तनाव के साथ की यहां गड़बड़ाने से फिर से सांप-सीढ़ी के खेल की तरह पहले चरण ओर पहुंच जाएंगे, जो फिल्म के एक दृश्य में गौरी भैया अपने अनुयायियों को समझाते हैं.
अंतिम प्रयास में फिल्म में जिस प्रकार मनोज शर्मा को सफलता मिल जाती है उसी प्रकार कई ऐसे अभ्यर्थी हैं, जिन्हें इस परीक्षा के अंतिम प्रयास में सफलता मिलती है, और बहुतेरों को नहीं मिलती है. पर इन दोनों ही प्रकार के लोगों से यह पूरी यात्रा कितना कुछ ले लेती है, इसके व्यक्तिगत-मानसिक-सामाजिक मूल्य पर चर्चा होती रहनी चाहिए. यह सफलता कितने मानसिक-भौतिक संघर्षों के बाद मिलती है, उनकी युवावस्था की ऊर्जा को कितना सोख लेने के बाद मिलती है, इसका आकलन न तो यह परीक्षा लेने वाली संस्था लगा सकती है और न ही इस नौकरी मात्र से अपने परिवार-समाज का नाम होता देखने वाली मानसिकता.
इसलिए यह फिल्म सफलता के लिए चुकाये मूल्यों को तो दिखलाती है, पर बस यहीं तक हर बार रुक जाना सही नहीं है. इन युवाओं का आदर्श कब तक आंखों में ज़िंदा रहता है? ज़मीनी वास्तविकता आदर्शवादी सपनों से कितने अलग होते हैं? या कब वह व्यवस्था की मशीनरी में बस एक पुर्ज़ा बनकर फिट हो जाते हैं? या कई वाक़ई में कुछ अलग और कुछ बेहतर कर पाते हैं?- इस यात्रा को समेटती फिल्में भी बननी चाहिए.
फिल्मों की तरह जीवन भी हैपिली एवर आफ्टर वाले मोड़ पर थमा नहीं रहता. इसलिए ऐसी फिल्में व्यवस्था और व्यक्ति की टकराहट, उसके अपने आस-पास के हालात से समझौता करने या इन सबसे उभरने की वास्तविकता को भी दिखलाए तो हमारे युवाओं को एक समग्र चित्रण देखने को मिलेगा और वो संभवतः अधिक प्रामाणिक होगा. एक ऐसा वर्णन जो संघर्षों का रोमांटिक चित्रण मात्र नहीं, जहां नायक हर हाल में सफ़ल हो ही जाता है, बल्कि असफलताओं को भी स्वीकारने, उनका भी उत्सव मनाने की कहानियां.
(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में शोधार्थी हैं.)




