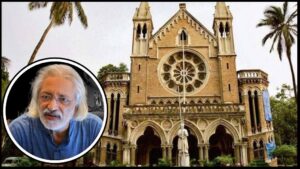बांग्लादेश की आज़ादी के पचास वर्ष होने पर दिसंबर 2021 में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने द टेलीग्राफ में पांच लेखों की श्रृंखला लिखी थी. आज जो हालात बांग्लादेश में है, उसकी आशंका इन लेखों के लिखे जाते वक्त भी थी. 2018 के चुनावों में अवामी लीग को बहुमत मिला था, लेकिन इन चुनावों की निष्पक्षता पर ख़ुद उनके नेताओं ने सवाल खड़े किए थे. बांग्लादेश की वर्तमान राजनीति को समझने में मदद करते ये लेख उसकी आज़ादी में भारत की भूमिका, दोनों देशों में जनतंत्र का स्वरूप और यह एहसास कि यदि एक देश धर्मनिरपेक्षता के रास्ते हो छोड़ता है तो दूसरा भी धर्मनिरपेक्ष नहीं रह सकता, बांग्लादेश की अभूतपूर्व आर्थिक उन्नति जैसे मुद्दों पर केंद्रित हैं.
इन लेखों की प्रासंगिकता को देखते हुए हम शुभेन्द्र त्यागी द्वारा किया इनका अनुवाद प्रकाशित कर रहे हैं.
§
बांग्लादेश की आजादी के 50 वर्ष होने पर ढाका के प्रवास (16- 23 दिसंबर 2021) के दौरान 50 साल पहले न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार सिडनी शैनबर्ग से हुई बातचीत बार-बार मेरे मस्तिष्क में कौंधती रही. ठीक आजादी के दिन यानी, 16 दिसंबर 1971 को मुझे बांग्लादेश में आवश्यक राहत सामग्री को पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई थी, ताकि यह नवोदित देश अपने एक करोड़ शरणार्थियों को पनाह दे सके. आजादी के शुरुआती 9 महीनों में इस जिम्मेदारी ने मुझे बांग्लादेश के भीतर और बाहर अनेक हिस्सों में जाने का अवसर दिया था.
इन यात्राओं की शुरुआत में एक सुबह नाश्ते के दौरान मेरी आकस्मिक मुलाकात सिडनी शैनबर्ग से हुई थी. पाकिस्तान द्वारा अपने ही देश के पूर्वी हिस्से की जनता के ऊपर किए जा रहे भयावह अत्याचारों को पश्चिमी दुनिया के सामने रखने वाले पत्रकारों में उनका नाम अग्रणी था. अपना सिर हिलाते हुए उन्होंने धीरे से कहा, ‘आप लोग यह लड़ाई हार चुके हैं.’ मैं चकित रह गया. कहां मैं अब तक के सबसे बड़े युद्ध में जीत के गर्व में डूबा था और शैनबर्ग कह रहे हैं कि हम हार चुके हैं!
थोड़ा रुककर अपनी बात को समझाते हुए उन्होंने आगे कहा ‘आपकी सेना के जवान यह कहते घूम रहे हैं कि युद्ध भारत की सेना ने जीता है. मुक्तिबाहिनी को उसकी निर्णायक भूमिका के लिए कोई श्रेय नहीं दिया जा रहा, जबकि जीत उनकी वजह से मिली.’
आत्मसमर्पण के समय शैनबर्ग की आशंका सच साबित हुई. भारतीय सेना और मुक्तिबाहिनी के संयुक्त सेनाध्यक्ष होने के कारण लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत अरोरा ने औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण करवाया था.लेकिन वास्तव में मुक्तिबाहिनी के योगदान को स्वीकार नहीं किया गया. (सिर्फ इतना भर किया गया कि मुक्तिबाहिनी के वायु प्रमुख को आधिकारिक फोटो में एक कोने में जगह दे दी गई).
मुक्तिबाहिनी का नेतृत्व करने वाले जनरल (तब कर्नल) एमएजी उस्मानी चाहते थे कि वे आत्मसमर्पण के दौरान मौजूद रहें. लेकिन सेना के कड़े औपचारिक नियमों ने ऐसा नहीं होने दिया. आखिर वे इतने वरिष्ठ तो थे नहीं कि उन्हें भारतीय सेना के जनरलों के समान महत्व दिया जाए. इसकी टीस आज 50 साल बाद भी है.
जहां हम इस बात पर गर्व करते हैं कि तीन महीने में ही हमने अपनी सेना को आजाद बांग्लादेश से वापस बुला लिया, वहीं बांग्लादेश में आज भी यह सवाल पूछे जाते हैं: ‘पाकिस्तान द्वारा समर्पित किए गए हथियारों को भारत ने क्यों हथिया लिया? हमें इनकी जरूरत ज्यादा थी क्योंकि हम अपनी सैन्य शक्ति का निर्माण अभी शुरू ही कर रहे थे.आपने 93,000 पाकिस्तानी युद्धबंदियों को छोड़ देने का फ़ैसला अकेले क्यों किया? इनमें वे 195 सैनिक भी शामिल थे जिन्हे उनके अपराधों और अत्याचारों के लिए हम सज़ा देना चाहते थे. युद्ध के बाद लूट का सारा माल हमसे साझा किए बिना क्यों अपने कब्जे में ले लिया?’ यह भी पूछा जाता है कि
‘आपने 26 मार्च 1971 को ही हस्तक्षेप क्यों नहीं किया,जब हम पर अत्याचारों की शुरुआत हुई, 9 महीनों तक इंतजार क्यों किया? ऐसा करने से लाखों बांग्ला ज़िंदगियां बच जातीं.’
मैं उनकी बातों का खंडन नहीं करता क्योंकि मैं यहां बहस करने नहीं सुनने आया हूं, और हो सके तो उन्हें समझने आया हूं.
बांग्लादेश की 70 फीसदी आबादी 35 वर्ष से कम की है. ऐसे लोग मुश्किल से मिलते हैं, जिन्हें उन गौरवपूर्ण दिनों की याद हो. जिन्हें वे दिन की याद है उनके बाल पक चुके हैं और चलने के लिए लाठी की जरूरत होती है. मुक्तिबाहिनी के सैनिक, जिनमें अनेक युद्ध में घायल हुए थे, गुरिल्ला के रूप में अपनी भूमिका और शहीद हो गए अपने साथियों को संजीदगी से याद करते हैं.लेकिन भारतीय सैनिकों से उनकी ऐसी कोई याद नहीं जुड़ी है.
एक व्यक्ति भारतीय जवानों का पक्ष लेता है, वह हैं कर्नल सज्जाद अली जहीर. वे युद्ध शुरू होने से पहले पाकिस्तानी सेना को छोड़कर आए थे. साथ ही पश्चिम मोर्चे पर पाकिस्तान की तैयारी और रणनीति की सूचनाएं भी लाए थे. अपनी जान को दांव पर लगाकर उन्होंने दुर्गम रास्तों से भारत की सीमा में प्रवेश किया था, और जो रहस्य उन्हें पता थे उनकी जानकारी दी थी. उनकी निस्वार्थ सेवा को पहचानने में भारत को 50 वर्ष लग गए.
उन्हें इसी साल पद्मश्री दिया गया. वे उस दौर की यादों से लबरेज हैं. ‘हम भारतीय सैनिकों को कैसे भूल सकते हैं, हमारी आजादी के लिए जिन्होंने अपनी जान तक दे दी. उनका खून पद्मा, तीस्ता, जमुना और मेघना के पानी में मिला हुआ है.’ लेकिन दूसरी प्रतिक्रियाएं इतनी उदार नहीं हैं, ‘आप पाकिस्तान को बांटना चाहते थे हम पाकिस्तान के जुल्मों से आजाद होना चाहते थे. दोनो के लक्ष्य मिल गए, बस इतनी सी बात है.’
वहीं दूसरी ओर शेख हसीना की सरकार के एक प्रमुख प्रवक्ता जोर देकर कहते हैं कि भारत (और इंदिरा) बांग्लादेश की स्मृति में गहरे बसा हुआ है, कारण: वे लाखों बांग्लादेशी शरणार्थियों की तब तक मदद करते रहे जब तक वे अपने मुल्क सुरक्षित न लौट आए, उनका वह समर्थन जो उन्होंने मुजीबनगर की अस्थाई सरकार को दिया गया; पाकिस्तान की जेल में बंगबंधु की सुरक्षा के लिए किए गए उनके अथक प्रयास. जीत के बाद इंदिरा गांधी को ‘मां दुर्गा’ कहने वाली अटल बिहारी वाजपेयी का भी बांग्लादेशी अनुमोदन करते हैं .
मुझे बांग्लादेश के आधिकारिक स्रोतों ने बताया कि राय यह है कि ‘सार्वजनिक रूप से आजादी में भारत के योगदान को स्वीकार किया जाए’ और ‘आभार भी जताया’ जाए.लेकिन साधारण जनता और बुद्धिजीवियों की राय अलग है. उनकी राय ज्यादा सीमित और संशयात्मक है. आक्रोश हमेशा कृतज्ञता से अधिक दीर्घजीवी होता है.
मुझे लगता है कि संदेह और प्रशंसा के इन दोनों ही नजरियों में सच्चाई है. आजादी का जश्न मनाना तो समझदारी है लेकिन उससे चिपके रहना ठीक नही.
आजादी के आंदोलन के प्रमुख नेता और मुजीबनगर की अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने वाले जिनमे शेख मुजीबुर्रहमान से लेकर अस्थाई राष्ट्रपति सैयद नूरुल इस्लाम, अस्थाई प्रधानमंत्री ताजुद्दीन अहमद और उस कैबिनेट में रहे मंत्री कैप्टन मंसूर अली और कमर जमान, अब जीवित नहीं हैं. अधिकांश की हत्या आज़ादी के चार वर्ष के भीतर उनकी सेना द्वारा कर दी गई. (जिसकी ट्रेनिंग पाकिस्तान में हुई थी और पाकिस्तान की सेना की तानाशाही प्रवृत्तियां जिसमें थीं).
बंगबंधु के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक सहयोगी जो आज भी सक्रिय हैं, वे हैं कमल हुसैन मुजीब, जिन्होंने बांग्लादेश के संविधान का निर्माण किया और विदेश मंत्री रहे और प्रसिध्द अर्थशास्त्री रहमान शोभन. दोनों ही अब अवामी लीग के विरोधी हैं, उसी लीग के, अपनी युवावस्था में जिसके वे सदस्य रहे थे. बेशक वे उत्साह से पचास वर्ष पहले के उन ऐतिहासिक दिनों को याद करते हैं लेकिन यह भी मानते हैं कि तब से समय का बड़ा अंतराल बीत चुका है, जिससे संघर्ष की याद धुंधली हो चुकीं है, अब वह सिर्फ बुजुर्गों द्वारा कहे जाने वाले किस्सों में ही सुरक्षित है. वह स्मृति अब इतनी जीवंत नहीं है कि हमारे वर्तमान को अनुप्राणित और संचालित कर सके.
तभी कोई तल्ख टिप्पणी होती है, ‘हम शहीद नायकों की स्मृतियों का सम्मान नहीं करते.’ मैं चौंक जाता हूं.यह आजादी के उत्सव का समय है और ढाका की सड़कें शेख मुजीबुर्रहमान के आदमकद बैनरों, पोस्टरों, फोटो और होर्डिंगों से पटी हुईं हैं. अनेक चौराहों पर बंगबंधु की आजादी से पहले और बाद की छवियां दिखाने वाले वीडियो प्रोजेक्टर लगाए गये हैं. कुछ अन्य नेताओं, मुक्ति बाहिनी के गुरिल्ला सिपाहियों और आम बांग्लादेशियों के चित्र भी हैं, जिन्होंने आजादी को हासिल करने में अपनी भूमिका निभाई.
इन सबके बीच विरोध की आवाजें भी उभरती हैं. कोई कहता है, ‘यह नायक पूजा की अति है, साधारण जानता और उसके संघर्षों पर जोर क्यों नहीं दिया जाता.’ क़िस्मत से मैं बांग्लादेशी नहीं हूं इसलिए इस बहस में पक्ष लेने के लिए भी बाध्य नहीं हूं.
भारत के विरोध के तीन प्रमुख कारण नजर आते हैं- सांप्रदायिक ताकतें, दक्षिणपंथी राजनीतिक दल और घरेलू कारणों से भारत को लेकर खड़ा किया गया भय. शेख हसीना की सरकार तीनों की विरोधी है, यह बात भारत के लिए सुकून भरी है. पर बांग्लादेश के इन घरेलू कारणों को नियंत्रित करने की ताकत हमारे पास नहीं है.
लेकिन भारत में हम ऐसे प्रयास जरूर कर सकते हैं जिससे इन ताकतों को कुंठित किया जा सके: सबसे प्रमुख है भारत में सांप्रदायिकता पर लगाम लगाना न कि भारत की वर्तमान सरकार की तरह उसे बढ़ावा देना. विचारपूर्वक प्रमुख विपक्षी पार्टियों से अच्छे संबंध कायम करना. इस तथ्य को स्वीकार करना कि विपक्ष को 40 फीसदी बांग्लादेशी मतदाताओं का समर्थन है और नीतियों के कार्यान्वन की समस्या को सुलझाना न कि ऐसी बहसें और बयानबाजी करना जो कि भारत विरोधी हौए को विश्वसनीयता देती है.
(मूल रूप से अंग्रेज़ी में लिखे गए इस लेख का अनुवाद शुभेन्द्र त्यागी ने किया है. वे दिल्ली विश्वविद्यालय में शोधार्थी हैं.)