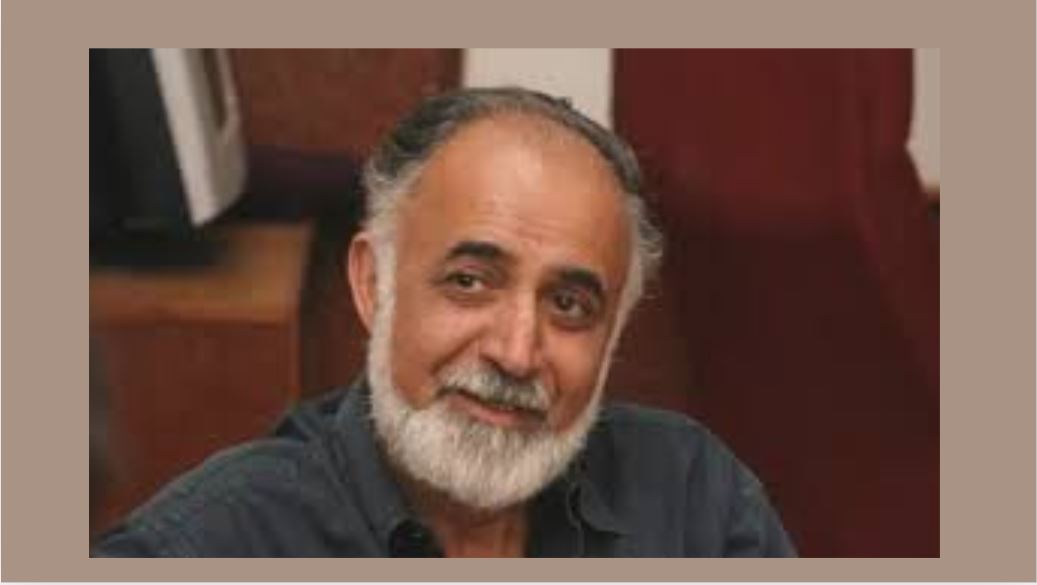प्रसिद्ध रंगकर्मी, अभिनेता और सांस्कृतिक कर्मी एमके रैना ने थिएटर की नयी भाषा रची है. युवा शोधार्थी मुकेश कुलरिया के साथ इस संवाद में वे सांस्कृतिक परंपरा में प्रतिरोध, नाट्य और सांगीतिक परंपरा के इतिहास, अपने अनुभवों पर चर्चा कर रहे हैं.
मुकेश: क्या भक्ति-सूफी रचनाएं नफरत के खिलाफ कारगर हो सकती है या नहीं?
एमके रैना: आपकी बातों का जवाब समाज, राजनीति और संस्कृति के संदर्भ में खोजना जरूरी है. आपने सूफी-भक्ति और धर्मनिरपेक्षता की बात की, और जो बारीकी से एक जटिल स्थिति को दर्शाता है, वो यह है कि इन विचारधाराओं को लेकर हमने कभी पूरी तरह से समझ नहीं बनाई. ये न केवल सियासत के प्रभावों को दर्शाता है, बल्कि हमारी समझ की सीमाओं को भी उजागर करता है. जब आप कहते हैं कि हम भक्ति, सूफीवाद और धर्मनिरपेक्षता को सिर्फ कुछ शब्दों या सिद्धांतों के रूप में समझते हैं, लेकिन उनके भीतर की गहरी सच्चाई को नहीं पहचानते, तो वो बहुत अहम बात है.
आपका यह कहना कि ‘हमने कभी जहर को निकाला नहीं’ यह एक बहुत बड़ा सच है, क्योंकि जब तक हम सामाजिक विषमताओं और सांप्रदायिक नफरत को सही तरीके से पहचानते नहीं हैं, तब तक समाधान नहीं हो सकता. और यही वो कमी है, जो हमारे समाज में साफ दिखाई देती है.
तो आपको लगता है कि जो सांस्कृतिक कर्मी हैं उन्हें जमीन पर भी काम करना होगा?
नाजीवाद और उसके बाद जर्मनी की थिएटर संस्कृति में बदलाव का उदाहरण भी है, ये सही है कि कला और संस्कृति में बदलाव न केवल राजनीति के प्रभावों से होता है, बल्कि एक सामूहिक मनोविज्ञान और जनता की वास्तविकता से भी जुड़ा होता है. इसी तरह, कश्मीर में हुए बदलाव को समझने के लिए, हमें केवल घटनाओं का नहीं, बल्कि उनके पीछे छुपी मानसिकता और सामूहिक भावना को भी समझना होगा. वर्तमान में बहुत कम लोग हैं जो ज़मीन पर काम करते हैं. बहुत कम, और ये हमारे समय के संकट से मुठभेड़ के लिए पर्याप्त नहीं है.
आपने कबीर और सूफियों के बारे में बात की, तो 1982 में, लगभग 42 साल पहले आपने उस पर काम शुरू किया था. वह आज भी अलग-अलग रूपों में चल रहा है. जब आपने शुरुआत की थी, क्या आपके दिमाग में बढ़ते सांप्रदायिक माहौल के प्रति प्रतिरोध था?
एमके रैना: उस वक्त हालात वैसे नहीं थे, थोड़ा सा आलोचनात्मक था बस. लेकिन सबने स्वागत किया. आज यह करना मुश्किल है. कबीर को गाली देना भी बहुत मुश्किल है. यही फर्क है.. आप नानक को गाली नहीं दे सकते, इसलिए उन धरोहरों को पकड़कर इस्तेमाल करना जरूरी है.
वो वक़्त आज से कैसे अलग था?
एमके रैना: हम अयोध्या गए. बाबरी मस्जिद के तुरंत बाद अयोध्या में 17-18 घंटे का बिना रुके कार्यक्रम किया. नब्बे के ही दशक का एक वाकिया है. एक हिंदी अख़बार में अटल बिहारी वाजपेयी ने एक पूरा पन्ना ‘सहमत’ को देशद्रोही कहते हुए लेख लिखा था. एक रोज संयोग से वे उसी फ्लाइट में आ रहे थे, जिसमें हमारे संगीतकार जा रहे थे. मुझे भी जाना था. मुझे जब पता चला तो मैंने कहा कि मैं उनसे लेख बाबत बात करूंगा. उन्होंने तबले और तानपूरे देखे तो वो सो गए, एयरक्राफ्ट में. वे उठे ही नहीं. मैंने कहा ये तो बड़ा शातिर आदमी है. फिर बस में जब बैठे तो वहां पर एक सीपीएम का एक सांसद था, एमे बेबी. उन्होंने हमारा परिचय करवाया. मैंने कहा, सर! आपने हमारे बारे में देशद्रोही लिखा है, हमारे चेहरे पर आपको ऐसा कुछ लगता है? फंस गए वे! मेरे पास ‘अनहद गरजे’ कार्यक्रम के दो टेप थे. ‘सहमत’ की और से उन्हें भेंट किये और कहा कि ये सुनिएगा फिर हमारे बारे में बोलिएगा. हम आप से ज्यादा देशभक्त हैं. वे हंसते हुए बोले– मैं सुनूंगा.
जैसा मैं समझ रहा हूं, आप कबीर या इस प्रतिवाद के उभरने के संदर्भ में बात कर रहे हैं?
एमके रैना: हां, वह भी ज़रूरी है. लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें लोगों की धार्मिक आस्था को नकारना चाहिए. मुझे लगता है कि हमने यह अंतर खुद से बनाया है. हम बहुत कट्टर हो गए हैं. कोई कहता है- ‘मेरा राम!’ लेकिन कबीर भी राम बोलता है, नानक भी बोलता है, कौन नहीं बोलता राम? क्यों चिंता करते हो? अंदर की सीता को किसने छोड़ा? मैं तो यही कहता हूं, भाई, सीता कहां गई ? अगर रामायण से सीता को निकाल दीजिये तो क्या रहता है? रावण भी नहीं रहता, राम तो रहता ही नहीं, हनुमान भी नहीं रहता.
हम अपनी परंपराओं में निहित प्रतिरोध का कैसे उपयोग कर सकते है? जैसे कबीर और सूफियों के अंदर एक क्रांतिकारिता, एक तीव्रता है… लेकिन उनके इस आयाम को पीछे धकेल दिया गया है.
एमके रैना: वे धरोहर हैं. मैं कभी लेक्चर देता हूं कि बुल्लेशाह ने कितना अच्छा कहा, तो वहां लोग वाह-वाह करते हैं. तुम्हें पता है कि सूली पर चढ़ाए गए थे, जब यह कलाम बोले थे? सूफियों की रात में खाल उतारी गई थी. तुम्हारे देश में. मैं उनसे कहता हूं कि बुल्लेशाह की कब्र कहां है, ज़रा बताओ. वह गांव में नहीं दफनाया गया, मौलवियों ने उसे दफनाया नहीं. यहां उसे दफनाएंगे ही नहीं, क्योंकि वह कुफ्र की बात करता था. खैर, बुल्लेशाह को तो ये अपने गांव में दफन नहीं होने दिया. पर हम सिर्फ़ कविता की बात करते हैं.
मैं झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक व्याख्यान के लिए गया था. वहां एक प्रोफ़ेसर मुझसे कहते हैं, ‘सर, आपके व्याख्यान का शीर्षक क्या है?’ मैंने पूछा, क्यों? वह कहते हैं, ‘हमारा नया कुलपति, वह आरएसएस का है.’ मैंने कहा, ‘ठीक है, लिख लो— ‘संस्कृत नाट्य में प्रतिरोध’. कहता है मरवाओगे क्या?
खैर, मैंने शुरू किया कि भाषा ने कैसे नाट्यशास्त्र को तोड़ा. उस प्ले में देखो कैसे? और मैं नाटकों, पात्रों का उद्धरण देने लगा. नाट्यशास्त्र कहता है कि मरता हुआ व्यक्ति मंच पर दिखा नहीं सकते. तब पंडितों ने भाष को क्या कहा होगा? उसका तो कुछ पता ही नहीं है. हमारी पूरी परंपरा है. चलिए इस परंपरा को आगे लेकर चलते देते बौद्धों ने क्या किया? सूफियों तक पहुंच गया मैं. अचानक एक ने कहा, लेकिन सर आपने जो कहा ये तो हिंदुओं का है ना. मैंने कहा अरे भाई आप कब आए मेरे व्याख्यान में? मैंने कहीं हिंदू शब्द बोला ही नहीं . मैंने कहा ये हमारी परम्परा है. संस्कृत परंपरा से लेकर यहां तक मैंने कहीं हिंदू शब्द का उल्लेख ही नहीं किया है.
अगर आपके आस-पास धर्मांधता बढ़ रही है, ऐसे में सम्बंधित धर्मों के अंतस की वे रचनाएं जो कहीं न कहीं एक समावेशिता की बात करती हैं, एक विविधता की बात करती हैं. तो आप धर्म से उनको हटाए बिना किस तरह समावेशिता सिखा सकते हैं?
एमके रैना: देखो, हम कट्टरता करते करते दो-तीन चीज़ें भूल गए हैं. गांधी क्या करते थे? वे दोनों हिंदू धर्म को पुनर्परिभाषित कर रहे थे. उन्हें समझ आया. गांधी का राम अलग है, इनका राम अलग है, कबीर का राम अलग है, और इनका राम अलग है, उसमें हमें उन चीज़ों को पकड़ना चाहिए. हम क्यों इनके राम के साथ जाएं. आडवाणी जी एक बार मेरा नाटक देखने आए थे, मैंने कहा ये राम जो अपने बनाया, वो तो था नहीं …
आपकी याददाश्त में हैं कि इस तरह की कोई पहल पहले हुई है?
एमके रैना: एक पहल हुई थी. दिल्ली में भी एक बार दंगे हुए थे. सफ़दर की हत्या के बाद की बात है. पुलिस प्रमुख तब बिहार से थे. बड़े धर्मनिरपेक्ष. मदद मांगने खुद सहमत के दफ्तर आए. हमारे सवाल से पहले बोल गए—हमें नहीं पता आर्ट-कल्चर फल्चर. आपका आयोजन हम देखते हैं, बड़ा असर पड़ता है. तो आप मुशायरा रखें. हमने उन्हें आश्वस्त किया कि हम मदद करेंगे, साथ में यह भी कहा कि आयोजन कैसा होना चाहिए, यह हम बताएँगे. चांदनी चौक में कर रहे थे. भाई साहब उसको करने के बाद धर्मनिरपेक्ष लोग ही हमारे जान के पीछे पड़ गए— तुम पुलिस के साथी बन के कर रहे हो.
यह जो महत्वपूर्ण बात निकलकर आ रही है, वो यह है कि धर्मनिरपेक्ष या प्रगतिशील का एक बड़ा तबका अपनी वैचारिक शुद्धता बचाए रखने में ज़्यादा तत्पर है, बजाय इसके कि देश और समाज में साझेदारी और एकता होनी चाहिए.
एमके रैना: देखिए, इस वक्त आप फंसे हुए हैं, बाढ़ आई हुई है, हम डूब जाएंगे. जो भी आपके साथ आना चाहता है, बांध बनाने के लिए, साथ लीजिये उसका. मैंने पिछली बार भी कहा था, मैं तो शैतान के साथ भी मिलने को तैयार हूं. मुझे लगता है कि बुद्धिजीवियों का जो एक बहुत बड़ा तबका है, उसे राजनीति पर दबाव डालना चाहिए. वे अपील करें. हमें चाहिए कि हम लोग दिखाएं कि दीवार पर क्या लिखा है. उन्हें इन नेताओं को एकजुट कर रैलियां करनी चाहिए. अगर नहीं करेंगे, तो हमेशा इसी पेच पर खेलते रहेंगे. तो बात यह है कि हमें उनका सामना करना होगा. मुझे नहीं लगता कि वह लड़ाई करने से संभव होगा, तर्क से जरूर संभव हो सकता है. हमें खुद को संगठित करना होगा.
(लेखक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, लॉस एंजिल्स में संगीत और धर्म पर शोध कर रहे हैं)