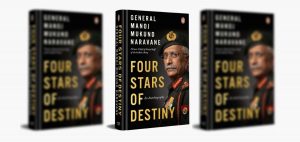(उमर खालिद के नाम)
पांच साल… यह कोई अंक नहीं था, बल्कि अब्दुल मन्नान की कोठरी की दीवारों पर जमी हुई वह काई थी जो अब उसकी सांसों में भी बस गई थी. शुरू-शुरू में, जब वह यहां आया था, तो हर पेशी एक उम्मीद लाती थी. वह अपनी क़मीज़ की सिलवटें ठीक करता, वकील के चेहरे पर किसी इशारे को तलाश करता और जेल वापसी पर साथियों को बताता कि ‘शायद अगली बार…’. लेकिन अब, तारीख़ का आना उसके लिए वैसे ही था जैसे अस्पताल के किसी वार्ड में ड्रिप की बूंद का गिरना. एक बेजान और थका देने वाला सिलसिला.
जेल की बैरक में अब्दुल मन्नान के लिए दो तरह की दुनिया थीं. एक वह छह-सात लड़के, जो उसी के साथ ‘देशद्रोह’ के लेबल के नीचे आए थे. उनके बीच अब बातचीत ख़त्म हो चुकी थी. वे एक-दूसरे की आंखों में भी अब नहीं झांकते थे क्योंकि वहां उन्हें अपना ही विकृत प्रतिबिंब नज़र आता था.
दूसरी ओर वे क़ैदी थे, जो उस ‘सरकारी राष्ट्रवाद’ का हिस्सा थे जहां अब्दुल मन्नान और उसके जैसे लोग इस मिट्टी के दुश्मन क़रार दिए जा चुके थे.
‘ओए पीएचडी! आज फिर तारीख़ मिली या फ़ैसला हो गया?’
बैरक के कोने में बैठा हुआ जगदीश, जो चोरी के जुर्म में अंदर था पर जिसका सीना ‘राष्ट्रवाद’ के गर्व से हमेशा चौड़ा रहता था, ठहाका लगाकर बोला. ‘तुम जैसे पढ़े-लिखे लोग देश को दीमक की तरह चाट रहे हो. सरकार ने तुम जैसे फलों को सड़ाने के लिए ही इस टोकरी में रखा हुआ है.’
अब्दुल मन्नान ने कोई जवाब नहीं दिया. उसने अपने काले कंबल पर पड़े एक बारीक तिनके को उठाया. उसे याद आया कि पांच साल पहले जब वह पीएचडी का थीसिस लिख रहा था, तो उसका विषय ‘प्रतिरोध की भाषा’ था. आज उसे अहसास हो रहा था कि असली प्रतिरोध ‘बोलने’ में नहीं, बल्कि इस ज़हर को ख़ामोशी से पी जाने में है जो आपको हर रोज़ पिलाया जाता है.
सबसे ज़्यादा बेदर्द वह लम्हा था जब पिछले महीने उसके दो साथियों, अदील और रिहान को ज़मानत मिल गई. पांच साल का साथ, एक ही थाली में खाना और एक ही खालीपन को ताकने के बाद, जब वे अपनी पोटलियां समेटकर बैरक से बाहर निकल रहे थे, तो अब्दुल मन्नान को लगा कि उसके अपने शरीर का कोई हिस्सा कटकर अलग हो रहा है.
‘भाई, घबराना मत, हम बाहर जाकर तुम्हारे लिए कुछ करेंगे, हम लोगों को हक़ीक़त बताएंगे…’ रिहान ने गले मिलते हुए कहा था. उसकी आवाज़ में वह जोश था जो जेल के गेट से बाहर क़दम रखते ही हवा हो जाता है.
अब्दुल मन्नान ने उसे देखा और बस एक फीकी-सी मुस्कुराहट के साथ उसे विदा किया. वह जानता था कि बाहर के मोर्चे, वे ट्विटर ट्रेंड्स और वे अख़बारी बयान इस लोहे के गेट के सामने रद्दी से ज़्यादा अहमियत नहीं रखते. जब वे चले गए, तो बैरक में छाने वाली ख़ामोशी उनकी मौजूदगी के अहसास से ज़्यादा बोझल थी.
उस रात अब्दुल मन्नान ने पहली बार महसूस किया कि वह अब सिर्फ़ एक क़ैदी नहीं, बल्कि एक ‘सबक़’ बना दिया गया है जिसे सत्ता ने दूसरे नौजवानों को डराने के लिए बचाकर रखा है.
दो बार उसे ‘पेरोल’ मिली थी. बीस-बीस दिन की वह ‘अधूरी आज़ादी’, जो क़ैद से ज़्यादा कष्टदायक थी. जब वह घर पहुंचा, तो उसे अपना ही कमरा अजनबी लगा. उसकी किताबों पर धूल की इतनी मोटी परत थी कि उसे अपना नाम भी धुंधला नज़र आया. उसकी मां की नज़रें हर वक़्त उसका पीछा करतीं, जैसे वे देखना चाहती हों कि उनके बेटे के अंदर से वह ‘पुराना अब्दुल मन्नान’ कहां ग़ायब हो गया.
‘पेरोल’ ख़त्म होने पर जब वह वापस जेल के गेट पर पहुंचा, और तलाशी लेने वाले सिपाही के खुरदरे हाथों ने उसके शरीर को छुआ, तो उसकी मां के हाथों का अहसास और उसके घर की ख़ुशबू वहीं गेट के बाहर ही झड़ गई. जेल के अंदर प्रवेश करना अब उतना मुश्किल नहीं था, जितना बाहर की दुनिया से बार-बार कटना.
अब वह किसी पेशी पर उम्मीद की उंगली थामे नहीं जाता था. वकील जब अदालती फ़ैसलों की व्याख्या करता, तो अब्दुल मन्नान को वे शब्द किसी प्राचीन और मृत भाषा के व्याकरण लगते. उसके लिए अब सच और झूठ में कोई अंतर नहीं रहा था, बस एक ‘रूटीन’ है जो बार-बार दोहराई जा रही थी. उसे पता है कि उसे रिहा भी किया गया, तो वह किसी ‘इंसाफ़’ की बुनियाद पर नहीं बल्कि सत्ता के किसी ‘राजनीतिक उपकार’ की शक्ल में होगा.
अब्दुल मन्नान ने दीवार पर लगे उस छोटे से सुराख़ की ओर देखा जहां से सूरज की एक मुरझाई किरण अंदर आने की कोशिश कर रही थी. क्या यह किरण भी ‘पेरोल’ पर आई है? क्या इसे भी थोड़ी देर बाद अंधेरे में वापस लौटना होगा?

रात के पिछले पहर जब बैरक की रोशनियां मद्धम कर दी जातीं, तो अब्दुल मन्नान को महसूस होता कि कोठरी की दीवारें धीरे-धीरे सिकुड़ रही हैं, यहां तक कि वे उसके वजूद को छूने लगतीं. यह वह वक़्त होता जब उसका ‘ज्ञान’ उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता. एक विद्वान की कल्पना उसके लिए जेल में सबसे ज़्यादा घातक हथियार होती है. वह दीवार के कोने में लगी हुई सीलन की नक़्क़ाशी में उन पत्थरों के अक्स ढूंढता जिन पर उसे शोध करना था. वह कच्ची दीवार पर नाख़ून से मिट्टी कुरेदता और उसे महसूस होता कि वह अपनी ही आत्मकथा के अक्षर मिटा रहा है.
जेल की लाइब्रेरी; जिसे वॉर्डन मज़ाक में ‘अब्दुल मन्नान का पुस्तकालय’ कहता था; सिर्फ़ कुछ धार्मिक किताबों और पुरानी पत्रिकाओं तक सीमित थी. अब्दुल मन्नान को जब नए काग़ज़ नहीं मिलते, तो वह इन पत्रिकाओं के हाशिए पर अपने अधूरे शोध के पॉइंट लिखने की कोशिश करता. लेकिन एक मुद्दत के बाद उसने महसूस किया कि उसके दिमाग़ से शब्द पलायन कर रहे हैं.
वह ‘प्रतिरोध’ की वर्तनी बार-बार भूल जाता. वह ‘आज़ादी’ के पर्यायवाची शब्द याद करने की कोशिश करता तो दिमाग़ में सिर्फ़ लोहे की सलाखों के टकराने की आवाज़ आती. यह उसकी याददाश्त की वह कमतरी थी, जिसका कोई हिसाब किसी अदालत के पास नहीं था.
‘अब्दुल मन्नान! मुलाक़ात आई है.’
यह आवाज़ उसे किसी गहरी खाई से आती हुई महसूस हुई. ‘मुलाक़ात’; वह शब्द जो कभी ख़ुशी लाता था, अब एक नया बोझ बन गया था. गंदे शीशे के उस पार उसकी मां बैठी थी. शीशे पर उंगलियों के इतने निशान थे कि उसे अपनी मां का चेहरा किसी धुंधले इतिहास जैसा लग रहा था. उनके बीच लगे इंटरकॉम की झिर्रियों से मां की आवाज़ किसी टूटी हुई रिकॉर्डिंग की तरह आ रही थी.
‘बेटा! वकील कह रहा है कि इस बार जज साहब बदल गए हैं. वे बहुत दयालु हैं. दुआ कर रही हूं…’
अब्दुल मन्नान ने मां के कांपते हाथ को देखा जो शीशे पर टिका हुआ था. वह चाहता था कि इस शीशे को तोड़ दे, पर उसने सिर्फ़ अपना हाथ उस जगह रख दिया जहां शीशे के दूसरी ओर उसकी मां की हथेली थी. उसे कोई स्पर्श महसूस नहीं हुआ, सिर्फ़ ठंडे कांच की उदासीनता थी.
‘मां को कैसे बताऊं कि यहां जज नहीं बदलते, सिर्फ़ तारीख़ें बदलती हैं. वह जज जो दयालु है, वह भी उसी क़ानून की ज़ंजीरों में जकड़ा हुआ है जिसने मेरे पांच सालों को एक ‘टेक्निकल एरर’ बना दिया है. मेरी बेगुनाही अब एक ऐसा बोझ है जिसे उठाते-उठाते अदालतें भी थक गई हैं.’
वापसी पर, तलाशी के बीच जब सिपाही ने उसके बग़ल में दबी वो पुरानी पत्रिका छीन ली जिसके हाशिये पर उसने कुछ लिखा था, तो अब्दुल मन्नान ने विरोध नहीं किया.
‘अब क्या योजना बना रहे हो?’ सिपाही ने नफ़रत से पूछा.
अब्दुल मन्नान ने ख़ामोशी से उसे देखा. उसने सोचा, अगर मैं इसे बताऊं कि ये ‘प्राचीन सुमेरी भाषा’ के रूपक हैं, तो क्या यह मुझे थप्पड़ मारेगा या हंसेगा? उसने सिर्फ़ इतना कहा: ‘कुछ नहीं साहब, बस समय काट रहा हूं.’
और फिर उस ‘विशेष सुनवाई’ का दिन आया.
पूरी जेल में अफ़वाह गर्म थी कि इस बार सुप्रीम कोर्ट ने सख़्त टिप्पणी की है. वकील ने अब्दुल मन्नान को इशारे से बताया कि ‘तैयार रहो, आज इंसाफ़ का मुखौटा उतरने वाला है.’ उसके अंदर मरती हुई उम्मीद ने एक आख़िरी करवट ली. उसे लगा कि शायद आज वह उस हवा में सांस ले सकेगा जिसमें किसी क़ैदी की बू शामिल नहीं होगी. उसने अपनी सबसे साफ़ क़मीज़ पहनी, जो अब उसे ढीली हो चुकी थी; जैसे उसका शरीर भी इन पांच सालों में थोड़ा सा ‘कम’ हो गया हो.
अदालत के कमरे में सन्नाटा था. जज साहब ने फाइल खोली, ऐनक साफ़ की, और वक़ील की तरफ़ देखकर एक ठंडी मुस्कुराहट उछाली.
‘यह अदालत संतुष्ट है कि अभियोजन के सामग्री से आरोपी अब्दुल मन्नान के खिलाफ पहली नज़र में आरोप सामने आए हैं. कानूनी धाराएं इस आरोपी पर लागू होती हैं. कार्रवाई के इस चरण पर उन्हें जमानत पर रिहा करना उचित नहीं है.’
जज साहब ने कलम उठाई और एक ऐसी हरकत की जैसे वह किसी कागज़ पर नहीं बल्कि अब्दुल मन्नान की ‘शह-रग’ पर निशान लगा रहे हों.
‘आरोपी जांच पूरी होने के बाद या इस फैसले की तारीख के एक साल पूरे होने के बाद जमानत के लिए फिर से आवेदन कर सकता है.’
कमरे में मौजूद वकीलों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई. अब्दुल मन्नान वहीं खड़ा रहा. उसे लगा कि वह किसी अदालत में नहीं, बल्कि किसी क़साई की दुकान पर खड़ा है जहां उसे ‘वज़न’ के हिसाब से नहीं बल्कि ‘ख़ौफ़’ के बटखरे से तौला जा रहा है.
वह ऊंचाई, जहां से उसे धकेला गया था, इतनी ज़्यादा थी कि गिरते समय उसे चीखने का मौक़ा भी नहीं मिला. जब पुलिस वाले उसे बाज़ू से पकड़कर बाहर ले जाने लगे, तो उसने मुड़कर जज के पीछे लगी हुई उस तराज़ू की तस्वीर को देखा. उसे लगा कि तराज़ू के दोनों पलड़े बराबर नहीं हैं, बल्कि एक पलड़े में सत्ता का पूरा बोझ है और दूसरे में एक जवान लाश, जो अभी सांस ले रही है.
वापसी में अब्दुल मन्नान ने गाड़ी की खिड़की से बाहर देखा. शहर की रोशनियां, ऊंची इमारतें और सड़क पर चलते हुए लोग; सब उसे किसी ऐसी फिल्म के किरदार लगे जो उसने कभी देखी थी लेकिन अब उसे उसकी कहानी याद नहीं.
जेल के गेट पर पहुंचकर, वॉर्डन ने व्यंग्य भरा सलाम किया.
‘वेलकम स्कॉलर साहब! मैंने कहा था ना, यहां से सिर्फ़ समय निकलता है, इंसान नहीं. चलो, अब अपने ‘पुस्तकालय’ की दीवारों का पाठ्यक्रम दोबारा शुरू कर दो.’
अब्दुल मन्नान ने अंदर क़दम रखा. उसे महसूस हुआ कि अब उसके अंदर की छटपटाहट अचानक ख़त्म हो गई है. उसे अब किसी ‘पेरोल’ की ज़रूरत नहीं थी, न किसी वकील की, न किसी मोर्चे की. उसने दीवार पर नाख़ून से एक और लकीर खींची.
यह लकीर किसी तारीख़ की नहीं थी, बल्कि यह उसकी आत्मा की वह आख़िरी लकीर थी जो अब ख़ामोश हो चुकी थी. उसने सोचा, अगर मेरा ज्ञान मुझे नहीं बचा सका, तो शायद मेरा मौन ही मेरा आख़िरी विरोध हो. उसने आंखें बंद कर लीं और उस शून्य में उतर गया जहां इंसाफ़ एक पुरानी पड़ चुकी चीज़ है और समय एक ऐसी ज़ंजीर, जो आपके अपने ही ख़ून से नम होती है.
ऊपर आसमान में एक कबूतर उड़ा, पर अब्दुल मन्नान ने उसे नहीं देखा. वह तो अब इस दीवार का हिस्सा बन चुका था जिस पर अन्याय का शिलालेख गड़ा था.
(अशअर नज्मी साहित्यकार हैं और प्रसिद्ध उर्दू साहित्यिक पत्रिका ‘इस्बात’ के संपादक हैं.)