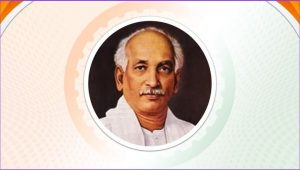उधम सिंह और भगत सिंह के चरित्रों को एक संदर्भ देते हुए शूजीत सरकार दो महत्वपूर्ण लक्ष्यों को साध लेते हैं. पहला, वे क्रांतिकारियों को वर्तमान संकीर्ण राष्ट्रवाद के विमर्श के चश्मे से दिखाई जाने वाली उनकी छवि से और बड़ा और बेहतर बनाकर पेश करते हैं. दूसरा, वे आज़ादी के असली मर्म की मिसाल पेश करते हैं. क्योंकि जब सवाल आज़ादी का आता है, तो सिर्फ दो सवाल मायने रखते हैं: किसकी और किससे आज़ादी?

अनेक भारतीयों की तरह मैं भी ‘एक आंख के बदले आंख से पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी’, को मोहनदास करमचंद गांधी का कथन मानता था. यह बात मेरे अंदर इतनी गहराई तक घुस गई थी कि यह कथन वास्तव में किसका है, इसकी जांच करने का ख्याल मेरे मन में कभी आया ही नहीं. बॉलीवुड की कई देशभक्ति वाली फिल्मों में भी यही मानसिकता झलकती है. ये फिल्में आजादी के योद्धाओं को हाड़-मांस के इंसान के तौर पर न देखकर एक प्रतीक के तौर पर पेश करती थीं – और उनका बेढंगा सामान्यीकरण करती थीं, उनकी जटिलताओं को छानकर उन्हें मल्टीप्लेक्स के दर्शकों के लिए एक सुंदर माल में बदल देती थीं. समय के साथ यह प्रवृत्ति और खराब होती गई.
पिछले सात सालों में बॉलीवुड के जबरा राष्ट्रवाद के बारे में काफी कुछ लिखा गया है. लेकिन अमेजन प्राइम वीडियोज, पर दिखाई जा रही शूजीत सरकार की हालिया फिल्म सरदार उधम ऐसी कमजोरियों को परे रखते कुछ ऐसा दिखाती है, जो बॉलीवुड के लिए विरल है : एक क्रांतिकारी और उसके विचार, एक विद्रोही और उसके -महाद्वीपों के आरपार फैले- सहयोगी, एक व्यक्ति और उसका व्यक्तित्व- जो लापरवाह सामान्यीकरणों और उथले चरित्रांकन में आनंदित होने वाली संकीर्ण मानसिकता से दागदार नहीं हुए हैं.
रितेश साह और शुभेंदु भट्टाचार्य द्वारा लिखित सरदार उधम ज्यादातर जीवनी आधारित फिल्मों की क्रमबद्ध जीवन वर्णन करने वाली शैली का त्याग करके एक नॉन-लीनियर नैरेटिव (यानी बिना किसी सीक्वेंस को अपनाए) के प्रयोग से भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण दास्तां को बयान करती है.
अगर एक इंसानी जीवन को कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं में सीमित किया जा सकता, तो उधम सिंह (विकी कौशल) की जिंदगी कुछ इस तरह से होती: जालियांवाला बाग नरसंहार (अप्रैल, 1919) का साक्षी बनना, पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ’डायर की हत्या (मार्च, 1940), फांसी (जुलाई, 1940).
इस फिल्म में ये घटनाएं इस क्रम में प्रस्तुत दर्शायी गई हैं (फिक्र न करें, इस जानकारी से फिल्म देखने का मजा किरकिरा नहीं होगा- लेकिन अगर आप इसके प्रति अतिरिक्त संवेदनशील हैं, तो आगे के कुछ शब्द न पढ़ें): हत्या (27 वें मिनट), नरसंहार (117वें मिनट) और फिर फांसी (150वें मिनट).
उधम की मृत्यु के अलावा अन्य घटनाएं एक निश्चित कालक्रमिक (क्रोनोलॉजिकल) पैटर्न का पालन नहीं करती हैं- एक धमाकेदार शुरुआत या क्लाइमेक्स को छोड़कर- क्योंकि सरकार एक स्वतंत्रता सेनानी के जीवन को एक बिकाऊ माल की तरह नहीं देखते हैं और एक पहले से ही एक सुलगती कहानी के सबसे नाटकीय लम्हों को भुनाने की कोशिश नहीं करते.
वे सबसे पहले फिल्म के केंद्रीय मर्म को समझना चाहते हैं- एक बड़ी तस्वीर के आपस में जुड़े हुए विभिन्न टुकड़ों को पकड़ना चाहते हैं- इस उम्मीद के साथ कि ये टुकड़े मिलकर एक मनोरंजक फिल्म भी बनाएंगे. इस जुड़ाव ने ही फिल्म निर्माता को संभवतः एक हर किसी के हाथ से छिटक जाने वाले लक्ष्य को हासिल करने में मदद की हो- और यह है बायोपिक को साध लेने की सफलता.
सरदार उधम का शुरुआती दृश्य पंजाब की जेल का है, साल है, 1931, जब उधम सिंह जेल से रिहा होते हैं. फिर कुछ समय तक दो कहानियां साथ चलती हैं: पहली, उधम सिंह का पंजाब पुलिस की निगरानी से फरार होना और दूसरी क्रांतिकारी के तौर पर उनके शुरुआती दिन, जब वे भगत सिंह (अमोल पाराशर) से प्रभावित हुए थे और उनसे उनकी दोस्ती हुई थी.
यह समानांतर नैरेटिव उधम सिंह द्वारा डायर (शॉन स्कॉट) की हत्या के बाद फिर दिखाई देता है: एक कथा स्कॉटलैंड यार्ड अधिकारी स्वैन (स्टीफन होगन) द्वारा वर्तमान में की जा रही पूछताछ पर केंद्रित है, जबकि दूसरी कहानी स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह की 1934 में यूनाईटेड किंगडम आने से लेकर 1940 तक की यात्रा पर केंद्रित है. यह शैली अंत तक बनी रहती है और नैरेशन जालियांवाला बाग नरसंहार और उधम सिंह के आखिरी दिनों के बीच बारी-बारी से आवाजाही करता रहता है.
भारत में अंग्रेजी शासन पर बनी ज्यादातर देशभक्ति वाली फिल्में आजादी की लड़ाई और उसके नेताओं के व्यक्तिगत पक्ष को दबा देती हैं. ऐसी ज्यादातर कवायदों का ध्यान बॉक्स ऑफिस मुनाफे पर होता है और ये सबसे बुनियादी- और सबसे फिल्मी- बातों के पार नहीं जा पातीं. दमित भारतीय, अत्याचारी अंग्रेज, भूख हड़ताल, जेल, विद्रोह; हत्याएं. यह इतिहास सिर्फ कठपुतलियों के लिए नहीं, बल्कि उनके लिए भी है, जो सोचने-समझने की शक्ति से हीन हैं.
वे दर्शकों को देश के वास्तविक मर्मस्थल से अलग कर देती हैं और उन्हें बस कुछ आकर्षक शब्द देकर छोड़ देती हैं- इस मानसिकता का एक आयाम हर रोज न्यज चैनलों, ट्विटर टाइमलाइनों और अनौपचारिक बातचीतों में प्रकाशित होता है, जिनमें धड़ल्ले से ‘राजद्रोह’, ‘एंटी नेशनल’, ‘अर्बन नक्सल’ जैसे अर्थभ्रष्ट हो चुके शब्दों, जिनकी एक लंबी सूची है, का इस्तेमाल होता है.
शूजीत सरकार की फिल्म को इस बात की समझ है कि सिर्फ एक सर्वआयामी फिल्ममेकिंग- जिसमें संदर्भों, अंतर्विरोधों और जटिलताओं के लिए जगह हो- भारतीय शहीदों के सच्चे मर्म की पहचान कर सकता है. क्या यह इन दिनों चलने वाली तीखी बहसों का केंद्र क्या यही नहीं है- भारतीय कौन है और भारत क्या है? वैसे सवाल जिनका समाधान 1947 में नहीं हो सका था, वैसे सवाल जो आज भी देश को दो हिस्सों में बांट देते हैं. और इसका काफी महत्व है, क्योंकि अगर आप अपनी कहानी, अपना इतिहास नहीं जानते हैं, तो कोई और आपकी जगह इसे लिखेगा और फिर उसे कैसे कहा जाता है, इस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं रहेगा. यह भी एक कारण है, जो सरदार उधम फिल्म को एक नायाब हीरा बनाता है.
लेकिन एक अर्थपूर्ण लय पाने में यह फिल्म अपना समय लेती है. शुरुआती एडिटिंग हड़बड़ी भरी और एकाग्रता भंग करने वाली है: इसमें कई बेमकसद कट्स हैं और मानीखेज संवाद की बात जाने दीजिए, किसी शॉट पर टिके रहने को लेकर एक अबूझ-सी अनिच्छा है. लेकिन डायर की हत्या के बाद ये कमियां पीछे छूट जाती हैं और एक परतदार कहानी हमारे सामने आती है.
हम कई भारतीयों को अंग्रेजों का साथ देते हुए देखते हैं, खासकर पंजाब पुलिस और स्कॉटलैंड यार्ड में. यह प्रतीक तब और चुभता है, जब डायर उधम को, जो डायर के नौकर के तौर पर काम कर रहे हैं, कहता है, ‘खुश करने की तत्परता- भारतीयों की यह चीज मुझे पसंद आती है. लेकिन इस सबप्लॉट (उपकथा) का अंत तब होता है, जब उधम कोर्ट से कहते हैं, ‘कुछ भारतीयों ने गुलामी का आनंद लेना शुरू कर दिया है.’- मानो किसी ने बंद कमरे की दीवार को ध्वस्त कर दिया हो.
यहां तक कि उधम, स्वैन और एक भारतीय अनुवादक को शामिल करने वाली रूटीन पूछताछ भी सिनेमाई उत्कर्ष का नमूना बनकर सामने आती है. इसमें एक निश्चित पैटर्न का पालन किया गया है: स्वैन द्वारा सवाल पूछा जाता है, पीछे से उसका हिंदी अनुवाद होता है और जवाब में उधम की चुप्पी- कोई डॉयलॉगबाजी नहीं, कोई अतिनाटकीय गुस्सा नहीं. लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा होता है, जो इस स्वतंत्रता सेनानी के चरित्र और फिल्म के मकसद को सामने ला देता है.
किसी भी तरह से उधम सिंह के मुंह से सच उगलवाने के लिए स्वैन कहता है, ‘तुम जरूर अंग्रेजों से नफरत करते होगे.’ दूसरी तरफ से एक हल्की हंसी के साथ एक शांत जवाब आता है, ‘नहीं, मेरे कई अंग्रेज दोस्त हैं.(…), मैं तुमसे भी नफरत नहीं करता. तुम सिर्फ अपना काम कर रहे हो.’
स्पष्ट दृष्टि वाले ऐसे गंभीर लेखन की छाप पूरी फिल्म में दिखाई देती है- और मेरे लिए एक पसंदीदा दृश्य को चुन पाना मुश्किल है. शायद यह वह दृश्य है जिसमें भगत सिंह अपनी समाजवादी प्रतिबद्धताओं को स्पष्ट करते हुए घोषणा करते हैं, ‘एक क्रांतिकारी के लिए निश्चित सिद्धांतों का पालन करना जरूरी है. आप पूर्वाग्रह से ग्रस्त, सांप्रदायिक या जातिवादी नहीं हो सकते हैं. इसमें सामाजिक या आर्थिक अंतरों के लिए जगह नहीं है. समानता ही एकमात्र सच्चाई है.’
या फिर वह दृश्य जिसमें वे कहते हैं, ‘एक सच्ची विचारधारा के बगैर आजादी, गुलामी से भी बदतर हो सकती है.’ या शायद वह दृश्य जिसमें लंदन की एक फैक्ट्री में काम करते हुए उधम सिंह उनके एक दोस्त के साथ एक ब्रिटिश सुपरवाइजर की बदतमीजी से आक्रोशित हो जाते हैं. लेकिन उनके गुस्से के पीछे सिर्फ राष्ट्रवादी भावना का हाथ नहीं है. वे हर किसी से, जिनमें कुछ ब्रिटिश कर्मचारी भी हैं, काम रोकने के लिए कहते हैं.
इसके बाद वे उन सबको संबोधित करते हैं और उन्हें दमन की विभिन्न भाषाओं के बारे में समझाते हैं, और शोषित कामगारों और गुलाम भारतीयों को एक डोर से जोड़ते हुए गरजते हैं, ‘हम भी तो इंसान हैं यार. दुनिया में जो है, हमारा भी तो है. या फिर वह दृश्य जिसमें पंजाब के लोग रॉलट एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस उन्हें रोकने के लिए उनकी तरफ बढ़ती है. यह दृश्य हमें बेचैन तरीके से समय के एक दूसरे दौर में ले आता है: हम खुद से पूछते हैं, क्या यह 1919 का अमृतसर है या 2021 की दिल्ली है?
विकी कौशल का अभिनय यहां शानदार और कसा हुआ है. जिस सधे हुए हाथ से इसे लिखा गया है, उतना ही सधा हुआ कौशल का अभिनय है. डायर पर गोली चलाने के बाद जब उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, तब वे क्रोधित या कड़वाहट से भरे हुए नहीं हैं; इसकी जगह उनकी आंखें एक संतोष और गर्व से रंगी हैं.
उनके बोलने में एक समझ में आने वाली आतुरता है, खासकर जब वे हिंदी और (टूटी-फूटी) अंग्रेजी को मिलाकर बोलते हैं. वे दृश्य को लंबा करने वाली तरकीबें नहीं आजमाते हैं, बल्कि फिल्म की लय के साथ एक प्रभावशाली सटीकता के साथ अपनी लय को मिलाते हैं.
जब कहानी नियंत्रण की मांग करती है, तब वे खुद को बैकग्राउंड में डाल देते हैं; जब यह उनसे अपनी बात कहने के लिए कहती है, तब वे जैसे फट पड़ते हैं. सहयोगी कलाकार भी काफी मंजे हुए हैं. एक छोटी-सी भूमिका में पाराशर भगत सिंह के किरदार के लिए शानदार पसंद साबित हुए हैं, जो सामान्य हास-परिहास से याद रह जाने वाली गंभीरता तक आते-जाते हैं.
डायर ओर स्वैन के रूप में होगन और स्कॉट भी हल्के नहीं पड़े हैं. यहां तक कि जासूस और उधम के रिश्ते में एक गर्माहट जैसी भी आ जाती है. उनके बीच के संबंधों का एक अप्रत्याशित करुण अंत होता है.
यह फिल्म हिंसा की राह पर चलने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को एक गरिमा से भी भरती है. वे अविवेकी या खून के प्यासे नहीं थे, यह बात बार-बार उभर कर आती है, बल्कि वे तीक्ष्ण और प्रेम भरा हृदय रखने वाले थे, जिन्हें हमेशा अपने अंतिम लक्ष्य के बारे में पता था, जो था ब्रिटिश साम्राज्यवाद का अंत.
डायर के लिए काम करते हुए उधम के पास पछतावे से रहित गर्वनर की जीवनलीला समाप्त करने के कई मौके थे, लेकिन उनके लिए समझा जाने वाला इरादा, परिणाम जितना ही महत्वपूर्ण था. वे एक गलती करते और उनकी कार्रवाई एक हत्या में बदल जाती- एक क्रांतिकारी की पहचान एक गुलाम की बना दी जाती.
यह सरलीकृत प्रस्तुतीकरणों से बिल्कुल अलग है, जिनमें लगभग हमेशा उनकी कार्रवाई को दिलेरी बताया जाता है (रंग दे बसंती को याद कीजिए). जब उधम सिंह अंग्रेजी साम्राज्य को एक ‘कारोबारी कंपनी’ कहते हैं, तब आप एक कामगार का एक कॉरपोरेशन के खिलाफ आक्रोश को महसूस करते हैं- यह आक्रोश आज भी कई देशों में न सिर्फ जिंदा है, बल्कि प्रासंगिक भी है.
ऐसे चित्र सरदार उधम को सच्चे अर्थों में वैश्विक बना देते हैं और यह फिल्म दुनिया भर के दमित तबकों की आवाज बन जाती है. इसने मुझे 2020 के नागराज मंजुले के एक इंटरव्यू की याद दिला दी, जिसमें उन्होंने भारत में राजनीतिक फिल्म बनाने में बढ़ रही मुश्किलों के सवाल को तूल न देते हुए कहा था, ‘मैं लंबे समय से जेल में हूं. बस जेलर बदलते रहते हैं.’
उधम सिंह और भगत सिंह के चरित्रों को एक संदर्भ देते हुए शूजीत सरकार दो महत्वपूर्ण लक्ष्यों को साध लेते हैं. 1. वे क्रांतिकारियों को वर्तमान संकीर्ण राष्ट्रवाद के विमर्श के चश्मे से दिखाई जानेवाली उनकी छवि- जो अक्सर उन्हें गलत तरीके से हथियाने की कोशिश करती है- से और बड़ा और बेहतर बनाकर पेश करते हैं.
2. वे आजादी के असली मर्म की मिसाल पेश करते हैं. क्योंकि जब सवाल आजादी का आता है, तो सिर्फ दो सवाल मायने रखते हैं : किसकी आजादी, किससे आजादी?
(इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.)