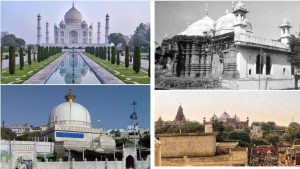बीते महीने चेबरोलू लीला प्रसाद और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ का फैसला एक बार फिर यह दिखाता है कि भारतीय संविधान की पांचवीं अनुसूची, जिस पर आदिवासी अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व है, को कितना कम समझा गया है.

चेबरोलू लीला प्रसाद और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ का हालिया फैसला हमें एक बार फिर यह दिखाता है कि भारतीय संविधान की पांचवीं अनुसूची, जिस पर आदिवासी अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व है, को कितना कम समझा गया है.
राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के शिक्षकों को शत प्रतिशत आरक्षण देने के वर्ष 2000 के आंध्र प्रदेश सरकार के फैसले को निरस्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जिन तर्कों का सहारा लिया है, वह 5वीं अनुसूची की बुनियाद पर आघात है.
आज अगर शिक्षकों की नौकरी के लिए 100 फीसदी आरक्षण अनुमति योग्य नहीं है, तो आगे चलकर कोई आदिवासी जमीन के हस्तांतरण पर प्रतिबंध के खिलाफ भी दलील दे सकता है, या अविभाजित आंध्र प्रदेश के पांचवीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में गैर आदिवासियों को माइनिंग लीज (खनन पट्टे) देने पर प्रतिबंध लगानेवाले समता फैसले को भी पलट सकता है. आखिर ये दोनों ‘गैर आदिवासियों’ के साथ ‘भेदभाव’ करते हैं.
ऐसे मे जबकि दूसरे जिलों के गैर आदिवासी अनुसूचित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में आकर बस रहे हैं, जिसका नतीजा स्पष्ट जनांकिकीय बदलाव के तौर पर सामने आ रहा है- पांचवी अनुसूची के सुरक्षात्मक प्रावधानों को खत्म कर देने की मांग लगातार तेज होती जा रही है.
आंध्र प्रदेश के 2000 के सरकारी आदेश का मकसद आदिवासी इलाकों में शिक्षा को बढ़ावा देना और शिक्षकों के अक्सर गायब रहने की समस्या का समाधान खोजना था.
आदिवासी इलाकों की समस्याओं के बारे में थोड़ी-सी भी जानकारी रखने वाला कोई भी व्यक्ति यह जानता है कि गैर-आदिवासी शिक्षक सुदूर आदिवासी गांवों में जाना या वहां रहना नहीं चाहते हैं. दूसरी बड़ी समस्या भाषा की है.
निचले स्तर के सरकारी अमले समेत कई गैर आदिवासी लोगों ने आदिवासी इलाकों में कई साल रहने के बावजूद कभी आदिवासी भाषा सीखने की जरूरत महसूस नहीं की है. प्राथमिक स्तर पर गैर आदिवासी शिक्षकों और आदिवासी छात्रों के बीच एक भाषाई दीवार होती है, जिससे वे एक-दूसरे को समझ नहीं पाते. इससे बच्चों की बुनियादी शिक्षा को नुकसान पहुंचता है.
जजों का कहना है कि ‘यह एक बुरा विचार है कि सिर्फ आदिवासियों को ही आदिवासियों को पढ़ाना चाहिए.’ (अनुच्छेद 133) लेकिन बेहद लंबे समय तक वास्तव में बुरा विचार यह रहा है कि आदिवासियों का उत्थान करने और उन्हें मुख्यधारा में शामिल करने के लिए गैर आदिवासियों को आदिवासियों को पढ़ाना चाहिए क्योंकि ‘उनकी भाषा और उनकी आदिम जीवन शैली उन्हें मुख्यधारा में शामिल होने और साधारण कानूनों द्वारा शासित होने के अयोग्य बना देती है. (अनुच्छेद 107)
इस संबंध में मानक विचार 2001 के आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के इसी मसले पर जस्टिस एसबी सिन्हा के (अल्पमत) फैसले में व्यक्त हुआ था, जिसके अनुसार गैर आदिवासी शिक्षकों को स्वतः सिद्ध ढंग से ज्यादा सक्षम और योग्य मान लिया जाता है (अनुच्छेद 86) और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के उत्थान के लिए यह जरूरी है कि उन्हें शिक्षा प्रदान करने का जिम्मा जाति का ध्यान दिए बगैर ज्यादा जानकार और योग्य शिक्षकों को सौंपा जाए.’ (अनुच्छेद 126)
सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि ‘उन्हें मानवीय अजायबघर और आदिम संस्कृति के आनंद उठाने के स्रोत और नृत्य प्रस्तुतियां देने वाले के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए’ (चेबरोलू फैसले का अनुच्छेद 107) उस मानसिकता के उलट है, जो अनुसूचित जनजातियों को वास्तव में ठीक इसी खांचे में रखकर देखती है, न कि ऐसे लोगों के तौर पर जिनके पास अपने शैक्षणिक भविष्य का फैसला करने का हक है.
भारत में काफी लंबे समय से सत्ता-प्रतिष्ठान शिक्षा को ‘सभ्यताकारी’ मिशन के तौर पर देखता आया है, जिसका मकसद आदिवासियों और दलितों को ऊंची जातियों का मानसिक प्रतिरूप (क्लोन) बनाना रहा है, भले ही वे उनके अधीन ही काम करना जारी रखें. काबिलियत को बस इस मकसद को हासिल करने की क्षमता के तौर पर ही परिभाषित किया जाता है.
स्थानीय पारिस्थितिक ज्ञान को हासिल करने, आदिवासी भाषाओं, संस्कृति का संरक्षण करने और रोल मॉडल की भूमिका निभाकर आदिवासी छात्रों में विश्वास पैदा करने की गिनती काबिलियत के तौर पर नहीं होती है. कई आदिवासी शिक्षकों ने भी गैर आदिवासी श्रेष्ठता के इस विचार को आत्मसात कर लिया है.
अनुसूचित इलाकों में शत प्रतिशत आदिवासी शिक्षकों का होना, इस धारणा को पलटने की दिशा में बस एक छोटा-सा कदम है.
इस निर्णय के पीछे का विचार मानवशास्त्रियों और निज़ाम सरकार के सलाहकारों क्रिस्टॉफ वॉन फ्यूरर-हैमेंडरफैंड डब्ल्यू जी. ग्रिगसन द्वारा चलाए गए शैक्षणिक प्रयोगों तक और बीडी शर्मा, एसआर शंकरण, बीएन युगंधर और ईएएस शर्मा जैसे संवेदनशील प्रशासकों द्वारा नक्सली आकर्षण के सामने सरकारी विकल्प मुहैया कराने की कोशिशों तक पीछे जाता है.
हालांकि सरकारी फैसले का कानूनी बचाव करने की जिम्मेदारी काफी हद तक मानवशास्त्री जेपी राव के अलावा आदिवासी शिक्षक एवं नेता सोंधी वीरियाह के साथ-साथ के. बालागोपाल और राजीव धवन जैसे वकीलों पर थी, जिन्होंने जनहित में यह मुकदमा बिना फीस लिए लड़ा.
सुप्रीम कोर्ट का फैसला हाईकोर्ट के 2001 के बहुमत के फैसले के खिलाफ गैर आदिवासियों द्वारा दायर अपील के जवाब में आया है, जिसमें 2000 के सरकारी आदेश को सही ठहराया गया था. सुप्रीम कोर्ट का फैसला वास्तव में हाईकोर्ट में गैर-आदिवासियों के पक्ष में अल्पमत की राय को दोहराता है.
कोर्ट ने चार सवालों पर विचार किया :
- पहला सवाल, पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में कानून बनाने की राज्यपाल की शक्ति से संबंधित है, साथ ही इससे कि क्या यह संविधान के भाग तीन या मौलिक अधिकारों को निरस्त कर सकती है?
- दूसरा, क्या 100 फीसदी आरक्षण संवैधानिक रूप से अनुमति योग्य है?
- तीसरा, क्या सरकारी आदेश, संविधान के आरक्षण से संबंधित अनुच्छेद 16 (4) की जगह, राज्य की नौकरियों में सबको बराबर मौके देने से संबंधित अनुच्छेद 16 (1) के तहत वर्गीकरण करता है?
- चौथा, आरक्षण के लिए आवश्यक शर्त- उस क्षेत्र में 1950 से लगातार निवास- तर्कसंगतता की जांच से संबंधित है.
लेकिन अफसोस की बात है कि इन सभी सवालों का जवाब देते हुए कोर्ट ने यह दिखाया कि वह देश की हकीक़तों और विरासत में हासिल संविधान के इतिहास के प्रति किस कदर बेपरवाह है.
कानून बनाने की राज्यपाल की शक्तियों का विस्तार
100 फीसदी आरक्षण को निरस्त करने के लिए कोर्ट का पहला तर्क यह है कि प्रभाव में यह एक नया कानून था क्योंकि 2000 के सरकारी आदेश ने खासतौर पर आरक्षण से संबंधित अधिनियम में संशोधन नहीं किया और नियम संसद या राज्य की विधानसभा के अधिनियम के बराबर नहीं नहीं होते हैं.
अनुसूची 5 के अनुच्छेद 5(1) के तहत सरकार सिर्फ संसद या राज्य विधानसभा द्वारा बनाए गये कानूनों को लागू कर सकती है या नहीं लागू नहीं कर सकती है, कोई नया कानून नहीं बना सकती है.
इसी बिंदु पर पुलुसम कृष्णामूर्ति मामले में हाईकोर्ट ने बहुमत से यह तजवीज दी थी कि कानून को लागू करना कानून बनाने या विधायन (लेजिसलेशन) के स्वीकृत रूपों में से एक है (अनुच्छेद 21) और यह कहना अतार्किक है कि यही शक्ति ‘प्रत्यायोजित विधान’ ( डेलिगेटेड लेजिशजेशन) को नहीं मिली है.’ (जस्टिस वीवीएस राव के निर्णय का अनुच्छेद 37)
किसी भी व्याख्या को चुनते वक्त, यह ध्यान रखना जरूरी है कि जब पांचवीं अनुसूची के तहत राज्यपाल की कानून निर्माण शक्ति पर संविधान सभा की बहिष्कृत और आंशिक तौर पर बहिष्कृत इलाकों की उपसमिति में चर्चा हो रही थी, तब मसला यह नहीं था कि क्या उसे (राज्यपाल को) नया कानून बनाना चाहिए या नहीं, बल्कि असल मसला यह था कि इस शक्ति का इस्तेमाल निर्वाचित विधायिका को दरगुजर करके अलोकतांत्रिक तरीके से नहीं किया जाना चाहिए.
इसी कारण से आदिवासी सलाहकार परिषद का गठन किया गया और राज्यपाल के लिए इसके समक्ष मामलों को भेजना जरूरी कर दिया गया. (उप समिति की रिपोर्ट का अनुच्छेद 11 बी) इस मामले में आदिवासी सलाहकार परिषद ने 100 फीसदी वाले नियम पर अपनी सहमति जताई थी.
मौलिक अधिकार बनाम पांचवीं अनुसूची
इस सवाल पर कि क्या पांचवीं अनुसूची के उपनियम 5 के तहत राज्यपाल की विधायी शक्तियां, मौलिक अधिकार का अतिक्रमण कर सकती हैं- सुप्रीम कोर्ट का जवाब था कि ऐसा नहीं किया जा सकता.
ऊपरी तौर पर देखें तो इस कथन का कौन विरोध करेगा कि अनुसूचित इलाकों के लिए कोई कानून बनाते वक्त या कानून लागू करते वक्त किसी राज्यपाल को मौलिक अधिकारों का ध्यान रखना चाहिए?
उदाहरण के लिए कोई भी ‘डायन’ बताकर की जाने वाली हत्या पर कानून लागू न करने को इसलिए नजरअंदाज नहीं कर देगा क्योंकि यह तो एक प्रथा रही है.
लेकिन यह तर्क देना कि मौलिक अधिकार- और वह भी तब जब इस केस की ही तरह इसकी संकीर्ण व्याख्या गैर आदिवासियों के लिए ‘बराबरी’ के तौर पर की जाए- को हमेशा संविधान के दूसरे प्रावधानों पर तरजीह मिलनी चाहिए, इस बात को भुला देना है कि किस तरह से संविधान का निर्माण विविधता में एकता को मुमकिन बनाने के लिए किया गया था, फिर वह चाहे अनुच्छेद 370 हो या पांचवीं और छठी अनुसूचियां.
मौलिक अधिकार और पांचवीं और छठी अनुसूची, दोनों ही संविधान सभा के अस्तित्व की बुनियादी और समान महत्व की पूर्वशर्त थी. कैबिनेट मिशन योजना, जिसके तहत संविधान सभा ने काम किया, के खंड 20 में ‘मौलिक अधिकारों की सूची, अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए प्रावधान और आदिवासी और बहिष्कृत क्षेत्रों के प्रशासन की योजना’ पर रिपोर्ट देने के लिए सलाहकार समिति का प्रावधान किया गया था.

भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों को दिए गए अधिकार ‘उन्हें मुख्यधारा में लाने और उनका उत्थान करने के लिए’ उनके ऊपर किया गया कोई उपकार नहीं है, बल्कि इस बात की स्वीकृति है कि भारतीय समाज की ‘मुख्यधारा’ की कई धाराएं हैं जो इसमें आकर मिलती हैं और इनमें से हर धारा बराबर रूप से वैध है.
जैसा कि जस्टिस वीवीएस राव ने हाईकोर्ट के बहुमत के फैसले में दर्ज किया है, संवैधानिक योजना में, अनुच्छेद 19 (5) की आवागमन की स्वतंत्रता समेत ऐसे कई कानून हैं, जहां ‘अनुसूचित जातियों की रक्षा और उनके हित को गैर अनुसूचित जनजातियों के मौलिक अधिकारों के ऊपर वरीयता दी जाएगी.’
सुप्रीम कोर्ट ने इस तथ्य को काफी तवज्जो दी है कि 2000 का सरकारी आदेश अनुच्छेद 371-डी के साथ सीधे टकराव में आ जाता है, जो नौकरियों के लिए बहाली और आरक्षण के लिए जिले को इकाई मानता है.
यह आदेश इसलिए अस्तित्व में आया, क्योंकि अविभाजित आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों के लोग हर जगह नौकरी पर कब्जा कर रहे थे. कोर्ट का यह दावा है कि चूंकि गैर-आदिवासी अपने जिले से बाहर आवेदन नहीं कर सकते हैं और अनुसूचित इलाकों में उन पर पाबंदी है, इसलिए उनके लिए नौकरी के मौके बचते ही नहीं हैं.
लेकिन दुर्भाग्यजनक ढंग से इस निष्कर्ष में सच्चाई का अंश बहुत कम है क्योंकि अनुसूचित इलाके किसी भी जिले का एक छोटा-सा हिस्सा होते हैं. उदाहरण के लिए विशाखापत्तनम जिले में (जो किसी भी जिले में अधिकतम है) अनुसूचित इलाका 52.9 फीसदी है, श्रीकाकुलम में 22.09 फीसदी है और पश्चिमी गोदावरी में (सबसे कम) यह 13 प्रतिशत है.
इन अनुसूचित इलाकों में अनुसूचित जनजातियां स्पष्ट तौर पर बहुमत में हैं इसलिए यह एक तरह से उनका हक बनता है कि उन्हें अपने भाषा समुदाय के व्यक्ति ही शिक्षक के तौर पर मिलें- पडेरू/विशाखापत्तनम में अनुसूचति जनजातियां आबादी का 88 फीसदी हैं. श्रीकाकुलम में 78 और पश्चिमी गोदावरी में 47 फीसदी हैं.
अनुसूचित इलाकों के बाहर सिर्फ 6 फीसदी पद ही अनुसूचित जनजातियों के लिए, 15% अनुसूचित जातियों के लिए, 25 फीसदी पिछड़ी जातियों के लिए और एक तरह से 54 फीसदी अगड़ी जातियों के लिए आरक्षित हैं.
हाईकोर्ट में जस्टिस सिन्हा के अल्पमत के निर्णय- जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी है- ने भी यह दावा किया था कि अनुसूचित जनजातियों के शिक्षकों के लिए 100 फीसदी आरक्षण अनुसूचित इलाकों के गैर-अनुसूचित छात्रों के साथ भेदभाव करता है:
‘अगर किसी स्कूल का प्रबंधन एक खास वर्ग के शिक्षकों के द्वारा किया जाता है, तो दूसरे वर्गों से संबंध रखने वाले छात्रों के साथ भेदभाव होगा.’ (अनुच्छेद 111).
यह सचमुच विस्मयकारी है कि वे लोग ही जो बेहद शिद्दत से जातिमुक्त समाज और जातिवाद की समस्या की बात करते हैं, वे खुद को जाति-पूर्वाग्रहों के शिकार के तौर पर देखते हैं. वे इस संभावना पर कभी विचार नहीं करते हैं कि वर्णाश्रमी/द्विज हिंदुओं द्वारा पढ़ाए जानेवाले आदिवासी (और दलित) बच्चों के साथ भेदभाव किया जा सकता है.
अनुच्छेद 16(1) या अनुच्छेद 16(4)
पुलुसम वाले मामले में हाईकोर्ट की बहुमत वाली पीठ को अधिवक्ता के. बालागोपाल और अन्यों द्वारा दी गई इस दलील ने प्रभावित किया था कि 100 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था करने वाला सरकारी आदेश आरक्षण की व्यवस्था करने वाले अनुच्छेद 16(4) के तहत नहीं, बल्कि राज्य के नियोजन में सभी को बराबरी के मौके देने का वादा करने वाले और इसकी प्राप्ति के लिए युक्तियुक्त वर्गीकरण की इजाजत देनेवाले अनुच्छेद 16(1) के तहत दिया गया था.
उनकी दलील थी कि अनुसूचित क्षेत्रों में शिक्षकों के पद नौकरियों की एक बिल्कुल ही अलग श्रेणी है- जिसकी जरूरतें और उद्देश्य अलग हैं.
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने काफी स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण (साथ ही अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए) पूरी तरह से 16 (4) के भीतर है और 16 (1) सिर्फ उन श्रेणियों के लिए है, जो 16 (4) में नहीं आती हैं.
इससे आगे कुछ भी स्पष्टीकरण दिये बगैर फैसला सुना दिया गया, ‘अगर इस दलील को मान भी लिया जाए कि यह अनुच्छेद 16 (1) के तहत वर्गीकरण का मामला है, तो भी यह पूरी तरह से भेदभावपूर्ण और पूरी तरह से मनमाना और तर्करहित और संविधान के दायरे से बाहर है.’
मूल निवासी बनाम बाहरी
अंत में, हम उस चौथे सवाल पर आते हैं, जो आज देश के कई विवादास्पद मसलों के केंद्र में है- अप्रवासियों और मूल निवासियों के अधिकारों के बीच संतुलन कैसे साधा जाए?
असम के मामले में इसने नागरिकों के संशोधित राष्ट्रीय रजिस्टर के नाम पर 19 लाख लोगों की नागरिकता छीन ली है; दूसरी तरह कश्मीर में अनुच्छेद 35 ए के तहत मूल निवास के लिए दी गई सुरक्षा को अवैध घोषित कर दिया गया.
अनुसूचित जनजातियों के मामले में, ऐसा प्रतीत होता है कि नौकरी के लिए आवश्यक योग्यता पर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अप्रवासियों की बढ़ती संख्या की समस्या को कोई मुद्दा ही नहीं माना.
न ही इसने 1950 में अनुसूचित इलाके बनाने के पीछे के तर्क का कोई ख्याल रखाः ‘इस विचाराधीन मामले में दिए गए सरकारी आदेश उम्मीदवारों के अभिभावकों का 26.01.1950 से आज तक उस इलाके में सतत निवास अनिवार्य बना देता है. पिछले 50 सालों से सतत निवास की शर्त के पीछे कोई तर्क नहीं है. यह कई अन्य लोगों के अधिकारों की पूरी तरह से अनदेखी करता है जो इन इलाकों में दशकों पहले आकर बस गए हों. निवास की यह शर्त (कटऑफ डेट) बेहद अतार्किक और मनमाने ढंग से तय की गई है और यह विचारणीय क्षेत्र को बिल्कुल संकुचित कर देती है, जबकि सार्वजनिक रोजगार के मौके पर्याप्त अधिकार रखने वाले सभी संबंधित व्यक्ति को दिए जाने चाहिए.’ (अनुच्छेद 147)
इस देश में लाभप्रद रोजगार में हिंदू उच्च जातियों के गैर आनुपातिकढंग से ज्यादा प्रतिनिधित्व को देखते हुए कोई चाहे तो यह कह सकता है कि इसका निर्धारण ‘बेहद अतार्किक और मनमाने ढंग से किया गया है.’
उच्च जाति के हिंदुओं के इस विश्वास का कोई तुक या तर्क नहीं है कि सिर्फ उनके पास ही इस देश पर शासन करने, न्याय देने या लोगों को शिक्षा देने का स्वाभाविक अधिकार है और दूसरी सभी जातियों और धर्मों को उन्हें मिलने वाली शिक्षा और न्याय के लिए उनका शुक्रगुजार होना चाहिए.
(नंदिनी सुंदर दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाती हैं.)
(इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.)