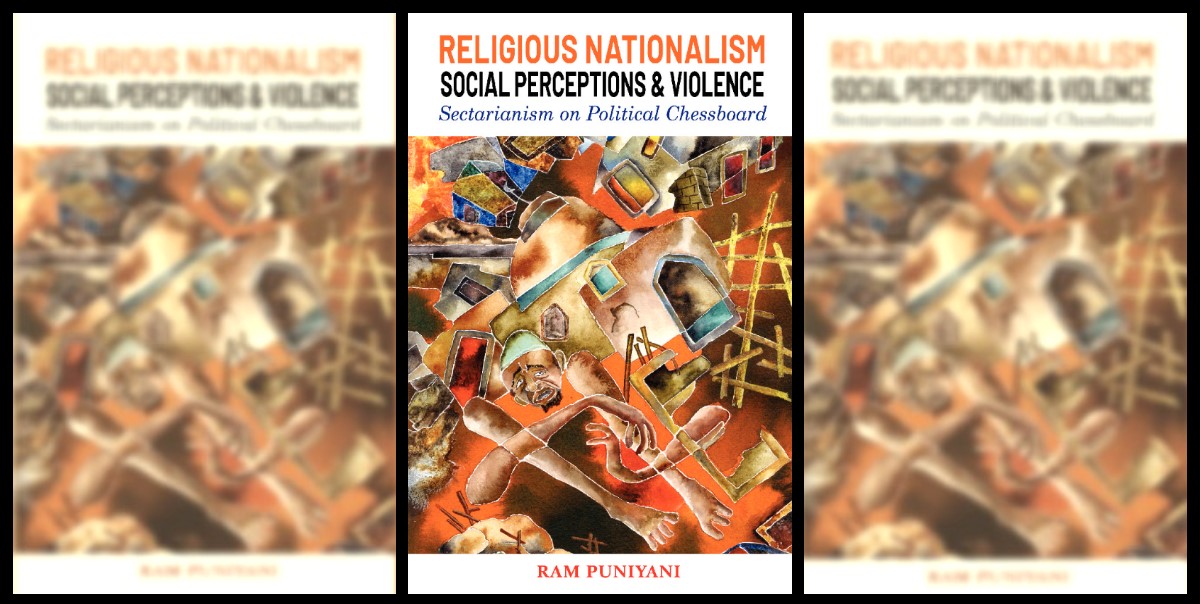ऐसे विरोधाभास बहुत कम देखने को मिलते हैं. पिछले दिनों ऐसा ही एक मंज़र सामने नमूदार हुआ जब अंतरराष्ट्र्रीय पत्रिका ‘टाइम ’ द्वारा जारी ‘100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में प्रधानमंत्री मोदी और शाहीन बाग़ की बिलकिस दादी दोनों के शामिल होने की ख़बर मिली.
एक मुल्क के वजीरे आज़म, तो दूसरी दारूल हुकूमत के एक नामालूम से मोहल्ले की 82 साल की बुजुर्ग महिला.
जनाब मोदी को पत्रिका के तहत ‘नेताओं’ की श्रेणी में शुमार किया जाना वैसे उनके अनुयायियों के लिए कोई बहुत उत्साहित करने वाला नहीं रहा होगा.
दरअसल पत्रिका में मोदी के लिए लिखे लब्जों में संपादक महोदय ने लिखा था, ‘अब तक भारत के अधिकतर प्रधानमंत्री अस्सी फीसदी हिंदू आबादी से जुड़े रहे हैं, अलबत्ता मोदी का ही शासन ऐसा रहा है गोया किसी और की कोई हैसियत न हो.’ (..almost all of India’s Prime Ministers have come from the nearly 80% of the population that is Hindu, only Modi has governed as if no one else matters.)
बिलकिस दादी शाहीन बाग आंदोलन के एक प्रतीक के तौर पर उभरी थी, जिसका आगाज़ जामिया मिलिया इस्लामिया में 15 दिसंबर में पुलिसबल द्वारा की गई कथित ज्यादतियों के विरोध में हुआ था, जब पुलिस परिसर में घुसी थी और उसने लाइब्रेरी में घुसकर भी छात्रों पर डंडे बरसाए.
लेकिन रफ्ता-रफ्ता वह आंदोलन मोदी सरकार द्वारा पारित विवादास्पद नागरिकता कानून के खिलाफ परिणत हुआ था, जिसके तहत आज़ादी के बाद पहली दफा धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करने की बात संविधान में जोड़ी जा रही है.
ठंड के उस मौसम में जबकि सर्दी ने अपने पुराने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, धरनास्थल पर सुबह आठ बजे से रात 12 बजे तक बिलकिस दादी की मौजूदगी मीडिया में भी चर्चा का विषय बनी थी.
जैसे-जैसे भारत विश्लेषकों की निगाह में ‘अधिनायकवाद के स्याह गर्त में’ जाता दिख रहा है और जनतंत्र के बढ़ते संकुचन को लेकर तथा विभाजक राजनीति के लगातार वैधता हासिल करने को लेकर चिंता की लकीरें बढ़ रही हैं.
ऐसी तमाम किताबें आई हैं, ऐसे मोनोग्राफ छपे हैं जो इस बात पर रोशनी डाल रहे हैं कि दुनिया के इस सबसे बड़े जनतंत्र ने किस तरह एक ख़तरनाक मोड़ लिया है.
राम पुनियानी जो लंबे समय से सांप्रदायिक सद्भाव और अमन के अभियानी के तौर पर सक्रिय रहे हैं, उनकी ताज़ा किताब ‘रिलीजियस नेशनलिज़्म‘ भी इस बहस में एक नया आयाम जोड़ती है.
जैसा कि लेखक बताते हैं कि यह किताब ‘एक कोशिश है विभाजक राजनीति पर निगाह डालने की और एक सामाजिक सहजबोध के निर्माण में, अल्पसंख्यकों के दानवीकरण में तथा धार्मिक राष्ट्रवाद के एजेंडा के मजबूती हासिल करने में उसकी भूमिका की पड़ताल करने की. इस एजेंडा का प्रगट हिस्सा है धार्मिक अल्पसंख्यकों का हाशियाकरण और गहरे स्तर पर इसके शिकार हैं दलित, स्त्रियां और आदिवासी भी.’ (पेज 36)
विघटनकारी राजनीति के साथ शोषण, लूट और डकैती के कॉरपोरेट एजेंडा के नाभिनालबद्ध होने को रेखांकित करने के साथ साथ किताब की ‘प्रस्तावना’ इस बात को स्पष्ट करती है कि जहां तक अवधारणाओं, नफरत, पूर्वाग्रहों के निर्माण का सवाल है और यह समझना है कि किस तरह वह धार्मिक राष्ट्रवाद के लिए रास्ता सुगम करते हैं, किताब का फोकस मुख्यतः ‘सियासत के सामाजिक पहलुओं पर’ होगा.
किताब बारह अध्यायों में बंटी है जिसकी शुरुआत होती है ‘सोशल कॉमन सेन्स: हेट एण्ड वायलेंस (सामाजिक सहज बोध: नफरत और हिंसा) शीर्षक अध्याय से.
पहला अध्याय सामाजिक सहज बोध की अवधारणा को खोलते हुए उसे ‘ऐसे विचारों के सेट के तौर पर देखता है जिस पर समाज का बहुमत यकीन करने लगता है.’ (पेज 41)
मध्ययुग से शुरुआत करते हुए और उपनिवेशवाद विरोधी कालखंड से गुजरते हुए वह भारत में सामाजिक विचारों की यात्रा की पड़ताल करती है.
लेखक के मुताबिक औपनिवेशिक शासन ने ‘सांप्रदायिक इतिहास लेखन’ (पेज 45) से परिचित कराने में अहम भूमिका निभाई, जिसे ‘समरूपीकरण की प्रक्रिया ने’ मदद पहुंचाई, जहां ‘समूचे धार्मिक समुदाय को एक ही नज़र से देखा गया.’
किताब आगे बताती है कि किस तरह ‘आज़ादी के आंदोलन में उभार के साथ’ राष्ट्रवाद की तीन किस्म की धारणाएं अस्तित्व में आई हैं, ‘भारतीय राष्ट्रवाद, मुस्लिम राष्ट्रवाद और हिंदू राष्ट्रवाद’ जिन्होंने इतिहास के तीन अलग अलग संस्करणों/रूपों को जन्म दिया.
यह अध्याय समकालीन दौर में भी पहुंचता है और इस परिघटना के ‘वैश्विक आयामों’ (पेज 54) की भी बात करता है, और इस बात को भी रेखांकित करता है कि किस तरह सामाजिक अवधारणाएं ‘सहमति के निर्माण’ (मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट) की नोम चोम्स्की द्वारा प्रतिपादित अवधारणाओं से निर्देशित होती हैं.
अगले तीन अध्याय प्राचीन भारत- जिसमें आयोग के आगमन, जाति व्यवस्था और विज्ञान की जड़ों पर चर्चा है तथा मध्ययुगीन भारतीय राज्यों तथा इन्हीं से विकसित हुई ‘साझी विरासत’ (शेयर्ड हेरिटेज) की चर्चा करते हैं.
प्राचीन भारत पर केंद्रित अध्याय एक ऐसा उद्घाटन करता है, जिसकी अधिक चर्चा नहीं हो सकी है. वह बताता है कि किस तरह मोदी सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है ताकि ‘हिंदू फर्स्ट अर्थात हिंदू सबसे पहले की इतिहास की उसकी धारणा पर मुहर लगाई जा सके.’
प्रस्तुत कमेटी को ‘बारह हजार सालों से चली आ रही भारतीय संस्कृति के उद्गम और विकास के समग्र अध्ययन और दुनिया के बाकी मुल्कों के साथ उसकी अंतर्क्रिया की पड़ताल’ के लिए बनाया गया है.’ (पेज 63)
इस परियोजना के पीछे का बुनियादी विचार यही है कि ‘लंबे समय से चली आ रही इस अवधारणा को प्रश्नाांकित करना कि मध्य एशिया के लोग लगभग 3 से 4 हजार साल पहले ही यहां पहुंचे हैं. (पेज 63)
अगर हम विशेषज्ञों की इस कमेटी पर ही निगाह डालें तो पता चलता है कि उसके लिए भारतीय होने के क्या मायने हैं?
‘इस कमेटी में 16 सदस्य हैं… कमेटी के 14 पदेन सदस्य पुरुष हैं. सभी उत्तर भारतीय हैं, हिंदी भाषी पुरुष हैं. अगर हम सरनेम के आधार पर देखें तो … वे सभी या तो ब्राह्मण हैं या उंची जाति के हिंदू पुरुष हैं.
इस कमेटी में एक भी स्त्री नहीं है, न ही एक मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन, यहूदी या जीववादी/एनिमिस्ट, या स्वघोषित दलित या आदिवासी नहीं है और न ही उत्तर पूर्व के सूबों से भी एक भी नहीं है, यहां तक कि समूचे दक्षिण भारत से किसी एक की टोकन उपस्थिति भी नहीं है.
हम आसानी से देख सकते हैं कि ‘विशेषज्ञों की इस कमेटी’ के गठन के पीछे सरकार की एकमात्र चिंता यही है कि किस तरह विजयी हिंदू के अपने एजेंडा को आगे बढ़ाएं और उसे इस बात की कोई चिंता नहीं कि भारतीय उपमहाद्वीप में पहली दफा मनुष्य कब पहुंचा इसके बारे में प्रस्तुत नवीन अनुसंधान क्या कह रहा है.’
टोनी जोसेफ की एक महत्वपूर्ण किताब ‘प्रारंभिक भारतीय’ (जो अंग्रेजी में प्रकाशित मूल किताब ‘अर्ली इंडियन्स’ 2018, Juggernaut) का हिंदी अनुवाद है, इसी मसले पर केंद्रित है.
उन्होंने अपनी किताब की मूल अन्तर्वस्तु को ‘द हिंदू’ के एक आलेख में प्रकाशित किया था. इसमें उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में पहला मनुष्य कब पहुंचा इसके बारे में दो अलग अलग सिद्धांतों की बात की थी.
उनके मुताबिक ‘आरंभिक संस्करण के मुताबिक वह अफ्रीका से निकलकर अरब प्रायद्वीप होते हुए और मध्यप्रस्तर युग के हथियारों जैसे खुरचनी/कुदाली के साथ जिससे उन्हें अपना शिकार करने, अनाज संग्रहित करने या कपड़े बनाने में मदद मिलती थी, लगभग 74 हजार सालों से लेकर एक लाख बीस हजार साल पहले पहुंचे.
‘बाद का संस्करण बताता है कि वे बहुत बाद में पहुंचे, लगभग 50 से 60 हजार साल पहले पहुंचे, जब उनके पास लघुपाषाणी (माइक्रोलेथिक) युग की उन्नत टेक्नोलोजी के उपकरण थे, जिनके आधार पर तीरों और भालों की नोंक को तीखा किया जाता होगा.’
‘शेयर्ड हेरिटेज’ (साझी विरासत) वाले अध्याय में लेखक मध्ययुग में उभरे समन्वय (emergence of syncretism) दार्शनिक मतों के बीच मतभेद दूर करके एकता स्थापित करने का प्रयत्न/की बात करता है जिसके बारे में जेजे रॉय बर्मन लिखते हैं- …वह एक तरह से ईश्वर की धार्मिक पहचानों के सम्मिश्रण या एक किए जाने का प्रयास था, जिसके तहत अन्य के रिवाजों को- जो एक दूसरे से बेहतर दिखता था- चुनने की बात दिखती है.’ (पेज 144) तथा धार्मिक विविधता और बहुलतावाद का सेलिब्रेशन दिखता है.
राजपुत्र दारा शिकोह अपनी किताब ‘मज़मा उलबहारें’ में इसी अंतर्क्रिया की बात करते हैं, जहां वह भारत को ‘हिंदू धर्म और इस्लाम के सम्मिलन स्थल’ (पेज 146) के तौर पर रेखांकित करते हैं, की बात करता है.
लेखक के मुताबिक ‘विभिन्न सांप्रदायिक ताकतों के हमलों के बाद भी मध्ययुगीन समाज की आपसी सद्भावना की सबसे अमूल्य धरोहर सूफी दरगाहों’ के रूप में बची है.
मध्ययुगीन दौर में उभरे भारतीय समाज की विशिष्टताओं को चिन्हित करने के बाद, लेखक औपनिवेशिक कालखंड की ओर बढ़ता है जहां वह न केवल ब्रिटिशों द्वारा लाए जा रहे बदलावों की बात करता है बल्कि उदितमान विभिन्न राजनीतिक संगठनों तथा सांप्रदायिक ताकतों- हिंदू राष्ट्रवाद और मुस्लिम राष्ट्रवाद- की भी बात करता है.
जहां तक बंटवारे की बात है वह इस मत का है कि ‘तीन प्रमुख कारकों के चलते मुल्क का बंटवारा हुआ. पहला था बांटो और राज करो की ब्रिटिश नीति, दूसरा था मुस्लिम जमींदारों और नवाबों की नुमाइंदगी करती मुस्लिम सांप्रदायिकता और हिंदू सांप्रदायिकता (राष्ट्र्रीय स्वयंसेवक संघ-हिंदू महासभा)’ जो उसी तरह हिंदू अभिजातों के हितों की नुमाइंदगी करते हैं. (पेज 173)
यह देखना दिलचस्प है कि हिंदू और मुस्लिम सांप्रदायिकता की बात करते हुए वह ‘राष्ट्र्रीय स्वयंसेवक संघ और मुस्लिम ब्रदरहुड’(पेज 231) की भी तुलना करता है, जो अक्सर नहीं की जाती.
एक अग्रणी राजनेता को उदध्रत करते हुए लेखक रेखांकित करता है कि किस तरह ‘संघ भारत के स्वरूप को बदलने में मुब्तिला है.’ और किस तरह उसका व्यवहार ‘अरब जगत में मौजूद मुस्लिम ब्रदरहुड जैसी संस्थाओं से मेल खाता है.
लेखक के मुताबिक यह विचार है कि ‘एक ही विचारधारा को हर संस्थान को संचालित करना चाहिए और वह एक ही विचार सभी अन्य विचारों को कुचल सकता है.’
लेखक यह भी बताता है कि इन संगठनों के लिए ‘समाज में गैर बराबरी को थोपने, जो एक तरह से उनका विशिष्ट सामाजिक संबंधों को लादने का मूलभूत एजेंडा है’ चैरिटी का काम एक तरह से ऊपरी आवरण का काम बनता है. (पेज 233)
उसके मुताबिक किस तरह यह दोनों संगठन केवल पुरुषों के संगठन है, जो अतीत के स्वर्णिम युग की बात करते हैं और आधुनिक मूल्यों के प्रति उनके विरोध पर जोर देते है और दोनों किस तरह अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए धार्मिक पहचान का इस्तेमाल करते हैं.
अगले अध्याय ‘स्वातंत्रोत्तर भारत में सांप्रदायिक हिंसा (कम्युनल वायलेंस इन पोस्ट इंडिपेडेंट इंडिया) लेखक सांप्रदायिक हिंसा के बारे में अपनी समझदारी पेश करता है, जो उसके मुताबिक ‘मूलतः एक औपनिवेशिक आधुनिक परिघटना है’ और आगे चलकर वह विगत तीन चार दशकों की सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं की चर्चा करता है.
वह अक्सर दोहराए जाने वाले इस अवधारणा पर भी बात करते हैं कि ‘ऐसी हिंसा दो समुदायों के बीच स्वतःस्फूर्त झगड़ों का परिणाम होती है’ (पेज 270) पॉल ब्रास, जो सांप्रदायिक हिंसा के चर्चित अध्येता माने जाते हैं, जिन्होंने आज़ादी के बाद की इस परिघटना पर बहुत कुछ लिखा है और यह प्रमाणित किया है कि किस तरह यहां ‘संस्थागत दंगा प्रणालियां’ (Institutionalised Riot Systems) अस्तित्व में आई है, उन्हें उद्धृत करते हुए लेखक ‘संस्थागत दंगा प्रणालियों के तीन अहम तत्वों पर रोशनी डालते हैं.
एक, खास लक्ष्य को हासिल करने के लिए आयोजित दंगे; दो, एक संगठन की मौजूदगी ताकि भूमिकाओं का बंटवारा करे; तीन, एक सांगठनिक नेटवर्क.
लेखक दलितों और समसामयिक राजनीति के मसले पर अगले अध्याय में रोशनी डालता है जहां वह हिंदू राष्ट्रवादी राजनीति द्वारा आम तौर पर संविधान के लिए तथा विशेषकर दलित अधिकारों के लिए बनी चुनौती की चर्चा करता है.
वह सवाल उठाता है कि किस तरह ‘यह राजनीति आंबेडकर के उद्देश्यों के बिल्कुल विपरीत खड़ी है और किस तरह वह सामाजिक समरसता मंच-वनवासी कल्याण आश्रम जैसे संगठनों के जरिये अनुसूचित जाति-जनजातियों को अपने आप में समाहित करने की कोशिश कर रही है’ (पेज 320) और किस तरह दूसरी तरफ ‘यह राजनीति सांस्कृतिक छलयोजना/हेरफेर के जरिये दलितों-आदिवासियों के प्रतीकों को हिंदुत्व राजनीति में ढाल रहा है.’
महिलाओं के अधिकार का मसला अगले अध्याय का फोकस है, जहां इस बात पर जोर दिया गया है कि ‘जहां तक महिलाओं के अधिकारों का सवाल है धर्म के नाम पर चलने वाली राजनीति, यहां भारत में हिंदुत्ववादी संगठनों की राजनीति हो या पड़ोसी मुल्कों में इस्लामिक बुनियादपरस्तों की सियासत हों या ईसाई मूलवादियों की राजनीति सभी एक ही सुर में चलते रहते हैं. (पेज 341)
उपसंहार में लेखक एनआरसी-सीएए के मसले को उठाता है और बताता है कि किस तरह भारत के बहुलतावादी जनतांत्रिक लोकाचार का वह उल्लंघन करते हैं.
कुल मिलाकर देखें तो यह किताब- जो तमाम संदर्भों से परिपूर्ण है जिन्हें कोई भी अध्येता या कार्यकर्ता बाद में देख सकता है- पठनीय है और भारतीय संविधान और जनतांत्रिक आज़ादियों के मूल्यों के सामने हिंदू राष्ट्रवाद द्वारा प्रस्तुत ख़तरे का बखूबी एहसास कराती है.
वैसे एक बात कही जानी जरूरी है कि किताब को अधिक सख्ती से संपादित करने की आवश्यकता थी ताकि उसे अधिक चुस्त बनाया जा सकता था.
प्रस्तुत लेखक का मानना है कि किताब का अंतिम अध्याय ‘पॉलिटिक्स, रिलीजन एंड टेररिज्म’ किताब के समूचे संदर्भ में अतिरिक्त जान पड़ता है.
दूसरे, लेखक द्वारा साझी विरासत और समन्वयवाद (देखें ‘शेयर्ड हेरिटेज: कॉमन एस्पिरेशन) की बेहद सकारात्मक अंदाज़ में चर्चा को मौजूदा वातावरण में समझा जा सकता है, जहां ‘अन्य’ के प्रति नफरत परवान चढ़ती दिख रही है और धार्मिक अल्पसंख्यकों के दोयम दर्जे का अधिकाधिक सामान्यीकरण( normalisation ) होता दिख रहा है.
इस वातावरण में अतीत की इन साझी परंपराओं के बारे में सुनना निश्चित ही मन को सुकून दे सकता है. लेकिन क्या यह स्थिति समूची सच्चाई को प्रतिबिंबित करती है?
इसमें कोई दोराय नहीं कि साझी विरासत या समन्वयवाद की इन बातों को उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के दौरान खूब मजबूती मिली, जब बर्तानिया के खिलाफ संघर्ष में अग्रणी नेताओं, संगठनों ने व्यापक जनता की आपसी एकजुटता को मजबूती दिलाने के लिए इसकी खूब बात की.
अपने एक आलेख में सामाजिक कार्यकर्ता एवं लेखक हर्ष मंदर बताते भी हैं कि,
‘यह धारणा काफी मजबूत है कि भारत अपने लंबे इतिहास में एक विविधतापूर्ण, बहुलतावादी और सहिष्णु सभ्यता रही है- यह बुद्ध, कबीर और नानक की, अशोक, अकबर और गांधी की भूमि रही है.’
इसमें कोई दोराय नहीं कि मध्ययुग में या उसके बाद की चली आ रही सच्चाई का इसमें प्रतिबिंबन दिखता है, लेकिन क्या सच्चाई का यही एकमात्र विवरण कहा जा सकता है या एक दूसरा पहलू भी रहा है जो स्याह है, आपसी रंजिशों, मारकाट, खून खराबे से भरा है.
मेरे खयाल से इस दूसरे सच के बारे में भी पड़ताल या खोजबीन करने की जरूरत है ताकि हम एक वस्तुनिष्ठ प्रतिक्रिया दे सकें.
मिसाल के तौर पर, साझा संस्कृति और समन्वयवाद की संस्कृति के चले आते रहने के बावजूद आखिर बंटवारे के वक्त दक्षिण एशिया का यह हिस्सा क्यों आपसी खून-खराबे का नज़ारा बना, जहां आधिकारिक तौर पर 20 लाख लोग मारे गए और लगभग डेढ़ करोड़ लोग विस्थापित हो गए?
आखिर वह ऐतिहासिक साझापन अचानक काफूर कैसे हो गया? मेरे खयाल से अब वक्त़ आ गया है कि बेहद बेबाकी के साथ साझा संस्कृति को लेकर पड़ताल की जाए ताकि तमाम वादों के बीच हम सच्चाई की तह तक पहुंच सकें.
(सुभाष गाताडे वामपंथी एक्टिविस्ट, लेखक और अनुवादक हैं.)