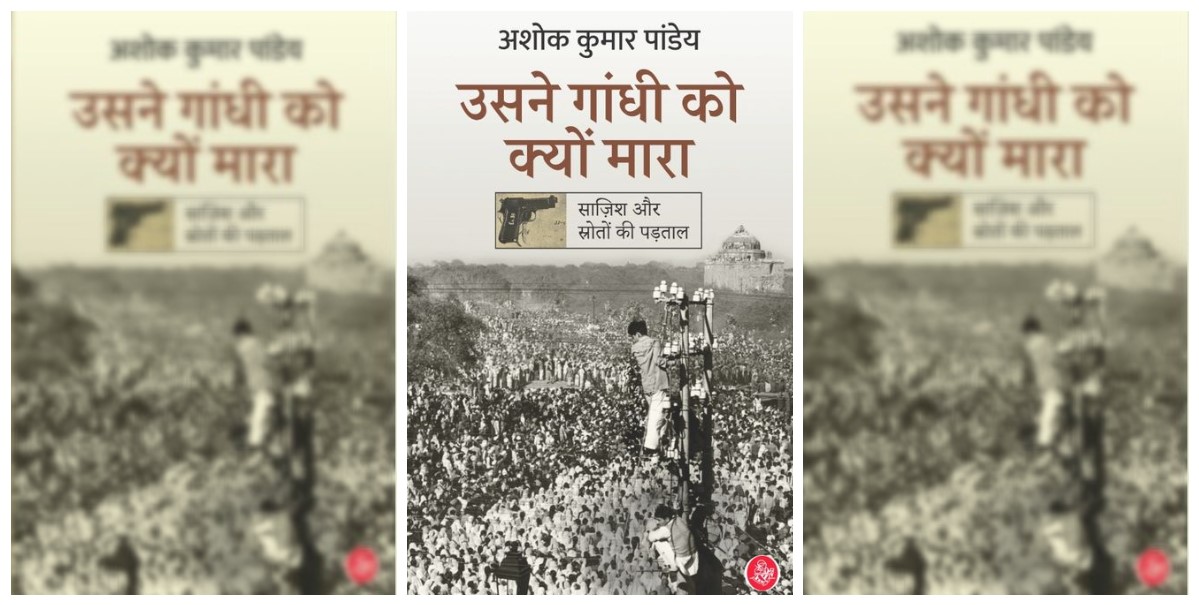(यह लेख मूल रूप से 01 नवंबर 2020 को प्रकाशित किया गया था.)
सांप्रदायिक फासीवाद के प्रतिरोध के लिए वर्तमान के राजनीतिक संघर्षों के साथ अपने अतीत की, अपने इतिहास की रक्षा जरूरी है. उन प्रतीकों, मिथकों और सांस्कृतिक संदर्भों को दुर्व्याख्याओं से बचाए रखने की जरूरत है जिसके उपयोग से जन-मन को बांटा जाता है.
गांधीजी के जीवन और मृत्यु पर अथाह लेखन के बावजूद अशोक कुमार पांडेय ने अगर ‘उसने गांधी को क्यों मारा’ को अपने शोध और लेखन का विषय बनाया तो उसके पीछे इसी चेतना को देखना चाहिए.
पुस्तक के फ्लैप पर इसे ‘इतिहास को भ्रष्ट करने वाले दौर में एक बौद्धिक सत्याग्रह’ कहा गया है.
‘उसने गांधी को क्यों मारा’ पुस्तक अपने उद्देश्य की दिशा में अपने नाम से ही आधी बाजी मार ले जाती है. नाम में काफी कुछ रखा है! यह नाम ही एक जबरदस्त प्रतिपक्ष तैयार कर देता है.
वैसे यह नाम जितना उचित और सार्थक है उतना ही भ्रामक भी. उचित इसलिए कि एक ही बार में यह पाठक का ध्यान पूरी तरह अपनी ओर खींच लेता है और सिर्फ गोडसे ही नहीं बल्कि उस पूरी विचारधारा की ओर ध्यान ले जाता है जिसके कारण गांधी की हत्या हुई.
भ्रामक इसलिए कि किताब सिर्फ गांधी के मृत्यु को संबोधित नहीं करती बल्कि उस दौर के और वर्तमान के अन्य कई महत्वपूर्ण प्रश्नों, दुष्प्रचारों से मुठभेड़ करते हुए चलती है.
और इसमें कोई दो राय नहीं कि इस भ्रम के बने रहने के बावजूद वर्तमान के हालात को देखते हुए विषय पर इससे बेहतर शीर्षक सुझाया नहीं जा सकता.
अशोक कुमार पांडेय घोषित मार्क्सवादी हैं. मार्क्सवादियों ने अपने राजनीतिक विचारों के प्रसार के क्रम में गांधी के वैसे पाठ पर ही ज्यादा ध्यान दिया है जिससे अपनी वैचारिक-राजनीतिक प्रस्थापनाओं को ज्यादा तार्किक दिखाकर प्रस्तुत किया जा सके.
आंबेडकरवादियों ने भी यह काम किया है. इन धाराओं द्वारा गांधी के उन पहलुओं की अपेक्षाकृत कम चर्चा की जाती है जो गांधीवाद के मजबूत पक्ष हैं.
पिछले कुछ वर्षों में यह एहसास गहरा हुआ है कि इन प्रगतिशील धाराओं की इस कमी को दूर किया जाए.
आंबेडकर को लेकर तो पिछले कुछ दशकों में वामपंथी दलों ने अपनी राजनीति में काफी बदलाव किया है, लेकिन दुखद है कि गांधी के सार्थक पहलुओं के महत्व को अभी भी काफी हद तक रेखांकित किया जाना बाकी है.
सुखद यह है कि अशोक कुमार पांडेय की यह पुस्तक उस दूरी, उस फर्क को एक मार्क्सवादी नज़र से मिटाने के पिछले कुछ वर्षों के बेहतरीन प्रयासों में से एक है.
इतिहास के भ्रष्ट होते जाने और समय के सत्यातीत होते जाने की चिंता इस किताब का प्रस्थान-बिंदु है. पुस्तक का स्वर यही है, इसकी बात का लहजा यही है, टोन यही है: जहां तक हो सके इतिहास को बचा लिया जाए और सत्य को इतने प्रमाणों के साथ रेखांकित किया जाए कि उत्तर-सत्य के माध्यम और मुहावरे कमजोर पड़ जाएं.
ये चिंताए इस किताब को शोधपरक भी बनाती हैं और आज से इतने दशकों पहले घटी घटना को समकालीन और प्रासंगिक भी.
यह अकारण नहीं है कि गांधी और नेहरू की मृत्यु के सत्तर साल बाद भी उन्हें मारने की कोशिश बदस्तूर जारी है. गांधी के व्यक्तित्व और विचारों से प्रतिक्रियावादी पीछा नहीं छुड़ा सकते. इसलिए गांधी पर हमले जारी रहेंगे. ऐसे में गांधी की हत्या के इतिहास को उसके पूरे यथार्थ से बचाए रखना निस्संदेह आने वाली पीढ़ियों की चेतना को कुंद किए जाने के खिलाफ एक मुनासिब कार्रवाई है, जिसे भविष्य में भी जारी रखना होगा.
इस पुस्तक में यह स्थापना है कि गांधी जी की हत्या किसी तात्कालिक प्रक्रिया की उपज नहीं है. यह एक ऐसी विचारधारात्मक प्रक्रिया के विकास की परिणति है जिसमें देश के किसी भी अन्य नेता की तुलना में गांधी सर्वाधिक सशक्त बाधा थे. सिर्फ वैचारिक स्तर पर नहीं, जमीनी स्तर पर भी.
हिंदू महासभा जैसे संगठनों ने और सावरकरवादियों ने जिस कट्टर हिंदूवादी विचारधारा को विकसित किया था, उसने नफरत की भावना को इस हद तक बढ़ा दिया कि गांधी जैसे जनसेवक भी इस विचारधारा से प्रभावित लोगों को सबसे बड़े दुश्मन दिखाई देने लगे.
स्वाधीनता-पूर्व महाराष्ट्र में रूढ़िवादी ब्राह्मणों की एक ऐसी कट्टर धारा विकसित हुई जो उस चेतना को अपने लक्ष्य में सर्वाधिक बड़ी बाधा पाती है जिसका विकास गांधी कर रहे थे.

ये लोग सक्रिय तो हिंदुत्व के नाम पर थे लेकिन इनके मूल्य विशुद्ध ब्राह्मणवादी थे. पुस्तक के पहले खंड ‘लाल किले के गुनहगार’ में इन गुनहगारों के मानस के निर्माण में दक्षिणपंथी हिंदुत्ववादी शक्तियों की भूमिका का परिचय दिया गया है.
गांधी, आंबेडकर और मार्क्स में एक सिंथेसिस की संभावना को सिरे से नकारकर सिर्फ उनमें प्रतिपक्ष कायम करने वालों को इस तरह के तर्क बिल्कुल याद नहीं रहते.
गांधी में सिर्फ वर्ण व्यवस्था ढूंढने वाले यह सवाल पूछते नहीं दिखाई देते कि गांधी की राजनीति में ऐसा क्या था कि यह कट्टर समुदाय उन पर और मुख्यतः उन्हीं पर कई बार हमले के प्रयास करता है.
लेखक की दृष्टि में यह इसलिए हुआ क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम और बराबरी पर आधारित एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के निर्माण की गांधी की संकल्पना इन्हें नागवार गुजरी.
अशोक रेखांकित करते हैं कि हिंदू महासभा जैसे संगठन अंग्रेज उपनिवेशवादियों को अपना शत्रु नहीं समझते बल्कि सर्वधर्म समभाव से संचालित गांधी जैसे हिंदू को ही अपना शत्रु समझते हैं. इसीलिए मुस्लिम लीग जैसी दक्षिणपंथी अलगाववादी ताकत से मिलकर सरकारें बनाने में इन्हें संकोच नहीं होता क्योंकि दोनों की आकांक्षाओं में काफी समानताएं थीं.
इस तरह से यह पुस्तक इस देश के विभाजन में इन संगठनों को जिम्मेदार ठहराती है, जिसके मूल में इनकी अलगाववादी सांप्रदायिक चेतना और कुंठाग्रस्त नेताओं का स्वार्थ था.
इस प्रक्रिया में सावरकर और जिन्ना की भूमिकाओं को यह पुस्तक सबल प्रमाणों के साथ उद्घाटित करती है. यह पुस्तक पढ़ते हुए सहज ही लगता है कि गांधी के हत्यारों में से कई पर सावरकर का इतना प्रभाव था कि उन्हें सावरकरवादी कहकर ही संबोधित किया जाना चाहिए.
इसके साक्ष्य इस पुस्तक में कदम-कदम पर हैं. साथ ही जांच प्रक्रिया की सीमाओं को दिखाते हुए पुस्तक कपूर आयोग की रिपोर्ट का सार्थक विश्लेषण करते हुए सावरकर के बारे में ऐसे तथ्यों को सामने लाती है जो पाठक को प्रचारित दुविधाओं से मुक्त कर देता है.
स्वाधीनता आंदोलन में दक्षिणपंथी दलों की नकारात्मक भूमिका पर भी पुस्तक अच्छे से प्रकाश डालती है. यह पुस्तक गांधी की अहिंसा और सत्याग्रह जैसे शब्दों के उन पहलुओं पर विचार करने के लिए आकर्षित करती है जो सामान्यतः हम नहीं करते.
इन पदों के दार्शनिक अर्थ में गए बगैर इनका महत्व नहीं समझा जा सकता. गांधी के उपवास के दर्शन की व्याख्या कर उनकी राजनीतिक कार्यवाहियों के बारे में अशोक ने महत्वपूर्ण निष्कर्ष देने के प्रयास किए हैं जिन पर गंभीर बहस होनी चाहिए.
इसके साथ ही यह पुस्तक गांधी के भयमुक्त व्यक्तित्व और अपराजित चेतना के विभिन्न आयामों को बेहतरीन ढंग से उद्घाटित करती है.
लेखक ने दिखाया है कि अहिंसा को एक जीवन दर्शन बनाने के क्रम में गांधी ने कितने खतरे उठाए हैं और अपने विरोधियों पर भी भयरहित विश्वास के माध्यम से गांधी सत्याग्रह को कैसे एक बेजोड़ अस्त्र बना लेते हैं.
ऐसे प्रसंग पुस्तक में लाए गए हैं जो दिखाते हैं कि गांधी को अपने ऊपर हुए हमलों के पीछे के षड्यंत्रों की भी समझ थी लेकिन वे अपने तौर-तरीकों और आदर्शों को छोड़ने को तैयार नहीं थे.
लेखक इसी को विस्तार देते हुए सफलतापूर्वक गांधी हत्या को एक व्यक्ति की धुरी से हटाकर एक विचार की धुरी तक ले जाता है. इन सबके बाद भी ऐसा नहीं है कि गांधी की सीमाओं को नज़रअंदाज किया गया है.
इसके संकेत मिलते हैं पुस्तक में कि लेखक गांधीवादी राजनीति के कई पहलुओं से असहमति रखता है लेकिन पुस्तक की जैसी परिकल्पना है उसमें उसके लिए ज्यादा अवकाश उन्हें नहीं मिल पाता.
फिर भी, जीवन के आरंभिक दौर में अंग्रेजी हुकूमत के प्रति गांधीजी द्वारा किए गए सहयोगों, देश के अतीत और गांवों की उनकी समझदारी में विद्यमान अतार्किकताओं, वर्ण-व्यवस्था के बारे में एकपक्षीय और सीमाओं में कैद उनके नजरिये आदि पर भी छिटपुट चर्चा की गई है.
यह दिखाया गया है कि अफ्रीका में जो वे न कर सके उस भूल-सुधार की चेतना गांधी में बनी रही और राज्य के साथ सहयोग के अपने गलत निर्णय पर भी वे विचार करते रहे.
इस किताब की एक खास बात यह है कि यह बात तो अतीत की कर रही है लेकिन इसमें संवाद निरंतर वर्तमान से है. जिस तरह की घटनाओं-प्रसंगो को जाने-अनजाने महत्व दिया गया है, वे वर्तमान संदर्भ में मायने रखती हैं.
चीज़ों की व्याख्या के क्रम में भी वर्तमान की चेतना स्पष्ट प्रकट होती है. दाभोलकर और गौरी लंकेश किताब में आ ही जाते हैं. शीर्षक में ‘क्रोनोलॉजी’ शब्द का प्रयोग अनायास ही नहीं है.
इधर अफ्रीका में गांधी को ‘स्ट्रेचर बियरर ऑफ एम्पायर’ (अश्विन देसाई और गुलाम वाहिद) साबित करने के जो प्रयास हुए हैं, पुस्तक उससे भी संवाद करती है. सूरज येंगडे, पेरी एंडरसन और अरुंधति राय के हाल के तर्कों से भी लेखक दो-चार होता है.

किताब की एक खास बात यह भी है कि इसमें ढेर सारे ऐसे मुद्दे और प्रसंग हैं जिनका पुस्तक के मूल प्रश्न से संबंध न होते हुए भी जिन पर समानांतर चर्चा जारी रहती है.
लेखक रोचक ढंग से इन्हें साथ लिए चलता है क्योंकि वह उन विभिन्न जिज्ञासाओं और भ्रमों को अनछुआ नहीं रहने देना चाहता जो स्वाधीनता आंदोलन, उसके नेताओं, विशेषकर गांधी, के बारे में पिछले कुछ दशकों में तैयार कर दी गई हैं. इसका निर्वाह भी सफलता के साथ किया गया है.
उदाहरण के लिए, भगत सिंह को फांसी से गांधी क्यों नहीं बचा सके, नेहरू और पटेल की असहमतियों से क्या समझा जाए, छुआछूत के प्रति गांधी की क्या दृष्टि थी, हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने गांधी की मृत्यु पर कैसी प्रतिक्रियाएं दीं, आंबेडकर गांधी की मृत्यु का हिंदुस्तान पर क्या असर देखते थे, नाथूराम और सावरकर का संबंध कैसा था, सावरकर के माफीनामों की सूची कितनी लंबी है, अपने आखिरी वर्षों में गांधी कांग्रेस के बारे में क्या विचार रखते थे- जैसे अनेक प्रश्नों पर लेखक अपनी स्पष्ट राय देते हुए आगे बढ़ता है.
इन सभी प्रश्नों पर दुष्प्रचारों के माध्यम से जो बाइनरी तैयार की जाती है, लेखक उसे तोड़ता जाता है. सबसे अच्छी बात यही है कि किसी भी प्रश्न से बचकर निकल जाने की प्रवृत्ति कहीं नहीं है. इसके विपरीत उन प्रश्नों से जूझने की प्रवृत्ति है जो असहज कर देते हैं.
पुस्तक की एक विशेषता है इसकी पठनीयता. इस गंभीर विषय को भी कहीं भी बोझिल नहीं होने दिया गया है. कुछ हिस्से तो ऐसे हैं जिन्हें पटकथा में रूपांतरित किया जा सकता है, वह भी तब जब यह शोधपूर्ण पुस्तक प्रमाणों से भरी हुई है.
ऐसे प्रसंगों और उद्धरणों से पुस्तक को और पठनीय बनाया गया है, जो आपको सहज ही उद्वेलित कर देते हैं, भावुक कर देते हैं, क्रोधित कर देते हैं और कभी-कभी आश्चर्यचकित.
यह भी साफ दिखाई देता है कि यह किताब एक देश के प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा की भावना से युक्त संवेदनात्मक प्रवाह में लिखी गई है, इसलिए भाषा में वेदना और आक्रोश को थामे रखने की कोशिश भी जगह-जगह झलक जाती है.
यह चेतना जरूरी है ताकि पाठक को शोध के प्रति लेखक की तटस्थ चेतना का भान रहे. इसके बावजूद, लेखक एक-दो जगहों पर क्रोधित होकर संबोधन की शैली में आ जाता है (देखें पृ.215) जिससे एक शोधपरक पुस्तक में बचा जाना चाहिए.
अध्यायों का क्रम और विभाजन भी अत्यंत व्यवस्थित है. खंड 2 के दूसरे बिंदु के शीर्षक ‘अहिंसा और हमलों के बीच निर्भय जीवनः जनवरी 1948 से गांधी पर हुए हमले’ से अर्थ निकालना थोड़ा कठिन है क्योंकि जिन हमलों की चर्चा है वे सिर्फ 1948 के नहीं बल्कि गांधी के पूरे जीवन से हैं.
आखिरी पृष्ठों में जो दिशा पुस्तक को दी गई है वह मानीखेज है. अशोक कुमार पांडेय गांधी और स्वाधीनता आंदोलन के अन्य नेताओं से पूछे जा रहे दुष्प्रचारों से प्रभावित सवालों का उत्तर देने के बाद बहस को एक नई दिशा देते हुए वही और अन्य महत्वपूर्ण सवाल हिंदू महासभा, सावरकरवादियों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर उछाल देते हैं और पूछते हैं कि अब आप बताइए कि आपने इन सारे प्रश्नों के संदर्भ में अतीत में कौन से सार्थक हस्तक्षेप किए हैं? कुछ भी. एकाध…
(लेखक असम विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं.)