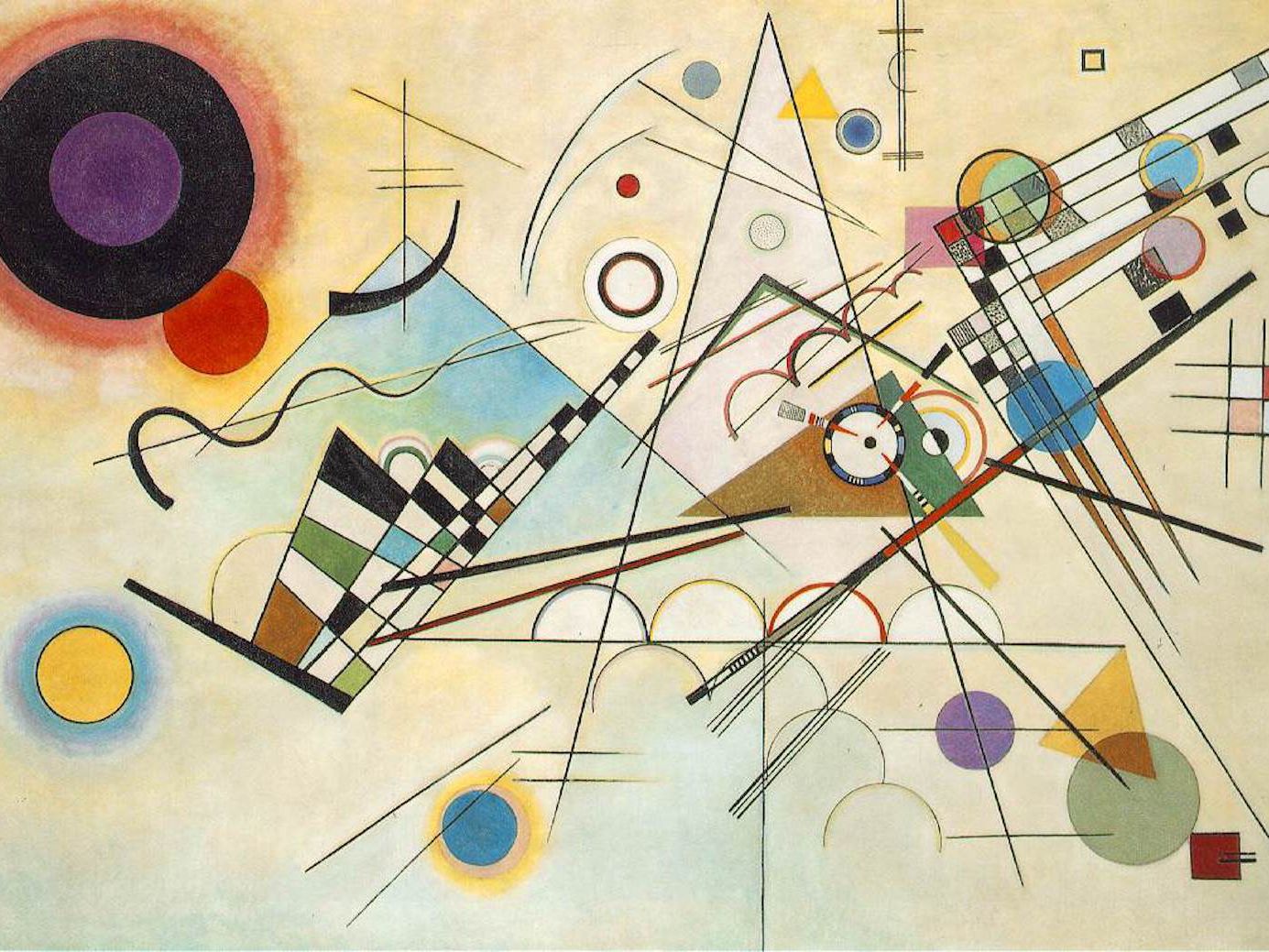बदसूरत से बदसूरत समय में जीवन में आस्था नहीं छोड़नी चाहिए. बदसूरती और नाइंसाफ़ी का दस्तावेज़ीकरण भी कितना ज़रूरी है. क्या हमारे दौर का भी दर्ज हो रहा है?

कल ही एक दोस्त से बात हो रही थी कि यह साल हम सबने किस किस तरह काटा है. उमर खालिद की गिरफ़्तारी के बाद हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी जब एक साथी ने अचानक पूछा कि कैसा चल रहा है तो क्षण भर के लिए मैं निरुत्तर हो गई थी.
सवाल याद है, लेकिन उस वक्त का अपना जवाब ठीक-ठीक याद नहीं है. शायद अपने को संयत करते हुए मैंने कहा था कि साहित्य-कविता और काम ने दिलोदिमाग को ठिकाने पर रखा है. उसमें प्यार को भी जोड़ती हूं अब.
नाटककार रतन थियाम की छोटी-सी मणिपुरी भाषा की कविता ‘चौबीस घंटा’ (अनुवाद: उदयन वाजपेयी) याद आई
समय को चौबीस घंटों ने
जकड़ रखा है
सुकून से बात करना है तो
चौबीस घंटों के बाहर के
समय में तुम आओ
मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा
बीते हुए समय को
अभी के समय में बदलकर
पहली मुलाक़ात के
क्षण से शुरू करें !
अपूर्व तो सख्त हो गई ज़मीन को अपनी छेनी से हर रोज़ कोड़ते जा रहे हैं, प्रेमचंद ने जो न्याय, विवेक, प्रेम और सौहार्द की खेती की बात की है उसे मानकर. मैं उस यकीन पर यकीन करने के लिए अपने को तैयार करती रहती हूं.
अमेरिकी कवयित्री लुइस ग्लूक, जो 2020 की साहित्य की नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, उनकी ‘अक्टूबर’ शृंखला की कविता की कुछ पंक्तियां बार-बार फ़्लैश करती हैं –
फिर से शीतऋतु, फिर ठंड
…
क्या वसंत के बीज रोपे नहीं गए थे
क्या रात खत्म नहीं हुई थी
…
क्या मेरी देह
बचा नहीं ली गई थी, क्या वह सुरक्षित नहीं थी
क्या ज़ख्म का निशान अदृश्य बन नहीं गया था
चोट के ऊपर
दहशत और ठंड
क्या वे बस खत्म नहीं हुईं,
क्या आंगन के बगीचे की
कोड़ाई और रोपाई नहीं हुई
और पापा (नंदकिशोर नवल) हर तरफ़ दिखाई पड़ते हैं. ढांढ़स देनेवाली उनकी आवाज़ तो अब नहीं सुनाई पड़ेगी, न ही अब वे मेरे अनमनेपन को समझ पाएंगे, मगर उनके लिखे शब्द मेरे मनोभाव को पकड़ रहे हैं.
उनकी एक छोटी-सी कविता है ‘दुख’ (हालांकि वे कभी अपने रहते ऐसा नहीं बोलते थे)
जिसे किसी ने नहीं
तोड़ा था –
उसे भी इस दुख ने तोड़
दिया है,
जिसने किसी को नहीं
छोड़ा था,
उसने खुद को
छोड़ दिया है.
इब्ने इंशा की ‘इंतज़ार की रात’ की पंक्तियां फिर लहर मारती हैं –
उमड़ते आते हैं शाम के साये
दम-ब-दम बढ़ रही है तारीकी
एक दुनिया उदास है
…
वो चला कारवां सितारों का
झूमता नाचता सू-ए-मंज़िल
वो उफ़क़ की जबीं दमक उट्ठी
वो फ़ज़ा मुस्कराई, लेकिन दिल
डूबता जा रहा है- जाने क्यों ?
जवाब चे ग्वेरा की कविता ‘ये तानाशाह’ में शायद है जिनको हिंदी में ढाला है सर्वेश्वरदयाल सक्सेना ने-
उन गन्नों में अभी भी एक बू बसी हुई है
खून और जिस्म का घोल,
एक पंखुरी बेधती, उबकाई आती है.
नारियल के दरख्तों के नीचे
कब्रें भरी हुई हैं तबाह हड्डियों और
ख़ामोश बेज़बान मौत की सरसराहटों से.
नाजुक तानाशाह बात कर रहा है
जहन्नुम से, सुनहरे फ़ीते और पट्टे लगाए
यह पिद्दी महल घड़ी की तरह चमकता है
और दस्ताने पहने तेज़ कहकहे
अक्सर गलियारे पार कर
मृत आवाज़ों
और ताज़े दफ़न नीले चेहरों में जा मिलते हैं.
वह रोना नहीं दिखाई देता, उस पौधे
की तरह जिसके बीज धरती पर
बेहिसाब गिरते जाते हैं
जिसकी बड़ी अंधी पत्तियां
बिना रोशनी के भी उगती बढ़ती जाती हैं.
एक एक क़दम करके नफ़रत बढ़ती है
चोट पर चोट करती
ख़ामोश चुचुआता थूथन लिए
इस दलदल के बदबूदार भयावह पानी में.
ऐसे में हंगरी के कवि इश्तवान अर्शी का यह कहना कि ‘अपना ख़्याल रखना’ भूलता नहीं. तभी तो रघुवीर सहाय ने इसका अनुवाद करना जरूरी समझा था. मैंने कोविड का आघात झेल रहे कई दोस्तों को भेजी यह कविता-
जब चीज़ें ऊपर को गिरने लगें, नीचे नहीं
सूरज गरमाई रख ले अपने वास्ते
तब दुनिया का कगार पकड़े रहना प्यारी
अपना ख़्याल रखना.
और मैंने भवानीप्रसाद मिश्र की ‘बेदर्द’ कविता का जाप किया-
मैंने निचोड़कर दर्द
मन को
मानो सूखने के ख़याल से
रस्सी पर डाल दिया है
और मन
सूख रहा है
बचा-खुचा दर्द
जब उड़ जाएगा
तब फिर पहन लूंगा मैं उसे
मांग जो रहा है मेरा
बेवकूफ़ तन
बिना दर्द का मन!
इस दौरान मैंने कई नई-पुरानी, देशी-विदेशी फिल्में देख डालीं. निर्देशक सत्यजित रे, माजिद मजीदी (ईरानी) की सिनेमाई टिप्पणी की दूरदर्शिता पर चर्चा की.
‘लूडो’ या ‘डॉली किट्टी और वो चमकते सितारे’ जैसी चर्चित फिल्मों की समीक्षा कर डाली जिनमें संवेदनशील मुद्दों को सतही ढंग से उठाने और बाज़ार में बिकने के लिए अनावश्यक विवरण डालने पर मेरा ऐतराज़ था.
‘मिर्ज़ापुर’ जैसी वेब शृंखला में यौनिकता और हिंसा के यथार्थ को जिस तरह पेश किया जाता है उससे ऐसा लगता है कि आसपास कुछ भी सुंदर नहीं बचा है. मानो चारों तरफ सबकुछ तबाह होता जा रहा है.
परतदार जटिलता का यह मतलब कतई नहीं कि किसी भी तरह के ईमानदार व्यवहार की उम्मीद छोड़ दें हम. ऐसे में नाज़ी दौर के बारे में ‘Playing for Time’, ‘The Photographer Of Mauthausen’ ‘Schindler’s List’ जैसी फिल्में बताती हैं कि बदसूरत से बदसूरत समय में जीवन में आस्था नहीं छोड़नी है.
बदसूरती और नाइंसाफ़ी का दस्तावेजीकरण भी कितना जरूरी है! क्या हमारे दौर का भी दर्ज हो रहा है?
यथार्थ से कैसा रिश्ता हो हमारा? पुर्तगाली कवि फ़र्नान्दो पेसोवा (1888-1935) की एक कविता शृंखला है ‘भेड़ों का रखवाला.’ उसकी 9 वीं कविता यथार्थ, सत्य और खुशी के त्रिकोण की तरफ इशारा करती है-
मैं भेड़ों का रखवाला हूं .
भेड़ें हैं मेरे विचार
और हर विचार एक संवेदना.
मैं सोचता हूं अपनी आंखों से और अपने कानों से
और अपने हाथों और पैरों से
और अपनी नाक और अपने मुंह से.
एक फूल को सोचना है उसे देखना और सूंघना
और एक फल को खाना है उसके मायने जानना.
यही वजह है कि किसी एक गर्म दिन
जिससे मैं इतना आनंदित होता हूं
मैं उदास महसूस करता हूं,
और मैं घास पर लेट जाता हूं
और अपनी गरमाई आंखें मूंद लेता हूं,
तब मैं महसूस करता हूं अपनी लेटी हुई पूरी देह यथार्थ में,
मैं सत्य को जानता हूं, और मैं खुश हूं.
मंगलेश डबराल ठीक ही लिखकर गए –
निराशा में हम कहते हैं
निराशा हमें रोटी दो.
हमें दो चार क़दम चलने
की सामर्थ्य दो.
और हमको वे बता गए –
मैं चाहता हूं कि स्पर्श बचा रहे
वह नहीं जो कंधे छीलता हुआ
आततायी की तरह गुज़रता है
बल्कि वह जो एक अनजानी यात्रा के बाद
धरती के किसी छोर पर पहुंचने जैसा होता है
मैं चाहता हूं स्वाद बचा रहे
मिठास और कड़वाहट से दूर
जो चीज़ों को खाता नहीं है
बल्कि उन्हें बचाए रखने की कोशिश का
एक नाम है
एक सरल वाक्य बचाना मेरा उद्देश्य है
मसलन यह कि हम इंसान हैं
मैं चाहता हूं इस वाक्य की सचाई बची रहे
सड़क पर जो नारा सुनाई दे रहा है
वह बचा रहे अपने अर्थ के साथ
मैं चाहता हूं निराशा बची रहे
जो फिर से एक उम्मीद
पैदा करती है अपने लिए
शब्द बचे रहें
जो चिड़ियों की तरह कभी पकड़ में नहीं आते
प्रेम में बचकानापन बचा रहे
कवियों में बची रहे थोड़ी लज्जा.
ऑडियो क्लिप में सुरक्षित नानाजी– पं. रामगोपाल शर्मा का स्वर बार-बार सुनती हूं. उनकी यह कविता ‘बंधु! जरूरी है’ मां भी गाती थी, मौसी भी. जब भी मन उचाट हो यह टेक ‘बंधु ! जरूरी है मुझको घर लौटना, एक मुझे भी ले लो अपनी नाव पर‘ सहारा देती है.
बंधु! जरूरी है मुझको घर लौटना,
एक मुझे भी ले लो अपनी नाव पर
देर तनिक हो गई वहां, बाजार में,
मोल-तोल के भाव और व्यवहार में ;
आईना था एक अनोखी आब का,
इन्द्रजाल-सा था जिसके दीदार में ;
मैं गरीब ले सका न अपने भाव पर
सनक नहीं तो क्या कहिए, इस ठाट को –
कौड़ी लेकर साथ, चला था हाट को,
जहां प्रसाधन बिकते हैं शृंगार के! –
कौन पूछता मुझ-जैसे बेघाट को?
पड़ता रहा नमक ही मेरे घाव पर!
दूर फ़िलीस्तीन से महमूद दरवेश अपनी ‘उदासीन बंदा’ शीर्षक कविता में उदासीनता का दर्शन समझाते हैं-
उसे किसी चीज़ से फ़र्क़ नहीं पड़ता. अगर वे उसके घर का पानी काट दें,
वह कहेगा, ‘कोई बात नहीं, जाड़ा क़रीब है.’
और अगर वे घंटे भर के लिए बिजली रोक दें वह उबासी लेगा:
‘कोई बात नहीं, धूप काफ़ी है’
अगर वे उसकी तनख़्वाह में कटौती की धमकी दें, वह कहेगा,
‘कोई बात नहीं! मैं महीने भर के लिए शराब और तमाखू छोड़ दूंगा.’
और अगर वे उसे जेल ले जाएं,
वह कहेगा, ‘कोई बात नहीं, मैं कुछ देर अपने साथ अकेले रह पाऊंगा, अपनी यादों के साथ.’
और अगर उसे वे वापस घर छोड़ दें, वह कहेगा,
‘कोई बात नहीं, यही मेरा घर है.’
मैंने एक बार गुस्से में कहा उससे, कल कैसे रहोगे तुम?’
उसने कहा, ‘कल की मुझे चिंता नहीं. यह एक ख़याल भर है
जो मुझे लुभाता नहीं. मैं हूं जो मैं हूं: कुछ भी बदल नहीं सकता मुझे, जैसे कि मैं कुछ नहीं बदल सकता,
इसलिए मेरी धूप न छेंको.’
मैंने उससे कहा, ‘न तो मैं महान सिकंदर हूं
और न मैं (तुम?) डायोजिनिस’
और उसने कहा, ‘लेकिन उदासीनता एक फ़लसफ़ा है
यह उम्मीद का एक पहलू है.’
तब भी अमेरिकी कवि चार्ल्स बुकोव्स्की की ‘सुरक्षित’ कविता की इन पंक्तियों पर मन अटका रह जाता है-
बगल का घर मुझे
उदास करता है.
लोग भले लोग हैं, मैं उन्हें
पसंद करता हूं.
लेकिन मैं महसूस करता हूं उन्हें डूबते हुए.
और मैं उन्हें बचा नहीं सकता.
वे जी रहे हैं.
वे
बेघर नहीं हैं.
लेकिन इसकी कीमत
भीषण है.
रोमानियाई कवयित्री आना ब्लांडिआना (मूल नाम : ओतेलिया वालेरिया कोमां) की ‘चीख़’ कविता में मुझे विषम परिस्थिति से निपटने का सूत्र मिलता है-
भले ही ठहाके हों या आंसू,
इनसे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता :
ज़रूरी चीज़ है चीख़.
उसके साथ चाहिए ‘कॉमन सेंस’. इसी शीर्षक से कवि एलन ब्राउनजॉन (Alan Brownjohn) की कविता टेरी इग्लटन की किताब ‘हाउ टू रीड अ पोएम’ में संकलित है.
दिल्ली की सिंघु सीमा और टिकरी सीमा पर अपनी मांगों को लेकर बैठे हजारों-लाखों किसानों को खबर सुनकर जो विचलित नहीं हुआ, जिसने उनकी ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचा वह कैसा इंसान है? एलन ब्राउनजॉन की ये पंक्तियां भारत के संदर्भ में क्या प्रासंगिक नहीं हैं?
एक खेतिहर मजदूर, जिसके
एक बीवी और चार बच्चे हैं, पाता है 20 शिलिंग एक हफ्ते के.
¾ से आता है भोजन, और परिवार के सदस्य
तीन शाम खाना खाते हैं प्रतिदिन.
तो फिर प्रति व्यक्ति प्रति खुराक कितना पड़ा?
-पिटमैन्स कॉमन सेन्स अरिथमेटिक,1917 से
…
नीचे दी गई तालिका में संख्या दी हुई है
गरीबों की यूनाइटेड किंगडम में, और
पूरा खर्च गरीबों को दी जाने वाली राहत का.
तो पता करो औसत संख्या
गरीबों की प्रति दस हज़ार व्यक्ति.
– पिटमैन्स कॉमन सेन्स अरिथमेटिक, 1917 से
क्या कवि ज्ञानेंद्रपति की ‘अधरात घास-गन्ध’ की बात को हम नहीं दोहरा सकते हैं?
क्या हम सब
अपने-अपने घर में बंद
अधरात अचानक
हवा में घास की गन्ध आने से
सिहरते रहेंगे चुपचाप
स्तब्ध
कि अब सुनाई देगा कोई साइरन
बजेगी कोई ख़तरे की घंटी
कि हम कहेंगे
बहुत बज चुकी ख़तरे की घंटी
अपने-अपने घर से बाहर आ
यह एक मुट्ठी की तरह कसने का वक़्त है
विषबेलमुंड से चिकने चमकीले
इस लोकतंत्र नहीं लोभतंत्र को फोड़ने का वक़्त है
इन सबके अलावा चोट, बीमारी, मृत्यु, अनुपस्थिति, उदासी को झेलने की मेरी ढाल है काम.
लेखन, संपादन, प्रशिक्षण के पेशेवर काम के साथ साथ मेरा समय जाता है नर्सरी से फूल-पौधे लाने, उनके लिए धूप-छांव का हिसाब-किताब रखने, घर पर सब्जी के काटन से खाद बनाने और नीम की खली के इस्तेमाल जानने के लिए गूगल खोज में.
रसोई में बेमन से भात-दाल बनाने से लेकर उत्साह से अपने हाथ का बाजरे का खिचड़ा, मशरूम सूप, चुकंदर का हलवा खाने में. 5 लीटर सैनिटाइज़र (लिक्विड और जेल दोनों) के डिब्बे से निकालकर छोटी-छोटी शीशियां भरने में.
बाहर से आए सामान को घंटों पड़े रहने के बाद धोने-धुलवाने, पोंछने-पोंछवाने में. वाशिंग मशीन से निकले अंतहीन कपड़ों को फैलाने में.
कपड़ों की तो पूछिए मत. समाज में जो स्तरीकरण है और छुआछूत है वो अभी समझ आएगा. कौन कहां रखा जाएगा और किस कपड़े के साथ सटेगा, किस कपड़े के साथ दो फुट की दूरी पर रहेगा, इसकी चौकसी बड़ी कठिन है.
उनमें मास्क की कथा अलग है. कुछ-कुछ अधोवस्त्र (अंडरगारमेंट- शब्द की चीर-फाड़ फिर कभी) की तरह है. सबका अपना-अपना, अलग-अलग. सब धुलेगा और सूखेगा भी अलग-अलग. एक का रंग दूसरे रंग पर न चढ़े. कोई किसी और का इस्तेमाल किया हुआ न पहने.
सूती कपड़े का सबसे अच्छा है. टिकाऊपन भी मायने रखता है. फिटिंग को भी नज़र अंदाज़ नहीं कीजिए. एक सज्जन आए तो उनका मास्क छोटा लग रहा था, खिसक रहा था और ऐसा लग रहा था मानो छोटा जांघिया दाढ़ी पर लग गया है.
आपने धो-धोकर घिस दिया है मास्क को या उसका रंग फीका पड़ गया है तो उस बदरंग, बदशक्ल को फौरन बदल डालिए. मास्क के डिजाइन की तो क्या बात की जाए.
ज़फ़र जहां बेगम के शब्दों को उधार लें तो ‘अमूमन फैशन की वबा रोज़ बरोज़ तरक़्क़ी पर है… बस काम में काम है तो सिर्फ’ मास्क ‘की तराश खराश से कि सुबह को एक वज़ा है तो शाम को दूसरी. नए नए तर्ज़ से’ मास्क ‘बनाए जा रहे हैं.’ मास्क लगाने वालों का अंदाज़ भी जुदा जुदा है.
खैर, अब रुकना होगा. कविता तो नहीं, कुछ काम है जो मुझे पुकार रहा है.
(लेखक शिक्षा और लैंगिक समानता के क्षेत्र में काम करती हैं.)