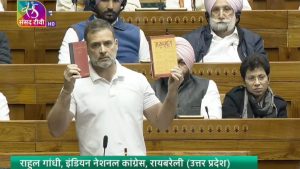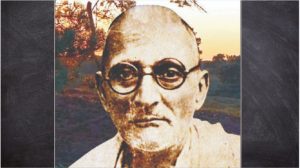1971 रिवाइंड: पचास साल बाद भी हृषिकेश मुखर्जी का ‘आनंद’ भाषा, जाति, मज़हब की हदों के परे जाकर उसी तरह ख़ुशियां लुटा रहा है.

भारतीय इतिहास के कैलेंडर में 1971 के नाम कई बड़ी जीतें दर्ज हुईं- सियासत हो, क्रिकेट या फिर जंग. भारत के लिए इन सबका दूरगामी नतीजा निकलनेवाला था. भले ही भारत घरेलू मोर्चे पर कई समस्याओं से जूझ रहा था, लेकिन फिर भी देश एक नई उमंग से भरा हुआ था.
50 सालों के बाद हम मुड़कर उस समय को देख रहे हैं और उसका अक्स उभारने की कोशिश कर रहे हैं. लेखों की एक श्रृंखला के तहत नामचीन लेखक उन महत्वपूर्ण घटनाओं और प्रक्रियाओं को याद करेंगे जिन्होंने एक जवान, संघर्षरत मगर उम्मीदों से भरे भारत पर अपनी छाप छोड़ने का काम किया.
§
हाल ही में आनंद को फिर से देखना एक अलहदा फिल्म को देखने के अनुभव सरीखा था. कहानी वही थी, दो अस्वाभाविक दोस्तों की. डॉक्टर भास्कर बनर्जी (अमिताभ बच्चन)- एक डॉक्टर और आनंद शीर्षक से एक किताब के लेखक और आनंद (राजेश खन्ना) जिसकी जीवन लीला कैंसर से समाप्त होने वाली है, मगर जो जीवन में बचे हर क्षण का आनंद लेना चाहता है. यह भास्कर और आनंद के बीच के रिश्ते की कहानी है.
इस फिल्म में हंसी को सर्वश्रेष्ठ दवाई के तौर पर दिखाया गया है. दो मेडिकल डॉक्टरों, डॉ. भास्कर और डॉ. कुलकर्णी का जीवन अपने ढंग से चल रहा है. डॉक्टर भास्कर को लगता है कि सबसे बड़ी बीमारी है गरीबी, जिसका वह इलाज नहीं कर सकता है. जबकि डॉक्टर कुलकर्णी ज्यादा व्यावहारिक है और अमीर रोगियों, जिन्हें रोग से ज्यादा रोग का भ्रम है, को रंग-बिरंगी मीठी गोलियां देकर उनसे पैसे लेने में संकोच नहीं करता. सिनेमा मेडिकल नैतिकता की बहसों के फेर में नहीं फंसता. यहां दवाई वास्तव विज्ञान की जगह एक रूपक है.
कैंसर को बाकी सभी अन्य रोगों की तुलना में लाइलाज बताया गया है. आज यह बात थोड़ी पुरानी लग सकती है. आनंद को जो कैंसर है वह करोड़ों में एक को होने वाला कैंसर है, लेकिन भारतीय फिल्मों के सभी प्रशंसकों को इसके बारे में पता है- ‘लिंफोसरकोमा ऑफ द इनटेस्टाइन।’
सिनेमा का एक संदेश यह है कि लोगों को भरपूर जीवन जीना चाहिए (जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं) ऑन्कोलोजिस्ट (कैंसर विशेषज्ञ) भास्कर आनंद को बचा नहीं सकता, लेकिन आनंद उसे जीवन देता है और उसके नाम से छपने वाली एक किताब. (यह आश्चर्यजनक नहीं है कि एक डॉक्टर होने का दिखावा करनेवाला हुए मुन्ना भाई एमबीबीएस एक मरीज के मस्तिष्क का एक्स-रे देखते हुए रोग की पहचान लिंफोसरकोमा ऑफ द इंटेस्टाइन के तौर पर करता है, क्योंकि शायद इसी एक बीमारी का नाम उसे पता है. मुन्ना रोगियों को जादू की झप्पी का नुस्खा बताता है और इस तरह से एक बार फिर यहां दिखाया गया है कि मरीज के लिए दवाइयों से ज्यादा महत्व स्नेह भरे देखभाल का है.)

हालांकि हमारा सामना कुछ डरावने अस्पताल उपकरणों से होता है, लेकिन आनंद काफी स्वस्थ दिखता है और आंत के कैंसर के किसी भी अप्रिय लक्षणों को नहीं दिखाता है. वह एक एक सुंदर और पूरी तरह से मेलोड्रामा से भरी मौत को प्राप्त करता है.
मेडिकल संबंधी संदर्भ ज्यादातर बस एक प्लॉट आगे बढाने की तरकीब है, क्योंकि ज्यादातर दर्शकों के लिए यह फिल्म दो पुरुष सितारों के बीच के स्नेहपूर्ण रिश्ते के बारे में है. अपने शिखर पर खड़े राजेश खन्ना अपनी सर्वाधिक यादगार भूमिकाओं में से एक में एक सितारे के तौर पर अपनी छटा बिखेर रहे हैं, जबकि अमिताभ बच्चन उस समय लगभग अनजान थे.
मध्यवर्गीय हिंदी सिनेमा में बच्चन की भूमिका को मुख्यधारा के सिनेमा में उनके काम ने ढक लिया है. आनंद ज़ंजीर से सिर्फ दो साल पहले और शोले और दीवार से सिर्फ चार साल पहले बनाई गई थी. बच्चन को एक बंगाली के तौर पर अच्छी भूमिका दी गई है (हालांकि वे अपनी डायरी हिंदी में लिखते हैं). जया भादुड़ी से शादी करने से पहले उन्होंने कलकत्ता में काम किया था. भादुड़ी का करिअर सत्याजित रे के साथ शुरू हुआ था और उन्होंने हृषिकेश मुखर्जी के साथ बेहतरीन काम किया.
खन्ना, जो उस समय एक सनसनी के मानिंद थे यहां काफी धूमधाम के साथ एक शानदार स्टार एंट्री करते हैं. उन्हें देखकर मेरे अंदर उठकर ताली बजाने की इच्छा जाग गई. अपनी किताब हंड्रेड बॉलीवुड फिल्म्स में मैंने बच्चन द्वारा अपने भावावेग से राजेश खन्ना पर छा जाने के बारे में लिखा था, लेकिन अब मैं इस बारे में इतनी निश्चित नहीं हूं.
बच्चन का अभिनय असाधारण है : काफी गैर-फिल्मी, संवेदनशील और अर्थपूर्ण. उनका चरित्र देवदास की तरह नहीं था, क्योंकि यहां आत्मध्वंस का कोई तत्व नहीं है, न ही वे अपने विजय के किरदार की तरह एंग्री यंग मैन हैं, क्योंकि यहां उनका गुस्सा अन्याय और गरीबी को लेकर है, न कि किसी के द्वारा उनके परिवार के साथ किए गए किसी सुलूक को लेकर.
खन्ना पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति हैं, या कहें ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें आप अपना पड़ोसी बनाना चाहते, जो एक खास तरह से अपनी पलकें झपकाते और माथा एक झटकते थे, लेकिन हमेशा दिलकश लगते थे. वे एक कस्बाई नायक थे (हालांकि खुद काफी नफीस थे,) जो हिंदी उपन्यास से बाहर निकला था. आनंद में जिस चीज ने मेरा ध्यान खींचा वह थी नाचे बगैर गाने को निभा पाने की उनकी आश्चर्यजनक क्षमता. गाने के बोल पर अपने होंठ मिलाने के वक्त चलते और मुद्रा बनाते हुए मूर्ख न दिखना ज्यादा कठिन है.
यह कह देना आसान है कि उन्हें अच्छे संगीत का साथ मिला, लेकिन जिस तरह से उन्होंने गानों को निभाया वह काबिलेतारीफ़ है.
कहा जाता है कि यह फिल्म राज कपूर के साथ हृषिकेश मुखर्जी की दोस्ती से प्रेरित थी. डॉक्टर के तौर पर बच्चन का किरदार निर्देशक पर आधारित था (यहां तक कि आनंद डॉक्टर को बाबू मोशाय भी कहता है जो कि मुखर्जी के लिए कपूर का नाम था) जबकि आनंद, कपूर थे. निश्चित ही आनंद में एक अपरिपक्व लेकिन उल्लास से भरे हुए पुरुष की कई चारित्रिक विशेषताएं हैं, जिसे कपूर और अपनी कई शुरुआती भूमिकाओं में शाहरुख खान समेत कई दूसरों ने पर्दे पर निभाया है.
ललिता पवार मिसेज डीसा- कड़क मगर दयालु नर्स- के तौर पर एक तरह से अपनी भूमिका दोहराती हैं (मुखर्जी के निर्देशन में 1959 में बनी अनाड़ी में भी वे मिसेज डीसा बनी थीं). राजकपूर के अभिनय से सजी इस फिल्म में मुखर्जी के स्टाइल के कई तत्व हैं.
आनंद के लिए मुखर्जी की अभिनेताओं की पहली पसंद बहुत अटपटी लग सकती है- आनंद के तौर पर किशोर कुमार और डॉ. भास्कर के तौर पर महमूद. कहानी यह है कि एक स्टेज शो को लेकर किशोर कुमार की एक बंगाली प्रस्तुतकर्ता से लड़ाई हो गई इसलिए उन्होंने अपने दरबान से किसी बंगाली को घर के अंदर नहीं आने देने के लिए कहा. दरबान ने हृषिकेश मुखर्जी को वह बंगाली समझ लिया…
गुलजार जो पंजाबी होने के बावजूद बंगाली समूह में बाद में शामिल हुए, ने इस फिल्म में एक अहम भूमिका निभाई. कहानी के सह-लेखन के साथ-साथ, दोहराए जा सकने लायक शानदार डॉयलॉग, कुछ गाने और डॉक्टर द्वारा सुनाई जाने वाली कविता ‘मौत एक कविता है’ के लेखन तक में उनकी भूमिका रही.
आनंद में शब्द इतने कीमती हैं कि टेप रिकॉर्डर साथ-साथ कहानी को आगे बढ़ाते हैं. सुमन (सीमा देव) को आनंद के प्रेम प्रसंग, जिसे उसने समाप्त कर दिया, की जानकारी टेप रिकॉर्डर से मिलती है (जैसे अमन माथुर (शाहरुख खान) कल हो न हो (2003) में यह जानने के बाद कि वह मरने वाला है, अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर देता है). इसी तरह से सिनेमा के अंत में आनंद की अपनी रिकॉर्डिंग उसे मृत्यु के बाद भास्कर से बात करने की इजाज़त देती है.
देखने में यह फिल्म कहीं-कहीं समस्यादायक नजर आती है. यह काफी गैर फिल्मी है और इसमें काफी कठोर और उबाऊ लाइटिंग का इस्तेमाल किया गया है जो राजेश खन्ना की त्वचा के रंग को चित्तीदार और अमिताभ बच्चन को विषादमय बना देती है. इनडोर लोकेशन ज्यादातर गैरनाटकीय और भूल जाने लायक हैं, जो पूरी फिल्म के दौरान शानदार आउटडोर दृश्यों के सामने और ज्यादा अखरते हैं.
सिनेमा का संगीत सलित चौधरी के ऊचे मानकों के हिसाब से भी शानदार है. इन गानों में सबसे लोकप्रिय ‘कहीं दूर जब’ मुकेश की आवाज में गाया गया जो कि एक सदाबहार गीत रहा है और जिसे कई लोगों ने फिर से रिकॉर्ड किया है, जिसमें जगजीत सिंह भी शामिल हैं.
असली गाना बंगाली का अमाय प्रोश्नो करे तबसे 20 साल पहले हेमंत कुमार की आवाज में गाया गया था (इसका एक बहुत प्यारा संस्करण खुद सलिल दा की आवाज में है).
ऐसा जान पड़ता है कि इस गाने के लिए मुकेश को चुनने के कारण हेमंत कुमार और सलिल चौधरी में संबंध विच्छेद हो गया था. चौधरी इस गाने में मुकेश की आवाज से खास किस्म की करुणा का समावेश करना चाहते थे.
मुझे ये तीनों संस्करण प्यारे लगते हैं क्योंकि हर गायक क अपनी विशिष्टता है और संगीतकार-गीतकार सलिल दा को खुद यह गीत गाते हुए सुनना शानदार अनुभव है. इस गाने के फिल्मांकन में आनंद बंबई के मशहूर सूर्यास्त को देख रहा है, लेकिन महसूस कर रहा है कि कोई चीज उसे एक अलौकिक ढंग से छू रही है और उसे अतीत की याद दिलाती है. अंत में भास्कर आता है और और उसे वापस धरती पर ले आता है.
योगेश द्वारा ही लिखा गया दूसरा हिट गाना मन्ना डे की आवाज में ‘ज़िंदगी कैसी है पहेली’ प्रफुल्लित और उमंग भरा है, जो आज तक लोकप्रिय बना हुआ है. जुहू बीच पर यह गाना मेरे ख्याल से तब फिल्माया गया जब वहां भीड़ कम थी, आकाश में गुब्बारे उड़ रहे थे. यह एक छुट्टी का गीत है, लेकिन अपने शब्दों के जरिये यह जीवन के रहस्य को दिखलाता है.
गुलज़ार ने बाकी गानों के बोल लिखे, जिसमें मुकेश द्वारा गाया गया मेरा पसंदीदा गाना ‘मैंने तेरे लिए’ भी शामिल है. यह गाना पियानो पर बैठकर गाया गया है, हालांकि इसके साउंड ट्रैक में कोई पियानो नहीं है. यह सपनों और छोटी-छोटी चीजों के जरिये रोज-ब-रोज के जीवन में सुंदरता लाने के बारे में है.
एक को छोड़कर बाकी सभी गाने आनंद पर फिल्माए गए हैं जो इस फिल्म के सितारे के तौर पर और उस व्यक्ति के तौर पर जिसके आंतरिक जीवन का हम पीछा कर रहे हैं, उसकी स्थिति पर मुहर लगाते हैं. ये गाने ख़ुशी और उत्साह से हमेशा भरे रहने वाले आनंद को अपने अंतर्जगत को अर्थपूर्ण तरीके से अभिव्यक्त करने में मदद करते हैं, हालांकि यह उसके पर्दे पर आमतौर पर चित्रित स्वभाव से भिन्न है.
हो सकता है कि मैं ध्यान न दे पाई हूं, लेकिन बंबई आने से पहले आनंद क्या करता था? ऐसा एहसास होता है कि वह रेडीमेड आता है- दयालु, और इस तरह से लोगों की मदद और खुशी बांटने की कोशिश करता हुआ कि वह वास्तविक नहीं लगता है. वह किसी देवदूत की तरह है, जैसा कल हो न हो में अमन है.
भास्कर को कोई गाना नहीं मिला है, लेकिन खुशकिस्मती से हमारे पास सलिल चौधरी और लता मंगेशकर की जुगलबंदी में ‘ना जिया लागे न’ है, हालांकि यह अरुचिपूर्ण तरीके से रेणु (सुमिता सान्याल) पर उनके घर को ठीक करते हुए फिल्माया गया है.
बंगाली में मूल गाना ना मोन लागे न है, जिसका गीत और संगीत दोनों सलिल चौधरी का दिया हुआ है. यह भी हिंदी वाले गीत ही की ही तरह बेहद कर्णप्रिय है.
चौधरी 1950 के दशक में बिमल रॉय और अन्यों, जिनमें हृषिकेश मुखर्जी भी शामिल थे, के साथ बंबई आनेवाले बंगाली समूह का हिस्सा थे. इनमें से कई कलकत्ता में न्यू थियेटर्स से आए थे. हृषिकेश मुखर्जी बॉम्बे में बिमल रॉय की पहली फिल्म लेखक थे. कलकत्ता में अवस्थित दो बीघा जमीन (1953) की कहानी चौधरी ने लिखी और उसे मुखर्जी ने एडिट किया.
मुखर्जी ने 1957 में मुसाफिर से अपनी फिल्मों का निर्देशन शुरू किया और 1950 से 1970 के दशक तक सभी बड़े सितारों के साथ काम किया. वे खुद ऑल इंडिया रेडियो पर सितारवादक थे. उनकी फिल्मों में कुछ बेहद शानदार संगीत है, जिसमें रविशंकर द्वारा अनुराधा (1960) के लिए दिया गया संगीत भी शामिल है.
उन्होंने बिमल रॉय के साथ संपादन का काम जारी रखा. बाद में रामू करियत निर्देशित मलयाली फिल्म चेम्मीन (1965) जैसी क्लासिक फिल्मों के निर्देशकों और मनमोहन देसाई की कुली (1983) को भी अपना योगदान दिया. उनकी सभी फिल्में मुख्यधारा के सितारों और गानों का इस्तेमाल करते हुए भी मध्य वर्ग और उच्च मध्यवर्ग के मुद्दों और मूल्यों को जिस तरह से उठाती हैं, वैसा बाद के वर्षों में बहुत कम फिल्मों में देखा गया. यह बात दीगर है कि आज की हिंदी फिल्में इस शैली का हिस्सा हैं.
यह मध्यवर्गीय सिनेमा करीबी तौर पर बंबई में काम करने वाले बंगालियों से जुड़ा है, जिसने बंगाली भद्रलोक को मध्यवर्गीय उत्तर भारतीयों के तौर पर पुनर्कल्पित किया.
मुखर्जी ने कलकत्ता की तुलना में अपने जीवन का ज्यादा हिस्सा बंबई में बिताया, लेकिन उनकी फिल्में अक्सर हिंदी में बंगाली फिल्मों जैसी दिखाई देती हैं और उनका समर्पण अक्सर कलकत्ता में उनके सहयोगियों का स्मरण करता है: आशीर्वाद (1968) न्यू थियेटर्स के बीएन सरकार को, अनुपमा (1966) बिमल रॉय को, और आलाप, केएल सहगल (मूल रूप से पंजाबी जिन्होंने न्यू थियेटर्स के लिए गाया) और मुकेश को.
कई बंगाली आज हिंदी भाषा में बंगाली फिल्में बनाते हैं, मिसाल के लिए, प्रदीप सरकार की परिणीता (2005), सुजॉय घोष की कहानी (2012) या दिबाकर बनर्जी की डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी (2015). शूजीत सरकार की पीकू (2015), जिसे सत्यजित रे की शॉर्ट फिल्म पीकू (1980), पर आधारित कहा जाता है, में बच्चन को भास्कोर (भास्कर) बनर्जी नाम दिया गया है.

फिल्म की जो थीम मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई वह यह है कि बंबई, बंगालियों समेत सबका स्वागत करने वाला एक महान कॉस्मोपॉलिटन शहर, पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है. यह फिल्म बंबई शहर और राज कपूर को समर्पित है, जो इस शहर के सबसे महान फिल्मकारों में से एक हैं, जिनकी शैली ने मुख्यधारा के सिनेमा, इसके सितारों और इसके संगीत को स्थापित करने का काम किया.
वे भी बंगालियों की तरह भारत के एक ऐसे इलाके से आए थे, जो 1947 में दूसरा मुल्क बन गया, लेकिन दूसरी तरफ वे कई सालों तक कलकत्ता में भी रहे, जब उनके पिता न्यू थियेटर्स में काम करते थे और बंगाली सीख ली थी.
मुझे लगता है यह फिल्म ‘जिंदगी कैसी है पहेली’ से शुरू होती है, जो किसी सिनेमाई जुलूस की तरह है. यहां हम बंबई, ज्यादातर दक्षिणी बंबई, को उसकी अट्टालिकाओं से देखते हैं, दिन की उस घड़ी में जब यह कसक भरे ढंग से सुंदर दिखाई देती है, जहां ट्रैफिक वेगवान है, रेंग नहीं रहा है- एक कॉस्मोपॉलिटन (विश्वनगरी), सच में दुनिया के महान शहरों में से एक- एक शहर जहां की सड़कें जीवंत हैं और लोगों में गति है. वीटी और अट्टालिकाओं जैसी सुंदर इमारतों को विस्मयकारी मरीन ड्राइव के आमने-सामने रखा गया है.
इस शहर में देशभर के लोग जमा होते हैं. बंगाली डॉक्टर भास्कर, पंजाबी आनंद (जो अपनी कविता उर्दू में पढ़ता है महाराष्ट्रियन कुलकर्णी, पंजाबी पहलवान (दारा सिंह) ईसाई मिसेज डीसा, और गुजराती भाषी मुस्लिम ईसाभाई सूरतवाला (जॉनी वॉकर) और विधवा मां की भूमिका में प्यारी दुर्गा खोटे. ये सब अपनी भाषाएं बोलते हैं, अपने मजहबों और संस्कृति का पालन करते हैं, मगर वे सब एक महान विश्वनगरी में एक साथ रह सकते हैं.
भास्कर के नौकर रघु काका अपने बनाए भोजन- खिचड़ी, जो अपने आप में एक महान मिश्रण है- से उनका ख्याल रखते हैं और अपने लिए आवाज उठाते हैं. यहां औरतें अभिकर्ताएं (एजेंट) हैं और विश्वास के साथ हर जगह आती-जाती हैं. सिर्फ एक व्यक्ति है जिसे चिढ़ाया जाता है- बड़े तोंद वाले अभिनेता मूलचंद को.
आनंद अनजान व्यक्तियों से, उन्हें दिल्ली का अपना पुराना दोस्त मुरारी लाल बताकर, मिलता है. सिर्फ ईसाभाई (जॉनी वॉकर) उसके इस खेल को समझ लेते हैं और उसी अंदाज में जवाब देते हैं. शायद यह एक छोटा-सा मजाक है कि दिल्ली नहीं, बंबई में कुछ भी संभव है?
आनंद 50 साल पहले रिलीज हुई थी. आजादी के महज 24 सालों के बाद. इस फिल्म के कई अभिनेता और निर्माण टीम के सदस्य ब्रिटिश भारत में बड़े हुए और यहां एक नए भारत के विचार को आकार दे रहे हैं. उनके लिए ब्रिटिश लगभग पूरी तरह से हास्य के पात्र हैं. लिंफोसरकोमा ऑफ द इनटेस्टाइन का मजाक बनाया जाता हैः ‘किसी वायसराय का नाम लगता है. आदमी विविध भारती पर अनाउंस कर सकता है.’
यह सांस्कृतिक आत्मविश्वास दिखलाता है कि किरदार खुद को लेकर और दूसरी संस्कृतियों को लेकर, बगैर उन पर हंसे या बगैर उनकी खुशामद किए आश्वस्त हैं. अलग मगर समान के फलसफे में श्रेष्ठतावाद की अनुपस्थिति इस फिल्म के सदाबहार आकर्षण का हिस्सा है.
(लेखक एसओएएस, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में भारतीय संस्कृति और सिनेमा की प्रोफेसर हैं.)
(इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.)