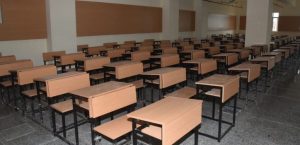‘ग़रीबी हटाओ’ के नारे के साथ उस साल इंदिरा की जीत ने कांग्रेस को नई ऊर्जा से भर दिया था. 1971 एक ऐतिहासिक बिंदु था क्योंकि इंदिरा गांधी ने लक्ष्य और दिशा का एक बोध जगाकर सरकार की संस्था में नागरिकों के विश्वास की बहाली का काम किया.

भारतीय इतिहास के कैलेंडर में 1971 के नाम कई बड़ी जीतें दर्ज हुईं- सियासत हो, क्रिकेट या फिर जंग. भारत के लिए इन सबका दूरगामी नतीजा निकलनेवाला था. भले ही भारत घरेलू मोर्चे पर कई समस्याओं से जूझ रहा था, लेकिन फिर भी देश एक नई उमंग से भरा हुआ था.
50 सालों के बाद हम मुड़कर उस समय को देख रहे हैं और उसका अक्स उभारने की कोशिश कर रहे हैं. लेखों की एक श्रृंखला के तहत नामचीन लेखक उन महत्वपूर्ण घटनाओं और प्रक्रियाओं को याद करेंगे जिन्होंने एक जवान, संघर्षरत मगर उम्मीदों से भरे भारत पर अपनी छाप छोड़ने का काम किया.
इतिहास महानता का तमगा सिर्फ एक किस्म के नेता लिए महफूज रखता है- वे जो राज-व्यवस्था को मौत के मुंह से खींचकर उसकी हिफाजत करते हैं और और उसे नया जीवन देते हैं. इतिहास उन नेताओं को मान्यता देता है जो राजनीतिक परिदृश्य का कायापलट करने के लिए रंगमंच पर कब्जा कर लेते हैं.
इन दोनों कामों को एक ही क्षण में अंजाम दिये जाने का काम विरले ही होता है. भारत में यह लम्हा 1971 में आया और इंदिरा गांधी इस मौके को लपकते हुए राजनीतिक सुदृढ़ीकरण और बदलाव की प्रक्रिया की कर्णधार बनीं.
1971 इंदिरा गांधी का साल था, लेकिन इस 1971 की इबारत पिछले कई सालों से लिखी जा रही थी. 1964 में नेहरू की मृत्यु के बाद, नेहरू का भारत एक यथास्थितिवाद और जड़ता से आगे बढ़ रहा था. राहत की एकमात्र बात यह थी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस अब भी भारतीय सत्ता की सेवा कर रही थी.

इसके नेतृत्व ने 1964 और 1966 में बगैर किसी झंझावात या चरमराहट के दो शांतिपूर्ण और व्यवस्थित सत्ता परिवर्तनों को साफ-सुथरे ढंग से अंजाम दिया था. 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध ने निश्चित ही देश के गौरव को फिर से बहाल किया था, लेकिन इसके साथ ही इसने जड़ता और बदलाव के जमा हो रहे संकट के समाधान को भी मुल्तवी कर दिया था.
नेहरू के अवसान के बाद राष्ट्रीय दिशा और उद्देश्य के अनसुलझे संघर्ष एक बार फिर दस्तक देने लगे और इसके अनिवार्य नतीजे के तौर पर कांग्रेस खुद विभाजित, भ्रमित और आपसी संघर्षों से ग्रस्त हो गई.
1967 के लोकसभा चुनाव के मौके पर बड़े कारोबारी घराने, धार्मिक दक्षिणपंथ और बची हुई सामंती व्यवस्था की प्राथमिकताएं और पूर्वाग्रह नेहरू के भारत को स्पष्ट तौर पर खारिज करते हुए गोलबंद हो गए थे. इस मजबूत गठबंधन ने यह मांग की थी कि राज्य को अर्थव्यवस्था पर अपने सर्वाधिकार को त्याग देना चाहिए और समाजवादी भारत को लेकर अपने विभ्रमों से बाहर निकल आना चाहिए.
2 जनवरी, 1967 को इंजीनियरिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वार्षिक सत्र के उद्घाटन के मौके पर जीडी बिरला ने सरकार पर अभियोग लगाते हुए कहा था:
‘कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी, कम से कम केंद्र में, लेकिन काफी घटे हुए बहुमत के साथ… मुझे लगता है कि सरकार में एक ज्यादा मजबूत कैबिनेट होगी. हमारे कुछ मंत्री जो नारों और वामपंथी भाषा में बात कर रहे हैं, अभी तक यह बात नहीं समझ पाए हैं कि यह 1967 है, 1952 नहीं. आज दुनिया दूसरी भाषा में बात कर रही है…’
कुछ दिन बाद अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन में इसी आरोप को दूसरी तरह से जेआरडी टाटा ने दोहराया. उन्होंने दलील दी कि सरकार को कृषि और परिवार नियोजन जैसे अहम क्षेत्रों में ध्यान लगाना चाहिए और ‘शेष क्षेत्रों को डिमांग और सप्लाई (मांग और आपूर्ति) की शक्तियों के हवाले छोड़ देना चाहिए.’ यह साफ तौर पर नेहरू के भारत पर वैचारिक और बौद्धिक हमला था.
वास्तव में लाखों बगावतें सिर उठा रही थीं. गो हत्या पर प्रतिबंध की मांग करते हुए साधु दिल्ली में उपद्रव कर रहे थे; नक्सली जत्थे पश्चिम बंगाल में अपनी क्रांतिकारी लपटें उठा रहे थे और यहां-वहां ‘आज़ाद इलाकों’ का निर्माण कर रहे थे; और महाराष्ट्र में शिवसेना आधुनिक नागरिकता के विचारों पर सवालिया निशान लगा रही थी.
इन विभिन्न शक्तियों, विचारों और कल्पनाओं ने मिलकर, जिसे इतिहासकार ज्ञानप्रकाश ने ‘उदार लोकतंत्र के प्रोटोकॉल’ कहा है, को चुनौती दी. और ऐसा लगने लगा कि उदार लोकतंत्र में इन बगावतों का हल करने के लिए जरूरी जज्बा और आंतरिक बल नहीं बचा है.
भारतीय सत्ता के मुख्य राजनीतिक उपकरण होने के नाते यह फैसला करना कांग्रेस पार्टी का यह ऐतिहासिक दायित्व था कि सुदीर्घ स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निर्मित राष्ट्रीय आदर्शों और आकांक्षाओं के साथ विश्वासघात किए बगैर भारत को आगे कैसे बढ़ना है.
इंदिरा गांधी और उनके सलाहकार इस बात को लेकर बिल्कुल साफ थे : यथास्थिति को कायम नहीं रखा जा सकता और एक नई राजनीतिक अर्थव्यवस्था का निर्माण करना जरूरी है.
साथ ही वे इस बात को भी पूरी तरह समझ चुकी थीं कि सामने खड़े ऐतिहासिक राष्ट्रीय कार्य को पूरा करने में कांग्रेस नेतृत्व की न कोई दिलचस्पी है, न ही उनके पास इसके लिए जरूरी उपकरण हैं, न ही उनमें इस कार्य को कर सकने की क्षमता है.
इससे पहले कि वे राजनीति में सामान्य रूप से मौजूद यथास्थितिवादी शक्तियों के खिलाफ जंग छेड़ पातीं, उन्हें अपनी ही पार्टी के भीतर शक्ति परीक्षण से गुजरना पड़ा. भारत की ग्रैंड ओल्ड पार्टी में विभाजन अवश्यंभावी हो गया था.
इंदिरा गांधी ‘इंदिरा’ इसलिए बन पाईं, क्योंकि उन्होंने विभाजन की अगुआई करने में रणनीतिक स्पष्टता और चातुर्य का परिचय दिया. उन्होंने सीधे तौर पर पार्टी के शीर्ष नेताओं को चुनौती दी, जिन्होंने जवाब में भद्दे तरीके से भारत की सबसे प्रतिक्रियावादी और पुरातनपंथी शक्तियों – स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ- के साथ गठबंधन किया.

जैसा कि इंदिरा और पार्टी में उनके सहयोगियों ने समझा, विकल्प स्पष्ट था: अगर कांग्रेस को राष्ट्रीय पुनर्नवीकरण और पुनराविष्कार का वाहक बनाना है, तो इसके ऊपर पसरे पुराने सड़े-गले तत्वों को हटाना पड़ेगा, इसे नई दृष्टि और नया आकार देना होगा.
28 दिसंबर, 1969 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बंबई सत्र के अध्यक्षीय वक्तव्य में जगजीवन राम ने इस दृष्टि को रेखांकित किया:
‘..कांग्रेस एक ऐसी स्थिति में पहुंच गई है जहां इसे या तो क्रांतिकारी नीतियां अपनानी होंगी या विखंडित हो जाना होगा…
और सिर्फ कांग्रेस ही अकेले संकट में नहीं है. देश एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जिसमें व्यावहारिक तौर पर सभी राजनीतिक पार्टियां आंतरिक असंतोष और विखंडन से जूझ रही हैं. ये आंतरिक असंतोष और कुछ नहीं लोकतांत्रिक कामकाज को लेकर विरोधी रवैयों और एक विकासशील देश की चुनौतियों की अभिव्यक्तियां हैं.
चिंता इस बात को लेकर है कि यह रुझान लोकतांत्रिक मोर्चे के विखंडन और लोकतांत्रिक कार्यकलाप और सरकार की स्थिरता के लिए खतरा पेश करनेवाले छोटे-छोटे समूहों के निर्माण की ओर लेकर जाएगा. लेकिन, अगर राजनीतिक दलों के बीच ये आंतरिक संघर्ष और असंतोष राजनीतिक शक्तियों के ध्रुवीकरण का रास्ता तैयार करेंगे, तो यह एक स्वागतयोग्य रुझान होगा और मैं इसका स्वागत करूंगा. मैं हमारी विचारधारा में यकीन करनेवाली सभी प्रगतिशील शक्तियों को हमारे संगठन में शामिल होने होने के लिए आमंत्रित करता हूं…’
बंबई सत्र में एक राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें ‘एक नई सामाजिक व्यवस्था के निर्माण की प्रक्रिया में मदद देने के लिए लोकतंत्र और समाजवाद में यकीन रखनेवाली प्रगतिशील शक्तियों से कांग्रेस में शामिल होने का आह्वान किया गया.’
एक नई कांग्रेस का निर्माण किया जाना था. इंदिरा गांधी के प्रमुख सिपहसलार पीएन हस्कर ने 1969 में ही समस्या के सार को पहचान लिया था: ‘गरीब कांग्रेस को अनंत काल तक वोट देते नहीं रहेंगे, अगर यह गरीब किसानों और भूमिहीन मजदूरों के प्रति चिंतित दिखाई देने की अपनी छवि को सुरक्षित रखने में कामयाब नहीं होगी.
कांग्रेस के चुनावी भाग्य के परे एक रणनीतिक चालाकी भी काम कर रही थी: जनता को उनकी सुषुप्त क्रांतिकारी आवेगों और प्रवृत्तियों से दूर करने के लिए एक नए राजनीतिक स्वप्न का ईजाद किया जाना भी जरूरी था. कांग्रेस को भारत में शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक कायापलट के विचार की विश्वसनीयता का भी नवीकरण करना था.
राजनीति असल में संसाधनों का बंटवारे को लेकर संघर्ष से संबंधित है. इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को एक ऐसी पार्टी के तौर पर नया रूप देने का काम किया जो गरीबों के हित में खेल में पक्षपात करने के लिए तैयार थी.
14 निजी बैंकों के राष्ट्रीयकरण को वंचितों के पक्ष में सबसे ज्यादा असकरक कदम के तौर पर पेश किया गया. यह कदम यथास्थितिवादी शक्तियों और बड़े कारोबारी घरानों के खिलाफ व्यूह रचना का हिस्सा था. और जब 15 दिसंबर, 1970 को सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व रजवाड़ों के प्रिवीपर्स और दूसरे विशेषाधिकारों को समाप्त करनेवाले राष्ट्रपति के आदेश को रद्द कर दिया, तब इंदिरा गांधी ने इसे बेहद चालाकी से जनता का ध्यान खींचने वाले एक बड़े मुद्दे का रूप दे दिया.
उन्होंने 1971 के महाचुनावी संग्राम में सामाजिक कायापलट के एजेंडा के पक्ष में एक नये जनादेश की मांग की. 1971 का लोकसभा चुनाव विचारधारा के आधार पर लड़ी गई सबसे बड़ी लड़ाई बन गया.
एक तरफ महागठबंधन के बैनर तले यथास्थितिवाद में धंसी पुरानी व्यवस्था की अलग-अलग शक्तियां थीं, तो दूसरी तरफ नए विचारों, परिवर्तन और नवाचार के पैरोकार थे.
यह चुनाव एक व्यक्तिगत लड़ाई में तब्दील हो गया, जब इंदिरा गांधी के ‘गरीबी हटाओ’ के नारे के जवाब में ‘इंदिरा हटाओ’ का नारा दिया. ऐसा कोई नहीं चाहता था, लेकिन 1971 का चुनाव इंदिरा गांधी और भारत को सामाजिक कायापलट के रास्ते पर ले जाने के उनके वादे के नाम पर जनमत संग्रह में तब्दील हो गया.
‘गरीबी हटाओ’ का नारा अपने भीतर भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था को आमूलचूल तरीके से पुनर्व्यवस्थित करने का अभूतपूर्व संकल्प धारण किए हुए था. इंदिरा गांधी ने अपनी अभिव्यक्ति हासिल कर ली, जनता से जुड़ीं और उन्होंने एक नयी राष्ट्रीय दिशा के लिए जनादेश मांगा.
इंदिरा गांधी की राजनीतिक जीत का संभवतः सबसे अहम आयाम यह था कि उनके आग्रह पर मतदाताओं ने स्वतंत्र और लोकतांत्रिक भारत में जीवित रह गई एक खासतौर पर असंगत व्यवस्था का डेथ वारंट लिख दिया: पूर्व रजवाड़ों की व्यवस्था, जो अपने विशेषाधिकारों और प्रिवीपर्स के साथ अकड़ कर चल रही थी.

इंदिरा गांधी ने चुनावी लोकतंत्र में अंतर्निहित वैधता और लोकप्रिय जनादेश को पलट कर गोलबंद किया और भारत की सामंती व्यवस्था के सर्वाधिक सामंती तत्व से, जो अपनी भूतपूर्व प्रजा पर परंपरागत प्रभाव का दिखावा करने की जिद पर अड़े हुए थे, बीस साबित हुईं
प्रिवीपर्स की समाप्ति अतीत से मुकम्मल और नाटकीय विच्छेद थी.
पुरातनपंथी शक्तियां, परंपरानुगामी तत्व और सुप्रीम कोर्ट संविधान में किए गए वादे को तोड़ने के खिलाफ थे, लेकिन इंदिरा गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी ने इस बात पर जोर दिया कि विशेषाधिकारों से कोई लक्ष्य हासिल नहीं हो रहा है और ये समतावादी सामाजिक व्यवस्था से किसी तरह के मेल में नहीं था और लोकतांत्रिक इरादों और व्यवहारों पर एक आघात था.
यहां यह ध्यान में रखना चाहिए कि 1971 से पहले भी इनमें से कुछ महाराजाओं को स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ द्वारा बढ़ा-चढ़ाकर संसदीय और विधानसभा चुनावों में अपना उम्मीदवार बनाया गया था और लगभग हर बार पूर्व सामंती व्यवस्था ने आसान जीतें दर्ज की. लेकिन 1971 में कहानी बदल जाने वाली थी.
इससे पहले कभी भी महाराजाओं ने एक वर्ग के तौर पर खुद को कांग्रेस के खिलाफ एकजुट नहीं किया था. सबसे ज्यादा नाटकीय और लच्छेदार शब्दों वाला हस्तक्षेप संभवतः मेवाड़ के महाराणा ने किया, जिनका पूर्व हिंदू शासकों के बीच सर्वाधिक सम्मान था.
अखबारों में पैसे देकर छपवाए गए विज्ञापनों द्वारा महाराणा ने ‘मेवाड़ के महाराणा के वंशज’ के तौर पर अपने परंपरागत प्राधिकार का हवाला दिया जो अपने जाति और पंथ का भेद किए बगैर अपने लोगों की आस्था, संस्कृति और स्वतंत्रता की रक्षा करने में सबसे आगे रहे हैं.’
उन्होंने खुद को ‘अपने पूर्वजों द्वारा सौंपी गई सेवा और बलिदान की महान परंपरा के वारिस’ के तौर पर पेश किया. उन्होंने लोगों से ‘राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों के केंद्रीकरण’ को खारिज करने का आह्वान किया और उन्हें एक ‘अधिनायकवादी पैटर्न’ के खतरों से आगाह कराया जिसके भीतर ‘न तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और न ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया जीवित रह पाएगी.’
यह एक महासंग्राम जैसा था. एक तरफ पूर्व सामंती शासक थे, तो दूसरी तरफ लोकतांत्रिक नेता. रजवाड़ों ने राजशाही की परंपरागत वैधता को धर्म प्रदत्त दैवीय अधिकारों से जोड़ कर संविधान की वैधता के खिलाफ खड़ा कर दिया था, जिसने लंबे स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान लोकतांत्रिक मांगों और आकांक्षाओं से अपनी स्वीकार्यता और जीवन हासिल हासिल किया था. आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था की आत्मा दांव पर थी.
महराजाओं का ‘परंपरागत प्राधिकार’ पदानुक्रम आधारित सामाजिक व्यवस्था पर टिका था जो बगैर किसी अपराधबोध के दयालु निरंकुशता को वैधानिकता प्रदान करता है.
दो दशक से कुछ ज्यादा साल पहले तक इन राजाओं और महाराजाओं के पास अपनी प्रजा के ऊपर जीवन और मृत्यु की बेहिसाब, अबाध और चुनौती से परे शक्ति थी. और अब इन्हीं सामंती शासकों और जमींदारों ने भारत के संविधान में वर्णित लोकतांत्रिक व्यवस्था को सीधे चुनौती देने का फैसला कर लिया.
1971 की लड़ाई का एक उपपाठ यह था कि भारत ने काफी दृढ़ता के साथ सामंतों और सभी अतीत के मूल्यों और भावनाओं से अपना मुंह मोड़ लिया. और इस तरह से लोकतांत्रिक क्रांति अपने अंजाम पर पहुंच कर पूर्ण हो गई.
1971 की चुनावी सफलता के बाद दोनों ही पक्षों द्वारा बड़े पैमाने पर यह स्वीकार किया गया कि यह इंदिरा गांधी की व्यक्तिगत जीत थी. अब उन्होंने एक करिश्मा अख्तियार कर लिया था.
कांग्रेस पर उनका नियंत्रण पूर्ण हो गया था और उन्होंने चुनावी जनादेश का उपयोग मोहन कुमार मंगलम, केवी रघुनाथ रेड्डी और केआर गणेश, नुरुल हसन जैसे प्रगतिशील आवाजों को अपने मंत्रिपरिषद में शामिल करने के लिए किया.
भारतीय सत्ता के एक मजबूत उपकरण के तौर पर कांग्रेस एक नई ऊर्जा से भर गई थी. एक तरह की व्यक्तित्व पूजा की शुरुआत हुई. कुछ सालों के भीतर ही इसके अपने नुकसानदेह नतीजे दिखाई देनेवाले थे.
1971 एक ऐतिहासिक बिंदु था क्योंकि इंदिरा गांधी ने लक्ष्य और दिशा का एक बोध जगाकर सरकार की संस्था में नागरिकों के विश्वास की बहाली का काम किया. अगले दो दशकों तक भारत की सत्ता ठीक थी.
लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं.
(इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.)