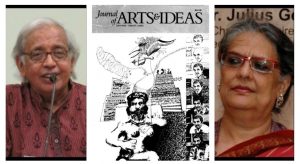ईद मुबारक के जवाब में अक्षय तृतीया या परशुराम जयंती की बधाई देना कैलेंडरवादी धार्मिकता का प्रतीक है. हम हर जगह अपना क़ब्ज़ा चाहते हैं. ध्वनिभूमि पर, ध्वनि तरंगों पर भी, दूसरों के उपासना स्थलों पर और समाज के मनोलोक पर.

‘ईद मुबारक!’ जवाब आया, ‘अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं’, ‘परशुराम जयंती की बधाई.’ इस उत्तर से मन खिन्न हुआ.
किसी एक प्रसन्नता के अवसर पर प्रतियोगिता करके उस अवसर को छेंक लेने की कोशिश में कौन-सा सुख मिलता है? जिनकी उम्र 50 के आसपास या उससे ज्यादा है वे जानते हैं कि हिंदुओं के लिए न तो ‘परशुराम जयंती’ और न ‘अक्षय तृतीया’ ऐसे पर्व हैं जो पूरे भारत में उस पैमाने पर मनाए जाते हों जैसे दुर्गा पूजा या होली-दीवाली मनाए जाते हैं.
अक्षय तृतीया तो पूरी तरह से बाज़ार के द्वारा प्रचारित किया गया त्योहार है जिसमें आभूषण खरीदने के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाता है. उसी प्रकार हिंदू परिवार और समाज और उसमें भी ऐसे ब्राह्मणों के बीच जो खुद को शेष ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ मानते हैं, कभी परशुराम जयंती की कोई स्मृति नहीं है.
फरसाधारी परशुराम को तुलसीदास ने अवश्य लोकप्रिय बनाया लक्ष्मण परशुराम संवाद के माध्यम से, जिसमें किशोर लक्ष्मण शिव के धनुष भंग से कुपित ब्राह्मण देवता से विनोदपूर्ण विवाद करते हैं और उनके ज्येष्ठ भ्राता राम भी उसका भरपूर आनंद लेते हुए बाद में किसी तरह उनका कोप शांत करते हैं. कब से वे ब्राह्मणों के और फिर उनके मिस (बहाने) हिंदुओं के सर्वस्वीकृत आराध्य हो गए, यह बाद में धर्मों के इतिहासकार तय करेंगे.
कोई चाहे तो कह सकता है कि आपकी पीढ़ी जो नहीं करती थी, वह हम न करें ऐसा विधान कहां है! हम नई धार्मिक परंपराएं क्यों नहीं चला सकते? और यह ठीक ही होगा. लेकिन ऐसा तर्क देने वाला अपनी पद्धति की जांच कर ले. क्योंकि वह हर चीज़ की प्रामाणिकता उसकी प्राचीनता में खोजता रहा है. फिर जो प्रथा प्राचीन नहीं, वह प्रामाणिक कैसे?
उससे भी अलग प्रश्न सिर्फ एक है और वह खुद से ईमानदारी से पूछना चाहिए कि क्या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक प्रेरणा है या मात्र पंचांग या कैलेंडर को भी ‘अपने’ रंग में रंग देने की एक विस्तारवादी प्रवृत्ति है. वह शुद्ध सांसारिक क्षुद्रता है. मैंने आपकी कोई जगह देखी और चालाकी से उस पर अपना रूमाल रख दिया.
यह प्रवृत्ति पिछले 7-8 साल में बढ़ी है. इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी अपनी भूमिका निभाई है. ईसाइयों के सबसे महत्त्वपूर्ण दिन क्रिसमस यानी बड़े दिन को सुशासन दिवस घोषित करके उसे ढंक देने की दयनीय कोशिश हुई. नए हिंदू संतों में से एक ने ‘वेलेंटाइन डे’ को मातृ-पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव किया.
14 फरवरी का यह दिन मोहब्बत करने वालों का अंतरराष्ट्रीय दिवस है. लेकिन मारे हीनता ग्रंथि के उस पर विदेशी छाप मिटाने का एक अभियान चला दिया गया. मारपीट के बावजूद भारत के हिंदू युवक-युवतियों में इस दिवस की लोकप्रियता के बढ़ते जाने से उम्मीद यही बंधती है कि शायद प्रेम या मोहब्बत घृणा के संकरेपन से उबरने में सबसे कारगर सिद्ध हो!
लेकिन इस क्षुद्रता, जिसे कैलेंडरवादी धार्मिकता कह सकते हैं, का क्या करें?
कुछ वक्त पहले भारतीय जनता पार्टी ने केरल के लोगों को केरल के सबसे लोकप्रिय त्योहार ओणम को वामन जयंती के रूप में मनाने का प्रस्ताव दिया. क्रुद्ध केरलवासियों ने भाजपा को लताड़ लगाई. लेकिन उससे वह प्रयास बंद नहीं कर दिया गया. बल्कि भाजपा से प्रेरणा लेकर आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली में वामन जयंती के पोस्टर लगवाए.
यह विचार न किया गया कि दिल्ली में रहनेवाले केरलवासियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा. वामन जयंती क्या उत्तर भारत के ब्राह्मणवादी हिंदुत्व की परियोजना को एक अंग है? क्या उसमें हम हिंदू अविचारित भाव से शामिल हो रहे हैं?
आखिर एक ऐसे चरित्र को किस प्रकार पूजा जा सकता है जो किसी दानवीर की उदारता का लाभ उठाकर उसे धोखा देकर सर्वस्वहीन कर दे? वामन के अवतार का तात्पर्य क्या है?
परशुराम हों या वामन, ये मिथक कथाओं के चरित्र हैं. सबके सब अनुकरणीय हों, पूजनीय हों, ऐसा नहीं. इन सबमें एक मानव सत्य अवश्य निहित है. आखिर क्यों कृष्ण और राम के चरित्रों में जटिलता है, दोष है?
ठीक ही गांधी ने गीता को इतिहास ग्रंथ मानने की जगह काव्य माना था जैसे रामायण है या महाभारत. काव्यात्मक चरित्र अधिक दिलचस्प होते हैं. जैसे ही आप उन्हें पूजनीय बना देते हैं, उन चरित्रों से आपका संवाद असंभव हो जाता है. उन्हें जड़ कर दिया जाता है. आश्चर्य नहीं कि अब कोई नई राम कथा संभव नहीं.
आज जो धार्मिक चरित्र नए भगवान के रूप में आरोपित किए जा रहे हैं, उनकी एक विशेषता यह भी है कि वे एक हिंसक हिंदू के देवता हैं. उनका इस्तेमाल एक राजनीतिक बहुसंख्यकवादी हिंदू के द्वारा अपने हिंसक कृत्य के आवरण के रूप में किया जा रहा है.
जैसे हनुमान चालीसा को ही ले लीजिए. किसने सोचा था कि हनुमान चालीसा को एक चिल्लाहट या नारे की तरह इस्तेमाल किया जाएगा? वह भी मुसलमानों की पवित्र अजान की आवाज़ को डुबाने के लिए? इससे बड़ा पाप कोई हो सकता है? किसी की प्रार्थना को भंग करना, बाधित करना, उसमें व्यवधान पैदा करना?
आपकी अजान है तो हमारे पास हनुमान चालीसा है! गायित्री मंत्र भी हो सकता था जिसके लाउडस्पीकर से प्रसारण का रिवाज़ कोई 40 साल पहले शुरू होते सीवान में देखा था. हनुमान चालीसा नया हिंदुत्ववादी धार्मिक रिवाज़ है.
बच्चे कभी अंधेरे में, किसी भूतग्रस्त वृक्ष के नीचे से गुजरते वक्त अपना भय मिटाने के लिए इसे पढ़ा करते थे, जिसकी ढेरों कहानियां हैं. अब दिनदहाड़े समूह में दूसरों पर अपने कंठबल और संख्या के सहारे अपना दबदबा कायम करने, दूसरे को डराने, दबाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है. यह कैसी शिक्षा है और किस विराम पर पहुंच गए हैं हम?
पिछले क्रिसमस को ऐसी ख़बरें मिलीं कि हिंदुत्ववादी गिरोह गिरिजाघरों में घुस गए, उपासना स्थलों पर चढ़ गए और यीशु की आराधना को बंद करवाने के लिए जय श्री राम के नारे लगाने लगे. अजान के मुकाबले हनुमान चालीसा के पहले जुमे की नमाज़ के मुकाबले भजन का हमला हमने किया.
असल में हम हर जगह अपना कब्जा करना चाहते हैं. ध्वनिभूमि पर, ध्वनि तरंगों पर भी, दूसरों के उपासना स्थलों पर और समाज के मनोलोक पर. इससे समझ सकते हैं कि क्यों इधर 10-20 वर्षों में हम अपने नए-नए धार्मिक दिवस या चरित्र खोज-खोजकर निकाल रहे हैं. क्योंकि हम वहां भी जनसंख्या की उस बेचैनी से पीड़ित हैं जो देश में अन्य धर्मालंबियों की संख्या को लेकर हमारे भीतर पैदा होती है.
क्या इसी कारण हम कैलेंडर में अपने धार्मिक दिवसों को संख्या बढ़ाना चाहते हैं? क्या उन सारे दिनों पर हम अपनी छाप आरोपित कर देना चाहते हैं? क्या यह एक प्रकार का हीनता बोध है जिसे छिपाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं?
जो किसी दूसरे की धार्मिकता में कोई आनंद लाभ न कर सके, वह कैसा मनुष्य है? जो किसी की पवित्रता से अपने लिए पवित्र भाव का लाभ न कर सके, वह क्या स्वस्थ मनुष्य है? जो यह कहे कि मैं इसलिए इसका साझीदार नहीं बनना चाहता कि यह विदेशी है उसे एक जैन धर्मावलंबी लेखक जैनेंद्र कुमार को सुनना चाहिए:
‘इस्लाम को मानने वाला भारतीय अरब से अपनी स्फूर्ति लाता है, तो बुरा क्या करता है? स्फूर्ति तो उपयोगी चीज़ है. जीवन उससे समर्थ होता है. …मुसलमान का देश भारत था, तीर्थ अरब था. उस तीर्थता से भारत को नुकसान क्या था?
धर्म-भाव आदमी कहीं से भी प्राप्त करे, लाभ तो उसका आस-पास के समुदाय को मिलता है. आप क्या ब्रह्मपुत्र का स्रोत तिब्बत में (और आज चीन में ) है, तो उसके जल को अपवित्र और विदेशी मानेंगे? सच यह है कि चेतना जहां से भी अपने लिए स्फूर्ति प्राप्त करे, वह शुभ ही है.’
तो अरब से अगर तीर्थ करके मुसलमान लौटता है तो वह हमारे लिए भी पवित्रता का भाव लाता है. जैसे कहा जाता है कि रोज़ा जो रखता है उसका फल सिर्फ उसे नहीं, उसके परिजन को भी मिलता है. जैनेन्द्र के ये विचार उनकी रचनावली के छठे खंड के तृतीय खंड ‘भारत’ में विस्तार से पढ़ सकते हैं.
असल बात यह है कि क्या आप हिंदू होते हुए इस्लाम या ईसाइयत या बौद्ध अथवा यहूदी धर्म से अपने लिए स्फूर्ति प्राप्त कर पाते हैं या नहीं? या उनसे आप में ईर्ष्या और हिंसा पैदा होती है? इस सवाल पर अगर हम विचार कर लेंगे तो ईद मुबारक कहते ही अक्षय तृतीया या परशुराम जयंती की बधाई नहीं देने लगेंगे.
(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं.)