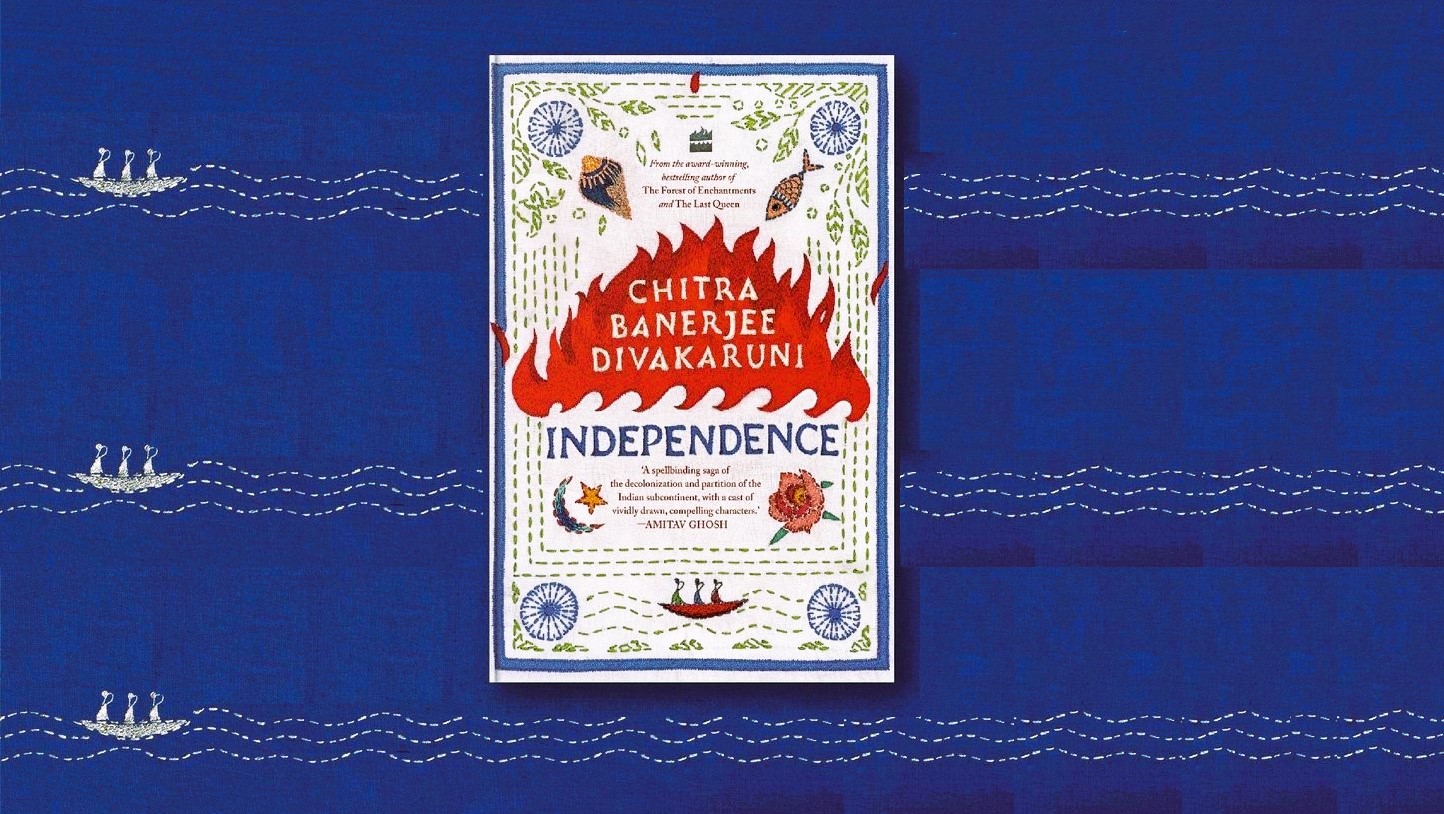साल 2022 – विभाजन और स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने का साल. पर 1947 को लेकर जो राजकीय आख्यान हैं वह 200 सालों की ब्रिटिश ग़ुलामी से मिलने वाली स्वतंत्रता के उल्लास को तो रेखांकित करते हैं, पर राष्ट्र के जन्म से पहले जिस भीषण प्रसव-पीड़ा से इसे गुज़रना पड़ा-विभाजन- उसे राष्ट्रवादी नेता भी स्वीकार कर अंततः भविष्य की तरफ, राष्ट्र निर्माण की तरफ देखने का आह्वान करते रहे.
लेकिन विभाजन- किसी सुदूर इतिहास की घटना मात्र न रहकर हर आने वाली पीढ़ी के अनुभवों और स्मृतियों का हिस्सा बना रहा. इतिहास ने इसके कारण ढूंढे, इस खेल के पात्रों को चिह्नित किया, थोड़े बाद आए वाचिक इतिहासकारों ने लोगों के अनुभव दर्ज़ किए, विभाजन की खामोशी के दूसरी पार उतरकर देखने का प्रयास किया.
आज की चौथी-पांचवी पीढ़ी ने अपने पुरखों के विस्थापन के दौरान कभी साथ लाई चीज़ों के द्वारा, तो कभी उस विरासत का हिस्सा होने की नैतिक ज़िम्मेदारी के तहत उस अतीत को खोदने का प्रयास किया, तो कभी अपनी जड़ों से दूर हो गए प्रवासियों ने अपने खोए घरों की स्मृतियां के कोलाज डिजिटल माध्यमों के द्वारा खड़े किए. कहने का भाव यह कि विभाजन 75 साल बाद भी उपमहाद्वीप के सार्वजनिक विमर्श, लोक- स्मृतियों का हिस्सा बना रहा.
पर इतिहास चाहे वह किसी भी प्रकार का क्यों न हो, एकमत होकर यह स्वीकार करता है कि जिस विधा ने विभाजन को बीते हुए जीवन का एक त्रासद यथार्थ मान पुनर्जीवित किया है- वह साहित्य ही है. इसलिए विभाजन-साहित्य अपने आप में उन असंख्य लोगों का इतिहास है, जिसे शासकीय ब्योरों में भुला दिया गया. यह प्रभावों का, अनुभवों का अनुवाद है और इन सबसे अधिक इतिहास पर एक प्रश्न-चिह्न है.
उपमहाद्वीप में इस विषय ने जितने साहित्यकारों की कल्पना को स्वर दिए हैं, वह विरल है. इसलिए अगर 1956 में खुशवंत सिंह ‘अ ट्रेन टू पाकिस्तान’ लिखते हैं, तो साल 2018 में आई ‘रेत समाधि’ (गीतांजलि श्री) जिसे इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय बुकर दिया गया है, भी विभाजन को अपना नेपथ्य बनाती है. और इन सालों के दरमियान विभाजन साहित्य का वह विस्तृत भंडार है, जो वस्तुतः राजनीतिक इतिहास का पूरक नहीं बल्कि विकल्प है.
विभाजन साहित्य के इसी विशद भंडार में साल 2022 में चुपचाप आई लेखिका चित्रा बनर्जी दिवाकरुनी का उपन्यास ‘इंडिपेंडेंस’ एक नितांत नया तो नहीं, पर एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ता है. नया इसलिए नहीं कि, यहां भी नेपथ्य में विभाजन है, खूनी हिंसा के बीच जन्म लेते दो राष्ट्र हैं, और सबसे अहम वो सभी पात्र हैं, जिनकी ज़िंदगियां इस ऐतिहासिक क्षण से प्रभावित होती हैं- जो कमोबेश विभाजन साहित्य की मुख्य अंतर्धारा है.
महत्वपूर्ण, इसलिए, क्योंकि यहां इस पूरी घटना, राष्ट्रों के जन्म, विभाजन की हिंसा और उपद्रव, विभाजन के प्रभावों को स्त्रियों की दृष्टि से देखा गया है और कहीं भी कहानी इस दृष्टि को छोड़ती नहीं है. किताब बंगाल के हिस्से के विभाजन पर आधारित है, और इस तरह से ज्योतिर्मयी देबी (इपार गंगा ओपार गंगा), महमूद-उल हक़ (ब्लैक आइस ) अमिताव घोष (द शैडो लाइंस) की परंपरा का अगला आख्यान लगती है.
विभाजन को आधार बना कर लिखे गए साहित्य के सामने एक बड़ी चुनौती यह रहती है कि इसमें इतिहास को कथा में पिरोने के लिए ‘जगह’ या वह ‘रिक्त स्थान’ ढूंढने होते हैं, जहां जड़ कर वह कथानक का सहज हिस्सा बन सकें, क्योंकि अंततः लेखक एक साहित्य की रचना कर रहा है/रही है, वह इतिहासकार नहीं है. इसलिए इतिहास और कल्पना का मिश्रण या उनका ताल-मेल बिठाना विभाजन साहित्य लिखने वाले लेखक के लिए आवश्यक है.
विभाजन साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण हस्ताक्षर मसलन, सियाह हाशिये (सआदत हसन मंटो), तमस (भीष्म साहनी), झूठा-सच (यशपाल), आइसकैंडी मैन (बापसी सिदवा), बस्ती (इंतिज़ार हुसैन), आधा गांव (राही मासूम रज़ा), अ बेंड इन द गेनज़ेस (मनोहर मालगोनकर), काला जल (शानी) इत्यादि इसलिए भी विभाजन साहित्य में श्रेष्ठ बन सके क्योंकि इतिहास पर आधारित होते हुए भी अंततः यह साहित्य था.
यहां ऐतिहासिक यथार्थ को कथा-वस्तु में बस किसी भी प्रकार जड़ देने की की कोशिश नहीं की गई है. चित्रा बनर्जी की यह नई किताब भी बहुत हद तक इतिहास और कल्पना का सामंजस्य बिठाने में सफल हुई है पर, कुछ हिस्से हैं जहां, इतिहास को याद करके लाया गया है. अलग-अलग पैराग्राफ में मुख्य कथा के बीच पाठकों को याद दिलाया जाता है कि देश में राजनीतिक स्तर पर अभी विभाजन की सरगर्मियां चल रही थीं, परिवेश में तनाव है, अनिर्णय बना हुआ है- ऐतिहासिक घटनाओं को जल्दी-जल्दी आंखों के सामने से गुज़ारा जाता है.
पर इतिहास को अगर पृष्ठभूमि में रहने दें, तो उपन्यास में कथानक भले ही सरल है, पर एकरैखिय नहीं. कहानी तीन बहनों की है. डॉक्टर पिता की तीन बेटियां दीपा, जामिनी, बिष्णुप्रिया (प्रिया) कलकत्ता से दूर सरसी नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव रानीपुर में एक शांत जीवन जी रही हैं. गांव के जमींदार चौधरी सोमनाथ बाबू , न केवल डॉक्टर के परम मित्र हैं, बल्कि प्रिया के साथ भी शतरंज की बाज़ियां लगाते हैं. बेटा अमित, कलकत्ते में पढ़ने वाला, नफीस कपड़े और फैशन के साथ, डॉक्टर परिवार की बेटियों का चिर-साथी है, विशेषकर प्रिया का, जो न केवल अपने पिता की तरह डॉक्टर बनना चाहती है, बल्कि तीनों बहनों में सबसे अधिक स्वाभिमानी और महत्वाकांक्षी है. कहानी इन्हीं दोनों परिवारों के प्रगाढ़ संबंधों के इर्द-गिर्द घूमती है और इस प्रक्रिया में नेपथ्य में चल रही राजनीतिक हलचलें सभी के जीवन को प्रभावित करती हैं.
डॉक्टर नबकुमार 16 अगस्त 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे की सांप्रदायिक हिंसा में मारे जाते हैं. सोमनाथ बाबू की मदद से प्रिया डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाती है, बड़ी बहन दीपा जो सबसे सुंदर और व्यावहारिक है, वह अंततः सारी व्यावहारिकता त्यागकर डॉ. रज़ा से प्रेम करके विभाजन के बाद ढाका चली जाती है. मंझली जामिनी जो अमित को हमेशा से चाहती है, यह जानते हुए भी कि अमित और प्रिया बचपन के साथी है, अंततः परिस्थितियों के कारण अमित की पत्नी और और बेटे तपन की मां के रूप में चौधरी खानदान का हिस्सा बन जाती है.
अमित, पूर्वी पाकिस्तानी सीमा के सैनिक की गोली से मारा जाता है और इस प्रकार सोमनाथ बाबू इन तीन बहनों के साथ जीवन की शेष यात्रा शुरू करते हैं. कहानी एक साथ कई रंग लिए हुए है- जामिनी-अमित-प्रिया के प्रेम का एक वृत्त है, ग्रामीण सामाजिक संबंधों की पृष्ठभूमि है, विभाजन से ज़मीनों पर रहने वालों की बदलती ज़िंदगियां हैं-उस जीवन के दुख-दर्द हैं, सांप्रदायिक हिंसा में बेक़सूरों के मारे जाने और स्त्रियों की दुर्गति के चित्र हैं और इस पूरे उन्माद के खत्म होने के बाद ज़िंदगी को दोबारा से गढ़ने के आख्यान हैं.
कहानी सरल है, पर यह शायद लेखन शैली ही है कि नाटकीयता के प्रयोग से एक विस्मय, एक प्रकार का रोमांच बना रहता है. मसलन, दीपा जो पूर्वी पाकिस्तान में रज़ा की हत्या के बाद अब बेवा आलिया बेग़म के रूप में रह रही है और जिसे जबरन सेना के मेजर मामून से निकाह करना पड़ेगा), उसे जिस नाटकीयता के साथ वापस भारतीय सीमा में, नदियों के रास्ते वापस लाने का काम प्रिया, जामिनी और अमित करते हैं, वह हिस्सा संशय से भरा हुआ है- दीपा का अब क्या होगा? क्या वह अपने परिवार से वापस मिल पाएगी भी या नहीं? कहीं उसे फिर से तो मामून के सिपाही पकड़ नहीं लेंगे?
बहरहाल, नाटकीयता इतिहास के प्रयोग से भी लाई गई है. मसलन, पूरी कहानी में सरोजिनी नायडू के व्यक्तित्व को और अंत में स्वयं उन्हें लाकर बनर्जी न केवल प्रिया के लिए जीवन में प्रेरणा ग्रहण करने का एक रोल मॉडल गढ़ती हैं, बल्कि एक नारीवादी दृष्टि से नायडू के व्यक्तित्व का पात्र के रूप में प्रयोग उपन्यास की नारीवादी दृष्टि को बहुगुणित करता है.
15 से भी अधिक उपन्यासों और कहानी संग्रह लेखिका के प्रकाशित हो चुके हैं. पर बनर्जी के अब तक लिखे लेखन में उनकी नारीवादी दृष्टि ही बारंबार उभरती है, विशेषकर दक्षिण एशिया के संदर्भ में विकसित होता नारीवाद. उनके केंद्रय पात्र स्त्रियां हैं- साधारण भी और असाधारण भी.
‘द फॉरेस्ट ऑफ एंचनमेंट्स’(2019) अगर रामायण को सीता की दृष्टि से देखने का प्रयास है तो ‘द पैलेस ऑफ इल्यूज़न’(2008) महाभारत को द्रौपदी की नज़रों से देखने का, ‘द लास्ट क़्वीन’ (2021) में महाराजा रंजीत सिंह की छोटी रानी जिंदन कौर जो आगे चलकर अपने अपने राज्य की सीमा की रक्षा के लिए घर की सीमा तोड़कर बाहर निकलती है.
इंडिपेंडेंस को भी इस दृष्टि से देखा जाए तो ऐतिहासिक होते हुए भी यह कहानी अंततः स्त्रियों के ही संघर्ष की है. यहां राजनीति, धार्मिकता, सामाजिकता सब कुछ उपस्थित होकर भी अदृश्य है, पर किस तरह यह तीनों इन बंगाली ग्रामीण, साधारण स्त्रियों को अपने आप में असाधारण बना देते हैं, किस तरह प्रिया, जामिनी, दीपा , कठिन और भीषण परिस्थितियों में अंततः अपने अंदर की क्षमताओं से वाकिफ़ होती हैं, उपन्यास का मुख्य स्वर वही है.
हालांकि कई ऐसे क्षण उपन्यास में हैं , जहां लगता है कि पीछे जाकर कुछ घटनाओं को, कुछ निर्णयों को अगर बदल दिया जाए -संशोधित कर दिया जाए, तो शायद इन पात्रों की ज़िंदगियां इतनी मुश्किल न हों. पर कुछ परिस्थितियां, या कुछ निर्णय स्वयं लेखक भी अपने पात्रों के लिए नहीं बदल सकते, क्योंकि वो उस समय के, उस इतिहास के निर्णय हैं, जिन पर किसी का नियंत्रण नहीं होता.
1946-47 के उन वर्षों ने राष्ट्रों के ही रुख नहीं बदले बल्कि उस समय में जी रहे और भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के जीवन की दिशा भी बदल दी और यह उपन्यास उसे पकड़ सका है. जिस प्रकार महात्मा गांधी की हत्या के बाद शोकाकुल सरोजिनी नायडू कहानी के अंत में प्रिया को कहती है वह कई अर्थों में सही भी है:
‘You are a daughter of independence, the country’s future. Women like you are the ones for whom we fought and died, the ones who will transform India. You must carry the flag forward. You may fall from time to time. We all did. What is important is to get up again.’
[तुम आज़ादी की बेटी हो, इस देश का भविष्य. तुम्हारे जैसी महिलाओं के लिए हम लड़ें हैं और जान गंवाई, तुम जैसी औरतें ही हैं, जो भारत की तस्वीर बदलेंगी। तुम्हें इसे आगे ले जाना चाहिए। हो सकता है तुम इस कोशिश में कई बार असफल भी हो जाओ. हम सभी हुए हैं, लेकिन जो बात मायने रखती है, वो है गिरकर दोबारा उठना.]
यह स्त्री को उत्तरदायित्व के रूप में शायद एजेंसी देने की ही कवायद है. बहरहाल, बनर्जी की भाषा सहजता लिए हुए है और देखा जाए तो ‘अंग्रेज़ी में भारतीय लेखन’ की विवादास्पद संज्ञा से परे वाकई एक अच्छा लेखन है. ग्रामीण बंगाल के एक सुरम्य गांव के चित्रण में सिर्फ सुरुचि ही का ही ध्यान नहीं रखा गया, बल्कि- गांव में फैली ग़रीबी, वर्ग-विषमता, धीरे-धीरे और गहराती सांप्रदायिकता-यह सब भी लेखन का हिस्सा हैं.
उपन्यास में गति है. न केवल पात्रों के जीवन में, बल्कि गांव-घरों में तेज़ी से बदलते हुए हालातों में भी. नोआखली में हुई हिंसा, रानीपुर के मुसलमानों के लिए भी कहर लाती है. खबरों से सामाजिकता रातों-रात बदल सकती है, यह अच्छे से दिखलाया गया है.
एक बात जो ध्यान आकर्षित करती है वह है कथा को गीतों के साथ भी एक संगति देना. ‘मैला आंचल’ में फणीश्वरनाथ रेणु लोकगीतों के प्रयोग से आंचलिकता को सघन करते हैं, कथा को विस्तार देते हैं, बहुत हद तक बनर्जी भी रवींद्रनाथ टैगोर और आगे चलकर ढाका में काज़ी नज़रुल की गीतियों से कथा के संवेदनशील हिस्सों को विस्तार देती हैं.
उपन्यास में अधिकतर वही हिस्से खटकते हैं जहां इतिहास को ज़बरदस्ती घुसाया जाता है. पर जिनकी भारतीय इतिहास के इन सालों की क्रमानुसार वारदातों की स्मृतियों पर धूल पड़ गई हो, उनके लिए यह आरोपित पृष्ठभूमि भी काम की ही है. लेखन की शैली दिलचस्प है, जहां हर खंड को सालों के महीनों के हिसाब से और अध्यायों को तीनों बहनों के नाम से बार-बार बांटा गया है. हर खंड की शुरुआत में लेखक जिस प्रकार नाटकों के लेखन के में रंग निर्देश दिए जाते हैं, उसी तरह परिवेश, पात्रों इन सबका उल्लेख कर देती हैं, जो कथा में नाटकीयता लाने का एक सोद्देश्य प्रयास लगता है. पर देखा जाए तो उन असंख्य साधारण लोगों के लिए विभाजन अंततः एक बड़ा राजनीतिक नाटक ही था, जिसे खेलने वाले पात्र राजनीतिक थे, पर जिसे देखने और भोगने वालों को बड़ी कीमतें चुकानी पड़ीं.
प्रिया, जामिनी, दीपा, इस नाटक की कुछ ऐसी ही भुक्तभोगी थीं. लेखिका ने इनकी कहानी तो बता दी, पर किताब की शुरुआत में अमृता प्रीतम की कही ये पंक्तियां क्या इतिहास और साहित्य, दोनों ही को विभाजन की त्रासदी बयां करने में अक्षम नहीं मानती?
‘There are many stories which are not on paper, they are written on the minds and bodies of women.’
[कई ऐसी कहानियां हैं, जो कागज़ पर नहीं लिखी गईं, वो औरतों के मन और उनके जिस्मों पर लिखी हैं.]
(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में शोधार्थी हैं.)