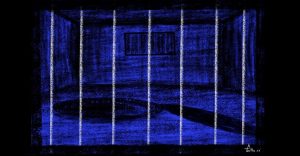धर्मवीर भारती की ‘मुनादी’ कविता जब भी याद आती है तो याद आता है कि इस बीच उक्त इतिहास की ऐसी पुनरावृत्ति हो गई है कि इमरजेंसी की मुनादी बिना ही देश में इमरजेंसी से भी विकट हालात पैदा कर दिए गए हैं, मौलिक अधिकारों को छीनने की घोषणा किए बिना उन्हें सरकार की अनुकंपा का मोहताज बना दिया गया है.

खलक खुदा का, मुलुक बाश्शा का/हुकुम शहर कोतवाल का…/हर खासो-आम को आगाह किया जाता है/कि खबरदार रहें/और अपने-अपने किवाड़ों को अंदर से/कुंडी चढ़ाकर बंद कर लें/गिरा लें खिड़कियों के परदे/और बच्चों को बाहर सड़क पर न भेजें/क्योंकि एक बहत्तर बरस का बूढ़ा आदमी अपनी कांपती कमजोर आवाज में/सड़कों पर सच बोलता हुआ निकल पड़ा है!…मुजिर है वह/कि हालात को हालात की तरह बयान किया जाए/कि चोर को चोर और हत्यारे को हत्यारा कहा जाए/कि मार खाते भले आदमी को/और अस्मत लुटती औरत को/और भूख से पेट दबाए ढांचे को/और जीप के नीचे कुचलते बच्चे को/बचाने की बेअदबी की जाए!
अपने वक्त के बड़े साहित्यकार और प्रतिष्ठित साप्ताहिक ‘धर्मयुग’ के संपादक स्मृतिशेष धर्मवीर भारती ने ‘मुनादी’ शीर्षक यह कविता चार नवंबर, 1974 को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बिहार की तत्कालीन कांग्रेस सरकार (जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर कर रहे थे) के भ्रष्टाचार के विरुद्ध रैली के बाद निकले जुलूस का नेतृत्व कर रहे लोकनायक जयप्रकाश नारायण पर आयकर चौराहे पर हुए निर्मम पुलिस लाठीचार्ज से बेचैन होकर रची थी- नौ नवंबर, 1974 को रात दस बजे, यह महसूस करते हुए कि ‘तानाशाही का असली रूप सामने आते देर नहीं लगी है.’
उन्हीं के शब्दों में कहें तो ‘जेपी ने पटना में भ्रष्टाचार के खिलाफ रैली बुलाई. रोकने के हर सरकारी उपाय के बावजूद लाखों लोग सरकारी शिकंजा तोड़कर उसमें आए. उन निहत्थों पर निर्मम लाठी-चार्ज का आदेश दिया गया. अखबारों में धक्का खाकर नीचे गिरे हुए बूढ़े जेपी उन पर तनी पुलिस की लाठी, बेहोश जेपी और फिर घायल सिर पर तौलिया डाले लड़खड़ाकर चलते हुए जेपी. दो-तीन दिन भयंकर बेचैनी रही, बेहद गुस्सा और दुख… 9 नवंबर को रात 10 बजे यह कविता अनायास फूट पड़ी.’
इसी कविता में आगे ‘बुड्ढे के पीछे दौड़ पड़ने वाले एहसानफरामोशों’ को संबोधित करते हुए उन्होंने व्यंगपूर्वक लिखा है: जीप अगर बाश्शा की है तो/उसे बच्चे के पेट पर से गुजरने का हक क्यों नहीं?/आखिर सड़क भी तो बाश्शा ने बनवाई है!/…..क्या तुम भूल गए कि बाश्शा ने तुम्हें/एक खूबसूरत माहौल दिया है/ जहां भूख से ही सही, दिन में तुम्हें तारे नजर आते हैं/और फुटपाथों पर फरिश्तों के पंख रात भर/तुम पर छांह किए रहते हैं/और हूरें हर लैंप पोस्ट के नीचे खड़ी/मोटर वालों की ओर लपकती हैं/कि जन्नत तारी हो गई है जमीं पर!
फिर पूछा है कि: आखिर क्या दुश्मनी है तुम्हारी उन लोगों से/जो भलेमानुसों की तरह अपनी कुर्सी पर चुपचाप/बैठे-बैठे मुल्क की भलाई के लिए/रात-रात जागते हैं-और गांव की नाली की मरम्मत के लिए/मॉस्को, न्यूयॉर्क, टोकियो, लंदन की खाक/छानते फकीरों की तरह भटकते रहते हैं…
इसके बाद शुरू की है असली मुनादी: तोड़ दिए जाएंगे पैर/और फोड़ दी जाएंगी आंखें/अगर तुमने अपने पांव चलकर/महल-सरा की चहारदीवारी फलांगकर/अंदर झांकने की कोशिश की!/….खबरदार यह सारा मुल्क तुम्हारा है/पर जहां हो वहीं रहो/यह बगावत नहीं बर्दाश्त की जाएगी कि/तुम फासले तय करो और/मंजिल तक पहुंचो/इस बार रेलों के चक्के हम खुद जाम कर देंगे/नावें मझधार में रोक दी जाएंगी/बैलगाड़ियां सड़क-किनारे नीम तले खड़ी कर दी जाएंगी/ट्रकों को नुक्कड़ से लौटा दिया जाएगा/सब अपनी-अपनी जगह ठप!/क्योंकि याद रखो कि मुल्क को आगे बढ़ना है/और उसके लिए जरूरी है कि जो जहां है/वहीं ठप कर दिया जाए!
यह मुनादी यहीं नहीं ठहरती. ‘जलसा-जुलूस, हल्ला-गुल्ला, भीड़-भड़क्के का शौक’ रखने वाली रियाया को बेताब न होने को कहकर उसके ‘दर्द’ की दवा बताती हुई कहती है कि बाश्शा को उससे पूरी हमदर्दी है और उसके (बाश्शा के) खास हुक्म से उसका अपना दरबार जुलूस की शक्ल में निकलेगा, जिसके दर्शन के लिए रेलगाड़ियां रियाया को मुफ्त लादकर लाएंगी, बैलगाड़ी वालों को दोहरी बख्शीश मिलेगी, ट्रकों को झंडियों से सजाया जाएगा, नुक्कड़-नुक्कड़ पर प्याऊ बैठाया जाएगा और जो पानी मांगेगा उसे इत्र-बसा शर्बत पेश किया जाएगा.
रियाया को लाखों की तादाद में उस जुलूस में शामिल हाने का फरमान सुनाती हुई मुनादी और आगे बढ़ती है: हमने अपने रेडियो के स्वर ऊंचे करा दिए हैं/और कहा है कि जोर-जोर से फिल्मी गीत बजाएं/ताकि थिरकती धुनों की दिलकश बलंदी में/इस बुड्ढे की बकवास दब जाए!
इतिहास गवाह है कि देश की तत्कालीन दमनकारी सत्ता ने इस मुनादी के सात महीने बाद ही आतंरिक सुरक्षा को खतरे के नाम पर विपक्षी नेताओं को बरबस जेलों में ठूंस दिया और समाचार माध्यमों पर सेंसर लगा दिया था. देश पर इमरजेंसी थोपकर देशवासियों के प्रायः सारे मौलिक अधिकार छीन लिए थे, सो अलग. उनके ये अधिकार तभी बहाल हो पाए थे जब 1977 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने इस सत्ता को बेदखल कर डाला था.
इतिहास की इस गवाही के बीच इन दिनों यह कविता जब भी याद आती है (और सच कहें तो याद तो बारंबार आती है, क्योंकि इस बीच उक्त इतिहास की ऐसी पुनरावृत्ति हो गई है कि इमरजेंसी की मुनादी किए बिना ही देश में इमरजेंसी से भी विकट हालात पैदा कर दिए गए हैं, मौलिक अधिकारों को छीनने की घोषणा किए बिना ही उन्हें सरकार की अनुकंपा का मोहताज बना दिया गया है, साथ ही समाचार-माध्यमों को खुद ही खुद को सेंसर कर लेने को मजबूर.) कलेजे में हूक-सी उठने लग जाती है.
कारण यह कि आज जो भी नागरिक अपने किवाड़ों को अंदर से/कुंडी चढ़ाकर बंद कर लेने और खिड़कियों के परदे गिराने यानी आज्ञापालक प्रजा बन जाने को राजी नहीं हो रहे, सत्ता की भृकुटियां उन पर टेढ़ी हो जाने में एक पल भी नहीं लगा रहीं, न ही उनके मौलिक अधिकारों का कोई मतलब रह जाने दे रही हैं- नागरिक लोकगायक या गायिका, कवि, कार्टूनिस्ट, कलाकार अथवा पत्रकार हो, तब तो और भी.
गौरतलब है कि ये भृकुटियां तक तक टेढ़ी नहीं होतीं, जब तक कोई लोकगायिका सवालिया न हो जाए या कवि चारण बनने से मनाकर न दे और मान करने पर तो वे कथावाचकों और कॉमेडियनों तक को नहीं बख्शती.
जहां तक मीडिया और पत्रकारों की बात है, उनके बड़े हिस्से ने खुद ही अपने हाथ-पांव सिकोड़ लिए हैं और जिन्होंने नहीं सिकोड़े हैं, उन पर सत्ताधीशों को आड़े हाथों लेने वाली खबरें ही नहीं, प्राइमरी स्कूलों में प्रधानाध्यापकों व अधिकारियों की मिलीभगत से छात्रों को घटिया मिड-डे मील परोसे जाने की खबर देना भी भारी पड़ जाता है. हां, कोई अखबार, एजेंसी या पोर्टल वगैरह अपनी वस्तुनिष्ठता से सत्ता की बड़ी हितहानि पर आमादा हो जाए तो उसके विरुद्ध छापों का ब्रह्मास्त्र चला दिया जाता है. नजीर तो यहां तक है कि किसी एक पत्रकार को निपटाने के लिए पूरे न्यूज चैनल को ही ‘खरीद’ लिया जाता है.
गौर कीजिए, नौ साल पहले तक सरकारों को शिकायत होती थी कि मीडिया हमेशा उसके प्रति विसंवादी या विपक्ष की भूमिका निभाता रहता है, मगर आज विपक्ष को शिकायत है कि सत्ता का पक्ष ही मीडिया का पक्ष हो गया है. पहले वह जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाता था, अब सरकार की आवाज जनता तक पहुंचाता है.
पहले अखबारों के संपादकीय पृष्ठों पर व्यंग्य का एक स्तंभ तो होता ही होता था, जो स्वनामधन्य संपादकों के बेवजह की विद्वता बघारने वाले अग्रलेखों के मुकाबले ज्यादा पढ़ा जाता था. पाठक उसका भरपूर रस लेते थे. पर अब यह स्तंभ अपवादस्वरूप ही किसी अखबार में छपता होगा.
कारण? एक संपादक मित्र की मानें तो सत्ताधीशों को आईना दिखाए बगैर व्यंग्य में धार नहीं आती और उसी से परहेज बरतने का रिवाज चला दिया गया हैं. कार्टूनों का हाल भी व्यंग्यों से अलग नहीं है.
कमाल यह कि कोई डॉक्यूमेंट्री प्रतिबंधित की जाती है तो उसकी गुणवत्ता के सवाल को दरकिनार करके उसे बनाने वालों महाभियोग लगाया जाता है कि उन्होंने इससे पहले फलां मसले पर डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाई थी और अब जो बनाई है, उसकी टाइमिंग गलत है. क्या अर्थ है इसका?
यही तो कि डॉक्यूमेंट्री बनाने की सशर्त इजाजत भी सिर्फ उन्हें होगी, जिन्होंने विगत में सत्ताधीशों के लिए अनुकूल विषयों पर उनके लिए उपयोगी डॉक्यूमेंट्रियां बनाई हों. एक ओर यह हाल है और दूसरी ओर कई विश्लेषक कहते हैं कि मीडिया संस्थान खुद ही डर गए हैं तो सरकार क्या करे? जैसे कि उनका डर दूर करने का दायित्व निभाने के लिए देश में कोई और सरकार है!
हां, 1975 के और आज के हालात में कम से कम एक फर्क है: तब विपक्षी नेताओं की एकमुश्त गिरफ्तारियां कर ली गई थीं लेकिन अब मौके ताड़कर सिलसिलेवार की जा रही हैं- बहाना कोई भी हो सकता है- भ्रष्टाचार में लिप्तता का या प्रधानमंत्री के अपमान का. कानून का पालन करने वाली एजेसियों को पहले तो स्वतंत्रतापूर्वक काम नहीं करने दिया जाता, फिर कहा जाता है कि सरकार उनके काम में दखल नहीं देती. हालांकि सरकारी हमलों से न्यायालय तक नहीं बच पा रहे.
विडंबना यह कि इमरजेंसी का नया इतिहास बना रहे ये सत्ताधीश खुद के उस यानी 1975 की इमरजेंसी के पीड़ित होने का दावा करते हुए उसकी आलोचना करते भी नहीं लजाते! क्या आश्चर्य कि उनकी यह निर्लज्जता अब तेजी से ऐसे उपक्रम में बदलती जा रही है जिसके तहत वे अपनी ‘इमरजेंसी’ में उस रोशनदान को भी नहीं बचने देना चाहते, जो 1975 की इमरजेंसी में बचा रह गया था!
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं.)