1971 में बांग्लादेश के संघर्ष के वक़्त जब भारत कई हलकों में पाकिस्तान के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप की तोहमतें झेल रहा था, लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि लोकतंत्र किसी देश का आंतरिक मामला नहीं हो सकता और उसका दमन सारे संसार की चिंता का विषय होना चाहिए.
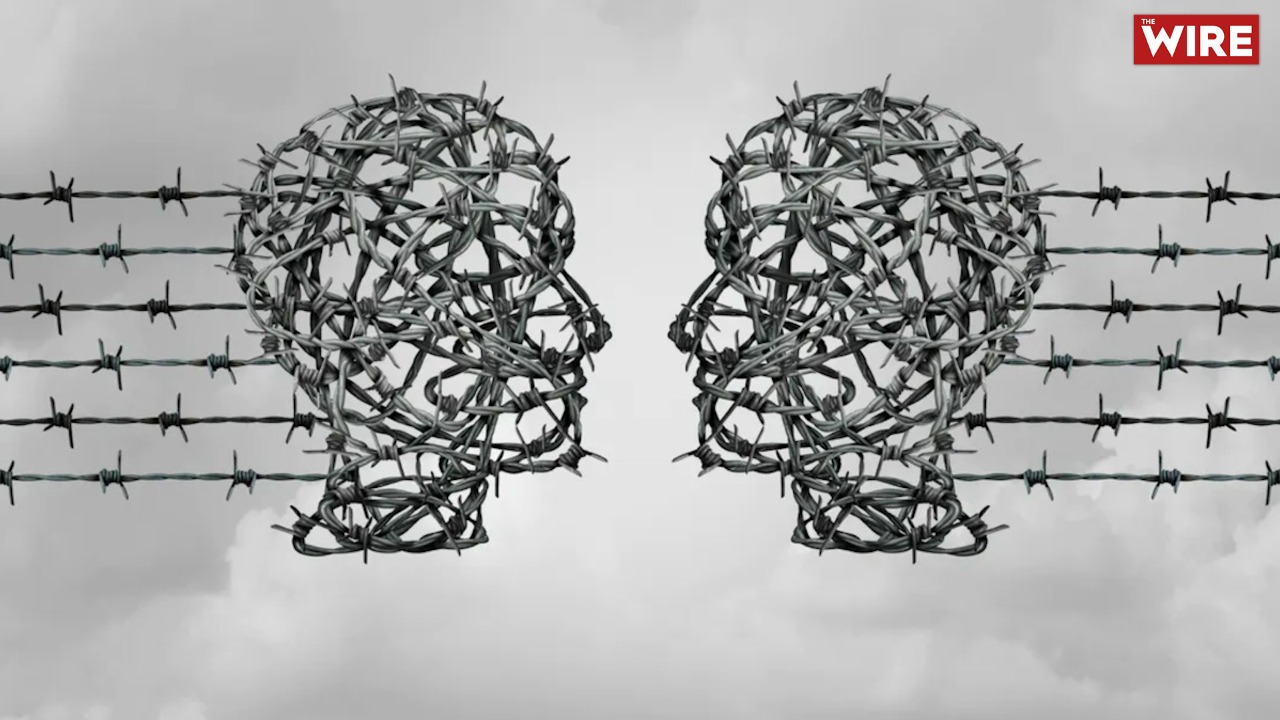
क्या आजादी और लोकतंत्र या इन दोनों के लिए किए जाने वाले संघर्ष किसी देश का आंतरिक मामला हो सकते हैं? और क्या विदेशियों की धरती पर उनसे इनके समर्थन के आह्वान या मांग को संबंधित देश के आंतरिक मामले में ‘विदेशी हस्तक्षेप को आमंत्रण’ माना जा सकता है?
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लोकनायक जयप्रकाश नारायण दोनों ने अपने-अपने वक्त में लगातार कठिन होती कसौटियों के बीच भी इन सवालों के जवाब नहीं में दे रखे हैं. अफसोस की बात है कि इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार किसी भी तरह मानने या समझने को तैयार नहीं हो पा रहे कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गत दिनों लंदन में कथित रूप से ऐसे विदेशी हस्तक्षेप को आमंत्रित करके कोई अपराध नहीं किया.
इसीलिए पहले तो समूचा सत्तापक्ष राहुल द्वारा इस सिलसिले में सार्वजनिक तौर पर दी गई सफाई को दरकिनार कर इस बेतुकी मांग को लेकर आसमान सिर पर उठाता रहा कि वे उस कसूर के लिए माफी मांगें, जो उन्होंने किया ही नहीं. फिर सत्तापक्ष द्वारा खुद ही संसद की कार्यवाही रोकने का रिकॉर्ड बनाने में भी संकोच नहीं किया गया और उसकी आड़ में बजट पर चर्चा और बहुचर्चित हिंडनबर्ग-अडानी मामले की संयुक्त संसदीय समिति द्वारा जांच की मांग से भागता रहा.
फिर जैसे इतने पर भी संतोष न हो, एक अदालती फैसले की आड़ में (जिसे सुनाने वाली अदालत ने खुद ही उसे अपील तक के लिए स्थगित कर रखा है) राहुल को लोकसभा की उनकी सदस्यता से वंचित करने के बाद भी केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू बारंबार रट्टा मारे जा रहे हैं कि राहुल ने देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप के लिए विदेशी शक्तियों को आमंत्रित करने का नाकाबिल-ए-माफी गुनाह किया. यह पंक्तियां लिखने तक रिजिजू ने आखिरी बार यह बात तब कही, जब राहुल के खिलाफ आए अदालती फैसले के साथ ही उनके संसदीय जनादेश के निलंबन को लेकर जर्मनी की सत्तापक्ष के लिए असुविधाजनक प्रतिक्रिया सामने आई.
सच्चाई यह है कि रिजिजू द्वारा राहुल की जिस बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है, उसमें उन्होंने इतना भर ही कहा था कि भारत जैसे विशाल देश में लोकतंत्र खत्म हुआ तो उसका असर उसकी सीमाओं के अंदर तक ही सीमित नहीं रहने वाला. इसलिए बाकी दुनिया को उसे इस रूप में देखना चाहिए कि अंततः वह भी उससे प्रभावित होगी ही होगी. इसके आगे उन्होंने साफ कहा था कि भारत के लोकतंत्र का क्षरण भारतवासियों की समस्या है और उससे वही अपने तई संघर्ष करेंगे.
लेकिन पल भर को मान लें कि उन्होंने अपने लोकतंत्र के संरक्षण के भारतवासियों के संघर्ष में विदेशी कहें या शेष विश्व का समर्थन मांगा या उसे हस्तक्षेप के लिए आमंत्रित किया, तो क्या इसके लिए उन्हें अपराधी करार दिया जा सकता है, जैसा कि नरेंद्र मोदी सरकार उन्हें कई तरह से ‘दंडित’ करके साबित करना चाहती है?
अगर हां, तो इससे एक नया प्रश्न यह पैदा होता है कि क्या अब हम ऐसी दुनिया में रहने लगे हैं, जिसमें खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहने वाले हमारे देश की सरकारों को विदेशी पूंजी निवेश तो दुनिया भर में कहीं से भी आमंत्रित करने की ‘आजादी’ है- भले ही उससे हमारे लोकतंत्र के समक्ष ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो कि वह उसके साइड इफेक्ट्स से बचने में ही हलकान होता रहता हो, लेकिन लोकतंत्र की रक्षा के संघर्ष में समर्थन का कोई भी आह्वान देश की भौगोलिक सीमाओं का मोहताज होकर रह गया है?
ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में, जब निरंकुश पूंजी को भौगोलिक सीमाओं के अतिक्रमण की हर तरह की सहूलियत हासिल है, लोकतंत्र को उनका मोहताज बनाना क्या उस पर जुल्म या जोर-जबरदस्ती का पर्याय नहीं है? अगर इन सवालों का जवाब हां में है, जो है ही, तो कहना होगा कि इससे भली तो लगभग सौ साल पहले की वह दुनिया ही थी, जिसमें रहते हुए हम अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे और गुलाम होने के बावजूद उसके लिए पूरी दुनिया का समर्थन जुटाने को आजाद थे.
वरिष्ठ गांधीवादी कुमार प्रशांत ने (जो गांधी शांति प्रतिष्ठान के प्रमुख हैं और जयप्रकाश नारायण के मानसपुत्र माने जाते हैं) हाल में ही एक लेख में लिखा है कि उस लड़ाई के दौरान महात्मा गांधी ने दुनिया भर से भारत की जनता के समर्थन की अपील की थी, लेकिन और तो और, वे जिस दुर्दमनीय गोरी सत्ता के मुकाबिल थे, उसने भी इसे विदेशी हस्तक्षेप को न्योता करार देने की हिमाकत नहीं की थी.
गौरतलब है कि 12 मार्च, 1930 को 79 साथियों के साथ ऐतिहासिक दांडी यात्रा पर निकले महात्मा गांधी ने घोषणा कर दी थी कि वे कौए या कुत्ते की मौत मर जाएंगे, लेकिन जब तक आजादी नहीं मिल जाएगी, तब तक लौटकर साबरमती आश्रम नहीं आएंगे. उन्हीं दिनों किसी अमेरिकी पत्रकार ने उनसे पूछा था कि इस लड़ाई में वे दुनिया से क्या कहना चाहते हैं? तब उन्होंने एक पर्ची पर लिखा था, ‘सत्ता की अंधाधुंधी और जनता के अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं.’
कुमार प्रशांत ने लिखा है कि ऐसा एक नहीं, कई बार हुआ, जब महात्मा ने उस लड़ाई में दुनियाभर को अपनी भूमिका निभाने का आमंत्रण दिया. ब्रिटेन व अमेरिका के नागरिकों को खुले पत्रों में उन्होंने यह भी लिखा कि वे भारत के स्वतंत्रता संघर्ष को ठीक से समझें और अपनी सरकारों पर उसके समर्थन के लिए दवाब डालें. क्योंकि सत्य व अहिंसा के रास्ते लड़ी जा रही इस लड़ाई से विश्व का व्यापक हित जुड़ा है. तब किसी ने उनसे यह नहीं कहा कि वे देश के आंतरिक मामले में विदेशी हस्तक्षेप आमंत्रित कर रहे हैं और उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए.
कुमार प्रशांत पूछते हैं कि तब वैसे ही ‘अपराध’ के लिए राहुल से माफी की मांग क्यों की जा रही है? उन्होंने लंदन में ‘भारत के लोकतंत्र के जिस वैश्विक आयाम की बात उठाई, उसने तो मेरे जैसे लोकतंत्र के सिपाहियों को मुदित ही किया है कि राहुल हमारे लोकतंत्र के इस आयाम को समझते भी हैं, तथा उसे इस तरह अभिव्यक्त भी कर सकते हैं.’ लेकिन ‘चूंकि यह छुद्र दलीय राजनीति का मामला नहीं है, इसलिए पार्टीबाज इसे न समझेंगे, न समझना चाहेंगे.’
तिस पर बात सिर्फ बापू या आजादी की लड़ाई की ही नहीं है, 1971 में बांग्लादेश के संघर्ष के वक्त भी, जब भारत कई हलकों में पाकिस्तान के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप की तोहमतें झेल रहा था, लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि लोकतंत्र किसी देश का आंतरिक मामला नहीं हो सकता और उसका दमन सारे संसार की चिंता का विषय होना चाहिए.
लेकिन विडंबना देखिए कि 1975 में देश पर इमरजेंसी थोपी जाने के बाद उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को समझानी चाही. तो उन्होंने समझने से साफ मना कर दिया था. बिल्कुल वैसे ही जैसे आजकल नरेंद्र मोदी सरकार मना कर रही है- वह भी आजादी के अमृतकाल में, जब बकौल कुमार प्रशांत ‘अगर देश का लोकतंत्र कमजोर पड़ता है या इसका संसदीय स्वरूप बदल कर कुछ दूसरा रूप लेता है तो संसार भर में लोकतंत्र की दिशा में हो रही यात्रा ठिठक जाएगी या दूसरी पटरी पर चली जाएगी. क्योंकि दुनिया भर में दक्षिणपंथ की लहर-सी उठी हुई है.’
ऐसे में राहुल या किसी और नेता का पश्चिमी लोकतांत्रिक शक्तियों को आगाह करते हुए यह कहना कि अपना संसदीय लोकतंत्र बचने का हम जो प्रयास कर रहे हैं, उसे वे सही संदर्भ में समझें और उसके हित में खड़ी हों, कुफ्र क्योंकर हो सकता है? खासकर जब अतीत में भारत अपनी ऐसी ही नीति के तहत दुनिया भर में मुक्ति युद्धों का समर्थन करता आया है.
लेकिन अंत में कहना होगा, यह सब तर्क और विवेक की बातें हैं, जबकि आज उन्हें सर्वथा दरकिनार कर अनुकूलित सत्यों (पढ़िए: अर्धसत्यों) व तथ्यों (पढ़िए: भ्रमजालों) से काम लिया जा रहा है और बात को वहां तक पहुंचा दिया गया है, जहां ऐसे ‘तर्क’ भी दिए जाने लगे हैं कि जब हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है तो खालिस्तान की बात करना अपराध कैसे हो सकता है! अब यह आप पर है कि इसे एक कुतर्क का दूसरे के लिए रास्ता बनाना कहें या यह कि एक कट्टरता अनिवार्य रूप से दूसरी की पूरक होती है.
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं.)




