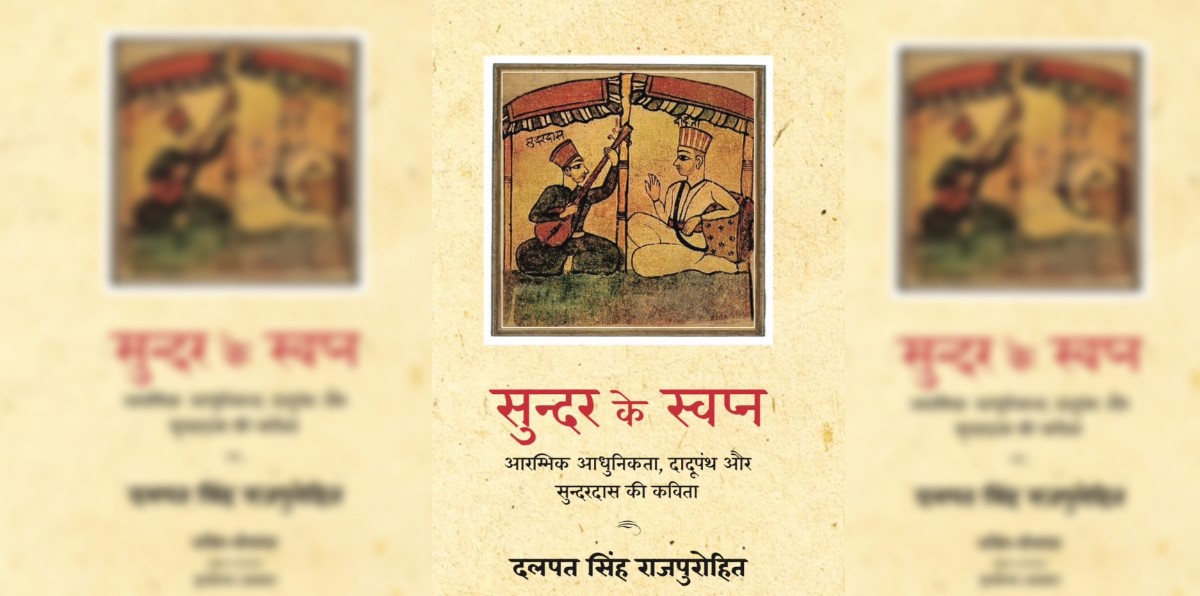दलपत सिंह राजपुरोहित की ‘सुंदर के स्वप्न’ हिंदी साहित्य के आलोचना-वृत में एक ज़रूरी हस्तक्षेप है जो संत सुंदरदास के जीवन और रचनाओं के ज़रिये भारत की आरंभिक आधुनिकता, उसकी बहु-धार्मिकता और बहु-भाषिकता, हिंदी साहित्य के इतिहास और उसके काल-विभाजन तथा रीतिकाल को लेकर किए गए दुष्प्रचार पर सोचने पर विवश करती है.
कबीर और दादू की परंपरा में आए संत सुंदरदास पर यह मौलिक काम करते हुए दलपत राजपुरोहित कई महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि रीतिकाल और भक्तिकाल के विभाजन के पुनर्मूल्यांकन पर सोचा जाना चाहिए. किताब का शीर्षक भले ही ‘सुंदर के स्वप्न’ हो लेकिन यह किताब संत सुंदरदास की जीवनी नहीं है बल्कि उनके ज़रिये एक बड़े विमर्श को छेड़ने की कोशिश है.
यह विमर्श भक्ति और रीति काल के समय विभाजन, भारत की आरंभिक आधुनिकता, बहुभाषिक परंपरा, और संतों के रचनाक्रम और समाज के साथ उनके अंतर्संबंधों को नई दृष्टि में देखने का है जिसमें कई स्त्रोतों के ज़रिये दलपत नई स्थापनाएं रखने की कोशिश करते हैं.
यह किताब अपने शुरुआती पन्नों में ही यह स्पष्ट करती है कि अगर भारत की देशज आधुनिकता को समझना है तो इसके लिए यूरोपीय मानदंडों से इतर जाकर सोचने की ज़रूरत है. इस बात को लेखक आगे बढ़ाते हुए इस दिशा में जॉन रिचर्ड, शेल्डन पोलॉक, सिंथिया टेलबट, कैथरीन एशर, संजय सुब्रहमण्यम, पुरुषोत्तम अग्रवाल और रामविलास शर्मा के काम का हवाला देते हैं लेकिन साथ ही कहते हैं कि देशज आधुनिकता को लेकर जो बहसें हुई हैं उनके अंतर्विरोधों पर भी चर्चा होनी ज़रूरी है.
दलपत इन अंतर्विरोधों की शुरुआत करते हैं रीति काल और भक्ति काल के विभाजन से और इस पारंपरिक विश्लेषण से कि ‘आरंभिक आधुनिक समाज के निर्माण होने तथा भक्तिकाल के आगमन व आधुनिक काल के बीच में रीतिकाल की उपस्थिति बाधा समझी गई है (पृष्ठ 29).’
लेखक के अनुसार, रीतिकाल के बारे में यह समझ कोलोनियल समझ से उपजी है. वो कहते हैं कि कर्नल जेम्स टॉड के मौखिक परंपराओं के संग्रहण और जॉर्ज ग्रियर्सन के काम के आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के काल विभाजन को सशक्त आधार दिया और भक्ति और रीति काल को दो कालखंडों में बांटा और आगे चलकर भक्ति को लोक से और रीतिकाल को सामंती व्यवस्था से जोड़ दिया गया. जाहिर है कि रीति काल को सामंती व्यवस्था से जोड़ते ही इसे खराब माना जाने लगा और इस समय में रचे साहित्य को निचले दर्जे का. रामविलास शर्मा ने रीति काव्य को सामंती या दरबारी काव्य तक कहा जिससे रीति-कविता के महत्व को नकारने की भूमिका बन गई.
अगर पारंपरिक काल-विभाजन से देखें, तो दादूपंथी कवि संत सुंदरदास रीतिकाल के कवि माने जाएंगे लेकिन उनकी कविता भक्ति से ओत-प्रोत है और उसमें भक्ति काव्य की कई चीज़ें परंपरा में आई हैं. दलपत कहते हैं कि रीति और भक्ति के बीच काल विभाजन से इतर इन्हें परंपरा के रूप में देखा जा सकता है और इसे परंपरा के रूप में देखने पर देशज आधुनिकता की एक लकीर पकड़ी जा सकती है जहां कबीर के लोकवृत से आगे निकलकर दादू जैसे संत होते हैं और खुद को कबीर से जुड़ा बताते हैं.
दादू के प्रसिद्ध शिष्यों में सुंदरदास न केवल लोकवृत्त से जुड़े होते हैं बल्कि वो कई मायनों में आधुनिक कवि भी हैं जहां शास्त्र और लोक की आवाजाही है, जहां लोक शास्त्र को देशिक प्रकृति के अनुसार ढाल रहा है. सुंदरदास एक बहुभाषिक और बहु-धार्मिक परिवेश के अंग तो थे ही, वे उस बहुलतावादी लोकवृत्त की रचना भी कर रहे थे. उनकी कविता को उस समय उभरे मुग़ल-राजपूत दरबारी वर्ग में प्रतिष्ठा मिली हुई थी. यह कविता व्यापारियों के नेटवर्क से भारत के बड़े हिस्से में पहुंच रही थी.
सुंदरदास संत-परंपरा में सर्वाधिक शिक्षित संत थे. उन्होंने बीस वर्षों तक औपचारिक रूप से बनारस में शिक्षा ग्रहण की और राजस्थान में अपना मठ निर्मित किया जहां बीसवीं सदी तक शिक्षित संत रहते आए हैं. उन्होंने हस्तलेखों के महत्व को समझते हुए अपनी कविता को लिपिबद्ध करवाया.
पुरुषोत्तम अग्रवाल और अन्य आलोचकों का मानना है कि कबीर जहां लोक के कवि हुए और भक्ति काल को को लोकवृत्त के संदर्भ में देखा जाना और समझना चाहिए वहीं जॉन एस. हॉली कहते हैं भक्ति या रीति काल को नेटवर्क की अवधारणा के तौर पर देखना चाहिए. यानी कि भक्ति काल की कविताएं एक किस्म के नेटवर्क के ज़रिये दूर-दूर तक पहुंची हैं और दरबारी वर्ग इसमें सहयोगी था.
अग्रवाल दलपत के काम को जॉन एस. हॉली की नेटवर्क अवधारणा का हिस्सा मानते हैं लेकिन मेरे हिसाब से दलपत का नेटवर्क जॉन हॉली से कम प्रेरित है. दलपत कहते हैं कि रीति काल के कवि खासकर सुंदरदास के काम को सिर्फ नेटवर्क की अवधारण से समझना उसका सरलीकरण होगा. वे दादूपंथ और सुंदरदास को या किसी भी भक्ति-समुदाय को अपने क्षेत्रीय परिवेश में स्थापित करके देखने का प्रस्ताव रखते हैं.
सुंदरदास को दादूपंथ की परंपरा में समझते हुए यह देखना भी ज़रूरी होगा कि दादू मुस्लिम धुनिया थे जबकि सुंदरदास वैश्य समुदाय से थे. दादू के प्रमुख शिष्य रज्जब हुए जबकि सुंदरदास का काम अधिक व्यापक हुआ. सुंदरदास के पास एक स्तर पर बनियों का नेटवर्क तो था ही लेकिन एक समझ और दूरदृष्टि भी थी जिससे उन्होंने अपने काम को लिपिबद्ध कराया और लेखन के महत्व को समझा. इतना ही नहीं, रजवाड़ों के साथ उन्होंने चारण-भाट का नहीं बल्कि सम्मान का संबंध रखा. वे जहां-जहां घूमे (उत्तर भारत में लंबा भ्रमण) वहां-वहां की भाषा में सुंदरदास ने रचनाएं की.
सुंदर दास के ‘पीर मुरीद अष्टक’ को पढ़कर कई बार लग सकता है कि वो सूफी परंपरा के हैं वहीं ‘अजब ष्याल अष्टक’ में उन्होंने अरबी-फारसी शब्दों का खूब प्रयोग किया है. इसी तरह जब वो पंजाब की तरफ जाते हैं तो उनके काव्य में पंजाबी शब्दों की प्रचुरता आ जाती है.
दलपत के अनुसार, यह लोकवृत से इतर सुंदरदास की भाषा-परंपराओं की समझ को भी दर्शाता है. सुंदरदास इस मायने में भी विलक्षण थे कि उन्होंने शास्त्रों का न केवल समुचित अध्यययन किया था बल्कि वो अद्वैत वेदांत पर साधिकार लिखते थे. दलपत मानते हैं कि सुंदरदास जैसे संतों ने ब्रजभाषा में न केवल काव्य लिखा बल्कि काव्यशास्त्र विमर्श, दर्शन, साधना पद्धति और सिद्धांत कथन भी किया जो उन्हें कथित दरबारी कवि के तमगे से अलग करती है और इस आधार पर रीतिकाल के कवियों पर लगे दरबारी-कवि के तमगे पर भी पुर्नविचार की ज़रूरत है.

आधुनिक समय में सुंदरदास जैसे संतों का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है जब भारत में हिंदी को थोपने की कोशिश हो रही है तब हम सुंदरदास जैसे संतों के काम में पाते हैं कि ब्रज भाषा में दर्शन, काव्य लिखा जा रहा था साथ ही संत एक नहीं बल्कि कई भाषा परंपराओं (यहां भाषा परंपरा से तात्पर्य विभिन्न भाषाओं में लिखी-कही जा रही चीज़ों को जानने और अपनाने से है, न कि विभिन्न भाषाओं में लिखने मात्र से) में रचनाक्रम कर रहे थे.
ब्रज कॉस्मोपॉलिटन भाषा बन चुकी थी लेकिन उन्नीसवीं सदी में उसे नियोजित रूप से खत्म कर के खड़ी-बोली हिंदी एक नई भाषा के रूप में उभरी. अगर हमें उत्तर भारत की बहुभाषिक परंपरा, देशज आधुनिकता को समझना है तो इसके लिए हिंदी से पीछे जाकर ब्रजभाषा और अन्य लोकभाषाओं में रचे गए साहित्य को भी देखने, सुनने की ज़रूरत है.
‘सुंदर के स्वप्न’ इन दृष्टियों से एक महत्वपूर्ण पुस्तक बन जाती है कि वो हमें न केवल रीति काल बल्कि नेटवर्क और लोकवृत की स्थापित अवधारणाओं पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करती है. मसलन कबीर लोकवृत के कवि थे लेकिन वे समाज में कैसे स्वीकृत हो रहे थे? कौन उनकी कविता को प्रश्रय दे रहा था? समाज का उनके प्रति रवैया कैसा था उनकी लोक के अलावा बाकी वर्गों में कैसी स्वीकार्यता थी क्योंकि स्वीकार्यता के बिना उनकी रचना का उनके जीवन काल के बाद भी परंपरा में बने रहना असंभव हो जाता है.
‘सुंदर के स्वप्न’ में दो चीज़ों की कमी मैंने महसूस की एक पाठक के तौर पर. दलपत शुरुआत में आरंभिक आधुनिकता की बात करते हुए उसे भारतीय संदर्भों में समझने आग्रह तो करते लेकिन उन भारतीय संदर्भो पर ज़्यादा चर्चा नहीं करते. वो कौन-से भारतीय टूल्स होंगे जिनसे भारतीय आधुनिकता को समझा जाए और क्या वो टूल्स पश्चिम के लिए भी लागू होंगे? संभवत वो आगे अपनी किसी पुस्तक में इस पर विचार करेंगे.
दूसरा, एक छोटा सा मुद्दा जो दलपत उठाते हैं अकबर की ‘सुलह ए कुल’ नीति का. आम तौर पर इतिहास में हमने ‘दीन ए इलाही’ का जिक्र पढ़ा है. इतिहास के जानकार बताते हैं कि अकबर के समय के फ़ारसी सूत्रों में कहीं भी ‘दीन ए इलाही’ का ज़िक्र नहीं है बल्कि ‘सुलह ए कुल’ की ही बात होती है. एक सामान्य पाठक के लिए यह भ्रामक हो जाता है. अगर लेखक कुछ पंक्तियों में यह स्पष्ट करते तो शायद आम पाठक के लिए ज्यादा सहूलियत होती.
इस पुस्तक के ज़रिये दलपत सुंदरदास को न केवल भारतीय साहित्यितिक इतिहास के कैनन में ला खड़ा करते हैं बल्कि कैनन के काल-विभाजन को लेकर भी रुचिकर व महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास के भी डिकोलोनाइजेशन की ज़रूरत है.
(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं.)