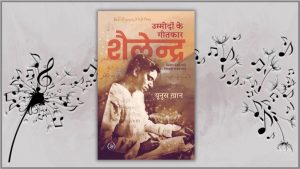अवध की बलरामपुर रियासत गंगा-जमुनी तहज़ीब का पूर्वी द्वार कही जाती थी. 1997 में कुछ क्षेत्रों को मिलाकर इसे ज़िला बनाया गया तो रहवासियों ने विकास के सपने देखे. पर अब हाल यह है कि 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में यह देश का सबसे बुरा प्रदर्शन करने वाला चौथा ज़िला रहा.

आजादी से पहले अवध में एक बलरामपुर नाम की रियासत हुआ करती थी. सूबे में सबसे बड़ी थी और उसकी ‘गंगा-जमुनी तहजीब का पूर्वी द्वार’ कहलाती थी. बदली हुई परिस्थितियों में अब वह उत्तर प्रदेश के देवीपाटन मंडल का इसी नाम का जिला है.
मायावती के मुख्यमंत्रीकाल में 25 मई, 1997 को उसके आस-पास के गोंडा व सिद्धार्थनगर जिलों के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर इस जिले को सृजित किया गया तो उसके निवासियों ने अपने सपनों को बडे़-बड़े पंख लगा लिए थे. लेकिन उसके बाद से अब तक का उसका चौथाई शताब्दी का इतिहास गवाह है कि जल्दी ही वे सपने टूटकर बिखर गए. इस हद तक कि नवंबर, 2021 में नीति आयोग ने राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया तो उसमें बलरामपुर देश के सबसे बुरा प्रदर्शन करने वाले जिलों में चौथे स्थान पर था.
अभी भी यह स्थिति बदली नहीं है. भले ही किसी के लिए वह ‘मिनी लखनऊ’ है तो किसी के लिए ‘लहुरी (छोटी) काशी’. हां, अवध की अनूठी तहजीब का पूर्वी द्वार तो वह है ही. उसकी भौगोलिक अवस्थिति की विशिष्टता के चलते उसकी पूर्वी सीमा खत्म हुई नहीं कि अलग तहजीबी ताने-बाने वाली हिमालय की तराई की झलक दिखलाई पड़ने लगती है.
स्वाभाविक ही इस जिले को दो तहजीबों के संगम के रूप में पहचाना जाता है. इसके बावजूद कि वह लंबे अरसे तक दक्षिणपंथी राजनीति और सामंतवाद का गढ़ रहा है, जिसके चलते एक कांग्रेस को छोड़ दें तो उसकी धरती पर राजनीति की समाजवादी व साम्यवादी धाराएं गंगा-यमुना के बीच लुप्त सरस्वती की तरह दिखती आई हैं.
इसलिए आज, दक्षिणपंथ के देशव्यापी उभार के दौर में, उसे यह बात कुछ ज्यादा ही जोर देकर याद दिलाई जाने लगी है कि वह प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ‘दूसरा गृह जनपद’ है और उसे दो भारतरत्नों- दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी (1957 व 1967) और नाना जी देशमुख (1977)-को लोकसभा का मुंह दिखाने का श्रेय हासिल है. इनमें अटल प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने नानाजी को राष्ट्रपति भी बनाना चाहा था, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया था.
हद यह कि अभी महिला पहलवानों द्वारा अपने कथित यौन उत्पीड़न के विरुद्ध मोर्चा खोलने से पहले तक जिले से इस पर भी ‘गर्व’ करने को कहा जाता था कि 2004 में उसने अपना ‘आखिरी सांसद’ बाहुबली बृजभूषण शरण सिंह को चुना था. दरअसल, 2004 के बाद नए परिसीमन में उसकी बलरामपुर लोकसभा सीट का अस्तित्व समाप्त कर उसे श्रावस्ती में समाहित कर दिया गया, इसलिए बृजभूषण उसके ‘आखिरी सांसद’ हो गए.
जिले के जानकार लोग बताते हैं कि बलरामपुर के पांच सौ सत्तर साल के इतिहास में उसकी ‘कभी जमीं तो कभी आसमां नहीं मिलता’ वाली नियति कभी नहीं बदली. 1857 में अपने तत्कालीन नरेश दिग्विजय सिंह (1836-1882) की अंग्रेजभक्ति के कारण वह देश की स्वतंत्रता के पहले संग्राम में लड़ने और बलिदान देने का इतिहास बनाने से चूक गया.
उस संग्राम में पड़ोस की गोंडा और तुलसीपुर रियासतें प्राणपण से-अपना अस्तित्व तक दांव पर लगाकर-अंग्रेजों ने जूझ रही थीं, तो दिग्विजय सिंह ने अंग्रेजों का पक्ष चुन लिया था, जिसके बदले अंग्रेजों ने उनको न सिर्फ ‘नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया’ (केसीएसआई) बनाया, बल्कि तुलसीपुर और गोंडा के नायकों के पराभव के बाद उनके कई क्षेत्रों को बलरामपुर में मिलाकर उसको अवध की सबसे बड़ी रियासत बना दिया.
इसके ठीक सौ साल बाद 1957 के लोकसभा चुनाव में बलरामपुर ने पं. जवाहरलाल नेहरू की, जो खुद कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगने आए थे, अनसुनी कर जनसंघ के अटल बिहारी वाजपेयी को पहली बार लोकसभा पहुंचाया और 1967 में इसकी पुनरावृत्ति भी की. लेकिन अटल प्रधानमंत्री बने तो उनकी सत्ता का सारा चाक्चिक्य बलरामपुर के बजाय लखनऊ के हिस्से आया, क्योंकि तब वे लखनऊ के सांसद थे.
इससे पहले 1977 में जनता पार्टी की आंधी में बलरामपुर ने उसके नानाजी देशमुख के मुकाबले कांग्रेस के टिकट पर मैदान में उतरी अपनी महारानी लक्ष्मी कुंअरि को हराने में भी संकोच नहीं किया था. तब नाना जी ने इन्हीं रानी से जमीन लेकर उस पर बहुचर्चित जयप्रभाग्राम बसाया और उसे लेकर कई सुनहरे सपने दिखाए थे. लेकिन यह गांव भी अब बलरामपुर नहीं गोंडा जिले में है और प्रतीकात्मक महत्व का ही रह गया है.
यहां जानना जरूरी है कि 1997 से पहले बलरामपुर लोकसभा क्षेत्र गोंडा जिले का हिस्सा हुआ करता था और उसके प्रतिनिधि बारंबार उसे जिला बनाने की मांग किया करते थे. लेकिन अब वह जिला है तो भी उसका विडंबना से पीछा नहीं छूटा है: नए परिसीमन का शिकार होकर लोकसभा क्षेत्र नहीं रह गया है.
बहरहाल, जो लोग भी बाहर से बलरामपुर आते हैं, एक सवाल जरूर पूछते हैं- क्या उसका नाम श्रीकृष्ण के बड़े भाई बलराम के नाम पर पड़ा? जवाब है- नहीं. राजा माधो सिंह (1339-1480) के कब्जे में आने से पहले उसका नाम रामगढ़ गौरी था. उस पर कब्जे के लिए हुई लड़ाई में माधो का छोटा बेटा बलरामदास शाह मारा गया तो उन्होंने उसके नाम पर इसका बलरामपुर नाम रख दिया.
लेकिन उसके निवासी कहते हैं कि तब से अब तक उसकी मुकम्मल जहां की तलाश कभी पूरी होने की ओर नहीं जा पाई. दो-दो बार उसके सांसद रहे अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री बनने पर भी उसके प्रति इतनी ही ‘कृतज्ञता’ बरती कि उसकी मीटरगेज रेलवे लाइन को ब्रॉड गेज में बदलवा दिया और अब उस पर बलरामपुर से उनकी जन्मभूमि ग्वालियर तक ‘सुशासन एक्सप्रेस’ चलती है.
हां, स्थिति का दूसरा पहलू थोड़ा आश्वस्त करने वाला है: राजनेताओं से निराश होते आए बलरामपुर को उसके जाये दानिश्वरों, अदीबों व साहित्यकार अपनी प्रतिभा व सृजन से उसको भरपूर सींचते और उसके गौरव का देश की सीमाओं के पार समूचे भारतीय उपमहाद्वीप में विस्तार करते रहे हैं. एक अली सरदार जाफरी को छोड़ दें, तो उसे उनमें किसी से भी बेगानापन नहीं झेलना पड़ा है.
ठीक है कि जाफरी एक बार उसे छोड़कर गए तो आगे वह उनसे छूटा ही रहा, लेकिन पद्मश्री बेकल उत्साही (शफी खां लोदी) हों, सर्वेश्वरदयाल सक्सेना, विश्वनाथ त्रिपाठी, शत्रुघ्नलाल या चंद्रेश्वरर, सबके सब बलरामपुर के और बलरामपुर इन सबका रहा है. देश के वरिष्ठ आलोचकों में शुमार कवि व संस्मरणकार विश्वनाथ त्रिपाठी ने बहुचर्चित ‘बिसनाथ का बलरामपुर’ नामक किताब लिखकर उसको अपना बताया है, तो चंद्रेश्वरर ने भी अपनी किताब का नाम ‘मेरा बलरामपुर’ रखा है. शायद ही कोई और जिला हो, जिसके लेखकों का उससे अपनापा इतनी भावप्रवण कृतियों के रूप में सामने आया हो.
प्रसंगवश, तीसरे सप्तक के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को जिस कुआनो का कवि कहा जाता है, वह नदी बलरामपुर के दक्षिणी छोर से होकर बहती है और इस अर्थ में अजूबा है कि उसके उद्गम का कुछ पता नहीं चलता. वह रहस्यमय ढंग से बहराइच जिले के बसऊपुर गांव के पास एक सोते से निकलती है.
दूसरी ओर, एक ही बलरामपुर के होकर भी बेकल उत्साही और अली सरदार जाफरी हमेशा दो अलग-अलग ध्रुवों पर रहते रहे. बेकल शायरी को राजनीति से दूर रखने पर जोर देते रहे, जबकि भारतीय उपमहाद्वीप के लासानी जनप्रतिबद्ध शायर, वामपंथ के पैरोकार और न सिर्फ बलरामपुर बल्कि सारे ‘अवध की खाक-ए-हसीं’ पर निसार जाफरी को ऐसा परहेज कतई कुबूल नहीं था. कथाकार शत्रुघ्नलाल ‘उम्मीद’ नाम की पत्रिका निकालते थे तो उसका ध्येयवाक्य रखा था ‘दीन को मानकर जो झगड़े हैं, दीन को जानकर नहीं होते.’
लेकिन कहना मुश्किल है कि बलरामपुर ने इसे कितना माना! चंद्रेश्वर की मानें तो अपने अतीत के किस्से किसी न किसी रूप में वह अब भी सुनाता रहता है. इतना ही नहीं, वह लोकतंत्र में राजतंत्र तो राजतंत्र में लोकतंत्र की पदचाप भी सुन लेता है. भले ही उसे अभी भी डी क्लास सिटी ही कहा जाता हो, उसने अपनी पारंपरिक व क्लासिक छवि के साथ कवि सम्मेलनों व मुशायरों के लिए जगह बचा रखी है. और बात है कि अपने रंगीन व शौकीन मिजाज के चलते वह अपनी बची-खुची सामंती भव्यताओं का जश्न मनाने को भी अभिशप्त है.
विश्वनाथ त्रिपाठी को वह स्वतंत्रता-पूर्व का मिनी भारत लगता है, जहां रियासत है, अंग्रेज अधिकारी हैं, स्वतंत्रता आंदोलन और उसके नेताओं को लेकर बड़े शहरों जैसी सजगता-सक्रियता है, हिंदू-मुसलमान के प्रश्न हैं, मुस्लिम लीग है और आरएसएस है. वे उसके लिए जेल भी गए, और फिर अपनी विचारशीलता के चलते उससे मुक्त हुए.
बिसनासथ का बलरामपुर में उसकी स्मृति-यात्रा में उन्होंने पूर्वी अवध के विडंबनाओं, आपदाओं व संकटों से भरे सांस्कृतिक-सामाजिक और राजनीतिक जीवन का अत्यंत जीवंत और व्यापक चित्र खींचा है, लेकिन इस सवाल का जवाब वे भी नहीं ही दे पाए हैं कि उसे मुकम्मल जहां कब और कैसे मिलेगा? मिलेगा भी या नहीं?
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं.)