कभी-कभार | अशोक वाजपेयी: बहुत ज़रूरी है कि कबीर को एक कवि के रूप में देखा-समझा जाए जो अपने विचार से कविता की स्वायत्तता को अतिक्रमित नहीं बल्कि पुष्ट करता है.
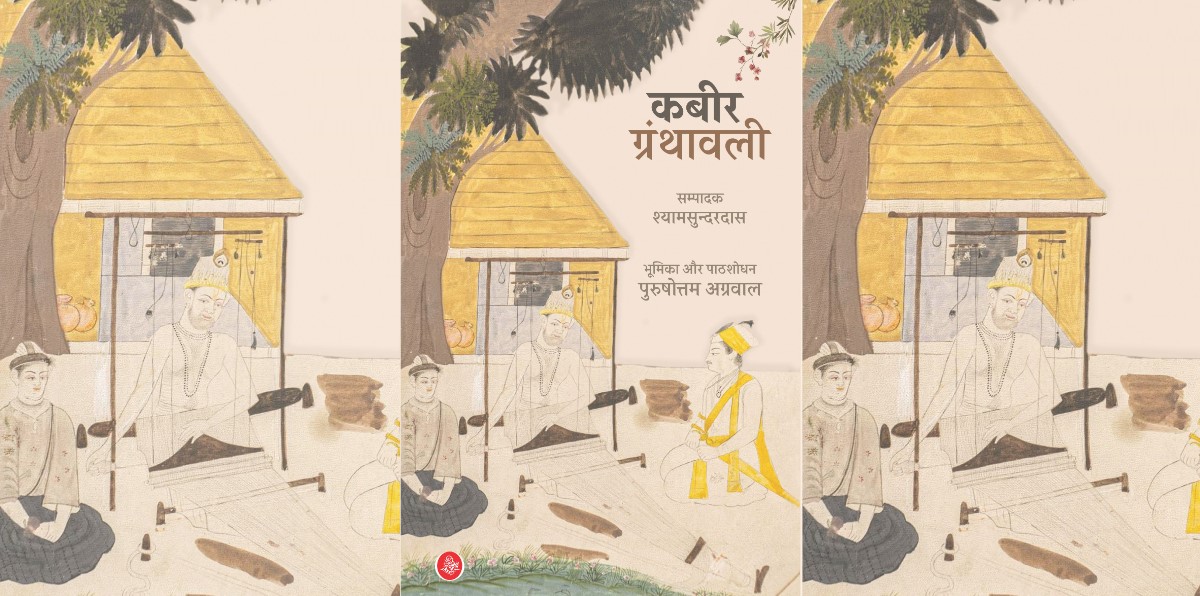
हमारे जिन कवियों को कालातीत और कालजयी निरंतरता प्राप्त है उनमें कबीर प्रमुख हैं, तुलसीदास के अलावा. एकाध दशक पहले एक व्यापक सर्वेक्षण से पता चला था कि इस उपमहाद्वीप में कबीर के अनुयायियों की संख्या लगभग छह करोड़ है. इनमें से अधिकांश उनके बाद उन्हें धर्म गुरु मानकर बने पंथों के अंतर्गत आते हैं.
पर कबीर साहित्य, कलाओं, विशेषतः संगीत में, इन दिनों विकराल हुए लोकप्रिय संगीत में भी लगातार मौजूद रहे आए हैं. उन्हें एक साथ अध्यात्म और सामाजिक प्रतिरोध के कवि के रूप में देखा-समझा और जब-तब उपयोग किया जाता है. वे एक किंवदंती पुरुष भी हैं जिनके जीवन और मृत्यु के बारे में, कविताओं के बारे में भी अपार किंवदंतियां हैं. उनके द्वारा मौलिक रूप से कितना रचा गया और कितना उनके लहजे में लोकरचना में यानी क्या प्रामाणिक कबीर है और क्या नहीं है इसका अंतिम निश्चय भी नहीं हो पाया है.
पिछले कुछ बरसों से आलोचक-रचनाकार पुरुषोत्तम अग्रवाल ने कबीर का गहन अध्ययन और अनुसंधान किया है और कबीर को समझने-देखने की कई नई दृष्टियां विन्यस्त की हैं. इसी क्रम में उन्होंने श्यामसुंदर दास द्वारा संपादित प्रसिद्ध ‘कबीर ग्रंथावली’ का एक सुसंपादित-सुशोधित नया संस्करण प्रकाशित किया है, राजकमल से, जिसका लोकार्पण पिछले सप्ताह नई दिल्ली में हुआ.
यह ग्रंथ अपनी लंबी भूमिका और नए पाठ दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. पाठ में जो संशोधन किए गए हैं वे तर्कसंगत हैं, गहरे अनुसंधान का प्रतिफल हैं और अब हम यह कह सकते हैं कि एक लगभग प्रामाणिक कबीर हमारे लिए उपलब्ध है. यह जानना दिलचस्प है कि जो भूलें दास-संस्करण में थीं उनमें से कितनी ही छापे की भूलों के साथ पिछले लगभग 80 वर्षों से बार-बार प्रकाशित होती रही हैं.
नागरी प्रचारिणी सभा ने प्रकाशक के रूप में इतनी लंबी अवधि तक बहुत ही बुनियादी ढंग की सावधानी भी नहीं बरती.
पुरुषोत्तम जी की लगभग सौ पृष्ठों की भूमिका विद्वत्ता, शोध से भरी-पूरी होते हुए भी बहुत रोचक और पठनीय है. उसकी शुरुआत में ग्रंथावली के इस नए संस्करण की ज़रूरत का औचित्य बताते हुए कुछ बेहद रोचक तथ्य दिए गए हैं- वैसे तथ्यों की रोचकता तो इस भूमिका में बार-बार मिलती है.
दास-संस्करण में, छपाई के स्तर पर जो असावधानी बरती गई है और जो एक सदी से बार-बार छपे उस ग्रंथ में लगभग एक सदी बरक़रार रही है उसमें गादह आदम में, इंद्र ईद में, ज्ञान श्वान में, जगनाथ जमनाथ में, साध साथ में बदल गए हैं और भयानक अनर्थ उपजा है. अनेक पदों की कई पंक्तियां ग़ायब हैं. कई दूसरे संस्करण इसी अशुद्ध पाठ का सहारा लेकर ऐसे ही अनर्थ उपजाते रहे हैं. ग़लत ढंग से पढ़े जाने का स्वाभाविक परिणाम है ग़लत व्याख्या- आवागमन से मुक्ति के स्थान पर स्तन पान और कुच-मर्दन. विभिन्न विद्वानों ने जो कबीर-पाठ निर्धारित किए उनकी भूलों का विस्तृत और सतर्क विवेचन इस भूमिका में किया गया है. यह भी स्पष्ट होता है कि अनेक विद्वान-संपादकों के अपने पूर्वाग्रहों के कारण कुछ भूलें या कुपाठ हुए हैं.
पुरुषोत्तम जी ने यह भी स्पष्ट कहा है कि ‘पांडुलिपियों के तुलनात्मक अध्ययन से हम बस सही अनुमान लगा सकते हैं कि सोलहवीं सदी में कबीर छाप के कौन-से पद किन-किन रूपों में उपलब्ध थे. वे अपने जीवन की चदरिया जो ज्यों की त्यों धर गए लेकिन उन्होंने जो काव्य रचा वह हमें ज्यों का त्यों, परवर्ती लिपिकारों के माध्यम से ही उपलब्ध हुआ है. हम कबीर के किसी सबद या साखी की भावना और उसमें निहित तर्क तक तो पहुंच सकते हैं लेकिन उनके मुख से निकले शब्दों को ज्यों का त्यों पाना हमारे लिए असंभव है.’
लंबे विवेचन के बाद पुरुषोत्तम जी कहते हैं कि ‘जो कुछ भी कबीर थे, अपनी खोज, अपने चुनाव के फलस्वरूप थे. वे विवेक-संपन्न व्यक्ति थे, किसी सामाजिक पहचान या किसी ख़ास विचार के निशान या प्रतीक भर नहीं. उन्होंने अनेक विचार-सरणियों और साधना-प्रणालियों से संवाद करते हुए विविध जीवनानुभवों से गुज़रते हुए अपना विवेक विकसित किया था.’
कबीर की अपने समय में लोकवृत्त में जो लगभग केंद्रीय उपस्थिति थी उस संदर्भ में आगे कहा गया है कि ‘वे नया पंथ निकालना भी नहीं चाहते थे, उनका रास्ता तो ब्रह्म विचार का, राम से भी और समाज से भी परस्पर सम्मान और समानता का रिश्ता बनाने का रास्ता था. …लेकिन यह तो धर्मसत्ता मात्र के विरुद्ध मनुष्य की आत्मसत्ता की आवाज़ है. तरह-तरह की सामाजिक अस्मिताओं के प्रवक्ताओं के विरुद्ध विवेकवान व्यक्तिसत्ता की आवाज़ है.’
दारा शिकोह के एक ग्रंथ ‘हसनात उल आरिफ़ीन’ से दिया गया यह उद्धरण मैंने पहली बार इस भूमिका में ही पढ़ा:
‘कबीर हिन्दोस्तान के आरिफ़ों में से हैं वे अपने ढंग से पेशवा (अग्रणी व्यक्तित्व, नेता) हैं, मुर्शिद हैं, बानी हैं. वे रामानन्द के पैरो (अनुयायी) हैं. वे हिन्दोस्तान के एक फुकरा (फ़कीरों) में से एक थे. कबीर अगरचे बुनकर थे लेकिन अज़ीम बुनकर थे. उनके अशआर में तौहीद बहुत ज़्यादा है जो उन्होंने हिन्दुस्तानी जुबान में कहे हैं. मुसलमान उनको मुसलमान समझते हैं, और ग़ैर-मुस्लिम उन्हें गै़र मुस्लिम समझते हैं. लेकिन वे खुद इन दोनों से ऊपर हैं.’
पुरुषोत्तम जी आगे यह बताते हैं कि ‘आरंभिक आधुनिक कालीन भारत में चल रहे सांस्कृतिक स्वभाव को समझे बिना आप समझ ही नहीं सकते कि खुद को न हिंदू न मुसलमान मानने वाले कबीर… जैसे लोगों के प्रशंसकों में हिंदू और मुसलमान दोनों क्योंकर शामिल थे…. कबीर से बहुत से लोग नाराज़ ज़रूर थे लेकिन उनके दौर में ऐसे भी लोग थे जो कबीर द्वारा स्वयं को अल्लाह और राम का पंगुड़ा (बेटा) एक साथ कहने के मर्म तक पहुंचते थे…’
भारत की देशज आधुनिकता और उसमें भक्ति युग की निर्णायक भूमिका एक ऐसी निर्णायक स्थापना है जिसका सतर्क सतथ्य प्रतिपादन पुरुषोत्तम जी पहले कर चुके हैं और इस भूमिका में उन्होंने उसे संक्षेप में बताया है.
उनके अनुसार ‘देशज आधुनिकता को स्वर देने वाला भक्ति-लोकवृत्त आरंभिक आधुनिक काल के सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता के परिणामस्वरूप ही विकसित हुआ.’ वे इस पर इसरार करते हैं कि ‘प्रशंसकों और निंदकों दोनों के ही आकलन में कबीर की ज्ञानमीमांसा के अनोखेपन की स्वीकृति अंतर्निहित है. किसी धर्मग्रंथ या शास्त्रवचन को किसी कथन, मान्यता या सामाजिक व्यवहार के प्रमाण के तौर पर स्वीकारने के लिए कबीर तैयार नहीं.’
एक और पक्ष जिसकी और पुरुषोत्तम जी इशारा करते हैं वह यह है कि ‘कबीर दार्शनिक व्यवस्था के साथ कविता के जैसे संबंध का प्रस्ताव अपनी रचनाशीलता में करते हैं, वह न तो आचार्य शुक्ल को स्वीकार्य है, न आचार्य द्विवेदी को. कारण यह कि इन दोनों के परस्पर संबंध की समझ दोनों आचार्यों की एक सी ही है- किसी न किसी दार्शनिक वाद का काव्यानुवाद होने में ही कविता की सार्थकता.’
यह बहुत ज़रूरी है कि कबीर को एक कवि के रूप में देखा-समझा जाए जो अपने विचार से कविता की स्वायत्तता को अतिक्रमित नहीं बल्कि पुष्ट करता है.
(लेखक वरिष्ठ साहित्यकार हैं.)




