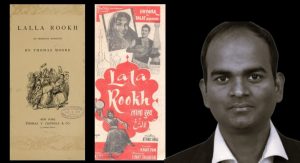यदि कोई विश्वविद्यालय अपने शिक्षक के अकादमिक कार्य के साथ खड़ा नहीं हो सकता तो वह कितना भी विश्वस्तरीय होने का दावा करे, वह व्यर्थ ही है.

यह मानी हुई बात है कि विश्वविद्यालय केवल पढ़ाई-लिखाई और नौकरी के लिए आवश्यक योग्यता प्रदान करने वाली जगह नहीं बल्कि समाज की चेतना तथा उस के सामान्य बोध (कॉमन सेंस) को भी निर्मित करने वाली संस्था है. यही कारण है कि जब कभी भी, कहीं तानाशाही जैसी व्यवस्था शासन के केंद्र में आ जाती है तो उस का गहरा नियंत्रण विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षण-संस्थान पर होने लगता है. यह इतना तीव्र, महीन और सूक्ष्म तरीक़े से होता है कि हर वह चीज़ जो सत्ता की आलोचना से जुड़ती है उस का अपराधीकरण कर दिया जाता है.
तानाशाही प्रथमत: और अंततः एक व्यक्ति केंद्रित व्यवस्था है. तानाशाह एक ओर तो सत्ता के सभी प्रतिष्ठानों का दुरुपयोग अपने प्रति हर आलोचनात्मक विचार के दमन एवं स्व के प्रक्षेपण के लिए करता है और फिर वह दूसरी ओर समाज में गहराई तक धंसे हुए हीनताबोध को लगातार सहलाता भी रहता है. यह सहलाना भी अपने प्रारूप में इस प्रकार होता है कि हीनताबोध से भरे हुए समाज को यह महसूस कराया जाता है कि तानाशाह जो कुछ भी कह रहा है या कर रहा है वह उन के उदात्त तथा उच्च संवर्धन के लिए है. यह प्रक्रिया इतनी नशीली और मादक होती है कि तानाशाह द्वारा धड़ल्ले से बोला जा रहा झूठ और निर्लज्जतापूर्वक की जा रही लफ़्फ़ाजी एकदम सच महसूस होते हैं.
समाज के इस बोध को बनाने में सत्ता संचार-तंत्र का भी ज़बरदस्त सहारा लेती है. संचार-तंत्र भी तानाशाह के महिमामंडन के लिए अपार झूठ और कुतर्कों का उपयोग करता है. आधुनिक समय में इस तरह की प्रक्रिया को तुरत ही चुनौती मिलने की यदि संभावना कहीं से भी है तो वे हैं उच्च शिक्षण-संस्थान. ऐसा इसलिए कि उच्च शिक्षण-संस्थान का सब से मुख्य काम सोचना और हर बात की परीक्षा करना है. यह इसलिए भी कि ज्ञान की शर्त ही है कि हर बात की परीक्षा हो, उसका विश्लेषण हो और जो ज्ञान सामने आ रहा है उसकी भी बार-बार परीक्षा हो सके.
अब समझा जा सकता है कि यदि तानाशाह और उसके सहयोगी लगातार झूठ बोल रहे हों और उच्च शिक्षण-संस्थानों को अपने अनुसार काम करने दिया जाए तो उच्च शिक्षण-संस्थानों का जितना भी अधिक पतन हुआ मान लिया जाए ( इस में बहुत हद तक सच्चाई भी है.) तब भी यह संभावना तो है ही कि झूठ और खोखले दावों की वस्तुस्थिति उजागर हो जाए. यही कारण है कि भारत के उच्च शिक्षण-संस्थानों पर कई तरह से शिकंजा लगातार कसा जा रहा है.
कभी उनके सामने भौंडे रूप में ‘सैनिक’ को रखकर यह कहा गया कि सीमा पर ‘सैनिक’ अपनी जान की बाजी लगाए हुए हैं और आप हैं कि सुविधाओं की मांग कर रहे हैं ? फिर अधिकांश केंद्रीय उच्च शिक्षण-संस्थानों पर ‘सिविल सेवा आचार-संहिता’ थोप दी गई जिसके अनुसार कोई भी कर्मचारी (ध्यान रहे कि शिक्षण और शोध की प्रकृति कितनी भी सामान्य सरकारी कार्यों से अलग हो पर उच्च शिक्षण-संस्थान में शिक्षक भी कर्मचारी है और उसकी कक्षा तथा शोध महज़ एक काम हैं!) किसी भी सरकारी नीति की आलोचना नहीं कर सकता.
अब सोचा जा सकता है कि यदि अर्थशास्त्र का कोई प्रोफेसर 2016 में की गई ‘नोटबंदी’ की आलोचना जितने भी प्रमाणों, तथ्यों एवं विश्लेषणों से करे पर उपर्युक्त प्रावधान के कारण उसे ‘कारण बताओ नोटिस’ ज़ारी करने से लेकर निलंबित या बर्ख़ास्त तक किया जा सकता है. ठीक इसी प्रकार अभी ‘नई शिक्षा नीति’ या ‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020’ का शोर बहुत है. इसके बारे में एक साधारण-सा तथ्य यह है कि इसे संसद में बहस या विचार करने मात्र के लिए भी नहीं प्रस्तुत किया गया.
अब अगर कोई भी शिक्षक इस में दर्ज़ बिंदुओं की तार्किक आलोचना सप्रमाण करे तब भी उसे कई तरह से कठघरे में खड़ा किया जा सकता है. पिछले नौ-दस वर्षों में ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं जिन से यह साफ़ समझा जा सकता है कि ऊपर के उदाहरण कल्पना मात्र नहीं बल्कि हक़ीक़त हैं.
कई शिक्षकों को कक्षा में पढ़ाते समय कुछ कहने के लिए निलंबित कर दिया गया, कहीं परीक्षा के प्रश्न पूछने पर यही स्थिति आई. कहीं शिक्षक को ज़बरदस्ती अवकाश पर भेज दिया गया. कहीं शिक्षकों को विद्यार्थियों के साथ खड़े होने पर निलंबित कर दिया गया. कहीं विश्वविद्यालय के एक विभाग द्वारा अंतरराष्ट्रीय संस्था के साथ मिलकर की गई आयोजित संगोष्ठी में निमंत्रित कुछ वक्ताओं के होने पर की गई शिकायत के कारण उस विभाग को ही उस आयोजन से जबरन अलग होना पड़ा.
इतना ही नहीं ऑनलाइन शिक्षण के एक निजी मंच पर भी ऑनलाइन अध्यापन में कहे एक सामान्य वाक्य पर भी शिक्षक को हटा दिया गया. ध्यान से देखने पर भारत के उच्च-शिक्षण संस्थान अभी इसी तरह के वातावरण में सांस लेने को विवश हैं.
अभी की एक ख़बर एक निजी विश्वविद्यालय से जुड़ी है. इस का नाम अशोका विश्वविद्यालय है. इसके अर्थशास्त्र के सहायक प्राध्यापक सब्यसाची दास ने एक शोध-पत्र लिखा जिस में उन्होंने 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में वर्तमान सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी द्वारा हेराफेरी की संभावना का विश्लेषण किया है. हालांकि उनका यह विश्लेषण केवल 11 ‘सीटों’ के प्रसंग में ही था पर इस शोध-पत्र के प्रकाशन के बाद ही अशोका विश्वविद्यालय ने इससे अपने-आप को अलग कर लिया.
सब्यसाची दास को इस्तीफ़ा भी देना पड़ा. अच्छी बात इस प्रसंग में यह है कि अशोका विश्वविद्यालय के शिक्षक और विद्यार्थी सब्यसाची दास के साथ खड़े हैं. लेकिन अशोका विश्वविद्यालय का जो बयान उपलब्ध है (यानी विश्वविद्यालय के प्रशासन और प्रबंधन की ओर से) उस में यह ध्वनि प्रतीत होती है कि उक्त शोध-पत्र को वह गंभीर अकादमिक कार्य नहीं मान रहा है.
समझा जा सकता है कि जब कोई भी विश्वविद्यालय (प्रशासन और प्रबंधन)अपने शिक्षक के अकादमिक कार्य के साथ खड़ा नहीं हो सकता तो वह कितना भी विश्वस्तरीय होने का दावा करे, वह व्यर्थ ही है. इसी अशोका विश्वविद्यालय में कुलपति के तौर पर कार्य कर रहे प्रताप भानु मेहता को भी पहले कुलपति पद से और बाद में प्रोफेसर के पद से भी इस्तीफ़ा देना पड़ा था. अब एक तरफ़ तो भारत के उच्च शिक्षण-संस्थानों में इस तरह की घटनाएं दिनोंदिन बढ़ रही हैं तो दूसरी ओर भारत के ‘विश्वगुरु’ बन जाने या भविष्य में ऐसी स्थिति प्राप्त कर लेने के दावे किए जा रहे हैं.
‘विश्वगुरु’ होने के दावे
औपनिवेशिक शासन और भयंकर क़िस्म से स्तरीकृत समाज होने के कारण भारत में पश्चिम को लेकर एक अज़ीब तरह की स्थिति महसूस की जा सकती है. एक ओर तो पश्चिम को लेकर हीनताबोध के कारण उसके प्रति बिना कारण ही नफ़रत का भाव है, तो दूसरी ओर उसी पश्चिम की तरह बनने तथा उस से स्वीकृति पाने की चाहत भी है. इस मनोविज्ञान का परिणाम यह होता है कि ज्ञान-विज्ञान के हर पश्चिमी विकास को अपने यहां पहले से ही उपस्थित होने मात्र की कल्पना से ही एक संतुष्टि का भाव मिलता है. इसीलिए ऐसे कथन जिन पर सारी दुनिया हंसने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकती उन्हें अभी के भारत में प्रमुखता दी जाती है.
उदाहरण के लिए, कभी कहा जाता है कि भगवान गणेश को हाथी का सिर लगाने की कथा में ‘प्लास्टिक सर्जरी’ थी, तो कभी यह कहा जाता है कि महाभारत के संजय को जो दिव्य-दृष्टि मिलने और फिर उन के द्वारा कुरुक्षेत्र के युद्ध का आंखों देखा वर्णन ‘इंटरनेट’ था और कौरवों के पैदा होने की कथा (कथा यह है कि धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी पांडु की पत्नी कुंती से पहले गर्भवती हुई थीं. दो वर्ष तक उन्हें कोई संतान नहीं हुई. कुंती ने युधिष्ठिर को जन्म पहले दिया, तो ज्येष्ठ पुत्र की परंपरा होने के कारण राजा बनने का अधिकार युधिष्ठिर को ही मिलेगा, यही सोचकर दुख एवं ग़ुस्से में गांधारी ने अपने पेट पर बहुत कसकर वार किया, जिससे उन का गर्भ सौ भागों में विभक्त हो गया. फिर महर्षि व्यास आए और उन्होंने गर्भ के इन टुकड़ों को सहेजकर पात्र में रखने का सुझाव दिया और यह भी आश्वासन दिया कि तेरी सौ संतानें इस से होंगी.) ‘टेस्ट ट्यूब बेबी’ का रूप था.
ऐसी बातें श्रेष्ठ संवैधानिक एवं शैक्षणिक पदों पर आसीन लोग बिना किसी संकोच के करते हैं और इसी के बल पर भारत को तथाकथित ‘विश्वगुरु’ बना रहे हैं.
यह तो मानी हुई बात है कि ज्ञान की कोई सरहद नहीं हो सकती. हर तरह का ज्ञान अंततः पूरी मनुष्यता के काम आता है. यदि ऐसा नहीं होता तो पीढ़ियों से पश्चिम और अमेरिका में भारतीय भाषा एवं साहित्य के समर्पित विद्वान इन विषयों पर उत्तम कार्य न कर रहे होते! जितना हल्ला भारतीय ज्ञान का किया जाता रहा है और किया जा रहा है उससे हटकर थोड़ा भी ध्यान दिया जाता तो हमारी स्थिति इतनी पंगु नहीं होती.
एक-दो उदाहरण ही पर्याप्त हों- अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय ने भारतीय भाषाओं के अधिकांश प्रामाणिक शब्दकोशों को ‘ऑनलाइन’ उपलब्ध करा दिया है. इसमें आप ‘ऑनलाइन’ उन शब्दकोशों में शब्दों के अर्थ खोज सकते हैं. पूछा जा सकता है कि ऐसा कोई उपक्रम भारत में क्यों नहीं हुआ?
इसी प्रकार अमेरिका की ही संस्था archive.org ने अधिकांश भारतीय भाषाओं के पुराने साहित्य को बिल्कुल मुफ़्त में ‘ऑनलाइन’ उपलब्ध कराया है. यह भी सोचा जा सकता है कि भारतीय भाषाओं की पत्रिकाओं का ‘जेस्टोर’ (https://www.jstor.org) जैसा कोई संग्रह क्यों नहीं है?
इसी प्रकार हिंदी के प्राचीन एवं मध्यकालीन साहित्य से जुड़े पांडुलिपि-अध्ययन एवं शोध का श्रेष्ठ काम अभी भी पाश्चात्य विद्वान कर रहे हैं. हिंदी के ही विदेशी विद्वानों की बात करें तो वे प्राय: हिंदी के साथ संस्कृत, फ़ारसी या उर्दू में से एक भाषा ज़रूर जानते हैं और इन सबके साथ एकाध दूसरी भारतीय भाषा (बांग्ला, मराठी या कन्नड आदि) भी सीखने की कोशिश करते हैं. भारत में ऐसा कोई अभ्यास नहीं किया जाता. इसलिए स्वाभाविक तौर पर हमारे शोध में वह गहराई तथा गंभीरता नहीं आ पाती. तब इन परिस्थितियों में कौन-सा विश्वगुरु और कैसा विश्वगुरु?
(लेखक दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाते हैं.)