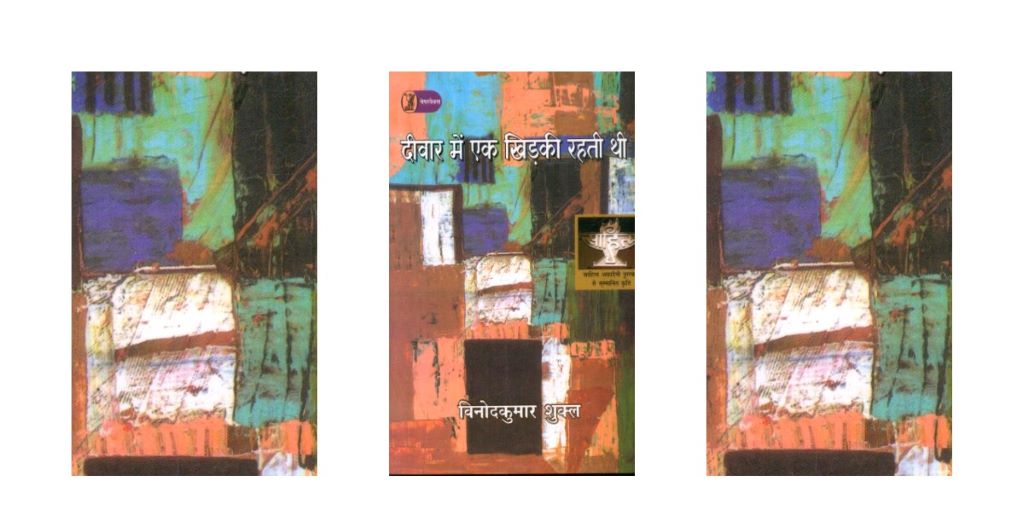साहित्यिक रचना के पाठ और पुनर्पाठ की प्रक्रिया उस शीशे को मांजने की तरह होती है, जिसकी चमक उसके बार-बार रगड़ने से निखरती है. कई रचनाएं इसीलिए पहले पाठ में अर्थ के जितने स्तर नहीं खोलती, वह उसके बाद के पाठ में अधिक मुखरित होकर आती है. हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल की रचना ‘दीवार में एक खिड़की रहती थी’, इस दृष्टिकोण से एक ऐसी ही रचना है, जिसके पुनर्पाठों के अंतराल में ही उसकी कई-कई अर्थ-छवियां स्पष्ट होती हैं.
यह उपन्यास पहले-पहल धारावाहिक रूप में ‘साक्षात्कार’ पत्रिका में अप्रैल 1996 से नवंबर 1996 के बीच अंकों में प्रकाशित हुआ था. आगे चलकर वाणी प्रकाशन ने 1997 में इसे पुस्तक रूप में प्रकाशित किया. शुक्ल को इसी पुस्तक के लिए वर्ष 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला.
विनोद कुमार शुक्ल की इस रचना को एकबारगी पढ़ने पर पहला सवाल जो किसी भी साधारण पाठक को परेशान कर सकता है वह यह है कि आखिर इस रचना की प्रासंगिकता क्या है? या लेखक ने इसे लिखने की अपनी योजना से भला किस उद्देश्य की पूर्ति की है? क्योंकि कथा नायक रघुवर प्रसाद के निम्न मध्यवर्गीय संसार में ऐसी कोई भी विशिष्टता नहीं है जिससे कि एकबारगी उसके जीवन को जानने का मन किया जाए. घटनाविहीन जीवन, जहां कुछ भी सनसनीखेज नहीं है, उसके ब्योरों को दर्ज़ करने की आवश्यकता पर देखा जाए तो सवाल उठाना अस्वाभाविक भी नहीं है.
क्योंकि यह रचना जैसा कि आलोचक संजीव कुमार कहते हैं- ‘किसी भी कृति को पढ़ने के हमारे बंधे-बंधाए पारंपरिक तरीकों को चुनौती देती है.’ पर अगर एक पारंपरिक पाठक की दृष्टि से थोड़ा गहरा और अलग हटकर विचार किया जाए तो हमें विनोद कुमार शुक्ल की भारतीय निम्न मध्य वर्ग के जीवन के मनोविश्लेषणात्मक पक्ष पर गहरी पैठ का पता चलता है. यहां एक ऐसा निम्न-मध्य वर्ग- जो अपनी संसाधनहीनता में भी जीवन को रंगीन सपनों से भर कर जीने का हौसला रखता है- शुक्ल की रचनात्मकता के केंद्र में है.
यहां असल उद्देश्य गरीबी में भी सुख के क्षणों को सहेजने और खुशियों से जीवन के अंधेरे कमरे में एक प्रकाश से भरी खिड़की खोलना है. स्वयं विनोद कुमार शुक्ल ने इस बात को कई साक्षात्कार में स्वीकार किया है कि कैसे ‘मैं ठीक-ठीक नहीं बता सकता कि कब और कैसे ‘दीवार में एक खिड़की रहती थी’ एक आम आदमी की खुशी को दिखाता उपन्यास बन गया.’
उपन्यास में रघुवर प्रसाद और सोनसी नवविवाहित युवा दंपति हैं, जो एक कस्बे के आखिरी छोर पर बसे मोहल्ले में रहते हैं. कथा का पूरा ताना-बना इनके जीवन से जुड़े लोगों और इनके आस-पास की प्रकृति के संयोग से बुना गया है. रघुवर प्रसाद आठ सौ रुपये की तनख्वाह पर कस्बे से आठ किलोमीटर की दूरी पर बसे एक महाविद्यालय में गणित के अध्यापक हैं. महाविद्यालय में उनके अलावा जिस एक और पात्र से हमारा परिचय शुक्ल करवाते हैं वह विभागाध्यक्ष हैं जो रघुवर प्रसाद से नियमित रूप से मिलते हैं. एक कमरे के मकान में रघुवर प्रसाद अपनी छोटी-सी गृहस्थी जो अब शादी के बाद बसानी अत्यंत आवश्यक हो गई थी, उसे तमाम कतर-ब्योंत के साथ चलाते हैं. इस एक कमरे में ही अंदर की तरफ लगी एक खिड़की है, जो देखा जाए तो उपन्यास के पूरे विधान में स्वयं एक सूत्रधार की भूमिका में है. यह खिड़की शुक्ल के लिए वह साहित्यिक उपकरण है, जो उन्हें एक साथ दो समानांतर दुनिया रचने का स्थान और अवसर देती है.
इस खिड़की के भीतर बसे कमरे में रोज़मर्रा की निम्न-मध्यवर्गीय ज़िंदगी अपनी पूरी छटा के साथ चलती है. पत्नी सोनसी के चौके से उठने वाले साग-भाजी की खुशबू और बर्तनों की खड़खड़ाहट से मकान का घर में रूपांतरित होते देखना जहां सुखद है, वहीं नित्य रघुवर प्रसाद का अपने महाविद्यालय के लिए निकलना जीवन की गति को रात-दिन के लय में बांधता है. खिड़की के अंदर बसे जीवन में परिवार जनों का एक छोटा-सा सुरक्षित और चिर-परिचित संसार है. एक तरफ, रघुवर प्रसाद के माता-पिता और दस वर्षीय छोटे भाई का परिवार है, जो कस्बे से पचास किलोमीटर की दूरी पर बसे गांव में रहता है और जिसका आना-जाना लगा रहता है. वहीं एक तरफ अगल-बगल के कमरों में रहने वाले पड़ोसी हैं जो कभी खिड़कियों से तो कभी दरवाजों से अपनी उपस्थिति का आभास देते हैं. तो इन सबके साथ ही रोज़ अपनी हाथी पर सवार आता एक युवा साधु भी है जो रघुवर प्रसाद को महाविद्यालय से लाने-ले जाने का काम करता है.
इन सबमें एक तत्व जो सामान्य है, वह है आत्मीयता का. इस आत्मीयता की परिधि का विस्तार सिर्फ अपने स्वजनों तक ही नहीं है, बल्कि अनजान व्यक्ति भी इस आत्मीयता के लेन-देन में बराबर के सहभागी हैं. चाहे वह माता-पिता हों जो, गांव से आते वक़्त सामान लेकर आते हैं या पास-पड़ोसी, जो पत्नी के ससुराल जाने पर रघुवर प्रसाद से दिन-रात खाने का पूछते हैं या फिर वह युवा साधु जो अपने हाथी को इस भरोसे रघुवर प्रसाद के पास बिना कुछ खबर दिए छोड़ कर जाता है कि वह उसका खयाल रख ही लेंगे या वह गूलर के पेड़ पर अपने पिता की मार से बचने के लिए दिन-रात बैठा हुआ मातृहीन लड़का, जिसे सोनसी भर-पेट खाना देती है- सब एक सामूहिक जीवन के स्वाभाविक अवयव हैं.
यह तो हुआ खिड़की के भीतर का संसार, जो कमरे के अंदर फैला हुआ है. पर शुक्ल की रचनात्मकता की असल कल्पनाशक्ति खिड़की के बाहर के संसार को गढ़ने में अपने उत्कर्ष पर दिखती है. कमरे की खिड़की के बाहर दूसरी तरफ खुलने वाली दुनिया, एक जादुई संसार है. लोग यहां भी हैं. मसलन एक बूढ़ी अम्मा जो अनजान पति-पत्नी के इस जोड़े पर अपना सारा स्नेह उड़ेलती है, कुछ बच्चे जो खिड़की के नीचे अधटूटी ईंटों को जमा कर खिड़की के भीतर झांकते हैं. पर देखा जाए तो खिड़की के बाहर का यह जादुई संसार प्रकृति के सुरम्य प्रतीकों का संसार है. यहां कसौटी की तरह परखने वाले चट्टान हैं, नीम के घने जंगल हैं, आम-महुआ की बौरों की सुगंध और मादकता से लदी हुई हवाएं हैं, गोबर से लेपी गईं कोमल पगडंडियां हैं, सज्जित झोंपड़ों के बाहर बनी हुई सुंदर अल्पनाएं हैं जो हवा के साथ-साथ बिना किसी व्यवधान के उड़ती हैं, स्वच्छ तालाब है जिसमें खिले हुए कमल हैं और जिसकी अंदर की रेत को छानने पर सोने के महीन कण तो कभी दाल बराबर टुकड़े भी बूढ़ी अम्मा को मिल जाते हैं.
रघुवर प्रसाद और सोनसी प्रायः खिड़की के बाहर कूदकर इस संसार में विचरते हैं. तालाब में नहाते हैं, चट्टानों पर चांदनी रात में सोते हैं और हवाओं के साथ झूमते हुए मानो स्वयं भी उड़ते हैं. इस जादू से भरे संसार की एक अनोखी बात यह है कि यह सिर्फ रघुवर प्रसाद के परिवार को ही दिखाई पड़ता है. इसीलिए जब विभागाध्यक्ष अपने परिवार को इस हिस्से को दिखलाना चाहते हैं तो उन्हें ढूंढने पर भी कहीं भी यह संसार नहीं मिलता है. पर जब सोनसी और रघुवर प्रसाद इस संसार में खिड़की के माध्यम से प्रवेश करते हैं तो कहीं से भी यह संसार मिथ्या नहीं लगता बल्कि यह जादुई संसार यथार्थ का ही एक सुंदर उज्ज्वल रूप लगता है.
जैसा कि संजीव कुमार कहते भी हैं ‘खिड़की से बाहर का संसार, उस समानांतर दुनिया का एक विकल्प प्रस्तुत करता है, जो वास्तविक दुनिया की तेज़ भागती ज़िंदगी, आपाधापी और यांत्रिकता के विरुद्ध है.’ खिड़की से कूदकर जिस स्वप्निल संसार में रघुवर प्रसाद और सोनसी जब मन चाहे प्रवेश कर जाते हैं वह इस अर्थ में देखा जाए तो एक रूपक है. एक ऐसा रूपक जहां प्रेम अपने सबसे सरल-सहज और आदिम रूप में बिना किसी आधुनिक जीवन के दबावों के फलता-फूलता दिखलाना संभव हो पाता है.
सूक्ष्म स्तर पर अगर इस रचना के पाठ से अर्थ ग्रहण किए जाएं तो यह स्पष्ट होता है कि कैसे यह रचना मानवीय और मानवेतर संबंधों का एक सुंदर और विविधतापूर्ण कोलाज है. यहां शुक्ल ने पारिवारिक जीवन के विभिन्न संबंधों को जितनी सहृदयता से खींचा है वह एक निम्न-मध्यवर्गीय जीवन के अच्छे-बुरे सभी पक्षों को खोल कर रख देता है. जैसा कि आलोचक योगेश तिवारी भी कहते हैं, ‘कहना न होगा कि पति-पत्नी संबंध और पर्यावरण विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यासों के केंद्रीय तत्व हैं. दांपत्य जीवन का इतना मधुर चित्रण- विशेषकर ‘दीवार में एक खिड़की रहती थी’ उपन्यास में- हिंदी उपन्यास में विनोद जी से पहले देखने को नहीं मिलता है.’
वस्तुतः लेखक ने इस पक्ष के चित्रण में एक अभूतपूर्व शैली का विन्यास रचा है. यहां पति-पत्नी न केवल अपने शब्दों से संवाद करते हैं, बल्कि मन की आकांक्षाओं और इच्छाओं का अनकहा संवाद भी उनके संबंधों का एक आयाम रचता है. यह विनोद कुमार शुक्ल की रचनाशक्ति की ही नवीनता है कि प्रेम और प्रणय के चित्र भी आभासी हैं और कहीं भी मांसलता और दैहिकता नज़र नहीं आती.
मसलन, एक प्रसंग उपन्यास से देखें. दिन की शुरुआत में रघुवीर प्रसाद कक्षा पढ़ाने की तैयारी करते रहते हैं और सोनसी खाना बना रही होती है. खाना बनाते-बनाते वह बीच-बीच में रघुवर प्रसाद को देख लेती है. रघुवर प्रसाद को ‘हर बार देखने में उसे छूटा हुआ कुछ नया दिखता था. क्या देख लिया है, यह पता नहीं चलता था. क्या देखना है, यह भी नहीं मालूम था. देखने में इतना ही मालूम होता होगा कि यह नहीं देखा था.’
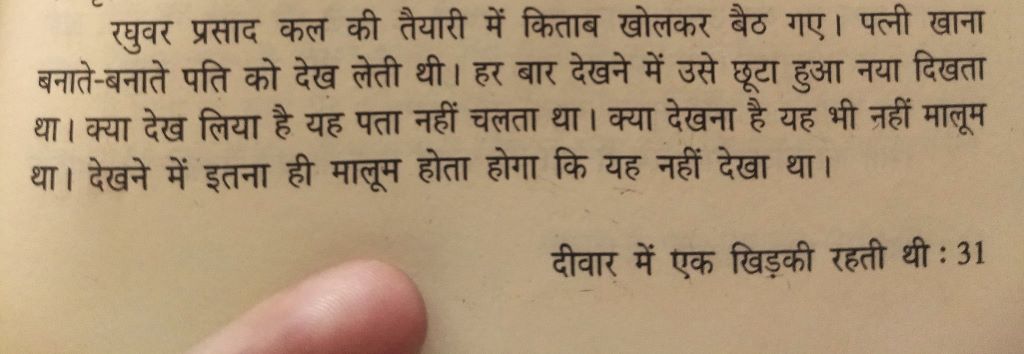
यह आंखों से मनोभावों का पता देता हुआ प्रेम है. इसी प्रकार, प्रकृति भी मानो उनके प्रेम का ही विस्तार है. मसलन, सोनसी के ससुराल जाने पर चिट्ठियां लिखने की कवायद बस इस बात से पूरी हो जाती है कि रात को आकाश देख लेने पर यह मान लिया जाए कि एक ने दूसरे को चिट्ठी भेजी है. आकाशों के द्वारा चलने वाला यह संवाद प्रेम की असीमता का ही बोध करवाता है. शुक्ल लिखते हैं:
‘रघुवर प्रसाद का आकाश देखना रघुवर प्रसाद का चिट्ठी लिखना होगा. चंद्रमा सोनसी के लिए लिखा हुआ संबोधन होगा. तारों की लिपि होगी जिसे तत्काल सोनसी पढ़ लेगी. … बड़ा आकाश लंबी चिठ्ठी होगी. सोनसी खिड़की से छोटा आकाश देखेगी तो छोटी चिठ्ठी होगी. आकाश एक-दूसरे को लिखी चिट्ठी होगी.’
इसीलिए जैसा कि उपन्यास के संदर्भ में आलोचक विष्णु खरे कहते हैं, ‘यहां भाषा कई-कई स्तरों पर अपने प्रयोग की प्रविधियों को स्वयं दर्शाती है. भाषा सिर्फ मुंह से कहे गए मनोभावों को प्रकट करने का माध्यम भर नहीं है बल्कि वह मन की आकांक्षाओं और न कही गई बातों को भी प्रकट करने का माध्यम बन सकती है, यह इस उपन्यास को पढ़कर ही समझ आता है.
मसलन एक उदाहरण से हम इसे समझ सकते हैं. एक दिन खिड़की से खुलने वाली बाहर की दुनिया में बरी चुआती बूढ़ी अम्मा से रघुवर प्रसाद ने कहा, ‘बूढ़ी अम्मा, कपड़े लेने आया था.’ पर बूढ़ी अम्मा ने सुना ‘ बरी चुआने सोनसी को भी बुला लेती.’ इस पर लेखक की यह टिप्पणी इस पूरे संवाद को स्पष्ट करती है ‘यह वाक्य रघुवर प्रसाद कहना चाहते थे, पर दौड़ते हुए कहना भूल गए थे जिसे बूढ़ी अम्मा ने सुन लिया था.’ इसीलिए, यहां बोली गई भाषा में मन के भावों और आकांक्षाओं को भी शुक्ल साथ-साथ गूंथते हुए चलते हैं.
इसी प्रकार भावों को अभिव्यक्त करने की शैली में शुक्ल एक नई भंगिमा ले कर आते हैं जहां कई बार जरूरी नहीं कि कह कर ही सब कुछ अभिव्यक्त किया जाए. मसलन, सोनसी जिन दिनों ससुराल गई हुई है, रघुवर प्रसाद का मन नहीं लग रहा होता है. वह आस-पास, प्रकृति सब से यही पूछते नज़र आते हैं कि सोनसी कब आएगी. खिड़की के बाहर की दुनिया वाली बूढ़ी अम्मा के हाथों की बनाई चाय पीकर ‘रघुवर प्रसाद ने बूढ़ी अम्मा को सोनसी कब आएगी की तरह देखा. दो एक दिन में आ जाएगी की तरह जवाब में बूढ़ी अम्मा ने रघुवीर प्रसाद की तरफ देखा.’
शैली की दृष्टि से बात की जाए तो इस उपन्यास को प्रायः आलोचकों ने जादुई यथार्थवाद के खांचे में रख कर देखा है और कइयों ने तो इसे गैबरिएल गार्सिया मार्क्वेज़ का एक भारतीय रूपांतरण भी समझा है. पर इस संकुचित दृष्टि से देखने के अपने खतरे हैं. एक तो यह कि इससे किसी भी कृति में लगने वाली रचनात्मक ऊर्जा और मानसिक श्रम की भारी उपेक्षा होती है और दूसरी यह कि इससे कृति के वृहत्तर अर्थ को समझने की दृष्टि को ही बाधित कर दिया जाता है. हम फिर किसी खास चश्मे से एक कृति को पढ़ने लगते हैं और पूर्वाग्रहों के कारण रचना और रचनाकार दोनों ही का गलत आकलन करते हैं.
यह रचना जीवन के साधारण-से-साधारण क्षणों और अनुभवों को साधारण शब्दावली में अभिव्यक्त करते हुए भी, असाधारण लगती है. इसका कारण यह भी है कि साधारण शब्दावली में लिखे जाने से ही संभवतः यह मानवीय मन की सुंदर और सशक्त अभिव्यक्ति कर सकी है. इसीलिए इन शब्दों से गुज़रता हुआ पाठक कहीं भी भाषा के इंद्रजाल में फंसाये जाने का अनुभव नहीं करेगा. यह सहज-सरल भाषा आत्मीयता का एक ऐसा संबंध, पाठ और पाठक के बीच बना देती है कि यहां की हर एक वस्तु चिर-परिचित, हमेशा से जानी-पहचानी लगती है. इसीलिए लेखक ने जीवन की साधारणता-घटनाविहीनता में भी एक सौंदर्यबोध को देखा है, जो अभावों और मुफ़लिसी में और बहुगुणित होता है.
एक कस्बाई जीवन के विविध चित्र को समेटने पर भी यह रचना फणीश्वर नाथ रेणु के ‘मैला आंचल’ की तरह या श्रीलाल शुक्ल के ‘राग दरबारी’ की तरह इस जीवन के, इस निम्न-मध्य वर्ग के स्याह पक्षों को नहीं दिखलाता. यह एक बात संभवतः इस उपन्यास के संदर्भ में अटपटी लग सकती है कि यहां वर्णित पात्र किसी भी दृष्टि से बुरे नहीं हैं या नाम के लिए भी उनमें मानवोचित बुराइयां या दुर्गुण नहीं है. चाहे वह विभागाध्यक्ष हों, या हाथी लेकर आने वाला साधु, यह सब ही अच्छे व्यवहार का मुज़ाहिरा करते हैं. यहां तक की खिड़की के बाहर की जादुई दुनिया में रहने वाली बूढ़ी अम्मा भी बिना किसी लोभ के पति-पत्नी को चाय पिलाती है और आगे चलकर तो वह सोनसी को सोने के कड़े यूं ही दे देती है. इस पूरे वातावरण में हम कहीं भी मानवीय कमज़ोरियों को खुलते -खेलते नहीं देखते.
पर इसकी वजह संभवतः यह भी हो सकती है कि चूंकि यहां जीवन के सुखद क्षणों को और विस्तृत रूप देते हुए उसे एक फैंटसी से भरे खिड़की से बाहर की दुनिया में देखा गया है, तो इसीलिए इस सुखद फैंटसी में किसी भी प्रकार के दुखद अनुभवों या दोषयुक्त व्यक्तियों की मिलावट नहीं की गई है. स्वप्नों के कोमलतम संसार में जब चित्र ही जुटाने हैं तो एक लेखक की कल्पनाशक्ति जीवन के उज्ज्वल पक्षों से ही अपने कैनवास में रंग भरती नज़र आती है.
देखा जाए तो यह उपन्यास पाठकों से धैर्य मिश्रित कल्पनाशीलता की मांग करता है. यहां बहुत जरूरी हो जाता है कि हम लेखक की कल्पनाशीलता से रचे गए संसार में प्रवेश कर सकें और उसके कहने का अर्थ समझ सकें. तब ही शायद कथा कहने की शैली हमें रोचक और कई मायनों में नायाब लगेगी. तब ही हम अभावग्रस्त ज़िंदगी में भी मिलने वाले सुखों को स्वयं अनुभूत कर पाएंगे.
रघुवर प्रसाद और सोनसी उस औसत भारतीय निम्न मध्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जो कम-से-कम में भी जी सकने और अपना हृदय विशाल कर पाने का हौसला रखते हैं. वह परिचय और अपरिचय की सीमा को धुंधला कर देने की क्षमता रखते हैं और प्रकृति और मानवेतर जीवन के प्रति भी उतनी ही संवेदना रख सकते हैं जितना किसी स्वजन-संबंधी के लिए. ठीक है, इसे लिखने में विशेषकर स्त्री-पुरुष संबंधों के वृतांत रचने में जिस लेखकीय दृष्टि का प्रयोग हुआ है वह आज के अत्याधुनिक शहरी जीवन में अनोखा लग सकता है और नारीवादी दृष्टि से अगर इसका पाठ करें तो आलोचक, यह कह सकते हैं कि सोनसी की एक पत्नी के रूप में वर्णित भूमिका से अधिक उसके स्वतंत्र स्त्रीत्व और घर से बाहर उसे किसी भी प्रकार की एजेंसी देने के पक्ष में लेखक नहीं दिखते. पर यह सब पाठ, या कृति को उसके कस्बाई और वर्गीय परिवेश से छिन्न-भिन्न कर के देखने की तरह होगा.
एक गंवई-कस्बाई परिवेश में जीवन मूलभूत प्रश्नों के इर्द-गिर्द अधिक चलता है, जहां रोटी-कपड़ा-मकान अधिक अनिवार्य आवश्यकताएं हैं. स्त्री-पुरुष यहां अपने समाज परिभाषित भूमिकाओं में ही सहज नजर आते हैं और शुक्ल भी इस जीवन के चित्र खींचने में विशेष बौद्धिकता का आवरण नहीं ओढ़ते. यह जीवन के उज्ज्वल पक्षों का कोलाज है, और उस जीवन का समारोह मनाता है जो मामूली है, जो आधुनिकता के किन्हीं भी दबावों से अभी भी अछूता है.
(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में शोधार्थी हैं.)