कभी-कभार | अशोक वाजपेयी: हिंदी में ऐसा आलोचनात्मक माहौल बन गया है कि भाषा को महत्व देना या कि उसकी केंद्रीय भूमिका की पहचान करना, उस पहचान को ब्योरों में जाकर सहेजना-समेटना अनावश्यक उद्यम मान लिया गया है.
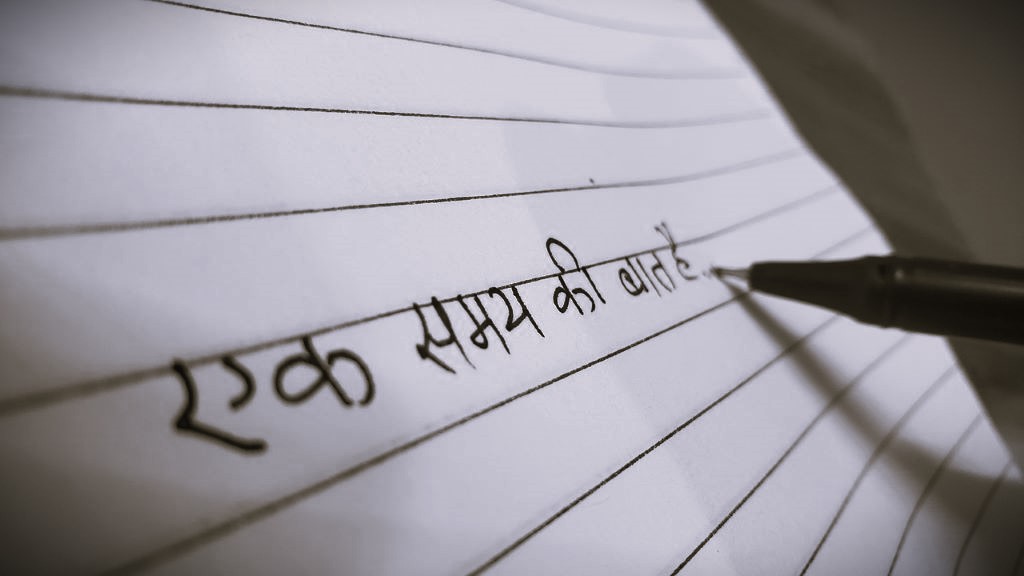
कृष्णा सोबती की जन्मशती का शुभारंभ 19-20 फरवरी 2024 को आयोजित एक लंबे परिसंवाद से हुआ है जिसका शीर्षक था ‘शब्दों के आलोक में’. 24 लेखकों ने बारी-बारी से उनकी विभिन्न कृतियों पर केंद्रित वक्तव्य दिए या निबंध प्रस्तुत किए. किसी बड़े लेखक की प्रायः सभी कृतियों पर एकाग्र यह एक अद्वितीय आयोजन सिद्ध हुआ. श्रोताओं में बड़ी संख्या में युवा छात्र शामिल थे जो कि बड़ी उत्साहजनक बात थी.
इस पर तो बरसों से आलोचनात्मक मतैक्य सा रहा है कि कृष्णा सोबती ने अपनी अनूठी कथा-भाषा विन्यस्त और विकसित की और परिसंवाद में इसका उल्लेख कई बार हुआ कि उन्होंने हिंदी-पंजाबी-उर्दू और बोलियों को मिला-जुलाकर यह कथाभाषा रची थी. लेकिन सारा विमर्श उनके चरित्रों, उस समय के समाज, विभाजन आदि के इर्दगिर्द ही रहा आया. उनकी भाषा पर गंभीर और विस्तृत विचार नहीं हो पाया. समस्या सिर्फ़ अलग-अलग जगहों से आए लेखकों की भर नहीं है- वह व्यापक रूप से हिंदी आलोचना की एक रूढ़ि जैसी है कि साहित्य की भाषा पर विचार बहुत कम होता आया है. यही नहीं कुछ इस तरह का भाव भी रूढ़ है कि भाषा पर विचार करना एक त्याज्य कलावादी हरकत है.
लेखक जो भी करता है, भाषा में ही करता है: जो भी चरित्र, कथानक, प्रसंग, घटनाएं, स्मृतियां, दृश्य, संवाद, अंतक्रियाएं आदि लिखी-रची जाती हैं वे सब भाषा में ही होती है.: उनके आशय, प्रामाणिकता, प्रासंगिकता आदि सब भाषा से ही उपजते हैं. कोई भी बड़ा लेखक बड़ा सिर्फ़ अपनी दृष्टि से नहीं होता: वह बड़ा होता है जब उस दृष्टि को भाषा में चरितार्थ करता है, कर पाता है. बड़ा वह इसलिए भी हो पाता है कि वह अपनी विशिष्ट भाषा अर्जित करता और उसमें एक बड़ा संसार रच पाता है.
लगता यह है कि हिंदी में ऐसा आलोचनात्मक माहौल बन गया है कि भाषा को महत्व देना या कि उसकी केंद्रीय भूमिका की पहचान करना, उस पहचान को ब्योरों में जाकर सहेजना-समेटना अनावश्यक उद्यम मान लिया गया है. इसका एक कारण तो शायद यह भी होता कि भाषा पर ध्यान देना चौकन्ना काम है और वह प्रचलित सामान्यीकरणों के सहारे नहीं किया जा सकता.
कई बार इस पर दुखद अचरज होता है कि अध्यापन और आलोचना दोनों में ही साहित्य की अपनी वैचारिकी विन्यस्त, विकसित करने और उसे निरंतर पुनर्नवा करने का आग्रह बहुत क्षीण है. हम पहले भी कह चुके हैं कि हिंदी में यह मानने में बहुत संकोच है कि साहित्य भी विचार की विधा है और वह हमेशा बाहर से, अन्य अनुशासनों से आए विचारों का उपनिवेश नहीं होता. अन्य अनुशासनों के लोग ऐसा न मानें पर दुर्भाग्य यह है कि स्वयं लेखक ऐसा नहीं मानते.
यह तब जब लेखकों को, सरसरी तौर पर विचारक या चिंतक कह देने का भी चलन है. मनुष्य की प्रकृति, नियति, संभावना, विडंबना आदि पर बड़ा लेखक अपने ढंग से विचार करता है. पर अकेला या निरा विचार साहित्य को सार्थक और मानवीय नहीं बनाता- इसका भाव-अनुभव, जीवन-प्रसंगों, स्मृतियों, संवेदना आदि से सम्गुम्फन प्रामाणिकता और प्रासंगिकता देता है.
गुलाम शेख़ का कारवां
हम जिस समय में रह रहे हैं उसमें इस एहसास से बचा नहीं जा सकता कि उसमें सारी तकनीकी संभावनाओं के बावजूद, दरअसल, अक्सर दरवाज़े बंद हो रहे हैं, खुलने या खुले रहने के बजाय. ऐसे दरवाजे बंद करते समय में कला का एक काम यह हो सकता है कि वह दरवाज़े खुले रखे और उन्हें बंद करने की कोशिश का, जो कई बार अभियान में बदलती रहती है, प्रतिरोध करे. ऐसा संभव है और संभावना को सचाई में बदला जा सकता है इसका एक बहुत उजला-सघन-विचारोत्तेजक उदाहरण गुलाम मोहम्मद शेख़ की प्रदर्शनी है जो वढ़ेरा गैलरी ने ‘कारवां’ शीर्षक से दिल्ली के बीकानेर हाउस में आयोजित की है.
दरवाज़ों के प्रति शेख का आकर्षण पुराना है. वे मानते हैं कि कला अपने सबसे रोमांचक और सर्जनात्मक मुक़ाम पर दरवाज़े खोलती है- वह खुद एक तरह का दरवाज़ा बन जाती है जिससे गुज़रकर हम सचाई और अनुभव के एक नए वितान या संयोजन में दाखि़ल हो पाते हैं. प्रदर्शनी के केंद्र में बाइस फ़ीट लंबा एक चित्र है जिसका शीर्षक है ‘कारवां’.
ऐसे सामाजिक समय में जिसमें स्मृति को अपदस्थ, विस्मृति को चढ़ाया-बढ़ाया जा रहा है और जिसमें सच्ची कृतज्ञता के बजाय झूठे गर्व की चकाचौंध मचाई जा रही है, इस विशाल कलाकृति में शेख़ याद करते, याद दिलाते हैं. कलाकृति में चित्रित विशाल नौका में (जो पहाड़ी मूर्धन्य नैनसुख के एक चित्र का एक तरह से पुनरवतरण करती है) भारत और संसार के अनेक संतों, विचारकों, कवियों के छोटे-छोटे व्यक्तिचित्र हैं. इस अद्भुत छबि-वीथी में बुद्ध, ईसा मसीह, महात्मा गांधी, कबीर, प्रेमचंद, रवींद्रनाथ, सुरेश जोशी आदि से लेकर बादेलेयर, रिल्के, लोर्का, वॉन गोग आदि शामिल हैं.
यह जैसे भवसागर पार करने की हम सबकी नौका है जिसमें हम अपना लगभग सब कुछ एक साथ ‘पैक’ कर रहे हैं. हम अकेले भवसागर पार नहीं कर सकते, न कर पाते हैं: हमारे जीवन में कितने दूसरों की शिरकत होती है इसे शेख़ कृतज्ञतापूर्वक याद करते लगते हैं. ऐसा लगता है कि जैसे भवसागर पार करने में पूरा भव ही नौका में बैठा हुआ है- जैसे भव को पार पूरा भव ही करता है, कोई और या अकेला नहीं.
इस कृति में विशाल और नन्हें सब एकमेल हैं: दोनों को साध पाने की निराली कलादृष्टि और बिरला कलाकौशल शेख़ के पास है. कम से कम मैं इस कलाकृति को हमारी अनिवार्य-अदम्य-अनश्वर बहुलता के आलेख के रूप में भी पढ़ता हूं. भव जीवन की अपार बहुलता की जगह है, उत्सव है.
कांवड़ शेख ही कलासंपदा में लाए हैं: यह राजस्थान के कुछ इलाकों में कथाकथन के लिए इस्तेमाल होती है और उसमें देवी-देवताओं की छबियां अंकित रहती हैं और उन्हें लटकाकर कलाकार उसकी कथाएं सुनाते और कांवड़ खोलकर उनकी छबियां दिखाते रहे हैं. शेख ने कांवड़ का पुनराविष्कार करते हुए उनमें बंद कई दरवाज़े खोलने की युक्ति का कल्पनाशील उपयोग करते हुए उनमें नई कथाएं कही हैं. जैसे, इस प्रदर्शनी में एक कांवड़ में गांधी-जीवन के कुछ प्रसंग चित्रित हैं. दरवाज़े खोलने और सब कुछ को फिर ‘पैक’ कर बंद कर देना दोनों की क्रियाएं कांवड़ में बखूबी घटती हैं: उसमें मानों रहस्य और विस्मय गलबहियां डाले साथ हैं.
दशकों पहले आधुनिक भारतीय कला में आख्यानमूलक वृत्ति उभरी थी, उसके गुलाम शेख़ मूर्धन्य चित्रकार रहे हैं. वे अपने चित्रों में नए-नए आख्यान रचते रहे हैं. एक तरह से वे हमारे समय और समाज के गाथाकार हैं. कभी अभिधा से, कभी व्यंजना से वे समकालीन हिंसा और अत्याचार की कथा कहते रहे हैं. पर जीवन की अपारता, बहुलता और अदम्यता का बोध उनकी कृतियों में हर हालत में सक्रिय रहता है.
अपने समय के जटिल और इन दिनों अक्सर लहूलुहान सच की शिनाख़्त हम शेख़ जैसे कलाकार की कृतियों से कर आश्वस्त होते हैं कि कला में मानवीय की शिनाख़्त दर्ज़ है. संयोगवश, मीर का एक शेर याद आया:
आलम के साथ जाएं चले किस तरह न हम
आलम तो कारवान है हम कारवानियां
कुमार शहाणी
कुमार शहाणी का कोलकाता में देहावसान एक मूर्धन्य फिल्मकार, बुद्धिजीवी, कलाप्रेमी और मित्र का अवसान है. देखने में सुकुमार लगते, कुमार में अपने माध्यम, दृष्टि और कलाओं में बड़ी सुदृढ़ और अविचल निष्ठा थी. उन्होंने अपने आठ दशकों से थोड़े अधिक जीवनकाल में विचारधाराओं के अपने उरूज पर पहुंचने के बाद उनका पराभव देखा था. उन्होंने विचार को सत्तारूढ़ होते, संकीर्ण और क्रूर होते, अपनी अप्रासंगिकता से बेख़बर होते देखा था.
पर वे एक महान् विचार की इस दुर्गति और अधःपतन को उसकी अनिवार्य परिणति नहीं मानते थे और उसकी अब भी शेष संभावना और पुनराविष्कार में विश्वास करते थे. भारत और, दुर्भाग्य से, सारे संसार में बढ़ती नवपूंजीवादी, बाज़ारू, मीडिया पोषित, धार्मिक तानाशाहियों से वे हमेशा चिंतित और विचलित रहते थे. फिर भी, उनका भरोसा था कि इस बढ़ती सांसारिक बर्बरता का प्रतिरोध वैकल्पिक यथार्थ रचकर कलाएं किसी हद तक, कर सकती हैं.
वे उन फिल्मकारों में अग्रणी थे जिन्होंने भारत में सिनेमा को मानवीय स्थिति, नियति और विडंबना पर विचार और संवेदना की विधा बनाया.
सिनेमा की, भारतीय सिनेमा की चकाचौंध, खर्चीली, अपराध-लिप्त दुनिया में कुमार अपने मित्र और सहकर्मी मणि कौल के साथ, एक तरह से, विरागी थे जिन्होंने, कला की अपनी शर्तों पर ज़िद कर अड़े रहकर, लोकप्रियता के प्रलोभन से अपने को दूर रखा. वे उन भारतीय फिल्मकारों में से थे, जिनकी फिल्मों के अनेक समारोह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संसार भर में हुए लेकिन स्वयं भारत में उनकी ज़्यादातर फिल्में लगभग अनदेखी रहीं.
सिनेमा में बिंब-रचना, छबि-संप्रेषण, अंतर्ध्वनियों, रूपक और व्यंजना आदि की असाधारण समझ और क्षमता रखनेवाले कुमार, अपवाद बनकर, हाशिये पर रहे. ऐसे हाशिये पर जो केंद्र की तानाशाही से अपने को मुक्त रखता रहा.
लगभग चालीस बरस पहले एक बार मुम्बई की जहांगीर आर्ट गैलरी में अकस्मात् कुमार से भेंट हो गई. मुझे तब तक यह पता नहीं था कि उन्होंने ख़याल गायकी की बाक़ायदा तालीम ली थी. हम वहां सीढ़ियों पर बैठकर काफ़ी देर गपियाते रहे. वे ध्रुपद के बाद ख़याल के उद्भव और विकास पर फिल्म बनाना चाहते थे. मणि कौल तब तक ‘सतह से उठता आदमी’ हमारे लिए बना चुके थे जो भले बाद में वह क्लासिक मानी गई पर तब हिंदी के वाम खेमे में बहुनिंदित थी. मैंने फिर एक जोखिम उठाने का तय किया और अनेक अड़चनों-अडंगों के बाद कुमार ने ‘ख़याल गाथा’ हमारे लिए बनाई.
नित-नई टेक्नोलॉजी के हमारे मानस, संवेदना, भावसंसार पर प्रभाव को समझने-आंकने को लेकर कुमार बहुत चौकन्ने थे और, उचित ही, उनको यह तीख़ा एहसास था कि सारा संसार नए क़िस्म की तानाशाही की गिरफ्त में है और उसका सजग-सशक्त प्रतिरोध आवश्यक है. वे कुछ दिनों से, अपने जीवन के अंतिम चरण में, इस पर, किसी न किसी तरह से, इसरार करते रहते थे. उनका देहावसान एक प्रतिरोधी, सावधान करने वाली बेचैन आवाज़ का ख़ामोश हो जाना है.
(लेखक वरिष्ठ साहित्यकार हैं.)




