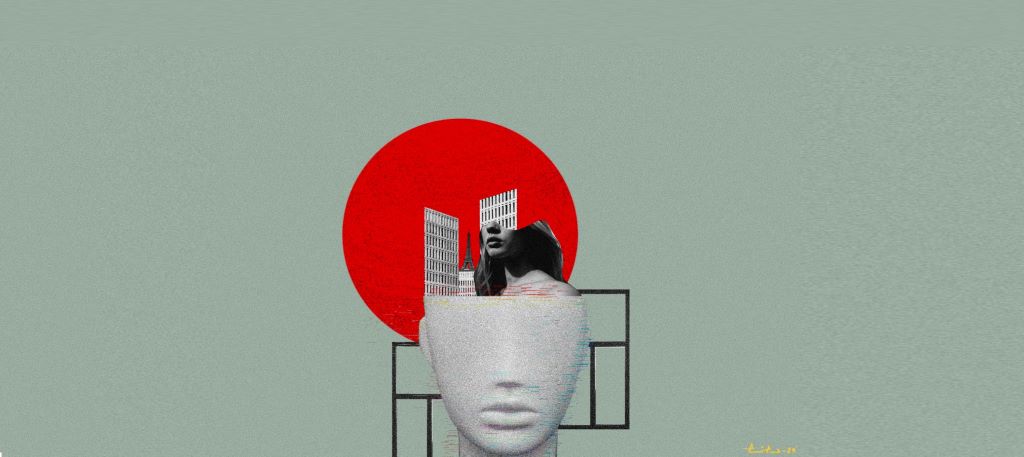रज़ा फाउंडेशन और कृष्णा सोबती-शिवनाथ निधि द्वारा आयोजित वार्षिक ‘युवा-24’ इस बार नौ कवियों पर केंद्रित था. उसमें देश के 36 शहरों से आए 47 युवा हिंदी लेखकों ने भाग लिया. उनमें से कइयों ने यह स्वीकार किया कि अगर इस आयोजन में भाग लेने के लिए इन नौ कवियों में से किसी एक कवि को पढ़ने और उस पर लिखने-बोलने का आग्रह न होता तो वे उस कवि को शायद कभी पढ़ते ही नहीं. उनमें से कुछ को शिकायत थी कि उन्हें संबंधित कवि की लिखी पर्याप्त सामग्री नहीं मिल सकी. उन पर हिंदी में जो लिखा गया है वह भी उनकी नज़र से नहीं गुज़र पाया.
दिलचस्प है कि ऐसे युवाओं ने इंटरनेट से अलग सामग्री खोजने-पाने की कोई कोशिश नहीं की. ऐसी हालत तेज़ी से बन रही है कि जो इंटरनेट पर नहीं है, लेखक भी मानने लगेंगे कि वह है ही नहीं है या कि उसका पुस्तकों में या पत्रिकाओं में होना उनके उद्यम के योग्य नहीं ठहरता. यह तब जब कि इनमें से कई कवियों की रचनावलियां या समग्र प्रकाशित हैं. ज़ाहिर है कि साहित्य में विस्मृति का वितान फैल रहा है.
हिंदी में पिछले लगभग पचास वर्षों से साहित्य को राजनीतिक-सामाजिक संदर्भों में पढ़ने-समझने की प्रथा लगभग रूढ़ हो गई है. ये संदर्भ साहित्य को समझने में सहायक होते हैं पर साहित्य को उन्हीं तक महदूद करना साहित्य की समग्रता से दूर जाना है. कोई भी कवि अपने समय-समाज से प्रभावित होता है पर वह सिर्फ़ इन दबावों में या उनके कारण नहीं लिखता. न सिर्फ़ लिखना एक निजी निर्णय है, किसी की कविता महत्वपूर्ण ही तब हो पाती है जब उसमें प्रतिभा-दृष्टि-भाषा-शिल्प की अद्वितीयता चरितार्थ या प्रगट होती है. इस ज़रूरी कुछ को, इस सबको नज़रंदाज़ या कमतर मानते हुए, राजनीतिक-सामाजिक संदर्भ और उनके प्रति रुख़ में घटा देना ईमानदार, सतर्क और जटिल बौद्धिक कर्म से विरत होना है. यह खेद का विषय है कि युवा लेखकों का एक बड़ा हिस्सा सामाजिकी की इस दकियानूसी की चपेट में है. उसका दुखद साक्ष्य इस बार फिर मिला.
बहुत युवा ध्यान से, संवेदना और तैयारी से दूसरों को नहीं पढ़ते और उन्हें सर्जनात्मक और बौद्धिक लापरवाही से सामाजिकी के किसी खाने में रखकर संतुष्ट हो जाते हैं. इन्हीं में से कई इस समय भारतीय समाज में जो राजनीतिक सर्वग्रसिता, झूठ, घृणा, हिंसा का बोलबाला है उसके संदर्भ में न स्वयं लिखते हैं, न ही अपने समवयसियों को उसकी रौशनी में आंकते हैं. यह एक क़िस्म की चतुर कायरता है.
इसलिए अगर ज़्यादातर कवियों की भाषा, शिल्प, दृष्टि की जटिलता पर कोई बात नहीं हो पाई तो यह लगभग प्रत्याशित ही था. सामाजिकी से आक्रांत होते हुए भी, बहुत कम ने विचाराधीन कविता को वर्तमान सामाजिक संकट से जोड़ने-समझने की कोशिश की. स्वयं हिंदी भाषा का जो रोज़ाना विदूषण हो रहा है उसके प्रति कोई सजगता का साक्ष्य नहीं मिला.
फिर भी, बीच-बीच में कम से कम एक तिहाई युवाओं ने कवियों को नए ढंग से पढ़ने के उत्साह और उद्यम का कुछ रोचक प्रमाण दिया. आलोचना की भाषा में, दुर्भाग्य से, अनेक ऐसी मान्यताएं और अभिव्यक्तियां प्रचलित हैं जो या तो अपना अर्थ खो चुकी है या जो नए सिरे से जांचे जाने की मांग करती हैं. प्रचलित की सीमाओं से आगे जाकर कुछ नया खोजने-करने की इच्छा कम है पर सौभाग्य से है. यह जोखिम का काम है. पर अगर युवा लेखक जोखिम नहीं उठाएंगे तो फिर किससे उम्मीद की जाए?
संगीत और जाति
इन दिनों कर्नाटक संगीत में उसके एक श्रेष्ठ गायक को मद्रास अकादमी द्वारा अपना सर्वोच्च और सुप्रतिष्ठित सम्मान दिए जाने का एक भीषण विवाद छिड़ गया है. टीएम कृष्णा श्रेष्ठ गायक और संगीत-चिंतक और बुद्धिजीवी हैं. उनकी संगीत-श्रेष्ठता को लेकर कोई विवाद नहीं है. विवाद इस मुद्दे को लेकर है कि कृष्णा ने कर्नाटक संगीत और उस पर कथित उच्च जाति के लोगों के एकाधिकार को लेकर प्रश्न खड़े किए हैं: उसकी शुद्धतापरक रूढ़ि पर प्रहार किया है और अपने गायन में ऐसी अनेक कृतियों को शामिल किया है जो दलित, ईसाई या अल्पसंख्यक संगीतकारों ने रची हैं और जो अब तक प्रचलित और वर्चस्वशाली संगीत-संपदा से बाहर रखी-रही आई हैं.
कृष्णा स्वयं ब्राह्मण हैं और उन्होंने कर्नाटक शैली के श्रेष्ठ कृतिकारों त्यागराज आदि सभी की कृतियां श्रेष्ठ ढंग से प्रस्तुत की हैं. इसने कर्नाटक शैली की सवर्ण व्यवस्था को क्षुब्ध और विचलित किया है. कई ब्राह्मण संगीतकारों ने मद्रास अकादमी का बहिष्कार करने की घोषणा की है. जहां तक हमें पता है कि इन आपत्तिकर्ताओं ने कृष्णा के संगीत की गुणवत्ता पर कोई प्रश्न नहीं उठाया है. उनकी यह पुरस्कार पाने की अपने संगीत के आधार पर पात्रता नहीं है ऐसा किसी ने दावा भी नहीं किया है. आपत्ति कृष्णा की वैचारिक दृष्टि और हस्तक्षेप को लेकर है जिसमें संगीत में समावेशिता के अभाव का एहतराम उसके लोकतांत्रिक विस्तार की ज़रूरत और संभावना का प्रयत्न शामिल है.
अकादमी का बहिष्कार करने वाले सभी संगीतकार उच्च वर्ण के हैं और ज़ाहिर है कि वे अपने वर्चस्व को कृष्णा द्वारा व्यवहार और विचार दोनों में दी जा रही चुनौती से अस्थिर होता देख रहे हैं. इसी कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में दशकों पहले पेरियार ने धर्म और जाति से मुक्त द्रविड़ता का प्रतिपादन किया था जो एक सामाजिक क्रांति थी. कृष्णा का पेरियार का समर्थन करना भी उच्चभ्रू संगीतकारों को स्वीकार्य नहीं.
उन्हें बहिष्कार करने का लोकतांत्रिक हक़ तो हैं पर वे उसका उपयोग जिस कारण कर रहे हैं वह स्वयं संगीत के लोकतंत्र को अपमानित करने जैसा है. दुर्भाग्य से उनके इस क़दम ने यह भी जगज़ाहिर कर दिया है कि कर्नाटक संगीत में जातिप्रथा कितनी गहरे धंसी हुई है और श्रेष्ठ कलाकार तक उसे बचाए रखना और पोसना चाहते हैं. अक्सर ऐसे अवसरों पर प्रतिष्ठान व्यवस्था के पक्ष में खड़े दिखते हैं. पर इस बार मद्रास अकादमी कृष्णा के साथ खड़ी है यह एक शुभ लक्षण है.
हो सकता है
हो सकता है कि लोग अब झूठों-झांसों-झगड़ों से तंग आ गए हों. हो सकता है धर्म और जाति के नाम पर हो रही हिंसा, निरपराध व्यक्तियों की हत्या, अबलाओं के बलात्कार आदि से उनकी वितृष्णा और नाराज़गी बढ़ने लगी हों. हो सकता है कि लाभार्थियों को यह समझ में आ गया हो कि जो उन्हें मिला है कोई लाभ नहीं उनका सहज अधिकार है, जिसके बदले में उन्हें कुछ नहीं देना है. हो सकता है कि उन्हें दिखाई देने लगा हो कि शिखर से, आत्मविश्वास और नाटकीय भंगिमाओं से बोला गया झूठ झूठ ही है और उसे सच मानने की भूल अब वे नहीं करेंगे.
हो सकता है कि हिंदीभाषियों को अब इस पर रोष होने लगे कि उनकी भाषा को घृणा-हिंसा-झूठ-हत्या-बलात्कार की भाषा बनाकर उसकी मानवीयता नष्ट की जा रही है. हो सकता है कि लोग देख पा रहे हों कि हमारे समय में घूस को क़ानूनी जामा पहनाकर और सर्वथा गोपनीय बनाकर भयानक भ्रष्टाचार किया गया है. हो सकता है कि लोगों को याद आए कि कोविड महामारी के दौरान एक करोड़ से अधिक लोग सत्ताओं द्वारा समुचित वाहन उपलब्ध न कराने या उन्हें बेहद खर्चीला बना देने के कारण सैकड़ों मील, भरी गरमी में पैदल घर-गांव लौटने पर विवश हुए थे.
हो सकता है यह एहसास व्यापक हो कि जुमलों और गारंटियों की घोषणाएं अब तक रोज़गार और नौकरियों में परिणत नहीं हुई हैं. हो सकता है कि युवा यह सोचने पर विवश हों कि जो आर्थिक व्यवस्था विकसित की और पोसी जा रही है वह पूंजी का सबमें न्यायसंगत बंटवारा करने से बहुत दूर उसे कुछ लोगों में केंद्रित करती रहेगी. हो सकता है कि युवाओं को यह समझ में आए कि समता और न्याय का सपना सपना ही रहेगा अगर वे आगे बढ़कर अपने हक़ों पर इसरार न करें.
संविधान की व्यवहार और सोच में हर दिन अवज्ञा के समय में हो सकता है कि लोग देख पाएं कि अगर यह होता रहे ओर स्वयं संवैधानिक संस्थाएं निस्तेज और निष्क्रिय होती जाएं तो, संविधान को बचाने की ज़िम्मेदारी किसी और की नहीं, उनकी है. हो सकता है कि स्त्रियों को यह समझ में आए कि उनकी शक्ति के कीर्तन के बावजूद भारत में सबसे अधिक जघन्य अपराध उनके विरुद्ध होते हैं और सत्ताएं और अवसरवादी राजनीति उनमें लिप्त हैं.
हो सकता है कि हिंदुओं को यह पता चल जाए कि हिंदुत्व का हिंदू धर्म के मूल तत्वों और अध्यात्म से कोई संबंध नहीं है और वह एक संकीर्ण घृणा-उपजाऊ राजनीतिक विचारधारा है. हो सकता है कि न्यायालयों को यह सद्बुद्धि आ जाए कि सत्ता के इशारों पर या उसके दबाव में आकर वे उसकी अन्यायपूर्ण व्यवस्था को पुष्ट और सशक्त कर रहे हैं और नागरिकों का उन पर से विश्वास उठ गया है.
हो सकता है कि गोदी मीडिया को यह विचार कि उसने सत्ता की पालतू और अन्धभक्ति ने साधन-संपन्न भले कर दिया हो, उसके पास कोई नैतिक बल नहीं बचा कुछ सताने लगे. हो सकता है कि शिक्षकों को यह सीधा-सच्चा ज्ञान अंततः मिल ही जाए कि सत्ता-व्यवस्था ज्ञान को अवमूल्यित करने, अज्ञान को महिमामंडित करने और उनकी स्वायत्तता-स्वतंत्रता हरने-हड़पने में व्यस्त है.
हो सकता है कि इनमें से कुछ भी न हो और यह सूची एक लेखक की कपोल-कल्पना भर हो. हो सकता है…
(लेखक वरिष्ठ साहित्यकार हैं.)