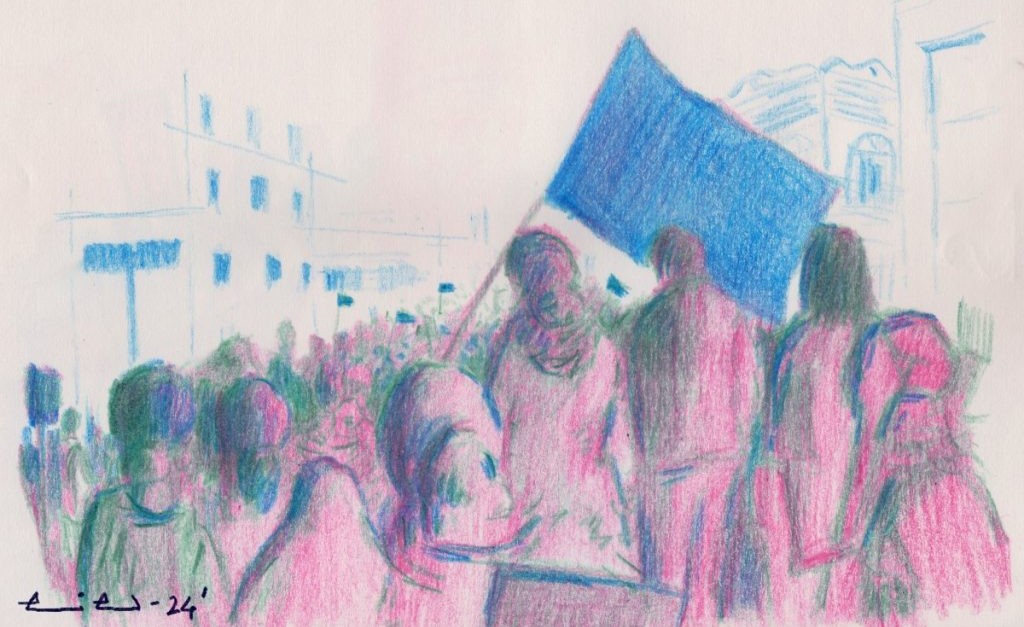‘एनोला होम्स’ नामक फिल्म सीरीज़ में जब एडिथ शेरलॉक से पूछती हैं कि राजनीति तुम्हें क्यों नहीं भाती, शेरलॉक कहते हैं कि क्योंकि वह घातक तरीक़े से उबाऊ होती है. एडिथ जवाब देती हैं कि असल बात यह है कि तुम उस दुनिया को बदलना ही नहीं चाहते जो तुम्हारे लिए उपयुक्त है.
कुछ दिन पहले ग्रेटर नोएडा की गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कुछ छात्र-छात्राएं कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे और नारे लगाने लगे. उन नारों से उनका कोई साबक़ा नहीं था. जब उनसे पूछा गया, वे अर्बन नक्सल को अर्बन ‘मैक्सवेल’ बोलने लगे. हिंदी और अंग्रेज़ी के बेहद सरल वाक्यों की तख्ती जो उन्होंने हाथ में ले रखी थी, वे उसे भी नहीं पढ़ पा रहे थे. मालूम चला कि उन्हें अटेंडेंस दिलाने के बहाने यहां लाया गया था, और वे कांग्रेस द्वारा दिए विरासत कर (Inheritance Tax) के प्रस्ताव पर अनजाने में अपना विरोध दर्ज कर रहे थे.
यही छात्र चुनाव में उस पार्टी को वोट दे आएंगे जिसके पोस्टर्स उन्हें सबसे ज़्यादा दिखेंगे. उन्हें विचारधारा और सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों से बहुत लेना-देना नहीं है. वे आसानी से बरगलाए जा सकते हैं, जा रहे हैं. ऐसे हालात महज़ गलगोटिया यूनिवर्सिटी के छात्रों के ही नहीं है. तमाम सरकारी विश्वविद्यालयों का भी गलगोटियाकरण हो रहा है. इस प्रक्रिया में विश्वविद्यालय प्रशासन, छात्रसंघ और गलगोटियातुर छात्रों की भूमिका अहम है.
एक वक्त बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू), दिल्ली, इलाहाबाद और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्रसंघ अध्यक्ष को किसी सांसद या विधायक जैसा सम्मान मिलता था. बीएचयू के छात्रसंघ अध्यक्ष को ‘प्रधानमंत्री मैटेरियल’ माना जाता था. लेकिन आज जब वैचारिक छात्र राजनीति की सबसे अधिक ज़रूरत दिखाई पड़ती है, हमें कुछ नज़र नहीं आता. देवव्रत मजूमदार अब किसी पिछले युग के छात्रनेता लगते हैं. मजूमदार ने बीएचयू का छात्रसंघ अध्यक्ष रहते हुए अंग्रेज़ी हटाओ आंदोलन की अगुवाई की थी. 70 के दशक में बनारस के छात्र नेताओं के प्रिय ‘देबू दा’ कई जेल यात्राओं और आंदोलनों की वजह से बनारस की छात्र राजनीति के प्रतीक बन गए थे.
जेएनयू के छात्रसंघ चुनाव के सिवाय उत्तर भारत के प्रमुख विश्वविद्यालयों में केवल धनबल और बाहुबल की राजनीति चलती है. दिल्ली विश्वविद्यालय के हालिया छात्रसंघ पदाधिकारियों के पास महंगी गाड़ियों, अकूत धन और रंगबिरंगे पैम्फलेट के सिवा कुछ नहीं है. वैचारिकी के नाम पर कोरे हैं.
दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र ‘एनोला होम्स’ के शेरलॉक हैं. समाजशास्त्री दीपांकर गुप्ता ने एक शब्द गढ़ा है- वेस्टॉक्सिकेटेड एलीट. वह अभिजात वर्ग जो पश्चिम से प्रभावित हो, लेकिन दीपांकर का तर्क है कि यह अभिजात वर्ग पश्चिम की अच्छाइयों- मसलन बराबरी, स्वतंत्रता, न्याय- जो उसका सामाजिक और राजनीतिक तौर पर सबसे बड़ा और ज़रूरी हस्तक्षेप है, उससे नहीं बल्कि उनके ऊपरी उपक्रमों जैसे महंगे कपड़े, महंगा खाना, महंगी गाड़ियां और महंगे रहन-सहन से प्रभावित है. भारतीय मध्यवर्ग इस फंसान का सबसे बड़ा गवाह है. ग्राम्शी का हेजेमनी (आधिपत्य) का तसव्वुर यहां प्रासंगिक हो जाता है.
दिल्ली विश्वविद्यालय में मुख्यतः दो छात्र संगठन हैं― अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) और नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई). पहला भाजपा व दूसरा कांग्रेस का. अभाविप के पोस्टरों से लगता है कि वे स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा लेते हैं. दिलचस्प है कि वे आंबेडकर और भगत सिंह को भी अपने पोस्टरों में शामिल करते हैं. इससे पहले उन्हें आंबेडकर और भगत सिंह के वैचारिक रुख को समझना चाहिए.
भगत सिंह लेनिन से प्रेरित थे. वैसे अभाविप के कार्यकर्ताओं ने विवेकानंद और सावरकर को भी नहीं पढ़ा है. और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के पास भी गांधी, नेहरू, पटेल, या मौलाना आज़ाद को लेकर ज़रूरी और मूल समझ नहीं है. ये छात्रसंघ अपने वैचारिक पुरखों पर पांच मिनट ढंग से नहीं बोल पाते.
पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर व वीपी सिंह, सीताराम येचुरी, प्रकाश करात, अरुण जेटली जैसे तमाम नेता इन्हीं विश्वविद्यालयों की छात्र राजनीति से निकले हैं. वर्तमान छात्र राजनीति की इस वैचारिक हत्या के जितने कुसूरवार ये छात्र हैं, उतनी कुसूरवार वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था है. बीएचयू और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रसंघ को समाप्त कर स्टूडेंट काउंसिल बनाई गई, और फिर उसे भी ख़त्म कर दिया गया. जाहिर है, विद्यार्थी की आवाज़ से सत्ता को दिक्कत है.
यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया के ज़रिये हुआ है. इसमें विश्वविद्यालय व संलग्न कॉलेज प्रशासन, कई प्रोफेसर्स और नई भर्तियां अहम किरदार निभा रही हैं. मुकुल केसवन अपने एक लेख में कहते हैं कि इन विश्वविद्यालयों में दाखिले की परीक्षाओं का मॉडल गड़बड़ है.
उनका तर्क है कि आईआईटी-जेईई का बहुविकल्पीय प्रश्नों का मॉडल ही अब हर परीक्षा का मॉडल बन गया है. जबकि सामाजिक विज्ञान में सही उत्तर चुनकर निशान लगाना आपकी काबिलियत साबित कर दे, ऐसा नहीं है. सामाजिक विज्ञान की असल मांग और चाह आपको अधिक अकादमिक और बहुपठित बनाने की होनी चाहिए. जहां आप किसी विषय पर किस क़दर सोच और लिख सकते हैं, आप कितने तार्किक हैं, इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए.
विश्वविद्यालय कैंपस जातिवाद, धार्मिकता और संप्रदायवाद का भी चलता-फिरता उदाहरण है, जहां ऊंची और ताकतवर जातियों से आए छात्रों का भौंडा जातीय प्रदर्शन आम है. इन वजहों से दिल्ली विश्वविद्यालय अकादमिक और राजनीतिक रूप से काफ़ी पीछे जा चुका है. ज़रूरत है कि छात्रों में और छात्र राजनीति में वह मूल्य कायम हों, जिनसे सीखकर छात्र सवाल पूछ सकें और सवाल पूछे जाने पर जवाब दे सकें. सरकारी विश्वविद्यालयी शिक्षा को ‘गलगोटियाइज़’ होने से बचाया जाए.
हमें आज़ादी के आंदोलन से सीख लेनी चाहिए. जब भगत सिंह छात्रों को पॉलिटिक्स की किताबें पढ़ने पर ज़ोर डाल रहे थे, उसकी कोई वजह तो ज़रूर होगी. और जवाहरलाल नेहरू 1947 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाकर विद्यार्थियों से कह रहे थे:
‘एक विश्वविद्यालय मानवतावाद, सहिष्णुता, तर्क, प्रगति, विचारों की साहसिकता और सत्य की खोज का प्रतीक है. यह मानव जाति के और भी ऊंचे उद्देश्यों की ओर आगे बढ़ने का प्रतीक है. यदि विश्वविद्यालय अपना कर्तव्य पर्याप्त रूप से निभाते हैं, तो यह राष्ट्र व लोगों के लिए अच्छा है. लेकिन अगर शिक्षा का मंदिर ही संकीर्ण कट्टरता और क्षुद्र उद्देश्यों का घर बन जाए, तो राष्ट्र कैसे समृद्ध होगा या लोगों का कद कैसे बढ़ेगा?’
(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हैं.)