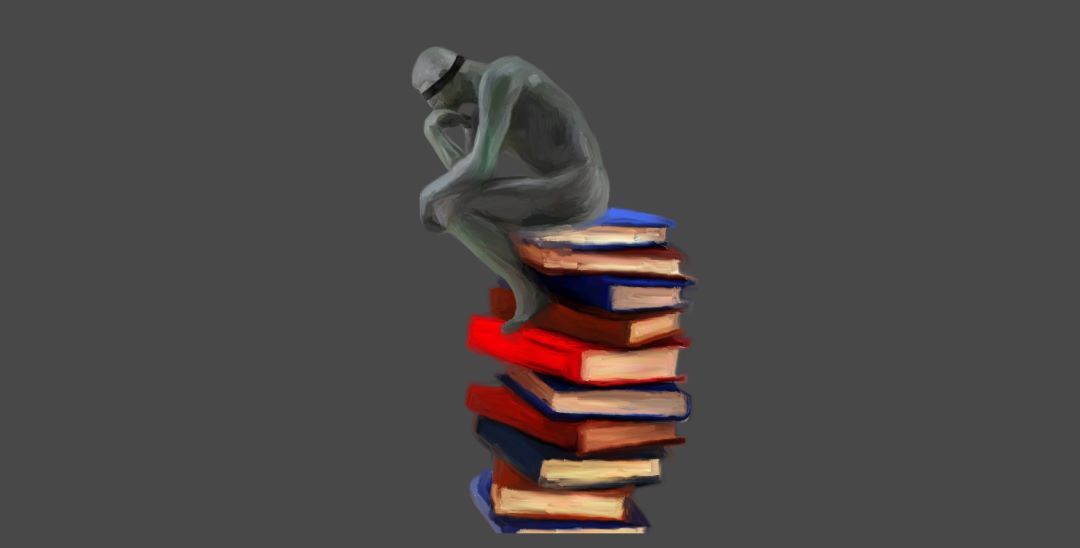यही मेरे लोग हैं
यही मेरा देश है
इसी में रहता हूं
इन्हीं से कहता हूं
अपने आप और बेकार.
लोग लोग लोग चारों तरफ़ हैं मार तमाम लोग
खुश और असहाय
उनके बीच में सहता हूं
उनका दुख
अपने आप और बेकार.
देश की व्यवस्था का विराट वैभव
व्याप्त है चारों ओर
एक कोने में दुबक ही तो सकता हूं
सब लोग जो कुछ रचाते हैं उसमें
केवल अपना मत नहीं दे ही तो सकता हूं
वह मैं करता हूं
किसी से नहीं डरता हूं
अपने आप और बेकार .
‘अपने आप और बेकार’ शीर्षक यह कविता रघुवीर सहाय ने बीसवीं सदी के 60 के दशक में लिखी थी. तब तक भारत में जनतांत्रिक प्रक्रियाएं जड़ जमा चुकी थीं. लोग चुनावों के अभ्यस्त हो चले थे जो हर कुछ वक़्फ़े पर आते ही थे. संसद और विधानसभाएं बैठा करती थीं. यह सब कुछ लोगों के नाम पर था. लोग जो जनतंत्र में सर्वोपरि हैं. आख़िर ‘हम भारत के लोगों’ ने ही भारत को एक जनतांत्रिक गणराज्य के रूप में गठित किया था.
लोगों की प्रभुसत्ता के मंगलाचरण के बाद ही उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि अपनी सत्ता स्थापित कर सकते थे. धर्म ने नर में नारायण देखा, जनतंत्र ने जनता को जनार्दन का दर्जा दिया. जनता ही जनतंत्र में सारी शक्ति का स्रोत है, उसी में सारी बुद्धि, सारे विवेक का निवास है. जनतंत्र में जनादेश से चलता है. यह जन या जनता ही सब कुछ चलाती है. वह प्रश्नातीत है. उसके फ़ैसले पर उंगली नहीं उठाई जा सकती.
जॉन कीन ने जनतंत्र के सबसे संक्षिप्त इतिहास वाली किताब में अमेरिकी रिपब्लिकन जॉन एडम्स को उद्धृत किया है जिनके मुताबिक़ जनता या लोगों की महिमा अपरंपार है, वे जानते हैं कि क्या सही है और क्या ग़लत, वे जो निर्णय लें उसे सिर माथे लेना ही जनतांत्रिक कर्तव्य है.
जनता निर्णय सिर्फ़ एक बार लेती है. इस बीच उसके नाम पर निर्णय वे लेते हैं जो कहते हैं कि उनके पास जनादेश है. एक तरह से जनता परे धकेल दी जाती है. जनादेश से चुनी सरकारों या उसके प्रतिनिधियों से जब कोई सवाल करता है, तो वे इस जनता या लोगों के नाम पर ही सवाल करने वालों पर हमला करते हैं. सवाल करने वाले जनद्रोही ठहरा दिए जाते हैं. जनता को बहुमत में शेष कर दिया जाता है.
जब जनता ने हमें 5 साल के लिए चुना है तो इस बीच आप कौन होते हैं इस बीच सवाल करके जनता के विवेक पर संदेह करनेवाले? यह प्रश्न सवाल को ही नाजायज़ बना देता है.
कवि को जनता की इस प्रभुता का पता है. वह उसी के बीच रहता है. और उसे जनता ने नहीं चुना है. इस जनता को उसका पता भी है, इसे लेकर संदेह है. कवि और जनता का यह रिश्ता कैसा है?
यही मेरे लोग हैं
यही मेरा देश है
इसी में रहता हूं
इन्हीं से कहता हूं
अपने आप और बेकार.
कवि की असहायता. कवि की निरुपायता. अपनी व्यर्थता का एहसास. क्या यह अपने लोगों और अपने देश में रहने की बाध्यता है: ‘यही मेरे लोग हैं/ यही मेरा देश है’. इसे छोड़कर मैं कहां जाऊं? या इसे छोड़कर मैं जा नहीं सकता?
मेरे लोग, मेरा देश जो इन लोगों से मिलकर बनता है, मेरी नियति है. इनसे ही मैं बात कर सकता हूं. आख़िर मैं इन्हीं की ज़बान बोलता हूं. लेकिन मुझे पता है कि मेरा बोलना बेकार है.
फिर भी मैं बोलता हूं. और वह इसलिए कि मैं उनका दुख सह रहा हूं जिसका एहसास शायद उन्हें ख़ुद नहीं:
लोग लोग लोग चारों तरफ़ हैं मार तमाम लोग
खुश और असहाय
उनके बीच में सहता हूं
उनका दुख
अपने आप और बेकार.
ये कौन हैं जो ख़ुश हैं और असहाय हैं? ये लोग लोग हैं या भीड़? ‘भीड़ में मैकू और मैं’ कविता में ये लोग भीड़ हैं जिनके बीच कवि मैकू को खोज रहा है. और अगर मैकू न मिले तो रामलाल ही मिल जाए! मिलती है लेकिन भीड़:
भीड़ में मैलखोरी गंध मिली
भीड़ में आदिम मूर्खता की गंध मिली
भीड़ में नहीं मिली मेरी गंध
जब मैंने उसे सांस भर सूंघा
भीड़ में खोता है व्यक्ति. भीड़ में अपनी गंध नहीं मिलती. लोग ख़ुद को भीड़ में बदलते हैं. झुंझलाहट कवि की अपने लोगों से है:
अलग-अलग खाना पकाती इस जाति ने
क्या किया जात पूछने के बाद प्यास का
प्यास का क्या किया? इस सवाल का जवाब जनतंत्र कैसे देता है? जात से परे जनता. या जात के साथ जनता? और वह प्यास का क्या करती है? वह तो उसका कुछ तभी कर सकती है जब उसके पास चेतना हो. वह क्या अपने आप बदलती है? क्या किसी क्रांति की प्रतीक्षा करनी है जो यह करेगी? मैकू की खोजवाली कविता में एक कार्यकर्ता है जो पार्टी की शक्ति है.
घर छोड़ आया अपढ़ बच्चों को शहर में विचरता
विचरता किसी दिन एक प्रबल उथल-पुथल
बदल देगी क़स्बे की चेतना
उसकी निराशा यह है:
बड़े कष्ट से मैं पिछल कुछ बरसों में
अपने को खींचकर लाया था दर्पण तक
उसमें जब देखा, देखी एक भीड़
कवि की बेचैनी यह है कि वह देख पाता है जो लोग कभी नहीं देख पाते कि वे रोज़ थोड़ा-थोड़ा मर रहे हैं:
रोज़-रोज़ थोड़ा-थोड़ा मरते हुए लोगों का झुंड
तिल-तिल खिसकता है शहर की तरफ़
और इस भीड़ में कहीं कोई छटपटाहट नहीं. यही कवि को व्याकुल करता है. जनतंत्र को लेकर दुविधा यह है कि प्रायः लोग इसमें भीड़ में शेष हो सकते हैं. दो ताक़तें एक साथ काम करती हैं. एक जो लोगों में जन भाव का सृजन करने की कोशिश करती हैं और दूसरी जो उसे भीड़ में बदल देना चाहती है.
जवाहरलाल नेहरू के लिए चुनाव अत्यंत ऊर्जादायी और उत्तेजनापूर्ण थे क्योंकि उनके मुताबिक़ ये जनता की जनतांत्रिक शिक्षा के लिए सबसे मुनासिब मौक़ा था. लेकिन चुनाव ही ऐसा अवसर भी ही सकता है जिसमें जनता को ‘देश की व्यवस्था का विराट वैभव’ चारों तरफ़ से दबोच ले.
उस वैभव से कवि अछूता रह सकता है, एक कोने में दुबका हुआ. वह जनता को सहला नहीं सकता. ‘नेता क्षमा करें’ कविता में वह अपनी निरुपायता को स्वीकार करता है,
लोगो, मेरे देश के लोगो और उसके नेताओ
मैं सिर्फ़ एक कवि हूं
मैं तुम्हें रोटी नहीं दे सकता और न उसके साथ खाने के लिए ग़म
न मैं मिटा सकता हूं ईश्वर के बारे में तुम्हारा संभ्रम
जनतंत्र में जनता और नेता के बीच एक रिश्ता है. नेता और दल जनता को बनाते और तोड़ते हैं. कवि का काम फिर क्या है? उसका और जनता का क्या संबंध है?
यानी कि आप ही सोचें कि जो कवि नहीं हैं
कि लोग सब एक तरफ़ और मैं एक तरफ़
और मैं कहूं कि तुम सब मेरे हो
पूछिए, मैं कौन हूं
वह अपने इन लोगों को छोड़ नहीं सकता लेकिन उनसे ख़ुद को अलग तो कर ही सकता है:
सब लोग जो कुछ रचाते हैं उसमें
केवल अपना मत नहीं दे ही तो सकता हूं
वह मैं करता हूं
किसी से नहीं डरता हूं
अपने आप और बेकार.
कभी-कभी मत नहीं देना भी जनतांत्रिक कर्तव्य है. यह न समझें कि कवि वोट नहीं देने को कह रहा है. वह सिर्फ़ अपने वक्त के लोकप्रिय मत से अपनी आवाज़ अलग करने के कर्तव्य को स्वीकार करता है. जानते हुए कि यह बेकार हो शायद. लेकिन प्रायः कवि का जनतंत्र के प्रति दायित्व यही है: लोकप्रिय से ख़ुद को अलग करना.
(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं.)
(इस श्रृंखला के सभी लेख पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.)