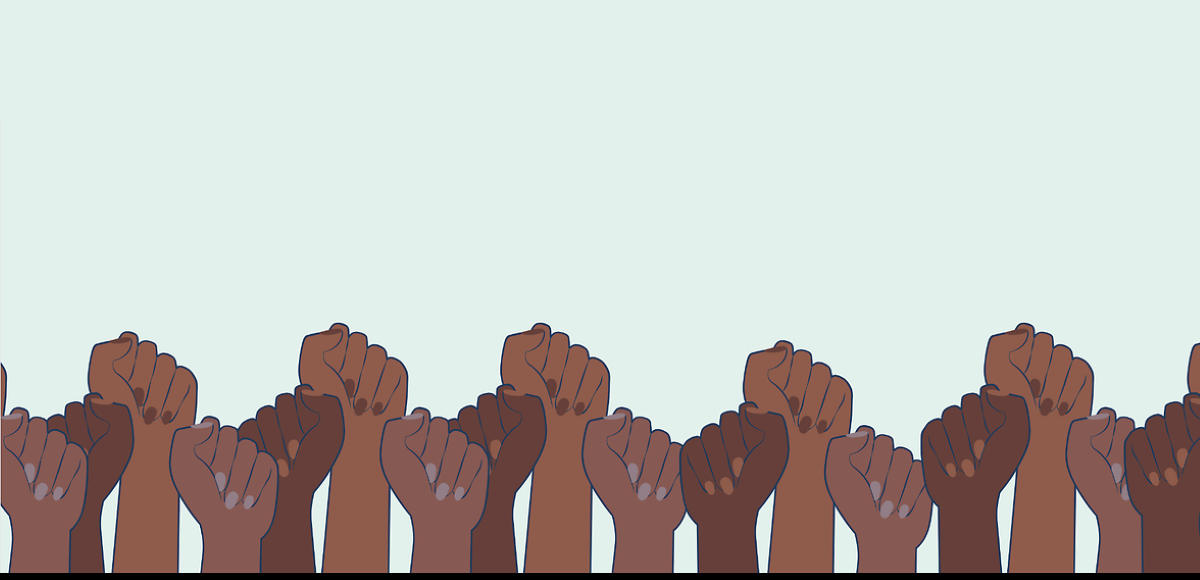[द गन इज़
नॉट इन द हैंड्स ऑफ
द पीपुल. – जे पी]
एक आदमी –
दूसरे आदमी की गरदन
धड़ से अलग कर देता है
जैसे एक मिस्त्री बल्टू से
नट अलग करता है.
तुम कहते हो- यह हत्या हो रही है
मैं कहता हूं- मेकेनिज्म टूट रहा है
नहीं …इस तरह चेहरा
मत सिकोड़ो और न कंधे ही
उचकाओ
मुझे मालूम है – सबूत के लिए
तुम कह सकते हो कि खून
बह रहा है.
लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है
और खून का रंग लाल है
असली सवाल है यह जानना
कि बहता हुआ खून क्या कह रहा है
यह हत्याकांड नहीं है सिर्फ़ लोहे को
एक नया नाम दिया जा रहा है
और सबूत के लिए यदि तुम
देखना चाहते ही चाहते हो
तो चलो मेरे साथ जंगल भाषा के जंगल में
कविता का वह वर्जित-प्रदेश
जहां कायरता –
एक ख़ाली तमंचा फेंक कर
भाग गई है और साहस
चंद पके हुए बालों के साथ
आगे बढ़ गया है –
अंधरे में.
(‘कविता – श्रीकाकुलम’)
यह धूमिल की ‘कविता- श्रीकाकुलम’ का अंश है. श्रीकाकुलम नक्सल आंदोलन को जानने वालों के लिए परिचित नाम है. वैसे ही जैसे नक्सलबाड़ी. बंगाल के एक छोटे से गांव के नाम पर भारत में वास्तविक जनतंत्र स्थापित करने के मक़सद से जो सशस्त्र संघर्ष 1967 में छेड़ा गया, वह अभी भी छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार के जंगलों में एक सपने की तरह चल रहा है.
कविता की इन पंक्तियों को पढ़िए:
एक आदमी –
दूसरे आदमी की गरदन
धड़ से अलग कर देता है
जैसे एक मिस्त्री बल्टू से
नट अलग करता है.
तुम कहते हो-य ह हत्या हो रही है
मैं कहता हूं- मेकेनिज्म टूट रहा है
कौन सा मेकेनिज़्म टूट रहा था? क्या वह संसदीय जनतंत्र का मेकेनिज़्म था? जिसके बारे में ‘जनतंत्र के सूर्योदय में’ धूमिल ने लिखा:
सिर कटे मुर्ग़े की तरह फड़कते हुए
जनतंत्र में
सुबह-
सिर्फ़, चमकते रंगों की चालबाजी है
1947 की भारत की आज़ादी के बारे में सबका खयाल एक सा नहीं था. दो तरह के लोग थे जो उसे असली नहीं मानते थे: एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग और दूसरे, कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े लोग. आरएसएस धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक गणतंत्र के रूप में भारत को स्वीकार नहीं कर सकता था. कम्युनिस्ट पार्टी की समझ थी कि असली आज़ादी वर्ग संघर्ष के बाद सर्वहारा की तानाशाही क़ायम करके ही लाई जा सकती है.
आरएसएस ने तिरंगा झंडा को अशुभ माना था और कहा था कि राष्ट्रध्वज पर मात्र एक रंग होना चाहिए. उसका वह सपना अभी भी ज़िंदा है जैसा उसके एक नेता ने हाल में कर्नाटक में कहा: भले ही 200 साल लगें, भारत पर भगवा ही लहराएगा.
कम्युनिस्टों का नारा भी था, ‘लाल क़िले पर लाल निशान, मांग रहा है हिंदुस्तान.’ अभी भी वह लगाया जाता है जैसा फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की एक नज्म कहती है, ‘हम हर इक देश के झंडे पर एक लाल सितारा मांगेंगे.’ कहा जा सकता है कि फ़ैज़ पूरे झंडे को लाल करने की बात नहीं कर रहे, हर झंडे पर सिर्फ़ एक लाल सितारा मांग रहे हैं. मुल्क पर मज़दूरों के हक़ की तसलीम.
आरएसएस ने अपने मुख्यालय पर आज़ादी के 53 साल बाद पहली बार तिरंगा फहराया. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने जब भारत की आज़ादी के 75वें साल में भारत में पार्टी के दफ़्तरों पर तिरंगा फहराने का निर्णय लिया तो उसे सबने नोट किया. ‘डेक्कन हेराल्ड’ ने लिखा कि पार्टी की स्थापना के बाद पहली बार सीपीएम मुख्यालय पर 15 अगस्त को तिरंगा फहराया जा रहा है. तिरंगा लहराने पर रोक न थी, लेकिन आम तौर पर उसे लेकर उदासीनता थी.
भारत का जनतंत्र बिना वर्ग संघर्ष के स्थापित हुआ जनतंत्र था. अगर इसे जनतंत्र मान लें तो भी यह अधूरा था. अधूरा इसे जवाहरलाल नेहरू भी कह रहे थे और भीमराव आंबेडकर भी. राजनीतिक जनतंत्र बिना आर्थिक जनतंत्र के पूरा नहीं, यह नेहरू का ख़याल था. आंबेडकर राजनीतिक आज़ादी को सामाजिक आज़ादी या बराबरी के बिना अपूर्ण मानते थे. दोनों ही इसके लिए संवैधानिक तरीक़ों से संघर्ष की वकालत कर रहे थे.
लेकिन कम्युनिस्ट इन दोनों से अलग थे. वे वर्ग संघर्ष, जो बिना सशस्त्र संघर्ष के हो ही नहीं सकता था, के ज़रिये असली आज़ादी लाने के संघर्ष को 1947 के बाद भी जारी रखना चाहते थे. सच्चे जनतंत्र का नमूना सोवियत संघ में ही देखा जा सकता था. भारत को उसी रास्ते चलना था.
बीटी रणदिवे के नेतृत्व में नारा दिया गया: ‘यह आज़ादी झूठी है.’ दो साल बाद पार्टी ने अपनी समझ बदली और सशस्त्र संघर्ष का रास्ता त्याग दिया.
इतिहासकार कहते हैं कि सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की तम्बीह के बाद यह निर्णय लिया गया. पार्टी ने संसदीय जनतंत्र में हिस्सा लेना शुरू किया. पहले आम चुनाव में वह संसद में ताकतवर विपक्ष बनकर उभरी. 1964 में पार्टी के विभाजन हुआ. उसके पहले माओ के नेतृत्व में चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई. जनतंत्र के बरक्स एक दूसरा प्रभावशाली मॉडल उभरा. लेकिन सोवियत संघ हो या चीन, एक पार्टी के शासन का ही मॉडल दोनों जगह था और वर्ग शत्रु के अंतिम सफ़ाये तक वर्ग संघर्ष दोनों जगह चलना था.
भारत का जनतंत्र बहुदलीय संसदीय जनतंत्र होना था. किसी एक पार्टी का स्थायी वर्चस्व इस मॉडल में संभव न था. आरएसएस को यह क़बूल नहीं जैसा अब उसकी राजनीतिक शाखा भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भारतीय जनतंत्र को विपक्ष मुक्त करना चाहती है.
कम्युनिस्टों के एक हिस्से का ख़्याल यह है कि चूंकि उसके पास ऐतिहासिक भौतिकवाद और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का ज्ञान मौजूद है जो इतिहास की और मानव समाज की सबसे अधिक वैज्ञानिक व्याख्या है, उसे ही भारत को सही रास्ते पर ले चलने का ऐतिहासिक अधिकार है. उसे ही पता है कि इतिहास का सही पथ कौन सा है!
भारतीय जनतंत्र के अधूरेपन के एहसास के भीतर एक कुंठा भी है: वह शत्रु का रक्त बहाए बिना हासिल की गई. आरएसएस का गांधी पर एक बड़ा आरोप है कि उन्होंने हिंदुओं को नामर्द बना दिया. कम्युनिस्टों का एक बड़ा हिस्सा गांधी के अहिंसा के सिद्धांत को किंचित् उपहास के साथ साथ ही देखता है. भारत की आज़ादी क्रांति न थी, यह विचार उसे कुछ छोटा बना देता है.
क्रांति के उस ख़याल को प्रायः स्थगित करके भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीएम) ने संसदीय जनतंत्र में हिस्सेदारी करना क़बूल किया. लेकिन क्रांति का वह विचार, वर्ग शत्रु के रक्त से अभिषिक्त और पवित्र क्रांति, जीवित रहा.
संसदीय जनतंत्र में क्रांति की उत्तेजना न थी. सीपीएम की स्थापना के 4 साल भी न गुजरे थे कि उसके एक सदस्य चारु मजूमदार ने इस विचार को अमली जामा पहनाने के विचार से एक अलग पार्टी का निर्माण किया. वे माओ के लोक युद्ध के सिद्धांत से प्रेरित थे जो किसानों की सेना बनाने और गुरिल्ला हथियारबंद संघर्ष के ज़रिये वर्ग शत्रुओं का सफ़ाया करके जनता का असली जनतंत्र स्थापित करता.
1967 में नक्सलबाड़ी में भूपतियों के घेराव और उन पर आक्रमण के बाद ग्रामीणों पर पुलिस की गोली चली. नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी. चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने इसे ‘भारत पर वसंत का वज्रनाद’ कहकर इसका स्वागत किया. इसके लिए कृतज्ञता के तौर पर चारु मजुमदार के नेतृत्व में गठित नई कम्युनिस्ट पार्टी ने माओ को अपना चेयरमैन घोषित किया.
हत्या या हिंसा इस क्रांति के लिए अनिवार्य थी. दिलीप सीमियन ने चारु मजूमदार को उद्धृत किया है, ‘एक समय आएगा जब युद्ध नाद होगा: जिसने वर्ग शत्रु के रक्त से अपना हाथ नहीं रंगा है, वह कम्युनिस्ट नहीं कहा जा सकता.’
वर्ग शत्रु के सफ़ाये का सिद्धांत बिहार में ‘6 इंच छोटा करो’ के रूप में लोकप्रिय हुआ. किसकी हत्या की जाएगी इसका निर्णय पार्टी का था और उस पर कोई सवाल नहीं हो सकता था. जो कम्युनिस्ट इस लाइन पर विश्वास नहीं करते, वे संशोधनवादी थे, वर्ग शत्रुओं के सहयोगी थे और उन्हें भी 6 इंच छोटा किया जा सकता था. इस तरह नक्सलवादियों ने सीपीआई और सीपीएम के भी कई सदस्यों की हत्या की.
नक्सलवादी आंदोलन ने प्रतिभाशाली नौजवानों को आकर्षित किया और वे सैकड़ों की तादाद में इसमें शामिल हुए. उनके बाद सबसे ज़्यादा उत्तेजित इसने लेखकों को किया. हर भाषा में धूमिल की तरह के कवि हुए जिन्होंने रक्तपात के सिद्धांत को वैध ठहराया.
एक-एक क़रके कई नक्सलवादी समूहों ने यह रास्ता छोड़ा और संसदीय जनतंत्र को स्वीकार किया. लेकिन वह विचार जीवित है. अब उसके वारिस और झंडाबरदार माओवादी हैं. लेकिन उनका यह दावा कि यह आंदोलन आदिवासियों का है, मिथ्या है. जैसा इतिहासकार दिलीप सीमियन लिखते हैं:
नक्सलवादी आंदोलन भूमिहीन किसानों और आदिवासियों का आंदोलन नहीं है जो राज्य सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहते हैं. यह उन लोगों द्वारा परिभाषित एक परियोजना है जो न तो किसान हैं, न ही मजदूर और न ही आदिवासी; लेकिन जो उनके हितों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं. यह दावा करने का अधिकार उस पर निर्भर था जिसे शुरुआती नक्सलवादी ‘क्रांतिकारी अधिकार’ कहा करते थे. यह इसलिए वैध अधिकार था क्योंकि इसे अंतरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन ने वैध ठहराया था, जिसका नेतृत्व चेयरमैन माओ के नेतृत्व वाली चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पास था.
नक्सलवादी अपनी हिंसा को इस आधार पर उचित ठहराते हैं कि उनके पास ही वैज्ञानिक विचार है और इतिहास की चाभी है. उनका विचार ही पहला और अंतिम विचार है और उसे जो चुनौती देगा, उसे जीवित रहने का अधिकार नहीं.
यह संसदीय जनतंत्र के विचार के ठीक उलट है. वह विचारों की बहुलता और समतुल्यता पर टिका है. वे एक दूसरे से प्रतियोगिता कर सकते हैं और उन्हें स्वीकार करने न करने का अधिकार जनता का है. जनता अपने विचार बदल भी सकती है. यह अधिकार उसे नक्सलवादी नहीं देते. सत्य उनके पास है और उस सत्य से इनकार करना धर्मद्रोह है.
अभी भी इस कविता के विचार को मानने वाले हैं जो रक्तपात को जायज़ मानते हैं:
नहीं …इस तरह चेहरा
मत सिकोड़ो और न कंधे ही
उचकाओ
मुझे मालूम है – सबूत के लिए
तुम कह सकते हो कि खून
बह रहा है.
लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है
और खून का रंग लाल है
असली सवाल है यह जानना
कि बहता हुआ खून क्या कह रहा है
यह हत्याकांड नहीं है सिर्फ़ लोहे को
एक नया नाम दिया जा रहा है
बहता हुआ खून क्या कह रहा है, यह कौन तय करेगा? किस खून पर कंधा उचकाया जाएगा? क्या माओवादियों द्वारा सामान्य लोगों की हत्या ‘मात्र ब्योरे का मामला’ है? क्यों खून का लाल होना भर काफ़ी नहीं?
जनतंत्र यह कहता है कि हरेक का खून लाल है और सबका मान समान है. जनतंत्र इसलिए अपने विरोधी की हत्या के सिद्धांत को स्वीकार नहीं कर सकता. लेकिन जो सिद्धांत हत्याकांड को यह कहकर महिमामंडित करे कि वह लोहे को नया नाम दे रहा है, उसके साथ आप जीवन कैसे साझा करें?
(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं.)
(इस श्रृंखला के सभी लेख पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.)