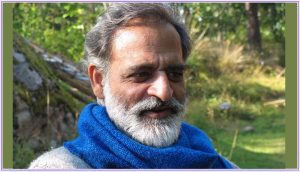हमें एक स्वतंत्र देश बने 77 वर्ष और एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बने 75 वर्ष हो गए. हम पश्चिम की औपनिवेशिकता से मुक्त हुए पर पश्चिमी ज्ञान, साहित्य, कलाओं को लेकर हमारे मन में एक तरह का दुचित्तापन अब तक ख़त्म नहीं हुआ है. एक ओर पश्चिमी मान्यता अब भी एक प्रतिमान बनी हुई है. हम उसे ही महत्वपूर्ण मानते हैं, चाहे कलाकार, लेखक, संगीतकार, नृत्यकार या लेखक या कृतियां जिन्हें पश्चिम में कुछ प्रतिष्ठता या पुरस्कार या अनुवाद के माध्यम से कुछ मान्यता मिल गई हो. और तो और राजनीति में हमारे राजनेता जब पश्चिमी राजनेताओं के साथ गलबहियां डाले नज़र आते हैं तो इसे पश्चिम में भारत की सशक्त उपस्थिति का प्रमाण माना जाता है.
लेकिन इसी पश्चिम की स्वायत्त आकलन संस्थाएं जब लोकतंत्र में हमारे उतार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में हमारे यहां हो रही कटौती, प्रेस की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों के साथ बढ़ रहे भेदभाव पर टिप्पणी और आलोचना करते हैं तो हम इसे अवांछित, तथ्यहीन, पूर्वाग्रहस्त आदि कहकर उनका प्रत्याख्यान करते हैं.
इस ओर हमारा ध्यान कम गया है कि आधुनिक भारतीय साहित्य और कलाओं में जो बड़े और प्रभावशाली आंदोलन हुए हैं जिनमें आधुनिकता, प्रगतिशीलता, विचारधारा के प्रतिबद्ध साहित्य और कला, उत्तर आधुनिकता, नई सामग्री का उपयोग कर इन्स्टलेशन आदि की धारा आदि सभी अपने मूल में पश्चिमी रहे हैं. इन्हें भले हमने अपना लिया, अपना बना लिया पर वे यहां की उपज नहीं रहे हैं.
यह थोड़ी चौंकाने वाली बात है कि भारत से निकला कोई विचार या आंदोलन या शैली संसार में व्याप्त नहीं हुआ. हमने औपनिवेशिकता से मुक्त स्वायत्त ढंग से भी जो कुछ किया अव्वल तो उसको पश्चिम ने पहचाना नहीं और दूसरे उससे कोई नई दृष्टि या विचार संसार में नहीं फैला.
यह तब है जब प्राचीन और मध्यकाल मे भारत से अनेक विचार, गणित, दर्शन, पद्धतियां, कथाएं आदि संसार भर में फैली थीं. हमारी आधुनिकता ने, महात्मा गांधी को छोड़कर, ऐसा कुछ नहीं रचा-सोचा जो फिर संसार भर में फैल गया हो. यह हमारी आधुनिकता की बुनियादी अनुर्वरता और विपन्नता का ही प्रमाण है.
ऐसा कहना आधुनिक कलाकारों-लेखकों के संघर्ष और अवदान की अवहेलना करना नहीं है. उनमें से कई ने, दुचित्तेपन को पहचान कर, उससे परे जाने या ऊपर उठने की महत्वपूर्ण चेष्टा की है. पर यह सचाई भी इस अधिक दारूण सचाई को छुपा-ढांप नहीं सकती कि हम अधकचरी परंपरा और अधकचरी आधुनिकता के बीच दयनीय ढंग से फंसे हैं.
कई बार लगता है कि युवा पीढ़ी आज इस दुचित्तेपन से बेख़बर है. उसे शायद इसकी ख़ास परवाह नहीं है कि हमारी बौद्धिक और सांस्कृतिक दुनिया किधर जा रही है. कम से कम मेरी बुढ़ाती आंखों को ऐसा कुछ नहीं दिखता जो मुझे बताए कि यह लापरवाही व्यापक नहीं है.
हाल के आम चुनाव का एक नतीजा तो, दुर्भाग्य से, यह है कि लोकतंत्र, संविधान और बहुलता को बचाने का काम ग़रीबों-वंचितों-दलितों-अल्पसंख्यकों आदि ने किया है और पढ़े-लिखे चिकने-चुपड़े वर्गों की भूमिका उसमें न के बराबर है.
दुचित्तेपन से मुक्त होने का आशय न तो यह है कि हम अपने को संसार में विकसित विचार-चिंतन-सृजन-टेक्नोलॉजी-विज्ञान-ज्ञान आदि से विरत-विमुख कर लें और न ही यह कि हम अपने यहां के पारंपरिक चिंतन-सृजन-कलाओं-ज्ञान आदि को पर्याप्त और आधुनिकता से संपन्न मानकर किसी छद्म आत्मगौरव में इठलाने लगें.
दुचित्तेपन से मुक्ति मिल सकती है एक दुधारी आलोचना दृष्टि से, जिसमें संसार भर से आए, तैरते, वर्चस्व पा गए विचारों-शैलियों आदि की गहरी विवेचना और क्रिटीक हो और अपनी परंपरा और आधुनिकता की ऐसी ही सख़्त पड़ताल भी. बिना सोचे-समझे या बिना किसी परीक्षण के, हमने जो बहुत सारा मान लिया या जिसका हम अपने बौद्धिक और सर्जनात्मक व्यवहार में अनुसरण या अनुगमन करने लगे हैं उसे हमें निर्मम होकर छोड़ना-बदलना होगा.
आत्मस्थ आधुनिक
जगदीश स्वामीनाथन के 96वें जन्मदिन पर उन पर एक भरी-पूरी पुस्तक का प्रकाशन, प्रयाग शुक्ल और श्रुति लखनपाल टंडन के संपादन में, धूमिमल गैलरी ने किया. इस अवसर पर स्वामी की दृष्टि पर विचार हुआ, उनकी कविताओं की नाट्यप्रस्तुति, मूल हिंदी के अलावा अंग्रेज़ी और बांग्ला में उनके अनुवाद का पाठ, शास्त्रीय सरोदवादन और फिल्म प्रदर्शन आदि हुए. बड़ी संख्या में, भीषण गर्मी के बावजूद, अनेक कलाकार और कला प्रेमी इस दिन भर चले आयोजन में शामिल हुए.
उदयन वाजपेयी ने स्वामी को विउपनिवेशीकरण की भारतीय धारा में महात्मा गांधी की परंपरा में अवस्थित करते हुए उनकी कला और चिंतन को व्यापक संदर्भ मे देखा: पश्चिम-पूर्व के लगभग भुला दिए गए द्वंद्व के परिप्रेक्ष्य में. ग्रीक कला-चिंतन ने सौंदर्य को ‘संपूर्ण रूप’ माना गया और उसने उसे परिभाषित कर सीमित कर दिया. उसी के प्रभाव में कला के परिसर के लोक अभिव्यक्ति को बाहर कर दिया गया. स्वामी की कोशिश थी हमें यह पहचानवाने की कि लोक और आदिवासी कलाएं हमारे पारंपरिक सौंदर्य चिंतन में उतनी ही कलाएं थीं, जितनी अधिक नागर कलाएं.
स्वामीनाथन जैसे बड़े कलाकार को, उनकी दृष्टि और अवदान को देखने-परखने की कई दृष्टियां हो सकती हैं और अब वे धीरे-धीरे सामने आ रही हैं. जो व्यक्ति पलाश वृक्ष से संवाद कर सकता था; जो भारत के राष्ट्रपति के सामने यह इसरार कर सकता था कि कोई कलाकृति खुद होती है और उसका किसी के बारे में होना ज़रूरी नहीं; जो यह भी कह सकता है कि मैंने यह कृति बनाई है पर मुझे तो समझ में नहीं आती है; जो पहाड़ी कोरवा के चित्रों में रहस्यमय जादुई लिपि की तलाश कर सकता था; वह एक असाधारण कलाकार ही नहीं, असाधारण कला-चिंतक भी था.
यह बात दोहराने की है कि स्वामी कला को सचाई का प्रतिनिधित्व करने या उसे प्रतिबिंबित करने की विधा नहीं मानते थे: उनके नज़दीक कला स्वयं सचाई होती है, जो दी हुई सचाई में इज़ाफ़ा करती है: ‘सचाई का बिंब नहीं, बिंब की सचाई’. उनकी अपनी कला, रंगों और आकारों की प्रचलित सचाई से अलग, एक मोहक अतियथार्थ रचती थी जिसमें प्रचलित यथार्थ झर जाता था. वहां प्रकृति मानों इतिहास को अतिक्रमित करती, उसे आक्रांत करती, उसे पोंछ देती है: स्वामी की कला एक तरह की समयहीनता में अवस्थित या तैरती है.
यह भारतीय आधुनिक कला में सौंदर्य और लालित्य ने पुनरूदय का क्षण भी है और कला में कॉस्मिक लय के पुनर्ग्रहण का. नए फिर भी सनातन सम्मोहन का. यह क्षण एक तरह के आदिम संकेत का है जिसमें संप्रेषण नहीं, तादात्म्य की प्रमुखता है. स्वामी कहते थे कि ‘मैं मनुष्य को नहीं चित्रित करता, मैं मनुष्य की तरह चित्रित करता हूं’.
यह आकस्मिक नहीं, स्वामी का सोचा-समझा फ़ैसला था कि जब कला पर विचारधारा का प्रभाव बहुत गहरा हो चुका था तब वे कला की स्वायत्तता पर इसरार कर रहे थे. जब जगहों और लोगों के चित्रण पर बल दिया जा रहा था, स्वामी के चित्रों में पक्षी और वृक्ष थे, पहाड़ और सीढ़ियां थे पर लोग नहीं. उनके चित्रों में जगह कोई विशेष जगह नहीं, एक अनंत वितान था.
स्वामीनाथन नायक कलाकार थे: उन्होंने कला की सार्वजनिकता में भी अपनी जगह बनाई: वे ‘ग्रुप 1890’ के लगभग संस्थापक और प्रवक्ता थे; कला की एक बेहद महत्वपूर्ण और हस्तक्षेपकारी पत्रिका ‘काण्ट्रा’ के संपादक-प्रकाशक थे. वे ललित कला अकादमी के 1975 के त्रिनाले के प्रमुख संयोजक थे; उन्होंने भारत भवन में रूपंकर संग्रहालय की स्थापना और संचालन किया और अपनी मृत्यु के समय वे भोपाल के केंद्रीय मानव संग्रहालय के उपाध्यक्ष थे.
स्वामी की दृष्टि और जीवन-शैली में कम से कम दो गांधी-तत्व थे जिनकी अब शिनाख़्त होना चाहिए. वे गांधी जी के विचार से असहमत होकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और फिर कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए थे. पर जीवन भर खादी के कपड़े ही पहनते थे. जटिल चिंतन और कला साधना करता सादा-सुथरा जीवन दूसरा तत्व था उनका लोक आदिवासी कला की शहराती कला के साथ समता और समकक्षता का एहतराम और उस पर इसरार.
यह केवल कलात्मक विस्तार नहीं था, यह एक नैतिक हस्तक्षेप भी था तथाकथित वंचित-शोषित को कला की बरादरी में शामिल करने, समान आदर और जगह देने, उनकी कला के सौंदर्य और स्फूर्ति को, उनके संघर्ष की निर्मल गरिमा को जगह देने का.
(लेखक वरिष्ठ साहित्यकार हैं.)