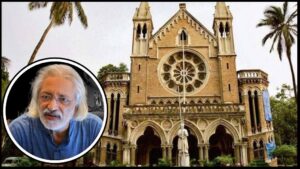बांग्लादेश की आज़ादी के पचास वर्ष होने पर दिसंबर 2021 में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने द टेलीग्राफ में पांच लेखों की श्रृंखला लिखी थी. आज जो हालात बांग्लादेश में है, उसकी आशंका इन लेखों के लिखे जाते वक्त भी थी. 2018 के चुनावों में अवामी लीग को बहुमत मिला था, लेकिन इन चुनावों की निष्पक्षता पर ख़ुद उनके नेताओं ने सवाल खड़े किए थे. बांग्लादेश की वर्तमान राजनीति को समझने में मदद करते ये लेख उसकी आज़ादी में भारत की भूमिका, दोनों देशों में जनतंत्र का स्वरूप और यह एहसास कि यदि एक देश धर्मनिरपेक्षता के रास्ते हो छोड़ता है तो दूसरा भी धर्मनिरपेक्ष नहीं रह सकता, बांग्लादेश की अभूतपूर्व आर्थिक उन्नति जैसे मुद्दों पर केंद्रित हैं.
इन लेखों की प्रासंगिकता को देखते हुए हम शुभेन्द्र त्यागी द्वारा किया इनका अनुवाद प्रकाशित कर रहे हैं. पहला भाग यहां पढ़ सकते हैं.
§
बंगबंधु ने ‘लोकतंत्र’ और ‘धर्मनिरपेक्षता’ को इस नवोदित देश की राष्ट्रीयता के प्रमुख आदर्शों के रूप में स्थापित किया था. बांग्लादेशियों ने अपने पिछले 25 वर्ष सैनिक तानाशाही में गुजारे थे, जिसमें उन्होने भयानक भेदभाव झेला था, ‘इस्लाम की एकता’ के नाम पर उनके संसाधनों का दोहन किया गया और अंत में आम जनता को भयानक हिंसा की आग में झोंक दिया गया. इसके बाद जब संविधान पर आधारित लोकतंत्र की स्थापना हुई तो जनता ने इसका स्वागत किया. लेकिन फिर भी शासन व्यवस्था कैसी हो इस पर व्यापक आम सहमति नहीं बन सकी.
अंध राजभक्ति ने ‘विवादप्रिय बंगाली’ के पनपने के लिए ज़मीन तैयार की, जिसने तबसे बांग्लादेश को बड़े अड्डे में बदल दिया है. ‘राजनिति अंधभक्ति का ही दूसरा नाम रही है’ और ‘दलगत राजनीति इतना गहरे पैठ चुकी है कि उसने सारी बहसों को संकीर्ण राजनीति के इर्दगिर्द समेट दिया है.’
मुजीब ने बांग्लादेश कृषक श्रमिक अवामी लीग (बीकेएसएल) के द्वारा अलग व्यवस्थित और सैद्धांतिक परंपरा की शुरुआत करनी चाही थी, जिसमें पार्टी खुद किसी पद के लिए चार प्रत्याशियों को उतारती थी, जो एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार भी करते थे और इस तरह शासन व्यवस्था को कमजोर किए बगैर मतदाताओं को चयन करने का विकल्प मिलता था. पर यह प्रयोग बुरी तरह विफल रहा. संभवतः यही बंगबंधु और उनके परिवार की हत्या और जनरल जियाउर रहमान और मुहम्मद हुसैन के नेतृत्व में 1975 से 1990 तक जनतांत्रिक सरकार को अपदस्थ करके फ़ौजी शासन के क़ायम होने का कारण भी बना.
उसके बाद फिर चुनाव हुए. आजादी की रजत जयंती (25 वर्ष) होने पर शेख हसीना गठबंधन सरकार का हिस्सा बनीं, लेकिन सरकार में उनकी भूमिका नगण्य रही. वे 2009 में अपनी स्पष्ट बहुमत की सरकार की नेता बनकर उभरीं. तबसे उन्होने पीछे मुड़कर नहीं देखा.
बांग्लादेश की राजनीति की समझ रखने वालों का यह मानना है कि वे इंदिरा गांधी के 18 वर्षों तक प्रधानमंत्री रहने के कीर्तिमान को पीछे छोड़ देंगी. उनके लगातार प्रधानमंत्री बने रहने से सरकार को स्थायित्व मिला है और इस देश को ‘आर्थिक कीर्तिमान’ स्थापित करने का अवसर भी. लेकिन इस देश ने इसकी कीमत भी चुकाई है- अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को गंवाकर.
अगले चुनाव में भी किसी दूसरे राजनीतिक दल की जीत की उम्मीद बहुत कम है. (यह स्थिति भारत लिए परिचित सी है न!).यह 2008-09 से अब तक उनकी लगातार चौथी जीत होगी. पहले वे 2008-09 में हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में जीतीं. उसके बाद के चुनाव में वे निर्विरोध जीती, तीसरे चुनाव में चुनाव प्रक्रिया में धांधली से जीत हासिल की. (जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उनकी जीत वैसे भी निश्चित थी). इसने सरकार के भीतर अहंकार पैदा किया. ‘जिसके कारण संस्थानों में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला’, ‘संस्थाओं को कमजोर किया’ गया और ‘लोकतांत्रिक व्यवस्था को लगभग ख़त्म कर दिया.’
ये बातें शेख हसीना की सरकार के एक समर्थक ने कहीं. नागरिक अधिकारों और मानवाधिकारों की कई बार बुरी तरह अनदेखी हुई और ‘भय का वातावरण’ पैदा हुआ. लेकिन इसका परिणाम लगभग ली क्वान यू के सिंगापुर की तरह रहा: तानाशाही के परिणामस्वरूप अप्रतिम आर्थिक संवृद्धि. इस आर्थिक संवृद्धि के बारे में इस श्रृंखला के अगले भागों में हम विस्तार से लिखेंगे. लेकिन इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि इस समय थोड़ी-सी भी राजनीतिक अस्थिरता शेख हसीना के कार्यकाल में हुए सामाजिक-आर्थिक विकास को गंभीर रूप से खतरे में डाल देगी.
इसके अलावा ‘आतंकवाद’ पर भी प्रभावी नियंत्रण रहा और ‘कट्टर सांप्रदायिकता’, ‘सेना’ को भी नियंत्रण में रखा गया. ये उपलब्धियां भी काम नहीं है और इनका श्रेय शेख हसीना को मिलना ही चाहिए. जैसा एक समझदार व्यक्ति ने कहा भी ‘उन्होने खुद को अपने पिता से कहीं बेहतर राजनेता साबित किया है.’
फिर भी उनके शासन की तीव्र और निर्मम आलोचना होती है. एक बैठक में अपनी बात रखते हुए जब मैंने कहा कि जब हम प्रधानमंत्री से मिले तो मेरी पत्नी- सुनीत ने उनसे कहा था कि ढाका के लोगों से बात कर और भारत के लोगों से मिलने पर जो प्रमुख अंतर उन्हें नजर आया कि बांग्लादेश की जनता की आंखों में उम्मीद है, मुश्किलों को जीतकर आगे बढ़ने का संतोष है, भविष्य को लेकर आशाएं हैं, लेकिन भारत में निराशा है, नाउम्मीदी है, अनिश्चय है. तभी सभा में बैठे एक सज्जन कहते हैं ‘जैसी राय भारत के बारे में आपकी है वैसी ही राय बांग्लादेश के बारे में बांग्लादेश के उन लोगों की जिनसे मिलने का आपको मौक़ा नहीं मिला.’
एक महिला सुनीत की बात को ‘उत्साहजनक’ बताती है और कहती है ‘हमने जो हमने हासिल किया है’ की तुलना हमेशा ‘जो हमारा लक्ष्य था’ से करते हैं. उन्हें इस बात का एहसास है कि युवा अधिक समझदार और विचारशील हैं. लेकिन ये विचार तब तक व्यर्थ है जब तक उन्हें व्यक्त होने का सही माध्यम नहीं मिले. लेकिन वे यह बताना भी नहीं भूलती जो संस्थान इन विचारों को पल्लवित कर सकें वे ही आज खतरे में हैं.
मैं शेख हसीना की सरकार के एक वरिष्ठ प्रवक्ता की मुझसे कही एक बात का जिक्र करता हूं. उन्होने कहा था कि आपने प्रेस पर सरकार के ‘दवाब’ के बारे में सुना होगा . फिर जिसका खंडन उन्होने यह कहते हुए किया था ‘आप कोई भी अखबार उठा कर देख लीजिए उनमें सरकार की कितनी निर्मम आलोचना होती है.’ एक युवा टीवी रिपोर्टर इस दावे का खंडन करती है. वे कहतीं हैं कि उन्हें अपने कार्यक्रम के लिए एक भी ऐसा पत्रकार नहीं मिला जो सरकार के विरुद्ध बोल सके- ‘गिरफ्तारी का डर है न.’
वे जोर देकर कहतीं हैं 2013 (शेख हसीना के प्रथम कार्यकाल का अंतिम वर्ष) से सरकार की आलोचना करने वाला एक कार्टून तक नहीं छपा है.
एक अन्य पत्रकार इसी बीच अपनी बात रखते हैं, ‘उम्मीद का अब कोई कारण नहीं बचा. हम बेशक तानाशाही शासन में रह रहे हैं. अपनी बात कहने पर बंदिशें हैं, न्याय व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, शिक्षा का; मुख्यतः देहातों में बुरी तरह पतन हुआ है. हम दिन रात भय के ही वातावरण में सांस लेते हैं.’
लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो इन बातों को अतिश्योक्ति कहकर खारिज करते हैं. वे कहते हैं प्रधानमंत्री एक ‘सजग’ नेता हैं और ‘योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू’ करती हैं. खालिदा के कार्यकाल से शेख हसीना का कार्यकाल कितना बेहतर है यह बताने के लिए वे कहते हैं कि पहले ‘भ्रष्टाचार था और अव्यवस्था’ भी थी ‘अब भ्रष्टाचार है लेकिन व्यवस्था अच्छी है.’
उनका मानना है कि देश के सामने समस्याएं दूसरी हैं. चूंकि भविष्य में अवामी लीग की सरकार जाती नहीं दिखती, इसलिए सरकारी महकमों में ‘स्थाई होने’ का भाव घर कर गया है, ‘किसी के प्रति कोई जवाबदेही नहीं’, ‘दूसरी आवाजों का कोई सम्मान नहीं’, बस ‘आत्मप्रशंसा आत्ममुग्धता.’
अपनी बात को समझाते हुए वे कहते हैं प्रधानमंत्री की अनुपलब्धता तो शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या है. अतः व्यापारी राजनेताओं की चापलूसी के लिए विवश हैं. यह व्यवस्था आखिर ऐसे ही कब तक चल पाएगी यह सवाल सबके मन में है और इसका जवाब है ‘निष्पक्ष चुनाव’ और ‘मजबूत लोकतंत्र.’
अन्य लोग ‘निष्पक्ष चुनाव’ और ‘लोकतंत्र को मजबूत’ करने की बात का समर्थन तो करते हैं लेकिन ऐसा होने की उम्मीद कम ही नजर आती है क्योंकि सरकार का मुख्य रूप से ध्यान तो रैपिड एक्शन बटालियन द्वारा किए जा रहे ‘अपहरण’ और ‘गैर कानूनी हत्याओं’ पर है. स्वतंत्र और निर्भीक विचारों के लिए जगह अब नहीं बची है. मीडिया मालिक तो पहले से ही घुटनों पर हैं, यदि वे थोड़ा-सा भी सरकार की विचारधारा के विरोध में जाते हैं तो सरकारी विज्ञापन बंद कर दिए जाते हैं जो उनकी आय के प्रमुख स्रोत हैं. डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट ने तो खोजी पत्रकारिता के ताबूत में आखरी कील ठोक दी है, और जो सूचना के अधिकार कानून का उपयोग करते हैं उन्हें प्रताड़ित किया जाता है. राजद्रोह की नंगी तलवार हमेशा नागरिकों की गर्दन पर रहती है (क्या ये परिस्थिति भारत के लिए परिचित सी नहीं है).
बैठक में भाग ले रहीं अन्य महिलाएं न्याय व्यवस्था की तीखी आलोचना करती हैं. ‘यह सबसे कमजोर संस्थान है, इसका पूरी तरह राजनीतिकरण हो चुका है क्योंकि न्यायिक नियुक्तियां ‘कार्यपालिका की इच्छानुसार’ होती हैं. पदोन्नति का आधार आपकी ‘वरिष्ठता, अनुभव और योग्यता’ नही बल्कि शासन के प्रति ‘वफादारी’ है.
वे यह भी कहती हैं कि न्यायधीशों में इतना भय है कि कुछ मामलों में उन्होने वकीलों से अभियुक्तों की पैरवी तक करने से मना किया है. पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार सिन्हा का जिक्र किया जाता है जिन्हें सरकार के खिलाफ फैसला देने के लिए कनाडा निष्कासित होकर भागना पड़ा था. न्यायपालिका में ऊपर से नीचे तक व्याप्त भ्रष्टाचार की भी बात की जाती है. स्वतंत्र न्यायपालिका के अभाव का परिणाम होता है कि मानवाधिकारों के भयावह उलंघन की न कोई जांच हो पाती है न किसी को सजा मिल पाती है, विशेषकर तब जब न्याय तक सामान्य लोगों की पहुंच ही न हो.
‘लोकतंत्र की मृत्यु अंततः न्याय की मृत्यु है.’ यह बात कितनी ही बार साबित हो चुकी है. राजनीति में मिली सफलता का असर आर्थिक समृद्धि पर भी होता है. इसका सीधा परिणाम होता है छोटे स्थानीय नेताओं द्वारा बड़े पैमाने पर धांधली और बदले में व्यापार और राजनीति का गठजोड़. एक दूसरे बुद्धिजीवी जो मुख्य रूप से मुझसे मिलने बुलाए गए थे, ताकि मुझे सभी पक्षों की राय मालूम हो सके- ‘खुद को लोकतंत्र कहना थोड़ा मुश्किल है हमारे यहां चुनाव केवल नाम के लिए है, वास्तव में तानाशाही सरकार और भ्रष्ट नौकरशाही है,’ उनका कहना था.
लेकिन जितना आक्रोश वरिष्ठ नागरिकों में है, उतना युवाओं में नहीं. एक व्यक्ति का मानना है कि युवा अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार का मुंह नहीं ताकते. वे खुद पर ही निर्भर होना ठीक समझते हैं. एक दूसरे का मनाना है कि वे ‘वास्तविकता को स्वीकार’ करतीं हैं लेकिन ‘आशावादी’ भी हैं. आखिरकार हम एक ‘नौजवान मुल्क हैं’, ‘आज़ादी ने हमारी सोच को भी मुक्त किया है.’ वे गर्व से माइक्रो फाइनेंस की उपलब्धियों, निजी क्षेत्र की उन्नति का और कोविड 19 से निपटने में सरकार की सफलताओं का जिक्र करती हैं.
मुझे लगता है अंत में उनके मत का जिक्र करना चाहिए जो इस सरकार के समर्थक तो हैं, लेकिन यह भी मानते हैं कि पिछले चुनाव धांधली से जीते गए थे. जिसका नतीजा देश 70 प्रतिशत सांसदों के व्यवसायियों और कैबिनेट में उद्योगपतियों की भरमार के रूप में भुगत रहा है. अतः ‘अगले आम चुनाव’ एक ‘अग्नि परीक्षा’ है जो यह तय करेगें कि बांग्लादेश लोकतंत्र के रूप में बच भी पाएगा कि नहीं. उन्हें इस बात का निश्चय है कि अगले चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होंगे और चुनी गई सरकार की ‘जनता की नज़र में विश्वसनीयता.’
(मूल रूप से अंग्रेज़ी में लिखे गए इस लेख का अनुवाद शुभेन्द्र त्यागी ने किया है. वे दिल्ली विश्वविद्यालय में शोधार्थी हैं.)