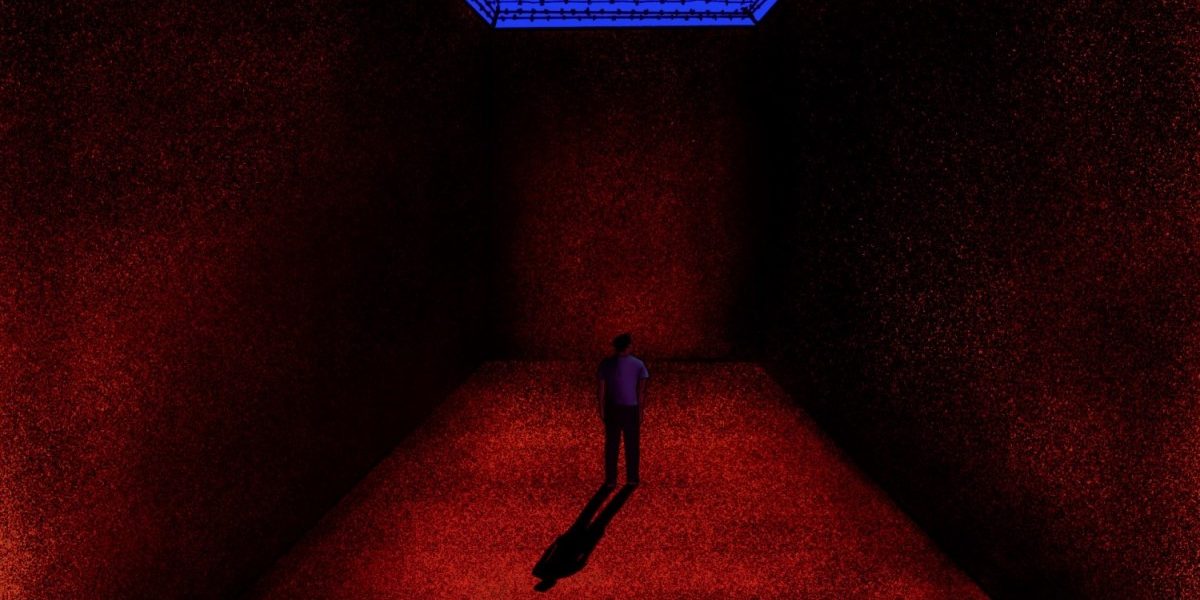आधुनिक समय में प्रायः सभी तरह की राजनीतिक व्यवस्थाओं में सत्ता और संस्कृति का संबंध और प्रश्न विवाद के घेरे में रहा है. यह विवाद विचारधारा और संस्कृति के संबंध और द्वंद्व को भी घेरे में लेता रहा है. यह विवाद और तीखा हो जाता है तब कोई सत्ता अपने को ही, यानी राज्य को समाज मानने लगे, उसे मनवाने पर ज़ोर देने लगे और अपने एजेंडा को मूलतः सांस्कृतिक बताने लगे. आज भारत में यही हो रहा है. इसलिए उस पर नए सिरे से विचार ज़रूर हो जाता है.
लोकतांत्रिक व्यवस्था में जैसे राज्य की सामाजिक जीवन के अनेक पक्षों में शिक्षा-स्वास्थ्य-खेती-सिंचाई-व्यापार-आयात-निर्यात-क़ानून-अंतरराष्ट्रीय संबंध-उद्योग-नागरिक सुविधाएं-यातायात आदि में ज़िम्मेदारी होती है वैसे ही संस्कृति के क्षेत्र में भी. संग्रहालय, सभागार-पुस्तकालय, पुरातात्विक संरक्षण, वीथिकाएं आदि अनेक सांस्कृतिक स्थान, सुविधाएं और संस्थाएं राज्य ही बनाता, विकसित और पोषित करता है. भले यह व्यापक संस्कृति का अपेक्षाकृत छोटा-सा क्षेत्र होता है पर वह महत्वपूर्ण और कई बार निर्णायक साबित होता है. दूसरी ओर, यह भी सही है कि संस्कृति समाज रचता-पोसता-बदलता है और यह राज्य का काम नहीं होता.
वर्तमान निज़ाम अपनी राजनीति और सामाजिक व्यवहार में संस्कृति के कई तत्वों और छवियों का इस्तेमाल करता आया है. अक्सर यह सत्ता की शोभा या रुतबा बढ़ाने के लिए होता है. हिंदुत्व, राम मंदिर, सेंगोल, केदारनाथ की गुफा में बेहद दृश्य चिंतन आदि उसके बहुत प्रगट रूप हैं. साथ ही साथ यह निज़ाम परस्पर सद्भाव के बजाय भेदभाव, प्रेम और समरसता के बजाय घृणा और अलगाव, अहिंसा और शांति के बजाय हिंसा और अशांति को खुल्लमखुल्ला बढ़ावा देता रहा है.
सचाई तो यह है कि इस निज़ाम ने न सिर्फ़ गांधी-नेहरू का अवमूल्यन किया है बल्कि वह लगातार भारतीय संस्कृति के बुनियादी तत्वों और आत्मा का भी अवमूल्यन करता आ रहा है. पहले के निज़ामों में कमोबेश संस्कृति की स्वतंत्रता और गरिमा का एहतराम और आदर दोनो ही थे: इस निज़ाम ने संस्कृति को राजनीति की दासी और अधिक से अधिक उसे सत्ता के महिमामंडन और शोभा की चीज़ बना दिया है.
इस व्यापक अवमूल्यन का एक पक्ष यह है कि स्वयं संस्कृति से संबंधित राष्ट्रीय संस्थाएं है. उनकी इस समय जो दुर्गति है वह अभूतपूर्व है. उनका अपना स्वाभाविक एजेंडा हाशिये पर चला गया है और वे सत्ता के राजनीतिक एजेंडा में सहायक के रूप में काम कर रहे हैं. उत्कृष्टता तो दूर ये संस्थान भयानक मीडियोक्रिटी के शिकार होकर एक तरह की साधन-संपन्न गुमनामी में चले गए हैं. उनके पास अनुदान बहुत है पर संसार-समाज-संस्कृति की तेज़ी से बदलती परिस्थिति के लिए कोई सशक्त सांस्कृतिक विचार या दृष्टियां नहीं हैं.
भारत में धर्म नहीं, संस्कृति सनातन रही है. इस समय सनातन के नाम पर हिंसा-हत्या-झूठ-घृणा-अत्याचार-अन्याय की जो बुलडोज़ी मानसिकता सशक्त-सबल-सक्रिय है उसका न तो सनातन संस्कृति, न ही किसी धर्म से कोई अनुमोदन मिल सकता है.
इस पर बहस मुमकिन है कि भारत में धर्म पहले आया कि संस्कृति, पर इसमें संदेह नहीं कि घनिष्ठ होते हुए भी दोनों परस्पर स्वतंत्रता का आदर करते रहे हैं. कम से कम इतना तो बिल्कुल ही स्पष्ट और अकाट्य कि भारत में धर्मों और संस्कृतियों की बहुलता रही है. नए निज़ाम ने बहुत तेज़ी-फुर्ती से दोनों को ही राजनीति के अधीन लाने की कोशिश की है. यह आकस्मिक नहीं है कि इन दिनों बहुत से धर्मनेता धर्म पर कम, राजनीति पर अधिक बोलते हैं और उनमें से ज़्यादातर सांस्कृतिक रूप से लगभग निरक्षर नज़र आते हैं.
जो नई दौलत पैदा हो रही है उसका एक लगभग नगण्य हिंसा संस्कृति के खाते में जा रहा है. कॉरपोरेट सोशल रिस्पान्सिबिलिटी के अंतर्गत अपने लाभ का जो हिस्सा कॉरपोरेट को क़ानूनन लोकहित में ख़र्च करना होता है उसका कुल दो प्रतिशत संस्कृति को मिल पाता है. ये आंकड़े भी चार-पांच बरस पहले के हैं- इस बीच यह प्रतिशत और घट गया होगा. इसका आशय यह है कि संस्कृति को अपने संवर्द्धन के लिए राज्य और समाज के एक बड़े साधन-संपन्न हिस्से से कुछ ख़ास नहीं मिल रहा है और न ही इसमें जल्दी किसी बदलाव की उम्मीद करना चाहिए.
इस समय भारत में ज्ञान, विज्ञान, बुद्धि और सृजन सभी पर गहरा संकट है. जो नई राजनीतिक संस्कृति विकसित हुई है उसमें ज्ञान के बजाय अज्ञान का महिमामंडन हो रहा है. उच्च से लेकर प्राथमिक शिक्षा तक में ज्ञान के बजाय आज्ञाकारिता, भक्ति पर बल दिया जा रहा है.
एक अख़बार में आंकड़े आए हैं कि भारत के पास हर दस लाख जनसंख्या पर कुल 260 वैज्ञानिक हैं जबकि अमेरिका और ब्रिटेन में यह संख्या 4,000 है. वैज्ञानिक शोधकों के क्षेत्र में विश्वसूची में भारत का नंबर 81वां है. इस स्थिति से स्पष्ट है कि इन क्षेत्रों में हम ग़रीब और पिछड़े हुए हैं और हमारा विश्वगुरु बनने का स्वप्न दयनीय और हास्यास्पद भर है.
सामाजिक संस्थाएं
इस बार अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जिन अर्थशास्त्रियों को दिया जाता है उनका योगदान यह माना गया है कि उन्होंने अपने अध्ययन और शोध से यह दिखाया है कि किसी देश की समृद्धि में उसकी सामाजिक संस्थाओं की निर्णायक भूमिका होती है: जिन समाजों में क़ानून व्यवस्था ख़राब हो और शोषक संस्थाएं हों उनमें ठोस प्रगति नहीं होती, न ही बेहतरी के लिए बदलाव.
इस नतीजे और स्थापना को लेकर पहले भी बहस होती रही है. नोबेल पुरस्कार ने इस बहस को नई तेज़ी दे दी है. यह भी पहले अमर्त्य सेन जैसे अर्थशास्त्री बता चुके हैं कि सच्ची और टिकाऊ प्रगति किसी देश में उसकी शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था और उनमें सार्वजनिक निवेश पर निर्भर करती है.
स्वीडिश अकादमी ने अपनी प्रशस्ति में यह बताया है कि अठारहवीं शताब्दी के मध्य तक (यानी आज से कुछ सवा दो सौ साल पहले) भारत का औद्योगिक उत्पादन संयुक्त अमेरिका के उत्पादन से ऊंचा था. इस स्थिति में औपनिवेशिक शासन के अधीन बुनियादी परिवर्तन हुआ. भारत में इन दिनों मुग़ल काल की जो अहर्निश निंदा सत्तारूढ़ शक्तियों के छोटे-बड़े प्यादे करते रहते हैं, उन्हें अपने झूठ और दुर्व्याख्या पर फिर से विचार करना चाहिए, हालांकि झूठ और अज्ञान के अटल बिहारी से ऐसी दुराशा करना व्यर्थ है.
बहरहाल, जो बहस अब हो रही है उसमें जिन तीन अर्थशास्त्रियों को इस बार नोबेल पुरस्कार मिला उनमें से एक ने यह जोड़ा है कि अनेक अंतरराष्ट्रीय संगठनों के सर्वेक्षण यह बताते हैं कि इस समय संसार में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास करने वाले बहुत घट गए हैं. इसका आशय यह है कि लोकतंत्र पर विश्वव्यापी संकट है.
ज़ाहिर है कि विश्व भर में लोकतंत्र से जो अपेक्षाएं की गई थीं, वह पूरी नहीं कर पाया है. अर्थशास्त्री यह कहते हैं कि बहुत ज़रूरी है कि लोकतंत्र अपनी ऊंचाई और बुलंदी फिर हासिल करे और ज़्यादा बड़ी संख्या में लोगों को स्वच्छ सुशासन मिलना सुनिश्चित करे.
भारत में संस्थाओं की जो हालत है उस पर विचार ज़रूरी है. हमारी क़ानून और व्यवस्था निष्पक्ष और सक्षम होने के बजाय आज अधिक पक्षपाती और ख़ासी सांप्रदायिक हो गई है. आलसी भी, जिसमें लोगों का भरोसा घट रहा है. हमारी न्याय व्यवस्था उच्च स्तरों को छोड़कर ज़मीनी स्तर पर मंदगति, आलसी और पक्षपाती है. हमारी शिक्षा व्यवस्था चरमरा रही है. भारत में ज्ञानोत्पादन, वैज्ञानिक शोध आदि बहुत क्षीण और पिछड़ते हुए हैं.
जाति प्रथा के मजबूत शिकंजे के कारण लोकतंत्र के अनेक लाभ नीचे तक पहुंचने से छेंके जा रहे हैं. राजनीति और धर्म के अपवित्र गठबंधन के कारण धार्मिक संस्थाएं अपार धन इकट्ठा और जमा कर रही हैं और उसके अधिकांश का कोई उत्पादक और सामाजिक उपयोग नहीं होता.
दुर्भाग्य से, हमारे धर्म लोकतंत्र से पिछड़ रहे-गए हैं और वे उसके बुनियादी मूल्यों स्वतंत्रता-समता-न्याय को स्वीकार और उनके अनुसार अपने को बदल और आचरण नहीं कर रहे हैं. ऐसी हालत में अगर बहुत सारा धन बहुत थोड़े हाथों में है तो इसे लेकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए: हमने व्यवस्था ही ऐसी बना ली है.
(लेखक वरिष्ठ साहित्यकार हैं.)