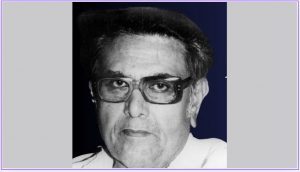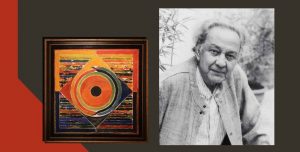सोचती हूं एक कहानी लिखूं. ऐसी कहानी जिसमें मेरा सच तो हो पर मैं न रहूं. मतलब कि मेरा नाम न रहे. दुःख तो पता लगे पर किसका दुःख है वो न पता लगे. दुःख सच भी है या नहीं वो न पता लगे. फिर सोचती हूं कि क्या सारी कहानियां ऐसी ही नहीं होतीं?
इतना सब सोच ही लिया है तो ये सोचने में क्या हर्ज़ है कि मैं इस कहानी में अपना नाम क्यों नहीं चाहती? और जहां चाहती हूं, वहां क्यों चाहती हूं? शायद एक जगह नाम ख़राब होने का डर है और दूसरी जगह नाम ऊंचा होने की संभावना.
मसला ये भी है कि मेरे कुछ कहने से सिर्फ़ मेरा ही नाम नहीं ख़राब होता, चंद लोग जो अपनों में गिने जाते हैं, उनका भी होता है. क्यों न हो भला? उन्होंने तो मेरे साथ बुरा ही किया था उस वक़्त. मन तो ये ही कहता है, पर फिर भी कोई एक हिस्सा है मेरा, जो उन लोगों को भी सुरक्षा देना चाहता है जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया. अगर कोई मुझसे इसका कारण पूछे तो शायद मैं नहीं बता पाऊंगी. शायद वो भी नहीं बता पाएंगे जिनको मेरे न बोलने से फ़ायदा हुआ है. क्योंकि उनको तो ये बात पता ही नहीं कि मैंने नहीं बोला. न ही ये पता है कि मेरे साथ कुछ बुरा हुआ. उन्होंने मुझे न बोलने को कहा ही नहीं था. उन्होंने तो बस उस एक पल में उन्हें जो मज़ेदार लगा था, वो कर दिया.
उनको क्या पता कि वो पल मेरे लिए खिंच कर साल हो गए-चालीस साल-साल खिंच कर डिप्रेशन बन गए, डिप्रेशन खिंच कर नर्वस ब्रेकडाउन बन गया, और अब जब उसका इलाज चल रहा है तो वो पल एक सवाल, एक हाय बन कर बिना चाहे मेरे सामने खड़े हो जाते हैं. जैसे कि मेरा डरा सहमा हुआ शरीर, धीरे-धीरे, कूं-कूं करके, मुझे कुछ बता रहा हो, कोई इशारा दे रहा हो, कोई सोई सी याद जगा रहा हो, इस डर में कि शायद इस बार भी मैं उसे चुप होने को न बोल दूं.
उनको क्या पता कि मेरे दिमाग़ ने ऐसी कितनी ही बातों के बोझ से बचने के लिए मेरी यादों को ही दबा दिया है. और मुझे भी ये बात समझने में सालों लग गए कि फिर भी, मेरे शरीर ने वो सब हमेशा याद भी रखा. जैसे एक बच्चा रूठ कर अपनी मां से बात करना बंद कर देता है, और चाहता है कि मां ख़ुद समझ जाए और मनाने आए, मेरे शरीर ने ठीक वैसा ही किया. जब यादें दबीं, तो मेरे शरीर की महसूस करने की क्षमता भी दब गई, और दबती ही चली गई. और इसका अंजाम ज़्यादातर यही होता है कि अगर एक ख़तरे को अपनी तरफ़ आते देखकर आप डर या ग़ुस्सा नहीं महसूस कर पाते, तो ख़ुद को बचा पाने की संभावना भी अपने आप ही बहुत कम हो जाती है.
मनोविज्ञान भी पुष्टि करता है कि उल्लंघन के शिकार ज़्यादातर वही बच्चे (लड़की और लड़के दोनों) होते हैं, जिनको परिवार में आत्मीय रिश्ते और भरोसे की कमी से गुज़रना पड़ता है. शिशु मन को इस दुख से बचाने के लिए उनका दिमाग़ उनकी महसूस करने की क्षमता को थोड़ा दबा देता है.
और उस स्थिति में शायद वो अपने साथ बुरा हो जाने के बाद भी थोड़े कंफ्यूज्ड ही रहते हैं, कि ये क्या हुआ? क्या ये ग़लत था? इसमें किसकी ग़लती थी? कहीं मेरी तो नहीं थी? क्योंकि मैं तो यूं भी किसी के लिए उतना मायने नहीं रखता/रखती तो शायद मेरी ही ग़लती होगी.
अपनी भावनाओं को महसूस करने की क्षमता, शरीर की संवेदनाओं को महसूस करने की क्षमता ही हमें हमारा सुरक्षित दायरा तय करने में मदद करती है. और अगर उस दायरे की ईंटें कहीं टूटी बिखरी दिखें, तो समझ जाना चाहिए कि कोई, कभी तो जबरन अंदर गया है. उल्लंघन हुआ है. बोल नहीं पाना, महसूस नहीं कर पाना – चाहे पूरे शरीर में या किसी ख़ास हिस्से में, उसी उल्लंघन की निशानियां हैं.
हमारी भावनाओं और संवेदनाओं की उदासीनता युवावस्था में बनने वाले हमारे संबंधों पर भी असर डालती है. संबंधों के लिए ज़रूरी मानसिक और भावनात्मक दायरों को सही से तय नहीं कर पाने का बहुत बड़ा कारण होती है. बचपन में हुए (शारीरिक या मानसिक) उल्लंघन का बीज, किसी पेड़ की तरह आपके अंदर बड़ा होता जाता है. बढ़ती उम्र के साथ डर, घृणा, ग़ुस्सा, कंफ्यूजन, अफ़सोस, दुख, हीनभावना, आत्मविश्वास की कमी, भरोसे की कमी, अकेलापन, और न जाने ऐसे कितने फल-फूलों से लदता जाता है. और हम मजबूरन उस भार को सहन करते-करते एक तरह से आदी भी हो जाते हैं. हमें पता ही नहीं होता कि इसके बिना जीवन कैसा हो सकता था. हमारी भावनाएं, हमारा व्यक्तित्व, हमारे संबंध उस पेड़ की जड़ों से न सींचे गए होते, तो कैसे होते? हमारा होना कैसा महसूस होता हमें, और दूसरों को?
उल्लंघन का रेखाचित्र
ऐसी कितनी ही भूली बिसरी यादों के गट्ठर के बोझ तले शायद हर लड़की ही चलती है, कम से कम हमारे देश में. ऐसा मैं इसलिए कह सकती हूं क्योंकि बहुत सारी लड़कियों ने अपना ऐसा ही गट्ठर मुझसे साझा किया है. किसी का बड़ा, किसी का छोटा, किसी का बेहिसाब बिखरा हुआ, पर आज तक कोई इससे ख़ाली नहीं मिली. नायाब है न ये विरासत! ऐसी विरासत जो बस हम औरतें हँसी के पर्दे के पीछे लेकर चली जा रही हैं, जाने कब से, जाने कब तक.
अब बात उस जगह आ पहुंची है जहां मुझे अपना गट्ठर खोलना ही पड़ेगा. बहुत हो गई प्रस्तावना. पर खोलने से पहले एक बात बता देना ज़रूरी है. आप ऐसा बिल्कुल न समझें कि ये गट्ठर अगर आपसे छुपा है तो मुझे पूरी तरह दिख रहा है. अभी भी इसमें कितनी ही यादें हैं जिनकी पोटलियां बंद हैं. उनमें क्या है, मुझे नहीं पता. हां! जब उम्र छोटी होती है और गट्ठर बड़ा, तो उसके बोझ को कम करने के लिए हमारा दिमाग़ पोटलियां बंद रखने के रास्ते अपनाता है. ताकि कम से कम आप चल सकें, बोल सकें, स्कूल जा सकें, खेल सकें, दोस्त बना सकें, कॉलेज जा सकें, नौकरी कर सकें, शादी कर सकें, बच्चे जन सकें.
आपको शायद अंदाज़ा नहीं होगा कि गट्ठर का भार इतना असहनीय भी हो सकता है कि जीवन के सामान्य काम रुक जाएं. मुझे भी ऐसा ही लगता था जब मैंने नहीं बोलना चुना था. मुझे भी ऐसा ही लगता था जब तक कि पोटलियां बंद होते-होते वो नौबत नहीं आ गई कि मेरे लिए मेरा बचपन लगभग खो सा गया. और मेरी आंखों से आंसू ही आने बंद हो गए. लड़कपन के बाद, गहरे से गहरे दुख से गुज़रते हुए भी मैं कभी रो न सकी. डॉक्टरों ने इसे ‘ड्राई आईज कंडीशन’ कहा जिसके न तो कारण का ठीक से पता है और न ही कोई पक्का इलाज है.
इसलिए इस धुंधले से आईने में मेरी तस्वीर भी धुंधली ही है. घटनाएं भी मेरे शरीर ने मुझे उतनी ही बताई हैं, जितना बर्दाश्त करने की हिम्मत मेरे अंदर अभी है. और वो कितनी है, ये पैमाना शरीर का है, अकेले मेरे दिमाग़ का नहीं. कहते हैं पूरी दुनिया ‘कॉज़ एंड इफ़ेक्ट’ से चलती है, पर मेरी कहानी में इन दोनों का साम्य नहीं बैठता. इफ़ेक्ट देखकर जितनी जानकारी मिलती है, उससे ये तो कहा जा सकता है कि कॉज़ बस एक पल की बात नहीं बल्कि लहर के थपेड़ों की तरह है. और ये थपेड़े सिर्फ़ मेरी ही यादों के नहीं है. सदियों से चले आ रहे थपेड़ों की गूंज भी इसमें शामिल है. Genes की तरह trauma भी पीढ़ी दर पीढ़ी मिलने वाली विरासत जैसा है, ऐसा तो अब मनोवैज्ञानिक भी कहने लगे हैं.
ये सारे असर सिर्फ़ घटना के ठीक बाद ही नहीं दिखाई देते. बल्कि ज़्यादातर लोगों में ये शारीरिक और मानसिक बदलाव धीरे-धीरे उभरते हैं और विक्टिम को ताउम्र उन्हें झेलना पड़ता है. मैं आज भी नहीं बता पाती कि मैं तब क्यों नहीं बोल पाई या आज भी बेनाम बोलना क्यों चुना है.
तो साहब बात शुरू होती है नब्बे के दशक में उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर से. एक तीसरी-चौथी क्लास में पढ़ने वाली बच्ची थी. उसकी एक दोस्त थी जो उसी की क्लास में पढ़ती थी और ठीक बगल वाले घर में रहती थी. दोनों घर इतने करीब थे जितने कि दो दरवाज़े हो सकते हैं. उस दोस्त की छोटी बहन हमसे एक क्लास पीछे पढ़ती थी और हम दोनों का जन्मदिन भी एक ही दिन था. इस बात की मुझे बेहद ख़ुशी होती थी. बहुत ख़ास सा महसूस होता था ये सोच कर कि ऐसा किसके साथ होता होगा भला! हम तीनों साथ स्कूल जाते थे और साथ ही आते थे.
गर्मी की छुट्टियां थीं. मेरी दोस्त की मम्मी दोनों बेटियों को लेकर अपने मायके चली जाया करती थीं. अंकल दोपहर में घर में अकेले रहते थे. इसके बाद का वो अंश मुझे याद नहीं कि एक दोपहर मैं कैसे उनके घर में, उनके बेडरूम में पहुंच गई. मुझे जो दिख पाता है वो बस यह कि मैंने अंकल के बेड पर अपने आप को नीचे और उनको अपने ऊपर महसूस किया. उनका भार ज़्यादा था. और उसके कुछ देर बाद मुझे लगा कि मुझे सुसु करने जाना है. मैं बाथरूम भी गई पर सुसु हुई नहीं और एक जलन सी महसूस हुई अंदर. पर उस वक्त मेरे अंदर कोई ग़ुस्सा नहीं था, उलझन थी. ‘सुसु नहीं हो रही’, यह मैंने अंकल को ही जाकर पहले बताया था. ये जलन चली जाए मुझे बस उतना ही चाहिए था. उसके बाद के अंश भी मुझे याद नहीं कि मैं कब घर आई, मैंने अपने घर में क्या किया, क्या बताया, क्यों नहीं बताया. सिर्फ़ धुंध है उस जगह. ये भी नहीं पता कि ये घटना मेरे साथ कितनी बार हुई. पर 2 बार की धुंधली याद तो है. इस घटना का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है और उल्लंघन के घाव का शुरू होता है.
दूसरी घटना उस रात की है जब सरकारी कॉलोनी के हमारे दो कमरे के घर में कुछ ज़्यादा मेहमान आ गए थे. सारी जगह भर गई तो किसी चाचा या मामा (यहां भी धुंध है) के साथ मुझे फोल्डिंग खटिए में सुला दिया गया. मैं थोड़ी बड़ी बच्ची थी तब, मेरा भाई मुझसे छोटा था इसलिए उसे रात में मां की ज़रूरत पड़ सकती थी. मैं ख़ुशी-ख़ुशी सोने चली गई अपने रिश्तेदार के साथ. आधी रात के बाद अचानक मेरी नींद खुली और कुछ ठोस डंडे की तरह महसूस हुआ पीछे. मैंने मुड़ कर देखा तो मामा/चाचा सोए हुए थे. मुझे समझ नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ, पर मुझे अच्छा महसूस नहीं हुआ. मैं शायद वापस सो भी नहीं पाई. पर मैं उस खटिए से उठ कर अपनी मां के पास भी नहीं जा पाई.
आज भी जब मैं ये सवाल ख़ुद से करती हूं कि मैं ग़लत महसूस करते हुए भी ख़ुद को उस जगह से हटा क्यों नहीं पाई, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है. मुझे किसी ने बांधा नहीं था. पर क्या ये कहना सही में सच है? अपनी भावनाओं को ठीक से नहीं महसूस कर पाना एक तरह का अपराध-बोध भी तो देता है कि कोई अटपटा क़दम उठा कर आप कहीं बड़ी ग़लती तो नहीं कर बैठेंगे? किसी ने पूछ दिया तो आप क्या बोलेंगे जब आपको ही ठीक से पता न हो?
तीसरी घटना पांचवी-छठी क्लास की है. फिर से एक दोस्त ही के घर की कहानी, जो मेरी क्लास में पढ़ती थी. और उसका बड़ा भाई उसी स्कूल में ग्यारहवीं में पढ़ता था. वो बड़ा ही शांत किस्म का, ज़्यादा बात न करने वाला इन्सान था. ज़ाहिर है मैं उससे बात नहीं करती थी और उसे भैया बुलाती थी. एक शाम मैं अपनी दोस्त को खेल के लिए बुलाने उसके घर गई हुई थी. मेरी दोस्त को तैयार होने में ज़रा वक्त लग रहा था. मैं दो कमरों को जोड़ने वाली बीच की संकरी गली में खड़ी इंतजार कर रही थी. तभी वो भैया उस गली में से, मेरे बहुत क़रीब से गुज़रे. इतने कि फ़िर से कुछ डंडे जैसा महसूस हो गया मुझे. बुरा तो लगा पर फिर भी वहां से भाग जाने की हिम्मत नहीं हुई. लगा मेरी दोस्त पता नहीं क्या सोचेगी? उसके भाई के बारे में मैं क्या कहूं? अगर आज उस क्षण में वापस जाकर भी सोचती हूं तो समझ नहीं आता कि अगर बोलने की हिम्मत होती भी, तो मैं क्या कहती? इस बात को किस तरह कहा जा सकता है, मुझे तो बहुत बाद तक भी नहीं पता था.
चौथी घटना नवीं क्लास की है जब मेरी एक कज़न बहन की शादी हुई थी. कुछ ही महीने हुए थे और वो बहुत रोमांटिक मिज़ाज में अपने पति को लेकर हमारे घर आई थी. उनके पति पहली बार हमारे घर आए थे. ‘साली आधी-घरवाली’ वाला मज़ाक चल ही रहा था, जिसका सही मतलब क्या होता है, मुझे आज तक नहीं पता. जब दोनों के विदा लेने का वक्त हुआ तो जीजाजी ने अपना बायां हाथ मेरी दीदी के कंधे पर डाला हुआ था और दायां मेरे. मैं छोटी थी इसलिए उनकी हथेलियां ठीक मेरे स्तन के पास लटक रही थीं. बस दरवाज़े से निकलने के ठीक पहले उन्होंने मेरे स्तन को स्पंज की तरह दबा दिया और चलते बने. मैं दंग रह गई. आपसी रिश्तों का सोचकर फिर से कुछ नहीं कह पाई किसी को. पर उसके बाद जीजाजी से हमेशा बहुत संभल कर रही.
लेकिन रिश्ते निभाने का भार किसी ने मुझे क्लास में समझा कर तो दिया नहीं था? ये कैसे आ गया अपने आप? और न ही सिर्फ़ मेरे ऊपर, बल्कि मेरी बहुत सारी दोस्तों को भी यही भार इसी तरह कैसे महसूस हुआ? क्या ये सोच भी विरासत में मिली थी?
अतीत देता था भविष्य को चेतावनी
यहां यह बताना भी बहुत ज़रूरी है कि हाई स्कूल में जाने के बाद मेरी मां ने एक दिन मुझे बुला कर अलग से कहा था कि बेटा अगर कभी भी कोई तुम्हारे साथ ग़लत करे या छुए भी, तो तुमको सामने जो भी मिले वो उठा कर मार देना. वो इंसान मर भी जाए, तो भी मैं तुमसे सवाल नहीं पूछूंगी. उसके बाद क्या करना है, वो ज़िम्मा मेरा है. मेरी मां के इन शब्दों में, मुझपर भरोसे के साथ डर और सुरक्षा का मिला-जुला भाव मुझे उस दिन बहुत अच्छा लगा था. पर वो ख़ुशी कभी इतनी हिम्मत नहीं दे पाई कि इसके बाद भी मेरे साथ जो हुआ, वो कभी मैं अपनी मां को जाकर बता सकूं. मैं अपने मन में अपनी मां को दुःख से बचा रही थी. पर इस बात को समझने में मुझे बहुत साल लगे कि मां का वो सुरक्षा भाव एक भुक्तभोगी की कराह ही थी. वो एक मां का बेटी को दिए गए वचन से ज़्यादा, एक भविष्य को अतीत के द्वारा दी जाने वाली चेतावनी थी.
पांचवीं घटना, जब मैं अपने शहर से दूर के एक कॉलेज में पढ़ रही थी. पहले जैसी डरी सहमी हुई भी नहीं थी, न ही कंफ्यूज्ड थी. ख़ुद बस-ट्रेन से कॉलेज आती-जाती थी. मेरे घर मेरे एक और मामा आए हुए थे. मेरा किसी से झगड़ा हुआ था. जब मामा जाने को हुए, मैं, मेरी मां, मेरा भाई, मेरी बहन, हम सब मामा को छोड़ने घर से बाहर सड़क तक निकले. मामा ने मुझे सांत्वना देने के लिए गले लगाया, और अचानक मुझे महसूस हुआ कि उस वक्त (न कभी उसके पहले, न कभी उसके बाद) मैं उनके लिए उनकी भांजी नहीं, बस एक लड़की थी. मुझे सांत्वना की आड़ में उस एक पल की छुअन थी, जो मुझे अच्छी नहीं लगी. और उस पल ये पता होने के बाद भी कि क्या हुआ, बोलने की हिम्मत होने के बावजूद भी, मैं कुछ नहीं बोल पाई.
उस एक पल को मैं क्या बोलूं, इंसान की बदनीयती या कमज़ोरी? उस एक पल के लिए क्या मैं अपनी मां को उसके भाई से अलग कर देती? मेरा तो पहले ही बहुत नुकसान हुआ पड़ा है. एक और सही. ये तो छोटा भी है. उस वक्त मेरे दिमाग़ में यही बात आई और मैंने रहने दिया.
लौटकर आता रहा घाव कि एक दिन….
छठी घटना तो छह सौवीं घटना भी कही जा सकती है. क्योंकि वो आपके साथ रोड पर, ट्रेन में, बस में, सिनेमाघर में, या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर किसी भी अनजान द्वारा की जा सकती है या की गई है. पीछे से टोकना, साइकिल से छू कर जाना, कुछ अश्लील बोल कर चले जाना, घूरना, पीछा करना, इसका तो कोई अंत ही नहीं है. ख़ासकर अगर आप उत्तर भारत के किसी प्रांत की निवासिनी हों. ये सांस लेने की तरह ही आम बात हुआ करती थी 90 के दशक में, और शायद आज भी है.
मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं ऐसी कोई आवाज पीछे से आती हुई सुनती थी, तो मेरे शरीर में कितनी घृणा और गुस्सा भर उठता था. शुरू में ये ग़ुस्सा उस इंसान की तरफ़ होता था. मैं सोचती थी कुछ उठा कर फेंक दूंगी. पर मैं ये कभी कर नहीं पाई. धीरे-धीरे मेरा यह ग़ुस्सा मेरी तरफ़ मुड़ने लगा. जो उस पल के दिनों-महीनों बाद तक मेरे दिमाग़ में घूमता रहता था. मुझे कोसता रहता था. अगली बार मैं कैसे बेहतर करूँगी (जो कि कभी नहीं हुआ) उसके प्लान बनाता रहता था.
सातवीं घटना, मैं कॉलेज के बाद दिल्ली में नौकरी कर रही थी. दिल्ली की बसें इस मामले में बहुत बदनाम हैं. वहां के मर्द अक्सर बस में डंडे के साथ पाए जाते हैं. इसलिए वो बस में आपके पीछे चिपकते भी हैं. अथाह भीड़ का होना उनका कवच बनता है. एक दिन ऐसे ही एक बस में मैं खड़ी सफ़र कर रही थी. पीछे की तरफ़ से एक डंडे के अहसास ने मेरे अंदर आग-सी लगा दी. ख़ुद पर ग़ुस्से का आलम था कि अगर आज कुछ नहीं किया तो ख़ुद को कोड़े से मारूंगी मैं घर जाकर. मैंने फैसला लिया कि कुछ तो करना ही है. चाहे छोटा ही क्यों न हो. मैंने चाकू, सूई या ब्लेड जैसी कोई तीखी चीज बैग में तलाशने की कोशिश की, पर कुछ नहीं मिला. मेरी हरकत से शायद वो आदमी सतर्क हो गया और मुझसे आगे निकल गया. मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई पर डंडे का महसूस होना बंद हो गया था. मैंने सोचा कि वो जहां उतरेगा, मैं वहीं उतर जाऊंगी. बस रुकी, वो उतरा, मैं ठीक उसके पीछे उतरी. मैंने अपने मुंह में ढेर सारा थूक भर कर रखा था. मैं उसके आगे गई और उसके मुंह की तरफ़ थूकने की कोशिश की. वो मुझसे बहुत लंबा था. फिर भी कुछ छींटे तो पहुंचे ही उसके चेहरे तक. पर उसके बाद उसके चेहरे पर बहुत विचित्र-सा भाव आया. मुझे धक्का लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वो आदमी हो ही न जो मेरी हद का उल्लंघन कर रहा था? और अचानक से मेरा सारा ग़ुस्सा अपराध बोध में बदल गया. कहीं मैंने किसी निर्दोष के साथ तो ऐसा नहीं कर दिया? आज भी मैं उस घटना को सोचती हूं तो मुझे अपराध भाव महसूस होता है. जब भी मेरा उल्लंघन हुआ, तब मैं भी निर्दोष ही थी, पर यह अहसास कभी उस अपराध भाव पर हावी नहीं हो पाता.
पर अब कहीं न कहीं सुकून भी महसूस होता है कि ख़ुद अपनी प्रहरी होने की तरफ़ मैं पहला क़दम तो उठा पाई. ख़ुद को सवाल करते-करते, सवाल के दायरे में वो लोग भी तो आए जिनके चेहरे हैं भी और नहीं भी. पर जिनका कृत्य मेरे अस्तित्व को झंझोड़ कर चला गया और मैं देखती रह गई. और मेरे अलावा मेरे आस-पास किसी को भी वो बात पता तक नहीं लगी.
क्या बोलने का काम सिर्फ़ ज़बान करती है? क्या शरीर की, भंगिमाओं की भाषा नहीं दिखाई देनी चाहिए? क्या इस देखे जाने से औरतें ही ज्यादा वंचित नहीं? क्या एक समाज की तरह हम कुछ चीज़ों को देखना और महसूस करना भूल गए हैं? क्या देख पाना, महसूस करना, और ख़ुद की सुरक्षा कर पाना, ये सब एक बच्ची की ज़िम्मेदारी है? क्या उस बच्ची को इतना कुछ कर पाने के काबिल बनाता है हमारा समाज और परिवार? सवाल बहुत सारे हैं और जवाब बहुत कम. पर शायद सवाल का होना, पूछा जाना, लिखा जाना, सुना जाना, समझा जाना, साझा किया जाना ही जवाब हो. ऐसी एक उम्मीद अभी भी बाक़ी है.
*****
(लेखिका अज्ञात रहना चाहती हैं.)