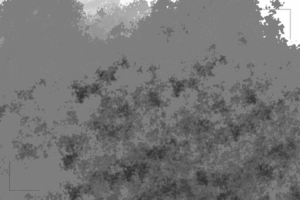सुकरात के शिष्य एंटीस्थेनीज़ से यह पूछे जाने पर कि मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है, उन्होंने उत्तर दिया, ‘खुशी खुशी मरना.’
27 दिसंबर 1797 को आगरा में पैदा हुए मिर्ज़ा असदुल्लाह खान ग़ालिब के बारे में यह कहना बड़ा मुश्किल है कि जिंदगी के आखिरी दिनों में अपने दौर का सबसे जिंदादिल कहे जाने वाले शायर ने भरपूर खुशी से इस दुनिया को अलविदा कहा हो. वे इस नश्वर दुनिया के फलसफे से बखूबी परिचित थे.
‘मौत से पहले आदमी ग़म से निजात पाए क्यों’, सो ग़म थे कि ग़ालिब को बख्शने को तैयार न थे. 1867 के एक खत में उन्होंने लिखा. ‘मैं अहाते में सोता हूं. सुबह-सुबह दो आदमी मुझे हाथों पर उठाते हैं. एक अंधेरी कोठरी है, उसमें डाल देते हैं और दिन भर अंधेरे कोने में पड़ा रहता हूं. शाम को फिर दो आदमी मुझे उठाते हैं और आंगन में पलंग पर लाकर डाल देते हैं.’
ग़ालिब क्या सोचते रहते होंगे? जीवन के आखिरी क्षणों में कभी व्यर्थता बोध और कभी कुछ न कर पाने का मलाल उन्हें कचोटता होगा. जवानी से लबरेज अपने दिनों में यह खुद ग़ालिब की अपनी दलील थी,
‘जब आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है,’ अब ग़ालिब यह महसूस करते कि ‘खूं हो के जिगर आंख से टपका नहीं ऐ मर्ग, रहने दो अभी यां कि अभी काम बहुत है.’
क्या ग़ालिब मर्ग से डर गए थे! वो ग़ालिब जो अक्सर तन्हाई में गुनगुनाते कि ‘मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद रात भर क्यों नहीं आती.’ अधूरी ख्वाहिशों ने ग़ालिब को एहतियात बरतने पर मजबूर कर दिया था.
फिर वज़’-ए-एहतियात से रुकने लगा है दम,
बरसों हुए हैं चाक गरेबां किए हुए
1867 से 1869 के मध्य में मिर्ज़ा ग़ालिब ने रामपुर के नवाब को कई खत लिखे. वह अपना कर्ज चुका कर मरना चाहते थे. 17 नवंबर 1868 को ग़ालिब ने बहुत व्याकुलता से रामपुर के नवाब को लिखा, ‘मेरी हालत बद से बदतर हो गई है.आपके दिए हुए 100 रुपये के वजीफे में से मेरे पास बस 54 रुपये बचे हैं, जबकि मुझे अपनी इज्जत को बचाए रखने के लिए करीब 800 रुपयों की जरूरत है.’
ग़ालिब ने अपनी मौत से तीन महीने पहले ये खत लिखा था. वह लिए हुए कर्ज के साथ मरना नहीं चाहते थे. उन जैसे कुलीन के लिए इस हालत में मरना बड़ी बे-ग़ैरती की बात थी.
10 जनवरी 1869 को अपनी मौत से करीब एक महीने पहले अपनी अंधेरी सीलन भरी कोठरी से नवाब को आखिरी बार लिखा, ‘हुज़ूर,परवरदिगार ने मुझे तबाही के पास लाकर खड़ा कर दिया है. मैं बस आपको फिर से याद दिलाने का फर्ज अदा कर रहा हूं, बाकी हुजूर की मर्जी.’
यह ग़ालिब का आखिरी खत था, जिसके जवाब में नवाब रामपुर ने सिर्फ तयशुदा 100 रुपये का वजीफा भेजा. यह ग़ालिब को 15 फरवरी को मिला. उनकी मौत से ठीक एक घंटा पहले. ग़ालिब आखिरी सफ़र के लिए तैयार थे.
दम-ए-वापसीं बर-सर-राह है
अज़ीज़ो अब अल्लाह ही अल्लाह है
ग़ालिब की ‘दम-ए-वापसीं’ ठीक वैसी थी जो एक साधारण से मनुष्य की होती है. अपनी तमाम गरीबी और माली मुश्किलातों के साथ वह कुलीनता के परिवेश में भले ही जिए. वह उस में रहते-रहते अचानक उसे तोड़कर बाहर निकल आते थे.
मशहूर उर्दू आलोचक हाली, जो ग़ालिब के शागिर्द थे, के मुताबिक ग़ालिब पालकी के बिना घर से नहीं निकलते थे. दिल्ली कॉलेज (अब ज़ाकिर हुसैन कॉलेज) में फारसी के प्रोफेसर पद को ठुकरा चुके थे क्योंकि इस पद के लिए साक्षात्कार लेने वाला अंग्रेज उनकी अगवानी के लिए बाहर नहीं आया था. जो ग़ालिब के मुताबिक एक शिष्टाचार था, जिसका उसे पालन करना चाहिए था.
ग़ालिब की यह कुलीन शख्सियत उनके दौर ने गढ़ी थी लेकिन ग़ालिब के मानवतावादी नजरिये पर यह कुलीनता कभी हावी नहीं हुई. भाव और परिवेश की इस भिड़ंत ने ही ग़ालिब को एक महान शायर में बदला था. वह पेंशन के लिये अंग्रेज़ों के चक्कर लगाते. विक्टोरिया रानी के लिए कसीदे लिखकर गवर्नर जनरल को भेंट करते और दोस्तों को खत में लिखते कि ‘गवर्न्मेंट का भाट था. भटई करता था. खिलअत पाता था.’
ग़ालिब जानते थे कि घर-गृहस्थी चलाने और ऊपरी हैसियत बनाने के लिए ‘शह का मुसाहिब’ होना जरुरी था. खुद मुगल दरबार का शाही शायर बनना ग़ालिब की हसरत थी और इसी बात पर चिढ़कर अपने हमवक्त शायर ज़ौक़ पर उन्होंने तंज कसा था
‘हुआ है शह का मुसाहिब फिरे है इतराता
वरना इस शहर में ग़ालिब की आबरू क्या है’
ग़ालिब का अपने शहर से एक ख़ास रिश्ता था. दिल्ली उनकी धड़कनों में बसती थी. यहां उन्होंने इज्जत भी पाई थी, रुसवाइयां भी. जुआ खेलने के अपने शौक के चलते जब शहर कोतवाल ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा और उन्हें छह महीने की जेल हुई, तो ग़ालिब को बड़ा धक्का पहुंचा.
‘रहिये अब ऐसी जगह चलकर जहां कोई न हो
हम-सुखन कोई न हो और हमजुबां कोई न हो’
वह कई बार विचलित हुए. गुरबत पीछा छोड़ने को राजी न थी और वह दिल्ली को. नतीजा- एक गहरा मलाल,
‘गर मुसीबत थी तो ग़ुरबत में उठा लेता,असद
मेरी दिल्ली में ही होनी थी ये ख़्वारी हाय हाय’
बरसात का मौसम आते ही दिल्ली उन्हें कसकर पकड़ लेती.
‘सरे आग़ाज़े मौसम में अंधे हैं हम
कि दिल्ली को छोड़ें, लोहारू को जाएं.’
और इसलिए जब उनकी आंखों के सामने दिल्ली बिखरने लगी तो ग़ालिब भी ‘तिमसालदार आईने’ की तरह टूटने लगे.
1857 की बगावत के बाद अपने एक दोस्त के खत में यह पूछे जाने पर कि दिल्ली के क्या हाल हैं, ग़ालिब ने बड़े उदास लहजे में खत में जवाब लिखा, ‘पांच चीजों से दिल्ली, दिल्ली थी. किला, चांदनी चौक, जामा मस्जिद के भीड़भाड़ वाले बाजार,जमुना पुल पर हर हफ्ते की सैर और फूल वालों का सालाना मेला. इनमें से कुछ भी नहीं बचा. फिर दिल्ली कैसे बची रहती. हां, कभी इस नाम का एक शहर हुआ करता था.’
दिल्ली में हाकिम बदल गए थे. नए हाकिम ‘अपनी दिल्ली’ अपनी तरह से रच रहे थे. पुरानी सड़कें, इमारतें तोड़ी जा रहीं थीं. शहर के साथ ग़ालिब भी टूटे जा रहे थे.
इसी खत में उन्होंने झल्लाकर आगे लिखा, ‘आकर देखो, निसार खान छत्ता से नई सड़क निकाल दी गई है. खान चंद गली से भी एक नई सड़क निकली है. बुलाकी बेगम वाली गली को तोड़ा जा रहा है.’ यह जितना एक शहर का टूटना था, उतना ही एक शायर का टूटना.
‘अब मैं हूं और मातम-ए-यक शहर-ए-आरज़ू
तोड़ा जो तूने आईना तिमसालदार था’
बगावत के बाद के दिनों में ब्रिटिश दिल्ली पर नियंत्रण कर लेने के बाद दिल्ली को इस तरह बदल देना चाहते थे कि एक ओर उसकी पुराने प्रतीकों को या तो ध्वस्त कर दिया जाय या उनकी सूरत को बदल दिया जाए, ग़ालिब के लिए यह एक सदमे जैसा था.
दिल्ली और लाहौर दरवाजों के नाम बदल दिए गए. फतेहपुरी मस्जिद को निजी संपत्ति के रूप में बेच दिया गया. कई सारी इमारतों को सिपाहियों की बैरकों में बदल दिया गया. चारों तरफ़ बदहवासी का माहौल था.
क्रांतिकारियों से ताल्लुक होने के जरा से संदेह पर अंग्रेज किसी को भी पकड़कर फांसी पर लटका देते. 1858 के एक खत में ग़ालिब ने लिखा, ‘अफसर अपनी मर्जी से जो चाहे करते हैं. न कोई कायदा है, न कानून.’ एक अराजक शहर का तसव्वुर ग़ालिब ने इस तरह बयान किया,
‘रोज इस शहर में एक हुक्म नया होता है
कुछ समझ में नहीं आता कि क्या होता है’
ग़ालिब की संवेदनाओं में ताउम्र बेबसी झलकती रहती थी. अपने एक खत में उन्होंने लिखा था, ‘ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा मैंने नाक़ाबिल लोगों के क़सीदे लिखने में ज़ाया कर दिया.’ मृत्यु की घनीभूत वेदना ने इस मलाल और गहन कर दिया था. उन्हें लगता था कि उनकी प्रतिभा को समाज ने कभी वाजिब हक नहीं दिया.
13 फरवरी 1865 के खत में उन्होंने अलाई को लिखा, ‘मैंने खुद लिखा, अपने लिखे को ख़ुद ही सराहा. मुझे ख़ुदा ने इतना न दिया, वरना मेरी आरज़ू थी कि मैं इस तमाम दुनिया की मेहमान नवाजी करता और अगर इस पूरी दुनिया को कुछ न खिला-पिला पाता, तो कम से कम इस शहर में तो कोई भूखा नंगा न रहता.’
यह ग़ालिब का अपने शहर से इश्क था और यह इश्क कभी तंजकशी के रूप में था और कभी वाहवाही के रूप में. यह जानते हुए कि वह शाह के ‘वज़ीफ़ाखोर’ थे. अपनी रौ में आकर वह यह भी कह सकते थे,
‘बादशाही का जहां ये हाल हो ग़ालिब तो फिर
क्यों न दिल्ली में हर एक नाचीज़ नवाबी करे’
या फिर दिल्ली का वह रूप जहां रोजी-रोटी और रोजगार दोनों एक बड़े सवाल थे,
‘है अब इस मामूरे में क़हत-ए-ग़म-ए-उल्फ़त ‘असद’
हम ने ये माना कि दिल्ली में रहें खावेंगे क्या’
‘खावेंगे क्या’… ग़ालिब शहर में होने के हर पहलू से रूबरू करा रहे थे और फिर आखिर में शहर की अंधेरी सीलनभरी कोठरी में शून्य में निहारते, बुदबुदाते निश्चेष्ट पड़े अपने समय को आंक रहे थे. महाप्राण निराला की तरह…
‘लीला का संवरण-समय फूलों का जैसे
फलों फले या झरे अफल, पातों के ऊपर
सिद्ध योगियों जैसे या साधारण मानव,
ताक रहा है भीष्म शरों की कठिन सेज पर’
हाली ने लिखा, ‘ग़ालिब के जनाजे में बड़े सम्मानित लोग आए. सैयद सफदर सुल्तान साहब चुपचाप से आगे बढ़े. नवाब जियाउद्दीन साहब से कान में कहा, मिर्ज़ा साहब शिया थे, आपकी इजाज़त हो तो आखिरी रस्म हम अपनी तरह से कर लें.’ नवाब साहब चुप रहे और नवाब असदुल्लाह खान ग़ालिब उर्फ मिर्ज़ा नौशा को सुन्नी तरीके से दफ़ना दिया गया.’
ये और बात है कि ग़ालिब जो थे वो सिर्फ़ ग़ालिब थे, जिन्हें यक़ीन था कि दुनिया में ‘होना’ या ‘न होना’ वजूद के एहसास की नुमाइंदगी है और जब तक वह है उसे ‘आंख से लहू टपका कर’ ख़ुद को ज़ाहिर करना चाहिए. ग़ालिब भले खुशी-खुशी न मरे हों, वह जिए जिंदादिली से.
(लेखक भारतीय पुलिस सेवा में उत्तर प्रदेश कैडर के अधिकारी हैं.)