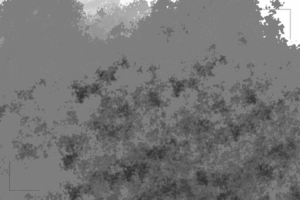पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के अभिजात्य और शासक वर्गों में पर्यावरण और सामाजिक-नागरिक प्रतिरोध के केंद्र के रूप में सघन वन्य इलाक़ों को नकारात्मक रूप से देखने की प्रवृत्ति मिलती है.

16 फरवरी 1519 को ज़हीरुद्दीन मुहम्मद बाबर जब पहली बार बजौरा से आगे चलकर सिंधु नदी पार करके भीरा में उतरा तो उसके सामने जंग के लिए दुश्मनों का कोई लश्कर न था.
सामने सिंधु नदी के किनारे-किनारे घने जंगल फैले हुए थे. उसकी कश्ती घाट के किनारे आकर जहां रुकी वो जगह बाबर के अपने अल्फ़ाज़ों में ‘क़र्ग़-खाना’ थी.
क़र्ग़-खाना; अर्थात गैंडों का घर और जिस कुमुक ने बाबर को पहला मुक़ाबला पेश किया उसमें महज़ तीन ही सिपाही थे. एक मां और उसके दो नन्हें शावक.
ज़िंदगी में होने वाले तजुर्बों को रोज़ डायरी में दर्ज करने वाले शख़्स बाबर ने इस तज़ुर्बे को भी इन अल्फ़ाज़ों में दर्ज किया:
‘जंगल में आग लगा दी गई लेकिन वह गैंडा न मिला. एक बच्चे को तीरों से वेध दिया गया. दूसरा आग में जल चुका था. वह हांफ रहा था और मरने के क़रीब था.’
बाबर इस भीमकाय वन्य पशु को देखकर हैरान था. लेकिन ऐसा करने वाला वह पहला व्यक्ति न था. वर्ष 1330 में, जब इब्न-बतूता अपना ‘चर्र-मर्र’ करता हुआ जूता पहने मुल्तान के पास से हिंदुस्तान में दाख़िल हुआ तो उसे भी इस जानवर को देखने का मौका मिला.
वह भी हैरान था लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के आज के ज़िले बहराइच तक पहुंचते-पहुंचते उसकी हैरानी ख़त्म हो चुकी थी. पूरा उत्तर भारत ही जैसे ‘क़र्ग़-खाना’ हो.
बाबर लिखता है कि सरयू नदी के किनारे वो बड़ी तादाद में टहलते थे. अलबरूनी (1030) के मुताबिक़ पूरी गंगा घाटी कर्ग़ (गैंडा) से आबाद थी. जो वन्य जीव आज उत्तर-पूर्व के काज़ीरंगा और मानस के जंगलों में अपना वजूद बचाए रखने के लिए लहूलुहान सा जूझ रहा है, 1398 में तैमूर ने जब कश्मीर की सरहदों पर उसे देखा तो शिकार खेलने के आकर्षण से स्वयं को रोक न सका. (Shivani Bose- From Eminence to Near Extinction, Page 78/79, Shifting Grounds. Oxford University Press)
अबुल फ़ज़ल ने उन्हें आज के संभल परगने में देखा था. आईन-ए-अकबरी में दर्ज इस जानवर का इस इलाक़े से वजूद पाए जाने का यह शायद अंतिम उल्लेख था.
सिर्फ़ दो दहाई वर्षों बाद जब जहांगीर ने यहां कमरगाह (मुग़लकाल में घेरा बनाकर शिकार खेलने की पद्धति) से शिकार खेला तो उसकी तुज़ुक-ए-जहांगीरी के पन्नों पर कोई क़र्ग़ (गैंडा) मौजूद न था.
17वीं सदी की शुरुआत से ही उन सभी इलाक़ों से जहां बाबर और उसके कुछ वंशजों ने इस जानवर को देखा था, वह विलुप्त हो चुके थे. सरयू के पास की रेत पर वह अब टहलने को नहीं बचे थे. (देखें: इरफ़ान हबीब: भारत का पारिस्थितिकीय इतिहास, पेज संख्या 113, राजकमल 2015)

अपना अस्तित्व बचाए रखने की कितनी ही लड़ाइयां एक साथ लड़ी जा रहीं थी. इस संघर्ष के एक सिरे पर आदमी था और दूसरे पर प्रकृति और ठीक मध्य में सत्ता.
सत्ता दोनों से जिस रिश्ते के ज़रिये जुड़ती थी वह रिश्ता था- ताक़त का निर्मम प्रयोग. ताक़त दोनों को कुचलती थी. प्रकृति को भी, मनुष्य को भी. पर्यावरण को यह छूट कभी हासिल नहीं रही कि वह किसी हुक़ूमत की राह का रोड़ा बने.
आज गुजरात के गिरि के वनों तक महदूद रह जाने वाले एशियाटिक शेर (Panthera Leo Persica) कभी पूरे उत्तर भारत के घास के मैदानों में मनुष्य के साथ-साथ इस ज़मीन को आपस में बांटे हुए विचरते थे.
ब्रिटिश कूटनीतिज्ञ सर थॉमस रो को 1617 में मांडू ज़िले में जहांगीर से एक शेर को मारने की अनुमति लेनी पड़ी थी. बादशाह और उसके परिवार को छोड़कर ‘बड़े शिकार’ को मारना एक गंभीर अपराध था जिसकी सज़ा मृत्युदंड थी.
फ्रांसीसी दार्शनिक और इतिहासकार बर्नियर के कहे अनुसार, एक साधारण व्यक्तियों को छोटे हिरणों, नीलगाय, पैट्रिज, तमाम तरह के क़्वेल और अन्य पक्षियों का शिकार करने की छूट थी.
जहांगीरनामा से पता चलता है कि जहांगीर अपने किए सभी शिकारों का पूरा तथ्यात्मक ब्योरा रखता था. उसके अपने कथनानुसार 39 सालों में सभी प्रकार के वन्य जीव और पक्षी मिलाकर उसने 28,532 शिकार किए जिसमें से 86 शेर थे.
वर्ष 1623 में उसने आगरा के रहीमाबाद में जिस शेर का शिकार किया वह उसके जीवन का सबसे बड़ा शिकार था. (जहांगीरनामा, अनु.थेकसन, पेज संख्या 411)
इस कल्पना से ही मन कैसा सुखद रोमांच से भर जाता है कि कचरे, धुंए, धूल और शोर से बेहाल आज का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर कहा जाने वाला इलाक़ा तब प्राकृतिक रूप से कितना विविधतापूर्ण रहा होगा!
1562 में मथुरा से गुज़रते हुए अकबर का सामना शेरों के एक बड़े झुंड (प्राइड) से हुआ जिसमें सात शेर थे. इनमें से एक को ज़िंदा पकड़ लिया गया और शेष को शिकार के रूप में मार दिया गया.

इसी तरह हरियाणा में जहां से आज घने वन क्षेत्र विलुप्त हो चुके हैं, जहांगीर ने 1608 में करनाल और पानीपत के बीच में शेरों के एक जोड़े का शिकार किया.
1857 के बाद उत्तर भारत के मैदानों में इस जानवर के देखे जाने का कोई साक्ष्य नहीं मिलता.अब तक इस देश के शक्ति पटल पर नए शासकों का प्रवेश हो चुका था. वो नए हथियारों से लैस थे. एक ज़मीन का स्पेस कई तरह की प्रजातियां आपस में बांट कर एक सह-जीवन में साथ-साथ रह सकती हैं. ये विचार उनके लिए अटपटा सा था.
विस्तारवाद ही नया दर्शन था. वनों को उजाड़ने और वन्य-जीवन का अंधाधुंध विनाश उनका शौक़ था. 1820 के आसपास के वर्षों में एक अंग्रेज़ अधिकारी विलियम फ़्रेज़र ने अकेले 84 शेरों को गोली मारी.
कहा जाता है कि पंजाब और हरियाणा के इलाक़ों से इस जानवर को विलुप्त कर देने के लिए ‘वह अकेला ज़िम्मेदार था’. 1850 के दशक में कर्नल जॉर्ज ऑक्लेंड स्मिथ ने लगभग 300 शेर मारे जिसमें से 50 अकेले दिल्ली की जमुना नदी और आसपास के इलाक़ों से थे.
इसी समय के आसपास बूंदी के राजा बिशन सिंह ने कोटा के जंगलों से 100 शेर मारे. 1880 तक वह यहां से पूरी तरह ख़त्म होकर कुछ सैकड़ा की तादाद में सिर्फ़ काठियाबाड़ में बचे थे जो कुछ संजीदा लोगों और संवेदनशील सरकारी प्रयासों अब तक बचे रह गए हैं. (Lions, Cheetahs and Others in Mughal Landscape; Page-94 Divyavhanu Singh, Quoted In Shifting Grounds. Oxford Press)
लेकिन एशियाटिक चीता इस मामले में अपने पारिवारिक वंशज की बनिस्बत बदकिस्मत था. मुग़ल बादशाहों को घास के मैदानों के इस जानवर से बहुत लगाव था. शेरों और बाघों के विपरीत, वे उसके जीवित पकड़े जाने को प्राथमिकता देते थे.
उसे प्रशिक्षित किया जाता था. फिर मनोरंजन के तौर पर उसकी मदद से छोटा शिकार पकड़वाया जाता. अकबर उनका दीवाना था. जहांगीर की आत्मकथा से पता चलता है कि उसके पास लगभग 3,000 प्रशिक्षित चीते थे.
औरंगज़ेब के समय में आए एक विदेशी यात्री जीन थेवनोट के मुताबिक़, चीतों पर ‘राज्य का एकाधिकार’ था. राज्य की इज़ाज़त के बिना उन्हें कोई नहीं पकड़ सकता था.
चीते आज के राजस्थान के झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, मेड़ता के इलाक़ों और उत्तर प्रदेश में इटावा के पास चंबल नदी के पास से पकड़े जाते थे. बिहार से लेकर गुजरात तक के मैदानों में ये बड़ी तादाद में मिलते थे.

मुग़ल साम्राज्य के पतन के बाद घास के मैदानों से वो तेजी से विलुप्त हुए और 1947 में जिस साल हमारे देश को आज़ादी मिली, उसी वर्ष जंगल में पाया जाने वाला आख़िरी चीता मार दिया गया.
हिंदी के एक समकालीन कवि केदारनाथ सिंह की एक कविता है. शीर्षक है- नदियां. कविता का एक अंश यह है:
पुल
पृथ्वी के सारे के सारे पुल
एक गहरा षड्यंत्र हैं, नदियों के ख़िलाफ़
और नदियां उन्हें इस तरह बर्दाश्त करती हैं
जैसे क़ैदी ज़ंजीरों को…
नदियां बर्दाश्त कर लेती थीं लेकिन सूखा, अकाल पड़ने पर जब लगान देना असह्य हो जाता था तो किसान बग़ावत कर देते और भागकर इन जंगलों में शरण लेते थे.
इन जंगलात के फ़ायदे केवल वहां रहने वाले व्यालों को ही नहीं मिले. साल 1330 में दोआब में किसानों ने लगान बढ़ाए जाने के ख़िलाफ़ बग़ावत कर दी.
बरनी लिखता है कि सुल्तान उन जंगलों को घेर लिया जहां किसान छुपे हुए थे. उनमें आग लगा दी गई. किसानों को निर्ममता से दंडित किया गया.
जहांगीर अपनी आत्मकथा में लिखता है कि 1621 में उसने घने जंगलों में छिपे हुए उन ‘गंवारान’ (गांव के आम लोग) और ‘मुज़ारियान’ (खेती-बाड़ी वाले किसान) को दंडित किया जो ज़मींदारों को लगान देने से मना करते थे.
इन दृष्टांतों से साबित होता है कि घने वन-क्षेत्र केवल कवियों और लेखकों को कविता के लिए रूमानी विषय उपलब्ध कराने का ही काम नहीं करते थे. पर्यावरण आम आदमी को वह स्पेस भी उपलब्ध कराता था जहां रहकर एक साधारण किसान सत्ता से अपने प्रतिरोध को दर्ज करा सकता था.
पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के अभिजात्य और शासक वर्गों में पर्यावरण और सामाजिक-नागरिक प्रतिरोध के केंद्र के रूप में सघन वन्य इलाक़ों को नकारात्मक रूप से देखने की प्रवृत्ति मिलती है.
प्रो. सुमित गुहा की Environment and Ethnicity In India Since 1200 to 1991, (Cambridge University Publication, 1999) इस विषय पर एक असाधारण पुस्तक है जो इतिहास की धारा में बिखरे हुए ऐसे कई सूत्रों को पकड़ने का प्रयास करती है.

विजयनगर के प्रतापी शासक कृष्ण देव राय की एक राजाज्ञा यह थी कि ‘जंगलों को वहीं पनपने दिया जाए जो राज्य के सुदूर सीमांत इलाक़े हों. इन्हें छोड़कर राज्य के मध्य में पड़ने वाले सभी इलाक़ों से उन्हें नष्ट करके उजाड़ दिया जाए’.
उत्तर भारत की तरह ही कोंकण के क्षेत्रों में यात्रा करते हुए 1675 में जॉन फ़्रेयर ने लिखा कि देहात के साधारण किसान सेनाओं से बचने के लिए जंगलों में भाग जाते थे. इससे क्रोध में आकर इन जंगलों में आग लगाने के फ़रमान जारी किए जाते थे.
प्रायद्वीपीय भारत में मराठा और उनके बाद ब्रिटिश शासकों ने भी वनों और भील, गोंड़ जैसी वन्य जातियों के प्रति यही दृष्टिकोण अपनाया.
1813 के एक मराठी शाही फ़रमान में जो खानदेश के राजस्व अधिकारियों को संबोधित है यह लिखा गया है कि
‘इस इलाक़े में जंगल की भरमार है. बाघों और डाकुओं को दूर रखने का एक ही तरीक़ा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काटे जाएं’.
सत्ता समर्थित निर्वनीकरण की इस प्रक्रिया पर दूसरा दबाव बढ़ती हुई आबादी का था. आईन-ए-अकबरी में अबुल फ़ज़ल द्वारा दिए गए आंकड़ों के आधार पर इतिहासकार मोरलैंड ने 1601 में देश की जनसंख्या का अनुमान लगाया.
उसके मुताबिक़ 1601 में यह क़रीब 100 मिलियन थी. मध्यकालीन भारत के एक अन्य समकालीन इतिहासकार शीरीन मूसवी के अनुसार, 1601 में आबादी का यह आंकड़ा क़रीब 145 मिलियन होना चाहिए.
सिंचाई के साधनों में उत्तरोत्तर हुई तकनीकी प्रगति और बढ़ते हुए जनसांख्यिकी दबाव ने अधिक से अधिक भूमि को कृषि भूमि में बदलने के लिए प्रेरित किया.
1650 में प्रति वर्ग किलोमीटर आबादी का घनत्व 35 था. मुग़ल साम्राज्य के चरम पर 1608 में आगरा सूबे में कुल उपलब्ध भूमि का केवल 27.5 प्रतिशत ही खेती-बाड़ी के लिए इस्तेमाल हो रहा था.

1656 से 1668 तक भारत में रहे फ़्रेंच यात्री बर्नियर के आंखों देखे सूरत-ए-हाल के मुताबिक, दिल्ली से आगरा तक जमुना के किनारे और लाहौर तक जाने वाले प्रमुख मार्गों के दोनों ओर घास के बड़े-बड़े मैदान थे. इससे राज्य सत्ता के राजस्व में भी बढ़ोतरी होती थी.
इन सब कारकों का मिला-जुला परिणाम यही हुआ कि हमारी धरती से वन सिकुड़ने लगे.
मध्य भारत का वन क्षेत्र जो महानदी और गोदावरी के बीच बस्तर से लेकर, झारखंड और गुजरात के दाहोद और राजपीपला तक फैला हुआ था, शाहजहां के समय तक पूरे देश में जंगलों का सबसे बड़ा विस्तार था.
शाहजहां के दरबारी इतिहासकार लाहौरी के मुताबिक़, इस पूरे इलाक़े से जंगली हाथियों को पकड़ा जाता था. लेकिन 18वीं शताब्दी के मध्य तक यह जंगल पर्याप्त रूप से सिमट चुका था.
गुजरात से प्राप्त मिरात-ए-अहमदी का लेखक बताता है कि राजपीपला से होकर जाने वाला वह रास्ता जो हाथियों के गुज़रने का कॉरिडोर था, बंद हो चुका था. (पेज 32, मैन एंड नेचर इन मुग़ल एरा, शीरीन मूशवी. इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस 1992)
गंगा-यमुना के दोआब में जहां के जंगलों में किसान बग़ावत कर छिपने की जगह पाते थे, सर्वाधिक जनसांख्यिकीय दबाव था. बदायूं और दिल्ली के बीच फैले घास के मैदान और जंगल 18वीं सदी के आख़िर तक ख़त्म हो चुके थे और उनमें विचरने उड़ने वाले तमाम व्याल और परिंदे भी.
औपनिवेशिक हाकिमों का लालच और भी बड़ा था. हिमालय और तराई के उप-पर्वतीय इलाक़ों के वन उन्हें उच्च गुणवत्ता की सागौन और साल की लकड़ी उपलब्ध कराते थे. वनों से ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करने के लक्ष्य घोषित किए गए.
1849 में लंदन की दो बड़ी कंपनियों को जंगल की लकड़ी का ठेका दिया गया. एक किलो मीटर रेलवे लाइन बिछाने के लिए औसत 250 पेड़ काटने होते थे. साल की अच्छी से अच्छी लकड़ी के स्लीपर भी दस साल से ज़्यादा नहीं टिकते थे. इसलिए हर दस साल बाद फिर उतने ही पेड़ काटे जाते.
प्रो. इरफ़ान हबीब के एक आंकलन के मुताबिक़, केवल 1879 तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए क़रीब 20 लाख पेड़ काट डाले गए. इंजन का इंधन अलग से.
एक अनुमान के मुताबिक़ एक किलोमीटर की यात्रा के लिए हर साल क़रीब 50 टन लकड़ी रेल इंजन के लिए चाहिए होती थी. अकेले 1890 तक जब भाप के कोयला चालित इंजनों का चलन शुरू हुआ, लाखों पेड़ और हज़ारों वर्ग किलोमीटर के जंगल ‘आधुनिक प्रगति’ के लिए उजाड़े जा चुके थे.
1865 में बने वन अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने आरक्षित और संरक्षित वनों के रूप में सभी प्रकार के जंगल अपने नियंत्रण में ले लिए. वन समुदाय जो वनोत्पादों पर सदियों से निर्भर थे, अपनी आजीविका के लिए अंग्रेज़ अधिकारियों के रहमो-करम पर निर्भर हो गए.
पीलीभीत के कलेक्टर टी. डब्लू की एक रिपोर्ट में जो 13 अप्रैल 1888 की है, उस ज़िले की ग़रीब वनवासी महिलाओं की गवाही दर्ज है.
उनके मुताबिक़, ‘उन्हें जलावन लकड़ी के लिए चौकी से परमिट लेना पड़ता था. पीलीभीत शहर जाकर उसे दो-ढाई आने में बेचतीं और अगले दिन का खाना जुटातीं. भरपेट खाना कभी नहीं मिलता था. कभी-कभी तो दो-दो दिन भूखा रहना पड़ता था.’ (इरफ़ान हबीब, पेज संख्या 170 राजकमल 2015).

यह वनों में राज्य और नौकरशाही की ऐसी घुसपैठ थी जो यहां के लोगों ने अब तक न देखी थी. वनों पर नियंत्रण मुग़ल शासकों का भी था. लेकिन उसका स्वरूप जटिल नौकरशाही जैसा नहीं था. उसमें स्थानीय परंपराओं का अनुमोदन था. अब जंगल और उसकी संपदा राज्य के द्वारा अनुमोदित ठेकेदारों के लिए थी.
मुग़लों द्वारा किए जाने वाले सीमित शिकार की जगह अब बारूद चालित राइफ़लों ने पूरा खेल शिकारी के पक्ष में मोड़ दिया और फिर जो संहार शुरू हुआ वह इस देश के पर्यावरण और उसकी जैविक विविधता के इतिहास में कभी नहीं हुआ था.
वो हाथी जिन्हें मुग़ल मारने की जगह सेना के लिए पकड़ते थे अंग्रेज़ों के किसी काम के न थे. वो ‘जंगली’ थे. इसलिए 1860 में नीलगिरी के वनों में बाग़ान मालिकों द्वारा सैकड़ों हाथी प्रतिदिन मारे गए.
1933 से 1940 के मध्य में नेपाल के राजा ने तराई में अपने मेहमानों को क़रीब 500 से अधिक बाघ और सैकड़ों गैंडे मरवाए. यहां तक कि ख़ुद ब्रिटेन के महामहिम जॉर्ज पंचम ने एक सप्ताह की अपनी तराई की पिकनिक में 39 बाघों को गोली से मार दिया.
एक अंग्रेज़ प्रशासक डॉनल्ड बटर के 1837 में दाख़िल एक रिपोर्ट में जो दक्षिणी अवध में जंगलों की सूरत-ए-हाल पर है, इस अंधाधुंध दोहन और संहार पर इस काव्यात्मक भाषा में चिंता व्यक्त की गई:
‘वह दिन अब दूर नहीं रह सकता जब हमारी राजस्व व्यवस्था के साथ वनों से आबाद ये क्षेत्र हरी भरी छाया और पत्तियों पर सीधी गिरने वाली ओस की निर्मल बूंदों से खाली हो जाएंगे.’ (इरफ़ान हबीब, मनुष्य और पर्यावरण में पेज संख्या 169 पर उद्धृत)
हुआ भी यही. जब पेड़ ही न होंगे तो ओस कहां होगी.
इस देश के इतिहास का एक बड़ा हिस्सा उसकी भव्य प्राकृतिक और पर्यावरणीय विरासत से जुड़ा है. यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि अभी भी हम अपनी इस बची-खुची विरासत से उदासीन हैं.
आधुनिकता के घोड़े पर सवार होकर हमने वह सब रौंद डाला जो हमें तात्कालिक रूप से अनुपयोगी और एक बाधा लगा. अलग-अलग दौर में सत्ता ने विनाश की इस मुहिम का नेतृत्व किया और हमने अनुगमन.
हमने महीनों शहर पर छायी रहने वाली धुंध और धुंओं के रूप में इसकी क़ीमत चुकाना शुरू कर दिया है. आने वाले समय में हमारी पीढ़ियां हम से भी ज़्यादा क़ीमत चुकाने वाली हैं.
जंगलों से हमेशा सत्ता को ज़्यादा डर रहा है. वह स्वयं में एक सत्ता हैं. सत्ताओं के युद्ध में अब वह जीत लिए गए हैं. जंगलों पर हमारी जीत दरअसल हमारी हार है लेकिन शायद हमें यह महसूस होते-होते बड़ी देर हो चुकी है. भवानी प्रसाद मिश्र के शब्दों में;
धंसो इनमें डर नहीं है
मौत का यह घर नहीं है
उतर कर बहते अनेकों
कल-कथा कहते अनेकोंनदी निर्झर और नाले
इन वनों ने गोद पाले.
लाख पंछी सौ हिरण-दल
चांद के कितने किरण-दलनींद में डूबे हुए से
ऊंघते अनमने जंगल
वात-झंझा वहन करते
चलो इतना सहन करते
कष्ट से ये सने जंगल
ऊंघते अनमने जंगल.
(लेखक भारतीय पुलिस सेवा में उत्तर प्रदेश कैडर के अधिकारी हैं.)