साक्षात्कार: ‘ये वो मंज़िल तो नहीं’, ‘धारावी’, ‘इस रात की सुबह नहीं’, ‘हज़ारों ख़्वाहिशें ऐसी’ जैसी फिल्में बनाने वाले राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त निर्देशक सुधीर मिश्रा से प्रशांत वर्मा की बातचीत.

भारत के अलावा पाकिस्तान को मिला लें तो देवदास पर तकरीबन 16 फिल्में बन चुकी हैं. ऐसा कौन सा आकर्षण है जो निर्देशकों को देवदास की ओर खींचता है. आपकी फिल्म ‘दासदेव’ में क्या ख़ास है जो इसे देवदास पर बनी दूसरी फिल्मों से अलग करता है?
देवदास की बात करें तो ये चरित्र बाकी हीरोज़ के विपरीत है. इसके आकर्षण की बात करें तो ये आकर्षण है एक लूज़र (असफल व्यक्ति) का. एक आदमी है जिससे वो इश्क़ करता है, पहले उसकी ज़िंदगी बर्बाद करता है. फिर अपनी ज़िंदगी बनाने के बजाय उसका हीरोइज़्म ये है कि वो ख़ुद को ख़त्म कर देता है. एक अर्थ में वह अमन पसंद व्यक्ति है, विद्रोह नहीं करता.
इसके उलट एक हीरो होता है जो निर्णय ले लेता है, अटल होता है, वो बदले की ओर अग्रसर होता है और एक देवदास है.
अब सवाल है कि इस किरदार पर मैंने क्यों बनाई फिल्म… मेरे दोस्त हैं प्रीतीश नंदी, बहुत पहले उन्होंने मुझे देवदास पर फिल्म बनाने के लिए बोला था. तब तक अनुराग (कश्यप) ने देव डी बना ली थी. मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट नहीं था.
फिर मुझे ख़्याल आया कि देवदास कुछ-कुछ हैमलेटनुमा (शेक्सपीयर का नाटक हैमलेट) है. मुझे ख़्याल या कि क्या देवदास किसी राजनीतिक परिवार का वारिस हो सकता है? जैसे राजनीतिक परिवार के कुछ लोग वापस आते हैं अपनी विरासत संभालने, जब परिवार समस्या में होती है.
अगर देवदास को राजनीतिक परिवेश में रखूं तो कैसा होगा? अगर पारो का पिता देवदास के पिता का राजनीतिक सचिव हो और देव के पिता की मौत के बाद दोनों के परिवार बंट जाएं, देव अमीरों के बिगड़े बच्चे जैसा होता है और उसे परिवार संभालने के लिए बुलाया जाता है.
देव और पारो राजनीतिक मतभेदों के चलते एक-दूसरे से अलग होते हैं. चंद्रमुखी इस फिल्म में सत्ता के लिए लॉबीइंग करती है.
अब पता नहीं ये कितनी शरत बाबू (शरत चंद्र चट्टोपाध्याय) के देवदास की तरह है लेकिन उसके रिश्ते कुछ-कुछ वैसे ही हैं. ये एक पॉलीटिकल थ्रिलर है कि कैसे सत्ता देवदास और पारो के इश्क़ के आड़े आती है. सत्ता का जो नशा होता है उससे मुक्त होने की कोशिश है ये फिल्म.
शेक्सपीयर के बराबर कोई थ्रिलर राइटर है नहीं. मेरी फिल्म में शेक्सपीयर का असर ज़्यादा है और शरत बाबू का कम. फिल्म की शुरुआत देवदास से ज़रूर है लेकिन उसके ज़रिये मैं लोगों से एक दूसरी तरह की कहानी कहना चाह रहा हूं.

बॉलीवुड में अभी भी महिला किरदार बहुत ही स्टीरियोटाइप तरीके से लिखे जाते हैं, लेकिन आपकी फिल्मों में महिला किरदार बहुत ही मज़बूत होते हैं.
मेरी फिल्म की महिला किरदार पीड़ित नहीं होती हैं. वे अपनी ख़्वाहिशें पूरा करना चाहती हैं और उसकी वजह से वो आपको (हीरो) छोड़ भी सकती हैं. वो फिल्मों में मर्द की जागीर बनकर नहीं रहती हैं. वो इश्क़ शब्द के जाल में भी नहीं फंसती हैं.
ये उस तरह की औरतें हैं, जो अपने में आज़ाद हैं और कभी-कभी जैसे मर्द ग़लत होते हैं, वो भी ग़लत होने की क्षमता रखती हैं. उनकी ख़्वाहिश अलग है, वो अपनी ज़िंदगी को समझना चाहती हैं.
चाहे वो हज़ारों ख़्वाहिशें ऐसी की गीता (चित्रांगदा सिंह) हों, चाहे इनकार की माया (चित्रांगदा सिंह) हों, चाहे वो धारावी की शबाना हों, चाहे मैं ज़िंदा हूं की दीप्ति नवल हों.
मुझे बड़ा बोरिंग लगता है जब महिलाओं के किरदार को पीड़ित के तौर पर दिखाया जाता है. अभी भी जब लिखते हैं तो एक विक्टिमहुड (पीड़िता) की कहानी लिखी जाती है, जहां एक मर्द बचाने आता है उन्हें. ऐसी कहानियां अक्सर लिखी जाती हैं, जिसको बड़ा प्रोग्रेसिव भी बोला जाता है.
मैं इन सबसे थोड़ा मुक्त हूं, शायद अपने ख़्यालों की वजह से, अपनी ज़िंदगी की वजह से या जो औरतें मुझे मिली हैं, उनकी वजह से.
‘धारावी’, ‘इस रात की सुबह नहीं’, ‘हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी’ आपकी चर्चित फिल्मों में से एक हैं. इन फिल्मों के बारे में ख्याल कैसे आया. अपनी फिल्मों के लिए कहानी और किरदार कहां से खोजते हैं?
हर आदमी के अंदर पांच से सात फिल्में ही होती हैं. यानी वो पांच-सात फिल्में ही बना सकता है. आपका ख़ुद का एक एनवायरमेंट रहता है, जहां आप पले-बढ़े होते हैं. अपनी मां की तरफ़ से कहूं तो एक राजनीतिक खानदान से ताल्लुक रखता था. हालांकि राजनीतिक खानदान तो वो बन नहीं सका.
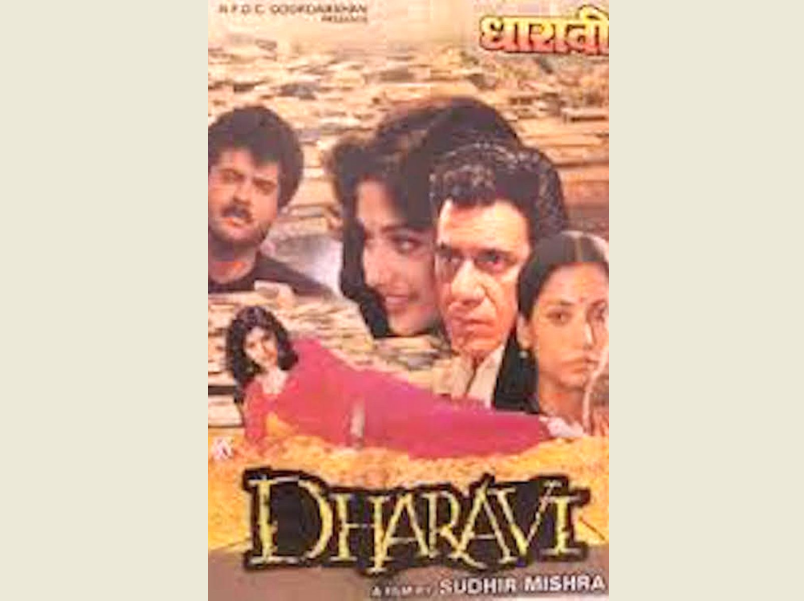
मैं एक गणितज्ञ का बेटा हूं. थोड़ा लखनऊ का हूं, थोड़ा सागर (मध्य प्रदेश) से हूं, थोड़ा दिल्ली का हूं और अब ज़्यादातर मुंबई का हूं. जो भी पढ़ा-लिखा, जो भी ज़िंदगी में समझा, शायद उसका प्रभाव भी होगा.
मेरी फिल्मों के पात्र वास्तव में कहां से आते हैं, ये तो रहस्य है. मेरी दादी मां ने मेरे पापा और उनके चार भाइयों को अकेले पाला, उसका भी कहीं असर होगा. मेरे नाना थे डीपी मिश्रा (मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री), उन्होंने मुझे बोला था कि सत्ता तुम्हारी नहीं है. उन्होंने किसी तरह की मदद करने से ही हमें मना कर दिया था. उन्होंने कभी सामान्य नाना होने की भी जो मदद होती है वो भी नहीं की. उनका भी प्रभाव कहानी और पात्रों में रहा होगा.
कहीं लेफ्ट विंग से जुड़े आंदोलन का प्रभाव रहा तो राइट विंग भी इर्द-गिर्द ही रहा. पात्र पता नहीं कहां से आते हैं, लेकिन कहानीकार के अंदर जो कमियां या ख़ालीपन होता है वो उसे कहीं न कहीं कहानियां लिखकर पूरा करता है.
फिल्मों की सफलता बॉक्स आॅफिस पर उसके प्रदर्शन पर तय होती है. आपने इस पैमाने को दरकिनार करते हुए फिल्में बनाई हैं. कभी किसी मसाला या कॉमर्शियल फिल्म पर दांव क्यों नहीं लगाया?
कलकत्ता मेल के ज़रिये मैंने कॉमर्शियल फिल्म बनाने की कोशिश की थी, लेकिन यह बुरी तरह से फेल हुई थी. अच्छी बात ये है कि अलग तरह की फिल्मों से दर्शक अवगत हुए हैं. ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा नहीं था. पहले भी लीक से हटकर फिल्में बनती थीं लेकिन जो आपकी फ़ितरत होती है उसमें आप रहें, क्योंकि फिल्म बनाना आपके कंट्रोल में इतना नहीं है. आप जिस फ़ितरत के हैं, आप वही कर सकते हैं.
अगर आप उस फ़ितरत से हटेंगे तो आप फेल होंगे. मुझे ऐसा लगता है कि आदमी को अपनी सीमाएं भी पहचाननी पड़ती हैं. आप सब कुछ नहीं कर सकते. जो आप बेहतर कर सकते हैं जिस टर्फ पर आप अच्छा खेल सकते हैं, उसी पर ही खेलना चाहिए. बीच में मैं डगमगाया था लेकिन अब मैं अपनी फ़ितरत की तरफ़ और जाने की कोशिश में हूं.
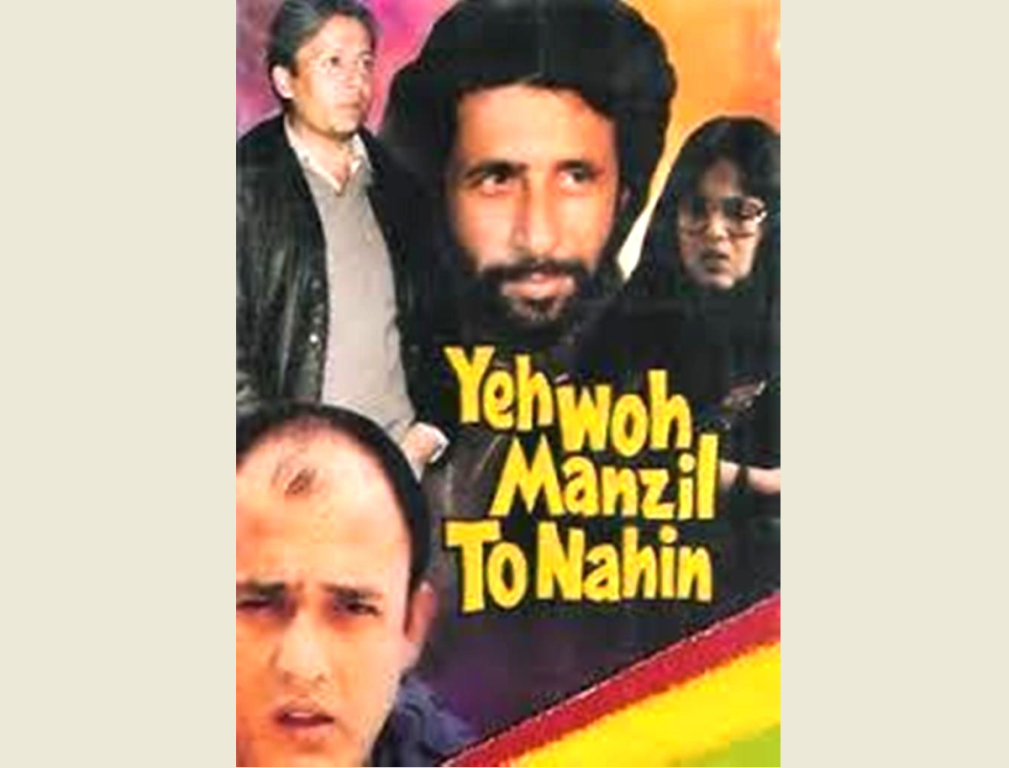
मुझे आजकल के युवा फिल्मकार अच्छे लगते हैं. मुझे अमित मसूरकर (न्यूटन) भी प्रेरित करता है और अलंकृता श्रीवास्तव (लिपस्टिक अंडर माई बुरखा) भी. अनुराग (कश्यप) तो प्रेरित करता था ही और विशाल (भारद्वाज) करते ही हैं. आप अपने हिसाब से ही काम कर सकते हैं, वो आपकी फ़ितरत में है. आपकी एक समझ है, उसके हिसाब से आप फिल्म बना सकते हैं.
आपका जन्म और परवरिश लखनऊ की है, लखनऊ के एक युवा के लिए बॉलीवुड तक का सफ़र कैसा रहा, ख़ासकर तब जब उसे हीरो नहीं फिल्म निर्देशक बनना था?
मुझे तो हमेशा से ही फिल्म निर्देशक बनना था. मैं ख़ुशकिस्मत था कि मैं यहां (मुंबई) आया और कुंदन शाह, विधु विनोद चोपड़ा और सईद मिर्ज़ा जैसे निर्देशक मिले. मैं बाइस-साढ़े बाइस साल (1980) का था. किसी ने बोला कि तुम इस स्क्रिप्ट पर काम करोगे, वो कुंदन शाह था. तो कोई गाना-वाना नहीं था. वो पहली फिल्म बना रहा था. फिल्म का नामजाने भी दो यारो था.
लोगों को ये फिल्म बहुत पसंद आई और हम अपनी तरह की फिल्में बनाने लगे. मैं हमेशा से निर्देशक बनना चाहता था और सौभाग्य से ये हो गया. कभी-कभी सोचकर घबराहट होती है कि वो लड़का जो लखनऊ से बंबई आया था, वो क्या सोचकर आया था लेकिन कुछ चीज़ें ठीक ही हो गईं. और अभी भी यहां हैं तो इसका मतलब है कि बुरा भी नहीं हुआ कुछ.
तो अभी तक जो हुआ या किया उससे अच्छा हो सकता था, लेकिन ये तो सभी के लिए हो सकता था. दुनिया भी बेहतर हो सकती थी और मुल्क भी बेहतर हो सकता था और हो सकता है.
मेरे पिता लखनऊ में फिल्म सोसाइटी चलाते थे, उनका भी असर रहा होगा यहां तक आने में. लखनऊ से दिल्ली गया था तो बादल सरकार (थियेटर निर्देशक) जैसे बड़े आदमी मिले थे. उन्होंने रंगमंच के क्षेत्र में दिमाग खोल दिया था. तो दिमाग अगर आपका कोई खोल देता हैं न तो चीज़ें आसान हो जाती हैं.
इस सफ़र में जो लोग भी मिले, उनकी बातें सुनी, उनसे प्रेरणा ली. उनका भक्त नहीं बना, वैसी प्रवृत्ति नहीं थी अंदर, क्योंकि गणितज्ञ का बेटा था. बचपन में जो माहौल मिलता है उससे थोड़ा आज़ाद ख़याल हो जाते हैं आप.

मेरे ख्याल से जिस लखनऊ को मैं जानता हूं या जो मेरे परिवार का लखनऊ है, वो काफी पढ़ा-लिखा और समझदार है. आप जब लखनऊ से होते हो तो आप हिंदी कविता से भी परिचित होते हो, उर्दू से भी होते हो. वो थोड़ा अर्बन (शहरी) था, सोफिस्टिकेटेड (प्रबुद्ध) था. तो दिमागी तौर पर यहां तक का सफ़र कोई मुश्किल नहीं था.
आप तकरीबन 35 सालों से बॉलीवुड में सक्रिय हैं. इतना लंबा समय गुज़ारने के बाद बॉलीवुड को किस तरह से देखते हैं. कहा जाता है कि यहां आज भी फिल्मी परिवारों का दबदबा है. इस बात से कितना इत्तेफ़ाक़ रखते हैं?
भई, हम तो बाहर से ही आए थे. शुरुआत में जो भी बंबई आए, वो बाहर से ही आए थे. फिल्मी परिवारों का एकाधिकार है, लेकिन वो तो क़ानून के क्षेत्र में भी है और डॉक्टरी में भी है, शिक्षा के क्षेत्र में भी है और बिज़नेस के क्षेत्र में भी है. यहां (बॉलीवुड) भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग घुस नहीं पाते और उनकी जगह नहीं बनती.
आजकल तो और बेहतर हो गया है. जो मध्यमवर्गीय युवा आए हैं वो आज़ाद ख़याल हैं. इस माध्यम (सिनेमा) को समझ रहे हैं और कंट्रोल भी कर रहे हैं. लड़ाई थोड़ी ज़्यादा है लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा अंधकार है. यहां टैलेंट होना चाहिए और मुश्किलें और रिजेक्शन झेलने का साहस होना चाहिए. जो पांच-सात साल लगते हैं, अगर आप ख़ुशकिस्मत नहीं हैं तो ये लड़ाई मुश्किल है. अगर इसको झेल लो तो फिर सब ठीक हो जाता है.
आप देख लो चाहे राजकुमार हिरानी हों, विशाल भारद्वाज, चाहे अनुराग कश्यप, इम्तियाज़ अली या चाहे आनंद एल. राय हों… आज जो भी फिल्में बना रहे हैं सब बाहर के ही हैं. थोड़ा वक़्त लगता है. संघर्ष में जो वक़्त लगता हैं उसमें आप बनते हैं, आप तैयार होते हैं.
जो संघर्ष आप करते हैं उसमें अच्छाइयां भी हैं. मुश्किल हैं, थोड़ा अनुचित भी है लेकिन ये तो पूरे हिंदुस्तान में है. टैलेंट को आप कर्स (श्राप) मानिए तो आप बेहतर समझेंगे. अगर आप में है वो तो सिवाय ये करने के आपके पास चारा भी तो नहीं है. तो मुश्किलें आएंगी लेकिन आप इसके अलावा करोगे क्या.
फिल्म एडिटर को सिनेमा का अनसंग हीरो कहा जा सकता है. इनके बारे में लोग ज़्यादा नहीं जानते. फिल्म एडिटर रेनू सलूजा आपकी पत्नी थीं और उन्हें तीन-तीन राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं. फिल्म एडिटर के काम और रेनू सलूजा के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
रेनू कहानीकार थी. फिल्म एडिटर स्क्रिप्ट का लास्ट ड्राफ्ट लिखता हैं, वही फिल्म को फाइनल करता है. फिल्म एडिटर का काम होता है कि वो निर्देशक को बताए कि उसने कौन-सी फिल्म बनाई है. उस तरफ फिल्म को ले जाना जिस तरफ आपने (निर्देशक) सोचा है. जो आपके ख्याल में है वो अलग फिल्म है और जो बनी है वो अलग.

रेनू को फिल्मों की बहुत ही कमाल की समझ थी. इस क्षेत्र में उससे प्रसिद्ध लड़की कोई हुई नहीं है. अस्सी के दशक में मर्दों के पेशे में अकेले उसने अपनी जगह बनाई. आप एक बात उसके साथ काम कर लो तो मुश्किल होता था किसी और के साथ काम करना. वो कमिटेड (समर्पित) थी और अड़ियल भी बहुत थी.
आपकी फिल्मों में गाली-गलौज का भी इस्तेमाल किया जाता है. ऐसे में सेंसर बोर्ड से कैसे संबंध रहे. आज के समय में सेंसर बोर्ड के कामकाज को कैसे देखते हैं?
नहीं-नहीं… मेरी फिल्मों में गाली-गलौज बहुत कम होती है. ये पात्र के हिसाब से होती है. जहां तक सेंसर बोर्ड की आपत्ति की बात है तो मैंने हर जगह उसके ख़िलाफ़ बात की है. सेंसर बोर्ड की ज़रूरत है ही नहीं, मेरे ख़्याल से केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) की ज़रूरत है.
वो सेंसर बोर्ड क्यों बनना चाहता है मुझे समझ नहीं आता. वो सीबीएफसी रहे और सर्टिफिकेशन का काम करे. वो परिवार के दकियानूसी पिता की तरह न बने.
ये गाली मत दो… ऐसे बात करो… ऐसे न करो… ये भाषा मत इस्तेमाल करो… वो कहानी मत सुनाओ… ये मत बोलो, ये कहो… हमारी जनता इसके लिए तैयार है, इसके लिए तैयार नहीं… आप कौन होते हैं, ये तय करने वाले.
हमारा रिश्ता स्वतंत्र रहने दो. मैं तो सरकार से ये भी कहता हूं कि हम पर टैक्स मत लगाओ. मैं ये भी कहता हूं कि केवल इनकम टैक्स होना चाहिए. जो पैसे कमाए, आप उस पर टैक्स लो. बाकी सारे टैक्स आप हटा दो.
आप एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं? आपके नाना डीपी मिश्रा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं. ऐसे में क्या आपने कभी राजनीति में आने के बारे में सोचा?
दासदेव जो फिल्म है ये कुछ वैसा ही है कि अगर मैं राजनीति में गया होता तो क्या होता. मैंने ये फिल्म तीन लोगों को समर्पित की है. शरत बाबू, दूसरे शेक्सपीयर और तीसरे मेरे नाना, जिन्होंने हमें अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंका था.

अगर फेंका नहीं होता तो शायद मैं भी किसी राजनीतिक खानदान का सदस्य होता. राजनीति एक दूसरी ही फ़ितरत के लोगों का काम है. मुझे किसी दल या किसी लीडर के अधीन रहने की आदत नहीं है.
आज की राजनीति को किस तरह से देखते हैं. अभी के राजनीतिक माहौल के बारे में कहा जा रहा है कि इमरजेंसी जैसे हालात हैं. कला और सिनेमा के लिए ख़राब समय है.
इस माहौल से, सेंसर बोर्ड से मुझे हमेशा ही कुछ न कुछ दिक्कत हुई है और हमेशा होगी भी. मैं तो हर बार लड़ने को तैयार हूं. किसी भी तरह की फिल्म पर रोक होती है तो मैं झगड़ा करने के लिए तैयार हूं.
मुझे लगता है कि आपको इसमें भाग लेना चाहिए, भागना नहीं चाहिए. अगर माहौल ख़राब है तो फिर आप उसमें और दख़ल दीजिए. सिर्फ़ शिकायत करने से कुछ नहीं होगा. फिर आप अलग-अलग तरीके से फिल्म बनाइए.
अपनी बात को इस तरह से नहीं तो उस तरह से कहिए. बहुत सारी जगहों पर ऐसा हुआ है. ईरान में ऐसा हुआ है तो लोगों ने वहां इसी तरह से फिल्में बनाई हैं.
आपको हर वक़्त दख़ल तो देना पड़ेगा और आप खड़े रहेंगे तो बात बनेगी. मेरे ख़्याल में अनुराग कश्यप, विशाल भारद्वाज जिस हिम्मत से फिल्म बनाते थे, अभी भी उसी हिम्मत से बना रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद भी पद्मावत फिल्म की रिलीज़ में करणी सेना जैसे संगठन ने काफी मुश्किल खड़ी की. इसी तरह एक फिल्म नानक शाह फकीर को भी सेंसर बोर्ड और सुप्रीम कोर्ट से रिलीज़ की अनुमति मिल गई है लेकिन यह फिल्म किसी सिनेमाघर ने नहीं लगाई. इन स्थितियों के बारे में आप क्या कहेंगे?
सिनेमाघर संवेदनशील होते हैं. अगर सरकार फिल्मकारों और सिनेमाघरों को सुरक्षा नहीं देगी तो फिर वो कैसे फिल्म को रिलीज़ कर पाएंगे. ये बातें इतनी बार कहीं जा चुकी है कि अब बार-बार यही बात कहें, ये अजीब लगता है.
हमारा समाज बहुत संवेदनशील समाज है और समाज के ठेकेदार और ज़्यादा संवेदनशील हैं. कुछ असंवैधानिक संगठन हैं जैसे कि करणी सेना. जो कभी कहती है कि फिल्म देखो, कभी कहती थी कि फिल्म न देखो.
इन सबके ख़िलाफ़ तो झगड़े चलेंगे. ये एक जटिल मुल्क है और ऐसे मुल्क में थोड़ी सी दिक्कतें भी होंगी ही, लेकिन उसके ख़िलाफ़ आगे बढ़ते रहना पड़ेगा.
सिनेमा को आज़ाद करने का एक तरीका ये भी है कि वो महंगा न हो.





