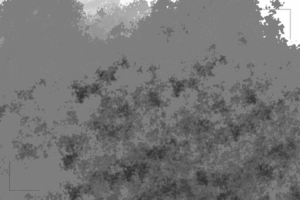श्रीकांत वर्मा के साहित्य में जीवन-मरण का स्मरण किसी प्रकार के रहस्यवाद से परे है. बात सीधी-सपाट है. आदमी अपने ‘रक्तचाप’ से मरता है, अपने ‘पाप’ से नहीं.

मंगलवार, 11 मार्च 1986, न्यूयॉर्क
————–
‘जब से बीमारी का पता चला है, भूख ही बुझ गई है. डॉक्टर कहते हैं, कैंसर में ऐसा अक्सर होता है. क्या कहूं! कितना अभागा हूं मैं! …बचपन से रोगग्रस्त रहा. अभी जवान भी नहीं हुआ था कि पिता निकम्मे हो गए. कोई काम नहीं कोई आए नहीं. जिस उम्र में लोग सपने देखते हैं, मैंने स्कूल मास्टरी की; मां-बाप, भाई बहनों को पाला और अपनी शिक्षा पूरी की.
दिल्ली आया तो… पराजय, विफलता, पीड़ा, रोग, धोखा सब मुझसे चिपकते गए. कभी निराला की पंक्ति याद आती है ‘क्या कहूं आज जो नहीं कही, दुख ही जीवन की कथा रही’ तो कभी मुक्तिबोध की,’पिस गया वह भीतरी और बाहरी, दो कठिन पाटों के बीच.’
नहीं जानता यह डायरी जारी रहेगी या यह इसका अंतिम पन्ना होगा.
मगर इतना अवश्य कहूंगा, मैं जीना चाहता हूं.
[पृष्ठ.467, श्रीकांत वर्मा रचनावली, खंड 2, राजकमल प्रकाशन ]
11 मार्च 1986 को न्यूयॉर्क में एक अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले श्रीकांत वर्मा ने अपनी डायरी लिखी. यह उनकी डायरी का अंतिम पन्ना था. जीवन की डायरी के पन्ने के कुछ 2 महीने और फड़फड़ाये. 25 मई 1986 को स्लोन केटरिंग मेमोरियल अस्पताल,न्यूयॉर्क में जीवन-दैनन्दिनी का अंतिम सर्ग पूरा हुआ. डायरी समाप्त हुई.
‘मगध’ में सन्नाटा छा गया-
‘महाराज बधाई हो-
कोई नहीं रहा
श्रावस्ती की कोख उजड़ चुकी,
कौशाम्बी विधवा की तरह
सिर मुंडाये खड़ी है.
कपिलवस्तु फटी फटी आंखों से
सिर्फ़ देख रहा है
अवंती निर्वसन है
…
और मगध में ?
मगध में सन्नाटा है !
क्षमा करें महाराज
आप नहीं समझेंगे
यह कैसा सन्नाटा है .
[मगध- कविता संग्रह, श्रीकांत वर्मा, रचनाकाल 1984]
श्रीकांत वर्मा हिंदी की नई कविता धारा के एक बड़े नाम थे. यह और बात है कि हिंदी भाषी समाज में अपने अन्य समकालीनों के उलट उन्हें बहुत देर से जाना गया. उससे भी दुखद यह कि कम जाना गया.
वह सक्रिय राजनीतिज्ञ भी थे. जीवन के आरंभिक दौर में लोहिया से प्रभावित थे. बाद में देश के एक बड़े राजनीतिक दल से जुड़े. राज्यसभा में रहे. हिंदी के ही नहीं, तीसरी दुनिया के देशों में रचे जा रहे साहित्य के गहरे जानकार और अनुवादक, मिजाज से तीक्ष्ण-दर्शी यायावर, सिद्धांत से उत्कट मानवतावादी और शख्सियत से एक ठेठ ‘कस्बाई ‘ जो ‘मॉडर्निज़्म’ से आक्रांत वातावरण में अपने चारों सिम्त एक सच्चे आदमी को तलाशता रहा.
तलाशते तलाशते वह क़स्बाई कितनी दूर निकल गया! ‘मगध’ तक जा पहुंचा. (मगध श्रीकांत वर्मा का आख़िरी कविता-संग्रह था) घुड़सवार से पूछा- भाई मगध किधर है. मुझे मगध जाना है.
श्रीकांत वर्मा के लिए ‘मगध’ इतिहास का बिंब है. सत्ता और मनुष्य की दुर्दम महत्वाकांक्षा का प्रतीक है. वह एक शहर है और लिच्छवियों पर भारी एक विजिगीषु संस्कृति भी है. वह वर्तमान के अंतर्द्वंदों में गुंथी हुई एक निर्दोष स्मृति भी है, जो रह-रहकर आधुनिक मनुष्य के नैतिकताविहीन परिवेश के अंधकार को और गहरा देती है. सब कुछ को विडंबनामय बनाती है.
‘केवल अशोक लौट रहा है
और सब
कलिंग का पता पूछ रहे हैं
केवल अशोक सिर झुकाए हुए है
और सब
विजेता की तरह चल रहे हैं
केवल अशोक के कानों में चीख गूंज रही है
और सब
हंसते हंसते दोहरे हो रहे हैं
केवल अशोक ने शस्त्र रख दिये हैं
केवल अशोक
लड़ रहा था’
[मगध- कविता संग्रह, श्रीकांत वर्मा, रचनाकाल 1984]
श्रीकांत वर्मा कई मायनों में अपने साथी सुखनवरों से बहुत अलग थे. उनका प्रखर शताब्दी-बोध उन्हें चिंतन और संवेदना के फलक पर सतह से उठाकर एक विश्व-चेतस नागरिक और सृजनकार के रूप में स्थापित करता था.
साहित्यकार हो या फिर आर्टिस्ट दोनों के लिए उसका अपना लैंडस्केप बहुत महत्वपूर्ण है. वह लैंडस्केप, जो उसके आसपास होता है. वह उसकी संवेदना को संवारता, उधेड़ता और फिर से बनाता है.
श्रीकांत वर्मा के यहां यह लैंडस्केप तनाव भरता है. वह एक छोटे से कस्बे से आए थे. अपने एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा था-
‘कस्बे में आदमी की जड़ें ज्यादा गहरी होती हैं. महानगर में रहने वाले का ‘एलिएनेशन’ जितनी जल्दी होता है, उतना जल्दी गांव या कस्बे के व्यक्ति का नहीं होता. आज भी मेरी जड़ें परिवार और उसके परिवेश में हैं- बावजूद इसके कि आधुनिकता मेरे लिए ‘फेटिश’ बन गई. पश्चिमी माहौल और संस्कृति- उससे उत्पन्न मृत्युबोध ने मुझे दबोच लिया… लेकिन मेरी जड़ें अब तक उखड़ नहीं पाईं हैं.’ [पृष्ठ 310,रचनावली खंड 4,राजकमल प्रकाशन]
कोई भले न उखड़े लेकिन शहर हमेशा से जड़ों को हिलाते रहे हैं. रॉबर्ट रेडफील्ड, जिन्हें लेविस मम्फोर्ड ने अपनी वृहद पुस्तक ‘द सिटी इन हिस्ट्री’ में उद्धृत किया है, ने कहा था The remaking of man was the work of city यानी आदमी का पुनर्गठन शहरों का काम रहा है.
लेविस मम्फोर्ड (1895-1990) ने रेडफील्ड के इस सूत्र का और विस्तार किया. आदिम गैर-शहरी समाज भी मनुष्य की इस ‘री-मेकिंग’ में हिस्सा लेते थे. जब उन समाजों को लगता था कि आदमी को अपेक्षित भूमिका निभाने लायक बना लिया गया है और वह अब उनके इच्छित समाज का पुर्जा बन कर रह सकता है, वह मनुष्य पर परिवर्तन के अतिरिक्त दबाव डालना बंद कर देते थे.
शहर इसी बात पर अलग हैं. नयी-नयी भूमिकाएं प्रस्तावित करके, वह मनुष्य के ‘आत्म’, उसके ‘सेल्फ’ का निर्माण-पुनर्निमाण करते हैं. [पृष्ठ-116, द सिटी इन हिस्ट्री, हार्वेस्ट बुक, न्यूयॉर्क]
एक शहरी परिवेश में ‘आत्म’ के निर्माण और पुनर्निमाण का यह भयानक संघर्ष नई कविता के सभी कवियों में से श्रीकांत वर्मा में सबसे सघन और संश्लिष्ट है. मलयज के अनुसार उनकी कविताओं में दो दुनिया हैं- एक नगर की दूसरी प्रकृति की. दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है, बल्कि गहरी असंगति है. नामवर सिंह ने मलयज के इस निष्कर्ष से असहमत होते हुए यह निष्कर्ष दिया कि ‘प्रकृति और नगर इस दुनिया में अलग-अलग नहीं बल्कि वन्य-प्रकृति नगर-जीवन की ऊब के बीच ‘अवकाश’ का विस्फोट है. यह सरल पलायन नहीं, बल्कि ऊब का कवित्व है. इस दुनिया में सब कुछ निहायत साधारण है और यह साधारणता ही उसे अत्यंत असाधारण और भयावह बना देती है.’ [पृष्ठ 216, कविता के नए प्रतिमान, राजकमल प्रकाशन]
यह ऊब इस कारण असाधारण है कि वह निहायत एकांतिक न रहकर अपने परिवेश के अनुभूत सत्य को नैतिक-अनैतिक के सामाजिक बोध से भयग्रस्त हुए बिना उसकी पूरी समग्रता में पकड़ती है, इसलिए शिल्प और संवेदन दोनों के स्तर पर एक ‘कोठे’ से धूप के उतरने और उस पर एक ‘दलाल’ के चढ़ने का दृश्य निपट साधारण नहीं रहता-
‘एक टाइपराइटर पृथ्वी पर छापता है
दिल्ली, बम्बई,कलकत्ता,
जलाशय पर अचानक छप जाता है
मछुए का जाल
चरकट के कोठे से
उतरती है धूप
और चढ़ता है दलाल,
एक चिड़चिड़ा बूढ़ा थका क्लर्क ऊबकर
छपे हुए शहर को छोड़कर चला जाता है’
[श्रीकांत वर्मा: माया दर्पण]
उनकी कविता में प्रकृति की आमद नए शहरी मनुष्य की सबसे दर्दनाक अवस्था का निरूपण है, लेकिन यह केवल हिंदी के कवि का ‘मरसिया’ नहीं है. एलेन गिन्सबर्ग (1926-1997) अमेरिकी अंग्रेज़ी साहित्य में उस पीढ़ी के प्रतिनिधि कवि हैं, जिसे ‘बीट जनरेशन’ कहा गया है.
गिन्सबर्ग की एक कविता है- ए सुपरमार्केट इन कैलिफोर्निया, जहां कवि ‘सुपरमार्केट’ में खोया हुआ अपने प्रिय कवि वॉल्ट व्हिट्मैन को याद करता है-
‘What peaches and what penumbras
Whole families shopping at night!
Aisles full of husbands!
Wives in the avocados, babies in the tomatoes!
And you, Garcia Lorca,What were you doing down by the watermelons?
Where are we going, Walt Whitman?
The doors close in an hour,
Which way does your beard point tonight?
Will be stroll dreaming of the lost America
Of love past blue automobiles in driveways!’
[पृष्ठ. 59, एलेन गिन्सबर्ग-सलेक्टेड पोअम्ज़, पेंग्विन बुक्स]
कैलिफोर्निया के ‘सुपरमार्केट’ में गिन्सबर्ग की कविता का नायक खोया हुआ है. वह अपने ‘खोए हुए’ देश को ढूंढ लेना चाहता है. यह दोहरी तलाश है, जितनी ‘स्पेस’ की है उतनी ही अस्मिता की.
श्रीकांत वर्मा के ‘जलसाघर’ की एक कविता में उसका पात्र भटका हुआ है. वह समरकंद ढूंढता है. यह जड़ों की तलाश है और अत्यंत कारूणिक है. ‘समरकंद अब कितनी दूर है?’ वह चिल्लाता है. कोई जवाब नहीं. रास्तों पर भीड़ है. बाबर भीड़ के बीच से गुज़रता है. वह गिड़गिड़ाता है-
‘समरकंद अब कितनी दूर है?
वह-
शहर देख रुकता है.
समरकंद!समरकंद !
बुर्ज देख बाबर किलकारी भरता है.
‘समरकंद पीछे रह गया है!’
कहता हुआ शहरयार
बाबर के पास से गुज़रता है.’
[जलसाघर, श्रीकांत वर्मा]
इसी बिंदु पर श्रीकांत वर्मा का काव्य गहन त्रासदी और विडंबना का काव्य बन जाता है. ‘मणिकर्णिका का डोम’ मणिकर्णिका को संबोधित करता है-
‘दुःखी मत होओ,मणिकर्णिका
ऐसे भी शमशान हैं
जहां एक भी शब नहीं आता
आता भी है
तो गंगा में नहलाया नहीं जाता’
युवावस्था का ‘जाना’ भी एक नियति नहीं विडंबना है. टीएस इलियट के प्रारंभिक दौर की (1910) एक कविता-पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी में एक पात्र कहता है-
‘Ah,My friend, you do not know
You do not know
What life is,You who hold it in your hands’
‘You let it flow from you,you let it flow
And youth is cruel,and has no remorse
And smiles at situations which it can not see’
श्रीकांत वर्मा की एक कविता में सब लौट कर आते हैं.
‘लौट कर सब आएंगे
सिर्फ़ वह नहीं जो युवा था
युवावस्था लौटकर नहीं आती
आया भी तो
वही नहीं होगा’
[मगध, श्रीकांत वर्मा]
विडंबना (Irony) ‘लौटकर न आने में’ नहीं रहती. वह आख़िरी दो संक्षिप्त पंक्तियों में सन्निहित हो जाती है-
‘आया भी तो/वही नहीं होगा’
श्रीकांत वर्मा जिस दौर में लिख रहे थे, उस समय की कविता पर फ़्रांसीसी दार्शनिक ज़्यां पॉल सात्र के अस्तित्ववाद का प्रभाव था. यूरोप में यह विचारधारा दो विश्वयुद्धों के मध्य पनपी.
अस्तित्ववाद मानता था कि मनुष्य के लिए मूल्यों का निर्धारण उसके आत्मगत ज्ञान के ज़रिए ही संभव है. वह वस्तुगत ज्ञान का निषेध करता था. भाषा में नए उपमानों का प्रयोग, अस्तित्व की खंडित अनुभूति, मृत्युबोध, वक्तव्यों में आत्मानुभूत ईमानदारी का आग्रह, परिवेश की विडंबना का चित्रण इत्यादि कुछ ऐसी प्रवृत्तियां थीं, जिनका खंडन करते हुए मार्क्सवादी आलोचक डॉ. रामविलास शर्मा ने एक लंबा लेख लिखा- अस्तित्ववाद और नई कविता.
अपने लेख में उन्होंने नई कविता पर यह आक्षेप किया कि ‘नई कविता के लेखक यदि वास्तव में विद्रोही होते तो नए यथार्थ बोध से हिंदी कविता को समृद्ध करते. स्थिति इसके उलट है. नई कविता ने अपने भाव-बोध और उपमानों का ऐसा कल्पना-लोक रच लिया है, जो छायावाद से ज़्यादा काल्पनिक और रीतिवाद से कहीं ज़्यादा रूढ़िबद्ध है.’
वस्तुतः जिस परिवेश में भारतीय साहित्य में अस्तित्ववादी एहसासों का हस्तक्षेप हुआ वह यूरोप के परिवेश से भिन्न था. यूरोप युद्ध से तबाह था तो भारतीय समाज औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था से निकलकर अपना भविष्य तलाश रहा था. ऊपर से बढ़ती आबादी, बेरोज़गारी, नगरीकरण के दबाव से जनित पलायन, राजनीतिक शुचिता का अभाव और चहुं ओर फैलीं सामाजिक विषमताएं, अन्याय, सब मिलकर एक ऐसे वातावरण को रच कर रहे थे, जो परिवेशगत भिन्नता के बावजूद अनुभूतिगत समानता में अस्तित्ववाद के निकट था.
कुंवर नारायण के ‘आत्मजयी’ के ‘नचिकेता’ पर अपने आलेख (1965) में श्रीकांत वर्मा ने लिखा, ‘दो तरह के नरक हैं, एक समृद्धि का, एक दारिद्रय का. एक में आदमी जीते जी दफ़न है. दूसरे में मरने को अभिशप्त है. दोनों तरह की मृत्यु, मृत्यु है. दोनों तरह का साहित्य साहित्य है और उसे उसी जीवन-संदर्भ में रखकर देखना चाहिए जिसका वह दावा करता है या जिससे वह पैदा हुआ है.’
श्रीकांत वर्मा ने उन जीवन-संदर्भों को अपने तीक्ष्ण इतिहास बोध से और अधिक धार दी. उनकी सर्जना की भाव-भूमि का स्रोत क्या था? उन्होंने स्वीकार किया-
‘मेरे चारों ओर मृत्यु थी. गरीबी, भुखमरी और असहायता से उत्पन्न मृत्यु नहीं, बल्कि एक ऐसी मृत्यु जिसे सैकड़ों नामों से पुकारा जा सकता है. आत्म-निर्वासन, सामाजिक पलायन, प्रेम-विफलता, मूल्यहीन संसार में जीने का एहसास, चारों ओर ‘मारो’ या ‘मार दिया गया’ का शोर. इन सबके बीच एक निर्दोष बौद्धिक रचना करने के लिए मैं और मेरे चारों ओर की परिस्थितियां यही थीं.
मैंने लिखकर, फिर चाहे वे कविताएं हों या कहानियां, जीवन और मरण को ही सहस्त्रों व्यंग्यों और पात्रों के रूप में याद किया है… जैसे तुलसीदास ने लिखा है कि उन्होंने लिखा नहीं है, सिर्फ राम का स्मरण किया है.’ [पृष्ठ 456, रचनावली खंड 1, राजकमल प्रकाशन]
उनके साहित्य में जीवन-मरण का यह स्मरण किसी प्रकार के रहस्यवाद से परे है. बात सीधी-सपाट है. आदमी अपने ‘रक्तचाप’ से मरता है. अपने ‘पाप’ से नहीं.
श्रीकांत वर्मा का यह वक्तव्य उनकी कविताओं और अन्य साहित्य को जान सकने का सूत्र है. इस सूत्र को सामने रखकर उनकी कविता के माध्यम से आधुनिक मनुष्य का संत्रास, उसका संघर्ष और हर पग विसंगतियों से आवेशित जीवन-बोध बिलकुल नग्न वस्तविकताओं के साथ प्रकट होता है.
उनकी कविता सिर्फ प्रलाप की कविता नहीं रहती. वह कटाक्ष की कविता बन जाती है. लेकिन उग्र नहीं करुण कटाक्ष की. यह करुण कटाक्ष उग्र और उत्तेजित वक्तव्य से अधिक मर्मांतक है.
‘मुझे मृत्यु ने दबोचा
मुंह दबाये कुछ देर खपरैल- खपरैल चलती रही
दर्शकों ने सोचा-
गया
मगर तभी मृत्यु ने बिना किसी वजह
मुझे छोड़ दिया
छोड़ा तो क्या मुंह से गिरा दिया
दर्शकों की करुणा निराशा में बदल गयी.
भीड़ छंटने लगी
मैंने पुकारा रुको
मगर फ़िजूल !
मैंने कहा-
सुनो तो भाइयो !
मैं अभी मरा नहीं हूं
… मगर फ़िजूल
तब मैंने कहा-
रुको, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है
रुक गए पैर
अपने और गैर
दोनों मेरी ओर मुड़ पड़े
मैंने कहा
सबको मरना है
यह सुनते ही
भीड़ मुझ पर झपट पड़ी…
[पृष्ठ 424, रचनावली खंड 1, रचनाकाल 1984]
पूरी कविता एक गतिक बिंब है! समाज के निपट अनैतिक और मूल्यविहीन होते जाने का एक गतिक बिंब! मृत्यु को तमाशे में बदल देने वाले समाज की बेपर्दगी. यह मूल्यहीनता देशज नहीं, सर्वत्र है.
मृत्यु की छाया में बीसवीं सदी के यूरोप ने अपना यौवन काटा. अस्तित्व काल से सिमटकर एक क्षण में कैद हो गया. इसे केवल एक संयोग नहीं कहा जा सकता कि पतन और निरर्थकता पर दो बड़ी रचनाएं, बीसवीं सदी के तीसरे दशक में अभिव्यक्ति की दो अलग-अलग विधाओं में लगभग स्वतंत्र लेकिन एक साथ रची गयीं.
ओस्वॉल्ड स्पेंगलर की ‘द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट’ 1918 में और टीएस इलियट की ‘द वेस्टलैंड’ 1922 में. इलियट को आभास भी नहीं था कि खंदकों की एक लंबी दुनियावी जंग लड़कर भी यूरोप अभी थका नहीं था. उसमें युयुत्सा यानी युद्ध की अभिलाषा शेष थी. घृणा बची रह गयी थी अन्यथा वह अपनी लंबी कविता अंत का उपनिषदों में व्यक्त ‘Shantih, Shantih, Shantih!’ (शांति, शांति शांति) लिखकर न करते!
श्रीकांत वर्मा की कविता में बीसवीं सदी के मनुष्य के युद्धविलास का चित्रण उन्हें अपने समकालीन मित्र-लेखकों से दूर ले जाता है. वह स्थानबद्ध नहीं रहते .’नींद में चलता हुआ’ यूरोप देखते हैं, शांति मोरपंख की तरह किताब में रखी हुई है और ‘पृथ्वी की एक-एक सड़क पर आदमी भाग रहा है. युद्ध पीछा कर रहा है.’ कवि लिख रहा है लेकिन वह थक जाता है. कलम को किनारे सरका देता है. हताश हो कहता है-
‘संभव नहीं है
कविता में वह सब कह पाना
जो घटा है बीसवीं शताब्दी में मनुष्य के साथ!
कांपते हैं हाथ!’
उनके समकालीन एलेन गिन्सबर्ग ‘Hum Bom!’ में लिखते हैं-
‘What do we do?
You bomb!You bomb them!
What do we do?
We bomb! We bomb you!
What do we do?
You bomb! You bomb you!’
(1971)
बीसवीं सदी में ‘बम’ की इस निर्णायकता के बीच वह इतिहास के अपवादों और शांत ‘अवकाश-प्रिय’ स्थलों को अपने यात्रा-संस्मरणों में एक अलग नज़रिए और भाषा के साथ देखते हैं. स्वीडन में घूमते हुए वह उसे शेष यूरोप से भिन्न एक व्यक्तित्व देते हैं. एक मछुए का व्यक्तित्व.
वह अपनी डायरी में लिखते हैं-
‘स्वीडन यूरोप का हिस्सा नहीं लगता. स्वीडन की जनता को यूरोप की गतिविधियों से अधिक समुद्र और मछलियों में दिलचस्पी है. स्वीडन समुद्र के किनारे बैठे हुए एक मछुए की तरह है, जिसके पास अनंत अवकाश है.’
यूरोप और उसकी संस्कृति पर उनके यात्रा संस्मरण कुछ ऐसे लिखे गए हैं कि आप उन्हें पढ़ते-पढ़ते यूरोप के इतिहास की बर्बरता और उसके सांस्कृतिक प्रदेय को एक चलचित्र की भांति सामने से देखते हुआ महसूस करते हैं.
1984 में ‘मगध’ प्रकाशित हुआ जो उनका अंतिम कविता-संग्रह था. इस काव्य संग्रह की अधिकांश कविताओं के शीर्षक या तो प्राचीन ‘गणराज्य’ हैं या ऐतिहासिक आख्यानों के नायक.
माया-दर्पण और जलसाघर का विप्लव ‘मगध’ में आते-आते तिरोहित हो जाता है. ‘मगध’ की कविताओं में मानो वह स्वयं ‘अनंत अवकाश पाए हुए किसी मछुए’ में बदल जाते हैं जिसके पास कोई हड़बड़ी नहीं, कोई अधैर्य नहीं. अतीत वर्तमान में मिल जाता है. कविताएं शब्द मात्र न रहकर किसी स्ट्रीट फोटोग्राफर द्वारा ली गई तस्वीरों में बदल जाती हैं.
प्रकाश और अंधकार की छायायों के मध्य शब्दों के फ़्रेम में क़ैद अतीत और समकालीनता के आंखों देखे ब्योरे, जो अपने आप में समग्र हैं. जिन्हें समझने के लिए न आगे के अंश की आवश्यकता न पीछे के अंश की.
अपने ‘काल’ से दो वर्ष पूर्व 1984 की शीत ऋतु में 30 जनवरी को ‘मगध’ के बारे उन्होंने अपनी डायरी में लिखा-
‘अवंती, मालवा, उज्जयिनी, क्षिप्रा, चम्पा, काशी, कौशाम्बी, कपिलवस्तु, कोसल, कलिंग, आम्रपाली, चंद्रगुप्त, बिंबसार, अशोक, अजातशत्रु- पात्रों चरित्रनायकों, नगरों, स्मृतियों का एक रेला है जो चला आ रहा है. एक भीड़ है जो उमड़ी पड़ रही है. इनका मुख्य सरोकार है- मृत्यु, संहार, नैतिक क्षय. इन कविताओं का संग्रह दो महीनों में लिख दूंगा. नाम होगा-मगध. मैं जानता हूं, मगध क्या है? कालातीत काल!
श्रीकांत वर्मा का साहित्य आधुनिक मनुष्य और ‘काल’ के मध्य ठने मल्लयुद्ध का साहित्य है जिसमें कभी एक भारी है तो कभी दूसरा. इतना अवश्य है कि यह मल्लयुद्ध अनिर्णीत है. न काल थका है न मनुष्य उससे लड़ते हुए निढाल हुआ है.
वह ख़ुद इससे लड़ते हुए पराजित न हुए थे. जीने की इच्छा रखना मोह नहीं अभिलाषा है. ‘मित्रों के सवाल’ के जवाब में उन्होंने अपने जीवन के आखिरी क्षणों में एक कविता लिखी जो इस तरह थी-
‘मित्रो !
यह कहने का कोई मतलब नहीं
कि मैं समय के साथ चल रहा हूं
सवाल यह है कि समय तुम्हें बदल रहा है
या तुम समय को बदल रहे हो
मित्रो!
कहना कोई अर्थ नहीं रखता
कि मैं घर आ पहुंचा
सवाल यह है
इसके बाद कहां जाओगे?
[मित्रों के सवाल, श्रीकांत वर्मा, रचनाकाल 1984]
(लेखक भारतीय पुलिस सेवा में उत्तर प्रदेश कैडर के अधिकारी हैं.)