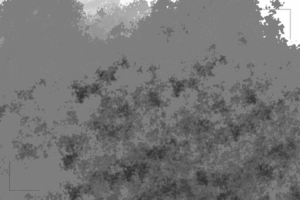मृणाल सेन का सिनेमा कलात्मक और बौद्धिक संवेदना का नायाब संयोजन था. वह चाहते थे कि सिनेमा उपेक्षितों के पास और सुदूर देहातों में पहुंचे. उन्हें ‘नए सिनेमा’ से यह उम्मीद थी. उनकी फिल्म देखने के बाद बहुत देर तक उसकी छवियां बेताल की तरह सिर पर नाचती रहती हैं.

‘सत्य जेब में रखकर घूमने की चीज़ नहीं है. असल सवाल उसे ढूंढने का है’. कलकत्ता की नेशनल लाइब्रेरी (जो स्वतंत्रता पूर्व इम्पीरियल लाइब्रेरी के नाम से जानी जाती थी) में बैठकर मृणाल सेन ने एलीयो विटोर्नी नाम के अपने मित्र को लिखे गए एक ख़त की इन पंक्तियों को मैंने पढ़ा था.
विटोर्नी (1908-1960) 20वीं सदी के प्रख्यात इतालवी लेखक और उपन्यासकार थे. साधारण सी दिखने वाली पंक्तियां सेन को प्रतिबद्धता के स्तर पर आत्ममंथन की गहराइयों में खींच ले गईं.
‘I felt confused. I withdrew into my own thoughts and seeking silence, questioned myself as I had done often in the past, ‘Am I going in the right direction?’
मृणाल सेन ने अपनी जीवन-यात्रा में बरती गई उस सावधानी की ओर ‘जो सही दिशा में जाने के’ नज़रिसे से जुड़ी हुई थी, इशारा किया.
‘So it has been. Checking and double checking-on my journey through life.’
(See: p.9 An uncertain journey, Mrinal Sen’s paper read at National institute of Advanced studies,Bangalore.1994 Seagull Books,2018)
अविभाजित भारत के फ़रीदपुर (अब बांग्लादेश में) में वर्ष 1923 में मृणाल सेन का जन्म हुआ था. 30 दिसंबर 2018 को अपने जीवनकाल में मृणाल सेन ने कुल 28 फिल्मों का निर्देशन किया.
1956 में बांग्ला भाषा में आई ‘रतभोर’ उनकी पहली फिल्म थी. आम आदमी और उसके जीवन संघर्ष को कलात्मक सौंदर्य का वास्तविक प्रेरणास्रोत मानकर उसे कैमरे की रील के बीचोबीच स्थान देने के विचार से लबरेज़ यूरोपीय सिनेमा के लिए 50 का दशक नव-यथार्थवादी सिनेमा का दशक था.
विश्व-युद्धोत्तर परिवेश में बड़े-बड़े स्टूडियो में फिल्म बनाने की संस्कृति धराशायी हो चुकी थी. नई सोच ये थी कि कैमरे को ठीक उन्हीं तंग गलियों, फुटपाथों और कार्य-स्थलों पर ले जाया जाए जहां साधारण मनुष्य का यथार्थ घटित होता है.
रॉबर्ट रोसलीनी की ‘रोम ओपन सिटी’ और विटोरियो द सिका की चर्चित फिल्म ‘बाइसकिल थीव्स’ इस विचारधारा की प्रतिनिधि फिल्में थीं. वैचारिक और राजनीतिक स्तर पर यह उथल-पुथल भरा समय था.
ऊपर से कलकत्ते का माहौल जो मृणाल सेन का ‘एल डोरादो’ (El Dorado) था और जहां, बकौल स्वयं मृणाल सेन ‘रहते हुए राजनीतिक विचारों से अप्रभावित रह सकना असंभव’ था.
मृणाल सेन को इप्टा के नाटक देखने का शौक लग गया, लेकिन वो जगह जिसने आगे चलकर मृणाल सेन के सिनेमा को बौद्धिक कलेवर से सराबोर किया कोई स्टूडियो या स्टेज न होकर कलकत्ता की नेशनल लाइब्रेरी थी.
किताबें ख़रीदने के पैसे नहीं होते थे. सेन घंटों लाइब्रेरी में बैठे किताबें पढ़ते. उन्होंने क्या न पढ़ा! हैरानी होती है! उन्होंने फ़िरदौसी के शाहनामा का फ़िट्जजेरल्ड द्वारा किए गए अनुवाद के सभी चौदह वॉल्यूम पढ़ डाले.
नीत्शे की चर्चित कृति दस स्पेक जरथुस्त्र (Thus spake Zarathustra).. राल्फ़ फ़ॉक्स (1900-1937) की रचना नॉवल एंड द पीपल और क्रिस्टफ़र कॉडवेल (1907-1937) की एस्थेटिक्स पर लिखी गई ‘इलूज़न एंड रियलिटी’.
एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि इन दोनों किताबों ने उन्हें बहुत गहराई से प्रभावित किया. 1946 आते-आते मृणाल सेन विपुल अध्ययन कर चुके थे.
यहां तक कि चेक उपन्यासकार और लेखक कैरल चेपक (karel capek) जिससे वह बहुत प्रभावित थे, के उपन्यास ‘द चीट’ (1938) का उन्होंने बांग्ला में अनुवाद कर दिया. ये वही कैरेल थे जो सात बार साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए नामित हुए थे और जिन्होंने अपने साहित्य में पहली बार ‘रोबोट’ शब्द का प्रयोग किया था.
यथार्थ की व्याख्या पर वह केवल पश्चिम के लेखक ही नहीं पढ़ रहे थे. अपने मिट्टी के लेखन को भी उन्होंने उसी शिद्दत से पढ़ा. किसी भी भाषा में लिखे जा रहे समकालीन साहित्य से वह पूरी तरह परिचित रहते थे.
उन्होंने अपनी मृत्यु से ठीक एक वर्ष पहले मुंशी प्रेमचंद के लिखे गए लेख ‘महाजनी सभ्यता’ को भी पढ़ा. 1977 में मुंशी प्रेमचंद की कहानी ‘कफ़न’ से प्रेरित होकर उन्होंने तेलुगू में ओक ओरी कथा (oka ori katha) नाम से फ़िल्म बनायी.

एक अलग भाषा और एक अलग लैंडस्केप में बनाए गए इस सिनेमा के निर्माण में आने वाली भाषाई और अन्य समस्याओं पर पूछे जाने पर सेन ने जवाब दिया.
‘भाषा और भूगोल चाहे जितना भी अलग हो. मैं जिस तरफ़ भी जाऊं एक ग़रीबी है जो मुझे हर जगह समान रूप से दिखती है.’
1958 में उन्होंने ‘नील आकाशेर नीचे’ बनायी. लेकिन तमाम प्रशंसा के बावजूद इसकी ‘ओवर-सेंटिमेंटल’ टोन उन्हें स्वयं नहीं भाई. 1960 में उन्होंने कन्हाई बसु की कहानी पर आधारित बाइसे श्रावण (Baishey Sravan) का निर्देशन किया.
पहली दो फ़िल्मों से असंतुष्ट सेन की यह पहली फिल्म थी जिसने उन्हें अच्छा महसूस कराया. फिल्म का कथानक 1943 के बंगाल के भीषण अकाल की पृष्ठभूमि और उसके बीच एक पति-पत्नी के आपसी संबंधों पर आधारित था.
पूरी फ़िल्म में मृणाल सेन का कैमरा इंडोर रहकर इंसानी रिश्तों के बीच में मौजूद दरारों की पड़ताल करता है. सेन केवल केवल एक लम्बा आउटडोर शॉट लेते हैं- रोटी की तलाश में भूख से बेहाल किसानों का अपना गांव छोड़ने का दृश्य.
इस दृश्य के अलावा मृणाल सेन अकाल के किसी अन्य विद्रूप को कैमराबद्ध नहीं करते. उन्हें जो कैमराबद्ध करना था, वह स्वयं उनके अनुसार था- ‘Slow but inevitable liquidation of every last vestige of human decency was what I had aimed for.’
(See: p.4 Mrinal sen,Montage: life,Politics,Cinema,Seegull books,2002)
फिल्म वेनिस फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीन की गई. कुछ समीक्षकों ने फिल्म से एक दृश्य हटाने को कहा. अकाल में तीन दिन तक कुछ न मिलने के बाद जब खाना मिलता है तो यह पति अपनी उंगलियों में डुबा-डुबाकर खाता है और फिर उंगलियों को चाट कर खाना चट कर जाता है.
पत्नी सामने बैठी है लेकिन उसकी चिंता किए बग़ैर भूख के दुर्दम आवेग में वह सब कुछ डकार लेता है. आयोजकों ने कहा कि फिल्म का ये ख़ास शॉट ‘नौशियेटिंग’ (Nauseating) है.
पश्चिम के दर्शक में तो यह बहुत जुगुप्सा का भाव पैदा करेगा. सेन ने यह शॉट हटाने से मना कर दिया. यह उनका खोजा हुआ यथार्थ था जिसका सामने का हिस्सा (facade) बाहर की दिख रही दुनिया से अलग था. उस हिस्से में ऊब और हताशा थी. जीवन के अंतर्विरोध और मध्यमवर्गीय दिनचर्या का नीरस अकेलापन था.
सरकारी बस के एक कमज़ोर हत्थे पर झूलकर सफ़र करने का जोखिम लेते हुए बेरोज़गार थे. बेसाख़्ता भागती हुई सड़कें थीं. खुले आसमान में रात बसर करते हुए मूक चरित्र थे और ‘कलकत्ता 71’ (सेन द्वारा निर्देशित फिल्म,1972) के क्लाइमैक्स शॉट में देश की ग़रीबी पर चर्चा करते हुए सेठ लोग थे. ये मृणाल सेन निर्मित सिनेमा का यथार्थ था.
1969 में मृणाल सेन ने ‘भुवन शोम’ का निर्माण किया. भुवन शोम को भारत में फ्रेंच सिनेमा की ‘न्यू वेब’ की तर्ज पर ‘न्यू सिनेमा’ की शुरुआत माना जाता है. फिल्म का बजट एक लाख रुपये था लेकिन तब भी उसमें कोई पैसा लगाने को तैयार नहीं था.
बाद में सेन ने यह फिल्म सरकारी फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन की मदद से बनाई. भुवन शोम बांग्ला कहानीकार बलाईचंद मुखर्जी की कहानी पर आधारित थी. फिल्म के नायक शोम बाबू रेल महकमे में एक सख़्त और अनुशासन प्रिय अधिकारी हैं जिन्होंने अनुशासनहीनता करने पर अपने अधीन रेलवे में ही काम करने वाले अपने बेटे तक को नहीं छोड़ा.
एक विधुर का जीवन जी रहे शोम बाबू के जीवन में सब कुछ शुष्क है. फिर एक दिन वह अपनी ऑफिस की चाहरदीवारी की दुनिया से बाहर निकलता है और चिड़ियों के शिकार के लिए कच्छ के इलाके में जाता है.
वहां पहुंचकर वह गांव की एक चंचल युवती से मिलता है. युवती का पति भी रेल में कर्मचारी होता है जिसके दंड की फाइल शोम बाबू की मेज पर होती है. युवती इस तथ्य से अनजान है लेकिन शोम बाबू को पता चल जाता है कि जिस युवती की मदद और मेहमाननवाज़ी का वह आनंद ले रहे हैं, उसके ही पति का मामला उनके विचाराधीन है.
शोम बाबू का जीवन को क़ानून के एक-एक अक्षर के साथ मिलाकर जीने का नज़रिया बदलने लगता है. देहात का धूल-धूसरित जीवन और निर्दोष आग्रहशील सौंदर्य उनकी सख़्तमिज़ाजी पर विजय पा लेता है.
रेलवे के सख़्त नौकरशाह शोम बाबू फिल्म के क्लाइमैक्स दृश्य में एक अल्हड़ बच्चे बन जाते हैं. युवती के पति को एक चेतावनी देकर क्षमा कर देते हैं.
साधारण से दिखने वाले इस कथानक में उत्पल दत्त के निभाए गए शोम बाबू के किरदार ने फिल्म को ऐतिहासिक बना दिया. एक लाख रुपये के कुल बजट में बनी इस फिल्म ने सिनमा में एक नए विमर्श को आरम्भ किया. पूरी फिल्म एक नए प्रकार के ह्यूमर को स्थापित कर रही थी जो अब तक के सिनेमा में गायब था. यह परपंरागत हंसोड़ कॉमडी से अलग था.
मृणाल सेन की फिल्मों की थीम में गुमशुदगी का अपना महत्व है. सामान्य रूप से चल रहे जीवन से अचानक कोई एक व्यक्ति अनुपस्थित हो जाता है. एक मिडिल क्लास परिवार में यह अनुपस्थिति एक दुर्घटना की तरह आती है.
1970 में मृणाल सेन ने बांग्ला में एक फिल्म बनायी- इंटरव्यू. नायक एक बेरोज़गार युवा है. जैसे-तैसे कर के अपने एक परिचित की मदद से वह एक विदेशी कंपनी (जैक्सन एंड कंपनी.) में इंटरव्यू देने की जुगत लगा लेता है लेकिन कंपनी का ड्रेस कोड है- सूट-पैंट.
उसके पास जो एक जोड़ी सूट पैंट थे वह संयोग से लॉन्ड्री वाले के पास था और उस दिन कलकत्ता में लॉन्ड्री वालों की हड़ताल है. एक अदद सूट-पैंट पाने के लिए बेरोज़गार युवक दिन भर जद्दोजहद करता है.
एक दोस्त के यहाँ वह सूट पा लेता है, लेकिन बस में घर-वापसी के दौरान एक पचड़े में पड़कर वह उसी बस में सूट भूल जाता है. धोती-कुर्ता ही अब एक विकल्प रहता है. वह जाता है और इसी बिना पर बाहर कर दिया जाता है.
यह जीवन से कोट-पैंट की अनुपस्थिति है जिसका परिणाम बाहर की दुनिया में एक नए प्रकार का अस्वीकार और बहिष्कार है. लेकिन जीवन से अचानक से अनुपस्थित हुई चीज़ एक जीता-जागता इंसान हो तब?
इस अनिश्चितता के साथ मिडिल क्लास जीता है. कोई एक उनके बीच होता है जिसकी उपस्थिति का मूल्य तब समझ में आता है जब ‘एक दिन अचानक’ वह हमारे बीच नहीं रहता.
मृणाल सेन ने इस थीम पर 1979 से लेकर 1982 के बीच में तीन फिल्में बनाईं जो ‘ऐब्सेन्स ट्रायोलॉजी’ के रूप में जानी जाती हैं. इन तीनों फिल्मों में घर का कोई न कोई सदस्य एक दिन चला जाता है.

‘एक दिन अचानक’ (1989) में यह जाना स्थायी रूप से है. जाने वाला वापस नहीं लौटता. ‘एक दिन प्रतिदिन’ (1979) में जो गया है वो घर की वह बड़ी लड़की है जो ख़ुद बाहर नौकरी करके एक बड़े परिवार का पेट भरती है. वह जब देर रात तक नहीं लौटती तो उस स्थिति में लड़की होने के कई सारे नतीजों और पड़ोसियों की प्रतिक्रियाओं से गुज़रती है.
इस थीम पर तीसरी फिल्म ‘ख़ारिज’ है जिसमें ग़ायब होने वाला चरित्र घर का एक नाबालिग नौकर है जो आत्महत्या कर लेता है. इन तीनों ही फिल्मों में मृणाल सेन मध्यमवर्गीय सामाजिक मूल्यों के बनावटी दोहरेपन, लैंगिक विद्वेष और उस जीवन में पसरी हुई मीडीयोक्रिटी को सतह पर लाते हैं.
‘कलकत्ता 71’ की शुरुआत श्रीकांत वर्मा की कविता के माफ़िक़ होती है. भूखे-बिलबिलाते बच्चे, गाड़ियों में ठूंस कर भरे गए लोग, दंगे-फसाद… पुलिस की कार्यवाहियां… ऊंची इमारतें और डिस्को में नाचते सम्पन्न युवा.
कांच के बॉक्स में रखा गया जैक्सन का पुतला उनकी फिल्म ‘इंटरव्यू’ में आता है. वह ‘कलकत्ता 71’ में भी आता है. कथा नायक जो एक बेरोज़गार नौजवान है, उस पुतले को खींचकर एक पत्थर मारता है.
घर में जितने लोग हैं,उससे अधिक बर्तन घर की चूती हुई छत के नीचे रखे गए हैं. बारिश ज़ोरों पर है. घर का मालिक एक ग़रीब मज़दूर अधेड़ पति एक पल के लिए बारिश को रात का संगीत समझता है कि तभी ज़ोर से छत का एक टुकड़ा नीचे गिरता है. अफ़रातफ़री क़ायम होती है. नीचे मां की गोद में बच्चा सोता रहता है.
मृणाल सेन की फिल्मों का संसार जीवन में व्यापी इसी अफ़रातफ़री को क़ैद करने का संसार है. उनकी फिल्मों की एस्थेटिक्स कला-सिद्धांतों की एक प्रगाढ़ बौद्धिक समझ और आमजन के प्रति एक प्रभूत सहानुभूति का परिणाम थी.
जिस समय हिंदी फिल्मों के नायक 10 लाख रुपये के मेहनताने में फिल्मों में अभिनय करने को तैयार होते थे, मृणाल सेन केवल एक लाख रुपये से एक ऐसा चरित्र गढ़ सके थे जिसने भारतीय सिनेमा में सिनेमाई समझ का एक नया दस्तावेज़ तैयार किया था.
सिनेमा में प्रतिबद्धता पर जिस तरह एलीयो विटोर्नी की कही पंक्ति को वह अपनी कला की कसौटी बना सकते थे, उसी तरह उनकी कैमरे की फोटोग्राफी का दर्शन महान रूसी फिल्मकार आइजेंस्टाइन से प्रभावित था.
वह जानते थे कि कैमरे को रोशनी की ज़रूरत कहां है और कहां अंधेरे की. सिगमंड फ्रायड की यह बात मृणाल सेन दोहराया करते थे. ‘Like Pompeii, memories are never annihilated.’
सत्यजीत रे और ऋत्विक घटक के साथ मिलकर मृणाल सेन भारतीय सिनेमा को दुनिया के बड़े कहे जाने वाले सिनेमा के साथ ले गए. वह भी खांटी समझौता-विहीन भारतीयता के साथ.
सिनेमा उनके लिए केवल आजीविका का स्रोत नहीं था. वह आम आदमी के साथ खोखे पर बैठकर चाय पीते हुए सिनमा रच सकते थे. इस से बड़ी बात यह कि उन्हें पता था कि ज़रूरी नहीं है कि हर फिल्म किसी बड़ी इवेंट को ही फोकस करे. जीवन ‘नॉन-इवेंट्स’ से भरा पड़ा है. हम उन पर क्यों न फिल्म बनाएं?
उनकी फिल्म ‘चलचित्र’ (1981) इसी सोच का परिणाम थी. वह चाहते थे कि सिनमा उपेक्षितों के पास और सुदूर देहातों में पहुंचे. उन्हें ‘नए सिनेमा’ से यह उम्मीद थी.
मृणाल सेन का सिनेमा कलात्मक और बौद्धिक संवेदना का नायाब संयोजन था. इस बात का साक्ष्य यह है कि उनकी फिल्म को अकेले कमरे में बैठकर देखे जाने के बाद जब आप बाहर निकलते हैं तो बहुत देर तक उसकी छवियां बेताल की तरह सिर पर नाचती रहती हैं.
(लेखक उत्तर प्रदेश कैडर में आईपीएस अधिकारी हैं.)