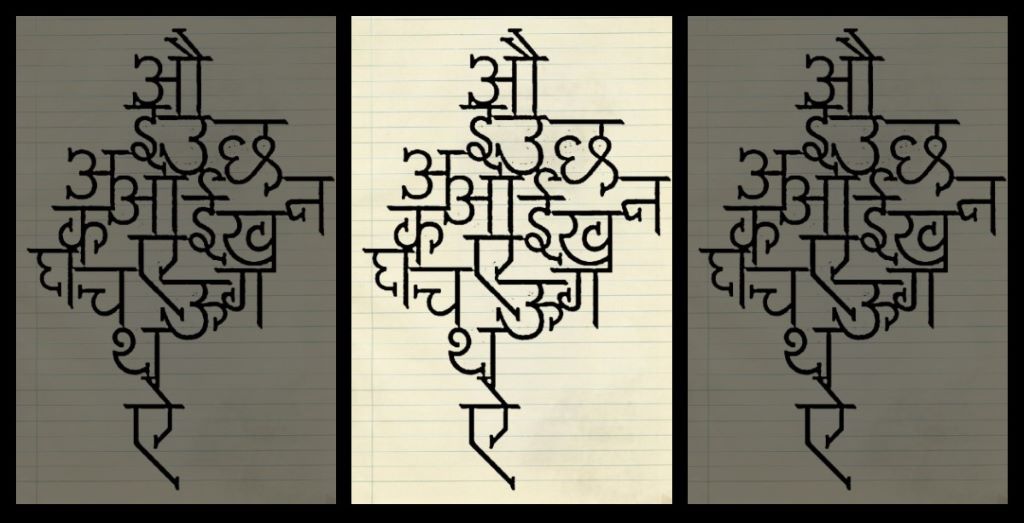निजी प्रसंग से बात शुरू करने के लिए माफ़ी चाहता हूं: हिंदी के हृदय प्रदेश में स्थित एक ‘प्रतिष्ठित’ कान्वेंट स्कूल में पढ़ रही मेरी नातिन को ‘हिंदी डे’ पर ‘एस्से’ लिखना था और उसके माम-डैड व ट्यूटर उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहे थे. फलस्वरूप इतना ‘डिफीकल्ट एस्से’ लिखने को कहने के लिए अपनी मै’म पर गुस्सा उतारती हुई वह मेरे पास आई.
मैंने उसे बताया कि आज़ादी के दो साल बाद 1949 में 14 सितंबर को संविधान सभा में एक वोट के बहुमत से हिंदी को देश की राजभाषा घोषित किया गया था.
चूंकि यह आज़ादी की लड़ाई में उसके योगदान के पुरस्कार जैसा था, इसलिए इससे उसके प्रेमियों की, जिनमें अनेक गैरहिंदीभाषी भी शामिल थे, खुशी का पारावार नहीं रह गया था.
इसके बाद वर्धा की राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ने इस दिन देश भर में हिंदी दिवस मनाने के प्रयत्न शुरू किए, जो सफल हुए तो 1953 में केंद्र सरकार के ऐलान के बाद हर चौदह सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाने लगा.
लेकिन मैंने देखा कि नातिन यह सब जानने को लेकर कतई गंभीर नहीं थी. इमोशनल भी नहीं. वह बस, इतना भर चाहती थी कि मैं जैसे-तैसे उसका एस्से ‘कम्प्लीट’ करा दूं.
हिंदी दिवस की परंपरा
इस बीच उसने एकमात्र यही जिज्ञासा व्यक्त की थी कि जब हिंदी को राजभाषा घोषित करने के चार चाल बाद तक इस दिन ‘हिंदी दिवस’ नहीं मनाया गया तो चार साल बाद इसकी परंपरा डालने की भला क्या जरूरत थी?
मैंने बताया कि देश के उन क्षेत्रों में राजभाषा के प्रचार-प्रसार और उन्नयन को प्रोत्साहित करने के लिए इसकी जरूरत थी, जो तब तक उसकी पहुंच से बाहर थे और इसीलिए 1975 में दस जनवरी को नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ तो उस दिन विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाने लगा. इसके बावजूद वह हिंदी और ‘हिंदी डे’ को लेकर अनिच्छुक व अन्यमनस्क ही बनी रही.
क्यों नहीं बनी रहती, जब हिंदी की जड़ें, और तो और, उसके हृदय प्रदेशों तक में बेहद शातिर ढंग से न सिर्फ काटने बल्कि उनमें मट्ठा डालने का सिलसिला लगातार जारी है.
इसी का फल है कि अब वह इन प्रदेशों में भी एक विडंबना का नाम हो गई है. न उसके लोगों में उसके प्रति गौरव का बोध रह गया है, न अपनत्व और न ही स्वाभिमान का. फलस्वरूप मेरी नातिन जैसे उनके बच्चों का हिंदी माध्यम स्कूलों में पढ़ने जाना गर्व की नहीं, लज्जा की बात हो गई है और इंग्लिश मीडियम अपनाना गर्व की.
इन प्रदेशों का जो समाज अपने को ‘हिंदी’ कहता है, उसकी विमूढ़ता की हद यह है कि वह ढोंग के तौर पर हिंदी को ‘अपनी’ तो कहता है, लेकिन उसकी बेकद्री को लेकर अपने माथे पर शिकन तक नहीं लाता. क्योंकि कद्र की भाषा तो उसके निकट अभी भी अंग्रेजी ही है, क्योंकि सत्ता में हिस्सेदारी का सारा चाक्चिक्य और साहबी उसी में बसती है.
स्वाभाविक ही, यह समाज चाहता है कि उसके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में इंग्लिश में दीक्षित होकर खूब हाय-बाय बोलें और हिंदी पर बस इतनी कृपा करें कि माता-पिता का चरण-स्पर्श करना न भूलें.
हिंदी काम-धंधों और रोजी-रोजगारों के उच्च स्तरों की भाषा नहीं बन पाई
फल यह हुआ है कि हिंदी प्रदेशों में भी हिंदी माध्यम स्कूल और हिंदी के शिक्षक इंग्लिश मीडियम स्कूलों और टीचरों से पनाह मांगने लगे हैं. क्या आश्चर्य कि हिंदी इन प्रदेशों में भी काम-धंधों और रोजी-रोजगारों के उच्च स्तरों की भाषा नहीं बन पाई है. जहां तक सरकारी कामकाज वाली हिंदी की बात है, वह तो खैर हिंदी लगती ही नहीं है.
बेधड़क बनारसी ने कभी इसी स्थिति पर तंज करते हुए लिखा था:
फादर पिता को कह रहा, माता को है ममी, जीवन की कामेडी को बेवकूफ आदमी, क्यों ट्रेजेडी करना रहा है, सोच रहा हूं. ये देश किधर जा रहा है, सोच रहा हूं. इसलिए अब देश व दुनिया के भाषाई परिदृश्य में हुए भारी उलट-पलट की अनदेखी कर हिंदी दिवसों पर ‘भूली-बिसरी’ हिंदी को याद किया जाता है, उसके ‘पिछड़ेपन’ पर आंसू बहाये जाते हैं, दर्शन, ज्ञान-विज्ञान और चिंतन मनन के बजाय, विज्ञापन व बाजार की ही भाषा होकर रह जाने को लेकर चिंताएं जताई जाती हैं और उसके प्रचार-प्रसार के प्रति समर्पण की झूठी-सच्ची कसमें खाई जाती हैं तो हंसी भी नहीं आती.
सरकारी दफ्तरों में मनाए जाने वाले हिंदी सप्ताह, पखवारे या माह वगैरह भी कर्मकांड से ज्यादा नहीं लगते. पिछले दिनों एक पत्रिका में छपा वह कार्टून इस विडंबना को बखूबी चित्रित करता है, जिसमें एक तथाकथित हिंदी प्रेमी हिंदी को साथ लिये सिंहासन के पास पहुंचता है तो उस पर विराजमान अंग्रेजी से प्रार्थना करता है कि आंटी, आज एक दिन के लिए आप उतर जाइये प्लीज़. आज मुझे मम्मी को इस पर बैठाने और माला पहनाने दीजिए. कल आप फिर विराजमान हो जाइएगा.
ऐसे हालात में कोई कहता है कि हिंदी वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ती भाषाओं में से एक और दुनिया की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, जो संयुक्त राष्ट्र की नौ आधिकारिक भाषाओं में भी शामिल है, तो दुष्यंत का शे’र याद आता है : तुम्हारे पाँवों के नीचे कोई ज़मीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यक़ीन नहीं.
हिंदी के ‘भरपूर सबलीकरण’ की बात
सवाल है कि अपने देश में अपने प्रदेशों तक में लगातार अपनी जमीन खोती जा रही हिंदी क्या इसे लेकर आश्वस्त हो सकती है कि कथित रूप से उसका वैश्विक दबदबा बढ़ रहा है? लेकिन कई बार इससे भी आगे बढ़कर नई तकनीकों से हिंदी के ‘भरपूर सबलीकरण’ की बात की जाती है, जबकि इन तकनीकों को ही बहाना बनाकर कई जगहों से हिंदी को विदा कर अंग्रेजी का बोलबाला कर दिया गया है.
तिस पर हिंदी के कई ‘शुभचिंतक’ उसके ज्ञान-विज्ञान व चिंतन-मनन की भाषा न बन पाने को लेकर स्यापा करते हैं तो इस सवाल तक जाते डरते हैं कि जब हिंदी प्रदेशों में ज्ञान-विज्ञान व दर्शन की कोई प्रतिष्ठा ही नहीं है, यहां तक कि संविधान में जरूरी बताये गये साइंटिफिक टेंपरामेंंट की भी कद्र नहीं है, तो वह उनकी भाषा होने का सपना भी क्योंकर देख सकती है?
राजनीतिक प्रवाहों की अनुकूलता व प्रतिकूलता के मद्देनजर ये शुभचिंतक कभी हिंदी की जमीनी हकीकतों व चुनौतियों को झुठलाने वाली अंतिरंजनाओं से काम लेते हैं तो कभी पूर्वाग्रहों से और कभी भी वस्तुनिष्ठ नहीं हो पाते. उन्हें यह सवाल भी निमकौड़ी जैसा लगता है कि आज़ादी के 75 साल भी हिंदी को अपनी स्थिति के लिए राज्याश्रय की मोहताज क्यों होना चाहिए?
क्या ‘संत को कहां सीकरी सों काम, आवत जात पनहियां टूटी, बिसरि गयो हरिनाम’ कहते और ‘नर का मनसबदार’ होने से इनकार करते हुए राज्याश्रय को हमेशा अपने ठेंगे पर रखने वाले भक्त कवियों ने अपने वक्त की प्रतिकूलताओं में भी कुछ कम हिंदीसेवा की थी?
‘हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान’ की जाई संकीर्णताओं से बाहर निकलने का संघर्ष
फिर आज क्यों यह स्थिति बन गई है कि एक वरिष्ठ आलोचक को कहना पड़ता है कि हिंदी में जितने भी महत्वपूर्ण काम हो रहे हैं, उनमें अधिकांश विश्वविद्यालयों व उच्च शिक्षा संस्थानों से बाहर हो रहे हैं और हिंदी के पास अवतार सिंह पाश जैसे अंतिम सांस तक अपनी जनता के संघर्षों में जूझने वाले कवियों या साहित्यकारों का भी अकाल है. तिस पर ‘हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान’ की जाई संकीर्णताओं से बाहर निकलने का उसका संघर्ष भी सफल या खत्म होने के बजाय निरंतर कठिन होता जा रहा है.
हां, उसके ‘विचारकों’ में ऐसे उलाहने देने की परंपरा बहुत समृद्ध है कि देश के दक्षिण के राज्यों के विरोध, नकार या अस्वीकार के कारण ही वह आज तक वास्तविक राजभाषा नहीं बन पाई है, अंग्रेजी रानी और वह नौकरानी बनी हुई है. लेकिन इस पर विचार नहीं किया जाता कि हिंदी प्रदेशों में भी वह अपनी स्थिति बेहतर क्यों नहीं कर पा रही है? इसलिए कि उसका समाज न ठीक से हिंदी पढ़ना चाहता है, न दक्षिण की कोई भाषा.
एक समय इस समाज में ‘अंग्रेजी हटाओ’ आंदोलन चलाए जाते थे, लेकिन अब कहा जाता है कि अंग्रेजी इस देश में रहने के लिए आई है, जाने के लिए नहीं और सारे अवसर व सहूलियतें उसी के नाम हैं.
क्या आश्चर्य कि ऐसे में हिंदी की धरती पर भी उसकी जड़ों में मट्ठा पड़ने लगा है. सवाल है कि ऐसे में उसके आरोहों व अवरोहों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन कैसे मुमकिन हो और इस मूल्यांकन को मुमकिन किए बिना उसकी राह के कांटे कैसे बुहारे जाएं?
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं.)