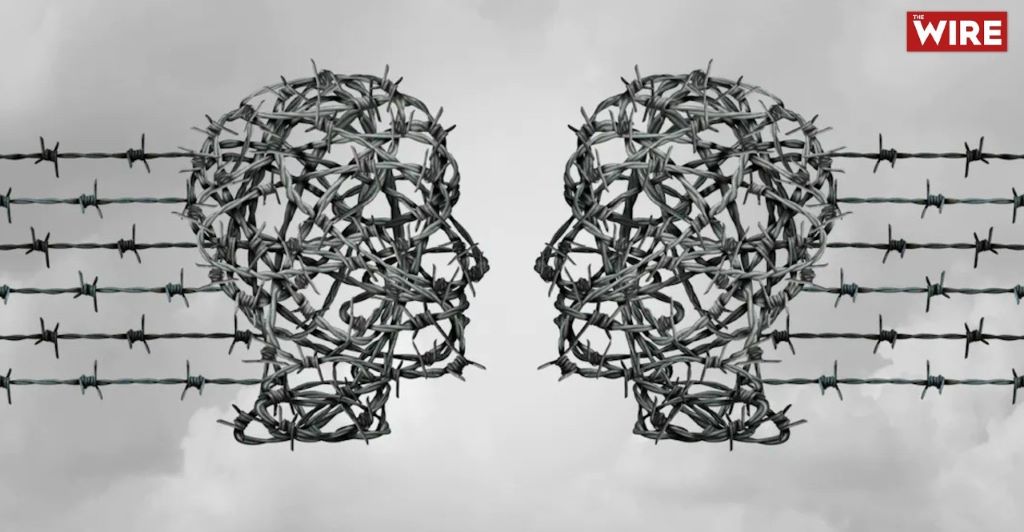परिवार, विद्यालय, धार्मिक संस्थाएं और आधुनिक राज्य- अक्सर सामाजिक व्यवस्था के स्तंभ कहे जाते हैं. लेकिन उन्हें शायद ही कभी उस रूप में पहचाना जाता है, जो वे वास्तव में भी हैं: यह वे पहली प्रयोगशालाएं हैं जहां मनुष्य यह सीखता है कि सत्ता को कैसे देखना है और उसका अनुसरण कैसे करना है. नागरिक मतदान करना सीखने से बहुत पहले आज्ञा मानना सीख लेते हैं.
अनुरूपता को सद्गुण, मौन को अनुशासन और अनुपालन को नैतिक परिपक्वता के रूप में सराहा जाता है. इस ‘व्यवस्था की शिक्षा’ में आज्ञाकारिता केवल प्रोत्साहित नहीं की जाती, बल्कि भीतर तक आत्मसात कर ली जाती है. पर लोकतंत्र केवल आज्ञाकारिता के सहारे जीवित नहीं रहता. वह इस समझ पर टिका होता है कि कब आज्ञाकारिता को ही बाधित करना आवश्यक हो जाता है.
इतिहास हमें याद दिलाता है कि प्रभुत्ववाद शायद ही कभी स्वयं को तानाशाही के रूप में घोषित करता है. वह प्रायः बूटों की आवाज़ और फरमानों के साथ नहीं आता बल्कि वह चुपचाप प्रवेश करता है- कानून, परंपरा, प्रक्रिया और दिनचर्या के वस्त्र पहनकर. जब आज्ञाकारिता को एक निर्विवाद नैतिक गुण मान लिया जाता है, तब सत्ता जवाबदेही से मुक्त हो जाती है और स्वयं को ऐसे पेश करती है जैसे यही कॉमन सेन्स यानी ‘सामान्य समझ’ है. यही वह क्षण होता है जब असहमति लोकतंत्र के लिए बाधा नहीं, बल्कि उसकी बचाने का आख़िरी रास्ता बन जाती है.
असहमति सामाजिक और राजनीतिक जीवन की कोई अपवाद नहीं है; वह उसका मूल सिद्धांत है. अवज्ञा- जब वह सामूहिक, तर्कसंगत और नैतिक रूप से आधारित होती है- वही प्रक्रिया है जिसके द्वारा नागरिक सत्ता की जड़ हो चुकी परतों से अपनी एजेंसी वापस हासिल करते हैं.
लोकतंत्र केवल तब नहीं ढहते जब चुनावों में धांधली होती है; वे तब भी क्षीण होते हैं जब आज्ञाकारिता भागीदारी का स्थान ले लेती है, जब मतभेद को अवैध ठहराया जाता है, और जब सत्ता से प्रश्न पूछना खतरे के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, कर्तव्य के रूप में नहीं.
इस क्षरण की शुरुआत बहुत जल्दी हो जाती है. परिवार तभी लोकतांत्रिक सरोकार सीखने के स्थल बनते हैं जब बड़े संवाद या किसी तरह की बातचीत के लिए जगह छोड़ते हैं. विद्यालय अपने नागरिक दायित्व में विफल हो जाते हैं जब वे आलोचनात्मक नागरिकों के बजाय सिर्फ अनुशासित छात्र का निर्माण करते हैं. जो शिक्षा युवाओं को प्रश्न करने के बजाय केवल याद करने, चुनौती देने के बजाय केवल बात मान लेने का प्रशिक्षण देती है, वह व्यवस्था तो पैदा कर सकती है, लोकतंत्र नहीं.
जो समाज मौन को परिपक्वता समझ लेता है, वह ऐसे नागरिक गढ़ता है जो नियमों का पालन करना जानते हैं, पर अन्याय को चुनौती देना नहीं.
यही तर्क सार्वजनिक जीवन में भी विस्तारित होता है. लोकतंत्र स्वयं को खोखला कर लेते हैं जब असहमति को देशद्रोह के रूप में पुनर्परिभाषित किया जाता है और विरोध को अवांछित शोर कहकर खारिज कर दिया जाता है. ऐसे समय में चुनाव होते रहते हैं, संविधान जीवित रहता है और संस्थाएं कार्य करती हैं- पर जन-सार्वभौमिकता मुरझा जाती है. जो बचता है वह है भागीदारी के बिना प्रक्रिया, न्याय के बिना व्यवस्था और एजेंसी के बिना नागरिकता.
इसलिए नैतिक अवज्ञा केवल एक सांकेतिक चीज नहीं है; वह पुनर्संस्थापन और यहां तक कि पुनर्संरचना का राजनीतिक कार्य है. वह प्रभुत्वशाली कथाओं को बाधित करती है, सहमति के भीतर छिपे बहिष्कारों को उजागर करती है और राजनीतिक क्षेत्र को फिर से खोलती है. यही कारण है कि प्रश्नों को अक्सर ख़तरे के रूप में देखा जाता है.
जिज्ञासा विरासत में मिली सत्ता को अस्थिर कर देती है- और यही वह मील का पत्थर है जहां यह समझना चाहिए कि ‘क्यों’ पूछना स्वयं में प्रभुत्व से इनकार करना है. और जब प्रश्नों को अनुशासन के नाम पर मौन में बदल दिया जाता है, तब लोकतंत्र केवल रूप में बचता है, व्यवहार में नहीं. आज्ञाकारिता अन्याय की मूक साझेदार बन जाती है.
भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में सत्तावादी जनवाद (ऑथरिटेरियन पॉपुलिज़्म) का पुनरुत्थान प्रायः उदार लोकतंत्र से एक नाटकीय विच्छेद के रूप में प्रस्तुत किया जाता है लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है. इसे लोकतंत्र के भीतर होने वाले क्षरण के रूप में बेहतर समझा जा सकता है- एक ऐसा क्षरण जो बाहर से हमला नहीं करता, बल्कि भीतर से खोखला करता है.
चुनाव होते रहते हैं, अदालतें काम करती हैं, संसदें बैठती हैं, पर उनकी आत्मा और सार खाली कर दिए जाते हैं. जो शेष रहता है वह एक प्रक्रियात्मक खोल है, जिसे ऐसी राजनीति जीवित रखती है जो प्रामाणिकता का अभिनय करते हुए आज्ञाकारिता की मांग करती है.
जनवादी नेता शायद ही कभी लोकतांत्रिक रूपों को समाप्त करते हैं; वे उन्हें नए प्रयोजनों के लिए ढाल लेते हैं. संस्थाएं तोड़ी नहीं जातीं, बल्कि अनुशासित की जाती हैं. ‘जनता’ की भाषा अनुरूपता थोपने का औज़ार बन जाती है और असहमति को विश्वासघात में बदल दिया जाता है. राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक आक्रोश और स्थायी संकट की भाषा इन सबको नैतिक आवरण प्रदान करती है. सत्ता स्वयं को घिरी हुई बताती है और इस प्रकार असाधारण उपायों को जायज़ ठहराती है. इस वातावरण में आलोचना को तोड़फोड़ का कार्य घोषित कर दिया जाता है और हल्की-सी अवज्ञा भी राजद्रोह के रूप में चिह्नित की जाती है.
भारत में यह तर्क विशेष रूप से स्पष्ट दिखाई देता है.
– आज्ञाकारिता को आगे बढ़ाते हुए देशभक्ति कहा जा रहा है.
– असहमति को निष्ठाहीनता, आलोचनात्मक चिंतन को अभिजात्यवाद या ‘अर्बन नक्सलवाद’, और अल्पसंख्यक अधिकारों की मांग को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ख़तरा बताया जाता है.
– वैधता अब संवैधानिक नैतिकता से कम और बहुसंख्यक भावनाओं से अधिक प्राप्त की जाती है.
– विश्वविद्यालयों पर दबाव डाला जाता है कि वे पंक्ति में खड़े रहें, मीडिया आत्म-सेंसरशिप की ओर धकेला जाता है, और नागरिक समाज को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है.
– क़ानून, अधिकारों की रक्षा करने के बजाय, अक्सर डराने-धमकाने का औज़ार बन जाता है.
यह व्यवस्था के नाम पर नहीं, बल्कि एक काल्पनिक राष्ट्र के नाम पर मांगी गई आज्ञाकारिता है- एक ऐसा राष्ट्र जो किसी तर्क को सहन नहीं करता.
संयुक्त राज्य अमेरिका में सत्तावादी जनवाद एक विरोधाभासी मुखौटा पहनता है. वह स्वतंत्रता की भाषा बोलता है, पर उन संस्थाओं पर हमला करता है जो स्वतंत्रता को संभव बनाती हैं. चुनाव तभी स्वीकार्य होते हैं जब वे सत्ता की पुष्टि करें. अदालतों, पत्रकारों और विशेषज्ञों को साज़िशकर्ता कहा जाता है जब वे सहमत न हों. स्थायी आक्रोश संरचनात्मक सुधार का स्थान ले लेता है. यहां आज्ञाकारिता राज्य से कम और नेता तथा उसके गढ़े हुए आख्यान से अधिक मांगी जाती है- जो भारत की स्थिति से काफ़ी मिलती-जुलती है.
यूरोप में, विशेषकर उसके पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में, सत्तावादी जनवाद आर्थिक असुरक्षा और सांस्कृतिक चिंता पर पलता है. प्रवासी, अल्पसंख्यक और असहमत बुद्धिजीवी सुविधाजनक शत्रु बना दिए जाते हैं. लोकतांत्रिक संस्थाएं बनी रहती हैं, पर उनका नैतिक आधार क्षीण हो जाता है. जो बचता है वह भय से संचालित एक प्रक्रियात्मक ढांचा है. आज्ञाकारिता को सीमाओं, परंपराओं और काल्पनिक समरूपता की रक्षा के नाम पर उचित ठहराया जाता है.
इन सभी संदर्भों में एक साझा तर्क काम करता है: असहमति तभी तक सहन की जाती है जब वह हानिरहित हो, बिखरी हुई हो या इतनी छोटी हो कि अनदेखी की जा सके. विरोध को छोटा करके अनुमति दी जाती है; प्रतिरोध को प्रबंधित किया जाता है; अस्वीकार को अपराध घोषित किया जाता है. नागरिकों को अपना ग़ुस्सा निकालने की छूट दी जाती है, पर उसे संगठित करने से रोका जाता है. क्रोध को बदलाव की शक्ति नहीं, केवल कैथार्सिस (भावनात्मक निकास) के रूप में स्वीकार किया जाता है.
संदेश स्पष्ट है: शिकायत करो, पर सत्ता को सार्थक ढंग से चुनौती मत दो.
यही समकालीन सत्तावाद की ‘शांत प्रतिभा’ है. वह सबको चुप नहीं कराता; वह विरोध को थका देता है, अलग-थलग कर देता है और पालतू बना देता है. नियंत्रित आक्रोश की अनुमति देकर वह असहमति की राजनीतिक धार कुंद कर देता है. प्रतिरोध को टुकड़ों में बांटकर वह एकजुटता को रोक देता है.
क़ानून को हथियार बनाकर वह दमन को दिनचर्या- यहां तक कि सम्मानजनक- बना देता है. जो व्यवस्था दिखाई देती है, वह वास्तव में लोकतांत्रिक कल्पना का सावधानीपूर्वक संकुचन है. इसलिए ख़तरा केवल मज़बूत नेताओं का उभार नहीं है, बल्कि साहस-रहित लोकतंत्र का सामान्यीकरण है.
जब इनकार को विकृति और अनुपालन को नैतिकता बना दिया जाता है, तो नागरिक सहनशीलता को सद्गुण और सावधानी को बुद्धिमत्ता समझने लगते हैं. समय के साथ भय स्वयं को तर्क की भाषा में व्यक्त करने लगता है. आज लोकतंत्र की रक्षा का अर्थ केवल उसकी संस्थाओं की रक्षा नहीं है, बल्कि ‘ना’ कहने की नैतिक वैधता को पुनः प्राप्त करना है- सामूहिक रूप से, सार्वजनिक रूप से और बिना किसी क्षमा-याचना के. यह आग्रह करना है कि असहमति कोई उपद्रव नहीं, बल्कि स्वतंत्र समाज की जीवनरेखा है.
1960 के दशक के सामाजिक सिद्धांतकार हमें इस गतिशीलता को असहज करने वाली स्पष्टता से समझने में मदद करते हैं.
हर्बर्ट मार्क्यूज़ ने चेतावनी दी थी कि उन्नत समाज किस प्रकार असहमति को हानिरहित रूपों में समाहित कर सहमति का निर्माण करते हैं. सी. राइट मिल्स ने लोकतांत्रिक विकल्पों के रंगमंच के पीछे अभिजात वर्गों के गठजोड़ को उजागर किया. फ्रांज़ फ़ैनन ने दिखाया कि प्रभुत्व कैसे शासितों के मनोविज्ञान को अपने पक्ष में भर्ती कर लेता है, आज्ञाकारिता को आत्म-अनुशासन में बदल देता है. हाना अरेंड्ट ने बताया कि अन्यायपूर्ण प्रणालियों के प्रति साधारण आज्ञाकारिता कैसे नैतिक विपदा उत्पन्न कर सकती है. मिशेल फ़ूको ने प्रदर्शित किया कि आधुनिक सत्ता बल से कम और मानकों से अधिक संचालित होती है- उससे जो ‘उचित’, ‘ज़िम्मेदार’ और ‘सम्मानजनक’ माना जाता है.
सत्तावादी जनवाद इसलिए फलता-फूलता है क्योंकि लोग तानाशाही चाहते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि इसलिए कि बचपन से ही आज्ञाकारिता को नैतिक बना दिया गया है. अनुशासन को ज़िम्मेदारी, मौन को परिपक्वता और धैर्य को सद्गुण बताया जाता है. नागरिकों से कहा जाता है कि वे व्यवस्था पर भरोसा करें, क़ानून मानें और अपनी बारी की प्रतीक्षा करें- यहां तक कि असमानता बढ़ती जाए, निगरानी फैलती जाए और असहमति को अवैध ठहराया जाता रहे.
इसके विपरीत, 1960 के दशक की तथाकथित ‘अवज्ञाकारी पीढ़ी’ कोई रोमांटिक आशावाद नहीं देती, बल्कि एक कठोर चेतावनी छोड़ जाती है: जब असहमति से वैधता छीन ली जाती है, तो लोकतंत्र केवल रूप में बचता है, सार में नहीं. उस दशक की विरासत विद्रोह की स्मृति नहीं, बल्कि एक अधूरी नैतिक परियोजना की ओर संकेत है.आज की समस्याएं- चाहे सत्तावादी जनवाद हो, निगरानी पूंजीवाद, स्थायी आपातकाल या आर्थिक अनिश्चितता- नई तरह की आज्ञाकारिता की मांग पर टिकी हैं. धैर्य रखो, अनुशासित रहो, असहज प्रश्न मत पूछो. भाषा बदल गई है, अपेक्षा वही है.
आज उस अवज्ञाकारी पीढ़ी की भावना को पुनः प्राप्त करने का अर्थ उनके हाव-भाव या नारों की नकल करना नहीं, बल्कि उनके साहस को नया रूप देना है- धारा के विरुद्ध सोचने का साहस, प्रवाह के विरुद्ध तैरने का साहस, और झूठी एकता के नाम पर मांगी गई आज्ञाकारिता से इनकार करने का साहस. 1960 के दशक के विद्रोह युवाओं की उच्छृंखलता नहीं थे, बल्कि सत्ता, अधिकार और लोकतंत्र की गहन पुनर्विचार प्रक्रिया पर आधारित थे.
नागरिक अधिकार आंदोलन से लेकर यूरोप और वैश्विक दक्षिण के छात्र आंदोलनों तक, असहमति को लोकतांत्रिक आवश्यकता के रूप में सिद्धांतबद्ध किया गया. इन सभी हस्तक्षेपों में एक साझा बात थी: व्यवस्था को पवित्र मानने से इनकार. उनका आग्रह था कि लोकतंत्र केवल प्रक्रियाओं से नहीं, बल्कि उन नागरिकों से जीवित रहता है जो सत्ता से प्रश्न करने और अन्याय को बाधित करने को तैयार हों.
आज असहमति को अव्यवस्था और मतभेद को निष्ठाहीनता के रूप में पुनर्परिभाषित किया जा रहा है. एकता की भाषा का उपयोग लोकतंत्र को गहरा करने के लिए नहीं, बल्कि उसे चुप कराने के लिए किया जा रहा है. समर्पण के बदले स्थिरता का वादा किया जाता है, और अन्याय व्यवस्था की भाषा में धाराप्रवाह बोलना सीख जाता है.
आइए हम सामूहिक रूप से इस सरल सत्य की पुनः पुष्टि करें: असहमति के बिना लोकतंत्र स्थिरता नहीं, ठहराव है- और ठहराव अंततः सड़ांध पैदा करने लगता है. जब आज्ञाकारिता को नागरिक सद्गुण बना दिया जाता है, तो अन्याय पीछे नहीं हटता; वह स्वयं को अनुशासित, सम्मानजनक और खतरनाक रूप से सुरक्षित रूप में पुनर्गठित कर लेता है.
(लेखक राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सदस्य हैं.)
(यह लेख मूल रूप से अंग्रेज़ी में फ्रंटलाइन में प्रकाशित हुआ है.)