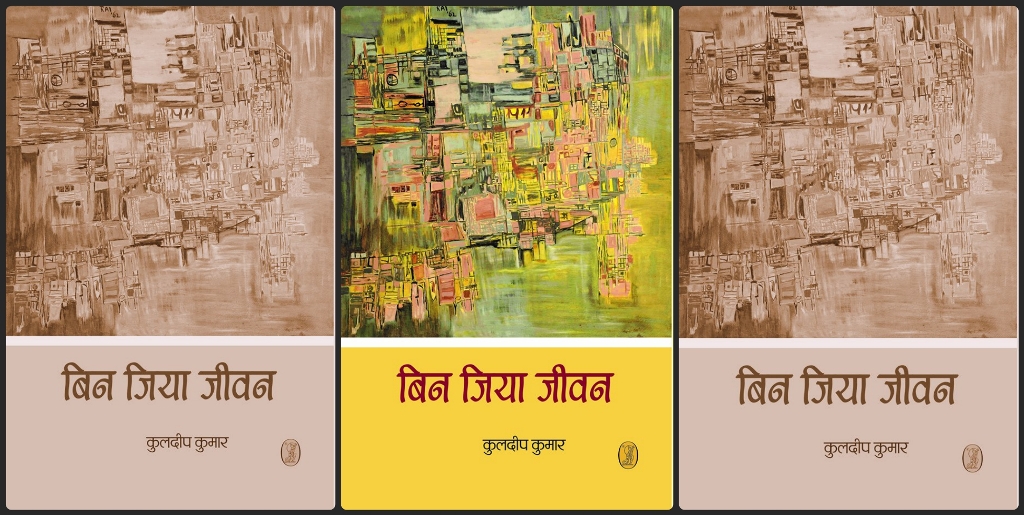कुलदीप कुमार की कविताएं पिछले तीन दशकों में हिंदी पत्र-पत्रिकाओं में आती रही हैं. पत्रकार की हैसियत से वे साहित्य-संस्कृति की जानी-मानी शख्सियतों से बातचीत करते रहे हैं और अक्सर समकालीन साहित्य पर लिखते रहे हैं.
अक्सर हिंदी अदब पर लिखने के लिए उन्होंने अंग्रेज़ी को माध्यम चुना है. जाहिर है कि ऐसे अदीब से यह उम्मीद रहती है कि अपनी मौलिक रचनाओं में वे नई अंतर्दृष्टि की तलाश कर रहे होंगे और अपने पाठकों से इसे साझा करेंगे. हाल में प्रकाशित उनके एकमात्र संग्रह ‘बिन जिया जीवन’ में सादगी के साथ इस उम्मीद को पूरा करने की कोशिश है.
अपनी भूमिका में उन्होंने लिखा है कि कविताओं का चयन मंगलेश डबराल ने किया है. मंगलेश ने भी अपनी भूमिका में कवि से ‘अलग तरह का दृष्टि-बोध’ की उम्मीद रखी है और यह भी कि ये कविताएं ‘उन महत्वाकांक्षाओं से मुक्त होंगी जिनसे समकालीन कविता काफी ग्रस्त नज़र आती है.’
संग्रह में कुल 64 कविताएं हैं. कुछ कविताएं बड़ी शख्सियतों, जैसे ओक्तावियो पाज़, मल्लिकार्जुन मंसूर आदि से प्रेरित हैं. संग्रह की सबसे सुंदर और मन को छू लेने वाली कविताएं वे हैं, जहां कवि निजी स्मृतियों और व्यथाओं को कहता है.
‘मां’ शीर्षक की चार टुकड़ों की लंबी कविता की पंक्तियों, ‘मैं तुम्हारा नाम लेता हूं/ और एक इक्यावन साल लंबा अंधेरा/ चुपचाप सामने आ खड़ा होता है’ में कवि खुद को खूबसूरती से उजागर करता है. ऐसी कविताओं में पाठक कुलदीप कुमार के करीब पहुंच पाते हैं.
ऐसे ही ‘मेरा कमरा’ में ‘मेरे शरीर की तरह यह कमरा भी हिलता है’ जैसी पंक्तियां भरोसा दिलाती हैं कि हम एक अच्छे कवि को पढ़ रहे हैं. इसके उलट शख्सियतों से जुड़ी कविताएं पाठक को खींच पाएंगी, ऐसा हमें नहीं लगता.
मल्लिकार्जुन मंसूर पर पहली कविता इसका अपवाद है. इस छोटी कविता में शास्त्रीय संगीत के इस महान कलाकार की अनोखी मानवीय तस्वीर है. सृजन में डूबे हुए बनाते हुए किसी कलाकार का अपनी दुनिया से अलग बाक़ी संसार के रूबरू होना (‘सुरों के बाहर भी है कोई दुनिया?’) कैसी सुरक्षाएं-असुरक्षाएं ला सकता है, इस पर यह छोटी कविता सादी-सी, पर खूबसूरत टिप्पणी है.
जाहिर है कि कवि किसी और पर टिप्पणी करते हुए खुद और समकालीन कला के जीवन पर भी कह रहा होता है. इस कविता के बरक्स ओक्तावियो पाज़ पर लिखी कविता के कथ्य में लक्षणा का अतिरेक है, जो बचकानी कोशिश में सिमट कर रह गया है – ‘पास बोले मैं पास हूं/ और चूंकि पास हूं/ तो जनाब फिर मैं आपसे मिलूं तो क्यों कर?’ संगीतकारों से कवि काफी प्रभावित लगता है, और यह बात छत्तीस लाइनों की कविता ‘रागदर्शन’ में नौ संगीतकारों और दस रागों के उल्लेख से साफ दिखती है.
क्या इस कविता को पढ़कर पाठक उतना ही ‘सुखी’ हो पाता है, जितना कि कवि बार-बार (पांच बार) कह रहा है , यह अलग सवाल है. अंत में कवि की घोषणा है कि ‘मैंने आज राग देख लिया’ – मुसीबत यह है कि जिस काव्यात्मक तनाव को कवि हम तक पहुंचाना चाहता है, वह नामों और बयानों के अतिरेक से खो-सा गया है. यह अतिरेक एक नाटकीय आत्मकथन-सा लगता है, जिससे जुड़ने के लिए पाठक को सभी संदर्भों पर सोचना पड़ेगा.
इससे बेहतर कविता ‘तिलक कामोद’ है, जो भाव-प्रधान है और हमें संगीत की कविता तक या कविता के संगीत तक पहुंचाती है. संगीत के साज अक्सर दूसरी कविताओं में भी प्रकट होते हैं.
कुछ कविताओं में कुलदीप विरह और मृत्यु-बोध पर दार्शनिक से होते हुए जीवन की नश्वरता पर बुदबुदाते से दिखते हैं. ये कविताएं उनकी निजी व्यथाओं की दूसरी कविताओं जैसी ही बेहतर रचनाएं हैं.
हर दिन जीवन में उपस्थित किसी के अचानक चले जाने और आखिर में कुछ न रहने का आतंक यहां दार्शनिक उलझन बन कर आते हैं, जिनमें पीड़ा है, पर हम इस एहसास को और जानना-सोचना चाहते हैं. सत्य प्रकांड खालीपन लिए सामने आ खड़ा होता है.
इनको पढ़ते हुए एकबारगी हम कवि के आत्मीय हो जाते हैं. पढ़ते हुए बिछोह में कवि और पाठक साथ-साथ सांस लेते हैं. यहां कवि आधुनिक जीवन-शैली से उत्पीड़ित शख्स बन कर सामने आता है, जिसमें जीवन में लगातार कुछ खोते रहने का एहसास है.
भावनात्मक विकार तक ले जाती ये कविताएं जीवन की सच्चाई हमारे सामने ले आती हैं. अपने वक्त में मानवता के खंडित मनोविज्ञान को कहने की कोशिश इनमें है.
इनके बरक्स दूसरी और कविताएं हैं, जहां निहायत ही आम-सी सपाट बातें कही गई हैं, जैसे ‘प्यार में बर्बादी के सिवा कुछ नहीं रखा/ फिर भी प्यार करते हैं/ एक बार नहीं/ कई-कई बार’. आजकल ऐसी बातें किशोरवय स्कूल के बच्चे लिखा करते हैं.
तक़रीबन सभी कविताओं में तरक्कीपसंद वैचारिक प्रवाह है. ‘दहशत’ कविता में बड़ी साफगोई के साथ वे गोरक्षकों के खिलाफ सोच्चार होते हैं. इसी तरह ‘चौकीदार की चिंता’ में अपनी पक्षधरता को साफ लहजे में सामने रखते हैं. आज जब हिंदी पत्रकारिता पर ‘गोदी मीडिया’ जैसे इल्ज़ाम आम हैं, पत्रकारिता से आए कवि कुलदीप की यह साफगोई काबिले-तारीफ है.
आखिरी पांच कविताएं ‘महाभारत व्यथा’ नाम से खंड में अलग रखी गई हैं. महाभारत से लिए गए पांच स्त्री- चरित्रों, माधवी, मत्स्यगंधा, गांधारी, माद्री और द्रौपदी पर केंद्रित ये कविताएं अपेक्षाकृत लंबी हैं. इनमें कवि ने स्त्रीवादी नज़रिया पेश करने की कोशिश में महाभारत के आख्यानों की पुनर्व्याख्या की है.
पर यहां भी पाठक को कोई खास नया नज़रिया नहीं मिलता है. स्त्री उपेक्षिता है, स्त्री भोग्या है, उसकी अपनी कामना को दरकिनार किया गया है, ये बातें इक्कीसवीं सदी में क्लीशे हो गई हैं और वक्त से ज्यादा नहीं तो आधी सदी पीछे हैं.
अंतत: स्त्री जद्दोजहद मेंं पिछड़ जाती है और अक्सर हारना ही उसकी नियति है, कुल मिलाकर इन कविताओं का यही कथ्य है. एक सचेत कवि से उम्मीद रहती है कि उसकी रचनाओं में सामाजिक अवहेलना और राजनीतिक सत्ता के अभाव में उत्पीड़ित मानस की अंतर्मुखी अभिव्यक्ति की गूंज हो.
मसलन संग्रह की आखिरी पंक्तियों में द्रौपदी कहती है- ‘अब हिमालय मुझे अपनी गोद में ले ले/ तो मेरी यात्रा पूरी हो/ अग्निकुंड से हिमशिखर तक की/ अर्थहीन यात्रा…’ इसी तरह ‘माद्री’ कविता में आखिर में माद्री कहती है ‘लेकिन प्रारब्ध से कौन बच सका है/ जो मैं बचूंगी/ विदा.’
पौराणिक या ऐतिहासिक आख्यानों की पुनर्व्याख्या की कोशिश आधुनिक साहित्य में लगातार होती रही है. हिंदी में धर्मवीर भारती का नाटक ‘अंधायुग’, श्रीकांत वर्मा की ‘मगध’ शीर्षक कविताएं और ओडिशा में प्रतिभा राय का उपन्यास ‘द्रौपदी’ इसके उदाहरण हैं.
कविता में भी ऐसी अनेकों कोशिशें होती रही हैं. इसलिए महज आख्यान को और पुराने पड़ चुके पाठ को दुहराने से कोई नई बात बनती नहीं है.
कवि का स्त्रीवादी नज़रिया दूसरी कविताओं में बेहतर दिखता है, जैसे ‘औरत का दर्द’ कविता में ये पंक्तियां देखिए- ‘मैं देखा जाना सहता हूं/ अपने पुरुष होने के अभिमान पर/ लजाता हुआ’. पर ‘महाभारत व्यथा’ की कविताओं में आग्रह ज्यादा दिखता है.
कवि की द्रौपदी युधिष्ठिर को ‘आत्मकेंद्रित, निकम्मा, ढुलमुल स्वभाव’ का और ‘क्लीव’ कहती है. मंच पर कविता पढ़ते हुए वाह-वाही के लिए ऐसे विशेषण काम आ सकते हैं, पर कविता में इनसे क्या मकसद पूरा होता है, यह सवाल रह जाता है.
खासकर हमारे समय में ‘क्लीव’ जैसा विशेषण वैचारिक उलझनें पैदा करता है. फिर भी समकालीन को पौराणिक संदर्भों में देखने की इस कोलाज जैसी कोशिश में हम कवि को बेहतर पहचान पाते हैं.
कहा जा सकता है कि इन कविताओं में नई ज़मीन बनाने की कोशिश है. इन कविताओं में संवेदना है, तरक्कीपसंद बयान हैं, समकालीन चिंताएं हैं, पर अभिव्यक्ति तीन दशकों पहले की है.
सभी कविताएं मुक्तछंद में हैं और कहीं भी ज़बरन तुक और लय गढ़ने की कोशिश नहीं है. कुछ हद तक रघुवीर सहाय की परंपरा में इन कविताओं को देखा जा सकता है.
कहीं-कहीं शब्दों का चयन भी तंग करता है, मसलन ‘… ज्योतित हो उठी’; पर कुल मिलाकर बोलचाल की और सरल भाषा का इस्तेमाल है. बेशक भाषा की सरलता और विषयों की विविधता संग्रह को पढ़ने लायक बनाती हैं.
(लेखक कवि और राजनीतिक टिप्पणीकार हैं.)