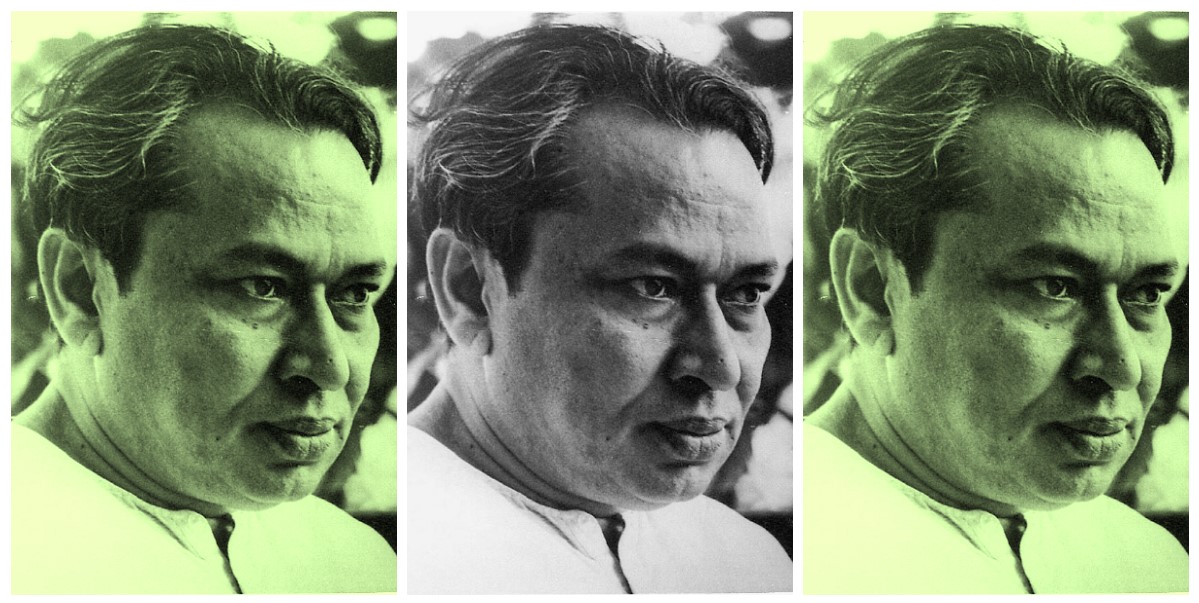राज्य का रुतबा इंसान से बड़ा हो, यह रघुवीर सहाय को बर्दाश्त नहीं. वह इंसान से उसकी आज़ादी की इच्छा छीन लेता है. हर व्यक्ति को आज़ादी का एहसास हो और वैसे मौके ज़्यादा से ज़्यादा पैदा कर सके, जिनमें वह खुद को ख़ुदमुख़्तार देख सके, उसे किसी सत्ता के अधीन और निरुपाय होने का बोध न रहे, यह हर मानवीय उपक्रम और साहित्य का भी दायित्व है.

‘मैं अपनी सारी कविताओं को जोड़ कर रख दूं
बीच-बीच में में रख दूं पत्र, पत्र में फुटकर टीपें,
कहानियां बीस-तीस
सबको मिलाकर एक बन जाएगा समाज?-‘
रघुवीर सहाय ‘मेरा कृतित्व’ शीर्षक कविता में इस प्रश्न का उत्तर देते हैं:
‘नहीं नहीं एक घुमड़ता हुआ दर्द एक खालीपन बोझ भरा.’
यह जो घुमड़ता हुआ दर्द है वह किसी ज़माने में कवि का या कविता का कम नहीं होता क्योंकि कविता जिस मनुष्य या मनुष्यता की तलाश में शुरू हुई होगी, वह कभी पूर्ण हो और कवि के विश्राम का क्षण आए, ऐसा होता नहीं.
फिर जीवन की चुनौती कविता को उसे रचने की उतनी ही बड़ी बनी रहती है:
‘किसी बड़ी कविता की रचना में
मैं जितना फालतू बोझ कम करता हूं
उतना ही मैं हल्का होता हूं
जीवन से बड़ी नहीं हो सकती है रचना
अच्छा लिखने का अभिमान एक बोझ है
भाषा पर लादकर उसे तुम चल न दो.’
कविता वास्तव में संबंधों को समझने और खोजने की अनवरत यात्रा है:
‘हम लोग रोज़ खाते और जागते और सोते हैं
कोई कविता नहीं मिलती है
जैसे ही हमारा रिश्ता किसी से साफ़ होने लगता है
कविता बन जाती है.’
कविता का काम इन इंसानी रिश्तों की खोज (और उसमें कुदरत के साथ उसके संबंध को भी शामिल कर लें) तो है ही, वह उस ‘दर्द’ और ‘आतंक’ को व्यक्त करते रहने का भी है जो जीवन को नष्ट करते हैं लेकिन इस तरह कि मनुष्य को सबल करे:
‘मैं पूछ रहा इसीलिए यह बार-बार
वह दर्द कहां मर गया रोज़ जो होता था
……
आतंक कहां जा छिपा भागकर जीवन से
जो कविता की पीड़ा में अब दिख नहीं रहा?
हत्यारों के क्या लेखक साझीदार हुए
जो कविता हम सबको लाचार बनाती है ?’
इस लाचारी से कैसे लड़ा जाए? उसके लिए ज़रूरी है उस अन्याय को समझना जो राज्य नामक संस्था को प्राकृतिक मान लिए जाने कारण मानवीय अवस्थिति में स्थायी हो गया है.
आश्चर्य नहीं, जैसा कृष्ण कुमार ने ठीक ही नोट किया है, रघुवीर सहाय के लिए ‘राज्य और व्यक्ति के संबंध को, अधिकाधिक समझना आधुनिक संवेदना की शर्त’ थी.
यह राज्य मनुष्य को राष्ट्र के सहारे छोटा बनाए रखता है और उसे उसकी सत्ता के बोध से वंचित कर देता है. राज्य का रुतबा इंसान से बड़ा हो, यह रघुवीर सहाय को बर्दाश्त नहीं.
वह इंसान से उसकी आज़ादी की इच्छा छीन लेता है. हर व्यक्ति को आज़ादी का एहसास हो और वैसे मौके ज़्यादा से ज़्यादा पैदा कर सके जिनमें वह खुद को खुदमुख्तार देख सके, उसे किसी सत्ता के अधीन और निरुपाय होने का ही बोध न रहे, यह हर मानवीय उपक्रम का और इसलिए साहित्य का भी दायित्व है.
यह इंसान को क्षुद्रता और टुच्चेपन से बचाने की लड़ाई है. इस लड़ाई या संघर्ष में जीत का कोई अंतिम बिंदु, इसलिए विश्राम नहीं है तो हार को भी आख़िरी नहीं माना जा सकता.
इसलिए इसका भी उपाय नहीं है हारकर, थककर, यह कहकर कि अब हमारे पास औजार नहीं बचे या उस रूप की कल्पना ही नहीं बची जिसमें जीवन को गढ़ना है, हम बैठ जाएं:
‘जो टूट गया है वह टूटकर खत्म नहीं हो चुका है: वह उसमें मिलकर के कि जो बचा है, टूटकर एक और रूप बन गया है. अब फिर से नया कुछ बनाने के लिए इसी बचे हुए रूप के नए रूप में से पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा ताकत हासिल करनी पड़ेगी. यदि हम इतिहास निर्माण का हौसला नहीं रखते तो हर बार टूटने पर हम कहेंगे कि जो बचा है वह दूषित हो गया है और रक्षणीय नहीं रह गया है.
क्या हमें उन धूर्त बहसों की याद नहीं जो अतीत में अक्सर यह कहकर उठाई जाती रही हैं कि लोकतंत्र या समाजवाद विफल रहा है इसलिए हमारे उपयुक्त नहीं?’
अगर कुछ भी अब बचाने लायक नहीं बचा तो फिर सत्ता के आगे समर्पण ही विकल्प है:
‘एक पूरी जाति अविश्वासियों की पैदा हुई
न्याय के नियमों से जो नहीं डरते
हंसते हैं वे तो डराते हैं.
कहते हैं वे
कि कुछ भी विश्वसनीय नहीं रहा
जीवन में सत्ता के चरणों में किन्तु वे आस्थावान
चढ़े जा रहे हैं
जिन्हें सचमुच जीवन में आस्था है
उनको धकेलते.’
अविश्वासियों की यह जाति जिस ‘उन्नति’ को पूज्य मानती है, वह क्या है?
‘राज्य राज्य सब जगह
कहीं जगह नहीं खाली
इसी तरह बजती है
एक हाथ से ताली
आस पास में पुलिस
सेना पड़ोस में
ऐश में धंसे जन
उतराए अफ़सोस में
मेले में धन लगे
विदेश से मिले साधन
हम उन्नति करते हैं
बार-बार निर्धन बन’
जो बलवान है वही अविश्वासी भी है:’एक समय था मैं बताता था
नष्ट हो गया है अब मेरा पूरा समाज
तब मुझे ज्ञात था कि लोग अभी व्यग्र हैं
बनाने को फिर अपना परसों कल और आज
आज पतन की दिशा बताने पर शक्तिवान
करते हैं कोलाहल तोड़ दो तोड़ दो
तोड़ दो झोंपड़ी जो खड़ी है अधबनी
फिजूल था बनाना जिद समता की छोड़ दो
एक दूसरा समाज बलवान लोगों का
आज बनाना ही पुनर्निर्माण है
जिनका अधिकार छीन जिन्हें किया पराधीन
उन्हें जी लेने का मिलता प्रतिदान है.’
क्या भारत बलवान लोगों का समाज बन जाएगा? भारत ही क्यों, क्या यह दुनिया बलवान लोगों की होगी और बल के सिद्धांत को ही नियम मान लेगी? फिर क्या सिर्फ ‘जी लेने’ को नियति मान लिया जाएगा?
‘हमारी मुठभेड़’ में कवि एक तरह से चुनौती देता है:
‘कितना अकेले तुम रह सकते हो
अपने जैसे कितनों को खोज सकते हो तुम
अपने जैसे कितनों को बना सकते हो
हम एक गरीब देश के रहनेवाले हैं इसलिए
हमारी मुठभेड़ हर वक्त रहती है ताकत से
देश के गरीब होने का मतलब है
अकड़ और अश्लीलता का हम पर हर वक्त हमला.’
इस अकड़ और अश्लीलता के हमले का मुकाबला हमें ही तो करना है! अगर हमने कुछ नहीं किया तो हम इतिहास की जूठन बन कर ही रह जाएंगे:
‘इतिहास का हम करते क्या हैं
जब करते हैं तभी
इतिहास बनता है नहीं तो हम उसके उच्छिष्ट होकर
रहने को बाध्य हैं’
सब कुछ खत्म हो रहा है, यह विलाप जो करते हैं उनके प्रति कवि की कोई सहानुभूति नहीं है:
‘टूटते समाज का रोना जो रोते हैं
उनके कल और परसों के आंसुओं का
प्रमाण मेरे पास लाओ
मुझे शक है ये टूटते समाज में
हिस्सा लेने आए है, उसे टूटने से रोकने को नहीं’
इतिहास को समझने का मतलब है इसे पहचानना कि
‘इतिहास का एक क्षण होता है
जब सारी शक्तियां
मिल जाती हैं उस अपने पक्ष में पलट लेने के लिए
और जिनको उन्होंने निकाल बाहर कर दिया है
धीरे धीरे
उनसे यह कहती है
कि तुम मेरे अधीन होकर रहो
सांप्रदायिकता को मान लो
नहीं मानते हो
सब शक्तियों के आक्रमण सहने को तैयार रहो.’
इन शक्तियों को पहचानना तो ज़रूरी है, यह जानना भी कि अगर पतन से उबरना है तो जाना किधर है? आदर्श क्या है? और वह किस मुकम्मल का हिस्सा है?
‘हम जानते हैं कि पतन अनेक रूप धरकर
हमें क्षय कर रहा है
और हम जानते हैं कि बदलना तो सब कुछ एक साथ होगा
पर समाज को एक साथ बदलने के लिए
एक व्यापक बहुआयामी आदर्श और उतना ही स्पष्ट कार्यक्रम चाहिए.
वह नहीं है इसलिए जनता जाग्रत नहीं हो सकती
तब जनता को उत्तेजित करने के प्रयत्न
हम करते हैं—
व्यापक पतन को विरोध के खंडों में बांटकर
और खंड
विरोध को अकेला और भ्रष्ट करता जाता है.’
उत्तेजना के प्रलोभन से बचना, उस व्यापक मुक्ति के आदर्श की खोज करना यह तब सब हो सकता है जब हम जो है उसे वैसा ही स्वीकार करने की दासवृत्ति से बचें:
‘हमने यह देखा अपनी सब इच्छाएं
रह ही जाती हैं थोड़ी बहुत अधूरी
– यह नहीं कि यह कहकर मन को समझाएं
– यह नहीं कि जो जैसा है वैसा ही हो
यह नहीं कि सब कुछ हंसते-हंसते ले लें
देने वाले का मतलब कैसा ही हो’
(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं.)