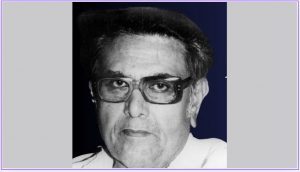आज़ादी के 75 साल: स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका के बारे में काफी कुछ लिखा गया है, मगर उत्तर-पूर्व को आज़ाद भारत के साथ जोड़ने में उन्होंने जिस तरह से नेतृत्व किया, इस बारे में काफी कम लिखा गया है.

(नोट:यह लेख मूल रूप से 15 अगस्त 2017 को प्रकाशित हुआ था.)
ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा, जब भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने महात्मा गांधी को ‘चतुर बनिया’ कहकर पुकारा था. इस टिप्पणी के पीछे शाह का मक़सद क्या था, इसको लेकर कई तरह के विचार समर्थन और विरोध में दिए गए. लेकिन मुझे याद आता है कि मेरे दिमाग में यह विचार आया कि मेरे जैसे उत्तर-पूर्व से आने वाले भारतीयों को इस ‘चतुर बनिया’ का ख़ासतौर पर शुक्रगुज़ार क्यों होना चाहिए?
हक़ीक़त ये है कि अगर नज़दीक से देखा जाए तो ख़ुद शाह को भी सबसे पहले गांधी के प्रति शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि आज़ाद भारत में असम नाम का एक राज्य है, जहां उनकी पार्टी मई, 2016 में हुए चुनावों में जबरदस्त जीत हासिल कर सकी.
भाजपा अध्यक्ष के तौर पर 2015 में बिहार में मिली शिकस्त के बाद असम की जीत ने अमित शाह साख़ बचाने का काम किया.
इस अगस्त में ब्रिटिश भारत के विभाजन के दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण के 72 साल पूरे हो रहे हैं, जिसे हम विभाजन के तौर पर याद करते हैं. उत्तर पूर्व के लोग ख़ुद को भारतीय कहकर पुकार सकें, इस मकसद से विभाजन की ओर बढ़ रहे समय में गांधी द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में सोचने-विचारने का शायद यह उचित समय है.
स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी की भूमिका के बारे में काफी कुछ और विस्तार से लिखा गया है, मगर उत्तर-पूर्व को आज़ाद भारत के साथ भौगोलिक रूप से जोड़ने में मदद करने के लिए असम कांग्रेस को उन्होंने जिस तरह से नेतृत्व दिया, इसके बारे में काफी कम और अपर्याप्त ढंग से लिखा गया है.
उनकी भूमिका को दो बेहद अहम हस्तक्षेपों के प्रिज़्म से देखा जाना चाहिए. गांधी जी ने यह हस्तक्षेप तब किया जब क्षेत्र के स्थानीय लोगों को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी.
अहम बात ये है असम के भौगोलिक चरित्र की रक्षा करने के लिए बयान के तौर पर किए गए एक हस्तक्षेप में गांधी ने ‘ज़रूरत पड़ने पर ‘हिंसक साधनों’ का इस्तेमाल करने की सलाह दी. जबकि गांधी इसके लिए कभी भी नहीं जाने जाते हैं.
असम में बांग्लादेश से आने वाले ‘अवैध प्रवासियों’ का मुद्दा बेहद अहम रहा है. हालांकि, 1980 के दशक में इसको लेकर छह साल तक आंदोलन भी चला और केंद्र सरकार के साथ शांति समझौते पर दस्तख़त करने के बावजूद इसका कोई समाधान निकलता नज़र नहीं आता, इसके बावजूद आज़ादी से पहले इस मसले पर असम के कांग्रेस नेताओं को गांधी द्वारा दिए गए समर्थन का कहीं ज़िक्र नहीं किया जाता.
और कुछ नहीं तो इससे कम से कम यह साबित करने में ही मदद मिलती कि इस विवादित मसले का इतिहास काफी पुराना है.

उत्तर-पूर्व पर बेहद महत्वपूर्ण किताब ‘स्ट्रेंजर्स ऑफ द मिस्ट’ में संजॉय हज़ारिका गांधी के सचिव और डायरी लेखक प्यारेलाल नैयर द्वारा दर्ज किए गए गांधी के बयान का हवाला देते हुए लिखते हैं, ‘असम में इसकी पूरी तरह से उपेक्षा की गई, शायद इसकी वजह यह है कि इसके बारे में लोगों को बहुत कम पता है.’
‘असम की जनता को एक संदेश’ शीर्षक से दिया गया यह बयान, महाराष्ट्र के पंचगनी नामक पहाड़ी नगर से 1944 में जारी किया गया था. गांधी जी के समय के असम में अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मिज़ोरम और मेघालय शामिल थे, यानी जिसे आज हम उत्तर-पूर्व कहकर पुकारते हैं, उसका ज़्यादातर हिस्सा इसमें शामिल था.
गांधीजी का यह बयान उस समय असम के कांग्रेस नेता गोपीनाथ बारदोलोई द्वारा मुस्लिम लीग के नेता और असम के प्रधानमंत्री मोहम्मद सादुल्लाह की भूमि बंदोबस्ती की नीति पर आपत्ति किए जाने के जवाब में आया था.
सादुल्लाह ने भूमि बंदोबस्ती की यह नीति भूतपूर्व पूर्वी बंगाल से आने वाले प्रवासियों से राज्य को भर देने के मकसद से आगे बढ़ाई थी.
लाइन सिस्टम नाम से जाने जाने वाली इस नीति का संबंध ज़मीन को ज़्यादा उत्पादक बनाकर असम से ज़्यादा राजस्व इकट्ठा करने की अंग्रेजी नीति से था (क्योंकि स्थानीय किसान अंग्रेजों के लिए काम करने को तैयार नहीं थे).
द्वितीय विश्वयुद्ध की तैयारियों के लिए ‘ज़्यादा अनाज उपजाओ’ कार्यक्रम के तहत प्रवास नीति को और बढ़ावा दिया गया. सादुल्लाह के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग सरकार ने इसे इतनी ज़्यादा मज़बूती दी कि बाद में वायसरॉय लॉर्ड वेवेल ने अपने संस्मरण में लिखा, सादुल्लाह वास्तव में ‘मुस्लिमों की संख्या बढ़ाने को लेकर ज़्यादा उत्सुक थे.’
हज़ारिका ने अपनी किताब में लिखा है:
‘बारदोलोई को सबसे ज़्यादा डर इस बात का था कि भविष्य में जिन्ना मुस्लिम आबादी के आकार और पूर्वी बंगाल के साथ इसके करीबी रिश्ते का हवाला देकर असम को पाकिस्तान में मिलाने की मांग कर सकते हैं और ये प्रवास इसकी ज़मीन तैयार कर रहा है.’
‘इन प्रवासों से सबसे ज़्यादा ख़तरा महसूस हुआ असमी हिंदुओं के ताकतवर तबके को. उन्हें इस बात का डर सताने लगा कि इससे उनकी राजनीतिक शक्ति घट जाएगी और उनके ऊपर प्रवासी मुस्लिमों का आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व कायम हो जाएगा.’
बारदोलोई ने इस नीति के कारण असम की जनसंख्या संरचना में आए बदलाव को ठीक करने के बारे में भले न सोचा हो, लेकिन उन्होंने इस नीति को समाप्त करने के लिए एक योजना बनाने की ज़रूरत महसूस की. इसमें और कोई नहीं, गांधी उनके समर्थन में आगे आए.
हज़ारिका ने अपनी किताब में रेखांकित किया है,
इस सवाल पर महात्मा बहुत साफ थे: ‘अगर लोगों को लगता है कि बसावट और प्रवास को लेकर सरकार की वर्तमान नीति दमनकारी और राष्ट्र-विरोधी है, तो उन्हें इसके लिए अहिंसक तरीके से और अगर ज़रूरत पड़े तो हिंसक तरीके से भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए.’
कुछ दिनों के बाद गांधीजी ने एक दूसरा संदेश भेजा, जिसमें उन्होंने कहा, ‘मेरे पास असमी भाइयों और बहनों के लिए आशा का कोई पैगाम नहीं है, लेकिन मैं उनके लिए अपनी गहरी संवेदना भेजता हूं. ईश्वर आपको इस अग्निपरीक्षा से सफलतापूर्वक बाहर निकलने के लिए आशीर्वाद दे.’

इन संदेशों ने बारदोलोई को नेशनलिस्ट इंडिपेंडेंट ग्रुप (राष्ट्रवादी स्वतंत्र समूह) के दक्षिणपंथी असमी हिंदू रोहिणी कुमार चैधरी के साथ मिलकर एक एक योजना बनाने के लिए प्रोत्साहित किया.
हज़ारिका ने इसे एक ‘तख्तापलट’ की संज्ञा दी है क्योंकि जब तक सादुल्लाह इस योजना के बारे में कुछ जान पाते, नवंबर, 1941 में उनकी सरकार गिर चुकी थी और इस तरह प्रांतीय सरकार द्वारा पूर्वी बंगाल से बड़े पैमाने पर प्रवास को समर्थन दिए जाने पर रोक लग गई.
हालांकि, इसकी उम्र छोटी थी. सादुल्लाह अगस्त, 1942 में सत्ता फिर लौट आए और फरवरी, 1946 तक कुर्सी पर बने रहे.
दिल्ली में बैठे हुए मुस्लिम लीग के नेताओं की गुप्त योजना के तहत सादुल्लाह सरकार जिस रास्ते पर चल रही थी और जैसी कार्रवाइयां कर रही थी, उसके कारण 1946 के मध्य तक, असमी कांग्रेस के प्रमुख होने के नाते बारदोलोई अपने जीवन के सबसे कठिन इत्मिहान का सामना करने वाले थे.
यह इम्तिहान था, राज्य को ‘पाकिस्तान के पक्ष में काम करने वालों के हाथों’ बिकने से बचाना. यहां भी गांधी ने उनको अपना समर्थन दिया.
बारदोलोई के जीवनीकार और जाने-माने इतिहासकार निरोद बरुआ ने अपनी किताब गोपीनाथ बारदोलोई, ‘द असम प्रॉब्लेम’ एंड नेहरूज़ सेंटर में लिखा है:
‘पहले के सभी अहम राजनीतिक फैसलों की तरह ही बारदोलोई इस मामले मे भी गांधी जी से सलाह लेना चाहते थे. इस मकसद से उन्होंने अपने दो भरोसेमंद सहयोगियों, बिजॉय चंद्र भगवती और महेंद्र मोहन चौधरी को दिसंबर 1946 के मध्य में सेरामपुर भेजा.’
उस समय भगवती असम कांग्रेस के और चौधरी असम में कांग्रेस संसदीय दल के सचिव थे.

मुस्लिम लीग, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित समूहीकरण योजना के पक्ष में थी, जिसके तहत भारत को दो भागों में बांटा जाना था. असम कांग्रेस, कांग्रेस आलाकमान द्वारा राज्यों को वर्गों में बांटने की संविधान सभा की योजना को स्वीकार करने के संभावित फैसले के ख़िलाफ़ थी, क्योंकि यह आख़िरकार समूहीकरण की योजना की तरफ ले जाता था.
वर्गों का हिस्सा बनना स्वीकार करने से इस बात का ख़तरा बढ़ जाता कि असम को बंगाल वाले वर्ग में रख दिया जाता, जहां पहले ही राज्य कांग्रेस और दक्षिणपंथी हिंदू संगठनों और लीग के बीच सीमा के निर्धारण को लेकर धर्म आधारित द्वेषपूर्ण झगड़े की स्थिति बनती दिख रही थी.
असम के नेताओं को इस बात का डर था कि अगर मुस्लिम बहुसंख्या वाले सिलहट के साथ धर्म के आधार पर वोटिंग कराई जाएगी, तो असम को पाकिस्तान का हिस्सा बनना पड़ सकता है. सिलहट को बंगाल के विभाजन के वक्त असम में मिला दिया गया था और अंग्रेजों द्वारा 1905 के फैसले को 1911 में रद्द किए जाने के बाद भी यह असम से अलग नहीं हुआ था.
दूसरी तरफ इसे इस बात का भी डर था कि अगर इसे बंगाल वाले समूह में रख दिया गया, तो हिंदू बंगाली सांस्कृतिक और भाषाई रूप से असम पर अपना वर्चस्व कायम कर लेंगे, जैसा कि उन्होंने ब्रिटिश शासन के शुरुआती दिनों में किया था.
15 दिसंबर, 1946 को गांधीजी के साथ भगवती और चौधरी की बातचीत को मानवशास्त्री निर्मल कुमार बसु ने दर्ज किया था जिसका 29 दिसंबर, 1946 के हरिजन के अंक में प्रकाशन हुआ था.
इसमें कहा गया, ‘असम के दो मित्र श्री बिजय (बिजॉय) चंद्र भगवती और श्री महेंद्र मोहन चौधरी श्री बारदोलोई के प्रतिनिधि के तौर पर 15 दिसंबर, 1946 की सुबह गांधी जी से मिलने आए. उन्होंने गांधीजी से पूछा कि समूहीकरण के सवाल को लेकर असम को क्या करना चाहिए. यह असम के लिए जीवन-मरण का सवाल था. वे बंगाल वाले समूह में नहीं जाना चाहते थे. कुछ लोगों ने उन्हें कहा कि अगर वे इससे बाहर रहते हैं, तो इससे लीग को मदद मिलेगी. असम को देश की प्रगति की राह में आने की इजाज़त नहीं दी जा सकती… आदि-आदि. उन्होंने कांग्रेस कार्यकारिणी से इस मामले में दिशा-निर्देश देने को कहा था, लेकिन वे कोई स्पष्ट निर्देश देने में असफल रहे. इसलिए वे गांधी जी के पास सलाह के लिए आए थे.’

गांधी जी ने उन्हें साफ तौर समूहीकरण को स्वीकार न करने और ‘अपना विरोध जता कर संविधान सभा से बाहर निकल जाने’ के लिए कहा. उन्होंने दोनों आगंतुकों के दिल को ‘मज़बूत’ करने और उन्हें ‘साहस’ देने के लिए ‘कई ऐतिहासिक उदाहरण’ दिए, जिसका लब्बोलुआब ये था कि ‘अगर आज आप सही कदम नहीं उठाते हैं, तो असम नष्ट हो जाएगा.’
बसु के मुताबिक गांधी ने कहा था, ‘बारदोलोई से कहना कि मैं थोड़ी सी भी दुविधा का अनुभव नहीं कर रहा हूं. असम को अपनी आत्मा की रक्षा हर हाल में करनी होगी. इसे पूरी दुनिया से लड़कर भी बचाना होगा. अगर ऐसा नहीं किया गया तो मैं कहूंगा कि असम में सिर्फ पुरुषों के पुतले थे, कोई पुरुष नहीं था. बंगाल किसी भी तरह असम पर वर्चस्व कायम करे यह एक ढीठ प्रस्ताव है.’
दशकों बाद, हज़ारिका के सामने उन क्षणों को याद करते हुए, भगवती ने, जो तब उम्र के नवें दशक में थे, कहा था कि वे रेल, सड़क और नाव की यात्रा करके, गांधी जी के पास सेरामपुर पहुंचे थे.
सेरामपुर पहुंच कर उन्होंने गांधी जी से मुलाकात के लिए समय मांगा. ‘हमें 3 बजे उनके टहलने के वक्त उनके साथ जाने के लिए कहा गया. लेकिन, हम उनसे शायद ही एक शब्द भी बात कर सके, क्योंकि महात्मा एक सिख के साथ, जिसे हम नहीं जानते थे, चल और बात कर रहे थे. इसके बाद उनके नहाने और मालिश का वक्त हो गया.’
लेकिन, गांधीजी ने उस शाम उन्हें अपनी झोपड़ी में बुलाया और बारदोलोई द्वारा भेजी गई चिट्ठी पढ़ी, जिसमें उन्हें समूहीकरण को लेकर हुई प्रगति और इस मामले पर प्रांतीय और केंद्रीय कांग्रेस नेताओं के पक्ष के बारे में बताया गया था.
भगवती ने याद करते हुए कहा था, ‘हमने गांधीजी से कहा था कि यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है.’
असम कांग्रेस के इन दो नेताओं के साथ गांधी जी की बातचीत से एक दिलचस्प जानकारी सामने निकलकर आती है, जिसके बारे में भी लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है. इसके मुताबिक सुभाषचंद्र बोस गांधी जी के आह्वान पर प्रांतीय सरकार से असम कांग्रेस के इस्तीफे के फैसले के विरोध में थे, जिसने सादुल्लाह को राज्य में सरकार बनाने का और लाइन सिस्टम को आगे बढ़ाने का मौका दिया.

भगवती और चौधरी के साथ गांधी जी की मुलाकात का जो वर्णन बसु ने किया है, उसमें गांधी जी के हवाले से कहा गया है, ‘सुभाष बाबू ने इसका विरोध किया क्योंकि उन्हें लगा कि असम का मसला ख़ास है. मैंने बारदोलोई से कहा था कि सुभाष बाबू की बात काफी गहरी है, और भले ही बहिष्कार की योजना मेरी बनाई हुई है, लेकिन अगर असम को सही लगता है तो उसे (प्रांतीय सरकार से) बाहर नहीं आना चाहिए. लेकिन असम ने बाहर आने का फैसला किया. यह गलत था.’
इस बातचीत में एक और बात निकल कर आई, जो इस बात का संकेत दे रही थी कि पार्टी के सदस्यों पर ‘आलाकमान’ की पकड़ अलोकतांत्रिक होने की हद तक बढ़ती जा रही थी, जो इंदिरा गांधी द्वारा कमान संभालने तक अपने चरम पर पहुंच चुकी थी.
निरोद बरुआ लिखते हैं, ‘स्वभावतः कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के फैसले को स्वीकार कर लेने वाले के तौर पर पले-बढ़े दोनों कांग्रेसी गांधी जी की बात सुनकर अपने कानों पर यकीन नहीं कर सके.’
गांधी जी दोनों की दुविधा को ताड़ गए और उन्हें अपने कार्यों का उदाहरण देकर बताया कि वे कैसे ‘कांग्रेस की भलाई के लिए कांग्रेस के ख़िलाफ़ ही एक तरह का सत्याग्रह कर सकते हैं.’ उन्होंने ये कहते हुए अपनी बात समाप्त की: ‘जाइए (असम के) लोगों को यह कहिए कि अगर गांधी भी हमारे हितों के ख़िलाफ़ बात करते हैं, तो हम उनकी भी नहीं सुनेंगे.’
इसके बाद बारदोलोई को रोकने वाला कोई नहीं था. असम कांग्रेस ने समान विचारों वाली पार्टियों के साथ मिलकर पूरी असम को स्वतंत्र भारत का हिस्सा बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी.
बरुआ लिखते हैं कि 22 दिसंबर, 1946 की कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक के ठीक बाद पंडित नेहरू, जेबी कृपलानी और शंकर राव देव ने असम के सवाल पर व्यक्तिगत तौर पर गांधी से सेरामपुर में मिलने का फैसला किया. जाहिर है, वे उनके फैसले से नाखुश थे.

हालांकि, सरदार पटेल शुरू में बारदोलोई के पक्ष में थे, लेकिन बाद में वे भी पीछे हट गए. पटेल, नेहरू और कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं का यह मत था कि समूहों से अलग रहने का असम का फैसला भारत की आज़ादी को अटकाने का काम करेगा. लेकिन गांधी का मानना था कि ‘हर इकाई को अपने लिए फैसले लेने और कार्य करने के लिए सक्षम होना चाहिए.’
गांधी ने भगवती और चौधरी से कहा, ‘कोई भी असम को उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई काम करने के लिए विवश नहीं कर सकता. उसे स्वतंत्र और स्वायत्त तरीके से फैसला लेना चाहिए. मुझे नहीं पता, आपके पास इतना साहस, दृढ़ता और बुद्धिमत्ता है या नहीं. इस बारे में सिर्फ आप बता सकते हैं. लेकिन अगर आप ये घोषणा कर सकते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ होगी. जिस समय संविधान सभा में समूहों में जाने का समय आएगा आप कहेंगे, ‘भद्रजनों, असम बाहर होता है.’ भारत की आज़ादी के लिए यह एकमात्र शर्त है और मैं यह आशा कर रहा हूं कि असम इसमें नेतृत्व करेगा. सिखों के लिए भी मेरी यही राय है. लेकिन आपकी स्थिति सिखों की तुलना में कहीं अच्छी है. आप एक पूरा राज्य हैं. वे एक राज्य के भीतर समुदाय हैं. लेकिन, मुझे लगता है कि व्यक्तियों को अपने लिए फैसले लेने और कार्य करने का अधिकार है, ठीक वैसे ही जैसे कि मुझे है.’
यानी जब वृहद असम को आज के भारत के साथ मिलाने का सवाल आया, तो गांधी और सिर्फ गांधी ही असम कांग्रेस द्वारा ‘केंद्रीय आदेश’ का विरोध करने के फैसले के साथ खड़े थे.
बरुआ के मुताबिक, असम पर गांधी के फैसले के बाद ब्रिटिश सरकार को यह एहसास हुआ कि ‘संविधान सभा को कभी भी उस तरह से नहीं चलाया जा सकेगा, जैसी योजना कैबिनेट मिशन द्वारा बनाई गई है. इसके बाद उन्होंने नए वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन के नेतृत्व में सत्ता के हस्तांतरण की एक नई नीति बनाई. जिन्ना को लेकर पहले से ही खराब राय रखने वाले माउंटबेटन ने उनसे (जिन्ना से) अप्रैल, 1947 में साफतौर पर कहा कि उन्हें पूर्वी पाकिस्तान के भीतर असम को शामिल करने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए.’
माउंटबेटन ने लिखा है, मैंने इस ओर ध्यान दिलाया कि पूर्व में उन्हें बगैर कलकत्ता के बंगाल का सबसे अनुपयोगी हिस्सा मिलेगा और अगर उनकी इच्छा है तो वे सिलहट को असम से वापस ले सकते हैं.
भविष्य में असम के पहले मुख्यमंत्री बारदोलोई और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के बीच हुआ पत्राचार इस बात की गवाही देता है दोनों कांग्रेसी आपस में किसी समझौते के बिंदु पर पहुंचने की जगह एक दूसरे से असहमत ही रहे, ख़ासतौर पर पूर्वी पाकिस्तान से असम में जारी रहनेवाले प्रवास के सवाल पर.

दिलचस्प बात ये है कि इसने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच बहस की ज़मीन को बनाए रखा, जो आज के समय और राजनीति के लिहाज़ से एक असंभव सपना ही कहा जा सकता है.
वैसे यहां यह भी उल्लेख करना मुनासिब होगा कि राष्ट्र निर्माण में बारदोलोई की भूमिका और भारत के विचार को लेकर उनके कार्यों, ख़ासतौर पर विभाजन के वक्त उनकी भूमिका को कांग्रेस आलाकमान ने आने वाले दशकों में कभी रेखांकित नहीं किया.
1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने बारदोलोई को भारत रत्न पुरस्कार दिया, तब असम में कई लोगों को यह समझ में नहीं आया कि दिल्ली से आने वाली इस ख़बर पर खुश हुआ जाए या इसे अपमान माना जाए.
बारदोलोई को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जो उत्तर-पूर्व के किसी व्यक्ति को पहली बार दिया गया था, उनकी मौत के करीब आधी सदी बीत जाने के बाद दिया गया.
जबकि बीसी रॉय को, जो असम के पड़ोसी पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे, लेकिन जिन्हें वास्तव में बारदोलोई का समकालीन कहा जा सकता है और जो स्वतंत्रता आंदोलन से आए बारदोलोई जितने बड़े कद के ही कांग्रेसी नेता थे, काफी पहले 1961 में ही भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका था.
आज अगर गांधी को उत्तर पूर्व के एक बड़े हिस्से को आज़ाद भारत के साथ मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए याद किया जाता है, तो बारदोलोई को भले ऐसे कांग्रेसी के तौर पर याद न किया जाए, जिन्होंने अपनी पार्टी के भीतर जगह बनाने और जैसा कि गांधी ने कहा था, ‘कांग्रेस की भलाई के लिए कांग्रेस के भीतर ही सत्याग्रह’ करने का साहस किया, तो भी उन्हें सिर्फ भारत के साथ रहने की लड़ाई के लिए ही नहीं, बल्कि उत्तर-पूर्व के लोगों के अंदर की उप-राष्ट्रीयता की मज़बूत भावना के साथ दृढ़ता के साथ खड़े रहने के लिए भी याद किया जाना चाहिए.
इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.