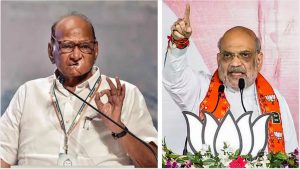प्रताप भानु मेहता के इस्तीफ़े के बाद हुई बहस के दौरान एक अध्यापक ने कहा कि निजी के मुक़ाबले सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में अधिक आज़ादी है. शायद वे सोचते हैं कि यहां अध्यापकों को उनकी सार्वजनिक गतिविधि के लिए कुलपति तम्बीह नहीं करते. पर इसकी वजह बस यह है कि इन विश्वविद्यालयों के क़ानून इसकी इजाज़त नहीं देते.

बात पिछली सदी के आख़िरी सालों की है. मैं पटना के ठाकुर प्रसाद सिंह कॉलेज में अध्यापक हुआ ही हुआ था. यह मगध विश्वविद्यालय का एक कॉलेज था. अब उसे खंडित करके बनाए गए पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का अंग है.
कक्षाएं यहां शायद ही होती थीं, अक्सर इम्तिहान हुआ करते थे, तरह-तरह के. प्राचार्य को इसका गर्व था कि यह हर प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा का केंद्र हुआ करता है.
हम अध्यापक से अधिक परीक्षा में चौकसी करने वाले थे. एक छोटा-सा कक्ष था जिसमें अध्यापक साथ बैठा करते थे. उसके करीब पेशाबखाना था या वह पेशाबखाने के करीब था, कहना मुश्किल है. लेकिन वहां वक्त गुजारते हुए मुझे शेखर जोशी की कहानी ‘बदबू‘ कायदे से समझ में आई.
कक्षा हो न हो, प्राचार्य को हर शिक्षक की हाजिरी लेने में जो अधिकार सुख मिलता था, उसकी कल्पना ही की जा सकती है. हाजिरी लेने का जिम्मा एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी का था. उसकी ताकत का अंदाजा भी किया जा सकता है.
उसी’स्टाफ रूम’ में एक दिन चर्चा सुनी कि सभी अध्यापकों को गांधी मैदान की सफाई पर जाना है. ताज्जुब हुआ. लेकिन अधिकतर सहकर्मी उत्साहपूर्वक गांधी मैदान को रवाना हो गए. मालूम हुआ हुक्म सांसद जी का है.
उच्च शिक्षा में सांसदजी का अर्थ था रंजन यादव. इन्हें तत्कालीन मुख्यमंत्री का जिगरी माना जाता था. ये कुलपतियों के कुलपति बल्कि कुलाध्यक्ष के भी ऊपर थे.
पटना की सड़क नाला रोड की चूड़ी गली में इनके निवास पर उस वक्त बिहार की उच्च शिक्षा की किस्मत तय की जाती थी. गली के बाहर सड़क पर दूर तक गाड़ियों की कतार और अंदर सांसदजी के दर्शनों के अभिलाषी और उनके कृपाकांक्षी अध्यापकों की भीड़.
अगर यहां से हुक्म जारी हो तो किसकी मजाल थी कि वह उसे नज़रअंदाज करे! बल्कि उसका पालन करते हुए दिखने में गौरव था. सो, अध्यापक बिना हंकाए गांधी मैदान को चल पड़े तो हैरानी क्या!
फिर सफाई क्या बुरा काम था? क्या अध्यापकों को स्वच्छता के पवित्र कार्य में योगदान नहीं करना चाहिए था!
2014 में एक दूसरी ही दुनिया में था. दिल्ली विश्वविद्यालय. केंद्रीय विश्वविद्यालय.स्वायत्त. 2 अक्टूबर आने को था. 15 अगस्त को लाल किले से देश की सफाई का ऐलान किया जा चुका था.
गांधी जयंती से बेहतर और कौन-सा दिन हो सकता था इस राष्ट्र स्वच्छता अभियान के उद्घाटन का! और स्कूलों और कॉलेजों से बेहतर जगहें कौन-सी हो सकती थीं जहां से एकमुश्त स्वच्छता अभियानी मिल सकें?
सितंबर के आख़िरी हफ्ते में किसी काम से जामिया मिलिया इस्लामिया जाना हुआ. शिक्षा विभाग के करीब मैदान में झाड़ू लगाते छात्र दिखे.
धूल उड़ रही थी. इस मैदान में झाड़ू लगाने से बड़ी बेवकूफी कुछ नहीं हो सकती थी. लेकिन हाथ चल रहे थे. पूछा कि क्या यह नियमित काम है. नहीं, यह 2 अक्टूबर का पूर्वाभ्यास कह लीजिए. कुलपति आने वाले हैं तैयारी का जायजा लेने. सो सब मुस्तैद थे.
1 अक्टूबर को मेरे विभागाध्यक्ष का फोन आया. अगले दिन विभाग आने का अनुरोध था, इसे आदेश कह नहीं सकता. पूछा, क्या गांधी जयंती का राष्ट्रीय अवकाश निरस्त हो गया है. वह तो नहीं हुआ लेकिन कुलपति कार्यालय से निर्देश है कि सभी अध्यापक और शेष कर्मी उपस्थित रहें और स्वच्छता अभियान में भागीदारी करें.
मैंने कहा कि जब तक यह लिखित आदेश नहीं मिलता कि अवकाश रद्द हो गया है, आना कठिन होगा. फिर फोन नहीं आया. लेकिन अलग-अलग जगह अध्यापकों द्वारा ही उत्साहपूर्वक झाड़ू के साथ तस्वीरें दिखलाई पड़ीं.
कक्षा के लिए जो न देखी, गांधी भवन से अपना झाड़ू हासिल करने में वह तत्परता दिखलाई पड़ी. बाद में झाड़ू को तलवार की तरह ताने हुए कुलपति की तस्वीर भी कई अध्यापकों ने भेजी.
इस अभियान में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के छठे वेतन आयोग की तनख्वाह पा रहे अध्यापकों को इसमें कोई बुराई न दिखी.
मुझे टीपीएस कॉलेज से गांधी मैदान जाते हुए अपने सहकर्मी याद आ गए. उन्हें आधा वेतन ही मिला करता था. लेकिन दोनों जगह स्वैच्छिक स्वीकृति थी. जिसने हिस्सा न लिया उसे कोई दंड झेलना पड़ा, इसका सबूत नहीं. लेकिन क्या यह सचमुच स्वैच्छिक था?
दिल्ली विश्वविद्यालय के तत्काल कुलपति ने प्रधानमंत्री की ऊर्जा की प्रशंसा करते हुए कहा कि लंबी विदेश यात्रा के बाद उनका सुबह-सुबह स्वच्छता अभियान में जुट जाना कितना प्रेरणादायक था. यह प्रशंसा भी स्वैच्छिक ही थी. जिस कुलपति ने यह नहीं किया वह निकाल दिया गया हो, ऐसा नहीं. लेकिन तकरीबन सबने यह खुद ही किया.
सरदार पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दौड़ का नेतृत्व भी दिल्ली विश्वविद्यालय के उन्हीं कुलपति ने किया जिन्होंने स्वच्छता अभियान में प्रधानमंत्री का अनुकरण किया था.
इसी समय भीष्म साहनी की जन्मशती के मौके पर हमारे छात्रों ने उनके उपन्यास पर आधारित गोविंद निहलानी की फिल्म ‘तमस’ दिखलाने की इच्छा व्यक्त की. हमारे अध्यक्ष ने समझाया कि अभी छात्रसंघ का चुनाव है. इस फिल्म को लेकर एक राष्ट्रवादी छात्रसंघ हंगामा कर सकता है. फिल्म नहीं दिखलाई जा सकी.
इसके बाद जाने ऐसे कितने तजुर्बे हुए. इतिहासकार दिलीप सीमियन को लेडी श्रीराम कॉलेज में बुलाकर दावत वापस ले ली गई. निमंत्रित करके बाद में भेजे शर्मिंदा माफीनामों का अंत नहीं है. सिर्फ विश्वविद्यालय के अंदर नहीं बल्कि पूरे भारत से.
कुछ नाम असुविधाजनक हो गए. गोष्ठियों में, परीक्षकों के तौर पर, उनका जिक्र बंद हो गया. अपने कला संकाय में अंग्रेज़ी के सहकर्मी हेनी बाबू पर जब पहला आक्रमण हुआ तो हमने उनके समर्थन में एक छोटी सभा अपने संकाय के समिति कक्ष में की. अगले दिन से उस पर ताला लग गया.
हमारे कला संकाय में जिस कमरा नंबर 22 में हमेशा ‘गैर अकादमिक विषय’ पर गोष्ठियां होती रहती थीं, अब वहां मात्र अकादमिक या राष्ट्रवादी गोष्ठियां होती हैं.
अकादमिक स्वतंत्रता क्या स्वेच्छापूर्वक आदेशपालन से बाधित होती है? क्या सरकारी फ़रमान को खुद ही लागू कर देना अकादमिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है?
क्या नंदिनी सुंदर की किताब की जगह कोई और किताब पाठ्यक्रम में लगा देने से अकादमिक स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है? क्या विश्वविद्यालय में ‘लाल आतंक’ के विरुद्ध अभियान चलाना अकादमिक स्वतंत्रता पर हमला है?
क्या छात्रसंघ की पत्रिका के लोकार्पण के आयोजन की स्वीकृति देकर उसे वापस ले लेना अकादमिक स्वतंत्रता को बाधित करता है?
क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आदेश पर सीबीसीएस व्यवस्था को लागू करना स्वतंत्र निर्णय है? क्या विश्वविद्यालयों का बड़े दिन को ‘गुड गवर्नेंस डे’ के तौर पर मनाना अपना निर्णय था?
ये सवाल अशोका विश्वविद्यालय में प्रोफेसर प्रताप भानु मेहता के इस्तीफे के बाद चल रही बहस के दौरान उठ खड़े हुए. तब जब एक अध्यापक ने कहा कि निजी विश्वविद्यालयों के मुकाबले सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में अधिक आज़ादी है.
शायद उनका विचार यह होगा कि यहां अध्यापकों को बुलाकर उनकी सार्वजनिक गतिविधि के लिए कुलपति तम्बीह नहीं करते. यह नहीं होता तो इसका कारण यह है कि इन विश्वविद्यालयों के कानून इसकी इजाजत नहीं देते.
लेकिन यह कोशिश की जा रही है कि विश्वविद्यालयों में सरकारी कर्मचारियों वाली आचार संहिता लागू कर दी जाए. वह जब हो जाएगी तब देखना दिलचस्प होगा कि वह आज़ादी कितनी रह जाती है.
(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं.)