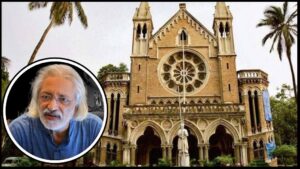उर्दू है जिसका नाम हमीं जानते हैं दाग़, हिन्दोस्तां में धूम हमारी ज़बां की है, दाग़ देहलवी का ये शेर उर्दू ज़बां से प्यार करने वालों को बेहद अज़ीज़ है. किसी भाषा से प्रेम की मिसाल देखनी हो तो उर्दू और उसके चाहने वालों का नाम शायद सबसे ऊपर आएगा. और उर्दू के इन ‘दिलदारों’ में अव्वल होंगे संजीव सराफ. आईआईटी खड़गपुर से पढ़े, कभी क़ारोबारी रहे संजीव सराफ ने उर्दू के प्रति अपने प्यार को नाम दिया ‘रेख़्ता’ का. रेख़्ता वेबसाइट की शक्ल में दुनिया के सामने आया, जहां उर्दू की हज़ारों क़िताबें, लाखों शेर और शायरों के काम को संजोया गया है.
2015 में इस संस्था ने जश्न-ए-रेख़्ता नाम का आयोजन शुरू किया जहां बकौल संजीव ‘हम उर्दू को सेलीब्रेट करते हैं, उसका जश्न मनाते हैं.’ इस साल का तीन दिवसीय जश्न-ए-रेख़्ता रविवार को ही संपन्न हुआ है. देश-दुनिया से उर्दू के लाखों चाहने वालों ने इसमें शिरक़त की और उर्दू के प्रति अपनी मुहब्बत ज़ाहिर की. यह दिलचस्प है कि उर्दू को ज़माने तक पहुंचाने का काम बखूबी करने वाले संजीव ख़ुद ज़माने के सामने कम ही आते हैं. उनसे बातचीत:
रेख़्ता का सफ़र कैसे शुरू हुआ?
यूं तो घर में शेरो-शायरी का माहौल बचपन से रहा था, जैसे तब हर आम हिंदुस्तानी घरों में हुआ करता था, ग़ुलाम अली साहब हों, चाहे मेहदी हसन साहब, ग़ज़लें कानों में पड़ती रहती थीं. तो उस तरफ झुकाव तब से था. रेख़्ता का सफ़र तब शुरू हुआ जब मैंने शायरी पढ़ना शुरू किया था. तब मुझे अहसास हुआ कि यह कितना मुश्किल है कि अगर कोई शायरी पढ़ना चाहता है मगर उर्दू नहीं समझता. मैंने उर्दू सीखी है. पर फिर लगा मेरे जैसे लाखों और भी होंगे जो पढ़ना चाहते होंगे पर या तो शायरी की क़िताबें उपलब्ध नहीं होंगी या भाषा आड़े आएगी. इन सब के बीच फिर पढ़ाई नौकरी… इन सबमें लगे रह गए. फिर एक दिन लगा कि पेट पालने के लिए तो बहुत कुछ कर लिया अब रूह के लिए कुछ किया जाए. बस फिर एक के बाद एक कड़ी जुड़ती चली गई और जनवरी 2013 में हमने रेख़्ता लॉन्च किया. यहां सबसे बड़ा पहलू नीयत है. अगर आपकी नीयत है किसी के लिए कुछ करने की तभी आप कर पाएंगे. दूसरा पहलू है एफर्ट यानी आपके प्रयास. उर्दू मेरी मादरी-ज़बान नहीं है, मेरा उर्दू से कोई सीधा ताल्लुक़ नहीं है पर ये मेरा पैशन है कि मैं इसके लिए कुछ करूं, तो वो मैं कर रहा हूं.
शुरुआती रिस्पॉन्स कैसा रहा?
रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था. लोगों ने इसे हाथों-हाथ लिया. इसी से हमारा हौसला बढ़ा और ये सफ़र यहां तक आ पहुंचा. जब हमने पहले साल जश्न-ए-रेख़्ता किया था तब लगा था कि दो-ढाई हज़ार लोग आएंगे, पर 18 हज़ार लोग आए, उसके अगले साल उससे भी ज्यादा… (हंसते हुए) तो अब समझिए हम शेर पर बैठे हुए हैं, न उतर सकते हैं न हिल सकते हैं. ये सिलसिला आगे कहां जाएगा यह नहीं पता पर हम जब तक कर सकेंगे, उर्दू के लिए काम करेंगे.
कई बार लोगों को कहते सुना जाता है कि उर्दू आम आदमी की ज़बान नहीं है.
मैं इस बात से इत्तेफ़ाक नहीं रखता. दिन-रात, सुबह-शाम ये सब लोकप्रिय शब्द हैं और ये उर्दू के लफ्ज़ हैं जिन्हें सब आम बोलचाल में बोलते हैं. और एक ग़लतफहमी है जो पिछले कुछ 40-50 सालों में बढ़ी है कि उर्दू मुसलमानों की ज़बान है. तो मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है. उर्दू हिंदुस्तान की ज़बान है, हिंदुस्तानियों की ज़बान है. और जब मैं हिंदुस्तान कहता हूं इसका मतलब 1947 से पहले वाले हिंदुस्तान से है. वरना बताइए, इस क्षेत्र के अलावा उर्दू कहां बोली जाती है! यह पैदा ही यहीं हुई है. और जहां तक उर्दू को मुल्क़ों में बांटने की बात आती है तो मैं यही कहना चाहूंगा कि भाषा को आप सरहद में नहीं बांट सकते. जो लक़ीर खिंची थी वो ज़मीन पर खींची गई थी, दिलों में नहीं.
इस बार जश्न में पाकिस्तानी कलाकारों की भागीदारी नहीं रही, क्या इसकी वजह दोनों मुल्क़ों के बीच चल रही सियासी तनातनी है?
नहीं, हमने अपनी तरफ़ से सभी को इनविटेशन भेजा था, पर आना- न आना उनकी मर्ज़ी पर निर्भर करता है.

जश्न केवल बड़े शहरों तक ही सीमित रहेगा या आप छोटे शहरों तक जाने की भी सोच रहे हैं?
बिल्कुल, हम छोटे शहरों तक जाना चाहते हैं. कुछ समय पहले हमने चंडीगढ़ में एक प्रोग्राम किया था, जो अच्छा रहा. हम देश के कई शहरों जैसे भोपाल, लखनऊ, हैदराबाद, जयपुर, रांची भी जाना चाहते हैं, जहां कहीं भी उर्दू के चाहने वाले हैं हम वहां जाना चाहेंगे पर इसके लिए काफ़ी व्यवस्थाओं की ज़रूरत होती है जो बदकिस्मती से अभी हमारे पास नहीं हैं. दिल्ली मेरा अपना शहर है, किसी और शहर के मुक़ाबले हमारे लिए यहां कोई कार्यक्रम करना ज़्यादा आसान होता है पर जब मुमकिन होगा हम बाकी शहरों का भी रुख़ करेंगे.
नए लोगों को भी मंच देने की कोई योजना है?
बिल्कुल, आपने देखा होगा रेख़्ता में हम नए शायरों को भी मौका देते हैं. बाकी हमारे साथ देश भर से कई युवा जुड़े हुए हैं. हमारी कोशिश है कि जो अच्छा काम कर रहे हैं या कर सकते हैं वो सामने आएं.
कई बार बुद्धिजीवियों की चिंता रहती है कि भाषा या साहित्य के नाम पर होने वाले ‘फेस्टिवल्स’ में सिर्फ फेस्टिवल बाक़ी रह जाता है, भाषा या साहित्य निकल जाते हैं, या यूं कहें कि कमर्शियलाइज़ हो जाते हैं.
ये दो सवाल हैं, मैं इनका जवाब अलग-अलग देना चाहूंगा. पहली बात ये हम कोई फेस्टिवल नहीं करते, ये जश्न है उर्दू का. उर्दू के इतने पहलू हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स में, तहज़ीब में, ये उनका जश्न है. तो इस जश्न में एक बात आती है क्वालिटी कि. क्वालिटी से हम कभी कोई समझौता नहीं करेंगे. अभी शुरुआत है, वक़्त के साथ और तज़ुर्बे होंगे, कुछ अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे पर हमारी क्वालिटी इससे प्रभावित न हो, यही कोशिश रहेगी.
अब बात आती कमर्शियलाइज़ होने की, तो मैं यही कहूंगा कि हम सरकारी संस्था तो नहीं हैं कि हमें फंडिंग मिलती हो और हमारा उद्देश्य इससे कोई पैसा या मुनाफ़ा कमाना तो है नहीं, हम बस यही चाहते हैं कि संस्था सेल्फ-सस्टेनेबल यानी अपने लिए कुछ करने लायक बनी रही. बाकी कभी क्वालिटी से तो किसी समझौते का सवाल ही नहीं उठता.
रेख़्ता ने कुछ समय पहले प्रकाशन भी शुरू किया है जिसमें सबसे पहले मुज़्तर ख़ैराबादी का दीवान आया. कई किताबों के अनुवाद भी देवनागरी में हुए हैं. उर्दू का हिंदी तर्जुमा मिल जाता है पर उर्दू जानने वालों को हिंदी कवि उर्दू लिपि में नहीं मिल पाते. क्या आप इस पर काम करने की सोचते हैं?
हमने उर्दू में लिखे हुए को देवनागरी में लाने पर काम किया है, ढेरों उर्दू क़िताबों को रिस्टोर करने का काम भी हो रहा है पर हिंदी कवियों को उर्दू में लाने की बात पर कभी ध्यान नहीं गया. अभी तो ऐसी कोई योजना नहीं है.
उर्दू के चाहने वालों के लिए कुछ नया करने की सोच रहे हैं?
बिल्कुल, अभी हम ‘आमोज़िश’ नाम की वेबसाइट लाए हैं जिससे आसानी से उर्दू सीखी जा सकती है. मसलन अगर आप अलिफ़ जानते हैं तो इसकी मदद से सिर्फ़ अलिफ़ से शुरू होने वाले लफ्ज़ सीख सकते हैं, सारे अल्फाबेट न भी आते हों, तब भी आप लफ्ज़ लिखना-पढ़ना जान सकते हैं.
तारेक फ़तेह का आरोप है कि उनके साथ जश्न-ए-रेख़्ता में हुई बदतमीज़ी पर आयोजकों ने कुछ नहीं किया और यह एक योजनाबद्ध हमला था.
उनके आने के बारे में किसी को कोई ख़बर नहीं थी, किसी को कोई इत्तेला नहीं थी तो यह योजनाबद्ध हमला कैसे हो सकता है?

इसके बाद उन्होंने ट्वीट करके कहा कि रेख़्ता उर्दू की आड़ में होने वाला इस्लामिक फेस्ट है, यहां जिहादी आते हैं.
(हंसते हुए) वहां डेढ़ लाख के क़रीब लोग आए थे, आप पूछ लीजिए किसी से भी जाकर कि कितने जिहादी थे उनमें से!
उनका कहना है कि आयोजकों ने कोई स्टैंड नहीं लिया, आपके अनुसार आयोजकों को क्या स्टैंड लेना चाहिए था?
अरे! क्या स्टैंड लेना चाहिए था आयोजकों को! वहां पुलिस की व्यवस्था की गई थी, जिससे शांति और व्यवस्था बनी रहे. लोगों से क्या आयोजक जाकर भिड़ेंगे! हमारी ज़िम्मेदारी थी और हमने पुलिस को इत्तेला दी.
यह बात भी उठी है कि अगर संजय लीला भंसाली पर हुआ हमला अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला था तो अगर कोई व्यक्ति कहीं जाता है, अपनी बात कहता है तो उसे ये हक़ होना चाहिए. फ़तेह साहब ने कहा कि पुलिस ने भी उनके साथ ग़लत व्यवहार किया.
हर एक को अपनी राय रखने का पूरा हक़ है पर कोई कहीं भी जाकर अपनी बात बोलने लगे तो यह कहां तक मुनासिब है, ये सोचने की बात है. यह एक कल्चरल फेस्टिवल था, भाषा का, यकजहती (एकता) का फेस्टिवल था. क्या यही जगह मिलती है लोगों को कोई एजेंडा आधारित बात करने की! ये तो वही बात हो गई कि आ बैल मुझे मार.
इस पूरे विवाद पर आप क्या कहेंगे?
हम जो काम कर रहे हैं उसका न सियासत से कोई लेना-देना है न किसी मज़हब से. मैं कई बार अर्ज़ कर चुका हूं कि ये सिर्फ़ ज़बान का मसला है. हम सिर्फ़ ज़बान की ख़िदमत कर रहे हैं. इसका किसी धर्म या राजनीति से कोई संबंध नहीं है. ख़ामख़्वाह का मसला बनाया जा रहा है. कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी कह सकता है. हम उसमें कुछ नहीं कर सकते.
फ़तेह साहब ने रेख़्ता को कई नामों से पुकारा जैसे कि यह इस्लामिक फेस्ट है… उन्होंने कहा कि आयोजकों या लिबरल्स ने कुछ नहीं कहा.
क्या इस्लामिक था भई इसमें! जो लोग आए थे उनसे पूछिए कि उन्हें वहां क्या इस्लामिक लगा. मैं इस तरह के ‘सेंसेशनलिज़्म’ का कुछ नहीं कर सकता. मैं हिंदू हूं, मुझे इस बात पर गर्व है पर इस फेस्टिवल का किसी भी धर्म से कोई लेना-देना था ही नहीं. अदब, भाषा में मज़हब कहां से आ गया! यह सिर्फ़ बिना बात के मुद्दे को सनसनीखेज़ बनाने की कोशिश है. वहां सवा लाख-डेढ़ लाख के करीब लोग आए थे, दो दिन वहां कुछ नहीं हुआ, सब कुछ शांतिपूर्वक ढंग से हुआ.
वहां कुमार विश्वास आए थे, गुलज़ार साहब आए थे अगर यह कोई मज़हबी फेस्ट होता तो क्या प्रसून जोशी, अन्नू कपूर जैसे लोग आए होते. वहां प्रेमचंद के पोते आलोक राय भी मौजूद थे. यह हिंदू-मुसलमान का मामला ही नहीं है. मुख्तलिफ़ लोग थे जो अलग-अलग संप्रदाय के थे. दर्शकों में हर तरह के लोग थे.
और जहां तक कुछ कहने की बात है तो हमें नहीं पता कि उन्होंने क्या कहा था! कुछ कहने के लिए पता होना चाहिए न कि असल में क्या हुआ था. हम किसी भी तरह की हिंसा के ख़िलाफ़ हैं चाहे मौखिक हो या शारीरिक. किसी भी तरह की हिंसा को सही नहीं ठहराया जा सकता. कोई मौखिक हिंसा का जवाब शारीरिक हिंसा से देता है तो वो भी ग़लत है. मुद्दे को कोई और रंग दिया जा रहा है.
और सिर्फ़ आयोजकों से बात मत कीजिए. जिन लोगों ने वहां शिरकत की थी उनसे भी जानिए कि वहां हुआ क्या था. जो वहां मौजूद थे उनसे भी पूछिए कि वहां किसको लगा कि जिहादी थे या ये इस्लामिक फेस्ट था.