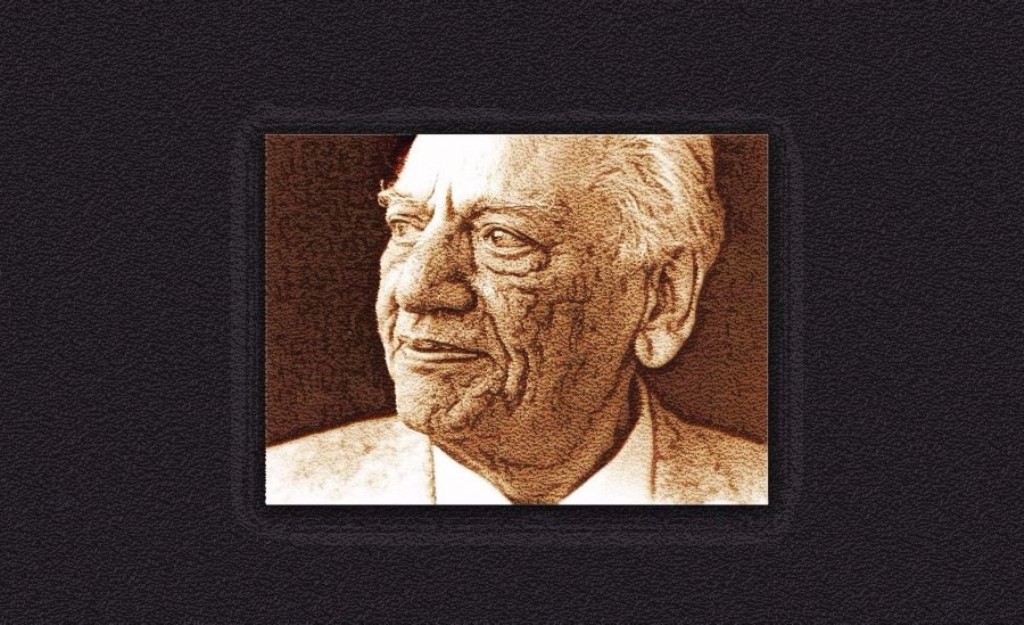गुलों में रंग भरे बाद-ए-नौबहार चले
चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले
क़फ़स उदास है, यारो सबा से कुछ तो कहो
कहीं तो बहर-ए-ख़ुदा आज ज़िक्र-ए-यार चले
कभी तो सुब्ह तेरे कुंज-ए-लब से हो आग़ाज़
कभी तो शब सर-ए-काकुल से मुश्कबार चले
बड़ा है दर्द का रिश्ता, ये दिल ग़रीब सही
तुम्हारे नाम पे आयेंगे, ग़मगुसार चले
जो हम पे गुज़री सो गुज़री है शब-ए-हिज़्रां
हमारे अश्क़ तेरी आक़बत संवार चले
हुज़ूर-ए-यार हुई दफ़्तर-ए-जुनूं की तलब
गिरह में लेके गरेबां का तार-तार चले
मुक़ाम ‘फ़ैज़’ कोई राह में जंचा ही नहीं
जो कू-ए-यार से निकले तो सू-ए-दार चले
उनकी मृत्यु के तीस साल बाद 2014 में विशाल भारद्वाज ने राजनीतिक स्वर लिए हुए एक मनोरंजन प्रधान फिल्म बनाई- हैदर. इसमें फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ (1911-1984) की ऊपर दी हुई ग़ज़ल को शामिल किया गया था.
भारत की एक बड़ी युवा जनसंख्या ने उनका पहली बार नाम सुना, ये वह पीढ़ी थी जिसने मेहदी हसन की आवाज़ में फ़ैज़ को नहीं सुना था, जिसे पाकिस्तान सहित भारतीय उपमहाद्वीप में लोकतंत्र पर आए हुए संकटों से अभी साबका नहीं पड़ा था और जो अभी बीस से तीस साल की उमर में है.
उसके लिए फ़ैज़ फिर एक बार आ खड़े हुए. वह फ़ैज़ जिसे पढ़ा जा सकता था, गाया जा सकता था और अपने दोस्तों से साझा किया जा सकता था.
लोकतंत्र का कवि
29 जनवरी, 1954 को मांटगोमरी जेल में रहते हुए फ़ैज़ ने यह सब लिखा था. यह उनकी आदत थी कि वे लिखें और जैसा हर दौर में सत्ता अपने भीतर तानाशाही विकसित करती है, फ़ैज़ के दौर में भी उसने किया. उन्हें जेल में डाला गया. जेल में उन्होंने फिर लिखा. उन्हें फिर जेल में डाला गया.
पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में, तुर्की, श्रीलंका, म्यांमार में जब आज़ादी आई तो उसका चेहरा वहां के लोग पहचान नहीं पा रहे थे. जब भारत में आज़ादी आई तब गांधी जी बेलियाघाट की तरफ थे, उधर लोग अपने हिंदू और मुसलमान भाइयों को आपस में मार-काट रहे थे. सभी को लगा कि यह तो वह है ही नहीं, जिसकी हमने ख़्वाहिश की थी. फ़ैज़ को भी यही लगा था-
ये दाग़ दाग़-उजाला, ये शब-गज़ीदा सहर
वो इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहींये वो सहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर
चले थे यार कि मिल जाएगी कहीं न कहीं
फ़लक के दश्त में तारों की आख़िरी मंज़िल
कहीं तो होगा शब-ए-सुस्त मौज का साहिल
कहीं तो जाके रुकेगा सफ़ीना-ए-ग़मे-दिल
जिन लोगों ने राजनीति विज्ञान पढ़ा होगा वे जानते हैं कि लोकतंत्र के द्वारा चुनी गई सरकारें भी अपने अंदर ऐसी संरचनाएं विकसित कर लेती हैं कि वे अपने ही नागरिकों का दमन करने लगती हैं. जब राजनीति विज्ञानी ज्यार्जियो अगम्बेन ने यह बात कही तो भारत के कई और विद्वान इस ओर उन्मुख हुए कि देखा जाय कि 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी क्यों लगा दी थी?
1974 के आसपास की रेलवे की हड़तालों और विद्यार्थियों ने आख़िर मांगा ही क्या था? वे अपने काम का दाम मांग रहे थे, वे अपने नियोक्ता से समतामूलक व्यवहार चाहते थे और चाहते थे कि उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की उपलब्धता हो. विद्यार्थियों को रोज़गार और शिक्षा चाहिए थी, वे विश्वविद्यालयों में आ रही सड़ांध से भी व्यग्र थे.
इंदिरा गाधी ने इमरजेंसी लगा दी! जो बोलता था, उसे चुप करा दिया गया, चाहे अख़बार हो या आदमी. शायर तो बोलेगा ही. इस दौर के भारत में फ़ैज़ को ख़ूब गाया गया, पढ़ा गया.
पाकिस्तानी हुक़ूमत की निगाह में तो वे 1950 के दशक से ही चढ़ गए थे. लग रहा था कि उन्हें फांसी की सज़ा दी जाएगी. लेकिन उन्होंने जनता से हुक़ूमत की शिकायत की. उन्हें जनता से ही आशा थी-
निसार मैं तेरी गलियों के ए वतन, कि जहां
चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले
जो कोई चाहने वाला तवाफ़ को निकले
नज़र चुरा के चले, जिस्म-ओ-जां बचा के चले
आख़िर वह क्या है जो फ़ैज़ को हमारे बीच में बार-बार ले आता है. पिछले दस सालों में भारत और पाकिस्तान ने काफ़ी प्रगति की है. पूरी दुनिया की तरह दोनों देशों में सूचना तकनीक का विकास हुआ है. भारत तो जापान और चीन की तरह इस क्षेत्र में नेतृत्वकारी हैसियत में आ चुका है. तकनीक ने पूरी दुनिया में सामान्य नागरिकों को मज़बूत बनाया है. उन्हें लामबंद होने में मदद की है.
दूसरी तरफ यह बात सरकारों को भी पता है. वे अपनी जनता को पहले पुचकारते हैं. उसके लिए योजनाएं लाते हैं, अगर मान गई तो मान गई, नहीं तो दमन का पुराना तरीक़ा नये क़ानूनों के मार्फ़त ले आया जाता है. इसमें सबसे पहले अभिव्यक्ति की आज़ादी को पाबंद किया जाता है.
वर्तमान भाजपा सरकार के समय अभिव्यक्ति की आज़ादी के बारे में काफ़ी बात हुई है. कहा जाता है कि भाजपा को इस मुद्दे पर बिहार का विधानसभा चुनाव गंवाना पड़ा, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी को थोड़ा व्यापक संदर्भ में देखें तो यह लोकतंत्र की परीक्षा लेने वाला विचार है.
अभिव्यक्ति की आज़ादी लोकतंत्र में जीवन भरती है और स्वतंत्रचेत्ता नागरिकों का निर्माण करती है दूसरी तरफ राज्य क़ानून बनाकर अपने नागरिकों पर बंदिश लगाता है. कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी का मामला इसका उदाहरण है, उस समय कांग्रेस की सरकार थी. इसलिए किसी पार्टी विशेष की निंदा या आलोचना से बेहतर यह होगा कि सरकारों के जन-हितैषी होने पर ज़ोर दिया जाए.
यहीं पर फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ जरूरी कवि हो जाते हैं जिनकी कविता पूरी दुनिया की लोकतांत्रिक सरकारों से जन-हितैषी होने की अपेक्षा करती है. इसी के साथ वे जनता को उद्बोधित भी करते हैं. फ़ैज़ के लिए बोलना ज़िंदा होना है. थोड़े से समय में बात भी कह देनी है-
बोल कि लब आज़ाद हैं तेरे
बोल ज़बां अब तक तेरी है
तेरा सुतवां जिस्म है तेरा
बोल कि जां अब तक तेरी हैबोल ये थोड़ा वक़्त बहोत है
जिस्म-ओ-ज़बां की मौत से पहले
बोल कि सच ज़िंदा है अब तक
बोल जो कुछ कहना है कह ले
विश्व नागरिक फ़ैज़ अहमद फ़ैज़
फ़ैज़ अहमद फ़ैज़, महमूद दरवेश और नाज़िम हिक़मत साहित्यिक और राजनीतिक व्यक्तित्वों की उस कड़ी का निर्माण करते हैं जो अपने देश से बाहर रहे या रहने को बाध्य किए गए. एक व्यापक अर्थ में वे विश्व नागरिक थे लेकिन उनके अंदर अपने देश का बोध सदा बना रहा.
वे जो कहना चाह रहे थे, उसे कहने के लिए उन्हें ‘देश की संरचना के भीतर’ वे जगहें या अवसर नहीं उपलब्ध हो पा रहे थे जिसकी उन्हें दरकार थी. वे अपना देश छोड़कर दूसरे देश गए.
वास्तव में फ्रांस की क्रांति के बाद पूरी दुनिया में आज़ादी की चाहतों में जो सबसे बड़ी चाहत उपजी, वह कहने की आज़ादी की चाहत रही है. फ़ैज़ की शायरी उनकी पत्रिका ‘लोटस’ के द्वारा फिलिस्तीन, बेरुत और अफ्रीका के नामालूम लोगों तक पहुंची. वास्तव में फ़ैज़ लोकतंत्र और आज़ादी के कवि थे. वे भला एक देश में बंधकर कैसे रह सकते थे!
किसे ज़रूरत है फ़ैज़ की?
उन्हें जो इश्क़ करते हैं, उन्हें ज़रूरत है फ़ैज़ की. जिन्हें दूसरों के सहारे की जरूरत है या जो दूसरों को सहारा देना चाहते हैं-
तुम मेरे पास रहो
मेरे क़ातिल, मेरे दिलदार, मेरे पास रहोजब कोई बात बनाए न बने
जब न कोई बात चले
जिस घड़ी रात चले
जिस घड़ी मातमी सुनसान, सियाह रात चले
पास रहो
मेरे क़ातिल, मेरे दिलदार, मेरे पास रहो
फ़ैज़ की जरूरत उन्हें भी है जो सोचते हैं कि एक दिन दुनिया बदल जाएगी और जनता का राज होगा. तमाम तरह की बेड़ियां टूट जाएंगी-
हम देखेंगे
लाज़िम है कि हम भी देखेंगे
वो दिन
कि जिसका वादा है
जो लौहे-अज़ल में लिखा है
जब ज़ुल्मो-सितम के कोहे गरां
रुई की तरह उड़ जाएंगे.
कहते हैं कि फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की इस लिखावट से पाकिस्तान के हुक्मरान बड़े नाराज थे. वे उन लोगों से भी नाराज़ थे जो इसे गाते थे लेकिन 1985 में इक़बाल बानो ने लाहौर के हज़ारों लोगों के सामने इसे गाया था. इसमें इक़बाल बानो की हिम्मत तो शामिल थी ही, फैज़ की शायरी भी हिम्मत बंधाने वाली शायरी थी.
(रमाशंकर सिंह भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला में फेलो हैं.)