नई दिल्ली: हिंदी पत्रिकाओं का इतिहास अत्यंत समृद्ध रहा है. ‘सरस्वती’, ‘दिनमान’, ‘धर्मयुग’, ‘सारिका’ से लेकर ‘साप्ताहिक हिंदुस्तान’ जैसी पत्रिकाओं ने हिंदी भाषा के साथ हिंदी समाज को भी संस्कार दिया था. संवैधानिक मूल्यों की वाहक इन पत्रिकाओं का देश की राजनीति और संस्कृति पर भी गहरा प्रभाव पड़ता था. नब्बे के दशक में आकर इन पत्रिकाओं की स्थिति बिगड़ने लगी. नई तकनीक और डिजिटल माध्यमों के बाद पत्रिकाओं के पाठक यूट्यूब और मोबाइल की ओर मुड़ गए.
आज हिंदी पत्रिकाओं की स्थिति पर चर्चा छिड़ने पर कई लोग हालावादी होकर बच्चन की शरण में चले जाते हैं, ‘अब न रहे वो पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला’.
इस विषय पर द वायर हिंदी ने एक परिचर्चा, ‘हिंदी पत्रिका का अवसान?’, के तहत हिंदी की कई प्रमुख हस्तियों के सामने कुछ सवाल प्रस्तुत किए.
1. हिंदी की अधिकतर ‘गंभीर वैचारिक पत्रिकाएं’ सिर्फ़ साहित्य-कला-संस्कृति के प्रश्नों तक सीमित क्यों हैं? वैचारिकी के अन्य विषय, मसलन राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय राजनीति, युद्ध, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था, इनके पन्नों में क्यों नहीं दिखाई देते?
मृणाल पांडे (वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक, ‘कादम्बिनी’ की भूतपूर्व संपादक): हिंदी के सामने 1947 के बाद पहला बड़ा मौक़ा था जब वह आज़ादी की लड़ाई और दुनिया में औपनिवेशवाद के पतन की कहानी को अपनी तरह के मुहावरों में अपने अनुभवों सहित पेश कर सकती थी. साथ ही, वह इस लड़ाई की अंतरंग साक्षी हिंदी पट्टी के उभरते विचारशील लेखन को पत्र-पत्रिकाओं में अधिक जगह दे सकती थी. पर यह अवसर उसने ‘मानक हिंदी बनारस वालों की हो कि फोर्ट विलियम वालों की?’ जैसे बेमतलब सवालों और हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा की राजनीतिक केंद्रीयता दिलवाने की कोशिशों के बीच गंवा दिया.
समसामयिक सवालों से वह बचती रही और आधुनिकतावाद का डट कर सामना करने की बजाय वह सांप्रदायिक पहचान के निकट आती गई. यही वजह है कि वह नई तरह के लेखन और शैलियां नहीं रच सकी. ‘क्या उपन्यास/ कहानी/ नई कहानी/नाटक मर गया?’ जैसे सवालों पर बहसियाने या छायावाद पर मुहल्ला-छाप लड़ाई लड़ना उसे आसान पड़ता था, वही उसने किया.
दूसरा मौक़ा 1975 से 84 तक आया जब हिंदी ने नई राजनीति से गहरे सरोकार बनाए और नए लेखक खोज कर उनसे राजनैतिक सामाजिक विषयों पर लिखवाया. हिंदी पत्रकारिता का यह स्वर्णिम दौर इसके बाद मालिकान की नई पीढ़ी की बढ़ती व्यावसायिक हरकतों से नष्ट होता गया. 1995 तक सब बड़ी पत्रिकाएं बंद हो गईं.

राहुल देव (वरिष्ठ पत्रकार, ‘जनसत्ता’ के भूतपूर्व संपादक): ऐसा नहीं है कि गंभीर हिंदी पत्रिकाओं में साहित्य, कला, संस्कृति के अलावा अन्य विषयों और क्षेत्रों पर सामग्री नहीं छपती. पर्यावरण पर तो खासी छपती है. पत्रिका हो या अखबार या टीवी चैनल हो या डिजिटल मंच, किसी भी समाचार-विचार मंच को अंततः एक विशिष्ट पाठक-दर्शक समुदाय को ही अपना लक्ष्य समूह बनाना पड़ता है, अर्थात् उसके पाठकों-दर्शकों के बहुमत की मनःस्थिति, मनोविज्ञान, झुकाव, सामाजिक-सांस्कृतिक रूचियां और पसंद-नापसंद उस मंच की भी सीमा बन जाते हैं. अच्छे विचारशील मंच अपने विवेक से कभी-कभी अपने पाठक के मनोजगत और अभिरुचियों को विस्तृत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसे नियमित नहीं कर सकते.
हिंदी की गंभीर वैचारिक पत्रिकाओं के पाठक उनके पास इसलिए आते हैं कि उन्हें हिंदी में साहित्यिक-वैचारिक ऐसी सामग्री मिलती है जो हिंदी अखबारों और दूसरे मंचों से नहीं मिलती. बहुत से पाठक ऐसे हैं जो अंग्रेजी में भी पैठ रखते हैं और राजनीति-युद्ध-वैश्विक मामलों- पर्यावरण-अर्थजगत जैसे विषयों पर अपनी जिज्ञासाएं अंग्रेजी समाचार माध्यमों से पूरा कर लेते हैं. मेरे जैसे लोग इस श्रेणी में आते हैं. इन विषयों पर अंग्रेज़ी जैसी सामग्री की उपलब्धता/प्रचुरता हिंदी/अन्य भारतीय भाषाओं में न अब है, न शायद होगी.

अरुण देव (लेखक, वेब पत्रिका ‘समालोचन’ के संपादक): हिंदी पत्रिकाओं का यह खराब समय है. धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान जैसी इस समय कोई पत्रिका नहीं है. इंडिया टुडे और आउटलुक के हिंदी संस्करण भी लुप्त होने को हैं. ये पत्रिकाएं समाज और राजनीति आदि की व्याख्या करती थीं. इनसे एक समझ बनती थी. बड़े प्रसार वाली इन पत्रिकाओं को बड़े संस्थान प्रकाशित करते थे. उनकी प्राथमिकताएं बदल गईं. अधिक मुनाफ़े के लिए वे दूसरे माध्यमों को प्रश्रय देने लगे. अब जो पत्रिकाएं निकल रही हैं, उनमें अधिकतर व्यक्तिगत प्रयासों से निकल रही हैं.
हिंदी के पास साहित्य का ही पाठक बचा है. राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय राजनीति और युद्ध आदि से संबंधित सामग्री के प्रकाशन के लिए आपको संवाददाताओं की आवश्यकता होगी. ज़ाहिर है यह खर्चीला होगा. यह बड़े प्रसार वाली पत्रिकाओं के लिए ही संभव है. पाठक इन विषयों को मूल हिंदी में पढ़ें, इसके लिए पत्रिकाओं को विश्वस्तरीय गुणवत्ता अर्जित करनी होगी. जो फिलहाल बहुत मुश्किल है.

आलोक श्रीवास्तव (कवि, ‘अहा ज़िंदगी’ के भूतपूर्व संपादक): ऐसा हमेशा से नहीं था. 1900 से 1950 तक भारत की आज़ादी ही नहीं, भारत के नवनिर्माण का भी स्वप्न था. उस समय की पत्रिकाओं को देखने पर पता चलेगा कि विषयों की विविधता और उनकी व्यापकता कितनी थी. लंबे समय से हिंदी पत्रिकाओं का लक्ष्य यह नहीं रह गया है कि वह अपने पाठक के बौद्धिक व आत्मिक स्तर का उन्नयन करें, अपितु वह उन्हें अपनी विचारधारात्मक स्थिति से कायल करने को प्रमुखता देने के कारण एकरस व एकायामी हो कर रह गई हैं. हालांकि गंभीर पत्रिकाएं भी कितनी हैं? और जो भी हैं, उनकी पाठक तक पहुंच भी कितनी है? इसी कारण हिंदी में पत्रिकाएं अब एकतरफा मामला हैं, उनकी समाज में कोई अंतर्क्रिया अब नहीं है.
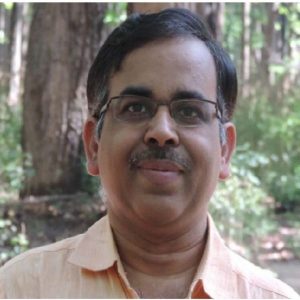
मधु कांकरिया (प्रतिष्ठित लेखिका): हिंदी के साथ सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आज़ादी मिलने के बाद वह गंभीर चिंतन मनन के आदान- प्रदान की भाषा कभी नहीं बनी. उसे राजभाषा के रूप में सीमित किया गया है या विशुद्ध मनोरंजन की भाषा बनती गई. पिछले कुछ दशकों में खाते-पीते मध्यमवर्गीय घरों की युवा पीढ़ी हिंदी भाषा से दूर होती चली गई. हिंदी की रोटी खाने वाले लोग हिंदी दिवस पर खूब रस्म अदायगी वाली भाषणबाजी कर लेते हैं और हिंदी के नाम पर अपनी दुकान चलाते हैं. ज्ञान- विज्ञान की भाषा वह कभी नहीं बन पाई. कई विषयों पर मूल पुस्तकें हिंदी में कभी लिखी ही नहीं गईं. यहां तक कि संस्कृति के गंभीर सवाल भी अब हिंदी मीडिया में अप्रासंगिक हो चले हैं. एक दोष विश्वविद्यालयों के हिंदी विभागों में कार्यरत उन हिंदी प्रोफेसर का भी है, जिनके लिए सारी समस्याएं आज भी केवल रीतिकाल, भक्तिकाल, छायावाद, प्रसाद और पंत की चर्चाओं तक सीमित हैं .साहित्य और पाठ्यक्रम के बाहर की दुनिया में राजनीति, वित्त, समाज विज्ञान, मनोविज्ञान, टेक्नोलॉजी आदि से जुड़ी समस्याओं पर वे लगभग शून्य हैं. उनका कोई वैचारिक संसार नहीं है.

संजय सहाय (वरिष्ठ लेखक, ‘हंस’ के संपादक): आप हंस के संपादकीय देखें, वह राष्ट्रीय, अतंरराष्ट्रीय राजनीति पर भी होते हैं, सामाजिक मुद्दों पर भी होते हैं. ज़्यादातर तो साहित्येतर ही होते हैं. हंस के आलेख पढ़िए… तो यह कहना गलत होगा कि सिर्फ साहित्य तक ही सीमित कर दिया गया है. दूसरी पत्रिकाएं भी अपनी सीमा में अच्छा काम कर रही हैं. जो ज़िम्मेदारी लघु पत्रिकाओं को निभानी चाहिए, अन्य पत्रिकाएं भी निभा रही हैं.

आशुतोष कुमार (आलोचक और कवि, ‘आलोचना’ पत्रिका के संपादक): हिंदी में अभी भी फिलहाल समकालीन जनमत, नया पथ, समयांतर और प्रतिमान जैसी गंभीर वैचारिक पत्रिकाएं निकल रही हैं जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रश्नों को भी महत्वपूर्ण स्थान देती हैं.
सरिता और कादम्बिनी जैसी लोकप्रिय पत्रिकाएं भी वैचारिक लेखों को जगह देती हैं. हालांकि, यह भी सच है कि इन पत्रिकाओं ने अपने पुराने मेयार को खो दिया है. धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, रविवार और माया जैसी पत्रिकाएं बीते हुए जमाने की चीज हो गई हैं, लेकिन उनकी यादें अभी तक बासी नहीं हुई हैं.

2. जिस भाषा ने अज्ञेय, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, मनोहर श्याम जोशी, प्रभाष जोशी जैसे राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संपादक दिए थे, उनके उत्तराधिकारी कहां हैं?
मृणाल पांडे: नए मालिकान और मनीजर खुद हिंदी पढ़ते-लिखते नहीं थे, पर वे अपने अंग्रेज़ी पत्र-पत्रिकाओं के हिंदी अनुवादों का बाज़ार में प्रचार-प्रसार करना जानते थे. इससे बड़े प्रकाशन संस्थानों के स्टाफ़ के खर्चे बचते और राजनैतिक पैरोकार भी मिलते थे. वैसे भी हिंदी पट्टी के पाठकों में इस बीच आत्मदया और हीनता बोध गहराने लगा था. वे जूठन को प्रसाद मान कर संतुष्ट हो रहे थे. उनके बच्चे अंग्रेज़ी स्कूलों की संस्कृति से जुड़े और हिंदी से दूर हो गए. संपादक भी 1990 तक प्रायः राजनैतिक आधारों पर ही नियुक्त किए जाने लगे थे. वे स्वायत्तता की बजाय राजनेताओें और विज्ञापनदाताओं के पक्षधर बनते गए. इसमें निजी लाभ लोभ निहित था. कुछ राज्यसभा में गए, कुछ राजदूत या हिंदी संस्थानों की रेवड़ियां पा कर संतुष्ट हो गए.
राहुल देव: इन जैसे बड़े कद और स्तर के संपादकों का अभाव हिंदी पत्रकारिता के लिए ही नहीं समूचे हिंदी समाज के लिए एक त्रासदी है, दुर्भाग्य है. आप ध्यान देंगे कि जो नाम आपने लिए अज्ञेय, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी, प्रभाष जोशी (मैं इनमें राजेंद्र माथुर, विद्यानिवास मिश्र, राहुल बारपुते (नई दुनिया) के नाम भी जोड़ूंगा), ये सब देश के उन तीन सबसे बड़े मीडिया घरानों के अखबारों के संपादक बन सके क्योंकि उनमें स्वामी और संपादक के पदों और दायित्वों में एक स्पष्ट विभाजन था. ये समूह हैं टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस. वे मालिक बड़ी सोच के थे, इसलिए इन बड़े लोगों को संपादक बना सके और संपादकीय स्वायत्तता दे सके. उनके अपने समय में ही दूसरे बड़े हिंदी अखबारों के संपादक आम तौर पर उनके मालिक ही हुआ करते थे. बड़े संपादकीय निर्णय मालिक ही लेते थे. हिंदुस्तान टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस समूह ने संपादक पद की गरिमा को कुछ हद तक बनाए रखा है, हालांकि बड़े निर्णयों में वहां भी पलड़ा प्रबंधन का ही भारी रहता है. एक्सप्रेस के हिंदी अखबार जनसत्ता का शायद मैं अंतिम स्वायत्त संपादक था. अब पूरे अखबार को ही कंकाल बना दिया गया है. सबसे बड़े समूह टाइम्स समूह ने संपादक पद को दशकों पहले तिलांजलि दे दी थी. उसने सारे बड़े-छोटे समूहों के लिए संपादकीय विभाग के ऊपर प्रबंधन के प्राधान्य/वर्चस्व को पूरे उद्योग का नियम बना दिया और अखबारों-पत्रिकाओं के लिए अच्छी पत्रकारिता की जगह लाभार्जन को अनुकरणीय ‘बिज़नेस मॉडल’.
बड़े संपादक के लिए बड़े दिल और दृष्टि का प्रकाशक/मालिक चाहिए. जब दोनों मिलते हैं तब वैचारिक स्वतंत्रता और संपादकीय उत्कृष्टता के मानक बनते हैं. आज के मीडिया मालिकों पर टिप्पणी की इससे ज्यादा ज़रूरत नहीं है. पाठकों को भी कमजोर सामग्री की आदत पड़ गई है. न भी पड़े तो उनके पास विकल्प नहीं है.
अरुण देव: पत्रिकाएं हमेशा अपने संपादकों के कारण जानी जाती हैं. संपादकों के उत्तराधिकारी नहीं होते हैं. महावीरप्रसाद द्विवेदी के बाद भी सरस्वती वर्षों निकलती रही. धर्मवीर भारती के बाद भी ‘धर्मयुग’ निकला. पर न वह सरस्वती सरस्वती थी, न वह धर्मयुग धर्मयुग. हर काल-खंड अपने लिए अपनी प्रतिनिधि पत्रिका गढ़ता है और अपने संपादक तलाशता है. ऐसा लगता है इस समय हिंदी समाज को किसी वैचारिक पत्रिका की जैसे जरूरत ही नहीं है. आम पाठकों के पढ़ने की भूख को सोशल मीडिया ने अपनी सम्मोहक उपस्थिति से नष्ट कर दिया है.
आलोक श्रीवास्तव: उपरोक्त सभी नाम बड़े पूंजीपति घरानों से निकलने वाले पत्र-पत्रिकाओं के संपादकों के हैं. इनका होना इस बात से जुड़ा था कि ऐसे समर्थ संस्थान थे, और उनके पास ऐसे संसाधन थे, जो बड़ी प्रसार संख्या वाली पत्रिकाएं प्रकाशित कर सकें. बड़ी प्रसार संख्या वाली स्तरीय पत्रिका के प्रकाशन का सीधा मतलब है कि आप उस भाषा के स्तरीय सामग्री की तलाश करने वाले पाठक तक पहुंचें और इसके लिए पत्रिका का स्वरूप और स्तर बेहतर हो. तो इनके उत्तराधिकारी का मसला नहीं है. भारत बदल गया है, अर्थात भारत का समाज अब एक उपभोक्तावादी समाज है. सभी बड़े संस्थान इस उपभोक्तावाद के ‘पार्ट एंड पार्सल’ हैं. अतः हिंदी में किसी स्तरीय पत्रिका को निकालने की उन्हें अब कोई जरूरत नहीं है. उपरोक्त नाम जिन पत्रिकाओं के संपादक रहे हैं, वे पत्रिकाएं आज भी यदि निकलें और भारी प्रसार संख्या, यहां तक की महंगे विज्ञापनों वाली हों तो भी वे बड़े संस्थान को अधिक मुनाफा नहीं दिला पाएंगी. यह पत्रिका के अर्थशास्त्र का मुख्य आयाम है. मोटे तौर पर बात यह है कि धर्मयुग जैसी पत्रिका अधिकतम मुनाफा भी दे तो आज साल में कुछ करोड़ का मुनाफा देगी, परंतु टाइम्स समूह का अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया एक दिन में ही उससे कई गुना अधिक मुनाफा देने में सक्षम है. ऐसी स्थिति में किसी भी बड़े संस्थान का मालिक यह नहीं चाहता कि उसकी बिल्डिंग की जगह में वह पत्रिका उतनी अनावश्यक जगह घेरे, या उसे उसके प्रबंधन आदि में धन, समय व दिमाग खर्च करना पड़े.
मधु कांकरिया: 90 के बाद का दशक हिंदी पत्रकारिता के पतन का दशक है. दिनमान जैसी पत्रिका आपातकाल के बाद रघुवीर सहाय के वहां से हट जाने के बाद आप्रासंगिक हो चुकी थी. धर्मयुग की लौ धर्मवीर भारती के बाद बुझ गई. भारती जी जैसी समझ किसी के पास नहीं थी, जहां लोकप्रिय पत्रकारिता और गंभीर सामग्री का एक संतुलन स्थापित किया गया था. संपादक नाम की संस्था समाप्त हो गई और बड़े प्रकाशन गृहों में संपादक नामक प्राणी मालिकों का सिर्फ एक आज्ञाकारी नौकर बनकर रह गया. पत्रकारिता का यह पतन 90 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उदय से भी जोड़कर देखना चाहिए. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कॉरपोरेट जगत का पैसा लगता गया और वहां सामाजिक यथार्थ, विज्ञापन, आर्थिक मुनाफा और मनोरंजन एक दूसरे में घुल मिल गए. धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, प्रभाष जोशी, राजेंद्र माथुर, मनोहर श्याम जोशी और किसी हद तक राजेंद्र यादव के बाद कोई ऐसा संपादक नहीं आया जो बड़ी प्रसार संख्या वाली हिंदी पत्रकारिता को एक दिशा दे पाता. लघु पत्रिकाओं में आज तद्भव, पक्षधर, बनास जन, अकार, समयांतर और वागर्थ जैसी पत्रिकाएं निश्चय ही अपनी सीमाओं में अच्छा कार्य कर रही हैं, लेकिन इनके अलावा किस पत्रिका का नाम लिया जाए जो कविता कहानी और साहित्य जगत की चौहद्दियों को पार कर अपने समय के समाज और संस्कृति के गंभीर सवालों से जुड़ती हो?
संजय सहाय: वो प्रिंट का समय था. आज के समय का माध्यम तेज़ी से बदल रहा है. सोशल मीडिया बड़ी भूमिका निभा रहा है और वह अपने आप में कोई बुरी बात नहीं है. केवल ये है कि कभी-कभी कमी खलती है. बहुत सारे फेसबुक पर जो पोस्ट आते है, वहां कभी-कभी संपादक की कमी खलती है. उन चीज़ों का सत्यापन करने से लेकर उन सभी चीज़ों के संपादन करने तक में… लेकिन समय बदेलगा तो चीज़ें बदलेगी. इससे प्रभावित नहीं होना चाहिए. जो भी समाज है वो अपने हिसाब से, अपने समय के हिसाब से, अपने रास्ते तलाश लेता है, इसमें विज्ञान की बहुत बड़ी भूमिका होती है. अब आप पीछे लौट कर तो नहीं जा सकते है. आप आगे ही जाइएगा.
आशुतोष कुमार: भारत में पत्र- पत्रिकाओं के पराभव का बड़ा कारण उन्मादी राष्ट्रवाद का प्रसार भी है. राष्ट्रवाद हमेशा भावेश को बढ़ावा देता है और विचारशीलता को निरुत्साहित करता है. आज विचार की जरूरत सबसे ज्यादा दलित, आदिवासी और स्त्री पाठकों को है जो सदियों से कुचले गए अपने अधिकारों के प्रति सचेत हुई हैं. यही कारण है कि आज इन वंचित श्रेणियों के मुद्दों को उठाने वाली पत्रिकाओं का उभार देखने को मिल रहा है.
3. हिंदी की प्रमुख समाचार पत्रिकाएं अपने अंग्रेज़ी संस्करण का अनुवाद बनकर क्यों रह गई हैं?
राहुल देव: पहला कारण तो प्रकाशन का सर्वोच्च और अंतिम लक्ष्य अधिकाधिक लाभार्जन बन जाना है. अनुवाद सस्ता पड़ता है. पूरी संपादकीय टीम, संपादक, समाचार-संकलन और अच्छे स्वतंत्र लेखकों पर खर्च सब आधे से भी कम हो जाते हैं. दूसरा, अच्छे हिंदी पत्रकार भी जब इतनी बड़ी संख्या और कम वेतन पर उपलब्ध हैं तो महंगे क्यों रखे जाएंं? तीसरा, मार्केटिंग विभागों और युवा मालिकों की कोई निजी रुचि और लगाव भाषाई प्रकाशनों से नहीं है क्योंकि उनकी पूरी आंतरिक-बाह्य दुनिया अंग्रेज़ी की है. हिंदी प्रकाशन उनके लिए केवल ‘ब्रांड एक्सटेंशन’ हैं जो विज्ञापन पैकेज में मुख्य अंग्रेज़ी प्रकाशन के साथ खासा अतिरिक्त राजस्व ले आते हैं.
अरुण देव: यह उनके लिए कम खर्चीला और सुविधाजनक है. जो पत्र-पत्रिकाएं अंग्रेजी में भी निकलती हैं उनके लिए हिंदी समाचार पत्रिकाएं कम मुनाफा देने वाला क्षेत्र है. इसमें वह न्यूनतम निवेश करते हैं और उसका दर्ज़ा दोयम बनाए रखते हैं. अधिकतर ये अनुवाद अपठनीय, अप्रासंगिक और बनावटी होते हैं इसलिए कुछ ही दिनों में इनसे पाठकों को ऊब होने लगती है और पत्रिकाओं का प्रसार गिर जाता है. हिंदी समाज को सिर्फ हिंदी में निकलने वाली किसी पत्रिका के लिए जगह बनानी चाहिए, जिसकी गुणवत्ता विश्वस्तरीय हो.
आलोक श्रीवास्तव: हिंदी की प्रमुख समाचार पत्रिकाएं अपने अंग्रेजी संस्करण का अनुवाद बनकर रह नहीं गई हैं, अपितु वे आरंभ से ही उसी स्वरूप में निकली थीं. वे निकली ही इस उद्देश्य से थीं कि अपने अंग्रेजी संस्करण की व्यावसायिक सफलता को बहुत अधिक खर्च किए बिना भुना सकें. और ऐसी पत्रिकाएं हैं ही कितनी? दो ही तो पत्रिकाएं हैं आउटलुक और इंडिया टुडे, जो अपने हिंदी पाठकों को उनके मूल अंग्रेजी प्रकाशन का अनुवाद, वह भी संपूर्ण नहीं आंशिक, पेश करती हैं. इन दोनों ही पत्रिकाओं के हिंदी संस्करण के प्रसार का वास्तविक आंकड़ा यह बता देगा कि बाजार में अथवा पाठकों तक इनकी पहुंच बेहद, बेहद कम है. तो मसला यह नहीं है कि वे अनुवाद हैं. मसला यह है कि हिंदी में व्यापक प्रसार वाली कोई भी पत्रिका अब नहीं है, और इसी कारण से हिंदी में व्यापक प्रसार वाली कोई समाचार पत्रिका भी नहीं है. यदि होती तो उसे हिंदी की मौलिकता के आधार पर खुद को खड़ा करने की जरूरत पड़ती.
मधु कांकरिया: इसका कारण ही ऊपर बताया जा चुका है- कॉरपोरेट जगत, मुनाफाखोरी, सनसनी और सस्ता मनोरंजन. बड़े कद, विचार दृष्टि और संस्कृति की चेतना वाले गंभीर संपादकों का हिंदी पत्रकारिता में अभाव है. एक उदाहरण हम दें. बहुत सारे लोग शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं जिन्हें अंग्रेजी का बहुत सीमित ज्ञान है. क्या हिंदी में कारोबार जगत की ही कोई ऐसी पत्रिका आई है जो वित्तीय विषयों पर गंभीर सामग्री देती हो? सिनेमा पर क्या कोई गंभीर पत्रिका आज आपको देखने को मिलती है? खेलकूद जगत पर कोई अच्छी पत्रिका आज है?
संजय सहाय: इंडिया टुडे साल में साहित्य वार्षिकी निकालती है, उसका अंग्रेजी से क्या लेना देना है? उनका जो अपना सेटअप है, उसे देखते हुए जो बेहतर समझते हैं, करते हैं. जो खबरी पत्रिकाएं होती हैं, जो खबरों का विश्लेषण करती हैं तो उनके लिए तो ये करना बनता है. ऐसा थोड़ी होगा कि जो इंडिया टुडे अंग्रेजी का पाठक है उसे अलग ज्ञान मिलेगा और हिंदी के पाठक को अलग ज्ञान मिलेगा. ये तो हो ही नहीं सकता. जो उनके मुख्य आलेख होंगे उनका अनुवाद तो आएगा ही आएगा चाहे- हिंदी से अंग्रेजी में हो, या अंग्रेजी से हिंदी में.
आशुतोष कुमार: आउटलुक और कारवां जैसी अंग्रेजी पत्रिकाओं के हिंदी संस्करण अभी भी बेहतर सामग्री दे रहे हैं. अंग्रेजी की ऑनलाइन पत्रिका द वायर का हिंदी संस्करण भी अच्छा है. लेकिन दलित, आदिवासी, स्त्री और पर्यावरण जैसे प्रश्नों को केंद्र में रखकर बहुत सी नई पत्रिकाएं सामने आई हैं जिनके पास बहुत बड़ा पाठक वर्ग भी है.
गिरावट तो अंग्रेजी और उर्दू के पत्रिका जगत में भी देखी जा रही है. इसका एक कारण इंटरनेट और सोशल मीडिया का विकट विस्तार है. दूसरा और इससे बड़ा कारण यह है कि 90 के बाद नवउदारवाद के वैश्विक प्रसार के चलते बाज़ार ने विचार को विस्थापित कर दिया है. अब लोगों का ध्यान प्रबंधन, मार्केटिंग, सूचना, तकनीक आदि पर अधिक है, विचारमूलक विधाओं और मानविकी पर कम.
4. हिंदी में सामरिक, आर्थिक, वैश्विक इत्यादि विषयों पर लिखने वालों की कमी क्यों है? हिंदी के धनाढ्य मीडिया संस्थान इन विषयों से क्यों कतरा रहे हैं, इन पर निवेश क्यों नहीं कर रहे हैं?
मृणाल पांडे: यह समय लिखित परंपरा नहीं, वाचिक परंपरा के उभार का है, जब मोबाइल पर सारी दुनिया सिमटी जा रही है. डिजिटल पत्रकारिता यहां फल-फूल सकती है. बहुत जगह है यहां हर विषय के लिए. अफ़सोस हिंदी ने हमेशा की तरह हिंदी के अच्छे पाठक, लेखक रचने में फिर कोताही की है. हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में लिखने में सक्षम पहली पीढ़ी के गुणाकर मुले, राहुल सांकृत्यायन, कपिला वात्स्यायन, डॉ. मोतीचंद्र जैसे बहुश्रुत, बहुपाठी भाषाविद्, इतिहासकार, अर्थशास्त्री, भू-वैज्ञानिक कहां हैं? वहीं, स्वाभिमानी, स्वायत्तता के पक्षधर गुणग्राही संपादकों को जाने-अनजाने परे कर दिया है.
राहुल देव: इसके दो आयाम हैं. किसी भी विषय में पढ़ने-लिखने-बोलने वाले विशेषज्ञ और विद्वान तब बनते हैं, जब उनको पढ़ने-सुनने-सराहने वाले बड़ी संख्या में हों. यह बहुत कुछ निर्भर करता है उस भाषा समुदाय की सामूहिक बौद्धिक/ज्ञानात्मक रुचियों-जिज्ञासाओं-आवश्यकताओं पर. जिस समुदाय में ये बड़ी मात्रा में मौजूद होती हैं वह अपने विद्वान-विशेषज्ञ पैदा कर लेता है. वे बीजरूप में तो हर समाज में मौजूद होते हैं लेकिन उभरने-चमकने के लिए उन्हें सामाजिक-सांस्थानिक-राजकीय प्रोत्साहन चाहिए.
वृहत्तर हिंदी समाज अधिकांशतः ज्ञान-विमुख है. उसकी पुरानी ज्ञान परिपाटियां सूख चुकी हैं. उसकी सर्वाधिक ऊर्जा जीवन के अस्तित्वमूलक संघर्षों, सस्ती राजनीति और सतही धार्मिकता में खप रही है. उसके उच्च शिक्षित युवा भी अपमानजनक स्तर और आय की नौकरियों के लिए भटक रहे हैं, पीटे-मारे जा रहे हैं. ऐसे में उच्चतर ज्ञान-संधान और ज्ञान-निर्माण को संभव बनाने वाली ज़मीन-खाद-पानी-हवा कहां हैं?
जिस समाज यानी पाठक-दर्शक वर्ग से ज्ञानात्मक सामग्री की मांग भरपूर मात्रा में नहीं उभर रही है उसे मीडिया संस्थान वह मंहगी सामग्री क्यों देंगे? इसलिए वे वही परोसते हैं जो बिकता है और उनके लक्ष्य वर्ग को संतुष्ट रखता है.
अरुण देव: हिंदी के धनाढ्य मीडिया संस्थान पत्रकारिता के अलावा दूसरे माध्यमों से भी पैसा कमा रहे हैं. अधिकतर लोग हिंदी का अख़बार अपना प्रभाव बढ़ाने या सत्ता साधने के लिए निकाल रहे हैं. वे अपने पाठकों को सिर्फ उतना ही देते हैं जितने से वे प्रतियोगिता में टिके रहें. अब पत्रकारिता मिशन नहीं है. दुर्भाग्य से उसमें पेशागत व्यावसायिकता भी नहीं आ पाई है. लगभग सभी हिंदी के अख़बार लोकल (स्थानीय) बन गए हैं. उन्हें सामरिक, आर्थिक या वैश्विक विषयों पर खबर या व्याख्या देने की आवश्यकता ही नहीं महसूस होती है. अपने पाठकों से खबरों को छुपाकर या बदलकर वे उनसे छल कर रहे हैं. इससे पाठक निराश होकर एक दिन इन्हें पढ़ना छोड़ देता है.
आलोक श्रीवास्तव: हिंदी में किसी भी विषय पर अच्छा लिखने वालों की कमी नहीं है. अगर सचमुच ऐसी पत्रिकाएं होतीं तो उनके साथ-साथ ऐसा लिखने वालों का और विकास भी होता. बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि अंग्रेजी की तुलना में हिंदी में सभी विषयों पर अच्छा लिखने वाले बहुतायत में हैं, बस उनके पास कोई मंच या जरिया नहीं है. अंग्रेजी में मंच हैं और इतने अधिक हैं कि भारत में उपरोक्त विषयों पर औसत या उससे भी कमतर लिखने वाले बड़े लेखकों और विशेषज्ञों के रूप में स्थापित हैं. हमें यह याद रखना चाहिए कि हिंदी का लेखक-वर्ग, जहां तक पत्रकारिता का संदर्भ है, अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाओं का स्रोत भी प्रयोग करता है, वह अंग्रेजी लेखकों की तरह वैसा एकायामी या सीमित नहीं है. हां, हिंदी की समस्या दूसरी है, वह यह कि एक तो मंच नहीं हैं, और जो होते हैं उन पर औसत किस्म के लोग बड़ी तत्परता से काबिज हो जाते हैं – खासकार पत्रकारिता और विश्वविद्यालयी तंत्र में.
मधु कांकरिया: वैश्विक पूंजीवाद की इस नई अवस्था में सारी गतिविधियों के केंद्र में केवल मुनाफाखोरी है. पत्रकारिता जो कि समाज का ‘चौथा स्तंभ’ कहलाती थी, जो समाज को एक रोशनी देती थी और ज्ञान- विज्ञान के प्रसार का एक माध्यम थी, उसको पूंजी के इस प्रभुत्व ने पूरी तरह से अपना गुलाम बना लिया है.
संजय सहाय: इन विषयों से कतराने का कारण है कि वे सरकार की नीतियों को ही देखते हैं. आप कॉरपोरेट की बात कर रहे हैं तो वह हमेशा सरकार का रुख और सरकार का हित देखकर ही अपना पक्ष चुनते हैं. उनकी कोई बहुत रुचि नहीं होती कि हम ऐसी कोई बात कहें कि विवादस्पद हो जाएं.
5. हिंदी पत्रिकाओं का क्या भविष्य है?
अरुण देव: जब तक हिंदी समाज में कोई बड़ा वैचारिक आंदोलन नहीं होता है या समाज अपने साहित्य और कलाओं के लिए आग्रही नहीं होता है, हमें हिंदी की किसी अच्छी पत्रिका ही नहीं नाट्य-शालाओं, सांस्कृतिक केंद्रों की भी प्रतीक्षा करनी होगी.
राहुल देव: हिंदी पत्रिकाओं का ही नहीं, अखबारों का भी दूरगामी भविष्य धूमिल है. पत्रिकाएं पहले काल कवलित होंगी. वे तब तक टिकेंगी जब तक हिंदी में ऐसा मध्यमवर्ग उपस्थित है जो समाचार-विश्लेषण के लिए मुख्यतः हिंदी पर निर्भर है और इंडिया टुडे जैसी मंहगी पत्रिका खरीद सकता है. उसके लिए भी अब यूट्यूब तेज़ी से बढ़ता हुआ लोकप्रिय विकल्प है. पत्रिकाओं को भी अखबारों की तरह और मंहगा बनना पड़ेगा. इससे उनकी मांग घटेगी.
भारत चूंकि तकनीक और जीवन शैली में समृद्ध पश्चिम से होड़ करके उनके बराबर पहुंचने के लिए दौड़ रहा है इसलिए वहां के मीडिया, विशेषतः अखबारों-पत्रिकाओं के पुराने मॉडल के साथ जो हुआ है वह यहां भी होगा. न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, टाइम मैगजीन और द इकोनॉमिस्ट जैसे प्रकाशन जैसे-तैसे अभी बचे हुए हैं, लेकिन संघर्ष कर रहे हैं. बड़े-बड़े अखबार-पत्रिकाएं लुप्त हो गए. ऊपर से यहां एक विशिष्टता है जो वहां नहीं. भारत में जो परिवार आर्थिक रूप से मध्यमवर्ग में शामिल हो जाता है या उसके सपने देखता है, वह एक न्यूनतम आय होते ही अंग्रेज़ी का हो जाता है. वह अपनी मातृभाषा/परिवेश भाषा से खूंटा तुड़ा कर अंग्रेज़ी की ओर भाग रहा है. हिंदी-पंजाबी में यह परिघटना सबसे तीव्र है.
अभी हिंदी अखबारों-पत्रिकाओं के पाठक वही हैं जो अंग्रेज़ी-सक्षम नहीं हैं. हिंदी उनकी मजबूरी है. आज तथाकथित अंग्रेजी-माध्यम प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे 50% से अधिक हो गए हैं. यह संख्या विस्फोटक तेजी से बढ़ रही है. गरीब मां-बाप पेट काट कर अपने बच्चों को अंग्रेज़ी-शिक्षित-दीक्षित बनाने की स्वाभाविक होड़ में हैं. मुझे विश्वास है एक दो-ढाई दशक में यह प्रतिशत 90-95 हो जाएगा. उस समय हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं के युवा, शिक्षित, समृद्ध पाठक कितने बचेंगे? जब एक न्यूनतम समृद्धि के पर्याप्त पाठक नहीं होंगे तो अखबारों-पत्रिकाओं को विज्ञापन कौन देगा? बिना पाठक-विज्ञापन कोई व्यावसायिक प्रकाशन कैसे चलेगा?
अंतिम संकट, बचपन से ही किताबों से सीधे यूट्यूब-इंस्टाग्राम-फेसबुक रील्स देखने की तकनीकी छलांग लगा कर अपनी ज्ञानात्मक और मनोरंजन ज़रूरतों के लिए डिजिटल-अभ्यस्त और निर्भर हो चुकी वर्तमान पीढ़ियां वयस्क होकर पढ़ने की ओर कैसे और कितनी उन्मुख होंगी? एक गूगलित और यूट्यूबित विश्व में पत्रिकाओं-पुस्तकों का स्थान कहां और कितना होगा? वह भी हमारे भारतीय भाषा संसार में.
आलोक श्रीवास्तव: फिलहाल तो बड़े प्रसार वाली, व्यापक पाठक वर्ग तक पहुंचने वाली कोई भी पत्रिका हिंदी में है ही नहीं, फिर भविष्य का क्या सवाल. हां, यह तय है कि ऐसी कोई भी पत्रिका किसी भी बड़े संस्थान से ही निकल सकती है और कोई भी बड़ा संस्थान ऐसी पत्रिका निकालेगा भविष्य में, इसमें संदेह है. जहां तक साहित्यिक-वैचारिक किस्म की पत्रिकाओं का संबंध है तो वे तो 100 से लेकर 500 प्रतियों तक छापी जाकर उसके प्रकाशक-संपादक की कई तरह की भौतिक जरूरतों को पूरा करती हैं, अतः वे न सिर्फ निकलेंगी, उनकी संख्या भी बढ़ेगी. इसलिए भी कि तकनीकी रूप से यह काम पहले की तुलना में अब बहुत ही आसान और सुविधाजनक है. ये पत्रिकाएं हिंदी के छोटे-मोटे सत्ता-तंत्रों की अपनी जरूरत हैं.
मधु कांकरिया: मेरे विचार से पत्रकारिता का समूचा भविष्य हमारे राजनीतिक वातावरण से जुड़ा हुआ है. जब हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं में ही भयानक विघटन है फिर चाहे वह न्याय व्यवस्था हो, नौकरशाही हो, कानून व्यवस्था हो, विश्वविद्यालय हों, जब सभी जगह पर मूल्य का पतन है तो हिंदी पत्रकारिता से क्या उम्मीद की जाए? लेकिन इस सबके बीच में एक बात यह भी कहनी पड़ेगी की सोशल मीडिया और यूट्यूब पर एक समानांतर पत्रकारिता का नया समय भी दिखाई देता है. यह बहुत छोटे-छोटे साहसिक प्रयासों में दिखाई दे रहा है. जो अपनी निर्भीक आवाज को सामने रखते हैं. वह फिलहाल तो एक उम्मीद की किरण है जब तक कि उस पर भी फासिस्ट व्यवस्था अपना कोई बुलडोजर न चला दे.
संजय सहाय: अभी हिंदी पत्रिकाओं का भविष्य बहुत उज्जवल नज़र नहीं आ रहा है. लेकिन लोग मेहनत कर रहे हैं. क्या नतीज़ा निकलेगा पता नहीं. हो सकता है कि इन पत्रिकाओं का स्वरूप बदल जाए. मुझे लगता है कि पत्रिकाएं निकलती रहेंगी, बस उनका स्वरूप बदल जाएगा. पढ़ने की आदत भले ही हमारे यहां काम हुई है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वैश्विक स्तर पर इसका भयानक असर पड़ रहा है. यहां भी लोग लौटेंगे, इतना भरोसा है भविष्य पर.
आशुतोष कुमार: हिंदी पत्रिकाओं का भविष्य उज्जवल है. उनका सुनहरा समय बस आने वाला है. जरूरत है इस बात को गहराई से समझने की. हिंदी के लोक वृत्त यानी पब्लिक स्फीयर का सामाजिक आधार बदल गया है. 90 पूर्व के जमाने में हिंदी के पाठक, लेखक और पत्रकार अधिकतर सवर्ण भद्रवर्ग के शिक्षित लोग हुआ करते थे. यह पूरा सामाजिक आधार नए जमाने के बाजार की मांगों के हिसाब से खुद को ढाल कर आज अंग्रेजीजीवी हो चुका है. लेकिन हिंदी में नए विशाल पाठक वर्ग का पदार्पण हो गया है. यह वर्ग है स्त्रियों का, उत्पीड़ितों का, वंचितों का, दलितों का, आदिवासियों का और गरीब अल्पसंख्यकों का. ये सभी समुदाय मिलकर एक ऐसे विराट पाठक वर्ग का निर्माण करते हैं जिसके सामने पुराना भद्रवर्गीय पाठकवर्ग हास्यास्पद रूप से लघुकाय नजर आता है.
वंचित उत्पीड़ित समुदायों ने अब अपने मीडिया, अपनी पत्र- पत्रिकाओं और अपने सिनेमा का निर्माण करना शुरू कर दिया है. हिंदी के आने वाले जमाने को संवारने वाले वर्ग यही हैं और इनका समय अब शुरू ही हो रहा है.





