अस्सी साल. आठ दशक. समय है कि दानव? जाने क्या-क्या पेट में समाया हुआ है. सोचिए ज़रा, मेरे बचपन में देश में कोक यानी कोका कोला की घुसपैठ नहीं हुई थी. पेय के नाम पर अव्वल नंबर पर था गोली वाला सोडा मय नींबू मसाला. और मज़ा यह कि हर व्यंजन, आलू टिक्की हो या तला पापड़; गोलगप्पे हों या बुढ़िया के बाल, जी हां, वही आपका कैंडी फ्लोस; सब माल फेरीवाले घर पर ला हाज़िर कर देते थे. गन्ने का रस और गंडेरी हो या भूभल में भुनी शकरकंदी या सामने भुने चनाज़ोर गर्म. सुबह शाम आता फेरी वाला हमारे खान पान और स्वाद का अहम हिस्सा था.
हम रहा करते थे आधुनिक नई दिल्ली में, पर पढ़ते थे हिन्दी माध्यम स्कूल में. ख़ुदा के फ़ज़ल से हमारे मां बाप ने हमें मिशनरी स्कूल के नर्सरी-किंडरगार्टन में नहीं भेजा, वरना ट्विंकल-ट्विंकल करते अजब घासलेट नज़र आते. प्राथमिक स्कूल पास करके गए लेडी इरविन स्कूल, जिसका सिर्फ़ नाम अंग्रेज़ था, था शुद्ध आज़ादी की लड़ाई लड़ने में मुब्तिला हिंदुस्तानी. 1947 से पहले मुसलमान टीचरों की भरमार थी. खूब उर्दू सुनी-बोली. मुल्क की तक्सीम में उनमें से काफ़ी पाकिस्तान चली गईं, पर सबने ख़ूब खुलूस और प्यार के साथ उन्हें विदा किया. बहुत याद आईं, अगले वक्त में. ऐसा नहीं था कि कोई मुसलमान टीचर रही नहीं, बस बहुतायत कम हो गई.
इस स्कूल की एक खास बात यह थी कि इसमें एक बांग्ला और एक हिंदी अनुभाग था. आप जानते ही होंगे कि जहां बंगाली रहें, इतनी गिरफ़्त के साथ कला-अभिव्यक्ति अपने हाथों में लेते हैं कि हिंदी भाषी, प्रशंसक और दर्शक बन रह जाते हैं. वही हमारे साथ हुआ. हमने खूब सरस्वती पूजा की, कांथा काढ़ना सीखा, तकली काती और आज़ादी की लड़ाई लड़ी, ख़ब्ती इतिहास की बंगाली टीचर का किया इतिहास का पुनर्लेखन भी पचा लिया. जी हां, 1857 की लड़ाई को, जिसे तब गदर कहने का रिवाज़ था, हमारी इतिहास टीचर मिस दासगुप्ता ने आज़ादी की पहली लड़ाई साबित कर दिया. वह भी ब्रिटिश काउंसिल के नुमाइंदों के सामने.
चूंकि हम जानते हैं, नारीवाद का एक अहम स्तंभ इतिहास का पुनर्लेखन है, तो कुछ लोग रौ में आकर मिस दासगुप्ता को नारीवादी घोषित कर दें तो कोई मुज़ायका न होगा. पर जनाब आप इतना तो मानेंगे कि वे केवल स्त्री की भूमिका को पार्श्व से निकाल कर इतिहास लेखन के केंद्र में नहीं लाई, एक सदी पहले हुए आंदोलन को ले बीच में ले आईं. अलबत्ता कह सकते हैं, एक स्त्री ही आठवीं कक्षा के बच्चों को यह पाठ पढ़ाने का जज़्बा रख सकती थी. इसलिए रहीं वे भीषण नारीवादी ही.
तब हम मात्र आठवीं कक्षा में थे. पर प्रतिरोध और लीक से हटकर चलने का जो कीड़ा ज़ेहन में घुसा, ताउम्र कुलबुल करता रहा. तभी न पक्की उम्र में शादी करने और बच्चे पैदा करने के बाद लेखक बने. जब हमारी साथी औरतें सहर्ष घरबार के भार से लदी देह पर परत-दर-परत चढ़ा सुकून से जी रही थीं. जो सुकून में नहीं थीं, और ज़्यादातर नहीं थीं, यह सच्चाई हमने ठहरकर समझी; वे भी लेखन जैसा ग़ैर-भरोसेमंद और पैसे से खाली पेशा अख्तियार करने को, बेवकूफ़ी और अय्याशी दोनों मानती थीं. तो माना करें. हमारी बला से. यूं हम समय से ज़रा आगे, समाज की सरहद पर मंडराते डोले, अपनी तमाम जवानी ही नहीं अब तक का बुढ़ापा भी.
§
खैर, बचपन पर लौटें तो यह वह ज़माना था जब घर को ठंडा रखने के लिए खस के पर्दे और टट्टियां (जी यही नाम था, फ़्रेम में जड़ी परतदार खस की पट्टियों का) लगाई जाती थीं. हमारे घर में पिताजी की तकनीकी हिकमत के चलते ऐसी व्यवस्था थी कि उन पर बराबर, ऊपर लगे पाइप के छिद्रों से पानी गिरता रहे. जिससे अन्य मध्यवर्गीय घरों की तरह बेचारे सेवक को लू में बाहर निकलकर खस पर पानी न डालना पड़े. पीने का पानी आमतौर पर मटकों में रखा जाता था जिसके मुंह पर घर के नल की मानिंद कपड़ा बंधा रहता था. उस वक्त का फ़िल्टर.
पर हमारे घर में सुराही का इस्तेमाल होता था, क्योंकि मटके से पानी निकालने के लिए कपड़ा हटाना पड़ता, जो स्वच्छ्ता के पैमाने पर खरा नहीं उतरता. फिर सुराही ज्यादा सुंदर हुआ करती थी, घर पर कई सुराहीदार गर्दनों की मल्लिका ख़ातूनों की रिहाइश के चलते सुराही, शायराना और इश्किया दर्जा पा चुकी थी. कमसिन स्टैंड में पोशीदा रखी जा सकती थी और उसे खस की चादर भी ओढ़ाई जा सकती थी. जिससे पानी कुछ और ठंडा दे सके.
जब 1954 में मैं बारहवीं कक्षा में पहुंची तब पहले पहल घर में फ्रिज आया. अरसे तक उसमें सिर्फ बर्फ़ जमाई जाती रही या घर पर बनी आइस्क्रीम रखी जाती रही. फ्रिज में रखा बासी खाना कोई खाता न था. फल, सब्ज़ी सब फेरीवाले से ताज़ा खरीद लिये जाते थे. बाज़ार जाना होता शौक़िया सामान खरीदने के लिए.
शौक़िया के सिलसिले में बतलाती चलूं कि 1946 में हमारे घर के पास बंगाली मिठाई की पहली दुकान खुली, जिसके चलते उस बाज़ार का नाम ही बंगाली मार्केट पड़ गया. बाद में यह चाट के लिए ज़्यादा मशहूर हुआ. दिल्लीवाले हुए तो ज़रूर खाई होगी. ज़्यादा खास बात यह कि 1947 के विभाजन के बाद, उससे कुछ दूरी पर, मुआवज़े में मिली ज़मीन पर पंजाब से आए शरणार्थियों ने फख्र के साथ रिफ्यूजी मार्केट खोला, जिसने बंगाली मार्केट को करारी स्पर्धा दी .
आप कहेंगे विभाजन की विभीषिका के बजाय, मैं यह सकारात्मक बात क्यों कह रही हूं. वह यूं कि नई दिल्ली में रिहाइश की वजह से मैंने मारकाट या फ़साद अपनी आंखों देखा न था. बल्कि वहां रहने वाले जो मुस्लिम परिवार पाकिस्तान जाना चाहते थे, उन्हें ख़ुलूस के साथ पिताजी व अन्य बाशिंदों ने सरहद तक पहुंचा दिया था. लेकिन दरियागंज और पुरानी दिल्ली जैसे इलाकों में, जो दिल्ली की गंगा जमुनी संस्कृति के मरकज़ थे, काफ़ी खून खराबा हुआ था. पर नौ बरस की कम उम्र में काफ़ी हद तक मेरे लिए विभाजन की विभीषिका मुल्क के दूसरे हिस्सों में होने वाली वारदात बनी रही.
मेरा भोगा हुआ यथार्थ कुछ था तो यह कि पंजाब से आए शरणार्थियों के कारण देश में उद्यम और कर्मठता का एक नया अध्याय खुला. यहां आने के कुछ दिन बाद ही उन्होंने व्यापार और व्यवसाय पर कब्ज़ा जमा लिया. केंचुए की चाल चलने वाले स्थानीय दिल्लीवाले भी सहसा, उन हिम्मती, नकचढ़े और ऊर्जावान लोगों की प्रतियोगिता में उचक-उछलकर आगे बढ़ने लगे. सारा समां बदल गया. सिर्फ आंखों देखी दिल्ली का नहीं, पूरे मुल्क का.
इसी के तुरंत बाद गांधीजी की हत्या हो गई. लाखों हिंदुस्तानियों की तरह वह मेरे लिए एक निजी त्रासदी थी. आज शायद मैं उन कम जीवित लोगों में से हूं, जो गांधीजी की रोज़ शाम होने वाली प्रार्थना सभा में जाते थे. हम तो खैर हफ़्ते में दो तीन बार जाते थे. फिर रेडियो पर रोज़ उनके प्रवचन का सीधा प्रसारण होता था. वह भी सुनते थे. रोज़ नहीं जाते थे सो बिन वजह उनकी हत्या के दिन 30 जनवरी को वहां नहीं थे. जिस दिन बम फटा, तब थे. पर लोग कुछ कसमसाए ही थे कि गांधीजी के संयत स्वर में कहने पर बैठ जाइए, चुपचाप बैठ गए थे. लगा जैसे कोई रद्दी नाटक था, वहां कुछ होने हवाने वाला नहीं था. होनी को न जानना ही तो उसे अनहोनी बनाता है.
मैं उनकी शवयात्रा में भी शामिल हुई थी. पिताजी ने बतलाया था, इलाहाबाद के कुंभ मेले के बाद उतनी भीड़ बस तब देखी थी.
13 दिन बिना किसी सरकारी हुक्म के लोगों ने बाक़ायदा सार्वजनिक मातम मनाया था. सिनेमाघर तक बंद रहे थे. और उसके विपरीत पिचहत्तर साल बाद की भी सुन लें.
कुछ दिन पहले लखनऊ रेडियो स्टेशन से पूछने पर पता चला कि रेडियो आर्काइव्स में उन के प्रवचनों की फ़ाइलों को दीमक लग चुकी! विरासत! कैसी विरासत? हम विस्मरण के पुरोधा हैं. फिर रेडियो ठहरा सरकार का पट्ठा! मेरे लिए, यह ख़बर मेरे शुरुआती रचनाकार के समय के बीत जाने की सबसे हैबतनाक, सदमा पहुंचाने वाली जानकारी थी.
बहुत जल्द हमने देश के भीतर उनके अहिंसा के पाठ को बिसरा दिया. शुरुआत तो विभाजन की भयानक मारकाट से हो ही चुकी थी. सो, देश के भीतर बराबर हिंदू-मुस्लिम फ़साद होते रहे. पर देश के बाहर नेहरू की करिश्माई निरपेक्ष विदेश नीति के चलते हम पूंजीवादी और साम्यवादी गुटों के बीच की हिंसा से बचे रहे.
§
पर बकरे की मां कब तक खैर मनाती. तिलिस्म टूटा चीन के आक्रमण से और अपने आज़ाद देश पर हमारा गर्व, अपनी बेहूदा हार से. 1962 का चीनी आक्रमण और हमारी हार, शायद मेरे समय और जीवन भर के सबसे दुखद क्षण होते, अगर उसके कुछ साल बाद 1984 में भोपाल में गैस रिसाव से हुआ भीषण नरसंहार न हुआ होता. और उससे कुछ पहले देश में जगह-जगह सिख नरसंहार!
वर्ष 1984 हमारे मुल्क और खुद मेरे लिए उतना ही भयावह वर्ष था जितना उस वर्ष के नाम से लिखे उपन्यास में ऑरवेल ने दर्शाया था.
जब पहली नवंबर को दिल्ली में नरसंहार शुरू हुआ, तभी मैंने उस पर कहानी लिखनी शुरू की, जिसे बिना नहाये-खाए मैं दो दिन तक लिखती रही. फिर अपनी सिख सहेली को दिखलाने पहुंच गई कि कुछ शब्दों को देख, बतला दे कि सही तरीके से प्रयुक्त हुए थे या नहीं. उसके साथ एक अत्यंत सकारात्मक पहलू यह घटा कि हमारे नए बन रहे घर में बिजली का काम करने वाले सरदारजी 4 नवंबर को हमारे पुराने घर पहुंचे और ठसके से बोले, ‘आपके पूजन में नहीं आ सका. आज गया तो देखा, खूब संभालकर एक कोक की बोतल रखी हुई है, सोचा ज़रूर मेरे लिए होगी, सो पीकर आ रहा हूं बधाई देने.’ इससे बड़ी इंसानियत और जवां मर्दानगी क्या होगी. हम नतमस्तक हुए.
वैसे भी वे बेटों को आईआईटी में वेल्डिंग सिखलाते थे तो दोनों ‘काके’ तो नतमस्तक होने ही थे. जैसे पहले हमारे दर्जनों मुसलमान दोस्त थे, अब सिख दोस्त थे. मेरी सच्ची कहानी में एक हिंदू औरत ने सिख नौजवान की जान बचाई थी. अब और सुनिए. हाल में वह कहानी, ‘अगली सुबह’, दुबारा प्रकाशित हुई तो आलोचकों को ऐतराज़ था कि जो हमलावर थे, उनकी जमात की औरत को ‘दूसरे’ की रक्षा करते क्यों दिखलाया गया था. तो समझे आप, यह फ़र्क आया इन चार दशकों में. इंसानियत दिखलाने से भी परहेज़ होने लगा कट्टरपंथियों को.
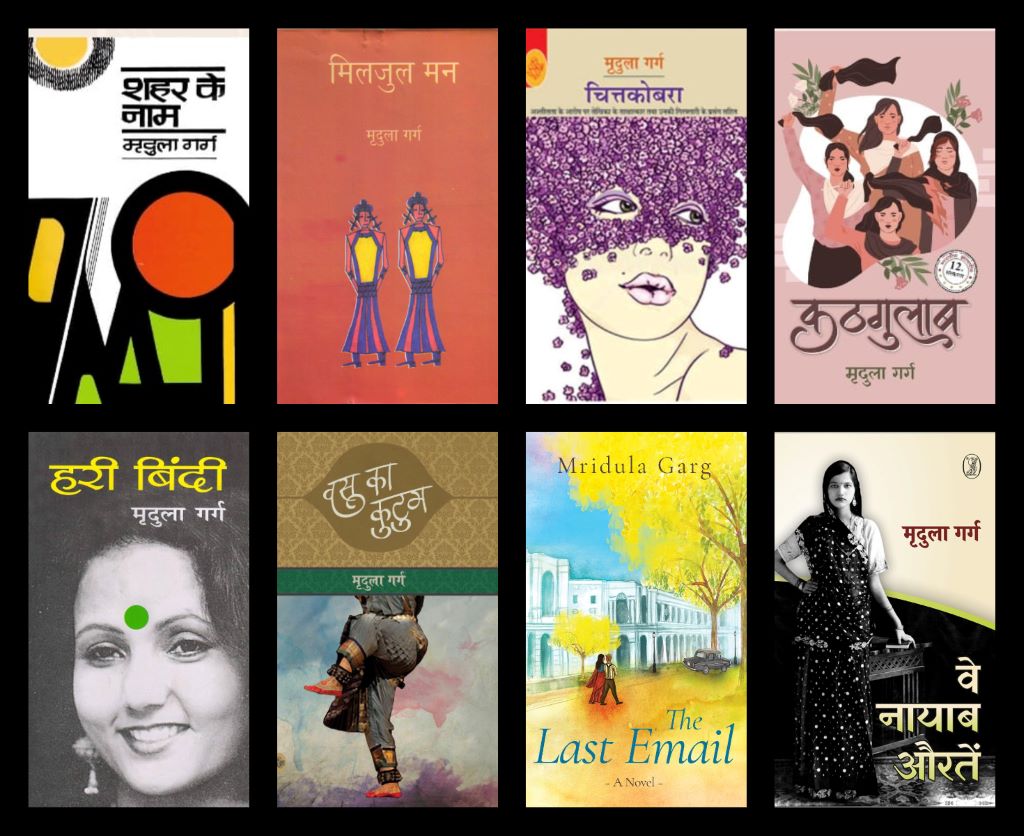
इन्हीं दशकों में हमने डिजिटल दुनिया में बहुत प्रगति की. मोबाइल, स्मार्ट फोन, कंप्यूटर, वेबसाइट्स और नेट बैंकिंग से होते हुए खुदा न करे, कृत्रिम बुद्धि (एआई) के जाल तक पहुंचने वाले बने. उधर सोशल मीडिया ने उत्तम और लुगदी का फ़र्क मिटा दिया. विचार को फ़ौरी प्रतिक्रिया में बदल दिया. हर फ़ेक खबर को बार-बार दोहराकर, यानी उनकी भाषा में वायरल करके, अंतिम सच बनाने का बीड़ा उठा लिया. हिटलर ने नहीं सोचा होगा कि अगली सदी में उसके कथन को हमारा सोशल मीडिया सच साबित करेगा.
तो आज हाल यह है कि मालूम नहीं रहता कि कौन ख़बर सच है या झूठ. दरअसल झूठ को अब झूठ नहीं, फेक कहते हैं. यानी झूठ और सच के बीच इतराता कथ्य. वही जो धर्मराज युधिष्ठिर ने बोला था और बोलकर भी धर्मराज कहलाते रहे थे.
ऑक्सफ़ोर्ड डिक्शनरी की भाषा में आजकल इसे कहते हैं, पोस्ट ट्रुथ या सत्य से परे. हमने तो सदियों पहले महाभारत के समय में ही इसे साध लिया था. अपने समय की बात करूं तो साठेक बरस पहले तक, समय-समय पर उजागर होती नफ़रत, दंगे और हिंसा, काफ़ी हद तक रोज़मर्रा की जिंदगी को महफ़ूज़ रहने देती थी. अब तो सदियों से चले आ रहे जाति भेद और उससे उत्पन्न शोषण, धार्मिक और वैचारिक भेदभाव, तमाम तबकों और धर्मों के बीच स्थायी नफ़रत और वैमनस्य जगा चुके हैं.
1939 के जर्मनी या आज के इज़रायल द्वारा रौंदे फ़िलिस्तीन की तरह, हमारे यहां भी किसी की ज़िंदगी या आज़ादी सुरक्षित नहीं हैं. हम प्रतिरोध तो कर रहे हैं, जितने भी हालात बिगड़ें, करने से बाज़ नहीं आते पर प्रतिरोधियों की गिनती दिन-पर-दिन कम होती जा रही है. मन के अंधकूप में डर समाया हुआ है कि कुछ भी कर लें, कुछ होने वाला है नहीं.
वैसे ही जैसे पराली को जलाने से पैदा हुए प्रदूषण को आसानी से रोकने के साधन उपलब्ध होने पर भी कुछ नहीं किया जा रहा. पूसा डिस्पेंसर बन गया, तकनीक में हम पिछड़े नहीं रहे, जो परली को खाद में तब्दील कर सकती है. पर काम को अंजाम देने का अपने यहां चलन जो था वह भी नहीं रहा. तो उसे खरीदे कौन? किसान के हिसाब से जाएं शहर वाले भाड़ में . वे कौन उसकी मदद को आ रहे हैं. शोषण ही किया है, 1947 से आज तक. यूं यह काम सरकार को करना चाहिए. पर सरकार अपने यहां आजकल सिर्फ चुनाव जीतने के लिए दंद फंद करती है, वोटर या नागरिक जाए भाड़ में अगले चुनाव तक. जिताने को ई.वी.एम. है ही. होता है किसी और माई के लाल देश में? ना जी ना. भारत सा कौन महान!!
बरसों पहले भी समय समय पर पीली काली आंधी आया करतीं थी. पर आज तो हर वक्त रोज़ -दर- रोज़ सिर पर प्रदूषण का जहरीला कोहरा टंगा रहता है. और अपनी फ़ितरत के मुताबिक, हमने इस जहर को भी शहरी ज़िंदगी का ज़रूरी हिस्सा मान लिया है.
मैं जानती हूं मेरे पाठकों को पराली का रोना रास नहीं आ रहा होगा. एंटी क्लाइमैक्स या विरेचन के विरुद्ध मालूम पड़ा रहा होगा. कहां विभाजन, गांधीजी की हत्या, सिख नरसंहार और धर्मराज के अर्ध-सत्य जैसे वजनी विषय और कहां आम नागरिक और किसान की ज़िंदगी और मौत का अदना फ़साना!
पर यही तो है आज का सत्य से परे घटती सच्चाई. बड़ी-बड़ी ऐतिहासिक घटनाएं, साहित्य के काल बोध को सिफ़र बना, लघु तम के सामने घुटने टेक देती हैं.
अब ऐसे लघु के विकराल बनते समय में क्या लेखक का समय और क्या लेखक का सत्य. सब गोलमाल है, बच्चा, सब गोलमाल है!!
(मृदुला गर्ग वरिष्ठ साहित्यकार हैं.)
(इस श्रृंखला के सभी लेख पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.)





