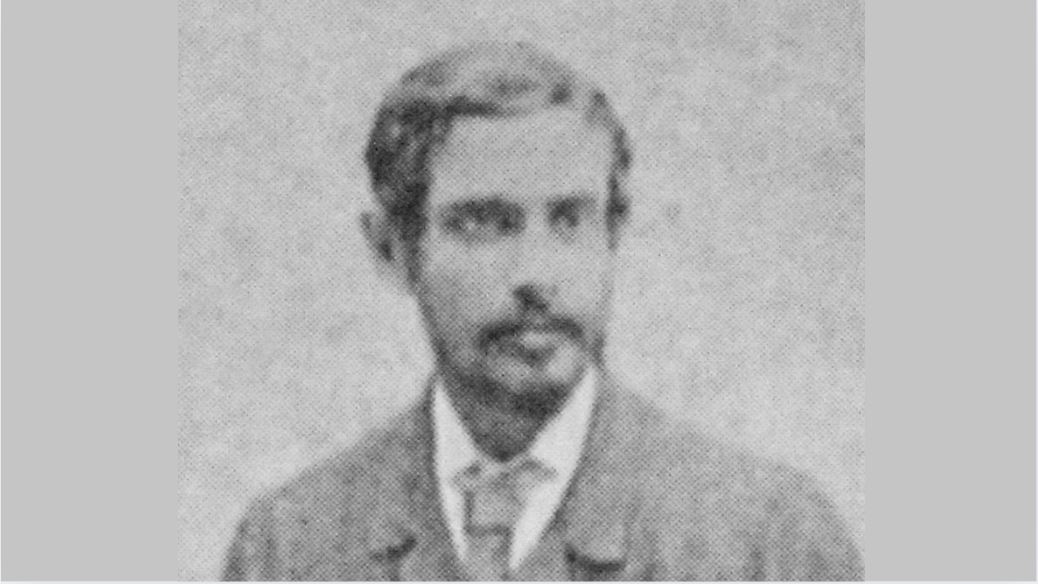हम भारतीयों की विस्मरण की प्रवृत्ति भी अजब है! हम अपने लेखकों, कवियों, कलाकारों और समाज सुधारकों आदि को उनके इस संसार से जाते ही या तो भुलाने में लग जाते हैं या फिर मजबूर-से अनमने व अधूरे ढंग से याद करते रहते हैं, जबकि ऐसे विस्मरण से भी और बेमन स्मरण से भी संबंधित शख्सियतों से लगभग एक जैसा अन्याय होता है.
हमारे पुनर्जागरण के नायकों में से एक स्मृतिशेष सत्येंद्रनाथ टैगोर भी हैं, जिनकी, गुरुवार (9 जनवरी) को पुण्यतिथि है, अब कुछ ऐसे ही अन्याय के शिकार हो चले हैं. उनकी जयंतियों व पुण्यतिथियों तक पर या तो उन्हें भुलाए रखा जाता है या कुछ इस तरह याद किया जाता है, जिसमें ज्यादातर जोर उनके ‘भारत के पहले भारतीय आईसीएस अफसर’ और ‘रवींद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई’ होने पर ही होता है.
हालांकि, उनका परिचय महज इतना नहीं है और 1857 में लड़े गए पहले स्वतंत्रता संग्राम को विफल कर देने के बाद कहीं ज्यादा क्रूर हो गए अंग्रेजों की गुलामी के दौरान उन्होंने अपने लेखन व सृजन के साथ देश, खासकर बंगाल के पुनर्जागरण के प्रयासों से जुड़कर भारतीयों के सामाजिक उन्नयन और महिला-पुरुष समानता के लिए जो बहुविध व बहुआयामी प्रयत्न किए, उनके उल्लेख के बगैर वह कतई पूरा नहीं होता.
यह ठीक है कि जून, 1863 में वे (इंपीरियल सिविल सर्विस के रूप में अंग्रेजों के एकाधिकार के लिए जानी जाने वाली) इंडियन सिविल सर्विस (आईसीएस) की प्रतिष्ठित परीक्षा पास कर उसके लिए चुने गए, तो कई हल्कों में उन्हें गोरों का गुरूर तोड़ने वाले ऐसे नायक के रूप में देखा गया था, जिसने सिद्ध कर दिया कि राजकाज के लिए भारतीय अंग्रेजों जितने ही सक्षम हैं और उन पर यह तोहमत सही नहीं है कि वे इसके लिए अंग्रेजों के मोहताज हैं.
पुनर्जागरण से बावस्ता
बहरहाल, उन्होंने लंदन में उक्त सेवा के लिए जरूरी प्रशिक्षण लिया और नवंबर 1864 में स्वदेश वापस लौटने के अगले बरस 1865 में अहमदाबाद के सहायक मैजिस्ट्रेट व कलेक्टर के पद पर नियुक्ति पाई. कोई तीन दशकों की नौकरी के उपरांत वे 1896 में सतारा (महाराष्ट्र) से जज के रूप में सेवानिवृत्त हुए .
उनकी तीन दशकों की सरकार की इस सेवा को इस मायने में महत्वपूर्ण माना जा सकता है कि इसकी परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों के भाग ले सकने के लिए भारतीयों को लगभग आधी सदी तक संघर्ष करना पड़ा था और इसके बावजूद इस परीक्षा को लंदन के बजाय भारत में कराने की मांग 1922 में उनके निधन से कोई साल भर पहले पूरी हो पाई थी.
लेकिन सत्येंद्र ने अपने व्यक्तित्व के विकास को इस सफलता की चकाचौंध पर ही रोक दिया होता तो वे देशवासियों की स्मृतियों में देशसेवक के रूप में शायद ही रचते-बसते. वैसे भी उन दिनों आईसीएस अफसरों का मुख्य काम जैसे भी बने, करों की अधिकतम उगाही करके ब्रिटिश साम्राज्य का खज़ाना भरना हुआ करता था और इस काम में यश के बजाय अपयश मिलने की संभावनाएं ही ज्यादा थीं.
सत्येंद्र भी इस बात को समझते थे, इसलिए उन्होंने अपनी शख्सियत को अफसरी रौब-दाब से परे रखा और बहुभाषाविद, लेखक/ कवि, गीतकार, संगीतकार व समाज-सुधारक वगैरह के रूप में उसका बहुआयामी विकास किया. देश, के पुनर्जागरण में तो भूमिका निभाई ही निभाई.
यही कारण है कि 1923 में 9 जनवरी को यानी आज के ही दिन उन्होंने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहा तो उनके व्यक्तित्व के इन आयामों से जुड़े हल्कों ने खुद को कहीं ज्यादा रिक्त महसूस किया.
जहां तक आईसीएस अफसरों के समुदाय की बात है, उसके सदस्यों ने आज़ादी के बाद आईएएस बन जाने के बाद भी अपवादस्वरूप ही सत्येंद्र की राह पर चलना गवारा किया अन्यथा उनका पहला भारतीय आईसीएस होना निस्संदेह थोड़ी अतिरिक्त आभा पा जाता.
आईसीएस बनने से पहले
जाहिर है कि सत्येंद्र उनके अपवाद, उनसे इतर और विरल होने के नाते स्मरणीय हैं. 1842 में एक जून को कोलकाता में जन्म के बाद उन्होंने वहां के मशहूर प्रेसिडेंसी कॉलेज से पढ़ाई की थी और लंदन जाकर आईसीएस की परीक्षा पास कर पाते, उससे कई साल पहले 1859 में महज सत्रह साल की उम्र में ज्ञानदानंदिनी देवी से विवाह रचा लिया था. वे ज्ञानदानंदिनी को अपने साथ लंदन ले जाना चाहते थे, लेकिन पिता देवेंद्रनाथ की सख्त मनाही के चलते ऐसा नहीं कर सके थे.
अलबत्ता, बाद में वे स्त्रियों के अधिकारों व स्त्री-पुरुष समानता के बड़े पैरोकार बनकर उभरे और ज्ञानदानंदिनी को न सिर्फ हर मोड़ पर हमकदम बनाया बल्कि आज़ादी के साथ आत्मविश्वास से संपन्न करने के लिए अकेली ही लंदन भेजा. बेटे सुरेंद्रनाथ के साथ, जो तब बच्चे ही थे.
उनका यह कदम कुछ वैसा ही था, जैसे पिता की उस मनाही का प्रतिकार कर रहे हों, जिसके चलते वे पहले ज्ञानदा को अपने साथ भी लंदन नहीं ले जा पाए थे. आगे चलकर उनके ही समर्थन से ज्ञानदा को उन दिनों की कुख्यात पर्दा प्रथा से निजात मिली और वे निर्द्वंद्व रहकर अपनी पसंद का जीवन जी सकीं. मगर इस सबकी तफसील थोड़ी बाद में.
अभी सत्येंद्रनाथ की बाबत यह जान लेना चाहिए कि अपनी आईसीएस की नौकरी के सिलसिले में उनको प्रायः देश भर में आना जाना होता था. इस आवागमन के क्रम में उन्होंने बांग्ला, हिंदी और अंग्रेज़ी के अलावा कई और देसी भाषाएं सीख ली थीं. कह सकते हैं कि इस लिहाज से यह नौकरी उनके बहुत काम आई थी और उन्हें बहुभाषाविद बना दिया था.
स्त्री-पुरुष समानता को समर्पित
सेवानिवृत्ति के बाद वे स्थायी रूप से कल्कत्ता में बसकर साहित्य, संस्कृति व समाज के पूर्णकालिक सेवक बन गए और अपने सृजन से भरपूर प्रसिद्धि पाई. उन्होंने बांग्ला व अंग्रेजी में अपनी खुद की तो कई किताबें लिखीं ही, बाल गंगाधर तिलक और संत तुकाराम की कई किताबों का बांग्ला में अनुवाद भी किया.
उनके खाते में संस्कृत की कुछ कृतियों का अनुवाद भी है, जबकि उनकी कृतियों के नाम हैं : सुशीला ओ बिरसिंह, बम्बई चित्रा, नबरत्नमाला, स्त्री स्वाधीनता, बौद्धधर्म, अमर बाल्यकोथा ओ बॉम्बे प्रभास, भारतवर्ष (अंग्रेजी), राजा राममोहन राय, बिरसिंह,अमर बाल्याकोथा और आत्मकोथा आदि.
प्रसंगवश, 1876 में उन्होंने पश्चिम बंगाल के बेलगछिया में हिंदी मेले के आयोजन में अहम भूमिका निभाई और उसके लिए गीत लिखे थे. उनके एक बांग्ला गीत ‘ मिले सबे भारत संतान, एकतन गागो गान!’ (एक हो जाओ भारत की संतानों, एक सुर में गाओ!) ने तो इतनी प्रतिष्ठा प्राप्त की थी कि उसे देश का पहला राष्ट्रगान तक माना जाने लगा था.
जैसा कि पहले बता आए हैं, अपने पांव पर खड़े होते ही उन्होंने पत्नी ज्ञानदानंदिनी को पर्दे की विवशता से मुक्ति दिलाकर ब्रिटिश अफसरों की पत्नियों की तरह जीवनयापन की आज़ादी दे दी थी. एक बार वे कलकत्ता स्थित ‘गवर्नमेंट हाउस’ में आयोजित एक पार्टी में उनको अपने साथ ले गए तो बंगाल के ‘भद्रलोक’ में इसे लेकर तरह-तरह की चर्चाएं होने लगीं. क्योंकि उस वक्त तक यह अकल्पनीय था कि कोई बंगाली महिला किसी खुले स्थान पर पुरुषों के बीच दिखे.
कई हल्कों में इसे लेकर लोग उनका मज़ाक उड़ाने पर भी उतरे, लेकिन पर्दा प्रथा की समाप्ति की दिशा में उठा उनका यह पहला कदम आगे चलकर मील का पत्थर सिद्ध हुआ. अनंतर, उनकी बहनों और बंगाल की दूसरी महिलाओं को भी इसका लाभ मिला.
हमकदम ज्ञानदानंदिनी
1877 में उनका ज्ञानदानंदिनी देवी को अकेली लंदन भेजने का फैसला भी तत्कालीन समाज में महिलाओं से बरती जा रही गैरबराबरी के खात्मे की दृष्टि से क्रांतिकारी कदम ही था. इससे पहले महिलाएं किसी पुरुष साथी के बगैर विदेश जाने व वहां रहने को कौन कहे, देश में भी लंबी यात्राएं करने की सोच तक नहीं सकती थीं.
यहां यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि ज्ञानदानंदिनी ने भी महिला के तौर पर उन्हें हासिल आज़ादी व अधिकारों के वृहत्तर महिला समुदाय के हित में बढ़-चढ़ कर उपयोग के लिए कई पहलें कीं. साथ ही महिला सशक्तिकरण के आरंभिक (उन्नीसवीं शताब्दी के) चरण की बाधाएं दूर करने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया.
इनमें एक बड़ी बाधा उन दिनों पहनी जाने वाली सीधे पल्लू वाली साड़ी भी थी, क्योंकि उसमें पल्लू दाहिने कंधे पर रखा जाता था, जो दाहिने हाथ के स्वतंत्रतापूर्वक काम करने में बाधक था. ज्ञानदानंदिनी ने यह बाधा दूर करने के लिए पारसी महिलाओं की साड़ी पहनने की शैली में तनिक बदलाव करके पल्लू को बाएं कंधे पर रखने की शुरुआत की. ताकि दाएं हाथ से काम करने में सुविधा रहे.
इतना ही नहीं, उन्होंने साड़ी के साथ ब्लाउज और पेटीकोट को भी जोड़ा, महिलाओं को नई शैली में साड़ी पहनने का प्रशिक्षण दिया और उसके साथ जूते-मोजे पहनने का चलन भी शुरू किया. इसे लेकर कई हल्कों में उनकी कटु आलोचना की गई लेकिन उन्होंने पांव पीछे नहीं हटाये.
हां, सत्येंद्रनाथ का अगस्त, 1828 में बंगाल में पुनर्जागरण के प्रयासों के तहत राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित ‘ब्रह्म समाज’ से भी गहरा जुड़ाव था और वे जीवन भर इस समाज के उद्देश्यों की प्राप्ति के प्रति समर्पित रहे थे.
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं.)